द्वादशतप (मूलाचार ग्रन्थ से)
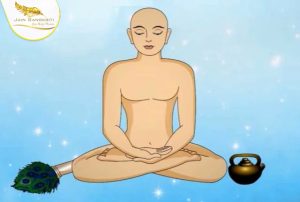
दुविहा य तवाचारो बाहिर अब्भंतरो मुणेयव्वो।
एक्कक्को विय छद्धा जधाकमं तं परूवेमो।।३४५।।
आचार वृत्तिः – द्विप्रकारस्तप आचारस्तपोऽनुष्ठानं। बाह्यो बाह्यजनप्रकटः। अभ्यन्तरोऽभ्यन्तर-जनप्रकटः।एकैकोऽपि च बाह्याभ्यन्तरश्चैकैकः षोढा षड्प्रकारःयथाक्रमं क्रममनुल्लंघ्य प्ररूपयामि कथयिष्यामीति।।३४५।।
बाह्यं षड्भेदं नामोद्देशेन निरूपयन्नाह—
अणसण अवमोदरियं रसपरिचाओ य वुत्तिपरिसंखा।
कायस्स वि परितावो विवित्तसयणासणं छट्ठं।।३४६।।
आचार वृत्तिः –अनशनं चतुर्विधाहारपरित्यागः। अवमौदर्यमतृप्तिभोजनं। रसानां परित्यागो रसपरित्यागःस्वाभिलषितस्निग्धमधुराम्लकटुकादिरसपरिहारः।
वृत्तेः परिसंख्या वृत्तिपरिसंख्या गृहदायकभाजनौदनकालादीनांपरिसंख्यानपूर्वको ग्रहः। कायस्य शरीरस्य परितापःकर्मक्षयाय बुद्धिपूर्वक शोषणं
आतापनाभ्रावकाशवृक्षमूलादिभिः। विविक्तशयनासनं स्त्रीपशुषण्ढकविवर्जितं स्थानसेवनं षष्ठमिति।।३४६।।
अब तप आचार को कहते हैं—
गाथार्थ — बाह्य और अभ्यन्तर के भेद से तप आचार दो प्रकार का जानना चाहिए। उसमें एक-एक भी छः प्रकार का है। उनको मैं क्रम से कहूँगा।।३४५।।
आचारवृत्ति — तप के अनुष्ठान का नाम तप-आचार है। उसके दो भेद हैं—बाह्य और आभ्यन्तर। जो बाह्य जनों में प्रकट है वह बाह्य तप है और जो आभ्यन्तर जनों—अपने धार्मिकजनों में प्रकट है उसे आभ्यन्तर तप कहते हैं। ये बाह्य-आभ्यन्तर दोनों ही तप छः-छः प्रकार के हैं। मैं इन सभी का क्रम से वर्णन करूँगा।
बाह्य तप के छहों भेदों के नाम और उद्देश्य का निरूपण करते हैं—
आगे प्रत्येक का लक्षण आचार्य स्वयं कर रहे हैं। अनशन का स्वरूप और उसके भेद बतलाते हुए कहते हैं—
गाथार्थ — अनशन, अवमौदर्य, रसपरित्याग, वृत्तिपरिसंख्यान, कायक्लेश और विविक्त शयनासन ये छः बाह्य तप हैं।।३४६।।
आचारवृत्ति — चार प्रकार के आहार का त्याग करना अनशन है। अतृप्ति भोजन अर्थात् पेट भर भोजन न करना अवमौदर्य है।
रसों का परित्याग करना—अपने लिए इष्ट स्निग्ध, मधुर, अम्ल, कटुक आदि रसों का परिहार करना रसपरित्याग है।
वृत्ति — आहार की चर्या में परिसंख्या—गणना अर्थात् नियम करना। बर्तनों का, भात आदि भोज्य वस्तु का या काल आदि का गणनापूर्वक नियम करना वृत्तिपरिसंख्यान है अर्थात् आहार को निकलते समय दातारों के घर का या किसी दातार आदि का नियम करना वृत्तिपरिसंख्यान तप है। काय अर्थात् शरीर को परिताप—क्लेश देना, आतापन, अभ्रावकाश और वृक्षमूल आदि के द्वारा कर्मक्षय के लिए बुद्धिपूर्वक शोषण करना कायक्लेश तप है। स्त्री, पशु और नपुंसक से वर्जित स्थान का सेवन करना विविक्तशयनासन तप है। ऐसे इन छः बाह्य तपों का नाम निर्देशपूर्वक संक्षिप्त लक्षण किया है।
आगे प्रत्येक का लक्षण आचार्य स्वयं कर रहे हैं। अनशन का स्वरूप और उसके भेद बतलाते हुए कहते हैं—
अनशनस्य भेदं स्वरूपं च प्रतिपादयन्नाह—
इत्तिरियं जावजीवं दुविहं पुणअणसणं मुणेयव्वं।
इत्तिरियं साकंखं णिरावकंखं हवे बिदियं।।३४७।।
आचार वृत्तिः –अनशनं पुनरित्तिरिययावज्जीवभेदाभ्यां द्विविधं ज्ञातव्यं इत्तिरियं साकांक्षं कालादिभिः सापेक्षं एतावन्तं कालमहमशनादिकं नानुतिष्ठामीति। निराकांक्षं भवेद् द्वितीयं यावज्जीवं आमरणान्तादपि न सेवनम्।।३४७।।
गाथार्थ — काल की मर्यादा सहित और जीवनपर्यन्त के भेद से अनशन तप दो प्रकार जानना चाहिए। काल की मर्यादा सहित साकांक्ष है और दूसरा यावज्जीवन अनशन निराकांक्ष होता है।।३४७।। आचारवृत्ति — इत्तिरिय—इतने काल तक और यावज्जीवं—जीवनपर्यन्त तक के भेद से अनशन तप दो प्रकार का है। उसमें ‘इतने काल पर्यन्त मैं अनशन अर्थात् भोजन आदि का अनुष्ठान नहीं करूंगा’ ऐसा काल आदि सापेक्ष जो अनशन होता है वह इत्तिरिय—साकांक्ष अनशन तप है। जिसमें मरण पर्यन्त तक अनशन का त्याग कर दिया जाता है वह यावज्जीवन निराकांक्ष नाम का दूसरा तप होता है।
साकांक्षानशनस्य स्वरूपं निरूपयन्नाह—
छट्ठट्ठमदसमदुवादसेिंह मासद्धमासखमणाणि।
.कणगेगावलिआदी तवोविहाणाणि णाहारे।।३४८।।
आचार वृत्तिः –अहोरात्रस्य मध्ये द्वे भक्तवेले तत्रैकस्यां भक्तवेलायां भोजनमेकस्याः परित्याग एकभक्तः। चतसृणां भक्तवेलानां परित्यागे चतुर्थः।षण्णां भक्तवेलानां परित्यागे षष्ठो द्विदिनपरित्यागः। अष्टानां परित्यागेऽष्ट मस्त्रय उपवासाः। दशानां त्यागे दशमश्चत्वार उपवासाः। द्वादशानां परित्यागे द्वादशः पंचोपवासाः। मासार्ध-पंचदशोपवासाः पंचदशदिनान्याहारपरित्यागः। मास—मासोपवासािंस्त्रशदहोरात्रमात्रा अशनत्यागः। क्षमणान्युपवासाः। आवलीशब्दः प्रत्येकमभिसम्बध्यते
कनकावल्येकावल्यौ तौ विधी आदिर्येषां तपोविधानानां कनकैकावल्यादीनि।
आदिशब्देन मुरजमध्य-विमानपंक्ति-िंसहनिष्क्रीडितादीनां ग्रहणं।
कनकावल्यादीनां प्रपंचः टीकाराधनायां द्रष्टव्यो विस्तरभयान्नेह प्रतयन्ते।
अनाहारोऽनशनं षष्ठाष्टमदशमद्वादशैर्मासार्धमासादिभिश्च
यानि क्षमणानि कनकैकावल्यादीनि च यानि तपोविधानानि
तानि सर्वाण्यनाहारो यावदुत्कृष्टेन षण्मासास्तत्सर्वं साकांक्षमनशनमिति।।३४८।।
अब साकांक्ष अनशन का स्वरूप कहते हैं—
गाथार्थ — बेला, तेला, चौला, पाँच उपवास, पन्द्रह दिन और महीने भर का उपवास कनकावली, एकावली आदि तपश्चरण के विधान अनशन में कहे गए हैं।।३४८।।
आचारवृत्ति — अहोरात्र के मध्य भोजन की दो बेला होती हैं। उनमें से एक भोजन बेला में भोजन करना और एक भोजन बेला में भोजन का त्याग करना यह एकभक्त है। चार भोजन बेलाओं में चार भोजन का त्याग करना चतुर्थ है अर्थात् धारणा और पारणा के दिन एकाशन करना तथा व्रत के दिन दोनों समय भोजन का त्याग करके उपवास करना—इस तरह चार भोजन का त्याग होने से जो उपवास होता है उसे चतुर्थ कहते हैं। छह भोजन बेलाओं के त्याग में षष्ठ कहा जाता है अर्थात् धारणा-पारणा के दिन एकाशन तथा दो दिन का पूर्ण उपवास इसे ही षष्ठ बेला कहते हैं। आठ भोजन बेलाओं में आठ भोजन का त्याग करने से अष्टम अर्थात् तेला कहा जाता है।
दश भोजन बेलाओं के त्याग करने पर दशम—चार उपवास होते हैं। बारह भुक्तियों के त्याग से द्वादश—पाँच उपवास हो जाते हैं। पन्द्रह दिन तक आहार का त्याग करने से अर्धमास का उपवास होता है। तीस दिन-रात तक भोजन का त्याग करने से एक मास का उपवास होता है तथा कनकावली, एकावली आदि भी तपो विधान है। यहाँ आदि शब्द से मुरजबन्ध, विमानपंक्ति, सिंहनिष्क्रीड़ित आदि व्रतों को ग्रहण करना चाहिए। इन कनकावली आदि व्रतों का विस्तृत कथन आराधना टीका में देखना चाहिए। विस्तार के भय से उनको यहाँ पर हम नहीं कहते हैं। तात्पर्य यह है कि आहार का त्याग करना अनशन है। बेला, तेला, चौला, पाँच उपवास, पन्द्रह दिन, एक महीने आदि के उपवास, कनकावली, एकावली आदि आचरण ये सब उपवास उत्कृष्ट से छः मास पर्यन्त तक होते हैं। ये सब साकांक्ष अनशन हैं।
निराकांक्षस्यानशनस्य स्वरूपं निरूपयन्नाह—
भत्तपइण्णा इंगिणि पाउवगमणाणि जाणाणि मरणाणि |
अण्णेवि एवमादी बोधव्वा णिरवकंखाणि ||३४९||
भक्तप्रत्याख्यानं द्व्याद्यष्टचत्वािंरशन्निर्यापकै
परिचर्यमाणस्यात्मपरोपकार-सव्यपेक्षस्य यावज्जीवमाहारत्यागः।
इङ्गणीमरणं नामात्मोपकारसव्यपेक्षं परोपकारनिरपेक्षं
प्रायोपगमनमरणं नामात्मपरोपकारनिरपेक्षं।
एतानि त्रीणि मरणानि। एवमादीन्यन्यान्यपि प्रत्याख्यानि
निराकांक्षाणि यानि तानि सर्वाण्यनिराकांक्षमनशनं बोद्धव्यं ज्ञातव्यमिति।।३४९।।
अब निराकांक्ष अनशन का स्वरूप निरूपित करते हैं—
गाथार्थ — भक्त प्रतिज्ञा, इंगिनी और प्रायोपगमन जो ये मरण हैं ऐसे और भी जो अनशन हैं वे निराकांक्ष जानना चाहिए।।३४९।।
आचारवृत्ति — दो से लेकर अड़तालीस पर्यन्त निर्यापकों के द्वारा जिनकी परिचर्या की जाती है, जो अपनी और पर के उपकार की अपेक्षा रखते हैं ऐसे मुनि का जो जीवन पर्यन्त आहार का त्याग है वह भक्त प्रत्याख्यान नाम का समाधिमरण है। जो अपने उपकार की अपेक्षा सहित है और पर के उपकार से निरपेक्ष है वह इंगिनीमरण है। जिस मरण में अपने और पर के उपकार की अपेक्षा नहीं है वह प्रायोपगमन मरण है। ये तीन प्रकार के मरण होते हैं अर्थात् छठे गुणस्थान से लेकर ग्यारहवें गुणस्थान तक के जीवों के मरण का नाम पण्डितमरण है उसके ही ये तीनों भेद हैं। इसी प्रकार से और भी जो अन्य उपवास होते हैं वे सब निराकांक्ष अनशन कहलाते हैं।
अवमौदर्यस्वरूपं निरूपयन्नाह—
बत्तीसा किर कवला पुरिसस्स, दु होदि पयदि आहारो।
एगकवलादििंह तत्तो, ऊणियगहणं उमोदरियं।।३५०।।
आचार वृत्तिः –द्वात्रिंशत्कवला: पुरुषस्य प्रकृत्याहारो भवति।ततो द्वात्रिंशत्कवलेभ्य: एककवलेनोनं द्वाभ्यां।त्रिभिः, इत्येवं यावदेककवलः शेषः एकसिक्थो वा।किलशब्द आगमार्थसूचकः आगमे पठितमिति।एककवलादिर्भििनत्यस्याहारस्य ग्रहणं यत् सावमौदर्यवृत्तिः।सहस्रतंदुलमात्रः कवल आगमे पठितः द्वात्रिंशत्कवलाःपुरुषस्य स्वाभाविक आहारस्तेभ्यो यन्न्यूनग्रहणं तदवमोदर्यं तप इति।।३५०।।
अब अवमौदर्य का स्वरूप कहते हैं—
गाथार्थ — पुरुष का निश्चित रूप से स्वभाव से बत्तीस कवल आहार होता है। उस आहार में से एक कवल आदि रूप से कम ग्रहण करना अवमौदर्य तप है।।३५०।।
आचारवृत्ति — पुरुष का प्राकृतिक आहार बत्तीस कवल प्रमाण होता है। उन बत्तीस ग्रासों में से एक ग्रास कम करना, दो ग्रास कम करना, तीन ग्रास कम करना, इस प्रकार से जब तक एक ग्रास न हो जाय तब तक कम करते जाना अथवा एक सिक्थ—भात का कण मात्र रह जाय तब तक कम करते जाना यह अवमौदर्य तप है। गाथा में आया ‘किल’ शब्द आगम अर्थ का सूचक है अर्थात् आगम में ऐसा कहा गया एक ग्रास आदि से प्रारम्भ करके एक ग्रास कम तक जो आहार का ग्रहण करना है वह अवमौदर्य चर्या है। आगम में एक हजार चावल का एक कवल कहा गया है अर्थात् बत्तीस ग्रास पुरुष का स्वाभाविक आहार है उससे जो न्यून है वह अवमौदर्य तप है।
किमर्थमवमोदर्यवृत्तिरनुष्ठीयत इति पृष्टे उत्तरमाह—
धम्मावासयजोगे णाणादीए उवग्गहं कुणदि।
ण य इंदियप्पदोसयरी उम्मोदरितवोवुत्ती।।३५१।।
आचार वृत्तिः –धर्मे क्षमादिलक्षणे दशप्रकारे। आवश्यकक्रियासु समतादिषु षट्सु। योगेषु वृक्षमूलादिषु। ज्ञानादिके स्वाध्याये चारित्रे चोपग्रहमुपकारंकरोतीत्यवमोदर्यतपोवृत्तिः। न चेन्द्रियप्रद्वेषकरी न चावमोदर्यवृत्येन्द्रियाणि प्रद्वेषं गच्छन्ति किन्तु वशे तिष्ठन्तीति। बह्वाशीर्धर्मं नानुतिष्ठति। आवश्यकक्रियाश्च न सम्पूर्णाः पालयति। त्रिकालयोगं च न क्षेमेण समानयति। स्वाध्यायध्यानादिवंâ च न कर्तुं शक्नोति। तस्येन्द्रियाणि च स्वेच्छाचारीणि भवन्तीति। मिताशिनः पुनर्धर्मादयः स्वेच्छया वर्तन्त इति।।३५१।।
किसलिए अवमौदर्य तप का अनुष्ठान किया जाता है ? ऐसा प्रश्न होने पर उत्तर देते हैं—
गाथार्थ — धर्म, आवश्यक क्रिया और योगों में तथा ज्ञानादिक में उपकार करता है क्योंकि अवमौदर्य तप की वृत्ति इन्द्रियों से द्वेष करने वाली नहीं है।।३५१।।
आचारवृत्ति — उत्तम क्षमा आदि लक्षण वाले दश प्रकार के धर्म में, समता, वन्दना आदि छः आवश्यक क्रियाओं में, वृक्षमूल आदि योगों में ज्ञानादिक—स्वाध्याय और चारित्र में यह अवमौदर्य तप उपकार करता है। इस तपश्चरण से इन्द्रियाँ प्रद्वेष को प्राप्त नहीं होती हैं किन्तु वश में रहती हैं। बहुत भोजन करने वाला धर्म का अनुष्ठान नहीं कर सकता है। परिपूर्ण आवश्यक क्रियाओं का पालन नहीं कर पाता है। आतापन, अभ्रावकाश और वृक्षमूल इन तीन काल सम्बन्धी योगों को भी सुख से नहीं धारण कर सकता है तथा स्वाध्याय और ध्यान करने में भी समर्थ नहीं हो पाता है। उस मुनि की इन्द्रियाँ भी स्वेच्छाचारी हो जाती हैं किन्तु मितभोजी साधु में धर्म, आवश्यक आदि क्रियाएँ स्वेच्छा से रहती हैं
भावार्थ — भूख से कम खाने वाले साधु के प्रमाद नहीं होने से ध्यान, स्वाध्याय आदि निर्विघ्न होते हैं किन्तु अधिक भोजन करने वाले के प्रमाद से सभी कार्यों में बाधा पहुँचती है इसलिए यह तप गुणकारी है।
रसपरित्यागस्वरूपं प्रतिपादयन्नाह—
खीरदहिसप्पितेल गुडलवणाणं च जं परिच्चयणं।
तित्तकटुकसायंविलमधुररसाणं च जं चयणं।।३५२।।
आचार वृत्तिः –अथ को रसपरित्याग इति पृष्टेऽत आह—क्षीरदधिर्सिपस्तैलगुडलवणानां घृतपूरलड्डुकादीनां च यत् परिच्चयणं—परित्यजनं एकैकशः सर्वेषां वा तिक्तकटुककषा-याम्लमधुररसानां च यत्त्यजनं स रसपरित्यागः। एतेषां प्रासुकानामपि तपोबुद्ध्या त्यजनम्।।३५२।।
याः पुनर्महाविकृतयस्ताः कथमिति प्रश्नेऽत आह—
चत्तारि महावियडी य होंति णवणीदमज्जमंसमधू।
कंखापसंगदप्पासंजमकारीओ एदाओ।।३५३।।
याः पुनश्चतस्रो महाविकृतयो महापापहेतवो भवन्तीति नवनीतमद्यमांसमधूनि,
कांक्षाप्रसंगदर्पासंयमकारिण्य एताः। नवनीतं कांक्षां—महाविषयाभिलाषं करोति।
मद्यं—सुराप्रसंगमगम्यगमनं करोति।
मांसं-पिशितं दर्पं करोति।
मधु असंयमं हिंसां करोति।।३५३।।
अब रसपरित्याग का स्वरूप प्रतिपादित करते हैं— गाथार्थ — दूध, दही, घी, तेल, गुड़ और लवण इन रसों का जो परित्याग करना है और तिक्त, कटु, कषाय, अम्ल तथा मधुर इन पाँच प्रकार के रसों का त्याग करना है वह रसपरित्याग है।।३५२।। आचारवृत्ति — रसपरित्याग क्या है ऐसा प्रश्न होने पर आचार्य कहते हैं—दूध, दही, घी, तेल, गुड़ और नमक तथा घृतपूर्ण पुआ, लड्डू आदि का जो त्याग करना है। इनमें एक-एक का या सभी का छोड़ना; तथा तिक्त, कटुक, कषायले, खट्टे और मीठे इन रसों का त्याग करना रसपरित्याग तप है। इस तप में इन प्रासुक वस्तुओं का भी तपश्चरण की बुद्धि से त्याग किया जाता है। जो महाविकृतियाँ हैं वे कौन सी हैं ? ऐसा प्रश्न होने पर कहते हैं—
गाथार्थ — मक्खन, मद्य, मांस और मधु ये चार महाविकृतियाँ होती हैं। ये अभिलाषा, प्रसंग—व्यभिचार, दर्प और असंयम को करने वाली हैं।।३५३।।
आचारवृत्ति — मक्खन, मद्य, मांस और मधु ये चारों ही महाविकृति पाप की हेतु हैं। नवनीत विषयों की महान् अभिलाषा को उत्पन्न करता है। मद्य, प्रसंग, अगम्य अर्थात् वेश्या या व्यभिचारिणी स्त्री का सहवास कराता है। मांस अभिमान को पैदा करता है और मधु हिंसा में प्रवृत्त कराता है।
एताः किंकर्तव्या इति पृष्टेऽत आह—
आणाभिकंखिणावज्जभीरुणा तवसमाधिकामेण।
ताओ जावज्जीवं णिव्वुड्ढाओ पुरा चेव।।३५४।।
आचार वृत्तिः –सर्वज्ञाभिकाक्षिणा—सर्वज्ञमतानुपालकेन। अवद्यभीरुणा—पापभीरुणा, तपःकामेन—तपोनुष्ठानपरेण, समाधिकामे—न च ता नवनीतमद्यमांसमधूनि विकृतयो यावज्जीवं—सर्वकालं निव्र्यूढाः—निसृष्टाः त्यक्ताः पुरा चैव पूर्वस्मिन्नेव काले संयमग्रहणान्पूर्वमेव। आज्ञाभिकांक्षिणा नवनीतं सर्वथा त्याज्यं दुष्टकांक्षाकारित्वात्। अवद्यभीरुणा मांसं सर्वथा त्याज्यं दर्पकारित्वात्। ततः तपःकामेन मद्यं सर्वथा त्याज्यं प्रसंगकारित्वात्। समाधिकामेन मधु सर्वथा त्याज्यं, असंयमकारित्वात्। व्यस्तं समस्तं वा योज्यमिति।।३५४।।
इन्हें क्या करना चाहिए ? सो ही बताते हैं—
गाथार्थ — आज्ञापालन के इच्छुक, पापभीरू, तप और समाधि की इच्छा करने वाले ने पहले ही इनका जीवन भर के लिए त्याग कर दिया है।।३५४।।
आचारवृत्ति — सर्वज्ञदेव की आज्ञा पालन करने वाले, पापभीरू, तप के अनुष्ठान में तत्पर और समाधि की इच्छा करने वाले भव्य जीव ने संयम ग्रहण करने के पूर्व में ही इन मक्खन, मद्य, मांस और मधु नामक चारों विकृतियों का जीवन भर के लिए त्याग कर दिया है। आज्ञापालन करने के इच्छुक को नवनीत का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए क्योंकि वह दुष्ट अभिलाषा को उत्पन्न करने वाला है। पापभीरू को मांस का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए क्योंकि वह दर्प—उत्तेजना का करने वाला है। तपश्चरण की इच्छा करने वाले को चाहिए कि वह मद्य को सर्वथा के लिए छोड़ दे क्योंकि वह अगम्या—वेश्या आदि का सेवन कराने वाला है तथा समाधि की इच्छा करने वाले को मधु का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए क्योंकि वह असंयम को करने वाला है। इनको पृथक-पृथक या समूहरूप से भी लगा लेना चाहिए।
भावार्थ — एक-एक गुण के इच्छुक को एक-एक के त्यागने का उपदेश दिया है। वैसे ही एक-एक गुण के इच्छुक को चारों का भी त्याग कर देना चाहिए अथवा चारों गुणों के इच्छुक को चारों वस्तुओं का सर्वथा ही त्याग कर देना चाहिए। वृत्तिपरिसंख्यान तप का स्वरूप प्रतिपादित करते हुए आचार्य कहते हैं—
वृत्तिपरिसंख्यानस्वरूपं प्रतिपादयन्नाह—
गोयरपमाणदायगभायण णाणाविहाण जं गहणं।
तह एसणस्स गहणं विविहस्स य वुत्तिपरिसंखा।।३५५।।
आचार वृत्तिः –गोचरस्य प्रमाणं गोचरप्रमाणं गृहप्रमाणं, एतेषु गृहेषु प्रविशामि नान्येषु बहुष्विति। दायका दातारो भाजनानि परिवेष्यपात्राणि तेषां यन्नानाविधानं नानाकरणं तस्य ग्रहणं स्वीकरणं—दातृविशेषग्रहणं पात्रविशेषग्रहणं च। यदि वृद्धो मां विधरेत् तदानीं तिष्ठामि नान्यथा। अथवा वालो युवा स्त्री उषानत्करहितो वत्र्मनि स्थितोऽन्यथा वा विधरेत् तदानीं तिष्ठामिति। कांस्यभाजनेन रूप्यभाजनेन सुवर्णभाजनेन मृन्मयभाजनेन वा ददाति तदा गृहीष्यामीति यदेवमाद्यं।तथाशनस्य विविधस्य नानाप्रकारस्य यद्रग्रहणमवग्रहोपादानं,अद्य मकुष्ठं भोक्ष्ये नान्यत्। अथवाद्य मंडकान् सक्तून् ओदनं वा ग्रहीष्यामीति यदेवमाद्यं ग्रहणं तत्सर्वं वृत्तिपरिसंख्यानमिति।।३५५।।
गाथार्थ — गृहों के प्रमाण, दाता का, बर्तनों का नियम ऐसे अनेक प्रकार का जो नियम ग्रहण करना है तथा नाना प्रकार के भोजन का नियम ग्रहण करना वृत्तिपरिसंख्यान व्रत है।।३५५।।
आचारवृत्ति — गृहों के प्रमाण को गोचर प्रमाण कहते हैं। जैसे ‘आज मैं इन गृहों में आहार हेतु जाऊँगा और अधिक गृहों में नहीं जाऊँगा’ ऐसा नियम करना। दायक अर्थात् दातार और भाजन अर्थात् भोजन रखने के या भोजन परोसने के बर्तन—इनकी जो नाना प्रकार से विधि लेना है वह दायक-भाजन विधि अर्थात् दाता विशेष और पात्र विशेष की विधि ग्रहण करना है। जैसे ‘यदि वृद्ध मनुष्य मुझे पड़गाहेगा तो मैं ठहरूँगा अन्यथा नहीं अथवा बालक, युवक, महिला या जूते अथवा खड़ाऊँ आदि से रहित कोई पुरुष मार्ग में खड़ा हुआ मुझे पड़गाहे तो मैं ठहरूँगा अथवा ये अन्य अमुक विधि से मुझे पड़गाहें तो मैं ठहरूँगा’ इत्यादि नियम लेकर चर्या के लिए निकलना। ऐसे ही बर्तन सम्बन्धी नियम लेना, जैसे ‘मुझे आज यदि कोई कांसे के बर्तन से, सोने के बर्तन से या मिट्टी के बर्तन से आहार देगा तो मैं ले लूँगा, या इसी प्रकार से अन्य और भी नियम लेना तथा नाना प्रकार के भोजन सम्बन्धी जो नियम लेना है वह सब वृत्तिपरिसंख्यान है। जैसे, ‘आज मैं मोठ ही खाऊँगा अन्य कुछ नहीं’, इत्यादि रूप से जो भी नियम लिए जाते हैं वे सब वृत्तिपरिसंख्यान तप कहलाते हैं।
भावार्थ — इन्द्रिय और मन के निग्रह के लिए नाना प्रकार के तपश्चरणों का अनुष्ठान किया जाता है और इस वृत्तिपरिसंख्यान के नियम से भी इच्छाओं का निरोध होकर भूख-प्यास को सहन करने का अभ्यास होता है।
कायक्लेशस्वरूपं विवृण्वन्नाह—
ठाणसयणासणेिंह य विविहेिंहय उग्गयेिंह बहुएहिं।
अणुवीचीपरिताओ कायकिलेसो हवदि एसो।।३५६।।
आचार वृत्तिः –स्थानं—कायोत्सर्गं शयनं—एकपाश्र्वमृतकदण्डादिशयनं।
आसनं—उत्कुटिका -पर्यंक—वीरासन-मकरमुखाद्यासनं।
स्थानशयनासर्नैिवविधैश्चावग्रहैर्धर्मोपकार-हेतुभिरभिप्रायै-र्बहुभिरनुवीचीपरितापः
सूत्रानुसारेण कायपरितापो वृक्षमूलाभ्रावकाशा-तापनादिरेष कायक्लेशो भवति।।३५६।।
विविक्तशयनासनस्वरूपमाह—तेरिक्खिय माणुस्सिय सविगारियदेवि
गेहि संसत्ते। वज्र्जेति अप्पमत्ता णिलए सयणासणट्ठाणे।।३५७।।
तिर्यंचो—गोमहिष्यादयः। मानुष्यः—स्त्रयो वेश्याः स्वेच्छाचारिण्यादयः।
सविकारिण्यो—देव्यो भवनवानव्यन्तरादियोषितः। गेहिनो गृहस्याः।
एतैः संसक्तान्—सहितान्, निलयानावसान् वर्जयन्ति—परिहरन्त्यप्रमत्ता
यत्नपराः सन्तः शयनासनस्थानेषु कर्तव्येषु एवमनुतिष्ठतो
विविक्तशयनासनं नाम तप इति।।३५७।।
कायक्लेश तप का स्वरूप बतलाते हैं—
गाथार्थ — खड़े होना—कायोत्सर्ग करना, सोना, बैठना और अनेक विधिनियम ग्रहण करना, इनके द्वारा आगमानुकूल कष्ट सहन करना, यह कायक्लेश नाम का तप है।।३५६।। आचारवृत्ति — स्थान—कायोत्सर्ग करना। शयन—एक पसवाड़े से या मृतकासन से या दण्डे के समान लम्बे पड़कर सोना। आसन—उत्कुटिकासन, पर्यंकासन, वीरासन, मकरमुखासन आदि तरह-तरह के आसन लगाकर बैठना। इन कायोत्सर्ग, शयन और आसनों द्वारा तथा अनेक प्रकार के धर्मोपकार हेतु नियमों के द्वारा सूत्र के अनुसार काय को ताप देना अर्थात् शरीर को कष्ट देना; वृक्षमूल, अभ्रावकाश और आतापन आदि नाना प्रकार के योग धारण करना यह सब कायक्लेश तप है।
भावार्थ — इस तपश्चरण द्वारा शरीर में कष्ट-सहिष्णुता आ जाने से, घोर उपसर्ग या परीषहों के आ जाने पर भी साधु अपने ध्यान से चलायमान नहीं होते हैं इसलिए यह तप भी बहुत ही आवश्यक है।
बाह्य तप उपसंहरन्नाह—
सो णाम बाहिरतवो जेण मणो दुक्कडं ण उट्ठेदि।
जेण य सद्धा जायदि जेण य जोगा ण हीयंते।।३५८।।
आचार वृत्तिः –तन्नाम बाह्यं तपो येन मनोदुष्कृतं-चित्तसंक्लेशो
नोत्तिष्ठति नोत्पद्यते। येन च श्रद्धा शोभनानुरागो जायत
उत्पद्यते येन च योगा मूलगुणा न हीयन्ते।।३५८।।
एसो दु बाहिरतवो बाहिरजणपायडो परम घोरो।
अब्भंतरजणणादं बोच्छं अब्भंतरं वि तवं।।३५९।।
आचार वृत्तिः –तद्वाह्यं तपः षड्विधं बाह्यजनानां मिथ्यादृष्टिजनानामपि
प्रकटं प्रख्यातं परमघोरं सुष्ठु दुष्करं प्रतिपादितं।
अभ्यन्तरजनज्ञातं आगमप्रविष्टजनैज्र्ञातं
वक्ष्ये कथयिष्याम्यभ्यन्त-रमपि षड्विधं तपः।।३५९।।
श्री पूज्यवाद स्वामी ने भी कहा है—
अदुःखभावितं ज्ञानं क्षीयतेदुःखसन्निधौ।
तस्माद् यथाबलं दुःखैरात्मानं भावयेद् मुनिः।।१०२।।
(समाधिशतक)सुखी जीवन में किया गया तत्त्वज्ञान का अभ्यास दुःख के आ जाने पर क्षीण हो जाता है इसलिए मुनि अपनी शक्ति के अनुसार दुःखों के द्वारा अपनी आत्मा की भावना करे अर्थात् कायक्लेश आदि के द्वारा दुःखों को बुलाकर अपनी आत्मा का चिन्तवन करते हुए अभ्यास दृढ़ करे। विविक्तशयनासन तप का स्वरूप कहते हैं—
गाथार्थ — अप्रमादी मुनि सोने, बैठने और ठहरने में तिर्यंचिनी, मनुष्य-स्त्री, विकारसहित देवियाँ और गृहस्थों से सहित मकानों को छोड़ देते हैं।।३५७।।
आचारवृत्ति — अप्रमत्त अर्थात् यत्न में तत्पर होते हुए सावधान मुनि सोना, बैठना और ठहरना इन प्रसंगों में अर्थात् अपने ठहरने के प्रसंग में—जहाँ, गाय, भैंस आदि तिर्यंच हैं; वेश्या, स्वेच्छाचारिणी आदि महिलाएँ हैं; भवनवासिनी, व्यंतरवासिनी आदि विकारी वेषभूषा वाली देवियाँ हैं अथवा गृहस्थजन हैं। ऐसे इन लोगों से सहित गृहों को, वसतिकाओं को छोड़ देते हैं। इस तरह इन तिर्यंच आदि से रहित स्थानों में रहने वाले मुनि के यह विविक्त शयनासन नाम का तप होता है। अब बाह्य तपों का उपसंहार करते हुए कहते हैं—
गाथार्थ — बाह्य तप वही है जिससे मन अशुभ को प्राप्त नहीं होता है, जिससे श्रद्धा उत्पन्न होती है तथा जिससे योगहीन नहीं होते हैं।।३५८।।
आचारवृत्ति — बाह्य तप वही है कि जिससे मन में संक्लेश नहीं उत्पन्न होता है, जिससे श्रद्धा—शुभ अनुराग उत्पन्न होता है और जिससे योग अर्थात् मूलगुण हानि को प्राप्त नहीं होते हैं अर्थात् बाह्य तप का अनुष्ठान वही अच्छा माना जाता है कि जिसके करने से मन में संक्लेश न उत्पन्न हो जावे या शुभ परिणामों का विघात न हो जावे अथवा मूलगुणों की हानि न हो जावे।
गाथार्थ — यह बाह्य तप बाह्य जैन मत से र्बिहभूत जनों में प्रगट है, परम घोर है, सो कहा गया है। अब मैं अभ्यन्तर—जैनदृष्टि लोगों में प्रसिद्ध ऐसे अभ्यन्तर तप को कहूँगा।।३५९।।
आचारवृत्ति — यह छः प्रकार का बाह्य तप का, जो मिथ्या दृष्टिजनों में भी प्रख्यात है और अत्यन्त दुष्कर है, मैंने प्रतिपादन किया है। अब आगम में प्रवेश करने वाले ऐसे सम्यग्दृष्टिजनों के द्वारा जाने गए छह भेद वाले अभ्यन्तर तप को भी मैं कहूँगा।
के ते षट्प्रकारा इत्याशंकायामाह—
पायच्छित्तं विणयंवेज्जावच्चं तहेव सज्झायं।
झाणं च विउस्सग्गो अब्भंतरओ तवो एसो।।३६०।।
प्रायश्चित्तं—पूर्वापराधशोधनं। विनयमनुतद्ध् वृत्तिः।
वैयावृत्यं स्वशक्त्योपकारः। तथैव स्वाध्यायः सिद्धान्ताद्यध्ययनं।
ध्यानं चैकाग्रिंचतानिरोधः व्युत्सर्गः। अभ्यन्तरतप एतदिति।।३६०।।
प्रायश्चित्तस्वरूपं निरूपयन्नाह—पायच्छित्तं त्ति तवो जेण
विसुज्झदि हु पुव्वकयपावं। पायच्छित्तं पत्तोति तेण वुत्तं दसविहं तु।।३६१।।
अभ्यन्तर तप के वे छह प्रकार कौन से हैं ? ऐसी आशंका होने पर कहते हैं—
गाथार्थ — प्रायश्चित्त, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, ध्यान और व्युत्सर्ग, ये अभ्यन्तर तप हैं।।३६०।। आचारवृत्ति — पूर्व के किए हुए अपराधों का शोधन करना प्रायश्चित्त है। उद्धतपनरहित वृत्ति का होना अर्थात् नम्र वृत्ति का होना विनय है। अपनी शक्ति के अनुसार उपकार करना वैयावृत्त्य है। सिद्धान्त आदि ग्रन्थों का अध्ययन करना स्वाध्याय है। एक विषय पर चिन्ता का निरोध करना ध्यान है और उपधि का त्याग करना व्युत्सर्ग है। ये छह अभ्यन्तर तप हैं।
प्रायश्चित्तमपराधं प्राप्तः सन् येन तपसा पूर्वकृतात्पापात्
विशुद्धयते हु—स्फुटं पूर्वं व्रतैः सम्पूर्णो भवति
तत्तपस्तेन कारणेन दशप्रकारं प्रायश्चित्तमिति।।३६१।।
के ते दशप्रकारा इत्याशंकायामाह—आलोयणपडिकमणं उभयविवेगो
तहा विउस्सग्गो। तव छेदो मूलं विय परिहारो चेव सद्दहणा।।३६२।।
आलोचना—आचार्याय देवाय वा चारित्राचारपूर्वकमुत्पन्नापराघनिवेदनं।
प्रतिक्रमणं—रात्रि भोजनत्यागव्रतसहितपंचमहाव्रतोच्चारणं
संभावनं दिवसप्रतिक्रमणं पाक्षिकं वा। उभयं—आलोचन प्रतिक्रमणे।
विवेको—द्वप्रकारो गणविवेकः स्थानविवेको वा।
तथा व्युत्सर्गः—कायोत्सर्गः। तपोऽनशनादिकं।
छेदो—दीक्षायाः पक्षमासादिभिर्हानिः। मूलं—पुनरद्य प्रभृति व्रतारोपणं।
अपि च परिहारो द्विप्रकारो गणप्रतिबद्धोऽप्रतिबद्धो वा।
यत्र प्रश्रवणादिकं कुर्वन्ति मुनयस्तत्र तिष्ठन्ति पिछिकामग्रतः
कृत्वा यतीनां वन्दनां करोति तस्य यतयो न कुर्वन्ति,
एवं या गणे क्रिया गणप्रतिबद्धः परिहारः। यत्र देशे धर्मो न
ज्ञायते तत्र गत्वा मौनेन तपश्चरणानुष्ठानकरणमगणप्रतिबद्धः परिहारः।
तथा श्रद्धानं तत्त्वरुचौ परिणामः क्रोधादिपरित्यागो वा।
एतद्दशप्रकारं प्रायश्चित्तं दोषानुरूपं दातव्यमिति।
कश्चिद्दोषः आलोचनमात्रेण निराक्रियते।
कश्चित्प्रतिक्रमणेन कश्चिदालोचनप्रतिक्रमणाभ्यां कश्चिद्विवेकेन
कश्चित्कायोत्सर्गेण कश्चित्तपसा कश्चिच्छेदेन कश्चिन्मूलेन
कश्चित्परिहारेण कश्चिच्छ्रद्धानेनेति।।३६२।।
अब प्रायश्चित्त का स्वरूप निरूपित करते हैं— गाथार्थ — अपराध को प्राप्त हुआ जीव जिसके द्वारा पूर्वकृत पाप से विशुद्ध हो जाता है वह प्रायश्चित्त तप है। इस कारण से वह प्रायश्चित्त दश प्रकार का कहा गया है।।३६१।।
आचारवृत्ति — अपराध को प्राप्त हुआ जीव जिस तप के द्वारा अपने पूर्वसंचित पापों से विशुद्ध हो जाता है वह प्रायश्चित्त है। जिससे स्पष्टतया पूर्व के व्रतों से परिपूर्ण हो जाता है वह तप भी प्रायश्चित्त कहलाता है। वह प्रायश्चित्त दश प्रकार का है। वे दश प्रकार कौन से हैं ऐसी आशंका होने पर कहते हैं—
गाथार्थ — आलोचना, प्रतिक्रमण, तदुभय, विवेक, व्युत्सर्ग, तप, छेद, मूल, परिहार और श्रद्धान ये दश भेद हैं।।३६२।।
आचारवृत्ति — आचार्य अथवा जिनदेव के समक्ष अपने में उत्पन्न हुए दोषों का चारित्राचारपूर्वक निवेदन करना आलोचना है। रात्रिभोजनत्याग व्रत सहित पाँच महाव्रतों का उच्चारण करना, सम्यव् प्रकार से उनको भाना अथवा दिवस और पाक्षिक सम्बन्धी
प्रायश्चित्तस्य नामानि प्राह—पोराणकम्मखवणं खिवणं णिज्जरण
सोधणं धुवणं। पुंच्छणमुछिवण छिदणं त्ति पायच्छित्तस्स णामाइं।।३६३।।
पुराणस्य कर्मणः क्षपणं विनाशः, क्षेपणं, निर्जरणं, शोधनं,
धावनं, पुच्छणं, निराकरणं, उत्क्षेपणं, छेदनं द्वैधीकरणमिति
प्रायश्चित्तस्यैतान्यष्टौ नामानि ज्ञातव्यानि भवन्तीति।।३६३।।
प्रतिक्रमण करना प्रतिक्रमण है। आलोचना और प्रतिक्रमण दोनों को करना तदुभय है।
विवेक के दो भेद हैं—गण विवेक और स्थानविवेक। कायोत्सर्ग को व्युत्सर्ग कहते हैं। अनशन आदि तप हैं। पक्ष-मास आदि से दीक्षा की हानि कर देना छेद है। आज से लेकर पुनः व्रतों का आरोपण करना अर्थात् फिर से दीक्षा देना मूल है।
परिहार प्रायश्चित्त के भी दो भेद हैं—गणप्रसिद्ध और गण अप्रतिबद्ध। जहाँ मुनिगण मूत्रादि विसर्जन करते हैं, इस प्रायश्चित्त वाला पिच्छिका को आगे करके वहाँ पर रहता है, वह यतियों की वंदना करता है किन्तु अन्य मुनि उसको वन्दना नहीं करते हैं। इस प्रकार से जो गण में क्रिया होती है वह गणप्रतिबद्ध परिहार प्रायश्चित्त है। जिस देश में धर्म नहीं जाना जाता है वहाँ जाकर मौन से तपश्चरण का अनुष्ठान करते हैं उनके अगणप्रतिबद्ध परिहार प्रायश्चित्त होता है। तत्त्वरुचि में जो परिणाम होता है अथवा क्रोधादि का त्याग रूप जो परिणाम है वह श्रद्धान प्रायश्चित्त है। यह दश प्रकार का प्रायश्चित्त दोषों के अनुरूप देना चाहिए। कुछ दोष आलोचनामात्र से निराकृत हो जाते हैं, कुछ दोष प्रतिक्रमण से दूर किए जाते हैं तो कुछेक दोष आलोचना और प्रतिक्रमण इन दोनों के द्वारा नष्ट किए जाते हैं, कई दोष विवेक प्रायश्चित्त से, कई कायोत्सर्ग से, कई दोष तप से, कई दोष छेद से, कई मूल प्रायश्चित्त से, कई परिहार से एवं कई दोष श्रद्धान नामक प्रायश्चित्त से दूर किए जाते हैं।
विशेष—आजकल ‘परिहार’ नाम के प्रायश्चित्त को देने की परम्परा नहीं है। प्रायश्चित के पर्यायवाची नामों को कहते हैं—
गाथार्थ—पुराने कर्मों का क्षपण, क्षेपण, निर्जरण, शोधन, धावन, पुंछन, उत्क्षेपण और छेदन ये सब प्रायश्चित्त के नाम हैं।।३६३।।
आचारवृत्ति—पुराने कर्मों का क्षपण—क्षय करना अर्थात् विनाश करना, क्षेपण—दूर करना, निर्जरण—निर्जरा करना, शोधन—शोधन करना, धावन—धोना, पुंछन—
विनयस्य स्वरूपमाह—दंसणणाणेविणओ चरित्ततवओवचारिओ विणओ।
पंचविहो खलु विणओ पंचमगइणायगो भणिओ।।३६४।।
दर्शने विनयो ज्ञाने विनयश्चारित्रे विनयस्तपसि विनयः
औपचारिको विनयः पंचविधः खलु विनयः पंचमीगतिनायकः
प्रधानः भणितः प्रतिपादित इति।।३६४।।
दर्शनविनयं प्रतिपादयन्नाह—उवगूहणादिआ पुव्वुत्ता तह
भत्तिआदिआ य गुणा। संकादिवज्जणं पि य दंसणविणओ समासेण।।३६५।।
उपगूहनस्थिरीकरणवात्सल्यप्रभावनाः पूर्वोक्ताः।
तथा भक्त्यादयो गुणाः पंचपरमेष्ठिभक्त्यानुरागस्तेषामेव
पूजा तेषामेव गुणानुवर्णनं, नाशनमवर्णवादस्या-सादनापरिहारो भक्त्यादयो गुणाः।
शंकाकांक्षाविचिकित्सान्यदृष्टिप्रशंसानां वर्जनं परिहारो दर्शनविनयः समासेनेति।।३६५।।
पोछना अर्थात् निराकरण करना, उत्क्षेपण—पेंकना, छेदन—दो टुकड़े करना इस प्रकार ये प्रायश्चित्त के आठ नाम जानने चाहिए। अब विनय का स्वरूप कहते हैं—
गाथार्थ — दर्शन विनय, ज्ञान विनय, चारित्र विनय, तपोविनय और औपचारिक विनय यह पाँच प्रकार का विनय पंचमगति का नायक कहा गया है।।३६४।।
आचारवृत्ति — दर्शन में विनय, ज्ञान में विनय, चारित्र में विनय, तप में विनय और औपचारिक विनय यह पाँच प्रकार का विनय निश्चित रूप से पाँचवीं गति अर्थात् मोक्षगति में ले जाने वाला प्रधान कहा गया है, ऐसा समझना अर्थात् विनय मोक्ष को प्राप्त कराने वाला है। दर्शन विनय का प्रतिपादन करते हैं—
गाथार्थ — पूर्व में कहे गए उपगूहन आदि तथा भक्ति आदि गुणों को धारण करना और शंकादि दोष का वर्जन करना यह संक्षेप से दर्शन विनय है।।३६५।।
आचारवृत्ति — उपगूहन, स्थिरीकरण, वात्सल्य और प्रभावना ये पूर्व में कहे गए हैं तथा पंच परमेष्ठियों में अनुराग करना, उन्हीं की पूजा करना, उन्हीं के गुणों का वर्णन करना, उनके प्रति लगाए गए अवर्णवाद अर्थात् असत्य आरोप का विनाश करना और उनकी आसादना अर्थात् अवहेलना का परिहार करना—ये भक्ति आदि गुण कहलाते हैं। शंका, कांक्षा, विचिकित्सा और अन्य दृष्टि—मथ्यादृष्टियों की प्रशंसा, इनका त्याग करना यह संक्षेप से दर्शन विनय है।
जे अत्थपज्जया खलु उवदिट्ठा जिणवरेिंह सुदणाणे।
ते तह रोचेदि णरो दंसणविणयो हवदि एसो।।३६६।।
येऽर्थपर्याया जीवाजीवादयः सूक्ष्मस्थूलभेदेनोपदिष्टाः
स्पुटं जिनवरैः श्रुतज्ञाने द्वादशांगेषु चतुर्दशपूर्वेषु, तान्
पदार्थांस्तथैव तेन प्रकारेण याथात्म्येन रोचयति नरो
भव्यजीवो येन परिणामेन स एष दर्शनविनयो ज्ञातव्य इति।।३६६।।
ज्ञानविनयं प्रतिपादयन्नाह—काले विणए उवहाणे
बहुमाणे तहेव णिण्हवणे। वंजणअत्थतदुभयं विणओ णाणम्हि अट्ठविहो।।३६७।।
द्वादशांगचतुर्दशपूर्वाणां कालशुद्ध्या पठनं व्याख्यानं परिवर्तनं वा।
तथा हस्तपादौ प्रक्षाल्य पर्यकेऽवस्थितस्वाध्ययनं। अवग्रहविशेषेण पठनं।
बहुमानं यत्पठति यस्माच्छ्रणोति तयोः पूजागुणस्तवनं।
तथैवानिह्नवो यत्पठति यस्मात्पठति तयोः कीर्तनं।
भावार्थ — शंकादि चार दोषों का त्याग, उपगूहन आदि चार अंग जो विधिरूप हैं उनका पालन करना तथा पंचपरमेष्ठी की भक्ति आदि करना यही सब दर्शन की विशुद्धि को करने वाला दर्शन विनय है।
गाथार्थ — जिनेन्द्रदेव ने आगम में निश्चित रूप से जिन द्रव्य और पर्यायों का उपदेश किया है, उनका जो मनुष्य वैसा ही श्रद्धान करता है वह दर्शन विनय वाला होता है।।३६६।।
आचारवृत्ति — सूक्ष्म और बादर के भेद से जिन जीव-अजीव आदि पदार्थों का जिनेन्द्रदेव ने द्वादशांग और चतुर्दशपूर्व रूप श्रुतज्ञान में स्पष्ट रूप से उपदेश दिया है, जो भव्य जीव उन पदार्थों का उसी प्रकार से जैसे का तैसा विश्वास करता है तथा जिस परिणाम से श्रद्धान करता है वह परिणाम ही दर्शनविनय है। ज्ञानविनय का प्रतिपादन करते हैं—
गाथार्थ — काल, उपधान, बहुमान, अनिह्नव, व्यंजन, अर्थ और तदुभय—इनमें विनय करना यह ज्ञान सम्बन्धी विनय आठ प्रकार का है।।३६७।।
आचारवृत्ति — द्वादशांग और चतुर्दश पूर्वों को कालशुद्धि से पढ़ना, व्याख्यान करना अथवा परिवर्तन—पेरना कालविनय है। उन्हीं ग्रन्थों का (या अन्य ग्रन्थों का) हाथ पैर धोकर पर्यंकासन से बैठकर अध्ययन करना विनयशुद्धि नाम का ज्ञानविनय है। नियम विशेष लेकर पढ़ना उपधान है। जो ग्रन्थ नियम से पढ़ते हैं और जिनके मुख से सुनते हैं उस पुस्तक और उन गुरु
व्यञ्जनशुद्धं, अर्थशुद्धं व्यञ्जनार्थोभयशुद्धं च यत्पठनं।
अनेन न्यायेनाष्टप्रकारो ज्ञाने विनय इति।।३६७।।
तथा—णाणं सिक्खदि णाणं गुणेदि णाणं परस्स उवदिसदि।
णाणेण कुणदि णायं णाणविणीदो हवदि एसो।।३६८।।
ज्ञान शिक्षते विद्योपादानं करोति। ज्ञानं गुणयति
परिवर्तनं करोति। ज्ञानं परस्मै उपदिशति प्रतिपादयति।
ज्ञानेन करोति न्यायमनुष्ठानं। य एवं करोति ज्ञानविनीतो भवत्येष इति।
अथ दर्शनाचारदर्शनविनययोः को भेदस्तथा ज्ञानाचारज्ञानविनययोः
कश्चन भेद इत्याशंकायामाह—शंकादिपरिणामपरिहारे यत्नः
उपगूहनादिपरिणामानुष्ठाने यत्नः कालादिविनयः, तथा
द्रव्यक्षेत्रभावादिविषयश्च यत्नः। ज्ञानाचारः पुनः कालशुद्ध्यादिषु
सत्सु श्रुतं पठनयत्नं। ज्ञानविनयः श्रुतोपकरणेषु च यत्नः श्रुतविनयः।
तथापनयति तपसा तमोऽज्ञानं उपनयति च मोक्षमार्गे
आत्मानं तपोविनयः नियमितमतिः सोऽपि तपोविनय इति ज्ञातव्य इति।।३६८।।
इन दोनों की पूजा करना और उनके गुणों का स्तवन करना बहुमान है। उसी प्रकार से जिस ग्रन्थ को पढ़ते हैं और जिनसे पढ़ते हैं उनका नाम कीर्तित करना अर्थात् उस ग्रन्थ या उन गुरु के नाम को नहीं छिपाना यह अनिह्नव है। शब्दों को शुद्ध पढ़ना व्यंजन शुद्ध विनय है। अर्थ शुद्ध करना अर्थशुद्ध विनय है और दोनों को शुद्ध रखना व्यंजनार्थ उभयशुद्ध विनय है। इस न्याय से ज्ञान का विनय आठ प्रकार से करना चाहिए। उसी ज्ञान की विशेषता को कहते हैं—
गाथार्थ — ज्ञान शिक्षित करता है, ज्ञान गुणी बनाता है, ज्ञान पर को उपदेश देता है, ज्ञान से न्याय किया जाता है। इस प्रकार यह जो करता है वह ज्ञान से विनयी होता है।।३६८।।
आचारवृत्ति — ज्ञान विद्या को प्राप्त कराता है। ज्ञान अवगुण को गुणरूप से परिवर्तित करता है। ज्ञान पर को उपदेश का प्रतिपादन करता है। ज्ञान से न्याय सत्प्रवृत्ति करता है जो ऐसा करता है वह ज्ञानविनीत होता है। प्रश्न — दर्शनाचार और दर्शन विनय में क्या अन्तर है ? उसी प्रकार ज्ञानाचार और ज्ञान विनय में क्या अन्तर है ?
उत्तर — शंकादि परिणामों के परिहार में प्रयत्न करना और उपगूहन आदि गुणों के अनुष्ठान में प्रयत्न करना दर्शनविनय है। पुनः शंकादि के अभावपूर्वक तत्त्वों के श्रद्धान में यत्न करना दर्शनाचार है। उसी प्रकार कालशुद्धि आदि विषय अनुष्ठान में प्रयत्न
चारित्रविनयस्वरूपं प्रतिपादयन्नाह—इंदियकसायपणिहाणपि
य गुत्तीओ चेव समिदीओ। एसो चरित्तविणओ समासदो होइ णायव्वो।।३६९।।
इन्द्रियाणि चक्षुरादीनि कषायाः क्रोधादयः तेषामिन्द्रियकषायाणां
प्रणिधानं प्रसरहानिरिन्द्रियकषायप्रणिधानं इन्द्रियप्रसरनिवारणं कषायप्रसरनिवारणं।
अथवेन्द्रियकषायाणां अपरिणामस्तद्गतव्यापारनिरोधनं।
अपि च गुप्तयो मनोवचनकायशुभप्रवृत्तयः। समितय
ईर्याभाषैषणादाननिक्षेपोच्चारप्रस्रवणप्रतिष्ठापनाः। एष चारित्रविनयः
समासतः संक्षेपतो भवति ज्ञातव्यः। अत्रापि। समितिगुप्तय आचारः।
तद्रक्षणोपाये यत्नश्चारित्रविनय इति।।३६९।।
तपोविनयस्वरूपं प्रतिपादयन्नाह—उत्तरगुणउज्जोगो सम्मं अहियासणा य सद्धा य।
आवासयाणमुचिदाणं अपरिहाणीयणुस्सेहो।।३७०।।
आतापनाद्युत्तरगुणेषूद्योग उत्साहः। सम्यगध्यासनं तत्कृतश्रमस्य निराकुलतया सहनं।
तद्गतश्रद्धा—तानुत्तरगुणान् कुर्वतः शोभनपरिणामः। आवश्यकानां
समतास्तव-वन्दनाप्रतिक्रमणप्रत्याख्यानकायोत्सर्गाणामुचितानां
कर्मक्षयनिमित्तानां परिमितानामपरि-हाणिरनुत्सेधः न हानिः
कर्तव्या नापि वृद्धिः। षडेव भावाश्चत्वारः पंच वा न कर्तव्याः।
करना काल आदि विनय हैं तथा द्रव्य, क्षेत्र और भाव आदि के विषय में प्रयत्न करना यह सब ज्ञानाचार है। कालशुद्धि आदि के होने पर श्रुत के पढ़ने का प्रयत्न करना ज्ञान विनय है और श्रुत के उपकरणों में अर्थात् ग्रन्थ, उपाध्याय आदि में प्रयत्न करना श्रुतविनय है। उसी प्रकार से जो तप से अज्ञान तम को दूर करता है और आत्मा को मोक्षमार्ग के समीप करता है वह तपोविनय है और नियमितमति होना है वह भी तप का विनय है ऐसा जानना चाहिए। चारित्र विनय का स्वरूप प्रतिपादित करते हैं—
गाथार्थ — इन्द्रिय और कषायों का निग्रह, गुप्तियाँ और समितियाँ संक्षेप से यह चारित्र विनय जानना चाहिए।।३६९।।
आचारवृत्ति — चक्षु आदि इन्द्रियाँ और क्रोधादि कषायों का प्रणिधान—प्रसार की हानि का होना अर्थात् इन्द्रिय के प्रसार का निवारण करना और कषायों के प्रसार का निवारण करना। अथवा इन्द्रिय और कषायों का परिणाम अर्थात् उनमें होने वाले व्यापार का निरोध करना, यह इन्द्रिय कषाय प्रणिधान है। मन, वचन और काय की शुभ प्रवृत्ति तथा सप्ताष्टौ न कर्तव्याः।
या यस्यावश्यकस्य वेला तस्यामेवासौ कर्तव्यो नान्यस्यां
वेलायां हािंन वृिंद्ध प्राप्नुयात्। तथा यस्यावश्यकस्य यावन्तः पठिताः
कायोत्सर्गास्तावन्त एव कर्तव्या न तेषां हानिर्वृद्धिर्वा कार्या इति।।३७०।।
भत्ती तवोधियम्हि य तवम्हि अहीलणा य सेसाणं।
एसो तवम्हि विणओ जहुत्तचारित्तसाहुस्स।।३७१।।
भक्तिः स्तुतिपरिणामः सेवा वा। तपसाधिकस्तपोऽधिकः तिंस्मस्तपोधिके।
आत्मनोऽधिकतपसि तपसि च द्वादशविधतपोऽनुष्ठाने च भक्तिरनुरागः।
शेषाणामनुत्कृष्ट-तपसामहेलना अपरिभवः। एष तपसि विनयः
सर्वसंयतेषु प्रणामवृत्तिर्यथोक्तचारित्रस्य साधोर्भवति ज्ञातव्य इति।।३७१।।
गुप्तियाँ हैं। ईर्या, भाषा, एषणा, आदाननिक्षेप और उच्चार प्रस्रवण प्रतिष्ठापना ये पाँच समितियाँ हैं। यह सब चारित्र विनय संक्षेप से कहा गया है। यहाँ पर भी समिति और गुप्तियाँ चारित्राचार हैं और उनकी रक्षा के उपाय में जो प्रयत्न है वह चारित्र विनय है। भावार्थ — इन्द्रियों का निरोध और कषायों का निग्रह होना तथा समिति, गुप्ति की रक्षा में प्रयत्न करना यह सब चारित्रविनय हैै। अब तपो विनय का स्वरूप कहते हैं—
गाथार्थ — उत्तर गुणों में उत्साह, उनका अच्छी तरह अभ्यास, श्रद्धा, उचित आवश्यकों में हानि या वृद्धि न करना तपोविनय है।।३७०।।
आचारवृत्ति — आतापन आदि उत्तर गुणों में उद्यम—उत्साह रखना, उनके करने में जो श्रम होता है उसको निराकुलता से सहन करना, उन उत्तर गुणों को करने वाले के प्रति श्रद्धा—शुभ भाव रखना। समता, स्तव, वंदना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और कायोत्सर्ग ये छह आवश्यक हैं। ये उचित हैं, कर्मक्षय के लिए निमित्त हैं। ये परिमित हैं, इनकी हानि और वृद्धि नहीं करना अर्थात् ये आवश्यक छह ही हैं, इन्हें चार वा पाँच नहीं करना तथा सात या आठ भी नहीं करना। जिस आवश्यक की जो बेला है उसी बेला में वह आवश्यक करना चाहिए अन्य बेला में नहीं अन्यथा हानि-वृद्धि हो जावेगी तथा जिस आवश्यक के जितने कायोत्सर्ग बताए गए हैं उतने ही करना चाहिए, उनकी हानि या वृद्धि नहीं करना चाहिए।
भावार्थ — उत्तर गुणों के धारण करने में उत्साह रखना, उनका अभ्यास करना और उनके करने वालों में आदर भाव रखना तथा आवश्यक क्रियाओं को आगम की कथित विधि से उन्हीं-उन्हीं के काल में कायोत्सर्ग की गणना से करना यह सब तपोविनय है। जैसे दैवसिक प्रतिक्रमण में वीरभक्ति में १०८
उच्छ्वासपूर्वक ३६ कायोत्सर्ग, पंचमौपचारिकविनयं
प्रपंचयन्नाह—काइयवाइयमाणसिओ त्ति अ तिविहो दु
पंचमो विणओ। सो पुण सव्वो दुविहो पच्चक्खो तह परोक्खो य।।३७२।।
काये भवः कायिकः। वाचि भवो वाचिकः। मनसि भवो मानसिकः।
त्रिविधस्रिप्रकारस्तु पंचमो विनयः। स्वर्गमोक्षादीन् विशेषेण नयतीति विनयः।
कायाश्रयो वागाश्रयो मानसाश्रयश्चेति। स पुनः सर्वोऽपि कायिको
वाचिको मानसिकश्च द्विविधो द्विप्रकारः प्रत्यक्षश्चैव परोक्षश्च।
गुरोः प्रत्यक्षश्चक्षुरादिविषयः। चक्षुरादिविषया-दतिक्रान्तः परोक्ष इति।।३७२।।
रात्रिक प्रतिक्रमण में ५४ उच्छ्वासपूर्वक १८ कायोत्सर्ग, देववंदना में चैत्य, पंचगुरुभक्ति सम्बन्धी कायोत्सर्ग इत्यादि कहे गए हैं सो उतने प्रमाण से विधिवत् करना।
गाथार्थ — तपोधिक साधु में और तप में भक्ति रखना तथा और दूसरे मुनियों की अवहेलना नहीं करना, आगम में कथित चारित्र वाले साधु का यह तपोविनय है।।३७१।।
आचारवृत्ति — जो तपश्चर्या में अपने से अधिक हैं वे तपोधिक होते हैं। उनमें तथा बारह प्रकार के तपश्चरण के अनुष्ठान में भक्ति अर्थात् अनुराग रखना। स्तुति के परिणाम को अथवा सेवा को भक्ति कहते हैं सो इनकी भक्ति करना। शेष जो मुनि अनुत्कृष्ट तप वाले हैं अर्थात् अधिक तपश्चरण नहीं करते हैं उनका तिरस्कार—अपमान नहीं करना। संयतों में प्रणाम की वृत्ति होना, यह सब तपोविनय है जो कि आगमानुवूâल चारित्रधारी साधु के होता है। पाँचवें औपचारिक विनय का विस्तारपूर्वक वर्णन करते हैं—
गाथार्थ — कायिक, वाचिक और मानसिक इस प्रकार पाँचवाँ औपचारिक विनय तीन भेद रूप है, पुनः वह तीन भेद रूप विनय प्रत्यक्ष तथा परोक्ष की अपेक्षा से दो प्रकार का है।।३७२।।
आचारवृत्ति — काय से होने वाला कायिक है, वचन से होने वाला वाचिक और मन से होने वाला मानसिक विनय है। जो स्वर्ग, मोक्षादि में विशेष रूप से ले जाता है वह विनय है। इस तरह औपचारिक नामक पाँचवाँ विनय तीन प्रकार का है अर्थात् काय के आश्रित, वचन के आश्रित और मन के आश्रित से यह विनय तीन भेद रूप है। वह तीनों प्रकार का विनय प्रत्यक्ष और परोक्ष के भेद से दो प्रकार है अर्थात् प्रत्यक्ष विनय के भी तीन भेद हैं और परोक्ष के भी तीन भेद हैं। जब गुरु प्रत्यक्ष में हैं, चक्षु आदि इन्द्रियों के गोचर हैं तब उनकी विनय प्रत्यक्ष विनय है तथा जब गुरु चक्षु आदि से परे दूर हैं तब उनकी जो विनय की जाती है वह परोक्षविनय है।
कायिकविनयस्वरूपं दर्शयन्नाह—अब्भुट्ठाणं किदिअम्मं
णवणं अंजलीय मुंडाणं। पच्चूगच्छणमेत्ते पछिदस्सणुसाहणं चेव।।३७३।।
अभ्युत्थानमादरेणासनादुत्थानं। क्रियाकर्म सिद्धभक्तिश्रुतभक्तिगुरुभक्तिपूर्वकं
कायोत्सर्गादिकरणं। नमनं शिरसा प्रणामः। अञ्जलिना करकुंडलेनाञ्जलिकरणं
वा मुण्डानामृषीणां। अथवा मुण्डा सामान्यवन्दना। पच्चूगच्छणमेत्ते—आगच्छतः
प्रतिगमनमभिमुखयानं। प्रस्थितस्य प्रयाणके व्यवस्थितस्यानुसाधनं
चानुव्रजनं च साधूनामादरः कार्यः। तथा तेषामेव क्रियाकर्म कर्तव्यम्।
तथा तेषामेव कृताञ्जलिपुटेन नमनं कत्र्तव्यं। तथा साधोरागतः
प्रत्यभिमुखगमनं कर्तव्यं तथा तस्यैव प्रस्थितस्यानुव्रजनं कर्तव्यमिति।।३७३।।
कायिक विनय का स्वरूप दिखलाते हैं—गाथार्थ — केशलोंच से मुण्डित हुए अतः जो मुण्डित कहलाते हैं ऐसे मुनियों के लिए उठकर खड़े होना, भक्तिपाठपूर्वक वन्दना करना, हाथ जोड़कर नमस्कार करना, आते हुए के सामने जाना और प्रस्थान करते हुए के पीछे-पीछे चलना।।३७३।।
आचारवृत्ति — मुण्ड अर्थात् ऋषियों को सामने देखकर आदरपूर्वक आसन से उठकर खड़े हो जाना, क्रियाकर्म—ाqसद्धभक्ति, श्रुतभक्ति, गुरुभक्तिपूर्वक कायोत्सर्ग आदि करके वन्दना करना, अंजलि जोड़कर शिर झुकाकर नमस्कार करना नमन है। यहाँ मुण्ड का अर्थ ऋषि है अथवा ‘मुण्ड’ का अर्थ सामान्य वन्दना है अर्थात् भक्तिपाठ के बिना नमस्कार करना मुण्ड-वन्दना है। जो साधु सामने आ रहे हैं उनके सम्मुख जाना, प्रस्थान करने वाले के पीछे-पीेछे चलना। तात्त्पर्य यह है कि साधुओं का आदर करना चाहिए। उनके प्रति भक्तिपाठ करते हुए कृतिकर्म करना चाहिए तथा उन्हें अंजलि जोड़कर नमस्कार करना चाहिए। साधुओं के आते समय सन्मुख जाकर स्वागत करना चाहिए और उनके प्रस्थान करने पर कुछ दूर पहुँचाने के लिए उनके पीछे-पीछे जाना चाहिए।
गाथार्थ — गुरुओं से नीचे खड़े होना, नीचे अर्थात् पीछे चलना, नीचे बैठना, नीचे स्थान में सोना, गुरु को आसन देना, उपकरण देना और ठहरने के लिए स्थान देना—यह सब कायिक विनय है।।३७४।।
आचारवृत्ति — देव और गुरु के सामने नीचे खड़े होना (विनय से एक तरफ खड़े होना), गुरु के साथ चलते समय उनके बाएँ चलना या उनके पीछे चलना, गुरु के नीचे आसन रखना अथवा पीठ, पाटे आदि आसन को छोड़ देना। गुरु को आसन आदि तथा—
णीचं ठाणं णीचं गमणं णीचं च आसणं सयणं।
आसणदाणं उवगरणदाण ओगासदाणं च।।३७४।।
देवगुरुभ्यः पुरतो नीचं स्थानं वामपाश्र्वे स्थानं। नीचं
च गमनं गुरोर्वामपाश्र्वे पृष्ठतो वा गन्तव्यं। नीचं च
न्यग्भूतं चासनं पीठादिवर्जनंं। गुरोरासनस्य पीठादिकस्य
दानं निवेदनं। उपकरणस्य पुस्तिकाकुंडिकापिच्छिकादिकस्य
प्रासुकस्यान्विष्य दानं निवेदनं। अथवा नीचं स्थानं
करचरणसंकुचितवृत्तिर्गुरोः सधर्मणोऽन्यस्य वा व्याधितस्येति।।३७४।।
तथा—पडिरूवकायसंफासणदा य पडिरूपकालकिरिया य।
पेसणकरणं संथरकरणं उवकरण पडिलिहणं।।३७५।।
प्रतिरूपं शरीरबलयोग्यं कायस्य शरीरस्य संस्पर्शनं मर्दनमभ्यंगनं वा।
प्रतिरूपकालक्रिया चोष्णकाले शीतक्रिया शीतकाले उष्णक्रिया
वर्षाकाले तद्योग्यक्रिया। प्रेष्यकरणं—आदेशकरणं।
संस्तरकरणं पट्टकादिप्रस्तरणं। उपकरणानां
पुस्तिकाकुण्डि-कादीनां प्रतिलेखनं सम्यग्निरूपणम् ।।३७५।।
देना, उनके लिए आसन देकर उन्हें विराजने के लिए निवेदन करना। उन्हें पुस्तक, कमण्डलु, पिच्छिका आदि उपकरण देना, वसतिका या पर्वत की गुफा आदि प्रासुक स्थान अन्वेषण करके गुरु को उसमें ठहरने के लिए निवेदन करना। अथवा ‘नीच स्थान’ का अर्थ यह है कि गुरु, सहधर्मी मुनि अथवा अन्य कोई व्याधिग्रसित मुनि के प्रति हाथ-पैर संकुचित करके बैठना। तात्पर्य यही है कि प्रत्येक प्रवृत्ति में विनम्रता रखना। उसी प्रकार से—
गाथार्थ — गुरु के अनुरूप उनके अंग का मर्दनादि करना, उनके अनुरूप और काल के अनुरूप क्रिया करना, आदेश पालन करना, उनके संस्तर लगाना तथा उपकरणों का प्रतिलेखन करना।।३७५।।
आचारवृत्ति — गुरु के शरीर बल के योग्य शरीर का मर्दन करना अथवा उनके शरीर में तेल मालिश करना, उष्ण काल में शीत क्रिया, शीतकाल में उष्णक्रिया करना और वर्षाकाल में उस ऋतु के योग्य क्रिया करना अर्थात् गुरु की सेवा आदि ऋतु के अनुवूâल और उनकी प्रकृति के अनुवूâल करना। उनके आदेश का पालन करना;
उनकेइच्चेवमादिओ जो उवयारो कीरदे सरीरेण।
एसा काइयविणओ जहारिहं साहुवग्गस्स।।३७६।।
इत्येवमादिरूपकारो गुरोरन्यस्य वा साधुवर्गस्य यः शरीरेण क्रियते
यथायोग्यं स एष कायिको विनयः कायाश्रितत्वादिति।।३७६।।
वाचिकविनयस्वरूपं विवृण्वन्नाह—पूयावयणं हिदभासणं मिदभासणं च मधुरं च।
सुत्ताणुवीचिवयणं अणिट्ठुरमकक्कसं वयणं।।३७७।।
पूजावचनं बहुवचनोच्चारणं यूयं भट्टारका इत्येवमादि।
हितस्य पथ्यस्य भाषणं इहलोकपरलोकधर्मकारणं वचनं।
मितस्य परिमितस्य भाषणं चाल्पाक्षरबह्वर्थं। मधुरं च मनोहरं श्रुतिसुखदं।
सूत्रानुवीचिवचनमागमदृष्ट्या भाषणं यथा पापं न भवति।
अनिष्ठुरं दग्धमृतप्रलीनेत्यादिशब्दै रहितं।
अकर्कशं वचनं च वर्जयित्वा वाच्यमिति।।३७७।।
लिए संस्तर अर्थात् चटाई, घास, पाटा आदि लगाना, उनके पुस्तक, कमण्डलु आदि उपकरणों को ठीक तरह से पिच्छिका से प्रतिलेखन करके उन्हें देना।
गाथार्थ — साधुवर्ग का इसी प्रकार से और भी जो उपकार यथायोग्य अपने शरीर के द्वारा किया जाता है यह सब कायिक विनय है।।३७६।।
आचारवृत्ति — इसी प्रकार से अन्य और भी जो उपकार गुरु या साधु वर्ग का शरीर के द्वारा योग्यता के अनुसार किया जाता है वह सब कायिक विनय है; क्योंकि वह काय के आश्रित है। वाचिक विनय का स्वरूप कहते हैं—
गाथार्थ — पूजा के वचन, हित वचन, मितवचन और मधुर वचन, सूत्रों के अनुकूल वचन, अनिष्ठुर और कर्तव्यशतारहित वचन बोलना वाचिक विनय है।।३७७।।
आचारवृत्ति — ‘आप भट्टारक!’ इत्यादि प्रकार बहुवचन का उच्चारण करना पूजा वचन है। हित—पथ्य वचन बोलना अर्थात् इस लोक और परलोक के लिए धर्म के कारणभूत वचन हितवचन हैं। मित—परिमित बोलना, जिसमें अल्प अक्षर हों किन्तु अर्थ बहुत हो मित वचन हैं। मधुर—मनोहर अर्थात् कानों को सुखदायी वचन मधुर वचन हैं। आगम के अनुकूल बोलना कि जिस प्रकार से पाप न हो सूत्रानुवीचि वचन हैं। तुम जलो मरो, प्रलय को प्राप्त हो जाओ इत्यादि शब्दों से रहित वचन अनिष्ठुर वचन हैं और कठोरतारहित वचन अकर्कश वचन हैं अर्थात् उपर्युक्त प्रकार के वचन बोलना ही वाचिक विनय है।
उवसंतवयणमगिहत्थवयणमकिरियमहीलणं वयणं।
एसो वाइयविणओ जहारिहं होदि कादव्वो।।३७८।।
उपशान्तवचनं क्रोधमानादिरहितं। अगृहस्थवचनं गृहस्थानां
मकारवकारादि यद्वचनं तेन रहितं बन्धनत्रासनताडनादिवचनरहितं।
अकिरियं असिमसिकृष्यादिक्रिया (दि) रहितं अथवा सक्रियमिति पाठः।
सक्रियं क्रियायुक्तमन्यच्चिन्तान्यदोषयोरिति न वाच्यं,
तदुच्यते यन्निष्पाद्यते। अहीलं—अपरिभवचनंं। इत्येवमादिवचनं य
त्र स एष वाचिको विनयो यथायोग्यं भवति कर्तव्य इति।।३७८।।
मानसिकविनयस्वरूपमाह—पापविसोत्तिअपरिणामवज्जणं पियहिदे य परिणामो।
णादव्वो संखेवेणेसो माणसिओ विणओ।।३७९।।
पापविश्रुतिपरिणामवर्जनं पापं हिंसादिकं विश्रुतिः सम्यग्विराधना
तयोः परिणामस्तस्य वर्जनं परिहारः। प्रिये धर्मोपकारे हिते
च सम्यग्ज्ञानादिके च परिणामो ज्ञातव्यः। संक्षेपेण
स एष मानसिकश्चित्तोद्भवो विनय इति।।३७९।।
गाथार्थ — कषायरहित वचन, गृहस्थी सम्बन्ध से रहित वचन, क्रियारहित और अवहेलना रहित वचन बोलना—यह वाचिक विनय है जिसे यथायोग्य करना चाहिए।।३७८।।
आचारवृत्ति — क्रोध, मान आदि से रहित वचन उपशान्त वचन हैं। गृहस्थों के जो मकार-वकार आदि रूप वचन हैं उनसे रहित वचन तथा बन्धन, त्रासन, ताडन आदि से रहित वचन अगृहस्थ वचन हैं। असि, मषि, कृषि आदि क्रियाओं से रहित वचन अक्रियवचन हैं। अथवा ‘सक्रियं’ ऐसा भी पाठ है जिसका अर्थ यह है कि क्रियायुक्त वचन बोलना किन्तु अन्य की चिन्ता और अन्य के दोषरूप वचन नहीं बोलना चाहिए। जैसा करना वैसा ही बोलना चाहिए। किसी का तिरस्कार करने वाले वचन नहीं बोलना अहीलन वचन हैं। और भी ऐसे ही वचन जहाँ होते हैं वह सब वाचिक विनय है जो कि यथायोग्य करना चाहिए। मानसिक विनय का स्वरूप कहते हैं—
गाथार्थ — पापविश्रुत के परिणाम का त्याग करना और प्रिय तथा हित में परिणाम करना संक्षेप से यह मानसिक विनय है।।३७९।।
आचारवृत्ति —सादि को पाप कहते हैं और सम्यक्त्व की विराधना को विश्रुति कहते हैं। इन पाप और विराधनाविषयक परिणामों का त्याग करना। धर्म और उपकार को प्रिय कहते हैं तथा सम्यग्ज्ञानादि के लिए हित संज्ञा है। इन प्रिय और हित में परिणाम को लगाना। संक्षेप से यह चित्त से उत्पन्न होने वाला मानसिक विनय कहलाता है।
इय एसो पच्चक्खो विणओ पारोक्खिओवि जं गुरुणो।
विरहम्मिवि वट्टिज्जदि आणाणिद्देसचरियाए।।३८०।।
इत्येष प्रत्यक्षविनयः कायिकादिः, गुर्वादिषु सत्सु वर्तते यतः,
पारोक्षिकोऽपि विनयो यद्गुर्रोिवरहेऽपि गुर्वादिषु परोक्षीभूतेषु यद्वर्तते।
आज्ञानिर्देशेन चर्याया वार्हद्भट्टारकोपदिष्टेषु जीवादिपदार्थेषु श्रद्धानं
कर्तव्यं तथा तैर्या चर्योद्दिष्टा व्रतसमित्यादि- का तया च
वर्तनं परोक्षो विनयः। तेषां प्रत्यक्षतो यः क्रियते स प्रत्यक्षमिति।।३८०।।
पुनरपि त्रिविधं विनयमन्येन प्रकारेणाह—अह ओपचारिओ
खलु विणओ तिविहा समासदो भणिओ।
सत्त चउव्विह दुविहो बोधव्वो आणुपुव्वीए।।३८१।।
अथौपचारिको विनय उपकारे धर्मादिकपरचित्तानुग्रहे भव
औपचारिकः खलु स्फुटं त्रिविधस्त्रिप्रकारः कायिकवाचिकमानसिकभेदेन
समासतः संक्षेपतो भणितः
गाथार्थ — इस प्रकार यह प्रत्यक्ष विनय है तथा जो गुरु के न होने पर भी उनकी आज्ञा, निर्देश और चर्या में रहता है उसके परोक्ष सम्बन्धी विनय होता है।।३८०।।
आचारवृत्ति — यह सब ऊपर कहा गया कायिक आदि विनय प्रत्यक्ष विनय है, क्योंकि यह गुरु के रहते हुए उनके पास में किया जाता है। और गुरुओं के विरह में—उनके परोक्ष रहने पर अर्थात् अपने से दूर हैं उस समय भी जो उनका विनय किया जाता है वह परोक्ष विनय है। वह उनकी आज्ञा और निर्देश के अनुसार चर्या करने से होता है अथवा अर्हन्त भट्टारक द्वारा उपदिष्ट जीवादि पदार्थों में श्रद्धान करना तथा उनके द्वारा जो भी व्रत, समिति आदि चर्याएँ कही गई हैं, उन रूप प्रवृत्ति करना यह सब परोक्ष विनय है अर्थात् उनके प्रत्यक्ष में किया गया विनय प्रत्यक्ष विनय तथा परोक्ष में किया गया नमस्कार, आज्ञा पालन आदि विनय परोक्ष विनय है। पुनः इन्हीं तीन प्रकार की विनय को अन्य रूप से कहते हैं—
गाथार्थ — यह औपचारिक विनय संक्षेप से कायिक, वाचिक और मानसिक ऐसा तीन प्रकार से कहा गया है। वह क्रम से सात भेद, चार भेद और दो भेदरूप जानना चाहिए।।३८१।।
आचारवृत्ति — जो उपचार अर्थात् धर्मादि के द्वारा पर के मन पर अनुग्रह करने वाला होता है वह औपचारिक विनय कहलाता है। यह औपचारिक विनय प्रकट रूप से कायिक, वाचिक और मानसिक भेदों की अपेक्षा संक्षेप में तीन प्रकार का कहा गया है। उसमें क्रम से सात, चार और दो भेद माने गए हैं अर्थात् कायिक विनय सात प्रकार का है, वाचिक विनय चार प्रकार का है और मानसिक विनय दो प्रकार का है।
कथितः। सप्तविधश्चर्तुिवधो द्विविधो बोद्धव्यः।
आनुपूव्र्यानुक्रमेण कायिकः सप्तप्रकारो
वाचिकश्चर्तुिवधः मानसिको द्विविध इति।।३८१।।
कायिकविनयं सप्तप्रकारमाह—अब्भुट्ठाणं सण्णदि
आसणदाणं अणुप्पदाणं च। किदियम्मं
पडिरूवं आसणचाओ य अणुव्वजणं।।३८२।।
अभ्युत्थानम् आदरेणोत्थानं। सन्नतिः शिरसा प्रणामः।
आसनदानं पीठाद्युपनयनं। अनुप्रदानं च पुस्तकपिच्छिकाद्युपकरणदानं।
क्रियाकर्म श्रुतभक्त्यादिपूर्वककायोत्सर्गः प्रतिरूपं यथायोग्यं,
अथवा शरीरप्रतिरूपं कालप्रतिरूपं भावप्रतिरूपं च क्रियाकर्म
शीतोष्णमूत्रपुरीषाद्यपनयनं। आसनपरित्यागो गुरोः पुरत उच्चस्थाने न स्थातव्यं।
अनुव्रजनं प्रस्थितेन सह विंâचिद्गमनमिति। अभ्युत्थानमेकः
सन्नर्तििद्वतीय आसनदानं तृतीयः अनुप्रदानं चतुर्थः प्रतिरूपक्रियाकर्म
पंचमः आसनत्यागः षष्ठोऽनुव्रजनं सप्तमः प्रकारः कायिकविनयस्येति।।३८२।।
कायिक विनय के सात प्रकार को कहते हैं—
गाथार्थ — गुरुओ को आते हुए देखकर उठकर खड़े होना, उन्हें नमस्कार करना, आसन देना, उपकरणादि देना, भक्ति पाठ आदि पढ़कर वन्दना करना या उनके अनुकूल क्रिया करना, आसन को छोड़ देना और जाते समय उनके पीछे जाना ये सात भेदरूप कायिक विनय है।।३८२।।
आचारवृत्ति — अभ्युत्थान—गुरुओं को सामने आते हुए देखकर आदर से उठकर खड़े हो जाना।
सन्नति —ाशर से प्रणाम करना। आसनदान—पीठ, काष्ठासन, पाटा आदि देना।
अनुप्रदान—पुस्तक, पिच्छिका आदि उपकरण देना। प्रतिरूप क्रियाकर्म— यथायोग्य श्रुतभक्ति आदिपूर्वक कायोत्सर्ग करके वन्दना करना अथवा गुरुओं के शरीर के प्रकृति के अनुरूप, काल के अनुरूप और भाव के अनुरूप सेवा-शुश्रूषा आदि क्रियाएँ करना; जैसे कि शीतकाल में उष्णकारी और उष्णकाल में शीतकारी आदि परिचर्या करना, अस्वस्थ अवस्था में उनके मल-मूत्रादि को दूर करना आदि।
आसनत्याग—गुरु के सामने उच्चस्थान पर नहीं बैठना।
अनुव्रजन—उनके प्रस्थान करने पर साथ-साथ कुछ दूर तक जाना। इस प्रकार से (१) अभ्युत्थान, (२) सन्नति, (३) आसनदान, (४) अनुप्रदान, (५) प्रतिरूपक्रियाकर्म, (६) आसनत्याग और (७) अनुव्रजन—ये सात प्रकार कायिक विनय के होते हैं।
वाचिकमानसिकविनयभेदानाह—हिदमिदपरिमिदभासा अणुवीचीभाषणं च बोधव्वं।
अकुसलमणस्स रोधो कुसलमणपवत्तओ चेव।।३८३।।
हितभाषणं मितभाषणं परिमितभाषणमनुवीचिभाषणं च।
हितं धर्मसंयुक्तं। मितमल्पाक्षरं बह्वर्थं। परिमितं कारणसहितं।
अनुवीचीभाषणमागमाविरुद्धवचनं चेति चतुर्विधो वचनविनयो ज्ञातव्यः।
तथाऽकुशलमनसो रोधः पापादानकारकचित्तनिरोधः।
कुशलमनसो धर्मप्रवृत्तचित्तस्य प्रवर्तकश्चेति द्विविधो मनोविनय इति।।३८३।।
स एवं द्विविधो विनयः साधुवर्गेण कस्य कर्तव्य इत्याशंकायामाह—रादिणिए
उगरादिणिएसु अ अज्जासु चेव गिहिवग्गे। विणओ जहारिओ सो कायव्वो अप्पमत्तेण।।३८४।।
रादिणिए—रात्र्यधिके दीक्षागुरौ श्रुतगुरौ तपोधिके च।
उणरादिणिएसु य—ऊनरात्रिकेषु च तपसा कनिष्ठेषु गुणकनिष्ठेषु वयसा
कनिष्ठेसु च साधुषु। अज्जासु—र्आियकासु। गिहिवग्गे—गृहिवर्गे श्रावकलोके च।
विनयो यथार्हो यथायोग्यः कर्तव्यः। अप्रमत्तेन प्रमादरहितेन।
साधूनां यो योग्यः आर्यिकाणां यो योग्यः, श्रावकाणां यो योग्यः,
अन्येषामपि यो योग्यः स तथा कर्तव्यः, केन ?
साधुवर्गेणाप्रमत्तेनात्म-तपोऽनुरूपेण प्रासुकद्रव्यादिभिः
स्वशक्त्या चेति। किमर्थं विनयः क्रियते इत्याशंकायामाह—वणएण
विप्पहीणस्स हवदि सिक्खा णिरत्थिया सव्वा। विणओ
सिक्खाए फलं विणयफलं सव्वकल्लाणं।।३८५।।
विनयेन विप्रहीणस्य विनयरहितस्य भवति शिक्षा श्रुताध्ययनं
निर्रिथका विफला सर्वा सकला विनयः पुनः शिक्षा या
विद्याध्ययनस्य फलं, विनयफलं सर्वकल्याणान्यभ्यु-दयनिःश्रेयससुखानि।
अथवा स्वर्गावतरणजन्मनिष्क्रमणकेवलज्ञानोत्पत्तिपरिनिर्वाणादीनि कल्याणादीनीति।।३८५।।
वाचिक और मानसिक विनय के भेदों को कहते हैं—
गाथार्थ — हितवचन, मितवचन, परिमितवचन और सूत्रानुसार वचन, इन्हें वाचिक विनय जानना चाहिए। अशुभ मन को रोकना और शुभ मन की प्रवृत्ति करना ये दो मानसिक विनय हैं।।३८३।।
आचारवृत्ति — हित भाषण—धर्मसंयुक्त वचन बोलना, मित भाषण—ाqजसमें अक्षर अल्प हों अर्थ बहुत हो ऐसे वचन बोलना, परिमित भाषण—कारण सहित वचन बोलना अर्थात् बिना प्रयोजन के नहीं बोलना, अनुवीचिभाषण—आगम से अविरुद्ध वचन बोलना, इस प्रकार से वचन विनय चार प्रकार का है। पाप आस्रव करने वाले अशुभ मन का रोकना अर्थात् मन में अशुभ विचार नहीं लाना तथा धर्म में चित्त को लगाना ये दो प्रकार का मनोविनय है। यह प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप दोनों प्रकार का विनय साधुओं को किनके प्रति करना चाहिए ? ऐसी आशंका होने पर कहते हैं—
गाथार्थ — एक रात्रि भी अधिक गुरु में, दीक्षा में एक रात्रि न्यून भी मुनि में, आर्यिकाओं में और गृहस्थों में अप्रमादी मुनि को यथायोग्य यह विनय करना चाहिए।।३८४।।
आचारवृत्ति — जो दीक्षा में एक रात्रि भी बड़े हैं वे रात्र्यधिक गुरु हैं। यहाँ रात्र्यधिक शब्द से दीक्षा गुरु, श्रुतगुरु और तप में अपने से बड़े गुरुओं को लिया है। जो दीक्षा में एक रात्रि भी छोटे हैं वे ऊनरात्रिक कहलाते हैं। यहाँ पर ऊनरात्रिक से जो तप में कनिष्ठ—लघु हैं, गुणों में लघु हैं और आयु में लघु हैं उन साधुओं को लिया है। इस प्रकार से दीक्षा आदि बड़े गुरुओं में, अपने से छोटे मुनियों में, र्आियकाओं में और श्रावक वर्गों में प्रमादरहित मुनि को यथायोग्य विनय करना चाहिए अर्थात् साधुओं के जो योग्य हो, र्आियकाओं के जो योग्य हो, श्रावकों के जो योग्य हो और अन्यों के भी जो योग्य हो वैसा ही करना चाहिए। किसको ? प्रमादरहित हुए साधु को अपने तप अर्थात् अपने व्रतों के, अपने पद के अनुरूप ही प्रासुक द्रव्यादि के द्वारा अपनी शक्ति से उन सबका विनय करना चाहिए।
विशेष—यहाँ पर जो मुनियों द्वारा र्आियकाओं की और गृहस्थों की विनय का उपदेश है सो नमस्कार नहीं समझना, प्रत्युत् यथायोग्य शब्द से समझना कि मुनिगण र्आियकाओं का भी यथायोग्य आदर करें, श्रावकों का भी यथायोग्य आदर करें क्योंकि ‘यथायोग्य’ पद उनके अनुरूप अर्थात् पदस्थ के अनुकूल विनय का वाचक है। उससे आदर, सन्मान और बहुमान ही अर्थ सुघटित है। विनय किसलिए किया जाता है ? ऐसी आशंका होने पर कहते हैं—
गाथार्थ — विनय से हीन हुए मनुष्य की सम्पूर्ण शिक्षा निरर्थक है। विनय शिक्षा का फल है और विनय का फल सर्व कल्याण है।।३८५।।
आचारवृत्ति — विनय से रहित साधु का सम्पूर्ण श्रुत का अध्ययन निरर्थक है। विद्याअध्ययन का फल विनय है और अभ्युदय तथा निःश्रेयसरूप सर्व कल्याण को प्राप्त कर लेना विनय का फल है अथवा स्वर्गावतरण, जन्म, निष्क्रमण, केवलज्ञानोत्पत्ति और परिनिर्वाण ये पाँच कल्याणक आदि कल्याणों की प्राप्ति का होना भी विनय का फल है।
विनयस्तवमाह—वणओ मोक्खद्दारं विणयादो संजमो तवो णाणं।
विणएणाराहिज्जदि आइरिओ सव्वसंघो य।।३८६।।
विनयो मोक्षस्य द्वारं प्रवेशकः। विनयात्संयमः। विनयात्तपः।
विनयाच्च ज्ञानं। भवतीति सम्बन्धः। विनयेन चाराध्यते आचार्यः सर्वसंघश्चापि।।३८६।।
आयारजीदकप्पगुणदीवणा अत्तसोधि णिज्जंजा।
अज्जवमद्दवलाहवभत्तीपल्हादकरणं चं।।३८७।।
आचारस्य गुणा जीदप्रायश्चित्तस्य कल्पप्रायश्चित्तस्य
गुणास्तद्गतानुष्ठानानि तेषां दीपनं प्रकटनं।
आत्मशुद्धिश्चात्मकर्मनिर्मुक्तिः। निद्र्वन्द्वः कलहाद्यभावः।
ऋजोर्भाव आर्जवं स्वस्थता, मृदो भावो मार्दवं मायामानर्योिनरासः।
लघोर्भावो लाघवं निःसंगता लोभनिरासः। भक्तिर्गुरुसेवा।
प्रह्लादकरणं च सर्वेषां सुखोत्पादनं। यो विनयं करोति
तेनाचरजीदकल्पविषया ये गुणास्ते दीपिता उद्योतिता भवंति।
आर्जव-मार्दवलाघवभक्तिप्रह्लादकरणानि च भवंति विनयकर्तुरिति।।३८७।।
कित्ती मित्ती माणस्स भंजण गुरुजणे य बहुमाणं।
तित्थयराणं आणा गुणाणुमोदो य विणयगुणा।।३८८।।
कीर्ति सर्वव्यापी प्रतापः ख्यातिश्च। मैत्री सर्वैः सह मित्रभावः।
मानस्य गर्वस्य भंजनमामर्दनं। गुरुजने च बहुमानं पूजाविधानं।
तीर्थंकराणामाज्ञा पालिता भवति। गुणानुमोदश्च कृतो भवति।
एते विनयगुणा भवन्तीति। विनयस्य कर्ता कीा\त लभते। तथा मैत्रीं लभते।
तथात्मनो मानं निरस्यति। गुरुजनेभ्यो बहुमानं लभते।
तीर्थकराणामाज्ञां च पालयति। गुणानुरागं च करोतीति।।३८८।।
वैयावृत्यस्वरूपं निरूपयन्नाह—आइरियादिसु पंचसु सबालवुड्ढाउलेसु गच्छेसु।
वेज्जावच्चं वुत्तं कादव्वं सव्वसत्तीए।।३८९।।
आचार्योपाध्यायस्थविरप्रवर्तकगणधरेषु पंचसु। बाला नवकप्रव्रजिताः।
वृद्धा वयोवृद्धास्तपोवृद्धा गुणवृद्धास्तैराकुलो गच्छस्तथैव बालवृद्धाकुले
गच्छे सप्तपुरुषसन्ताने। वैयावृत्यमुक्तं यथोक्तं कर्तव्यं
सर्वशत्क्या सर्वसामथ्र्येन उपकरणाहारभैषजपुस्तकादिभिरुपग्रहः कर्तव्य इति।।३८९।।
अब विनय की स्तुति करते हैं—
गाथार्थ — विनय मोक्ष का द्वार है। विनय से संयम, तप और ज्ञान होता है। विनय के द्वारा आचार्य और सर्वसंघ आराधित होता है।।३८६।।
आचारवृत्ति — विनय मोक्ष का द्वार है अर्थात् मोक्ष में प्रवेश कराने वाला है। विनय से संयम होता है, विनय से तप होता है और विनय से ज्ञान होता है। विनय से आचार्य और सर्वसंघ आराधित किए जाते हैं अर्थात् अपने ऊपर अनुग्रह करने वाले हो जाते हैं।
गाथार्थ — विनय से आचार, जीद, कल्प आदि गुणों का उद्योतन होता है तथा आत्मशुद्धि, निद्र्वंद्वता, आर्जव, मार्दव, लघुता, भक्ति और आह्लादगुण प्रकट होते हैं।।३८७।।
आचारवृत्ति — विनय से आचार के गुण, जीदप्रायश्चित्त और कल्पप्रायश्चित्त के गुण तथा उनमें कहे हुए का अनुष्ठान, इन गुणों का दीपन अर्थात् प्रकटन होता है। विनय से आत्मशुद्धि अर्थात् आत्मा की कर्मों से निर्मुक्ति होती है, निद्र्वंद्व—कलह आदि का अभाव हो जाता है। आर्जव—स्वस्थता आती है, मृदु का भाव मार्दव अर्थात् माया और मान का निरसन हो जाता है, लघु का भाव लाघव—नःसंगपना होता है अर्थात् लोभ का अभाव हो जाने से भारीपन का अभाव हो जाता है। भक्ति—गुरु के प्रति भक्ति होने से गुरु सेवा भी होती है और विनय से प्रह्लादकरण—सभी में सुख का उत्पन्न करना आ जाता है। तात्पर्य यह है कि जो विनय करता है उसके उस विनय के द्वारा आचार, जीद और कल्पविषयक जो गुण हैं वे उद्योतित होते हैं। आर्जव, मार्दव, लाघव, भक्ति और आल्हादकरण ये गुण विनय करने वाले में प्रकट हो जाते हैं।
गाथार्थ — कीर्ति, मैत्री, मान का भंजन, गुरुजनों में बहुमान, तीर्थंकरों की आज्ञा का पालन और गुणों का अनुमोदन ये सब विनय के गुण हैं।।३८८।।
आचारवृत्ति — विनय से सर्वव्यापी प्रताप और ख्याति रूप र्कीित होती है। सभी के साथ मित्रता होती है, गर्व का मर्दन होता है, गुरुजनों में बहुमान अर्थात् पूजा या आदर मिलता है, तीर्थंकरों की आज्ञा का पालन होता है और गुणों की अनुमोदना की जाती है। ये सब विनय के गुण हैं। तात्पर्य यह है कि विनय करने वाला मुनि र्कीित को प्राप्त होता है, सबसे मैत्री भाव को प्राप्त हो जाता है, अपने मान का अभाव करता है, गुरुजनों से बहुमान पाता है, तीर्थंकरों की आज्ञा का पालन करता है और गुणों में अनुराग करता है। अब वैयावृत्त्य का स्वरूप निरूपित करते हैं—
गाथार्थ — आचार्य आदि पाँचों में, बाल-वृद्ध से सहित गच्छ में वैयावृत्त्य को कहा गया है सो सर्वशक्ति से करनी चाहिए।।३८९।।
आचारवृत्ति — आचार्य, उपाध्याय, स्थविर, प्रवर्तक और गणधर ये पाँच हैं। नवदीक्षित को बाल कहते हैं। वृद्ध से वयोवृद्ध, तपोवृद्ध और गुणों से वृद्ध लिए गए हैं। सात पुरुष की परम्परा को अर्थात् सात पीढ़ी को गच्छ कहते हैं। इन आचार्य आदि पाँच पुनरपि विशेषार्थं श्लोकेनाह—
गुणाधिए उवज्झाए तवस्सि सिस्से य दुव्वले।
साहुगण कुले संघे समणुण्णे य चापदि।।३९०।।
गुणैरधिको गुणाधिकस्तस्मिन् गुणाधिके। उपाध्याये श्रुतगुरौ।
तपस्विनि कायक्लेशपरे। शिक्षके शास्त्रशिक्षणतत्परे दुःशीले या दुर्बले व्याध्याक्रान्ते वा।
साधुगणे ऋषियतिमुन्यनगारेषु। कुले शुक्रकुले स्त्रीपुरुषसन्ताने।
संघे चातुर्वण्र्ये श्रवणसंघे। समनोज्ञे सुखासीने सर्वोपद्रवरहिते।
आपदि चोपद्रवे संजाते वैयावृत्यं कर्तव्यमिति।।३९०।।
वै कृत्वा वैयावृत्यं कर्तव्यमित्याह—सेज्जोग्गासणिसेज्जो
तहोवहिपडिलेहणा हि उवग्गहिदे। आहारोसहवायण वििंकचणंवंदणादीिंह।।३९१।।
शय्यावकाशो वसतिकावकाशदानं निषद्याऽऽसनादिकं।
उपधिः कुण्डिकादि। प्रतिलेखनं पिच्छिकादिः। इत्येतैरुपग्रह उपकारः।
अथवैतैरुपगृहीते स्वीकृते। तथाहारौषध-वाचनाव्याख्यानवििंकचनमूत्रपुरीषादिव्युत्सर्गवन्दनादिभिः।
आहारेण भिक्षाचर्यया। औषधेन शुंठिपिप्पल्यादिकेन। शास्त्रव्याख्यानेन।
च्युतमलनिर्हरणेन। वन्दनया च। शय्यावकाशेन निषद्ययोपधिना
प्रतिलेखनेन च पूर्वोक्तानामुपकारः कर्तव्यः। एतैस्ते प्रतिगृहीता आत्मीकृता भवन्तीति।।३९१।।
केषु स्थानेषूपकारः क्रियतेऽत आह—अद्धाणतेणविदरायणदीरोधणासिवे
ओमे। वेज्जावच्चं वुत्तं संगहसारक्खणोवेदं।।३९२।।
प्रकार के साधुओं की तथा बाल, वृद्ध से व्याप्त ऐसे संघ की आगम में कथित प्रकार से सर्वशक्ति से वैयावृत्य करना चाहिए अर्थात् अपनी सर्व सामथ्र्य से उपकरण, आहार, औषधि, पुस्तक आदि से इनका उपकार करना चाहिए।
भावार्थ — तप और त्याग में आचार्यों ने शक्ति के अनुसार करना कहा है किन्तु वैयावृत्ति में सर्वशक्ति से करने का विधान है। इससे वैयावृत्ति के विशेष महत्त्व को सूचित किया गया है। पुनरपि विशेष अर्थ के लिए आगे के श्लोक (गाथा) द्वारा कहते हैं—
गाथार्थ — गुणों से अधिक, उपाध्याय, तपस्वी, शिष्य, दुर्बल, साधुगण, कुल, संघ और मनोज्ञतासहित मुनियों पर आपत्ति के प्रसंग में वैयावृत्ति करना चाहिए।।३९०।।
आचारवृत्ति — गुणाधिक—अपनी अपेक्षा जो गुणों में बड़े हैं, उपाध्याय—श्रुतगुरु, तपस्वी कायक्लेश में तत्पर, शिक्षक—शास्त्र के शिक्षण में तत्पर, दुर्बल—दुःशील अर्थात् दुष्ट परिणाम वाले अथवा व्याधि से पीड़ित, साधुगण—ऋषि, यति, मुनि और अनगार, कुल—गुरुकुल—परम्परा, संघ—चर्तुिवध श्रमण संघ, समनोज्ञ—सुख से आसीन या सर्वोपद्रव से रहित ऐसे साधुओं पर आपत्ति या उपद्रव के आने पर वैयावृत्ति करना चाहिए। विशेष—यहाँ पर कुल का अर्थ गुरुकुल परम्परा से है। तीन पीढ़ी की मुनिपरम्परा को कुल तथा सात पीढ़ी की मुनिपरम्परा को गच्छ कहते हैं। ‘मूलाचार-प्रदीप’ (अध्याय ७, गाथा ६८-६९) के अनुसार, जिस मुनि संघ में आचार्य, उपाध्याय, प्रवत्र्तक, स्थविर और गणाधीश ये पाँच हों उस संघ की कुल संज्ञा है। क्या करके वैयावृत्ति करना चाहिए ? सो ही बताते हैं—
गाथार्थ — वसति, स्थान, आसन तथा उपकरण इनका प्रतिलेखन द्वारा उपकार करना, आहार, औषधि आदि से; मलादि दूर करने से और उनकी वन्दना आदि के द्वारा वैयावृत्ति करना चाहिए।।३९१।।
आचारवृत्ति — शय्यावकाश—मुनियों को वसतिका का दान देना, निषद्या—मुनियों को आसन आदि देना, उपधि—कमण्डलु आदि उपकरण देना, प्रतिलेखन—ापच्छिका आदि देना, इन कार्यों से मुनियों का उपकार करना चाहिए अथवा इनके द्वारा उपकार करके उन्हें स्वीकार करना। आहारचर्या द्वारा, सोंठ, पिप्पल आदि औषधि द्वारा, शास्त्र-व्याख्यान द्वारा, कदाचित् मल-मूत्र आदि च्युत होने पर उसे दूर करने द्वारा और वन्दना आदि के द्वारा वैयावृत्ति करना चाहिए। तात्पर्य यह है कि वसतिका दान, आसनदान, उपकरणदान, प्रतिलेखन आदि के द्वारा पूर्वोक्त साधुओं का उपकार करना चाहिए। इन उपकारों से वे अपने किए जाते हैं। किन स्थानों में उपकार करना ? सो ही बताते हैं— गाथार्थ — मार्ग, चोर, हिंस्रजन्तु, राजा, नदी का रोध और मारी के प्रसंग में, र्दुिभक्ष में, सारक्षण से सहित वैयावृत्ति करना चाहिए।।३९२।।
आचारवृत्ति — मार्ग में चलने से जो थक गए हैं, जिन पर चोरों ने उपद्रव किया है, िंसह-व्याघ्र आदि िंहसक जन्तुओं से जिनको कष्ट हुआ है, राजा ने जिनको पीड़ा दी है, नदी की रुकावट से जिनको बाधा हुई है, अशिव अर्थात् मारी रोग आदि से जो पीड़ित हैं, र्दुिभक्ष से पीड़ित हैं ऐसे साधु यदि अपने संघ में आए हैं तो उनका संग्रह करना चाहिए। जिनका संग्रह किया है उनकी रक्षा करनी चाहिए। इसका ऐसा सम्बन्ध करना अध्वनि श्रान्तस्य।
स्तेनैश्चौरैरुपद्रु तस्य। श्वापदैः सिंहव्याघ्रादिभिः परिभूतस्य। राजभिः खंचितस्य।
नदीरोधेन पीडितस्य। अशिवेन मारिरोगादिव्यथितस्य।
ओमे—र्दुिभक्षपीडितस्य। वैयावृत्यमुक्तं संग्रहसारक्षणोपेतं।
तेषामागतानां संग्रहः कर्तव्यः। संगृहीतस्य रक्षणं कर्तव्यं।
अथचैवं सम्बन्धः कर्तव्यः। एतेषु प्रदेशेषु संग्रहोपेतं सारक्षणोपेतं च वैयावृत्यं कर्तव्यमिति।
अथवा रोधशब्दाः प्रत्येक मभिसम्बध्यते। पथिरोधश्चौररोधः
श्वापदरोधः राजरोधो नदीरोध एतेषु रोधेषु तथा अशिवे र्दुिभक्षे च वैयावृत्यं कर्तव्यमिति।।३९२।।
स्वाध्यायस्वरूपमाह—परियट्टणाय वायण पडिच्छणाणुपेहणा य धम्मकहा।
थुदिमंगलसंजुत्तो पंचविहो होइ सज्झाओ।।३९३।।
परिवर्तनं पठितस्य ग्रन्थस्यानुवेदनं। वाचना शास्त्रस्य व्याख्यानं।
पृच्छना शास्त्रश्रवणं। अनुप्रेक्षा द्वादशानुप्रेक्षाऽनित्यत्वादि।
धर्मकथा त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरितानि। स्तुतिर्मुनिदेववन्दना
मंगल इत्येवं संयुक्तः पंचप्रकारो भवति स्वाध्यायः। परिवर्तनमेको
वाचना द्वितीयः पृच्छना तृतीयोऽनुप्रेक्षा चतुर्थो धर्मकथास्तुतिमंगलानि
समुदितानि पंचमः प्रकारः। एवं पंचविधः स्वाध्यायः सम्यग्युक्तोेऽनुष्ठेय इति।।३९३।।
ध्यानस्वरूपं विवृण्वन्नाह—अट्टं च रुद्दसहियं दोण्णिवि झाणाणि
अप्पसत्थाणि। धम्मं सुक्क च दुवे पसत्थझाणाणि णेयाणि।।३९४।।
आर्तध्यानं रौद्रध्यानेन सहितं। एते द्वे ध्याने अप्रशस्ते
नरकतिर्यग्गतिप्रापके। धर्मध्यानं शुक्लध्यानं चैते द्वे प्रशस्ते
देवगतिमुक्तिगतिप्रापके। इत्येवंविधानि ज्ञातव्यानि।
एकाग्रचिन्तानिरोधो ध्यानमिति।।३९४।।
आर्तध्यानस्य भेदानाह—अमणुण्णजोगइट्ठविओगपरीसहणिदाणकरणेसु।
अट्टं कसायसहियं झाणं भणिदं समासेण।।३९५।।
अमनोज्ञेन ज्वरशूलशत्रुरोगादिना योगः सम्पर्क। इष्टस्य
पुत्रदुहितृमातृपितृबन्धु-शिष्यादिकस्य वियोगोऽभावः।
परीषहाः सुत्तृट्छीतोष्णादयः। निदानकरणं इहलोकपरलोकभोगविषयोऽभिलाषः।
इत्येतेषु प्रदेशेष्वार्तमनःसंक्लेशः कषायसहितं ध्यानं भणितं
समासेन संक्षेपतः। कदा ममानेनामनोज्ञेन वियोगो भविष्यतीत्येव
कि इन स्थानों में संग्रह से सहित और उनकी रक्षा से सहित वैयावृत्य करना चाहिए। अथवा रोध शब्द को प्रत्येक के साथ लगाना चाहिए। जैसे मार्ग में जिन्हें रोका गया हो, चोरों ने रोक लिया है, हिंस्र जन्तुओं ने रोक लिया हो, राजा ने रुकावट डाली हो, नदी से रुकावट हुई हो तो ऐसे रोध के प्रसंग में तथा दुःख में र्दुिभक्ष में वैयावृत्ति करना चाहिए। स्वाध्याय का स्वरूप कहते हैं—
गाथार्थ — परिवर्तन, वाचना, पृच्छना, अनुप्रेक्षा और धर्मकथा तथा स्तुति-मंगल संयुक्त पाँच प्रकार का स्वाध्याय करना चाहिए।।३९३।।
आचारवृत्ति — पढ़े हुए ग्रन्थ को पुनः-पुनः पढ़ना या रटना परिवर्तन है। शास्त्र का व्याख्यान करना वाचना है। शास्त्र का श्रवण करना पृच्छना है। अनित्यत्व आदि बारह प्रकार की अनुप्रेक्षाओं का चिंतवन करना अनुप्रेक्षा है। त्रेसठ शलाकापुरुषों के चरित्र पढ़ना धर्मकथा है।
स्तुति—मुनि वन्दना, देव-वन्दना, और मंगल इनसे संयुक्त स्वाध्याय पाँच प्रकार का होता है। तात्पर्य यह है कि (१) परिवर्तन, (२) वाचना, (३) पृच्छना, (४) अनुप्रेक्षा और (५) समूहरूप धर्मकथा स्तुतिमंगल—इन पाँच प्रकार के स्वाध्याय का सम्यक प्रकार से अनुष्ठान करना चाहिए। ध्यान का स्वरूप वर्णन करते हैं—
गाथार्थ — आर्त और रौद्र सहित दो ध्यान अप्रशस्त हैं। धर्म और शुक्ल ये दो प्रशस्त ध्यान हैं ऐसा जानना चाहिए।।३९४।।
आचारवृत्ति — आर्तध्यान और रौद्र ध्यान ये दो ध्यान अप्रशस्त हैं। ये नरकगति और तिर्यंचगति को प्राप्त कराने वाले हैं। धर्मध्यान और शुक्लध्यान ये दो प्रशस्त हैं। ये देवगति और मुक्ति को प्राप्त कराने वाले हैं, ऐसा समझना। एकाग्रचिन्तानिरोध—एक विषय पर चिन्तन का रोक लेना यह ध्यान का लक्षण है। आर्तध्यान के भेदों को कहते हैं—
गाथार्थ — अनिष्ट का योग, इष्ट का वियोग, परीषह और निदानकरण इनमें कषाय सहित जो ध्यान है वह संक्षेप से आर्तध्यान कहा गया है।।३९५।।
आचारवृत्ति — अमनोज्ञयोग—ज्वर, शूल, शत्रु, रोग आदि का सम्पर्क होना, इष्ट वियोग—पुत्र, पुत्री, माता, पिता, बन्धु, शिष्य आदि का वियोग होना, परिषह—क्षुधा, तृषा, शीत, उष्ण आदि बाधाओं का होना; निदान—इस लोक या परलोक में भोग-विषयों की अभिलाषा करना। इन स्थानों में जो आर्त अर्थात् मन का संक्लेश होता है वह कषाय सहित ध्यान आर्तध्यान कहलाता है। इनका वर्णन यहाँ संक्षेप से किया गया है। जैसे—कब मेरा इस अनिष्ट से वियोग होगा इस प्रकार से चिन्तन करना चिन्तनमार्तध्यानं प्रथमं।
इष्टैः सह सर्वदा यदि मम संयोगो भवति वियोगो न कदाचिदपि
स्वाद्यद्येवं चिन्तनमार्तध्यानं द्वितीयं। क्षुत्तृटछीतोष्णादिभिरहं
व्यथितः कदैतेषां ममाभावः स्यात्। कथं मयौदनादयो लभ्या
येन मम क्षुधादयो न स्युः। कदा मम वेलायाः प्राप्तिः स्याद्येनाहं भुंजे
पिबामि वा। हाकारं पूत्कारं जलसेकं च कुर्वतोऽपि न तेन मम प्रतीकार
इति चिन्तनमार्तध्यानं तृतीयमिति। इहलोके यदि मम पुत्राः स्युः परलोके
यद्यहं देवो भवामि स्त्रीवस्त्रादिकं मम स्यादित्येवं चिन्तनं चतुर्थमार्तध्यानमिति।।३९५।।
रौद्रध्यानस्वरूपं प्रतिपादयन्नाह—तेणिक्कमोससारक्खणेसु तध चेव छव्विहारंभे।
रुद्दं कसायसहिदं झाणं भणियं समासेण।।३९६।।
स्तैन्यं परद्रव्यापहरणाभिप्रायः। मृषाऽनृते तत्परता।
सारक्षणं यदि मदीयं द्रव्यं चोरयति तमहं निहन्मि, एवमायुधव्यग्रहस्तमारणाभिप्रायः।
स्तैन्यमृषावादसारक्षणेषु। तथा चैव षड्विधारम्भे पृथिव्यप्तेजोवायुवनस्पतित्रसकायिकविराधने
च्छेदनभेदन-वधता-डनदहनेषूद्यमः रौद्रं कषायसहितं ध्यानं भणितं।
समासेन संक्षेपेण। परद्रव्यहरणे तत्परता प्रथमं रौद्रं। परपीडाकरे मृषावादे
यत्नः द्वितीयं रौद्रं। द्रव्यपशुपुत्रादिरक्षणविषये चौरदायादिमारणोद्यमे
यत्नस्तृतीयं रौद्रं। तथा षड्विधे जीवमारणारम्भे कृताभिप्रायश्चतुर्थं रौद्रमिति।।३९७।।
ततः—अवहट्टु अट्टरुद्दे महाभए सुग्गदीयपच्चूहे।
धम्मे वा सुक्के वा होहि समण्णागदमदीओ।।३९७।।
यत एवंभूते आर्तरौद्रे। िंकविशिष्टे, महाभये महासंसारभीतिदायिनि (नी)
सुगतिप्रत्यूहे—देवगतिमोक्षगतिप्रतिवूâले। अपहृत्य निराकृत्य।
धर्मध्याने शुक्लध्याने वा भव सम्यग्विधानेन गतमतिः।
धर्मध्याने शुक्लध्याने च सादरो सुष्ठु विशुद्धं मनो विधेहि समाहितमतिर्भवेति।।३९७।।
पहला आर्तध्यान है। इष्टजनों के साथ यदि मेरा संयोग होता है तो कदाचित् भी वियोग न होवे ऐसा चिन्तन होना दूसरा आर्तध्यान है। क्षुधा, तृषा आदि के द्वारा मैं पीड़ित हो रहा हूँ, मुझसे कब इनका अभाव होवे ? मुझे कैसे भात—भोजन आदि प्राप्त होवें कि जिससे मुझे क्षुधा आदि बाधाएँ न होवें ? कब मेरे आहार की बेला आवे कि जिससे मैं भोजन करूँ अथवा पानी पिऊँ ? हाहाकार या पूत्कार और जल-सिञ्चन आदि करते हुए भी उन बाधाओं से मेरा प्रतीकार नहीं हो रहा है अर्थात् घबराने से, हाय-हाय करने से, पानी छिड़कने से भी प्यास आदि बाधाएँ दूर नहीं हो रही हैं इत्यादि प्रकार से चिन्तन करना तीसरे प्रकार का आर्तध्यान है। इस लोक में यदि मेरे पुत्र हो जावें, परलोक में यदि मैं देव हो जाऊँ तो ये स्त्री, वस्त्र आदि मुझे प्राप्त हो जावें इत्यादि चिन्तन करना चौथा आर्तध्यान है। रौद्रध्यान का स्वरूप प्रतिपादित करते हुए कहते हैं—
गाथार्थ — चोरी, असत्य, परिग्रहसंरक्षण और छह प्रकार की जीविंहसा के आरम्भ में कषाय सहित होना रौद्रध्यान है, ऐसा संक्षेप से कहा है।।३९६।।
आचारवृत्ति — स्तैन्य—परद्रव्य के हरण का अभिप्राय होना, मृषा—असत्य बोलने में तत्पर होना, सारक्षण—यदि मेरा द्रव्य कोई चुराएगा तो मैं उसे मार डालूँगा, इस प्रकार से आयुध को हाथ में लेकर मारने का अभिप्राय करना, षड्विधानारम्भ—पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति और त्रस इन षट्कायिक जीवों की विराधना करने में, इनका छेदन-भेदन करने में, इनको बाँधने में, इनका वध करने में, इनका ताड़न करने में और इन्हें जला देने में उद्यम का होना अर्थात् इन जीवों को पीड़ा देने में उद्यत होना, कषाय सहित ऐसा ध्यान रौद्र कहलाता है। यहाँ पर इसका संक्षेप से कथन किया गया है। तात्पर्य यह है कि परद्रव्य के हरण करने में तत्पर होना प्रथम रौद्रध्यान है। पर को पीड़ा देने वाले असत्य वचन के बोलने में यत्न करना दूसरा रौद्रध्यान है। द्रव्य अर्थात् धन, पशु, पुत्रादि के रक्षण के विषय में, चोर, दायाद अर्थात् भागीदार आदि के मारने में प्रयत्न करना यह तीसरा रौद्रध्यान है और छह प्रकार के जीवों के मारने के आरम्भ में अभिप्राय रखना यह चौथा रौद्रध्यान है।
विशेष—इन्हीं ध्यानों के हिंसानन्दी, मृषानन्दी, चौर्यानन्दी और परिग्रहानन्दी ऐसे नाम भी अन्य ग्रन्थों में पाए जाते हैं। जिसका अर्थ है हिंसा में आनन्द मानना, झूठ में आनन्द मानना, चोरी में आनन्द मानना और परिग्रह के संग्रह में आनन्द मानना। यह ध्यान रुद्र अर्थात् क्रूर परिणामों से होता है। इसमें कषायों की तीव्रता रहती है अतः इसे रौद्रध्यान कहते हैं। इसके बाद—क्या करना ? सो कहते हैं—
गाथार्थ — सुगति के रोधक महाभयरूप इन आर्त, रौद्रध्यान को छोड़कर धर्मध्यान में अथवा शुक्लध्यान में एकाग्रबुद्धि करो।।३९७।।
आचारवृत्ति — महासंसार भय को देने वाले और देवगति तथा मोक्षगति के प्रतिवूâल ऐसे इन आर्तध्यान और रौद्रध्यान को छोड़कर धर्मध्यान, शुक्लध्यान में अच्छी तरह अपनी मति लगाओ अर्थात् धर्म और शुक्लध्यान में आदर सहित होकर अच्छी तरह अपने विशुद्ध मन को लगाओ, उन्हीं में
एकाग्रबुद्धि को करो। धर्मध्यानभेदान् प्रतिपादयन्नाह—एयग्गेण मणं
णिरुंभिऊण धम्मं चउव्विहं झाहि। आणापायविवायविचओ य संठाणविचयं च।।३९८।।
एकाग्रेण पंचेन्द्रियव्यापारपरित्यागेन कायिकवाचिकव्यापारविरहेण च।
मनो मानसव्यापारं। निरुध्यात्मवशं कृत्वा। चर्तुिवधं चतुर्भेदं।
ध्याय चिन्तय। के ते चत्वारो विकल्पा इत्याशंकायामाह—
आज्ञाविचयोऽपायविचयो विपाकविचयः संस्थानविचयश्चेति।।३९८।।
तत्राज्ञाविचयं विवृण्वन्नाह—पंचत्थिकायछज्जीवणिकाये कालदव्वमण्णे य।
आणागेज्झे भावे आणाविचयेण विचिणादि।।३९९।।
पंचास्तिकायाः जीवास्तिकायोऽजीवास्तिकायो धर्मास्तिकायोऽधर्मास्तिकायो
वियदास्तिकाय इति तेषां प्रदेशबन्धोऽस्तीति कृत्वा काया इत्युच्यन्ते।
षड्जीवनिकायश्च पृथिव्यप्तेजोवायुवनस्पतित्रसाः। कालद्रव्यमन्यत्।
अस्य प्रदेशबन्धाभावादस्तिकायत्वं नास्ति। एतानाज्ञाग्राह्यान् भावान् पदार्थान्।
आज्ञाविचयेनाज्ञास्वरूपेण। विचिनोति विवेचयति ध्यायतीति यावत्।
एते पदार्थाः सर्वज्ञनाथेन वीतरागेण प्रत्यक्षेण दृष्टा न कदाचिद्
व्यभिचरन्तीत्यास्तिक्यबुध्द्या तेषां पृथक्पृथग्विवेचनेनाज्ञाविचयः।
यद्यप्यात्मनः प्रत्यक्षबलेन हेतुबलेन वा न स्पष्टा तथापि
सर्वज्ञाज्ञानिर्देशन गृह्वाति नान्यथावादिनो जिना यत इति।।३९९।।
अपायविचयं विवृण्वन्नाह—कल्लाणपावगाओ पाए विचिणादि
जिणमदमुविच्च। विचिणादि वा अपाये जीवाण सुहे य असुहे य।।४००।।
कल्याणप्रापकान् पंचकल्याणानि यैः प्राप्यन्ते तान् प्राप्यान्
सम्यग्दर्शनज्ञान- चारित्राणि। विचिनोति ध्यायति।
जिनमतमुपेत्य जैनागममाश्रित्य। विचिनोति वा ध्यायति
धर्मध्यान के भेदों को कहते हैं—
गाथार्थ — एकाग्रतापूर्वक मन को रोककर उस धर्म का ध्यान करो जिसके आज्ञाविचय, अपायविचय, विपाकविचय और संस्थानविचय ये चार भेद हैं।।३९८।।
आचारवृत्ति — पंचेन्द्रिय विषयों के व्यापार का त्याग करके और कायिक, वाचिक व्यापार से भी रहित होकर, एकाग्रता से मानस व्यापार को रोककर अर्थात् मन को अपने वश में करके चार प्रकार के धर्मध्यान का चिन्तवन करो। वे चार भेद कौन हैं? ऐसी आशंका होने पर कहते हैं—आज्ञाविचय, अपायविचय, विपाकविचय और संस्थानविचय ये चार भेद धर्मध्यान के हैं।
भावार्थ — यहाँ एकाग्रचिन्तानिरोध लक्षण वाला ध्यान कहा गया है। पंचेन्द्रियों के विषय का छोड़ना और काय की तथा वचन की क्रिया नहीं करना ‘एकाग्र’ है तथा मन का व्यापार रोकना चिन्तानिरोध है। इस प्रकार से ध्यान के लक्षण में इन्द्रियों के विषय से हटकर तथा मन-वचन-काय की प्रवृत्ति से छूटकर जब मन अपने किसी ध्येय विषय में टिक जाता है, रुक जाता है, स्थिर हो जाता है उसी को ध्यान यह संज्ञा आती है।
गाथार्थ — उसमें से पहले आज्ञाविचय का वर्णन करते हैं—पाँच अस्तिकाय, छह जीवनिकाय और कालद्रव्य ये आज्ञा से ग्राह्य पदार्थ हैं। इनको आज्ञा के विचार से चिन्तवन करना है।।३९९।।
आचारवृत्ति — जीवास्तिकाय, अजीवास्तिकाय, (पुद्गलास्तिकाय) धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय और आकाशास्तिकाय ये पाँच अस्तिकाय हैं। इन पाँचों में प्रदेश का बन्ध अर्थात् समूह विद्यमान है अतः इन्हें काय कहते हैं। पृथिवी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति और त्रस ये षट्जीवनिकाय हैं। और अन्य—छठा कालद्रव्य है। इसमें प्रदेशबन्ध का अभाव होने से यह अस्तिकाय नहीं है अर्थात् काल एकप्रदेशी होने से अप्रदेशी कहलाता है इसलिए यह ‘अस्ति’ तो है किन्तु काय नहीं है। ये सभी पदार्थ जिनेन्द्रदेव की आज्ञा से ग्रहण करने योग्य होने से आज्ञाग्राह्य हैं। आज्ञाविचय से अर्थात् आज्ञारूप से इनका विवेचन करना—ध्यान करना आज्ञाविचय है। तात्पर्य यह है कि वीतराग सर्वज्ञदेव ने इन पदार्थों को प्रत्यक्ष से देखा है। ये कदाचित् भी व्यभिचरित नहीं होते हैं अर्थात् ये अन्यथा नहीं हो सकते हैं। इस प्रकार से आस्तिक्य बुद्धि के द्वारा उनका पृथव्-पृथव् विवेचन करना, चिन्तवन करना यह आज्ञाविचय धर्मध्यान है। यद्यपि ये पदार्थ स्वयं को प्रत्यक्ष से या तर्क के द्वारा स्पष्ट नहीं हैं फिर भी सर्वज्ञ की आज्ञा के निर्देश से वह उनको ग्रहण करता है; क्योंकि ‘नान्यथावादिनो जिनाः’ जिनेन्द्रदेव अन्यथावादी नहीं हैं। अपायविचय का वर्णन करते हैं—
गाथार्थ — जिनमत का आश्रय लेकर कल्याण को प्राप्त कराने वाले उपायों का चिन्तन करना अथवा जीवों के शुभ और अशुभ का चिन्तन करना अपायविचय है।।४००।।
आचारवृत्ति — जिनके द्वारा पंचकल्याणक प्राप्त किए जाते हैं वे सम्यग्दर्शन और चारित्र प्राप्य हैं अर्थात् उपायभूत हैं।
जैनागम का आश्रय लेकर इनका ध्यान करना वा।
अपायान् कर्मापगमान् स्थितिखण्डाननुभागखण्डानुत्कर्षापकर्षभेदान्।
जीवानां सुखानि जीवप्रदेशसंतर्पणानि। असुखानि दुःखानि
चात्मनस्तु विचिनोति भावयतीति। एतैः कर्तव्यैर्जीवा दूरतो भवन्ति शासनात्,
एतैस्तु शासनमुपढौकते, एतैः परिणामैः संसारे भ्रमन्ति जीवाः,
एतश्च संसाराद्विमुञ्चन्तीति चिन्तनमपायचिन्तनं नाम द्वितीयं धर्मध्यानमिति।।४००।।
विपाकविचयस्वरूपमाह—एआणेयभवगयं जीवाणं पुण्णपावकम्मफलं।
उदओदीरणसंकमबंधंमोक्खं च विचिणादि।।४०१।।
एकभवगतमनेकभवगतं च जीवानां पुण्यकर्मफलं पापकर्मफलं च विचिनोति।
उदयं स्थितिक्षयेण गलनं विचिनोति ये कर्मस्कन्धा उत्कर्षापकर्षादिप्रयोगेण
स्थितिक्षयं प्राप्यात्मनः फलं ददते तेषां कर्मस्कन्धानामुदय इति संज्ञा
तं ध्यायति। तथा चोदीरणमपक्वपाचनं। ये कर्मस्कन्धाः सत्सु
स्थित्यनुभागेषु अवस्थिताः सन्त आकृष्याकाले फलदाः क्रियन्ते तेषां
कर्मस्कन्धानामुदीरणमिति संज्ञा तद् ध्यायति।
संक्रमणं परप्रकृतिस्वरूपेण गमनं विचिनोति।
तथा बन्धं जीवकर्मप्रदेशान्योन्यसंश्लेषं ध्यायति।
मोक्षं जीवकर्मप्रदेशविश्लेषमनन्तज्ञानदर्शनसुखवीर्यस्वरूपं विचिनोतीति सम्बन्धः।
तथा शुभ प्रकृतीनां गुडखण्डशर्करामृतस्वरूपेणानुभागचिन्तनम्
अशुभप्रकृतीनां निम्बकांजीरविषहालाहलस्वरूपेणानुभागचिन्तनम्
अशुभप्रकृतीनां निम्बकांजीर विषहालाहल स्वरूपेणानुभागचिन्तनम्
तथा घातिकर्मणां लतादार्वस्थिशिलास मानानुिंचतनं।
नरवतिर्यग्मनुष्यदेवगतिप्रापककर्मफलचिन्तनं
इत्येवमादिचिन्तनं विपाकविचयधम्र्यध्यानं नामेति।।४०१।।
संस्थानविचयस्वरूपं विवृण्वन्नाह—उड्ढमहतिरियलोए
विचिणादि सपज्जए ससंठाणे।
एत्थेव अणुगदाओ अणुपेक्खाओ य विचिणादि।।४०२।।
ऊध्र्वलोकं सपर्ययं सभेदं संस्थानं त्र्यस्रचतुरस्रवृत्तदीर्घायतमृदंगसंस्थानं
पटलेन्द्रकश्रेणीबप्रकीर्णकविमानभेदभिन्नं विचिनोति ध्यायति।
तथाधोलोवंâ सपर्ययं ससंस्थानं वेत्रासनाद्याकृतिं
त्र्यस्रचतुरस्रवृत्तदीर्घायतादिसंस्थानभेदभिन्नं सप्तपृथिवीन्द्र-
उपायविचय धर्मध्यान है; जीव के प्रदेशों को संतर्पित करने वाला सुख है और आत्मा के प्रदेशों में पीड़ा उत्पन्न करने वाला दुःख है। इस तरह से जीवों के सुख और दुःख का चिन्तवन करना अर्थात् जीव इन कार्यों के द्वारा जिनशासन से दूर हो जाते हैं और इन शुभ कार्यों के द्वारा जिनशासन के निकट आते हैं, उसे प्राप्त कर लेते हैं। या इन परिणामों से संसार में भ्रमण करते हैं और इन परिणामों से संसार से छूट जाते हैं। इस प्रकार से चिन्तवन करना यह अपायविचय नाम का दूसरा धर्मध्यान है।
भावार्थ — कल्याण के लिए उपायभूत रत्नत्रय का चिन्तवन करना उपायविचय तथा कर्मों के अपाय—अभाव का चिन्तवन करना अपायविचय है। अब विपाकविचय का स्वरूप कहते हैं— गाथार्थ — जीवों के एक और अनेक भव में होने वाले पुण्य-पाप कर्म के फल को तथा कर्मों के उदय, उदीरणा, बन्ध और मोक्ष को जो ध्याता है उसके विपाकविचय धर्मध्यान होता है।।४०१।।
आचारवृत्ति — मुनि विपाकविचय धम्र्यध्यान में जीवों के एक भव में होने वाले या अनेक भव में होने वाले पुण्यकर्म के और पापकर्म के फल का चिन्तन करते हैं। कर्मों के उदय का विचार करते हैं। स्थिति के क्षय से गलन होना उदय है अर्थात् जो कर्मस्कन्ध उत्कर्षण या अपकर्षण आदि प्रयोग द्वारा स्थिति क्षय को प्राप्त करके आत्मा को फल देते हैं उन कर्मस्कन्धों की उदय यह संज्ञा है। वे जीवों के कर्मोदय का विचार करते हैं। अपक्वपाचन को उदीरणा कहते हैं अर्थात् जो कर्मस्कन्ध स्थिति और अनुभाग के अवशेष रहते हुए विद्यमान हैं उनको खींच करके जो अकाल में ही उन्हें फल देने वाला कर लेना है सो उदीरणा है अर्थात् प्रयोग के बल से अकाल में ही कर्मों को उदयावली में ले आना उदीरणा है। इसका ध्यान करते हैं। किसी प्रकृति का पर-प्रकृतिरूप से होना बन्ध है। जीव और कर्म के प्रदेशों का पृथक्करण होकर अनन्तज्ञान, अनन्तदर्शन, अनन्तसुख और अनन्तवीर्य स्वरूप को प्राप्त हो जाना मोक्ष है। इस संक्रमण का, बंध और मोक्ष का चिन्तवन करते हैं। उसी प्रकार से शुभ प्रकृतियों के गुड़, खांड, शर्करा और अमृत रूप अनुभाग का चिन्तवन करना तथा अशुभ प्रकृतियों का नीम, कांजीर, विष और हालाहलरूप अनुभाग का विचार करना तथा घातिकर्मों का लता, दारू, हड्डी और शिला के समान अनुभाग है ऐसा सोचना नरकगति, तिर्यंचगति, मनुष्यगति और देवगति को प्राप्त कराने वाले ऐसे कर्मों के फल का चिन्तन करना इत्यादि प्रकार से जो भी कर्मसम्बन्धी चिन्तन करना है, यह सब विपाकविचय नाम का धर्मध्यान है। संस्थानविचय का स्वरूप कहते हैं—
गाथार्थ — भेदसहित और आकार सहित ऊध्र्व, अधः और तिर्यग्लोक का ध्यान करते हैं और इसी से सम्बन्धित द्वादश अनुप्रेक्षा का भी विचार करते हैं।।४०२।।
कश्रेणिविश्रेणिबद्धप्रकीर्णकप्रस्तरस्वरूपेण स्थितं शीतोष्णनारकसहितं
महावेदनारूपं च विचिनोति। तथा तिर्यग्लोकं सपर्ययं सभेदं
ससंस्थानं झल्लर्याकारं मेरुकुलपर्वतादि ग्रामनगरपत्तनभेदभिन्नं
पूर्वविदेहापरविदेहभरतैरावतभोगभूमिद्वीपसमुद्रवननदीवेदिकाय-
तनकूटादिभेदभिन्नं दीर्घह्रस्ववृत्तायतत्र्यराचतुरस्रसंस्थानसहितं
विचिनोति ध्यायतीति सम्बन्धः। अत्रैवानुगता अनुप्रेक्षा द्वादशानुप्रेक्षा विचिनोति।।४०२।।
कस्ता अनुप्रेक्षा इति नामानीति दर्शयन्नाह—अद्धुवमसरणमेगत्तमण्ण
संसारलोगमसुचित्तं। आसवसंवरणिज्जर धम्मं बोिंध च िंचतिज्जो।।४०३।।
अध्रुवमनित्यता। अशरणमनाश्रयः। एकत्वमेकोऽहं। अन्यत्वं शरीरादन्योऽहं।
संसारश्चतुर्गतिसंक्रमणं। लोक ऊध्र्वाधोमध्यवेत्रासनझल्लरीमृदंगरूपश्चतुर्दश-रज्जवायतः।
अशुचित्वं। आस्रवः कर्मास्रवः। संवरो महाव्रतादिकं। निर्जरा कर्मसातनं।
धर्मोऽपि दशप्रकारः क्षमादिलक्षणः। बोधिं च सम्यक्त्वसहिता भावना
एता द्वादशानुप्रेक्षाश्चिन्तय। तत् एतच्चर्तुिवधं धर्मध्यानं नामेति।।४०३।।
शुक्लध्यानस्य स्वरूपं भेदांश्च विवेचयन्नाह—उवसंतो दु पुहुत्तं झायदि
झाणं विदक्कवीचारं। खीणकसाओ झायदि एयत्तविदक्कवीचारं।।४०४।।
उपशान्तकषायस्तु पृथक्त्वं ध्यायति ध्यानं। द्रव्याण्यनेकभेदभिन्नानि
त्रिभियोगैर्यतो ध्यायति ततः पृथक्त्वमित्युच्यते। वितर् श्रुतं
यस्माद्वितर्वेण श्रुतेन सह वर्तते यस्माच्च नवदशचतुर्दशपूर्वधरैरारभ्यते
तस्मात्सवितर्वक तत्। विचारोर्थव्यंजनयोगः (ग) संक्रमणः।
एकमर्थं त्यक्त्वार्थान्तरं ध्यायति मनसा संचित्य वचसा प्रवर्तते कायेन प्रवर्तते एव
आचारवृत्ति — ऊध्र्वलोक पर्याय सहित अर्थात् भेदों सहित तथा आकार सहित—त्रिकोण, चतुष्कोण, गोल, दीर्घ, आयत और मृदंग के आकार वाला है। इसमें पटलों में इन्द्रक, श्रेणीबद्ध और प्रकीर्णक विमानों से अनेक भेद हैं। इसका मुनि ध्यान करते हैं। अधोलोक भी भेद सहित और वेत्रासन आदि आकार सहित है। त्रिकोण, चतुष्कोण, गोल, दीर्घ आदि आकार इसमें भी घटित होते हैं। इसमें सात पृथिवियाँ हैं। इन्द्रक, श्रेणी, विश्रेणीबद्ध और प्रकीर्णक प्रस्तार हैं। कुछ नरकबिल शीत हैं और कुछ उष्ण हैं। ये महावेदनारूप हैं इत्यादि का ध्यान करना। उसी प्रकार से तिर्यग्लोक भी नाना भेदों सहित और अनेक आकृति वाला है, झल्लरी के समान है, मेरु पर्वत, कुलपर्वत आदि तथा ग्राम, नगर, पत्तन आदि से भेद सहित है। पूर्वविदेह, अपरविदेह, भरत, ऐरावत, भोगभूमि, द्वीप, समुद्र, वन, नदी, वेदिका, आयतन और कूटादि से युक्त है। दीर्घ, ह्रस्व, गोल, आयत, त्रिकोण, चतुष्कोण आकारों से सहित है। मुनि इसका भी ध्यान करते हैं अर्थात् मुनि तीनों लोक सम्बन्धी जो कुछ आकार आदि का चिन्तवन करते हैं वह सब संस्थानविचय धर्मध्यान है और इन्हीं के अन्तर्गत द्वादश अनुप्रेक्षाओं का भी चिन्तवन करते हैं। उन अनुप्रेक्षाओं के नाम बताते हैं— गाथार्थ — अध्रुव, अशरण, एकत्व, अन्यत्व, संसार, लोक, अशुचि, आस्रव, संवर, निर्जरा, धर्म और बोधि इनका चिन्तवन करना चाहिए।।४०३।।
आचारवृत्ति — अध्रुव—सभी वस्तुएँ अनित्य हैं। अशरण—कोई आश्रयभूत नहीं है। एकत्व—मैं अकेला हूँ। अन्यत्व—मैं शरीर से भिन्न हूँ। संसार—चतुर्गति में संसरण करना—भ्रमण करना ही संसार है। लोक—यह ऊध्र्व, अधः और मध्यलोक की अपेक्षा वेत्रासन, झल्लरी और मृदंग के आकार का है और चौदह राजू ऊँचा है। अशुचि—शरीर अत्यन्त अपवित्र है। आस्रव—कर्मों का आना आस्रव है। संवर—महाव्रत आदि से आते हुए कर्म रुक जाते हैं। निर्जरा—कर्मों का झड़ना निर्जरा है। धर्म—उत्तम क्षमा आदि लक्षणरूप धर्म दश प्रकार का है। बोधि—सम्यक्त्व सहित भावना ही बोधि है। इस प्रकार से इन द्वादश अनुप्रेक्षाओं का चिन्तवन करना चाहिए। शुक्लध्यान का स्वरूप और उसके भेदों को कहते हैं—
गाथार्थ — उपशान्तकषाय मुनि पृथक्त्ववितर्वâवीचार नामक शुक्लध्यान को ध्याते हैं। क्षीणकषाय मुनि एकत्ववितर्व अवीचार नामक ध्यान करते हैं।।४०४।।
आचारवृत्ति — उपशान्तकषाय नामक ग्यारहवें गुणस्थानवर्ती मुनि पृथक्त्ववितर्व-वीचार ध्यान को ध्याते हैं। जीवादि द्रव्य अनेक भेदों से सहित हैं, मुनि इनको मन, वचन और काय इन तीनों योगों के द्वारा ध्याते हैं इसलिए इस ध्यान का पृथक्त्व यह सार्थक नाम है। श्रुत को वितर्व कहते हैं।
वितर्व—श्रुत के साथ रहता है अर्थात् नवपूर्वधारी, दशपूर्वधारी या चतुर्दश पूर्वधरों के द्वारा प्रारम्भ किया जाता है इसलिए वह वितर्क कहलाता है। अर्थ, व्यंजन और योगों के संक्रमण का नाम वीचार है अर्थात् जो एक अर्थ—पदार्थ को छोड़कर भिन्न अर्थ का ध्यान करता है, मन से चिन्तवन करके वचन से करता है, पुनः काययोग से ध्याता है। इस तरह परम्परा से योगों का संक्रमण होता है अर्थात् द्रव्यों का संक्रमण होता है और व्यंजन अर्थात् पर्यायों का संक्रमण होता है। पर्यायों में स्थूल पर्यायें व्यंजन पर्याय हैं और जो वचन के अगोचर सूक्ष्म पर्याय हैं वे अर्थ पर्यायें कहलाती हैं। इनका संक्रमण इस ध्यान में होता है इसलिए यह ध्यान
परंपरेण संक्रमो योगानां द्रव्याणां व्यंजनानां च स्थूलपर्यायाणामर्थानां
सूक्ष्मपर्यायाणां वचनगोचरातीतानां संक्रमः सवीचारं यानमिति।
अस्य त्रिप्रकारस्य ध्यानस्योपशान्त-कषायः स्वामी। तथा क्षीणकषायो
ध्यायत्येकत्वं वितर्वâमवीचारं। एकं द्रव्यमेकार्थपर्याय- मेकं
व्यंजनपर्यायं च योगनैकेन ध्यायति तद्ध्यानमेकत्वं, वितर्क श्रुतं पूर्वोक्तमेव,
अवीचारं अर्थव्यंजनयोगसंक्रान्तिरहितं। अस्य
त्रिप्रकारस्यैकत्ववितर्कतवीचारभेदभिन्नस्य क्षीणकषायः स्वामी।।४०४।।
तृतीयचतुर्थशुक्लध्यानस्वरूपप्रतिपादनार्थमाह—सुहुसकिरियं सजोगी
झायदि झाणं च तदियसुक्कंतु। जं केवली अजोगी झायदि झाणं समुच्छिण्णं।।४०५।।
सूक्ष्मक्रियामवितर्कमवीचारं श्रुतावष्टम्भरहितमर्थव्यञ्जनयोगसंक्रान्तिवियुक्तं
सूक्ष्मकायक्रियाव्यवस्थितं तृतीयं शुक्लं सयोगी ध्यायति ध्यानमिति।
यत्कैवल्ययोगी ध्यायति ध्यानं तत्समुच्छिन्नमवितर्कमविचारमनिवृत्तिनिरुद्धयोगमपश्चिमं
शुक्लमविचलं मणिशिखावत्। तस्य चतुर्थध्यानस्यायोगी स्वामी। यद्यप्यत्र
मानसो व्यापारो नास्ति तथाप्युपचारक्रिया ध्यानमित्युपचर्यते।
पूर्वप्रवृत्तिमपेक्ष्य घृतघटवत् पुंवेदवद्वेति।।४०५।।
व्युत्सर्गनिरूपणायाह—दुविहो य विउस्सग्गो अब्भंतर बाहिरो
मुणेयव्वो। अब्भंतर कोहादी बाहिर खेत्तादियं दव्वं।।४०६।।
द्विविधो द्विप्रकारो व्युत्सर्गः परिग्रहपरित्यागोऽभ्यन्तरवाहिरो
अभ्यन्तरो बाह्यश्च ज्ञातव्यः। क्रोधादीनां व्युत्सर्गोभ्यन्तरः
क्षेत्रादिद्रव्यस्य त्यागो बाह्यो व्युत्सर्ग इति।।४०६।।
वीचार सहित है अतः इसका सार्थक नाम पृथक्त्ववितर्कवीचार है। इस ध्यान में तीन प्रकार हो जाते हैं अर्थात् पृथक्त्व—नाना भेदरूप द्रव्य, वितर्क—श्रुत और वीचार—अर्थ व्यंजन, योग का संक्रमण इन तीनों की अपेक्षा से यह ध्यान तीन प्रकार रूप है। इस ध्यान के स्वामी उपशान्तकषायी महामुनि हैं। क्षीणकषायगुणस्थान वाले मुनि एकत्ववितर्व अवीचार ध्यान को ध्याते हैं। वे एक द्रव्य को अथवा एक अर्थपर्याय को या एक व्यंजन पर्याय को किसी एक योग के द्वारा ध्याते हैं अतः यह ध्यान एकत्व कहलाता है। इसमें वितर्क—श्रुत पूर्वकथित ही है अर्थात् नव, दश या चतुर्दश पूर्वों के वेत्ता मुनि ही ध्याते हैं। अर्थ, व्यंजन और योगों की संक्रान्ति से रहित होने से यह ध्यान अवीचार है। इसमें भी एकत्व, वितर्व और अवीचार ये तीन प्रकार होते हैं। इस तीन प्रकाररूप एकत्व, वितर्व, अवीचार ध्यान को करने वाले क्षीणकषाय महामुनि ही इसके स्वामी हैं।
विशेषार्थ—यहाँ पर उपशान्तकषाय वाले के प्रथम शुक्लध्यान और क्षीणकषाय वाले के द्वितीय शुक्लध्यान माना है। श्री अमृतचन्द्रसूरि ने भी ‘तत्त्वार्थसार’ में कहा है—
‘द्रव्याण्यनेकभेदानि योगैध्र्यायति यत्रिभिः।
शांतमोहस्ततो ह्येतत्पृथक्त्वमिति कीर्तितम् ।।४७।।
द्रव्यमेवं तथैकेन योगेनान्यतरेण च।
ध्यायति क्षीणमोहो यत्तदेकत्वमिदं भवेत्।।४८।।
अभिप्राय यही है कि उपशान्तमोह मुनि पृथक्त्ववितर्ववीचार शुक्लध्यान को ध्याते हैं और क्षीणमोह मुनि एकत्ववितर्कवीचार को ध्याते हैं।
तृतीय और चतुर्थ शुक्लध्यान का स्वरूप प्रतिपादित करते हुए कहते हैं—
गाथार्थ — सूक्ष्मक्रिया नामक तीसरा शुक्लध्यान सयोगी ध्याते हैं। जो अयोगी केवली ध्याते हैं वह समुच्छिन्न ध्यान है।।४०५।।
आचारवृत्ति — जो सूक्ष्मकाय क्रिया में व्यवस्थित है अर्थात् जिनमें काययोग की क्रिया भी सूक्ष्म हो चुकी है वह सूक्ष्मक्रिया ध्यान है। यह अवितर्क और अविचार श्रुत के अवलम्बन से रहित है अतः अवितर्क है और इसमें अर्थ, व्यंजन तथा योगों का संक्रमण नहीं है अतः यह अविचार है। ऐसे इस सूक्ष्मक्रिया नामक तृतीय शुक्लध्यान को सयोग केवली ध्याते हैं। जिस ध्यान को अयोगकेवली ध्याते हैं वह समुच्छिन्न है। वह अवितर्क, अविचार, अनिवृत्तिनिरुद्ध योग, अनुत्तर, शुक्ल और अविचल है, मणिशिखा के समान है अर्थात् इस समुच्छिन्न ध्यान में श्रुत का अवलम्बन नहीं है अतः अवितर्क है। अर्थ व्यंजन योग की संक्रान्ति भी नहीं है अतः अविचार है। सम्पूर्ण योगों का—काययोग का भी निरोध हो जाने से यह अनिवृत्तिनिरोध योग है। सभी ध्यानों में अन्तिम है इससे उत्कृष्ट अब और कोई ध्यान नहीं रहा है अतः यह अनुत्तर है। परिपूर्णतया स्वच्छ उज्ज्वल होने से शुक्लध्यान इसका नाम है। यह मणि के दीपक की शिखा के समान होने से पूर्णतया अविचल है। इस चतुर्थ ध्यान के स्वामी चौदहवें गुणस्थानवर्ती अयोगकेवली हैं। यद्यपि इन तेरहवें और चौदहवें गुणस्थान में मन का व्यापार नहीं है तो भी उपचार क्रिया से ध्यान का उपचार किया गया है। यह ध्यान का कथन पूर्व में होने वाले ध्यान
अभ्यन्तरस्य व्युत्सर्ग भेदप्रतिपादनार्थमाह— मिच्छत्तवेदरागा तहेव हस्सादिया य छद्दोसा।
चत्तारि तह कसाया चोद्दस अब्भंतरा गंथा।।४०७।।
मिथ्यात्वं। स्त्रीपुंनपुंसकवेदास्त्रयः। रागा हास्यादयः षट् दोषा
हास्यरत्यरतिशोक-भयजुगुप्साः चत्वारस्तथा कषाया क्रोधमानमायालोभाः।
एते चतुर्दशाभ्यन्तरा ग्रन्थाः। एतेषां परित्यागोऽभ्यन्तरो व्युत्सर्ग इति।।४०७।।
बाह्यव्युत्सर्गभेद प्रतिपादनार्थमाह—खेत्तं वत्थु धणधण्णगदं दुपदचदुप्पदगदं च।
जाणसयणासणाणि य कुप्पे भंडेसु दस होंति।।४०८।।
क्षेत्रं सस्यादिनिष्पत्तिस्थानं। वास्तु गृहप्रसादादिवं। धनगतं सुवर्णरूप्यद्रव्यादि।
धान्यगतं शालियवगोधूमादिकं द्विपदा दासीदासादयः।
चतुष्पदगतं गोमहिष्याजादिगतं। यानं शयनमासनं। कुप्यं कार्पासादिकं।
भाण्डं हिंगुमरीचादिकं। एवं बाह्यपरिग्रहो दशप्रकारस्तस्य त्यागो बाह्यो व्युत्सर्ग इति।।४०८।।
द्वादशविधस्यापि तपसः स्वाध्यायोऽधिक इत्याह—बारसविधह्मिवि
तवे सब्भंतरबाहिरे कुसलदिट्ठे। णवि अत्थि णवि य होही सज्झायसमं तवोकम्मं।।४०९।।
द्वादशविधस्यापि तपसः सबाह्याभ्यन्तरे कुशलदृष्टे सर्वज्ञगणधरादिप्रतिपादिते
नाप्यस्ति नापि च भविष्यति स्वाध्यायसमानं तपःकर्म।
द्वादशविधेऽपि तपसि मध्ये स्वाध्यायसमानं तपोनुष्ठानं न भवति न भविष्यति।।४०९।।
सज्झायं कुव्वंतो पंचेंदियसंवुडो तिगुत्तो य।
हवदि य एअग्गमणो विणएण समाहिओ भिक्खू।।४१०।।
की प्रवृत्ति की अपेक्षा करके कहा गया है, जैसे कि पहले घड़े में घी रखा था पुनः उस घड़े से घी निकाल देने के बाद भी उसे घी का घड़ा कह देते हैं अथवा पुरुषवेद का उदय नवमें गुणस्थान में समाप्त हो गया है फिर भी पूर्व की अपेक्षा वेद से मोक्ष की प्राप्ति कह देते हैं।
भावार्थ — इन सयोगी और अयोगकेवली के मन का व्यापार न होने से इनमें ‘एकाग्रचिन्तानिरोधो ध्यानं’ यह ध्यान का लक्षण नहीं पाया जाता है। फिर भी कर्मों का नाश होना यह ध्यान का कार्य देखा जाता है अतएव वहाँ पर उपचार से ध्यान माना जाता है। अब अन्तिम व्युत्सर्ग तप का निरूपण करते हैं— गाथार्थ — आभ्यन्तर और बाह्य के भेद से व्युत्सर्ग दो प्रकार जानना चाहिए। क्रोध आदि अभ्यन्तर हैं और क्षेत्र आदि द्रव्य बाह्य हैं।।४०६।।
आचारवृत्ति — परिग्रह का परित्याग करना व्युत्सर्ग तप है। वह दो प्रकार का है—अभ्यन्तर और बाह्य। क्रोधादि अभ्यन्तर परिग्रह हैं, इनका परित्याग करना अभ्यन्तर व्युत्सर्ग है। क्षेत्र आदि बाह्य द्रव्य का त्याग करना बाह्य व्युत्सर्ग है। अभ्यन्तर व्युत्सर्ग का वर्णन करते हैं—
भावार्थ — मथ्यात्व, तीन वेद, हास्य आदि छह दोष और चार कषायें ये चौदह अभ्यन्तर परिग्रह हैं।।४०७।।
आचारवृत्ति — मिथ्यात्व, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, क्रोध, मान, माया और लोभ ये चौदह अभ्यन्तर परिग्रह हैं। इनका परित्याग करना अभ्यन्तर व्युत्सर्ग है। बाह्य व्युत्सर्ग भेद का प्रतिपादन करते हैं—
भावार्थ — क्षेत्र, वास्तु, धन, धान्य, द्विपद, चतुष्पद, यान, शयन-आसन, कुप्य और भांड ये दश परिग्रह होते हैं।।४०८।।
आचारवृत्ति—धान्य आदि की उत्पत्ति के स्थान को क्षेत्र—खेत कहते हैं। घर, महल आदि वास्तु हैं। सोना, चाँदी आदि द्रव्य धन हैं। शालि, जौ, गेहूँ आदि धान्य हैं। दासी, दास आदि द्विपद हैं। गाय, भैंस, बकरी आदि चतुष्पद हैं। वाहन आदि यान हैं। पलंग, सिंहासन आदि शयन-आसन हैं। कपास आदि कुप्य कहलाते हैं और हींग, मिर्च आदि को भांड कहते हैं। ये बाह्य परिग्रह दश प्रकार के हैं, इनका त्याग करना बाह्य व्युत्सर्ग है। बारह प्रकार के तप में भी स्वाध्याय सबसे श्रेष्ठ है ऐसा निरूपण करते हैं—
गाथार्थ — कुशल महापुरुष के द्वारा देखे गए अभ्यन्तर और बाह्य ऐसे बारह प्रकार के भी तप में स्वाध्याय के समान अन्य कोई तप न है और न ही होगा।।४०९।।
आचारवृत्ति — सर्वज्ञदेव और गणधर आदि के द्वारा प्रतिपादित इन बाह्य और अभ्यन्तर रूप बारह प्रकार के तपों में भी स्वाध्याय के समान न कोई अन्य तप है ही और न ही होगा अर्थात् बारह प्रकार के तपों में स्वाध्याय तप सर्वश्रेष्ठ माना गया है।
गाथार्थ — विनय से सहित हुआ मुनि स्वाध्याय को करते हुए पंचेन्द्रिय से संवृत्त और तीन गुप्ति से गुप्त होकर एकाग्रमन वाला हो जाता है।।४१०।।
स्वाध्यायं कुर्वन् पंचेन्द्रियसंवृतः त्रिगुप्तश्चेन्द्रियव्यापाररहितो
मनोवाक्कायगुप्तश्च, भवत्येकाग्रमनाः शास्त्रार्थतन्निष्ठो
विनयेन समाहितो विययुक्तो भिक्षुः साधुः।
स्वाध्यायस्य माहात्म्यं र्दिशतमाभ्यां गाथाभ्यामिति।।४१०।।
तपोविधानक्रममाह—सद्धिप्पासादवदंसयस्स करणं चदुव्विहं होदि।
दव्वे खेत्ते काले भावे वि य आणुपुव्वीए।।४११।।
तस्य द्वादशविधस्यापि तपसः किंविशिष्टस्य, सिद्धिप्रासादावतंसकस्य
मोक्षगृहकर्णपूरस्य मण्डनस्याथवा सिद्धिप्रासादप्रवेशकस्य
करणमनुष्ठानं चर्तुिवधं भवति। द्रव्यमाहारशरीरादिकं।
क्षेत्रमनूपमरुजांगलादिकं स्निग्धरूक्षवातपित्तश्लेष्म-प्रकोपकं।
कालः शीतोष्णवर्षादिरूपः। भावः (व) परिणामश्चित्तसंक्लेशः।
द्रव्यक्षेत्र-कालभावानाश्रित्य तपः कुर्यात्। यथा वातपित्तश्लेष्मविकारो न भवति।
आनुपूव्र्यानुक्रमेण क्रमं त्यक्त्वा यदि तपः करोति चित्तसंक्लेशो
भवति संक्लेषाच्च कर्मबन्धः स्यादिति।।४११।।
तपोऽधिकारमुपसंहरन् वीर्या सूचयन्नाह—अब्भंतरसोहणओ
एसो अब्भंतरो तओ भणिओ। एत्तो विरियाचारं समासओ वण्णइस्सामि।।४१२।।
अभ्यन्तरशोधनकमेतदभ्यन्तरतपो भणितं भावशोधनायैतत्तपः
तथा बाह्यमप्युक्तं। इत ऊध्र्वं वीर्याचारं वर्णयिष्यामि संक्षेपत इति।।४१२।।
आचारवृत्ति — जो मुनि विनय से युक्त होकर स्वाध्याय करते हैं वे उस समय स्वाध्याय को करते हुए पंचेन्द्रियों के विषय व्यापार से रहित हो जाते हैं और मन-वचन-काय-रूप तीन गुप्ति से सहित हो जाते हैं तथा शास्त्र पढ़ने और उसके अर्थ के चिन्तन में तल्लीन होने से एकाग्रचित्त हो जाते हैं। इन दो गाथाओं के द्वारा स्वाध्याय का माहात्म्य दिखलाया है। तप के विधान का क्रम बतलाते हैं—
गाथार्थ — मोक्षमहल के भूषणरूप तप के कारण चार प्रकार के हैं जो कि द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव रूप क्रम से हैं।।४११।।
आचारवृत्ति — यह जो बारह प्रकार तप है वह सिद्धिप्रासाद का भूषण है, मोक्ष महल का कर्णफूल है अर्थात् मोक्षमहल का मंडनरूप है अथवा मोक्षमहल में प्रवेश करने का साधन है। ऐसा यह तपश्चरण का अनुष्ठान चार प्रकार का है अर्थात् द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव इन चारों का आश्रय लेकर यह तप होता है। आहार और शरीर आदि को द्रव्य कहते हैं। अनूप—जहाँ पानी बहुत पाया जाता है, मरु—जहाँ पानी बहुत कम है, जांगल—जलरहित प्रदेश, ये स्थान स्निग्ध रूक्ष हैं एवं वात, पित्त या कफ को बढ़ाने वाले हैं। ये सब क्षेत्र कहलाते हैं। शीत, उष्ण, वर्षा आदि रूप काल होता है और चित्त के संक्लेश आदि रूप परिणाम को भाव कहते हैं। अपनी प्रकृति आदि के अनुकूल इन द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव को देखकर तपश्चरण करना चाहिए। जिस प्रकार से वात, पित्त या कफ का विकार उत्पन्न न हो, अनुक्रम से ऐसा ही तप करना चाहिए। यदि मुनि क्रम का उल्लंघन करके तप करते हैं तो चित्त में संक्लेश हो जाता है और चित्त में संक्लेश के होने से कर्म का बन्ध होता है।
भावार्थ — जिस आहार आदि द्रव्य से वात आदि विकार उत्पन्न न हो, वैसा आहार आदि लेकर पुनः उपवास आदि करना चाहिए। किसी देश में वात प्रकोप हो जाता है, किसी देश में पित्त का या किसी देश में कफ का प्रकोप बढ़ जाता है ऐसे क्षेत्र को भी अपने स्वास्थ्य के अनुकूल देखकर ही तपश्चरण करना चाहिए। जैसे, जो उष्ण प्रदेश हैं वहाँ पर उपवास अधिक होने से पित्त का प्रकोप हो सकता है। ऐसे ही शीत काल, उष्णकाल और वर्षाकाल में भी अपने स्वास्थ्य को संभालते हुए तपश्चरण करना चाहिए। सभी ऋतुओं में समान उपवास आदि से वात, पित्त आदि विकार बढ़ सकते हैं तथा जिस प्रकार से परिणामों में संक्लेश न हो इतना ही तप करना चाहिए। इस तरह सारी बातें ध्यान में रखते हुए तपश्चरण करने से कर्मों की निर्जरा होकर मोक्ष की सिद्धि होती है अन्यथा, परिणामों में क्लेश हो जाने से कर्म बन्ध जाता है। यहाँ इतना ध्यान में रखना आवश्यक है कि प्रारम्भ में उपवास, कायक्लेश आदि को करने में परिणामों में कुछ क्लेश हो सकता है किन्तु अभ्यास के समय उससे घबराना नहीं चाहिए। धीरे-धीरे अभ्यास को बढ़ाते रहने से बड़े-बड़े उपवास और कायक्लेश आदि सहज होने लगते हैं। अब तप आचार के अधिकार का उपसंहार करते हुए और वीर्याचार को सूचित करते हुए आचार्य कहते हैं—
गाथार्थ — अन्तरंग को शुद्ध करने वाला यह अन्तरंग तप कहा गया है। इसके बाद संक्षेप से वीर्याचार का वर्णन करूँगा।।४१२।।
आचारवृत्ति — भावों को शुद्ध करने के लिए यह अभ्यन्तर तप कहा गया है और इसकी सिद्धि के लिए बाह्य तप को भी कहा है। अब इसके बाद मैं वीर्याचार को थोड़े रूप में कहूँगा।
