भावनिर्जरा-द्रव्यनिर्जरा
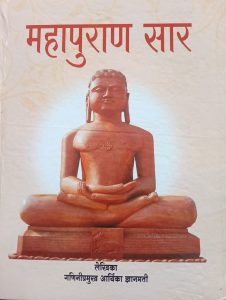
जिन परिणामों से यथाकाल, फल देकर पुद्गल कर्म झड़े।
और जिन भावों से तप द्वारा, फल दें अकाल में कर्म झड़ें।।
बस भावनिर्जरा कहलाता, है भाव वही ऐसा जानो।
है द्रव्यनिर्जरा कर्मों का, झड़ना यह बात सही मानो।।३६।।
यथासमय-उदय काल में फल देकर अथवा तप के द्वारा आत्मा के जिन भावों से कर्म झड़ जाते हैं, वह भाव निर्जरा है और कर्मपुद्गलों का आत्मा से अलग हो जाना द्रव्यनिर्जरा है। इस प्रकार निर्जरा के सविपाक और अविपाक ऐसे दो भेद हैं। जैसे आम आदि फल अपने समय पर पककर वृक्ष की डाल से गिर जाते हैं, वैसे ही अंतरंग और बहिरंग निमित्त को प्राप्त कर जब कर्म अपने उदय में आकर फल देकर झड़ जाते हैं उसे ही अविपाक निर्जरा कहते हैं तथा जैसे आम आदि फलों को पलाल आदि में रखकर बिना समय के भी पका लिया जाता है, उसी प्रकार असमय में ही कर्मों का फल देकर या बिना फल दिये निर्जीण हो जाना अविपाक निर्जरा है। प्रश्न-जो सविपाक निर्जरा है वह तो नरक आदि गतियो में अज्ञानियों के भी होती हुई देखी जाती है। इसलिए सम्यग्ज्ञानियों के सविपाक निर्जरा होती है, यह नियम नहीं है ? उत्तर-यहाँ पर जो संवरपूर्वक निर्जरा होती है उसी को ग्रहण करना चाहिए क्योंकि वही मोक्ष का कारण है किन्तु जो अज्ञानियों के निर्जरा होती है वह तो गजस्नान के समान निष्फल है क्योंकि अज्ञानी जीव थोड़े से कर्मों की तो निर्जरा करता है और बहुत से कर्मों को बाँध लेता है। इस कारण अज्ञानियों की सविपाक निर्जरा को यहाँ नहीं लेना चाहिए। जो सराग सम्यग्दृष्टियों के निर्जरा होती है वह यद्यपि अशुभ कर्मों का नाश करती है, शुभ कर्मों का नाश नहीं करती है फिर भी जीव की संसार स्थिति को थोड़ा करती है अर्थात् जीव के संसार परिभ्रमण को घटाती है। उसका पुण्य कर्मों का आस्रव भी तीर्थंकर प्रकृति आदि विशिष्ट पुण्यबंध का कारण हो जाता है, जो कि परम्परा से मोक्ष का ही कारण है और वीतराग सम्यग्दृष्टियों के पुण्य तथा पाप दोनों का नाश होने पर उसी भव में वह अविपाक निर्जरा मोक्ष का कारण हो जाती है। इसी बात को श्री कुन्दकुन्ददेव ने कहा है-
जं अण्णाणी कम्मं खवेदि, भवसदसहस्सकोडीहिं।
तं णाणी तिहिं गुत्तो खवेदि उस्सासमित्तेण।।
अज्ञानी जिन कर्मों का एक लाख करोड़ वर्षों में नाश करता है उन्हीं कर्मों को ज्ञानी जीव मन, वचन, काय की गुप्ति द्वारा एक उच्छ्वासमात्र में नष्ट कर देता है। यहाँ ज्ञानी जीव के लिए जो ‘तिहिं गुत्तो’ विशेषण दिया है, उससे निर्विकल्प ध्यान करने वाले तीन गुप्ति के धारक महामुनि को ही लिया है। ये मुनि शुक्लध्यानी होते हैं, ऐसा समझना चाहिए। श्री कुन्दकुन्ददेव की उपर्युक्त गाथा का ही पं. दौलतराम जी ने छहढाला में अनुवाद किया है-
कोटि जन्म तप तपें, ज्ञान बिन कर्म झरें जे।
ज्ञानी के छिन माहिं, त्रिगुप्ति तें सहज टरें ते।।
यहाँ कोई शिष्य प्रश्न करता है- सम्यग्दृष्टि के वीतराग विशेषण किसलिए लगाया है क्योंकि ‘रागादि भाव हेय हैं-त्याज्य हैं, ये मेरे नहीं हैं।’’ ऐसा भेद विज्ञान हो जाने पर भले ही वह राग का अनुभव करे तो भी उसके ज्ञानमात्र से मोक्ष हो जाता है। इसका उत्तर आचार्य देते हैं- अंधकार में दो मनुष्य हैं, एक के हाथ में दीपक है और दूसरा बिना दीपक के है। उस दीपक रहित पुरुष को अंधेरे के कारण न तो कुएँ का पता चलता है और न सर्प आदि का ही पता लगता है इसलिए वह अंधकार में यदि कुएँ आदि में गिर जाता है तो दोष नहीं किन्तु जिसके हाथ में दीपक है तो भी यदि वह मनुष्य देखकर भी कुएँ आदि में गिर जावे तो उसके हाथ में दीपक होने का कोई फल नहीं हुआ। यदि वह अंधकार में दीपक का प्रकाश लेकर कुएँ आदि में गिरने से बचता है, उसके ही दीपक लेने की सार्थकता है। इस दृष्टांत के अनुसार कोई मनुष्य तो ‘राग आदि भाव हेय हैं, मेरे नहीं है’ इस प्रकार के भेद विज्ञान को नहीं जानता है, वह तो कर्मों से बंधता ही है और दूसरा मनुष्य भेद विज्ञान के होने पर भी जितने अंशों से वह रागादि का अनुभव करता है उतने अंशों से वह बंधता ही है अत: उसके रागादि के भेद विज्ञान का भी फल नहीं है और जो राग आदि से भेद विज्ञान होने पर राग आदि भावों का त्याग कर देता है उसी के भेद विज्ञान का फल है, यह समझना चाहिए। कहा भी है-
चक्खुस्स दंसणस्स य सारो, सप्पादि दोस परिहारो।
चक्खू होदि निरत्थं, दट्ठूण विले पडंतस्स१।।
नेत्रों से देखकर मार्ग में सर्प आदि से बचना ही देखने का फल है और जो नेत्रादि के द्वारा सर्प आदि को देखकर भी सर्प के बिल में पड़ता है, उसके नेत्रों का होना व्यर्थ है। यही कारण है कि यहाँ ‘सम्यग्दृष्टि’ में वीतराग विशेषण लगाया है। वीतराग सम्यग्दृष्टि रागादि को हेय जानकर उनसे अपने आपको छुड़ाकर शुद्धोपयोग में स्थित होकर निर्विकल्प समाधि के द्वारा अपने आत्म गुणों का ही अनुभव करता है। ये जीव आठवें गुणस्थान से प्रारंभ कर बारहवें तक होते हैं। इनमें भी पूर्ण वीतराग सम्यग्दृष्टि ग्यारहवें-बारहवें गुणस्थान में ही माने गये हैं क्योंकि उन्हीं के सर्वथा रागरूप मोहकर्म का अभाव है। उन्हीं के यथाख्यात चारित्र है अत: उन्हीं का भेद विज्ञान मोक्ष का कारण है। उनसे अतिरिक्त जो सराग सम्यग्दृष्टि हैं, चौथे या पाँचवें गुणस्थान में रहने वाले गृहस्थ हैं उनके लिए वीतराग विशेषण नहीं घटता है। यही कारण है कि सम्यग्दृष्टि के सराग और वीतराग दो भेद किये हैं। समयसार में श्री जयसेन स्वामी ने कहा है कि जिस सम्यग्दर्शन के स्वामी सरागी हैं उनका सम्यग्दर्शन भी सराग कहलाता है और जिस सम्यग्दर्शन के स्वामी वीतरागी महाध्यानी मुनि हैं, उनका सम्यग्दर्शन वीतराग कहलाता है। इस निर्जरा तत्व के प्रकरण में वीतराग सम्यग्दृष्टि जीवों के जो संवरपूर्वक निर्जरा होती है, वही मुख्यरूप से विवक्षित है क्योंकि आस्रव और बंध तत्त्व संसार के कारण हैं और संवर तथा निर्जरा तत्त्व मोक्ष के लिए कारण है, ऐसा समझना चाहिए।
