भाव बंध और द्रव्य बंध
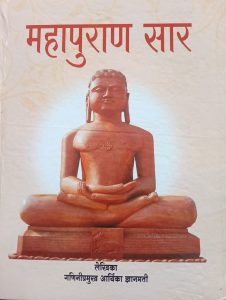
जिन चेतन के परिणामों से, ये कर्म जीव से बंधते हैं।
उन भावों को ही भावबंध, संज्ञा श्रीजिनवर कहते हैं।।
जो कर्म और आतम प्रदेश, इनका आपस में मिल करके।
अति एकमेक हो बंध जाना, यह द्रव्यबंध है बहुविध से।।३२।।
आत्मा के जिन भावों से कर्म बंधता है, वह आत्मा का भाव ही भाव बंध है। कर्म और आत्मा के प्रदेशों का परस्पर में प्रवेश हो जाना-एकमेक हो जाना द्रव्य बंध है। मिथ्यात्व, राग, द्वेष आदि रूप जो अशुद्ध भाव हैं वे आत्मा में उत्पन्न होते हैं अत: आत्मा ही उनका उपादान कारण है। इन अशुद्ध परिणामों में जो कर्म बंधता है, वह भाव बंध है। भाव बंध के निमित्त से कर्म के प्रदेशों का और आत्मा के प्रदेशों का जो दूध और जल की तरह एक-दूसरे में मिल जाना सो द्रव्य बंध है। बंध के भेद और कारण-
प्रकृति, स्थिति, अनुभाग बंध, औ प्रदेश बंध ये चार कहे।
इनमें से योगों के वश से, प्रकृति प्रदेश दो बंध कहे।।
होते कषाय से स्थिति औ, अनुभाग बंध बहु दुखकारी।
इनके ही वश से जीव भ्रमें, अतएव कषाय दुखद भारी।।३३।।
प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध और प्रदेश बंध इन भेदों से बंध चार प्रकार का है। इनमें से प्रकृति और प्रदेश बंध योग के निमित्त से होते हैं तथा स्थिति और अनुभाग बंध कषाय से होते हैं।
प्रकृति का अर्थ है स्वभाव – ज्ञानावरण कर्म की प्रकृति यानी स्वभाव क्या है ? जैसे देवता को पर्दा आच्छादित कर देता है-ढक देता है, उसी प्रकार ज्ञानावरण कर्म ज्ञान को ढक देता है-प्रगट नहीं होने देता है। यही ज्ञानावरण कर्म की प्रकृति है-स्वभाव है। ऐसे ही दर्शनावरण कर्म आत्मा के दर्शन को नहीं होने देता है, जैसे कि द्वारपाल राजा के दर्शन नहीं होने देता है। वेदनीय कर्म का स्वभाव है सुख-दु:ख का वेदन-अनुभव कराना है। जैसे कि शहद से लिपटी हुई तलवार की धार चाटने से कुछ सुख होता है और दु:ख अधिक होता है। मोहनीय कर्म का स्वभाव आत्मा को मोहित कर देने का है। जैसे-मदिरा को पीने वाला मनुष्य हेय-उपादेय के ज्ञान से रहित हो जाता है। आयु कर्म का स्वभाव उस-उस भव में रोके रखने का है। जैसे-बेड़ी मनुष्य को इच्छित स्थान में जाने से रोक देती है। नाम कर्म का स्वभाव है अनेक प्रकार के अच्छे-बुरे शरीर के आकार बना देना, जैसे कि चित्रकार अनेक चित्र बना देता है। गोत्र कर्म का स्वभाव है, उच्च-नीच बनाना, जैसे कि वुंभार छोटे-बड़े घट आदि बना देता है और अन्तराय का स्वभाव है-दान, लाभ, भोग, उपभोग तथा वीर्य में विघ्न डालना।
जैसे कि भंडारी राजा को देते हुए रोक कर लेने वाले के लिए विघ्न डाल देता है। इस प्रकार इन आठ कर्मों का प्रकृति बंध अपने नाम के अनुसार कार्य करता है। जैसे-बकरी, गाय, भैंस आदि का दूध दो प्रहर आदि समय तक अपने मधुर रस में रहता है, उसी प्रकार जीव के प्रदेशों के साथ जितने काल तक कर्मबंध रहता है, उतने काल को स्थिति बंध कहते हैं। आयु कर्म यदि १०० वर्ष तक बंधा है, तो १०० वर्ष बाद उसके निषेक फल देकर समाप्त हो जाते हैं, तब मरण हो जाता है। यह आयु कर्म का स्थिति बंध है। जीव के प्रदेशों में स्थित जो कर्मों के प्रदेश हैं, उनमें जो सुख-दु:ख देने में समर्थ शक्ति विशेष है उसको अनुभाग बंध कहते हैंं। जैसे-बकरी आदि के दूध में कम-अधिक मीठापन, चिकनाई शक्ति रूप अनुभाग कहा जाता है। वह घाति कर्म से संबंध रखने वाली शक्ति लता, काष्ठ, हड्डी और पाषाण के भेद से चार प्रकार की है। उसी तरह अशुभ अघातिया कर्मों में नीम, कांजीर, विष तथा हालाहल रूप से चार प्रकार की है। शुभ अघातिया कर्म प्रकृतियों की शक्ति गुड़, खांड, मिश्री तथा अमृत इन भेदों से चार प्रकार की है। आत्मा के कर्मों के प्रदेश का आकर चिपट जाना प्रदेश बंध है। एक-एक आत्मा के प्रदेश में सिद्धों से अनंतैक भाग और अभव्य जीवराशि से अनंतगुणे ऐसे अनंतानंत परमाणु प्रत्येक क्षण में बंध को प्राप्त होते हैं।
इस प्रकार प्रदेश बंध का स्वरूप है। बंध के चार भेदों का लक्षण संक्षेप से कहा गया है। योग से प्रकृति और प्रदेश बंध होते हैं तथा कषाय से स्थिति बंध और अनुभाग बंध होते हैं। निश्चयनय से आत्मा के प्रदेशों में क्रिया नहीं है किन्तु व्यवहारनय से उन आत्मप्रदेशों में जो परिस्पंदन-हलन चलन होता है उसे योग कहते हैं। उस योग से प्रकृतिबंध होता है तथा प्रदेश बंध होता है। आत्मा के शुद्ध गुणों के प्रतिबंधक जो क्रोध, मान, माया, लोभ आदि कषायें हैं ये सदा ही आत्मा को कषती हैं, दु:ख देती रहती हैं इन कषायों के निमित्त से ही कर्मों में स्थिति-मर्यादा और अनुभाग-सुख दु:ख रूप फल देने की शक्ति पड़ती है। दशवें गुणस्थान तक कषायें रहती हैं अत: वहीं तक स्थिति अनुभाग बंध पड़ता है किन्तु इससे ऊपर वीतराग छद्मस्थ अवस्था में ग्यारहवें, बारहवें गुणस्थान में तथा केवलज्ञानी भगवान के तेरहवें गुणस्थान में भी योग के निमित्त से प्रकृति-प्रदेश बंध होता रहता है। फिर भी वहाँ पर स्थिति अनुभाग न पड़ने से वह बंध कार्यकारी नहीं होता है, नाम मात्र का ही है। बंध व्यवस्था को समझने से स्पष्ट हो जाता है कि वहाँ पर मात्र साता प्रकृति का ही बंध होता है वह भी एक समय मात्र का बंध है इसीलिए इसे ईर्यापथ आस्रव संज्ञा दी है। इस कथन से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि ये कषायें ही जीवों को संसार में भ्रमण कराने वाली हैं, उनको हटाने का प्रयत्न करना चाहिए किन्तु जब तक कषायों को हटा नहीं सकते, तब तक पुरुषार्थ के बल से उन्हें घटाने का प्रयत्न करना ही चाहिए।
प्रश्न – यहाँ पर कषाय से ही स्थिति, अनुभाग बंध माना है अत: बंध में मिथ्यात्व अविंचित्कर ही रहा ?
उत्तर – ऐसा नहीं समझना, क्योंकि अनंतानुबंधी कषायों के साथ मिथ्यात्व रहता ही रहता है और उस मिथ्यात्व से सहचरित ही अनंतानुबंधी कषायें अनंत संसार का कारण बनती हैं। जब मिथ्यात्व नष्ट हो जाता है तब कषायें भी अनंत संसार के लिए कारण ऐसे स्थिति अनुभाग बंध को नहीं करा सकती हैं। उपशम सम्यक्त्व के काल में यदि कदाचित् किसी के अनंतानुबंधी में से किसी एक का उदय आ जाता है तब वह सम्यक्त्व से गिरकर द्वितीय सासादन गुणस्थान में आ जाता है लेकिन इस गुणस्थान का काल मात्र एक समय से लेकर अधिकतम भी छह आवली प्रमाण है, जो कि सेकेण्ड से भी छोटा है। इसके बाद वह जीव नियम से मिथ्यात्व गुणस्थान में आता ही आता है इसलिए अनंतानुबंधी कषायें मिथ्यात्व की सहचारिणी हैं। अथवा यों कहिये मिथ्यात्वरूपी पति के मर जाने के बाद अनंतानुबंधी कषायें अनंत संसार की सृष्टि परम्परा नहीं चला सकती हैं प्रत्युत् वह भी पति के पीछे सती हो जाती हैं। इस कारण मिथ्यात्व बंध में अकिंचित्कर नहीं है। तत्त्वार्थसूत्र महाशास्त्र में आचार्य श्री उमास्वामी ने कहा है-
‘‘मिथ्यादर्शनाविरतिप्रमादकषाययोगा बंधहेतव:।१’’
मिथ्यादर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग ये बंध के कारण हैं। पुन: मिथ्यात्व को बंध के कारणों से वैâसे हटाया जा सकता है। श्री कुन्दकुन्ददेव ने भी समयसार ग्रंथ में बंध के चार प्रत्यय-कारण माने हैं- ‘‘मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग ये चार आस्रव के भेद हैं। ये चेतन और पुद्गल के विकार अचेतन रूप से दो-दो भेद रूप हैं। उनमें जो चेतन के भावरूप आस्रव हैं, जीव में ही होते हैं, अनेक भेद रूप हैं तथा जीव से अभिन्न होने से जीव के ही परिणाम हैं। ये चारों आस्रव ज्ञानावरण आदि आठ प्रकार के कर्मों के बंधने के कारण हैं और इन मिथ्यात्व आदि भावो के लिए भी राग, द्वेष आदि भावों को करने वाला जीव कारण माना गया है।१’’ इन गाथाओं के अर्थ से यह बिल्कुल स्पष्ट है कि मिथ्यात्व बंध के लिए कारण है, अकिंचित्कर नहीं है इसलिए किसी भी आगम की गाथा या सूत्र का अर्थ करते समय अन्य ग्रंथों के गाथा सूत्रों पर भी लक्ष्य रखना चाहिए। किसी एक पंक्ति के अर्थ को पकड़कर सिद्धान्त को विसंवाद का विषय नहीं बनाना चाहिए
