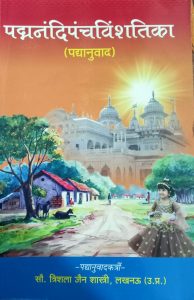मुनिधर्म का कथन
(पद्मनन्दिपञ्चविंशतिका ग्रंथ के आधार से विशेषार्थ सहित)
-शार्दूलविक्रीडित-
आचारो दशधर्मसंयमतपोमूलोत्तराख्यागुणा:,
मिथ्यामोहमदोज्झनं शमदमध्यानाप्रमादस्थिति:।
वैराग्यं समयोपवृंहणगुणा रत्नत्रयं निर्मलं,
पर्य्यन्ते च समाधिरक्षयपदानन्दाय धर्मो यते:।।३८।।
पांच प्रकार का आचार, दशधर्म, संयम, तप, मूलगुण और उत्तरगुण, ये गुण हैं। मिथ्यात्व, मोह और मदों का त्याग, शम-कषायों का शमन, दम-इन्द्रियों का दमन, ध्यान, प्रमाद से रहित स्थिति, वैराग्य, जैनसिद्धान्त या जैनधर्म को वृद्धिंगत करने वाले गुण, निर्दोष रत्नत्रय तथा अंत में समाधिमरण, ये सब मुनि के धर्म हैं जो कि अक्षय मोक्षपद के आनंद के लिए हैं।
विशेषार्थ-यतियों का जो धर्म है वह मोक्षपद के अतीन्द्रिय सुख को देने वाला है। उसमें ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तप आचार और वीर्याचार ये पांच आचार हैं। उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन्य और ब्रह्मचर्य ये दश धर्म हैं। पांच स्थावर और त्रस इन षट्काय जीवों की दया तथा पांच इन्द्रिय और मन इन छह का निरोध ऐसे संयम के बारह भेद हैं। अनशन आदि छह बाह्य तप और प्रायश्चित्त आदि छह अभ्यंतर तप ये बारह तप हैं।
पांच महाव्रत, पांच समिति, पांच इंद्रियनिरोध, केशलोंच, छह आवश्यक क्रिया, आचेलक्य, वस्त्र का त्याग, स्नान का त्याग, भूमिशयन, दंतधावन त्याग, खड़े होकर आहार और एक बार भोजन ये अट्ठाईस मूलगुण हैं। बारह तप और बाईस परिषह ये चौंतीस उत्तर गुण हैं अथवा बहुत से उत्तर गुण हैं जो पूर्णरूप से चौरासी लाख माने गए हैं। पांच प्रकार के मिथ्यात्व, ममत्व परिणामरूप मोह, आठ प्रकार के मद इन सबका त्याग, शम-दम, वैराग्य धर्म को बढ़ाने वाले अनेक प्रकार के गुण, रत्नत्रय और समाधि ये सब मुनीश्वरों का धर्म है। इनको धारण करने वाले दिगम्बर साधु ही मोक्ष के अधिकारी हैं। यदि ये सभी गुण अपूर्ण हैं या सम्यक्त्व से रहित हैं तो वे स्वर्ग को प्राप्त करते हैं पुनः परंपरा से मोक्ष को प्राप्त करते हैं।
स्वं शुद्धं प्रविहाय चिद्गुणमयभ्रान्त्याणुमात्रेऽपि यत्,
संबन्धाय मति: परे भवति तद्बंधाय मूढात्मन:।
तस्मात्त्याज्यमशेषमेव महतामेतच्छरीरादिकं,
तत्कालादि विनादियुक्तित: इदं तत्त्यागकर्मव्रतम्।।३९।।
जो अज्ञानी जीव की बुद्धि अपने शुद्ध, चिच्चैतन्य गुणमय आत्मा को छोड़कर भ्रांति से अणुमात्र भी पर वस्तु में संबंध रखने वाली होती है वह उसके कर्मबंध का ही कारण होती है। इसलिए महान पुरुषों को- मुनियों को समस्त शरीर आदि का त्याग काल आदि के बिना प्रथम युक्ति से कर देना चाहिए क्योंकि यह त्याग क्रिया ही व्रत है।
भावार्थ-मुनिराज यदि शरीर आदि बाह्य वस्तुओं में ममत्व भाव रखकर उनके संयोग आदि के लिए प्रयत्न करते हैं तो उन्हें कर्मबंध होता है और यदि शरीर आदि से ममत्व को छोड़कर शुद्ध आहार आदि के द्वारा रत्नत्रय की प्राप्ति के लिए केवल शरीर का रक्षण करते हैं तो वे मोक्ष को प्राप्त करने में समर्थ हो जाते हैं। यहां ‘कालादि बिना’ का अर्थ टीकाकार ने आहार क्रिया के बिना किया है अर्थात् शरीर से ममत्व छोड़ना चाहिए न कि आहार आदि को, क्योंकि मुनियों के अट्ठाईस मूलगुणों में एकभुक्ति, स्थितिभोजन ये दो मूलगुण हैं। चौबीस घंटे में दिन में एक बार आहार लेना व खड़े होकर लेना ये मूलगुण माने गये हैं। कारण कि शरीर को आहार दिए बिना व्रतों की रक्षा भी नहीं हो सकती है किन्तु जब असाध्य रोग आदि हो जावें और रत्नत्रय स्वरूप मुनिधर्म की रक्षा न होती दिखे तब शरीर के त्याग में भी प्रयत्न करना होता है, उसी का नाम समाधिमरण है। यही त्यागधर्म की विशेषता है।
मुक्त्वा मूलगुणान्यतेर्विदधत: शेषेषु यत्नं परं,
दण्डो मूलहरो भवत्यविरतं पूजादिकं वाञ्छत:।
एकं प्राप्तमरे: प्रहारमतुलं हित्वा शिरश्छेदकं,
रक्षत्यङ्गुलिकोटिखण्डनकरं कोऽन्यो नरो बुद्धिमान्।।४०।।
जो मूलगुणों को छोड़कर केवल शेष-उत्तर गुणों के परिपालन करने में ही प्रयत्न करते हैं तथा निरंतर पूजा-ख्याति, लाभ, पूजा की इच्छा रखते हैं उनका यह प्रयत्न मूलघातक ही होता है। ऐसा कौन बुद्धिमान मनुष्य है कि जो युद्ध में शत्रु के द्वारा शिर को छेदन करने वाले ऐसे अतुल एक प्रहार की तो परवाह न करे और अंगुलि के अग्रभाग को खंडित करने वाले ऐसे प्रहार से रक्षा करने का प्रयत्न करता हो।
भावार्थ-मूलगुण कारण हैं-साधन हैं और उत्तरगुण साध्य हैं। जैसे मूल-जड़ के बिना वृक्ष नहीं होता है वैसे मूलगुण के बिना उत्तरगुण मोक्ष के कारण नहीं होते हैं इसलिए मुनिगण पहले मूलगुणों की रक्षा करें पश्चात् उत्तर गुणों की, मूलगुणों को छोड़कर यदि कोई मुनि उत्तरगुणों को पालना चाहे या ख्याति, लाभ, पूजा आदि की इच्छा से व्रतों को पाले तो ऐसा समझना कि जैसे कोई मूढ़ योद्धा युद्ध में अंगुलि के केवल अग्रभाग की रक्षा करने का प्रयत्न करे और शिर को छेदने वाले प्रहार से रक्षा न करके शिर कटवा लेवे अतः मुनि को सबसे पहले मूलगुणों की रक्षा करनी चाहिए, मूलगुणों की रक्षा करते हुए ही उत्तरगुण पालना चाहिए।
मुनि नग्न दिगंबर क्यों रहते हैं ?
म्लाने क्षालनत: कुत: कृतजलाद्यारम्भत: संयमो,
नष्टे व्याकुलचित्तताथ महतामप्यन्यत: प्रार्थनम्।
कौपीनेऽपि हृते परैश्च झटिति क्रोध: समुत्पद्यते,
तन्नित्यं शुचिरागहृच्छ्रमवतां वस्त्रं ककुम्मण्डलम्।।४१।।
वस्त्र के मलिन हो जाने पर उसके धोने के लिए जल-क्षार-साबुन आदि लगाने रूप आरंभ्ा करना पड़ता है तो भला संयम वैâसे रहेगा ? यदि वस्त्र फट गया या नष्ट हो गया तो मन में व्याकुलता होती है और तब महापुरुषों को भी वस्त्र के लिए दूसरों से याचना करनी पड़ती है। यदि केवल लंगोटी ही है और उसका किसी ने अपहरण कर लिया-चुरा लिया तो तत्क्षण ही क्रोध उत्पन्न हो जाता है इसलिए शमभावी मुनिजन सदा ही पवित्र एवं रागभाव को दूर करने वाले ऐसे दिशारूपी अविनश्वर वस्त्र को धारण कर लेते हैं अर्थात् वस्त्र रहित दिगम्बर अवस्था धारण कर लेते हैं।
भावार्थ-दिगम्बर मुनि वस्त्रों का त्याग क्यों करते हैं ? इसी बात को यहां कहा है। यदि वे वस्त्र पहनेंगे तो मैले होने पर उन्हें जल आदि से धोने से आरंभ होगा तब जीवों की विराधना होने से संयम नहीं पलेगा। यदि लंगोटी मात्र रखेंगे तो भी उसके फटने या खो जाने पर दूसरों से मांगने से सिंहवृत्ति-निःस्पृहवृत्ति नहीं रहेगी यही कारण है कि महामुनि सर्व वस्त्रों को त्याग कर बालक के समान निर्विकार अथवा जन्मजात शिशु के समान नग्नता को ही स्वीकार करते हैं। वैसे यह दिगम्बर मुद्रा ही अर्हन्त मुद्रा है, तीनों लोकों में पूज्य है और आज सर्व संप्रदायों में भी किसी न किसी रूप में इसे अच्छा कहा गया है।
मुनि केशलोंच क्यों करते हैं ?
काकिण्या अपि संग्रहो न विहित: क्षौरं यया कार्यते,
चित्तक्षेपकृदस्त्रमात्रमपिवा तत्सिद्धये नाश्रितम्।
हिंसाहेतुरहोजटाद्यपि तथा यूकाभिरप्रार्थनैर्वैराग्यादिविवर्धनाय
यतिभि: केशेषु लोच: कृत:।।४२।।
दिगम्बर मुनि के पास कौड़ी मात्र भी परिग्रह नहीं है कि जिससे वे क्षौर-केशों का मुंडन करा सकें अथवा शिर का मुंडन करने के लिए उनके पास अस्त्र-उस्तरा, वैंâची आदि भी तो नहीं हैं क्योंकि इनसे क्षोभ उत्पन्न होगा। यदि वे मुनि जटा बढ़ा लेवें तो उनमें जूं आदि उत्पन्न हो जावेंगे तब शिर धोने आदि से हिंसा अवश्य होगी इसलिए अयाचक वृत्ति को धारण करने वाले मुनियों ने अपने शरीर से वैराग्य आदि की वृद्धि के लिए केशों का लोच किया है।
मुनि खड़े होकर आहार क्यों लेते हैं ?
यावन्मे स्थितिभोजनेऽस्ति दृढता पाण्योश्च संयोजने,
भुञ्जे तावदहंरहाम्यथ विधावेषा प्रतिज्ञा यतेः।
कायेऽप्यस्पृहचेतसोऽन्त्यविधिषु प्रोल्लासिनःसन्मतेर्नह्येतेन
दिविस्थितिर्न नरके सम्पद्यते तद्विना।।४३।।
जब तक मुझमें खड़े होकर भोजन करने की दृढ़ता है और जब तक दोनों हाथों को जोड़ने की-अंजुलि बनाकर आहार लेने की दृढ़ता है-शक्ति है तब तक ही मैं भोजन करूँगा अन्यथा भोजन का त्याग कर दूंगा। इस प्रकार जो यति प्रतिज्ञा करके अपने नियम में दृढ़ रहते हैं उनका मन शरीर से भी निस्पृह हो जाता है इसलिए वे सद्बुद्धि को धारण करने वाले साधु समाधिमरण के नियमों में आनंद का अनुभव करते हैं। खड़े होकर पाणिपात्र में आहार करने से स्वर्ग में जन्म होगा और ऐसा न करने से नरक में जाना पड़ेगा ऐसा कुछ नहीं है किन्तु यह तो दिगम्बर मुनि की चर्या ही है ऐसा समझना।।४३।।
विशेषार्थ-दिगम्बर मुनि संपूर्ण परिग्रह के त्यागी हैं अतः उनके पास भोजन हेतु पात्र नहीं है इसीलिए वे अपने हाथ की अंजुलि बनाकर आहार लेते हैं तथा वे खड़े होकर दिन में एक बार भोजन करते हैं। इसी विषय में यहां बतलाया है कि जो बैठकर भोजन करते हैं वे नरक जाएंगे और जो खड़े होकर आहार लेते हैं वे स्वर्ग जाएंगे ऐसा भी कोई नियम नहीं है यह तो मुनिराज की एक प्रतिज्ञा विशेष ही है। श्रीउमास्वामी आचार्य ने भी कहा है-
न श्वभ्रायास्थितेर्भुक्तिः, स्थितेर्नापि विमुक्तये।
किंतु संयमिनामेषा, प्रतिज्ञाज्ञानचक्षुषाम्।।४९।।
न तो बैठकर भोजन करने से नरक की प्राप्ति होती है और न खड़े होकर भोजन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है परन्तु ज्ञानरूपी नेत्रों को धारण करने वाले संयमी पुरुष खड़े होकर भोजन करने की प्रतिज्ञा कर लेते हैं। इसी प्रतिज्ञा के अनुसार ही वे खड़े होकर आहार करते हैं। स्थितिभोजन-खड़े होकर भोजन करना और करपात्र में करना यह मुनि का मूलगुण है।
एकस्यापि ममत्वमात्मवपुषः स्यात्संसृते: कारणं,
कोवाह्यर्थकथाप्रथीयसि तथाप्याराध्यमानेऽपि च।
तद्वासां हरिचंद्रनेऽपि च समःसंश्लिष्टतोऽप्यङ्गतो,
भिन्नं स्वं स्वयमेकमात्मनि धृतं यास्यत्यजस्रं मुनिः।।४४।।
महान तपश्चरण का आराधन करने पर भी जब एकमात्र अपने शरीर में भी होने वाला ममत्व संसार का कारण है तो पुनः बाह्य पदार्थों में होने वाले ममत्व के विषय में क्या कहना ? अर्थात् बाह्य पदार्थों का ममत्व तो संसार का कारण है ही, इसीलिए मुनिराज निरंतर वसूला और उत्तम चंदन इन दोनों में ही समताभाव को धारण करते हुए संयोग संबंध को प्राप्त ऐसे शरीर से भी अपने को भिन्न समझकर एकमात्र अपनी आत्मा को आत्मा में धारण कर आत्मा का ही अवलोकन करते हैं-आत्मा में आत्मा का ही अनुभव करते हैं।
भावार्थ-कोई मुनि यदि भावों से मिथ्यादृष्टि हैं तो भले ही वे घोर तप तपते हैं फिर भी उनके हृदय में भावी शरीर सुखों की इच्छा होने से या शरीर में ‘यह मेरा है’ या जो शरीर है ‘वही मैं हूं’ ऐसी भावना रहने से उनका वह शरीर संबंधी ममत्व भाव संसार का ही कारण है। कहा भी है-
‘मूलं संसारदुःखस्य देह एवात्मधीस्ततः।’
शरीर में आत्मा की बुद्धि ही संसार के दुःखों का मूल कारण है तब जो बाह्य धन, मकान, स्त्री, पुत्र आदि को अपना मानकर उनमें ममता करते हैं उन्हें तो संसार में भ्रमण करना पड़ेगा ही पड़ेगा।
अथवा सम्यग्दृष्टि मुनिराज के भी जब तक शरीर से पूर्ण निर्ममता नहीं आती है तब तक वे स्वर्गादि के सुखों को भोगते रहते हैं, जब शरीर से पूर्ण निर्मम होकर उपसर्ग परीषह को सहने में समर्थ हो जाते हैं तब उसी भव से शुक्लध्यानी बनकर मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं इसलिए शस्त्रप्रहार और चंदनलेपन में भी समभाव को धारण करके आत्मा में आत्मा का ध्यान करने वाले ही महामुनि होते हैं।
-शिखरिणी-
तृणं वा रत्नं वा रिपुरथ परं मित्रमथवा,
सुखं वा दुखं वा पितृबनमदो सौधमथवा।
स्तुतिर्वा निन्दा वा मरणमथवा जीवितमथ
स्फुटं निर्ग्रन्थानां द्वयमपि समं शान्तमनसाम्।।४५।।
अहो! शांतचित्त वाले ऐसे निर्ग्रन्थ महामुनियों को तो तृण हो या रत्न, शत्रु हो या मित्र, सुख हो या दुःख, श्मशानभूमि हो या महल, स्तुति हो या निन्दा, मरण हो या जीवन, इन दोनों प्रकार के इष्ट-अनिष्टों में स्पष्टतया समभाव रहता है।
भावार्थ-परमशांतचित्त को प्राप्त हुए महामुनि रत्न, मित्र, सुख आदि इष्ट पदार्थों में अनुराग नहीं करते हैं और तृण, शत्रु, दुःख आदि अनिष्ट पदार्थों में द्वेषभाव नहीं करते हैं प्रत्युत दोनों स्थितियों में परम समता भाव धारण करते हैं।
-मालिनी-
वयमिह निजयूथभ्रष्टासारङ्गकल्पाः
परपरिचयभीताः क्वापि किंचिच्चरामः।
विजनमधिवसामो न व्रजामः प्रमादं
सुकृतमनुभवामो यत्र तत्रोपविष्टाः।।४६।।
मुनिराज चिंतन करते हैं-यहां हम लोग अपने समुदाय से पृथव्â हुए मृग के सदृश हैं अतः उसी के समान हम भी दूसरों के परिचय से भयभीत होकर कहीं भी (श्रावक के यहां) किंचित् आहार ग्रहण कर लेते हैं, यहां एकांत स्थान में निवास करते हैं, प्रमाद को प्राप्त नहीं होते हैं और जहां कहीं भी बैठकर अपने द्वारा उपार्जित शुभ अथवा अशुभ कर्म का अनुभव करते हैं।
भावार्थ-जैसे घनघोर जंगल में हरिण यदि अपने समुदाय से अलग हो जाए-मार्ग भूल जाए तो वह कहीं भी घास चरता हुआ वहां आने वाले दूसरों-शिकारी या मनुष्यों से या सिंह आदि हिंसक प्राणियों से भयभीत होकर एकांत में रहता हुआ चौकन्ना रहता है। वैसे ही मुनिराज भी अपने स्वजन बंधुओं से अलग होकर जहां कहीं भी श्रावकों के यहाँ निर्दोष आहार लेते हुए पर पदार्थों के परिचय से दूर रहते हुए निर्जन वन में निवास करते हैं, प्रमादी न होकर अप्रमत्त मुनि अवस्था में रहकर जहां कहीं भी पर्वतों की कंदरा, गुफा या चोटी पर बैठकर अपने हित का या शुद्ध आत्मतत्त्व का अनुभव करते हैं।
कति न कति न वारान् भूपतिर्भूरिभूतिः कति
न कति न वारानत्र जातोऽस्मि कीटः।
नियतमिति न कस्याप्यस्ति सौख्यं न दुःखं
जगति तरलरूपे किं मुदा किं शुचा वा।।४७।।
पुनः विचार करते हैं-मैं न जाने कितनी बार बहुत से वैभव को धारण करने वाला राजा हुआ हूं और न जाने कितनी बार यहां क्षुद्र कीड़ा भी हुआ हूं। इस परिवर्तनशील संसार में किसी के भी न तो सुख ही निश्चित है और न दुःख ही निश्चित है। ऐसी अवस्था में हर्ष अथवा विषाद से भला क्या लाभ है ? अर्थात् कुछ भी नहीं है।
भावार्थ-मैं इस संसार में अनादिकाल से लेकर आज तक अनंतों बार तो विभूति वाला राजा हुआ हूं और अनंतों बार क्षुद्र कीड़े की पर्यायें पाई हैं अतः जब यहां किसी का कुछ सुख या दुःख कुछ भी नियत नहीं है तब भला हर्ष-विषाद क्या करना ? मुनिराज सुख-दुःख के आने पर ऐसा चिंतवन करते हुए परम साम्य भाव को धारण कर हमेशा आत्मा के आनंद का अनुभव करते रहते हैं।
-पृथ्वी-
प्रतिक्षणमिदं हृदि स्थितमतिप्रशान्तात्मनो,
मुनेर्भवति संवरः परमशुद्धहेतुर्ध्रुवम्।
रजःखलु पुरातनं गलति नो नवं ढौकते,
ततोऽपि निकटं भवेदमृतधाम दुःखोज्झितम्।।४८।।
जिनकी आत्मा अत्यंत शांत हो चुकी है ऐसे मुनि के हृदय में सदा उपर्युक्त विचार स्थित रहता है। इससे उनके परम विशुद्धि के निमित्त से निश्चित ही संवर-कर्मों के आस्रव का रुकना होता रहता है। तब नियम से पुराने-बंधे हुए कर्मों की निर्जरा हो जाती है और नये कर्म नहीं आते हैं, अतएव उन मुनिराज के अमृतधाम-मोक्षपद अतिनिकट हो जाता है जो कि सर्व दुःखों से रहित है।
-शिखरिणी-
प्रबोधो नीरन्ध्रं प्रवहणममन्दं पृथुतपः,
सुवायुर्यैः प्राप्तो गुरुगणसहायाः प्रणयिनः।
कियन्मात्रस्तेषां भवजलधिरेषोऽस्य च परः,
कियद्दूरे पारः स्फुरति महतामुद्यमवताम्।।४९।।
जिन मुनियोें ने छिद्ररहित और शीघ्रगामी ऐसा सम्यग्ज्ञानरूपी जहाज प्राप्त कर लिया है तथा विपुल तपरूप उत्तम वायु को भी प्राप्त कर लिया है एवं स्नेही गुरुजन जिनके सहायक हैं, ऐसे उद्यमशील उन महामुनियों के लिए यह संसार समुद्र कितने प्रमाण है ? अर्थात् उन्हें वह संसार समुद्र क्षुद्र ही प्रतीत होता है और उनके लिए इसका पार भी भला कितनी दूर है ? अर्थात् कुछ भी दूर नहीं है।
भावार्थ-जैसे जहाज का चालक यदि अनुभवी है, जहाज भी निश्छिद्र है, शीघ्रगामी है और हवा भी अनुकूल है तो उस जहाज में बैठने वाले मनुष्य अत्यंत गहरे एवं अपार भी समुद्र को छोटी सी नदी जैसा समझकर जल्दी ही तट पर पहुंच जाते हैं वैसे ही महामुनि सम्यग्ज्ञानरूपी जहाज में बैठे हुए हैं। यह कर्मास्रव- रूपी छिद्रों से रहित है, चारित्र वृद्धिंगत होने से वह शीघ्रगामी है और तपश्चरणरूपी अनुकूल हवा भी मिल रही है, स्नेही गुरुजन मार्गदर्शक हैं ऐसे मुनिराज संसाररूपी समुद्र को छोटी सी नदी जैसा शीघ्र ही पार कर लेते हैं।
-बसंततिलका-
अभ्यस्यतान्तरदृशं किमु लोकभक्त्या,
मोहं कृशीकुरुत किं वपुषा कृशेन।
एतद्द्वयं यदि न किं बहुभिर्नियोगैः
क्लेशैश्च किं किमपरैः प्रचुरैस्तपोभिः।।५०।।
हे मुनियों! आप अभ्यंतर दृष्टि-आत्मा में दृढ़ श्रद्धा का अभ्यास कीजिए, आपको लोकभक्ति से-जनसमूह की भक्ति-पूजा से क्या लाभ है ? ऐसे ही आपको केवल शरीर के कृश करने से कुछ भी लाभ नहीं है आप तो मोह को कृश करो क्योंकि यदि ये दोनों नहीं हैं तो फिर उनके बिना बहुत से यम नियमों से, कायक्लेश आदि तपश्चरणों से और नाना प्रकार के प्रचुर तपों से कुछ भी प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा।
भावार्थ-यहाँ मुनियों को संबोधित करते हुए आचार्यश्री ने कहा है कि आप अपनी आत्मा में स्थिर होने का अभ्यास करो या सम्यग्ज्ञान का अभ्यास बढ़ाकर अंतरंग के नेत्रों को उद्घाटित करो और मोह को घटाओ। इन दोनों को प्राप्त कर लेने से ही नानाविध तपश्चरण और सभी यम, नियम-व्रत, आवश्यक क्रियायें आदि मोक्ष के लिए कारण बनेंगी क्योंकि सब कुछ होते हुए भी यदि सम्यग्ज्ञान नहीं है और मोह-ममत्व भाव नहीं घटा है तो मोक्षमार्ग दूर ही है।
-वंशस्थ-
जुगुप्सते संसृतिमत्र मायया तितिक्षते प्राप्तपरीषहानपि।
न चेन्मुनिर्दुष्टकषायनिग्रहाच्चिकित्सति स्वान्तमघप्रशान्तये।।५१।।
इस संसार में यदि कोई मुनि अपने पापों की शांति के लिए दुष्ट कषायों का निग्रह करके अपने मन का उपचार नहीं करते हैं तो यह समझो कि जो वे संसार से घृणा करते हैं और आए हुए क्षुधा, तृषा आदि परीषहों को भी सहन करते हैं वे सब मायाचार से ही ऐसा करते हैं पुनः पापों की शांति वैâसे होगी ?
भावार्थ-संसार से विरक्त होकर जो मुनि नानाविध क्षुधा, तृषा, शीत, उष्ण, दंशमशक आदि परीषहों को भी सहन करते रहें किन्तु जब तक वे कषायों का शमन नहीं करते हैं तब तक कर्मों का नाश संभव नहीं है अतः कषायों को मंद करना बहुत आवश्यक है।
-शार्दूलविक्रीडित-
हिंसा प्राणिषु कल्मषं भवति सा प्रारम्भतः सोऽर्थतः,
तस्मादेव भयादयोऽपि नितरां दीर्घा ततः संसृतिः।
तत्रासातमशेषमर्थत इदं मत्वेति यस्त्यक्तवान्,
मुक्त्यर्थी पुनरर्थमाश्रितवता तेनाहतः सत्पथः।।५२।।
प्राणियों की हिंसा पाप है, वह हिंसा आरंभ से होती है, वह आरंभ धन से होता है और उस धन से ही अत्यन्त भय आदि भी उत्पन्न होते हैं पुनः उस भय से दीर्घ संसार होता है और उस संसार में परिपूर्णतया दुःख होते हैं। इस प्रकार इन समस्त दुःखों का कारण धन ही है ऐसा समझकर मोक्ष के इच्छुक मुनि ने धन का त्याग कर दिया है पुनः यदि मुनि धन का आश्रय ले लेवे तो उसने अपने मोक्षमार्ग को नष्ट कर दिया है ऐसा समझना चाहिए।
दुर्ध्यानार्थमवद्यकारणमहो निर्ग्रन्थताहानये,
शय्याहेतुतृणाद्यपि प्रशमिनां लज्जाकरं स्वीकृतम्।
यत्तत्किं न गृहस्थयोग्यमपरं स्वर्णादिकं साम्प्रतं
निर्ग्रन्थेष्वपि चैतदस्ति नितरां प्रायः प्रविष्टः कलिः।।५३।।
शय्या के लिए स्वीकार किये गए तृण-चावल की घास आदि भी मुनियों को लज्जाजनक प्रतीत होते हैं तथा दुर्ध्यान और पाप के कारण होकर उनकी निर्ग्रन्थता-निष्परिग्रहता को हानि पहुंचाते हैं। फिर गृहस्थ के योग्य अन्य सुवर्ण आदि क्या उस निर्ग्रन्थता के घातक नहीं होंगे ? अवश्य होंगे फिर भी यदि आजकल निर्ग्रन्थ कहे जाने वाले मुनियों के पास गृहस्थ के योग्य सुवर्ण आदि परिग्रह रहे तो समझना चाहिए प्रायः कलिकाल का प्रवेश हो चुका है।
विशेषार्थ-मुनियों के अट्ठाईस मूलगुणों में भूमिशयन एक मूलगुण है। इसके लक्षण में मूलाचार में संस्तर के चार भेद किए हैं। यथा-‘‘तृणमये काष्ठाये, शिलामये भूमिप्रदेशे च संस्तरे१।’’
तृण-घास, चावल या कोदों की घास जिसे पुराल, प्याल या पैरा भी कहते हैं। फलक-लकड़ी की फड़, पाटा, तखत आदि, पाषाण की शिला और भूमि ये चार प्रकार के संस्तर हैं। यद्यपि निर्ग्रन्थ दिगम्बर मुनियों के लिए ये घास, पाटे आदि ग्राह्य हैं फिर भी उन्हें लज्जा प्रतीत होती है। कदाचित् ये अपने अनुकूल अच्छे नहीं मिल पाये तो आर्त-रौद्रध्यान भी हो सकता है। कदाचित् खटमल आदि जंतु इनमें हो गये और निद्रा में मर गये तो प्रमादजन्य पाप बंध भी हो जाता है। जब ये घास आदि सर्दी के दिनों में सोने, बिछाने में लेने से मुनि के पूर्णतया निर्ग्रन्थता व निष्परिग्रहपना नहीं हो पाता है तब यदि कोई मुनि दिगम्बर होकर भी गृहस्थ के योग्य सुवर्ण आदि परिग्रहरूप कोई वस्तु रख लेवें तो उनके लिए महान दोषास्पद ही है। इसे कलिकाल का ही प्रभाव समझना चाहिए। ऐसे मुनि अपने मोक्षमार्ग को नष्ट करने वाले हैं।
-आर्या-
कादाचित्को बंधः क्रोधादेः कर्मणः सदा सङ्गात्।
नातः क्वापि कदाचित्परिग्रहग्रहवतां सिद्धिः।।५४।।
क्रोधादि कषायों के निमित्त से जो बंध होता है वह तो कभी-कभी ही होता है किन्तु परिग्रह के निमित्त से जो बंध होता है वह सदाकाल होता है इसलिए जो साधुजन परिग्रहरूपी ग्रह-पिशाच से पीड़ित हैं उनको कहीं पर और कभी भी सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती है।
-इंद्रवङ्काा-
मोक्षेऽपि मोहादभिलाषदोषो विशेषतो मोक्षनिषेधकारी।
यतस्ततोऽध्यात्मरतो मुमुक्षुर्भवेत्किमत्र कृताभिलाषः।।५५।।
जब मोह से मोक्ष के लिए भी की गई अभिलाषा दोषरूप है और वह विशेषतया मोक्ष का निषेध करने वाली है-मोक्ष में जाने से रोकने वाली है तब अपनी आत्मा में लीन हुए मुमुक्षु-मोक्षाभिलाषी मुनि क्या स्त्री, पुत्रादि अन्य बाह्य वस्तुओं की इच्छा करेंगे ? अर्थात् नहीं करेंगे।
-पृथ्वी-
परिग्रहवतां शिवं यदि तदानलः शीतलो,
यदीन्द्रियसुखं सुखं तदिह कालकूटः सुधा।
स्थिरा यदि तनुस्तदा स्थिरतरं तडिच्चाम्बरे,
भवेऽत्र रमणीयता यदि तदीन्द्रजालेऽपि च।।५६।।
यदि परिग्रहसहित जनों को मोक्ष मिल सकता है तब तो अग्नि भी शीतल हो सकती है। यदि इन्द्रियजन्य सुख वास्तविक सुख हैं तब तो कालकूट विष भी अमृत बन जावेगा। यदि शरीर स्थिर रह सकता है तब तो आकाश में चमकने वाली बिजली भी उससे भी अधिक स्थिर हो सकती है और यदि इस संसार में रमणीयता-सुंदरता हो सकती है तब तो वह इन्द्रजाल में भी हो सकती है।
भावार्थ-जैसे अग्नि कभी ठंडी नहीं हो सकती है वैसे परिग्रहधारी साधु मोक्ष नहीं जा सकते हैं। जैसे विष अमृत नहीं होता है, बिजली स्थिर नहीं है और इन्द्रजालिया-जादू के खेल सुंदर नहीं हैं वैसे इंद्रिय सुख सुखाभास हैं, शरीर क्षणिक है और संसार में कुछ भी सुंदर नहीं है।
स्मरमपि हृदि येषां ध्यानवन्हिप्रदीप्ते
सकलभुवनमल्लं दह्यमानं विलोक्य।
कृतभिय इव नष्टास्ते कषाया न तस्मिन्पुनरपि
हि समीयुः साधवस्ते जयन्ति।।५७।।
जिन मुनियों के हृदय में ध्यानरूपी अग्नि के प्रज्वलित हो जाने से तीनों लोकों को जीतने वाला ऐसा कामदेव योद्धा भी जलने लगा। इसको जलता हुआ देखकर मानो अतिशय भयभीत हुई कषायें इस प्रकार नष्ट हो गईं कि पुनः वे पास में नहीं आ सकीं, वे ही मुनिराज जयशील होते हैं।
-उपेन्द्रवङ्काा-
अनर्घ्यरत्नत्रयसम्पदोऽपि निर्ग्रंथतायाः पदमद्वितीयम्।
जयन्ति शान्ताः स्मरवैरिवध्वाः वैधव्यदास्ते गुरवो नमस्याः।।५८।।
जो मुनिराज अमूल्य रत्नत्रयरूपी संपत्ति से सहित होकर भी निर्ग्रंथता के अद्वितीय पद को प्राप्त हुए हैं। जो अत्यंत प्रशांत होकर भी कामदेव शत्रु की स्त्री को विधवा बनाने वाले हैं ऐसे गुरुदेव नमस्कार के योग्य हैं।
भावार्थ-जो अमूल्य तीन रत्न के स्वामी हों वे निर्ग्रन्थ-निष्परिग्रही वैâसे होंगे ? तथा जो परम शांत हों वे शत्रु को मारने वाले वैâसे होंगे ? यहां विरोधाभास अलंकार है। उसका परिहार ऐसा है कि निर्ग्रन्थ दिगम्बर मुनि ही रत्नत्रय के धनी होते हैं और परम शांत साधु ही कामदेव को जीत सकते हैं।
आचार्य परमेष्ठी की स्तुति
-शार्दूलविक्रीडित-
ये स्वाचारमपारसौख्यसुतरोर्वीजं परं पञ्चधा
सद्वोधाः स्वयमाचरन्ति च परानाचारयन्त्येव च।
ग्रंथगंथिविमुक्तमुक्तिपदवीं प्राप्ताश्च यैः प्रापितास्ते
रत्नत्रयधारिणः शिवसुखं कुर्वन्तु नः सूरयः।।५९।।
जो आचार्य परमेष्ठी सम्यग्ज्ञान से सहित हुए अपरिमित सौख्य रूपी, उत्तम वृक्ष के लिए बीजभूत ऐसे पांच प्रकार के आचार का स्वयं आचरण करते हैं और अन्य शिष्यों से भी पालन कराते हैं, जो परिग्रह रूपी गांठ से रहित ऐसे मोक्षमार्ग को स्वयं प्राप्त कर चुके हैं तथा अन्य शिष्यों को भी प्राप्त कराया है ऐसे रत्नत्रय के धारक आचार्यदेव हमको मोक्षसुख प्रदान करें।
-बसंततिलका-
भ्रान्तिप्रदेषु वहुवर्त्मसु जन्मकक्ष्ये पन्थानमेकममृतस्य परं नयन्ति।
ये लोकमुन्नतधियः प्रणमामि तेभ्यस्तेनाप्यहं जिगमिषुर्गुरुनायकेभ्यः।।६०।।
जो उत्तम बुद्धि के धारक आचार्य इस जन्म-मरण रूप संसार वन में भ्रांति को उत्पन्न करने वाले अनेक मार्गों के होने पर भी दूसरे भव्यजनों को केवल मोक्षमार्ग में ही लगाते हैं उन अन्य मुनियों को सन्मार्ग में ले जाने वाले आचार्यों को मैं भी उसी मार्ग में जाने का इच्छुक हुआ नमस्कार करता हूं।
उपाध्याय परमेष्ठी की स्तुति
-शार्दूलविक्रीडित-
शिष्याणामपहाय मोहपटलं कालेन दीर्घेण यज्जातं
‘स्यात्पदलाञ्छितोज्वलवचो-दिव्याञ्जनेन’ स्फुटम्।
ये कुर्वन्ति दृशं परामतितरां सर्वावलोके क्षमं लोके
कारणमन्तरेण भिषजस्ते पान्तु नोऽध्यापकाः।।६१।।
जो संसार में अकारण वैद्य के समान होते हुए शिष्यों के दीर्घकालीन मोह समूह को दूर कर ‘स्यात्’ पद से चिन्हित अनेकांतमय उज्ज्वल-निर्दोष वचनरूपी दिव्य अञ्जन से उनकी अत्यंत श्रेष्ठ दृष्टि को स्पष्ट तथा संपूर्ण पदार्थों के देखने में समर्थ बना देते हैं वे उपाध्याय परमेष्ठी हमारी रक्षा करें।
-शार्दूलविक्रीडित-
उन्मुच्यालयबंधनादपि दृढात्कायेऽपि वीतस्पृहाश्चित्ते
मोहविकल्पजालमपि यद्दुर्भेद्यमन्तस्तमः।
भेदायास्य हि साधयन्ति तदहो ज्योतिर्जितार्कप्रभं
ये सद्बोधमयं भवन्तु भवतां ते साधवः श्रेयसे।।६२।।
अरे! आश्चर्य है कि जो दृढ़ गृह रूपी बंधन से छुटकारा पाकर अपने शरीर से भी निःस्पृह हो चुके हैं, जो मन में स्थित दुर्भेद्य मोह से उत्पन्न विकल्प समूह रूपी अभ्यंतर अंधकार को नष्ट करने के लिए सूर्य की प्रभा को जीतने वाली ऐसी उत्कृष्ट ज्ञानज्योति के सिद्ध करने में लगे हुए हैं वे साधु परमेष्ठी आपके कल्याण के लिए होवें।
वीतराग की महिमा का वर्णन
-बसंततिलका-
वङ्को पतत्यपि भयद्रुतविश्वलोकमुक्ताध्वनि प्रशमिनो न चलन्ति योगात्।
बोधप्रदीपहतमोहमहान्धकाराः सम्यग्दृशः किमतु शेषपरीषहेषु।।६३।।
भय से अतिशीघ्र मार्ग को छोड़कर सभी जन पलायन कर जावें, ऐसे वङ्कापात के होने पर भी जो शांतचित्त मुनिराज ध्यान से चलायमान नहीं होते हैं, वे ज्ञानरूपी दीपक के द्वारा अज्ञानरूपी घोर अंधकार को दूर करने वाले सम्यग्दृष्टि महामुनि क्या शेष परीषहों के आने पर विचलित हो सकते हैं ? अर्थात् नहीं हो सकते।
भावार्थ-संपूर्ण जनसमूह को भय से भगा देने वाले ऐसे घोर वङ्कापात के होने पर भी जो मुनिराज ध्यान में लीन रह सकते हैं ऐसे महामुनि अन्य परीषहों को तो सहज ही जीत लेते हैं।
भावार्थ-ज्येष्ठ-आषाढ़ की भयंकर गर्मी में सूर्य की उग्र किरणों से पृथ्वी की धूलि भाड़ की बालू के समान तप्तायमान हो जाती है। गर्म-गर्म लू से सब तरफ से लपट लगने लगती है, सर्वत्र नदी, सरोवरों का जल सूख जाता है ऐसे समय में जो महामुनि पर्वत के शिखर पर ध्यान लगाते हैं वे मुनिराज हम सब लोगों का कल्याण करने वाले होवें।
-शार्दूलविक्रीडित-
प्रोद्यत्तिग्मकरोग्रतेजसि लसच्चण्डानिलोद्यद्दिशि
स्फारीभूतसुतप्तभूमिरजसि प्रक्षीणनद्यम्भसि।
ग्रीष्मे ये गुरुमेधनीध्रशिरसि ज्योतिर्निधायोरसि
ध्वान्तध्वंसकरं वसन्ति मुनयस्ते सन्तु नः श्रेयसे।।६४।।
जिस ग्रीष्मकाल में उदित होता हुआ सूर्य अपनी तीक्ष्ण किरणों को बिखेर रहा है, जिसमें तीक्ष्ण पवन-गर्म लू से दिशायें व्याप्त हो रही हैं, जिसमें भूमि की धूलि अत्यंत तप्तायमान हो रही है तथा जिस समय नदियों का जल सूख जाता है, ऐसे ग्रीष्मकाल में जो मुनिराज अपने हृदय में अज्ञान अंधकार को नष्ट करने वाली ज्ञानज्योति को धारण करके महापर्वत के शिखर पर निवास करते हैं वे साधुगण हमारे कल्याण के लिए होवें।
-शार्दूलविक्रीडित-
ते वः पान्तु मुमुक्षवः कृतरवेरब्दै रतिश्यामलैः
शश्वद्वारि वमद्भिरब्धिविषयक्षारत्वदोषादिव।
काले मज्जदिले पतद्गिरिकुले ‘धावद्धुनीसंकुले’
झंझावातविसंस्थुले तरुतले तिष्ठfिन्त ये साधवः।।६५।।
जिस वर्षाकाल में गरजते हुए काले-काले मेघ बरसते रहते हैं, ऐसा लगता है मानो समुद्रविषयक खारे जल के दोष से ही वे सतत पानी को उगल रहे हों, ऐसे उन मेघों की वर्षा से पृथ्वी जल में डूबने लगती है, पानी के अविरल प्रवाह से पर्वतों का समूह गिरने लगता है, जिसमें नदियां वेग से बहने लगती हैं तथा जो झ्ांझावात-जलमिश्रित भयंकर हवा से सहित है, ऐसे वर्षाकाल में जो मुनिराज वृक्षों के नीचे विराजमान रहते हैं वे आप लोगों की रक्षा करें।
-शार्दूलविक्रीडित-
म्यायत्कोकनदे गलत्पिकमदे भ्रंश्यद्द्रुमौघच्छदे
हर्षद्रोमदरिद्रके हिमऋतावत्यन्तदुःखप्रदे।
ये तिष्ठfिन्त चतुष्पथे पृथुतपः सौधस्थिताः साधवो
ध्यानोष्णप्रहितोग्रशीतविधुरास्ते मे विदध्युः श्रियम्।।६६।।
जिस शीतकाल में कमल मुरझाने लगते हैं, वानरों के मद गलित हो जाते हैं, वृक्षों से पत्ते झड़ जाते हैं, दरिद्री लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ऐसी अत्यंत दुःखप्रद शीत ऋतु में विशाल तपरूपी महल में स्थित तथा ध्यानरूपी उष्णता से अत्युग्र ठंड को दूर करने वाले जो महासाधु चतुष्पथ-खुले मैदान में स्थित रहते हैं वे साधु मुझे मोक्षलक्ष्मी प्रदान करें।
-बसंततिलका-
कालत्रये बहिरवस्थितजातवर्षा शीतातपप्रमुखसंघटितोग्रदुःखे।
आत्मप्रबोधविकले सकलोऽपि कायक्लेशो वृथा वृतिरिवोज्झितशालिवप्रे।।६७।।
जो साधुगण जिन तीन कालों में घर छोड़कर बाहर रहने से उत्पन्न हुए वर्षा, शीत और धूप आदि के तीव्र दुःखों को सहन करते हैं, वे यदि उन तीनों कालों में अध्यात्म ज्ञान से रहित हैं तो उनका ये सब कायक्लेश इसी प्रकार व्यर्थ है कि जिस प्रकार धान्यांकुरों से रहित खेत में कांटों से बाड़ का निर्माण करना।
भावार्थ-‘‘आत्मा भिन्न है और शरीर भिन्न है’’ ऐसे अध्यात्म ज्ञान से सहित अन्तरात्मा मुनि यदि वर्षा में वृक्ष के नीचे, ठंड में चौहटे में और ग्रीष्म ऋतु में पर्वतों की चोटी पर ध्यान करते हैं तो वे कर्मों के नाश में समर्थ होते हैं किन्तु आत्मज्ञान से रहित हैं उनका यह कायक्लेश तप अधिकतम नव ग्रैवेयक तक ले जा सकता है, सांसारिक वैभव दे सकता है किन्तु उसी भव से मोक्ष नहीं दे सकता है। हां, परंपरा से सम्यक्त्व आदि प्राप्त कराकर मोक्ष का कारण भी हो सकता है अतः सर्वथा निष्फल नहीं है।
-शार्दूलविक्रीडित-
सम्प्रत्यस्ति न केवली किल कलौ त्रैलोक्यचूडामणि
स्तद्वाचः परमासतेऽत्र भरतक्षेत्रे जगद्द्योतिकाः।
सद्रत्नत्रयधारिणो यतिवरास्तेषां समालंबनं
तत्पूजा जिनवाचिपूजनमतः साक्षाज्जिनः पूजितः।।६८।।
इस कलिकाल-पंचमकाल में इस भरतक्षेत्र में इस समय यद्यपि तीनों लोकों के चूड़ामणि ऐसे केवली भगवान विराजमान नहीं हैं फिर भी लोक को प्रकाशित करने वाले उन केवली के वचन तो विद्यमान हैं हीं और उन वचनों का आश्रय लेने वाले उत्तम रत्नत्रय के धारी महामुनि भी विद्यमान हैं, इसलिए उन मुनियों की पूजा वास्तव में जिनवचनों की ही पूजा है और जिनवचनों की पूजा से प्रत्यक्ष में जिन भगवान की ही पूजा की गई है ऐसा समझना चाहिए।
विशेषार्थ-इस श्लोक में श्रीपद्मनंदि आचार्य ने बहुत ही स्पष्ट कहा है कि आज भी इस निकृष्ट पंचमकाल में सच्चे दिगम्बर जैन मुनि होते हैं और भगवान की वाणी भी विद्यमान है। इन मुनियों की पूजा से जिनवचनों की पूजा हो जाती है और जिनवचनों की पूजा से साक्षात् समवशरण में विराजमान जिनेन्द्रदेव की ही पूजा हो जाती है। इस कथन से निर्दोष चारित्रधारी ऐसे महामुनियों की पूजा से जिनेन्द्रदेव की पूजा की गई है ऐसा अर्थ स्पष्ट है। दिगम्बर जैन संप्रदाय में ही आज कुछ ऐसे भी निश्चयाभासी एकांतवादी हैं जो कि अपने को अध्यात्मवादी कहते हैं, वे वर्तमान शताब्दी के चारित्रचक्रवर्ती आचार्य श्री शांतिसागर जी आदि किन्हीं भी महामुनियों के प्रमाण नहीं मानते हैं, सभी को द्रव्यलिंगी मिथ्यादृष्टि कहकर न इन्हें नमस्कार करते हैं और न ही इन्हें नवधाभक्तिपूर्वक आहार ही देते हैं। ये कुंदकुंददेव के ग्रन्थों का ही अधिकतर स्वाध्याय करते हैं। उनके लिए श्रीकुंदकुंददेव के ग्रंथों के आधार से ‘‘आजकल सच्चे मुनि हैं’’ यह बातें भी सिद्ध की जा रही हैं। यथा-
भरहे दुस्समकाले धम्मज्झाणं हवेइ साहुस्स।
तं अप्पसहावठिदे ण हु मण्णइ सो वि अण्णाणी।।७६।।
अज्ज वि तिरयणसुद्धा अप्पा झाएवि लहइ इंदत्तं।
लोयंतियदेवत्तं तत्थ चुदा णिव्वुदिं जंति।।७७।।
इस भरतक्षेत्र में दुःषमकाल में मुनि को आत्मस्वभाव में स्थित होने पर धर्मध्यान होता है, जो ऐसा नहीं मानता है वह अज्ञानी है। आज भी इस पंचमकाल में रत्नत्रय से शुद्ध आत्मा (मुनि) आत्मा का ध्यान करके इन्द्रत्व और लौकांतिक देव के पद को प्राप्त कर लेते हैं और वहां से चयकर निर्वाण को प्राप्त कर लेते हैं।१
श्री गौतमस्वामी से लेकर अंग-पूर्व के एकदेश के जानने वाले मुनियों की परम्परा के काल का प्रमाण ६८३ वर्ष होता है। उसके बाद-‘जो श्रुततीर्थ धर्म प्रवर्तन का कारण है, वह बीस हजार तीन सौ सत्रह वर्षों में कालदोष से व्युच्छेद को प्राप्त हो जावेगा’ अर्थात् ६८३+२०३१७ = २१००० वर्ष का यह पंचमकाल है तब तक धर्म रहेगा। ‘‘इतने समय तक चातुर्वर्ण्य संघ जन्म लेता है१।’’
-शार्दूलविक्रीडित-
स्पृष्टा यत्र मही तदंघ्रिकमलैस्तत्रैति सत्तीर्थतां
तेभ्यस्तेपि सुराः कृताञ्जलिपुटा नित्यं नमस्कुर्वते।
तन्नामस्मृतिमात्रतोऽपि जनता निष्कल्मषा जायते
ये जैना यतयश्चिदात्मनिरता ध्यानं समातन्वते।।६९।।
जो जैन महामुनि अपने चिच्चैतन्यस्वरूप आत्मा में परम स्नेह को करते हैं उनके चरणकमलों के द्वारा जहां की पृथ्वी स्पर्श की जाती है वहां की पृथ्वी उत्तम तीर्थ बन जाती है, देवगण भी नित्य ही उनको हाथ जोड़कर नमस्कार करते हैं और तो क्या, उनके नाम के स्मरण मात्र से भी जनसमूह पाप से रहित हो जाता है।
-शार्दूलविक्रीडित-
सम्यग्दर्शनवृत्तबोधनिचितः शान्तः शिवैषी मुनिः मन्दैः
स्यादवधीरितोऽपि विशदः साम्यं यदालम्ब्यते।
आत्मा तैर्विहतो यदत्र विषमध्वान्तश्रिते निश्चितं सम्पातो
भवितोग्रदुःखनरके तेषामकल्याणिनाम्।।७०।।
सम्यग्दर्शन, ज्ञान और चारित्र से सहित, शांत और मोक्ष के इच्छुक जो मुनिराज अज्ञानीजनों के द्वारा अपमानित होकर भी यदि परम साम्यभाव का अवलंबन लेते हैं तो वे निर्मल भाव करने वाले ही हैं प्रत्युत वैसा करने वाले अज्ञानीजन अपनी आत्मा का ही घात कर लेते हैं और तब कल्याण पथ से च्युत हुए उन अज्ञानियों को तीव्र अंधकार से व्याप्त एवं घोर दुःखों से संयुक्त ऐसे नरकों में नियम से जाना होता है।
-स्रग्धरा-
मानुष्यं प्राप्य पुण्यात्प्रशममुपगता रोगवद्भोगजालं
मत्वा गत्वा वनांतं दृशि विदि चरणे ये स्थिताः संगमुक्ताः।
कस्तोता वाक्पथातिक्रमणपटुगुणैराश्रितानांमुनीनांस्तोतव्यास्तेमहद्भिर्भुवि
य इह तदंघ्रिद्वयेभक्तिभाजः।।७१।।
जो मुनिराज पुण्य के प्रभाव से मनुष्य पर्याय को प्राप्त कर शांत परिणाम को प्राप्त हुए इन्द्रियजनित भोगों को रोग के समान समझकर वन में जाकर स्थित हो जाते हैं। वचन के अगोचर ऐसे उत्तम-उत्तम गुणों के निधान उन मुनियों की स्तुति भला कौन कर सकता है ? अर्थात् कोई भी नहीं कर सकता है। जो मनुष्य उन मुनियों के चरणकमलों में भक्ति सहित हैं वे यहां पृथिवी पर महापुरुषों-विद्वानों द्वारा स्तुति करने के योग्य हो जाते हैं।
विशेषार्थ-जो रत्नत्रयधारी निर्ग्रन्थ महामुनियों की भक्ति करते हैं, स्तुति करते हैं वे इस संसार में विद्वानों द्वारा प्रशंसा को प्राप्त करते हैं। कहा भी है-
उच्चैर्गोत्रं प्रणतेर्भोगो दानादुपासनात्पूजा।
भक्तेः सुंदररूपं, स्तवनात्कीर्तिस्तपोनिधिषु२।।
तपोनिधि साधुओं को नमस्कार करने से उच्च गोत्र मिलता है, उन्हें दान देने से भोगों की प्राप्ति होती है, उनकी उपासना करने से पूजा मिलती है, उनकी भक्ति से सुंदर रूप प्राप्त होता है और उन गुरुओं के स्तवन से कीर्ति होती है, ऐसा श्रीसमंतभद्र स्वामी का कथन है।
यहां तक मुनियों का धर्म कहा गया है।