जीवसमास प्रकरण
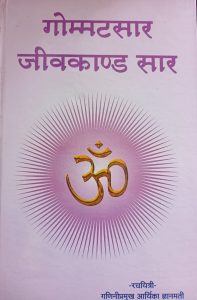
जीव समास का लक्षण
जेहिं अणेया जीवा, णज्जंते बहुविहा वि तज्जादी।
ते पुण संगहिदत्था, जीवसमासा त्ति विण्णेया।।२७।।
यैरनेके जीवा नयन्ते, बहुविधा अपि तज्जातय:।
ते पुन: संगृहीतार्था, जीवसमासा इति विज्ञेया:।।२७।।
अर्थ—जिनके द्वारा अनेक जीव तथा उनकी अनेक प्रकार की जाति जानी जाएँ, उन धर्मों को अनेक पदार्थों का संग्रह करने वाले होने से जीवसमास कहते हैं, ऐसा समझना चाहिए।
भावार्थ —उन धर्मविशेषों को जीवसमास कहते हैं कि जिनके द्वारा अनेक जीव अथवा जीव की अनेक जातियों का संग्रह किया जा सके क्योंकि केवलज्ञान के बिना जीवों का स्वरूप और भेद प्रत्यक्ष नहीं जाना जा सकता अतएव छद्मस्थों को उनका बोध कराना ही इस प्ररूपणा का प्रयोजन है। संग्रहनय से जिन पर्यायाश्रित अनेक जीवों में पाये जाने वाले समान धर्मों के द्वारा उनका संक्षेप में ज्ञान कराया जा सके उनको ही जीवसमास कहते हैं। टीकाकारों ने जीवसमास शब्द से एकेन्द्रियत्व आदि जातिधर्म अथवा उससे युक्त त्रस आदि अविरुद्ध धर्म तथा तद्वान् जीव इस तरह तीन अर्थ बताये हैं।
इसका कारण उन धर्मों में पाई जाने वाली सदृशता है जैसा कि आगे की गाथा में बताया गया।
इस गाथा में प्रयुक्त ‘‘अणेय’’ शब्द का अर्थ ‘‘अज्ञेया’’ ऐसा भी होता है जिससे अभिप्राय यह बताया गया है कि यद्यपि संसारी प्राणियों को जीव द्रव्य अज्ञेय है, फिर भी जिन सदृश धर्मों के द्वारा उनका बोध हो सकता है उनको ही जीवसमास कहते हैं। इस शब्द की निरूक्ति इस तरह होती है कि जीवा: समस्यन्ते-संक्षिप्यन्ते-संगृहयन्ते यै: धर्मैस्ते जीवसमासा:’’। अर्थात् अज्ञेया होने पर भी जिन एकेन्द्रियत्व बादरत्व आदि धर्मों के द्वारा संग्रहरूप में अनेकों जीवों और उनकी विविध जातियों का निश्चय हो सके, उनको ही जीवसमास कहते हैं।
संक्षेप से जीवसमास के चौदह भेदों को गिनाते हैं
बादरसुहुमेइंदिय, वितिचउिंरदिय असण्णिसण्णी य।
पज्जत्तापज्जत्ता, एवं ते चोद्दसा होंति।।२८।।
बादरसूक्ष्मैकेन्द्रियद्वि त्रिचतुरिन्द्रियासंज्ञिसंज्ञिनश्च।
पर्याप्तापर्याप्ता एवं ते चतुर्दश भवन्ति।।२८।।
अर्थ—एकेन्द्रिय के दो प्रकार हैं—बादर और सूक्ष्म तथा विकलत्रय के तीन भेद हैं-द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय और चतुरिन्द्रिय। पंचेन्द्रिय के दो भेद हैं—संज्ञिपंचेन्द्रिय और असंज्ञिपंचेन्द्रिय। इस तरह ये सातों ही प्रकार के जीव पर्याप्त और अपर्याप्त दोनों ही तरह के हुआ करते हैं इसलिये जीवसमास के सामान्यतया सब मिलकर चौदह भेद होते हैं।
भावार्थ —यहाँ पर जो ये जीवसमास के चौदह भेद गिनाये हैं वे संक्षेप में और सामान्यरूप से ही बताये हैं तथा इन भेदों को बताने का यह एक प्रकार हैै किन्तु जीवसमास का जो लक्षण बताया गया है उसके अनुसार प्रकारान्तरों से भी जीवसमास के भेद हो सकते हैं। जैसा कि इस जीवकाण्ड के कर्ता श्री नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती के उक्त लक्षणानुसार द्रव्यसंग्रह ग्रंथ में गुणस्थानों को, जिनका कि यहाँ पर पहले वर्णन किया जा चुका है तथा मार्गणाओं को भी, जिनका कि यहाँ आगे वर्णन किया जाएगा, जीवसमास के ही भेद बताया है। इसके सिवाय स्थावर के पाँच भेद और त्रस के चार भेद इस तरह मिलाकर जीवसमास के नौ भेद भी बताये हैं। षट्खंडागम में भी गुणस्थानों के लिए जीवसमास शब्द का प्रयोग किया गया है।
आकृतियोनि के भेद
संखावत्तयजोणी, कुम्मुण्णयवंसपत्तजोणी य।
तत्थ य संखावत्ते, णियमा दु विवज्जदे गब्भो।।२९।।
शंखावर्तकयोनि:, कूर्मोन्नतवंशपत्रयोनी च।
तत्र च शंखावर्ते, नियमात्तु विवर्ज्जयते गर्भ:।।२९।।
अर्थ—आकृति योनि के तीन भेद हैं—१. शंखावर्त, २. कूर्मोन्नत, ३. वंशपत्र। इनमें से शंखावर्त योनि में गर्भ नियम से वर्जित है।
भावार्थ —जिसके भीतर शंख के समान चक्कर पड़े हों उसको शंखावर्त योनि कहते हैं। जो कछुआ की पीठ की तरह उठी हुई हो उसको कूर्मोन्नत योनि कहते हैं। जो बाँस के पत्ते के समान लम्बी हो उसको वंशपत्र योनि कहररते हैं। ये तीन तरह की आकार योनि हैं, इनमें से पहली शंखावर्त योनि में नियम से गर्भ नहीं रहता।
कुम्मुण्णयजोणीये, तित्थयरा दुविहचक्कवट्टी य।
रामा वि य जायंते, सेसाए सेसगजणो दु।।३०।।
कूर्मोन्नतयोनौ, तीर्थकरा द्विविधचक्रवर्तिनश्च।
रामा अपि च जायन्ते, शेषायां शेषकजनस्तु।।३०।।
अर्थ—कूर्मोन्नत योनि में तीर्थंकर, चक्रवर्ती, अर्धचक्री व बलभद्र तथा अपि शब्द की सामर्थ्य से अन्य भी महान पुरुष उत्पन्न होते हैं। तीसरी वंशपत्र योनि में साधारण पुुरुष ही उत्पन्न होते हैं।
गुणयोनि के भेद
जम्मं खलु सम्मुच्छण, गब्भुववादा दु होदि तज्जोणी।
सच्चित्तसीदसउडसेदर मिस्सा य पत्तेयं।।३१।।
जन्म खलु सम्मूर्छनगर्भोपपादास्तु भवति तद्योनय:।
सचित्तशीतसंवृतसेतरमिश्राश्च प्रत्येकम्।।३१।।
अर्थ—जन्म तीन प्रकार का होता है—सम्मूर्छन, गर्भ और उपपाद तथा सचित्त, शीत, संवृत और इनसे उल्टी अचित्त, उष्ण, विवृत तथा तीनों की मिश्र, इस तरह तीनों ही जन्मों की आधारभूत नौ गुणयोनि हैं। इनमें से यथासम्भव प्रत्येक योनि को सम्मूर्छनादि जन्म के साथ लगा लेना चाहिये।
भावार्थ —सामान्यतया गुणयोनि के ये नौ भेद हैं—सचित्त, अचित्त, मिश्र अर्थात् सचित्ताचित्त, शीत, उष्ण, मिश्र और संवृत, विवृत, मिश्र, सचित्त, शीत, संवृत, अचित्त, उष्ण, विवृत, सचित्ताचित्त, शीतोष्ण और संवृतविवृत।
चौरासी लाख योनि के भेद
णिच्चिदरधादुसत्त य, तरुदसवियलिंदियेसु छच्चेव।
सुरणिरयतिरियचउरो, चोद्दस मणुए सदसहस्सा।।३२।।
नित्येतरधातुसप्त च, तरुदश विकलेन्द्रियेषु षट् चैव।
सुरनिरयतिर्यक्चतस्र:, चतुर्दश मनुष्ये शतसहस्रा:।।३२।।
अर्थ—नित्यनिगोद, इतरनिगोद, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु इनमें से प्रत्येक की सात-सात लाख, तरु अर्थात् प्रत्येक वनस्पति की दश लाख, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय इनमें से प्रत्येक की दो-दो लाख अर्थात् विकलेन्द्रिय की सब मिलाकर छ: लाख, देव, नारकी, पंचेन्द्रिय तिर्यंच प्रत्येक की चार-चार लाख, मनुष्य की चौदह लाख, सब मिलाकर ८४ लाख योनि होती हैं।
कुल कोटी के भेद
एया य कोडिकोडी, सत्ताणउदी य सदसहस्साइं।
पण्णं कोडिसहस्सा, सव्वंगीणं कुलाणं य।।३३।।
एका च कोेटि कोटी, सप्तनवतिश्च शतसहस्राणि।
पंचाशत् कोटि सहस्राणि, सर्वांगिनां कुलानां च।।३३।।
अर्थ—इस प्रकार पृथिवीकायिक से लेकर मनुष्यपर्यन्त सम्पूर्ण जीवों के समस्त कुलों की संख्या एक कोड़ाकोड़ी तथा सत्तानवे लाख और पचास हजार कोटि है।
भावार्थ —सम्पूर्ण संसारी जीवों के कुलों की संख्या एक करोड़ सत्तानवे लाख पचास हजार को एक करोड़ से गुणा करने पर जितना प्रमाण लब्ध हो उतना अर्थात् १९७५०००००००००००० है। ग्रंथान्तरों में मनुष्यों के १४ लाख कोटि कुल गिनाये हैं। उस हिसाब से सम्पूर्ण कुलों का जोड़ एक करोड़ निन्यानवे लाख पचास हजार कोटि होता है।
जीवसमास प्ररूपणा सार
जीवसमास—जिनके द्वारा अनेक जीव अथवा जीव की अनेक जातियों का संग्रह किया जावे, उन्हें जीवसमास कहते हैं।
चौदह जीवसमास
—एकेन्द्रिय के दो भेद हैं—बादर और सूक्ष्म तथा विकलेन्द्रिय के तीन भेद हैं—दो इन्द्रिय, त्रीन्द्रिय और चतुरिन्द्रिय। पंचेन्द्रिय के दो भेद हैं—संज्ञी पंचेन्द्रिय और असंज्ञी पंचेन्द्रिय। इस तरह ये सातों ही जीवसमास पर्याप्त और अपर्याप्त दोनों तरह के होते हैं इसलिये जीवसमास के सामान्यतया चौदह भेद होते हैं।
सत्तावन जीवसमास—
पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, नित्यनिगोद, इतरनिगोद। इन छह के बादर और सूक्ष्म से १२ भेद हुए। प्रत्येक वनस्पति के दो भेद हैं—सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित। त्रस के ५ भेद हैं—दो इंद्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, असंज्ञि पंचेन्द्रिय और संज्ञि पंचेन्द्रिय। ये सब मिला कर उन्नीस भेद हुए। यथा—१२+२+५·१९। ये सभी भेद पर्याप्त निर्वृत्यपर्याप्त एवं लब्ध्यपर्याप्त के भेद से तीन-तीन प्रकार के होते हैं।
इसलिये १९ का ३ के साथ गुणा करने पर ५७ भेद हो जाते हैं। यथा १९x३=५७।
अट्ठानवे जीवसमास—
जीवसमास के उक्त ५७ भेदों से पंचेन्द्रिय के ६ भेद निकाल दीजिये अर्थात् पंचेन्द्रिय के संज्ञी, असंज्ञी दो मेें पर्याप्त, निर्वृत्यपर्याप्त और लब्ध्यपर्याप्त से गुणा कर दीजिये तो २x३=६ भेद होते हैं। ५७ में से ६ के निकल जाने से ५७-६·५१ बचे हैं।
कर्मभूमि पंचेन्द्रिय तिर्यंचों के गर्भज और सम्मूच्र्छन दो भेद होते हैं। गर्भज के जलचर, स्थलचर, नभचर ऐसे तीन भेद हैं और इनमें संज्ञी, असंज्ञी से दो भेद होने से २x३=६ भेद हो गये, पुन: इनके पर्याप्त और निर्वृत्यपर्याप्त दो भेद करने से ६x२·१२ भेद हो जाते हैं। पंचेन्द्रिय सम्मूच्र्छन के जलचर, स्थलचर, नभश्चर। इनके संज्ञी-असंज्ञी दो भेद किये तो ३x२=६। इन ६ को पर्याप्त, निर्वृत्यपर्याप्त और लब्ध्यपर्याप्त इन तीन से गुणा करने पर ६x३=१८ भेद हो गये ऐसे कर्मभूमिज पंचेन्द्रिय तिर्यंचों के १२+१८·३० भेद हो गये।
भोगभूमि में पंचेन्द्रिय तिर्यंचों के स्थलचर-नभचर दो ही भेद होते हैं, ये दोनों ही पर्याप्त, निर्वृत्यपर्याप्त ही होते हैं इसलिये २x२=४ भोगभूमिज के ४ भेद हुये क्योंकि भोगभूमि में जलचर, सम्मूर्च्छन तथा असंज्ञी जीव नहीं होते हैं।
आर्यखंड के मनुष्यों के पर्याप्त, निर्वृत्यपर्याप्त और लब्ध्यपर्याप्त ये तीन भेद ही होते हैं। म्लेच्छ खंड में लब्ध्यपर्याप्तक को छोड़कर दो ही भेद होते हैं। इसी प्रकार भोगभूमि, कुभोगभूमि के मनुष्यों के पर्याप्त, निर्वृत्यपर्याप्त दो ही भेद हैं। देव और नारकियों के भी ये ही दो भेद होते हैं। इस तरह सब मिलाकर अट्ठानवे भेद होते हैं। यथा—एकेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय संबंधी ५१, कर्मभूमिज पंचेन्द्रिय तिर्यंचों के ३०, भोगभूमिज तिर्यंचों के ४, आर्यखंड के मनुष्यों के ३, म्लेच्छखण्ड के मनुष्यों के २, भोगभूमिज मनुष्यों के २, कुभोगभूमि के २, देवों के २, नारकियों के २ ऐसे—५१+३०+४+३+२+२+२+ २+२·९८ जीवसमास होते हैं।
जीवसमास के अवांतर भेदों को समझने के लिए चार अधिकार—
स्थान, योनि, शरीर की अवगाहना और कुलों के भेद इन चार अधिकारों के द्वारा जीवसमास को विशेष रूप से जानना चाहिए।
स्थान—एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय आदि जाति भेद को अथवा एक, दो, तीन, चार आदि जीव के भेदों को स्थान कहते हैं।
योनि—जीवों की उत्पत्ति के आधार को योनि कहते हैं।
अवगाहना—शरीर के छोटे-बड़े भेदों को अवगाहना कहते हैं।
कुल—भिन्न-भिन्न शरीर की उत्पत्ति के कारणभूत नोकर्मवर्गणा के भेदों को कुल कहते हैं।
जीवस्थान के भेद—सामान्य से जीव का एक ही भेद है क्योंकि ‘‘जीव’’ कहने से जीवमात्र का ग्रहण हो जाता है अत: सामान्य से जीव- समास का एक भेद, त्रस-स्थावर से दो भेद, एकेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय, सकलेन्द्रिय से तीन भेद, एकेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय, संज्ञी-असंज्ञी पंचेन्द्रिय से चार भेद, पाँच इंद्रियों की अपेक्षा पाँच भेद, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति और त्रस ऐसे षट्काय की अपेक्षा से छह भेद, पाँच स्थावर विकलेन्द्रिय, सकलेन्द्रिय से सात भेद, पाँच स्थावर, विकलेन्द्रिय, संज्ञी, असंज्ञी से आठ भेद, पाँच स्थावर, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, पंचेन्द्रिय से नौ भेद, पाँच स्थावर, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, संज्ञी-असंज्ञी पंचेन्द्रिय से दस भेद ऐसे ही उन्नीस तक भेद करते चलिये।
पूर्वोक्त १९ को पर्याप्त-अपर्याप्त से गुणा करने से १९x२=३८ भेद एवं १९ को पर्याप्त-निर्वृत्यपर्याप्त से गुणा करने पर १९x३=५७ भेद होते हैं एवं पूर्वोक्त प्रकार से ९८ तक भेद हो जाते हैं इन्हें जीवसमासों के स्थान कहते हैं।
योनि भेद—योनि के मुख्य दो भेद हैं—आकार योनि, गुण योनि।
आकार योनि के भेद—शंखावर्त, कूर्मोन्नत और वंशपत्र ये तीन भेद हैं।
जिसके भीतर शंख के समान चक्कर पड़े हों उसे शंखावर्त कहते हैं, इसमें नियम से गर्भ वर्जित है। यह योनि चक्रवर्ती की पट्टरानी की होती है।
जो कछुए की पीठ की तरह उठी हो उसे कूर्मोन्नत योनि कहते हैं, इस योनि में तीर्थंकर, चक्रवर्ती, अर्धचक्री, बलभद्र तथा अन्य भी महान पुरुष उत्पन्न होते हैं अर्थात् इनकी माताओं की यही योनि होती है।
जो बाँस के पत्ते के समान लम्बी हो उसे वंशपत्र योनि कहते हैं। इसमें साधारण जन ही उत्पन्न होते हैं।
जन्म तथा उनके आधारभूत गुणयोनि के भेद
जन्म के तीन भेद—सम्मूर्छन, गर्भ और उपपाद। इन जन्मों के आधारभूत योनि के नौ भेद हैं—सचित्त, शीत, संवृत, अचित्त, उष्ण, विवृत्त, सचित्ताचित्त, शीतोष्ण और संवृतविवृत।
सामान्य से योनि के ये नौ भेद हैं एवं विस्तार से ८४,००,००० भेद होते हैं। यथा—नित्य निगोद, इतर निगोद, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु इनमें से प्रत्येक की सात-सात लाख, वनस्पति की दस लाख, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय इनमें से प्रत्येक की दो-दो लाख, देव, नारकी, पंचेन्द्रिय तिर्यंच प्रत्येक की चार-चार लाख, मनुष्य की चौदह लाख, सब मिलाकर ६X७=४२±१०±६±१२±१४·८४ लाख योनियाँ होती हैं।
तात्पर्य—अनादिकाल से प्रत्येक प्राणी इन चौरासी लाख योनियों में परिभ्रमण कर रहा है। जब यह जीव रत्नत्रय को प्राप्त करता है तभी चौरासी लाख योनि के चक्कर से छुटकारा पा सकता है अन्यथा नहीं, ऐसा समझकर जल्दी से जल्दी सम्यग्दृष्टि बनकर सम्यक्चारित्र को ग्रहण कर लेना चाहिए।
कहाँ कौन सा जन्म होता है?
देवगति और नरकगति में उपपाद जन्म होता है। मनुष्य तथा तिर्यंचों में यथासंभव गर्भज और सम्मूर्च्छन दोनों ही जन्म होते हैं। लब्ध्यपर्याप्तक मनुष्य तथा एकेन्द्रिय एवं विकलेन्द्रिय का नियम से सम्मूर्च्छन जन्म ही होता है। कर्मभूमियाँ पंचेन्द्रिय तिर्यंच गर्भज, सम्मूर्च्छन दोनों ही होते हैं। उपपाद और गर्भ जन्म वाले नियम से लब्ध्यपर्याप्तक नहीं होते हैं। सम्मूर्च्छन मनुष्य नियम से लब्ध्यपर्याप्तक ही होते हैं। चक्रवर्ती की पट्टरानी आदि को छोड़कर शेष आर्यखण्ड की स्त्रियों की योनि, कांख, स्तन, मूत्र, मल आदि में ये लब्ध्यपर्याप्त सम्मूर्च्छन मनुष्य उत्पन्न होते हैं। विषयों में अति आशक्त, परस्त्रीलंपट, वेश्यागामी, निंद्य, पापी जीव मरकर इन सम्मूर्च्छन मनुष्यों में जन्म लेते हैं। इनके मनुष्यायु, मनुष्यगति नामकर्म का उदय है किन्तु पर्याप्तियाँ पूर्ण न होेने से शरीर के योग्य परमाणुओं को ग्रहण ही नहीं कर पाते हैं और मर जाते हैं, इनकी आयु लघु अंतर्मुहूर्त प्रमाण है अर्थात् एक श्वांस में अठारहवें भाग प्रमाण है।
अवगाहना के भेद
उत्पन्न होने से तीसरे समय में सूक्ष्मनिगोदिया लब्ध्यपर्याप्त जीव की घनांगुल के असंख्यातवें भाग प्रमाण शरीर की जघन्य अवगाहना कहलाती है अर्थात् ऋजुगति के द्वारा उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म-निगोदिया लब्ध्यपर्याप्तक जीव की उत्पत्ति से तीसरे समय में शरीर की जघन्य अवगाहना होती है और इसका प्रमाण घनांगुल के असंख्यातवें भाग प्रमाण है। उत्कृष्ट अवगाहना स्वयंभूरमण समुद्र के मध्य में होने वाले महामत्स्य की होती है। इस मत्स्य का प्रमाण हजार योजन लम्बा, पाँच सौ योजन चौड़ा, ढाई सौ योजन मोटा है। जघन्य से लेकर उत्कृष्टपर्यंत मध्य में एक-एक प्रदेश की वृद्धि के क्रम से मध्यम अवगाहना के अनेकों भेद होते हैं।
सूक्ष्मनिगोदिया लब्ध्यपर्याप्तक की जघन्य अवगाहना घनांगुल के असंख्यातवें भाग है। पर्याप्त द्वीन्द्रिय की जघन्य अवगाहना अनुन्धरी जीव की घनांगुल के संख्यातवें भाग, त्रीन्द्रिय कुंथु की इससे संख्यातगुणी अधिक, चतुरिन्द्रिय काणमक्षिका की इससे संख्यातगुणी अधिक एवं पंचेन्द्रिय सिक्थक मत्स्य की इससे संख्यातगुणी अधिक है।
उत्कृष्ट अवगाहना एकेन्द्रिय में कमल की कुछ अधिक हजार योजन, द्वीन्द्रिय शंख की बारह योजन, त्रीन्द्रिय चींटी की तीन कोश, चतुरिन्द्रिय भ्रमर की एक योजन, पंचेन्द्रिय महामत्स्य की एक हजार योजन है पहले जो महामत्स्य की अवगाहना उत्कृष्ट एक हजार योजन बतलाई है और यहाँ कमल की कुछ अधिक एक हजार योजन कहा है उसमें कमल की अपेक्षा महामत्स्य का घनक्षेत्र अधिक होता है इसलिये उसे ही अधिक समझना चाहिए।
