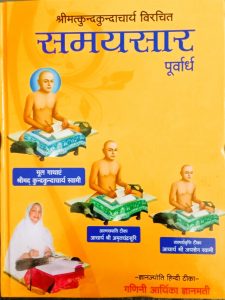क्या कर्मों का उदय कुछ भी बिगाड़ नहीं कर
सकता है?
(समयसार ग्रंथ के आधार से)
समयसार में आस्रव अधिकार में भगवान कुंदकुंददेव कहते हैं कि मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग ये चार बंध के कारण रूप आस्रव हैं जो कि चेतना के और जड़ पुद्गल के विकार रूप से दो-दो प्रकार के हैं। उनमें से जो जीव के विकार रूप हैं वे मिथ्यात्व, राग, द्वेष आदि परिणाम जीव से अभिन्न रूप हो रहे हैं और जो मिथ्यात्व आदि रूप पौद्गलिक कर्मवर्गणायें हैं जो कि ज्ञानावरणादि रूप कर्मों के बंध के कारण हैं और इन मिथ्यात्व आदि भावों के लिए रागादि भाव सहित संसारी जीव ही कारण हैं क्योंकि जीव को छोड़कर अन्यत्र ये राग-द्वेषादि नहीं पाए जाते हैं।
श्री जयसेनाचार्य तात्पर्यवृत्ति टीका में कहते हैं-
द्रव्यप्रत्यय के उदय होने पर जब यह जीव शुद्धात्मा स्वरूप की भावना को छोड़कर रागादि भाव से परिणमन करता है तब इसके कर्मों का बंध होता है किन्तु उदय मात्र से ही बंध नहीं होता है। यदि उदय मात्र से बंध माना जायेगा तब तो हमेशा संसार ही बना रहेगा। क्योें ? क्योंकि संसारी जीवों के सदा ही कर्मों का उदय विद्यमान रहता है।
‘‘तब१ तो कर्म का उदय बंध के लिए कारण नहीं रहा ?
ऐसा नहीं कहना, क्योंकि निर्विकल्प समाधि से भ्रष्ट हुए जीवों के मोहसहित कर्म का उदय व्यवहार से निमित्त रूप कारण होता है’’ अर्थात् आठवें, नवमें, दशवें अथवा ग्यारहवें, बारहवें गुणस्थानों में स्थित साधु निर्विकल्प ध्यान में लीन रहते हैं, उनके ही कर्मों का उदय बंध के लिये कारण नहीं होता है किन्तु उसके पूर्व छठे, पांचवें, चौथे आदि गुणस्थान तक मुनि अथवा श्रावकों के लिए तो कर्मों का उदय होने से बंध होता ही रहता है। हाँ, इतना अवश्य है कि असाता आदि कर्मों के उदय में अधिक संक्लेश न कर तत्व भावना करने वाले जीवों के कर्मों का बंध तीव्र न हो कर मंद हो सकता है किन्तु वीतराग निर्विकल्प समाधि से पहले जीव निर्बंध नहीं हो सकते हैं।
क्या रत्नत्रय भी बंध का कारण है ?
उसी का स्पष्टीकरण-
दंसणणाण चरित्तं, जं परिणमदे जहण्णभावेण।
णाणी तेण दु बज्झदि, पुग्गलकम्मेण विविहेण।।१८०।।
दर्शन, ज्ञान और चारित्र ये तीनों जब एक जघन्य अवस्था से परिणमन करते हैं अर्थात् यथाख्यात अवस्था को नहीं प्राप्त होते हैं, तब तक ज्ञानी जीव भी नाना प्रकार के पौद्गलिक कर्मों से बंधता ही रहता है।
तात्पर्यवृत्ति में श्री जयसेनाचार्य कहते हैं-
ज्ञानी जीव इच्छापूर्वक किसी भी वस्तु के प्रति रागादि विकल्प को कभी नहीं करता है इसलिए बुद्धिपूर्वक रागादि नहीं होने से वह निरास्रव ही होता है किन्तु जब तक उस ज्ञानी जीव को भी परमसमाधि का अनुष्ठान नहीं हो पाता है तब तक वह भी शुद्धात्मा के स्वरूप को देखने में, जानने में और वहाँ स्थिर रहने में असमर्थ होता है अत: तब तक उसका दर्शन, ज्ञान और चारित्र गुण भी जघन्य भाव से अर्थात् कषाय सहित भाव से इच्छा बिना भी परिणमन करता रहता है। इस कारण से वह-
‘भेदज्ञानी स्वकीयगुणस्थानानुसारेण १ परंपरया मुक्तिकारणभूतेन तीर्थंकर नामकर्म प्रकृत्यादि पुद्गलरूपेण विविधपुण्यकर्मणा बध्यते।’
भेदज्ञानी जीव भी परम्परा से मुक्ति के लिये कारणभूत ऐसे तीर्थंकर नामकर्म आदि रूप पुद्गल प्रकृतिमय नाना प्रकार के पुण्यकर्म से अपने-अपने गुणस्थान के अनुसार बंधता ही रहता है।’
निष्कर्ष यह निकला कि ये ज्ञान, दर्शन और चारित्र जब तब कषाय से अनुरंजित हैं तब तक ये अपने- अपने गुणस्थान के अनुरूप पुण्यकर्म रूप बंध को कराते रहते हैं। आठवें गुणस्थान के कुछ भाग तक आहारकद्विक और तीर्थंकर जैसी पुण्य प्रकृतियाँ बंधती रहती हैं। यहाँ टीकाकार ने तीर्थंकर आदि प्रकृतियों को परंपरा से मुक्ति के लिये कारण माना हैै। यह बात विशेष रूप से ध्यान में रखने योग्य है।
क्या आत्मा के दर्शन और ज्ञानगुण भी बंध के कारण हो सकते हैं ?-
चउविह अणेयभेयं बंधंते णाणंदंसणगुणेहिं।
समये समये जहना तेण अबधुत्ति णाणी दु।।१७८।।
मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग ये चार बंध के कारण हैं। ये आत्मा के ज्ञान और दर्शन गुण के द्वारा समय-समय पर अनेक प्रकार के नवीन कर्मों को बांधते रहते हैं इसलिये ज्ञानी तो स्वयं अबंधक ही है।
टीकाकार श्री जयसेनाचार्य कहते हैं-
‘‘२दर्शनज्ञानगुणौ कथं बंध कारणभूतौ भवत:? इति चेत् अयमत्र भाव:, द्रव्यप्रत्यया उदयमागता संतो जीवस्य ज्ञानदर्शनगुणद्वयं रागाद्यज्ञानभावेन परिणमयंति, तदा रागाद्यज्ञानभावपरिणतं ज्ञानदर्शन गुणद्वयं बंधकारणं भवति। वस्तुतस्तु रागाद्यज्ञानभावपरिणतं ज्ञानदर्शनगुणद्वयं, अज्ञानमेव भण्यते तत्।’
यदि कोई शंका करे कि ज्ञान और दर्शन तो आत्मा के गुण हैं पुन: वे बंध के कारण वैâसे हो सकते
हैं ? उसका समाधान करते हैं कि उदय में आए हुए मिथ्यात्व आदि प्रत्यय आत्मा के ज्ञान और दर्शन गुण को रागादिमय अज्ञान भाव के रूप में परिणमा देते हैं। उस समय वह अज्ञान भाव में परिणत हुए ज्ञान और दर्शन बंध के कारण होते हैं। वास्तव में रागादि रूप अज्ञान भाव में परिणत हुए ज्ञान और दर्शन अज्ञान ही कहलाते हैं।
ये मिथ्यात्व आदि कारण प्रतिसमय ज्ञान, दर्शन गुण को रागादि रूप अज्ञान भाव से परिणत करके नवीन-नवीन कर्मों को बंध करते रहते हैं।
निष्कर्ष यह निकला कि संसार अवस्था में मिथ्यात्व, अविरति, कषायादि द्रव्य पुद्गलवर्गणारूप कर्म उदय में आकर जीव के ज्ञान, दर्शन गुण को विकारी-रागादि अज्ञान रूप बना देत्ो हैं, इन्हीं का नाम भावकर्म है। इन्हीं भाव कर्मों से पुन: द्रव्य कर्मों का बंध होता रहता है। यही कारण है कि ज्ञान, दर्शन गुण ही अज्ञान रूप होकर जीव के घातक बने रहे हैं। सचमुच में दूध पौष्टिक होते हुए भी विष के संसर्ग से प्राणघातक हो जाता है।
सत्ता में बैठे हुए द्रव्य कर्म बंध के कारण नहीं हैं-
पूर्व की सराग दशा में बांधे गये मिथ्यात्व३ आदि द्रव्य कर्म वीतराग-सम्यग्दृष्टि जीव के सत्ता में विद्यमान रहते हैं वे कुछ नहीं कर सकते हैं किन्तु वे ही जब उदय में आते हैं तब जीव में रागादि भाव उत्पन्न करके नूतन कर्म बंध करने वाले हो जाते हैं। जैसे-पुरुष के लिए बाल कन्या उपभोग योग्य नहीं होती है वैसे ही उदय से पहले अनुदय में रहने वाले पूर्वबद्ध कर्मफल कारक नहीं होते हैं किन्तु उदय काल में वे ही सब कर्म फलकारक होने से आत्मा में रागादि विकार पैदा करके नवीन-नवीन कर्मों का बंध करा देते हैं। जैसे कि तरुण स्त्री पुरुष के भोग्य हो जाया करती है। अभिप्राय यह है कि बिना रागादि भाव के द्रव्य कर्म विद्यमान होते हुए भी कर्मबंध के कारण नहीं होते इसलिए सम्यग्दृष्टि जीव अबंधक माना गया है। यहाँ पर मुख्य रूप से वीतराग सम्यग्दृष्टि की विवक्षा है किन्तु गौण रूप से सराग सम्यग्दृष्टि चतुर्थ, पंचम गुणस्थानवर्ती आदि भी अपने-अपने गुणस्थान के योग्य ७७, ६७ आदि प्रकृतियों के बंधक होते हुए भी ४३, ५३ आदि प्रकृतियों के अबंधक हो जाते हैं, ऐसा समझना।
बंध-अबंध की व्यवस्था को समझने के लिए गोम्मटसार कर्मकांड, पंचसंग्रह आदि ग्रंथों का स्वाध्याय अवश्य करना चाहिए।