मुनिधर्म का कथन
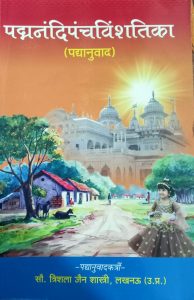
आचारो दशधर्मसंयमतपोमूलोत्तराख्यागुणा: मिथ्यामोहमदोज्झनं शमदमध्यानप्रमादस्थिति:।
वैराग्यं समयोपवृंहणगुणा रत्नत्रयं निर्मलं, पय्र्यन्ते च समाधिरक्षपदानन्दाय धर्मो यते: ।।३८।।
अर्थ—जनधर्म में दर्शनाचार, ज्ञानाचार, चारित्राचार, तप आचार, वीर्याचार इस प्रकार पांच प्रकार के आचार तथा उत्तमक्षमा, उत्तममार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम सत्य, उत्तम शौच, उत्तम संयम, उत्तमतप, उत्तम त्याग, उत्तम आविंâचन्य तथा उत्तमब्रह्मचर्य इस प्रकार का दश धर्म तथा बारह प्रकार का संयम तथा बारह प्रकार का तप और आठ प्रकार के मूलगुण तथा चौरासी लाख उत्तरगुण तथा मिथ्यात्व मोह मद का त्याग और शम दम ध्यान तथा प्रमाद रहित स्थिति और वैराग्य तथा जिन शासन की महिमा के बढ़ाने वाले अनेक गुण और सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान सम्यक्चारित्र स्वरूप निर्मलरत्नत्रय तथा अंत में समाधि विद्यमान हैं ऐसा मुनियों का धर्म अक्षयपद आनन्द के लिये है।।३८।।
स्वं शुद्धं प्रविहाय चिद्गुणमयभ्रान्त्याणुमात्रेऽपि यत् संबन्धाय मति: परे भवति तद्वंधाय मूढात्मन:।
तस्मात्त्याज्यमशेषमेव महतामेतच्छरीरादिवंâ तत्कालादि विनादियुक्तित: इदं तत्त्यागकर्मव्रतम् ।।३९।।
अर्थ—अपने शुद्धचैतन्य को छोड़कर परमाणुमात्र पर पदार्थों में भी चैतन्य गुण के भ्रम से यदि मूढ़ पुरूषों की बुद्धि लग जावे तो उस बुद्धि से केवल कर्मबंध ही होता है इसलिये सज्जन पुरूषों को शरीर आदि के समस्तपदार्थों का अवश्य त्याग कर देना चाहिये यदि आयु: कर्म के प्रबल होने से शरीरादि का त्याग न हो सके तो शरीरादि के त्याग करने के लिये मुनिव्रत ही धारण करने योग्य है क्योंकि मुनिव्रत धारण करना ही शरीर आदि के त्याग की क्रिया है।।३९।।
मुक्तवा मूलगुणान्यतेर्विदधत: शेषेषु यत्रं परं दण्डो मूलहरो भवत्यविरतं पूजादिवंâ वाञ्छत:।
एवं प्राप्तमरे: प्रहारमतुलं हित्वा शिरश्छेदवंâ रक्षत्यङ्गुलिकोटिखण्डनकरं कोऽन्यो नरो बुद्धिमान्।।४०।।
अर्थ—युद्ध करते समय अनेक प्रकार के प्रहार होते हैं उनमें कई एक तो शिर के छेदने वाले होते हैं तथा कई एक अंगुलि के अग्रभाग के छेदने वाले होते हैं उनमें यदि कोई पुरूष शिर के छेदने वाले प्रहार को छोडकर अंगुली के अग्रभाग को छेदन करने वाले प्रहार से रक्षा करे तो उसका जिस प्रकार उससे रक्षा करना व्यर्थ है उसी प्रकार जो यति मूलगुणों को छोड़कर शेष उत्तरगुणों के पालन करने के लिये प्रयत्न करते हैं तथा निरंतर पूजा आदि को चाहते है उनको आचार्य मूलछेदक दण्ड देते हैं इसलिये मुनियों को प्रथम मूलगुणव्रत पालना चाहिये पीछे उत्तरगुणों का पालन करना चाहिये।।४०।।
आचेलक्य मूलगुण किसलिये पाला जाता है इस बात को आचार्य दिखाते हैं।
म्लाने क्षालनत: कुत: कृतजलाद्यारम्भत: संयमो नष्टे व्याकुलचित्तताथ महतामप्यन्यत: प्रार्थनम् ।
कौपीनेऽपि हृते परैश्च झटिति क्रोध: समुत्पद्यते तन्नित्यं शुचिरागहृच्छ्रमवतां वस्त्रं ककुम्मण्डलम् ।।४१।।
अर्थ—यदि संयमी वस्त्र रक्खे तो उसके मलिन होने पर धोने के लिये जल आदि का उनको आरंभ करना पड़ेगा और यदि जल आदि का आरम्भ करना पड़ा तो उनका संयम ही कहां रहा तथा यदि वह वस्त्र नष्ट हो गया तब उनके चित्त में व्याकुलता होगी तथा उसके लिये यदि वे किसी से प्रार्थना करेंगे तो उनकी अयाचक वृत्ति छूट जावेगी और वस्त्रों को छोड़कर यदि वे कौपीन (लँगोट) ही रक्खे तो भी उसके खोजने पर उनको क्रोध पैदा होगा इसलिये समस्तवस्त्रों का त्यागकर मुनिगणों का नित्य पवित्र राग का नाशक दिशा का मंडल ही वस्त्र है ऐसा समझना चाहिये।।४१।।
आचार्यवर लोचनामक मूलगुण को दिखाते हैं।
काकिण्या अपि संग्रहो न विहित: क्षौरं यया कार्यते चित्तक्षेपकृदस्रमात्रमपिवा तत्सिद्धये नाश्चितम् ।
हिंसाहेतुरहोजटाद्यपि तथा यूकाभिरप्रार्थनैर्वैराग्यादिविवर्धनाय यतिभि: केशेषु लोच: कृत:।।४२।।
अर्थ—मुनिगण अपने पास एक कौड़ी भी नहीं रखते जिससे कि वे दूसरे से मुंडन करा सवेंâ तथा मुंडन के लिये छुरा, वैंâची आदि अस्त्र भी नहीं रखते क्योंकि उनके रखने से क्रोधादि की उत्पत्ति से चित्त बिगड़ता है तथा वे जटा भी नहीं रख सकते क्योंकि जटाओं में अनेक जूं आदि जीवों की उत्पत्ति होती है इसलिये जटा रखने से हिंसा होती है तथा मुंडन कराने के लिये वे दूसरे से द्रव्य भी नहीं मांग सकते क्योंकि उनकी अयाचक वृत्ति का परिहार होता है इसलिये वैराग्य की अतिशय वृद्धि के लिये ही मुनिगण अपने हाथों से केशों को उपाटते हैं, इसमें अन्य कोई मानादि कारण नहीं है।।४२।।
अब आचार्य स्थितिभोजन नामक मूलगुण को बताते हैं।
यावन्मे स्थितिभोजनेऽस्ति दृढता पाण्योश्च संयोजने भुञ्जे तावदहंरहाम्यथ विधावेषा प्रतिज्ञा यते:।
कायेऽप्यस्पृहचेतसोऽन्त्यविधिषु प्रोल्लासिन:सन्मतेर्नह्येतेन दिविस्थितिर्न नरके सम्पद्यते तद्विना।।४३।।
अर्थ—जो मुनिगण अपने शरीर में भी ममत्वकार रहित है तथा समाधिमरण करने में उत्साही है तथा श्रेष्ठज्ञान के धारक हैं उनकी विधि में यह कड़ी प्रतिज्ञा रहती है कि जब तक हमारी खड़े होकर अहार लेने में तथा दोनों हाथों को जोड़ने में शक्ति मौजूद है तब तक हम भोजन करेंगे नहीं तो कदापि न करेंगे जिससे उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है तथा उनको नरक नहीं जाना पड़ता किन्तु जो इस प्रतिज्ञा से रहित है उनको अवश्य नरक जाना पड़ता है।।४३।।
और भी आचार्य मुनिधर्म का वर्णन करते हैं।
एकस्यापि ममत्वमात्मवपुष: स्यात्संसृते: कारणं कोवाह्यर्थकथाप्रथीयसि तथाप्याराध्यमानेऽपि च ।
तद्वासां हरिचंद्रनेऽपि च सम:संश्लिष्टतोऽप्यङ्गतो भिन्नं स्वं स्वयमेकमात्मनि धृतं यास्यत्यजस्त्रं मुनि:।।
अर्थ—वस्तीर्णतप के आराधन करने पर भी यदि एक अपने शरीर में भी ‘‘ यह मेरा है’’ ऐसा ममत्व हो जावे तो वह ममत्व ही संसार में परिभ्रमण का कारण हो जाता है तब यदि शरीर से अतिरिक्त धनधान्य में ममता की जावेगी तो वह ममता क्या न करेगी ? ऐसा जानकर तथा चाहे कोई उनके शरीर में कुल्हाड़ी मारे चाहे उनके शरीर में चन्दन का लेप करे तो भी कुल्हाड़ी और चंदन में सम होकर मुनिगण क्षीरनीर के समान आत्मा शरीर का संबंध होने पर भी अपने में अपने से अपने को निरंतर भिन्न ही देखते हैं।।४४।।
शिखरिणी छंद-
तृृणं वा रत्नं वा रिपुरथ परं मित्रमथवा सुखं वा दु:खं वा पितृबनमदो सौधमथवा ।
स्तुतिर्वा निन्दा वा मरणमथवा जीवितमथ स्पुâटं निग्र्रन्थानां द्वयमपि समं शान्तमनसाम् ।।४५।।
अर्थ—तथा उन शान्त रस के लोलुपी मुनियों के तृण तथा रत्न, मित्र और शत्रु, सुख तथा दु:ख , श्मशानभूमि और राज मन्दिर, स्तुति तथा निन्दा, मरण और जीवित दोनों समान है।
भावार्थ —जो मुनि परिग्रहकर रहित हैं तथा शान्त स्वरूप है वे तृण से घृणा भी नहीं करते हैं तथा रत्न को अच्छा भी नहीं समझते हैं और अपने हित के करने वाले को मित्र नहीं समझते हैं तथा अहित के करने वाले को वैरी नहीं समझते है तथा सुख होने पर सुख नहीं मानते हैं दु:ख होने पर दु:ख नहीं मानते हैं और श्मशान भूमि को बुरी नहीं कहते है तथा राजमन्दिर को अच्छा नहीं कहते हैं तथा स्तुति होने पर संतुष्ट नहीं होते हैं तथा निन्दा होने पर रूष्ट नहीं होते हैं तथा जीवित मरण को समान मानते हैं।।४५।।
वीतरागी इस प्रकार का विचार करते हैं।
वयमिह निजयूथभ्रष्टसारङ्गकल्पा: परपरिचयभीता: क्वापि विंâचिच्चराम:।
विजनमधिवसामो न व्रजाम: प्रमादं सुकृतमनुभवामो यत्र तत्रोपविष्टा:।।४६।।
अर्थ—जिस प्रकार मृग अपने समूह से जुदा होकर तथा दूसरों से भयभीत होकर जहां तहां विचरता फिरता है तथा एकान्त में रहता है तथा प्रतिसमय प्रतिबुद्ध रहता है और जहां तहां बैठकर आनन्द भोगता है उसी प्रकार हमारे लिये भी वह कौन सा दिन आवेगा जिस दिन हम अपने कुटुम्बियों से जुदे होकर तथा फिर उन से परिचय न हो जावे इससे भयभीत होकर हम भी यहां वहां विचरेंगे तथा एकान्तवास में रहेंगे और प्रमादी न बनेेंगें , तथा जहां तहां बैठकर अपने आत्मानंद का अनुभव करेंगे।।४६।।
और भी वीतरागी इस प्रकार भावना करते रहते हैं।
कति न कति न वारान् भूपतिर्भूरिभूति: कति न कति न वारानत्र जातोऽस्मि कीट: ।
नियममिति न कस्याप्यस्ति सौख्यं न दु:खं जगति तरलरूपे विंâ मुदा िंक शुचा वा।।४७।।
अर्थ—इस संसार में कितनी—२ बार तो हम बड़ी—२ संपत्ति के धारी राजा न हो गये तथा कितनी—२ बार इसी संसार में हम क्षुद्र क्रीड़े न हो चुके इसलिये यही मालूम होता है कि चंचलरूप इस संसार में किसी का सुख तथा दु:ख निश्चित नहीं है अत: सुख और दु:ख के होने पर हर्ष और विषाद कदापि नहीं करना चाहिये।।४७।।
पृथ्वी छंद-
प्रतिक्षणमिदं हृदि स्थितमतिप्रशान्तात्मनो मुनेर्भवति संवर: परमशुद्ध हेतुध्र्रुवम् ।
रज:खलु पुरातनं गलति नो नवं ढौकते ततोऽपि निकटं भवेदमृतधाम दु:खोज्झितम् ।।४८।।
अर्थ—परमशांत मुद्रा के धारी मुनियों के इस प्रकार उपर्युक्त भावना करने से परम शुद्धि का करने वाला संवर होता है तथा उसके होते सन्ते जो कुछ प्राचीन कर्म आत्मा के साथ लगे रहते हैं तब गल जाते हैं तथा नवीन कर्मों का आगमन भी बंद हो जाता है तथा उन मुनियों के लिये समस्त प्रकार के दु:खों कर रहित मुक्ति भी सर्वथा समीप रह जाती है।।४८।।
और भी आचार्य मुनिधर्म की महिमा का वर्णन करते हैं।
शिखरिणी छंद-
प्रबोधो नीरन्ध्रं प्रवहणममन्दं पृथुतप: सुवायुर्यै: प्राप्तो गुरूगणसहाया: प्रणयिन: ।
कियन्मात्रस्तेषां भवजलधिरेषोऽस्य च पर: कियद्दूरे पार: स्पुâरति महतामुद्यमवताम् ।।४९।।
अर्थ—जिन मुनियों के पास छिद्ररहित सम्यज्ञानरूपी जहाज मौजूद है, तथा अमन्द विस्तीर्ण तपरूपी पवन भी जिनके पास है तथा स्नेही बड़े—२ गुरू भी जिनके सहायी हैं उन उद्यमी महात्मा मुनियों के लिये यह संसाररूपी समुद्र कुछ भी नहीं है तथा इस संसाररूपी समुद्र का पार भी उनके समीप में ही है।
भावार्थ— जिस मनुष्य के पास छिद्ररहित जहाज तथा जहाज के लिये योग्य पवन तथा चतुर खेवटिया होते हैं वह मनुष्य बात की बात में समुद्र की चौरस को तय कर लेता है उसी प्रकार जो मुनि सम्यग्ज्ञान के धारक हैं तथा विस्तीर्ण तप के करने वाले हैं, और जिनके बड़े—२ गुरू भी सहायी हैं वे मुनि शीघ्र ही संसार समुद्र से तर जाते हैं तथा मोक्ष उनके सर्वथा समीप में आ जाती है।।४९।।
आचार्य मुनियों को शिक्षा देते हैं।
वसंततिलका छंद-
अभ्यस्यतान्तरदृशं किमु लोकभक्तया मोहं कृशीकुरूत विंâ वपुषा कृशेन।
एतद्द्वयं यदि न विंâ बहुभिर्नियोगै: क्लेशैश्च विंâ किमपरै: प्रचुरैस्तपोभि:।।५०।।
अर्थ—भो मुनिगण ? आनन्दस्वरूप शुद्धात्मा का अनुभव करो लोक के रिझाने के लिये प्रयत्न मत करो तथा मोह को कृष करो शरीर के कृष करने में कुछ भी नहीं रक्खा है क्योंकि जब तक तुम इन दो बातों को न करोगे तब तक तुम्हारा यम नियम करना भी व्यर्थ है तथा तुम्हारा क्लेश सहना भी बिना प्रयोजन का है और तुम्हारे, नाना प्रकार के, किये हुवे तप भी व्यर्थ हैं।
भावार्थ—जब तक ज्ञान नन्दस्वरूप शुद्धात्मा का अनुभव न किया जायगा तथा मोह को कृष न किया जायगा तब तक बाह्य में तुम चाहे जितना यम नियम उपवास तप आदि करो सर्व तुम्हारे व्यर्थ हैं इसलिये सबसे प्रथम तुमको ज्ञानानन्दस्वरूप शुद्धात्मा का अनुभव करना चाहिये पीछे इन बातों पर ध्यान देना चाहिये।।५०।।
और भी आचार्य मुनिधर्म के स्वरूप का वर्णन करते है।।
वंशस्थ छंद-
जुगुप्सते संसृतिमत्र मायया तितिक्षते प्राप्तपरीषहानपि।
न चेन्मुनिर्दुष्टकषायनिग्रहाच्चिकित्सति स्वान्तमघप्रशान्तये ।।५१।।
अर्थ—जो मुनि सर्वथा आत्मा के अहित करने वाले दुष्ट कषायों को जीतकर पापों के नाश के लिये अपने चित्त को स्वस्थ बनाना नहीं चाहता वह मुनि समस्त लोक के सामने कपट से संसार की निन्दा करता है तथा कपट से ही वह क्षुधा तृषा आदि बाईस परीषहों को सहन करता है।
भावार्थ—संसार का त्याग तथा परीषहों को जीतना उसी समय कार्यकारी माना जाता है जबकि कषायों का नाश होवे तथा चित्त स्वस्थ रहे किन्तु जिन मुनियों का चित्त कषायों के नाश होने से शुद्ध ही नहीं हुवा है वे मुनि क्या तो संसार का त्याग कर सकते हैं ? तथा क्या वे परीषहों को ही सहन कर सकते हैं ; यदि ये संसार की निन्दा करे तथा परीषहों का सहन भी करे तो उनका वह सर्वकार्य ढोंग से किया हुवा ही समझना चाहिये। इसलिये मुनियों को चाहिये कि वे प्रथम कषाय आदि को नाशकर चित्तको शुद्ध बना लेवे पीछे संसार की निन्दा तथा परीषहों का सहन करे।।५१।।
शार्दूलविक्रीडित छंद-
हिंसा प्राणिषु कल्मषं भवति सा प्रारम्भत: सोऽर्थत: तस्मादेव भयादयोऽपि नितरां दीर्घा तत: संसृति: ।
तत्रासातमशेषमर्थत इदं मत्वेति यस्त्यक्तवान् मुक्त्यर्थी पुनरर्थमाश्रिवता तेनाहत: सत्पथ: ।।५२।।
अर्थ—प्राणियों को मारने से पाप होता है तथा वह पाप आरंभ से होता है और वह आरंभ धन के होते संते होता है तथा धन के होते संते लोभ आदि की उत्पत्ति होती है और लोभ आदि के होने से दीर्घ संसार होता है तथा संसार से अनन्त दु:ख होते हैं इस प्रकार से सब बातें द्रव्य से होती हैं इस बात को जानकर मोक्ष के अभिलाषी मुनियों ने द्रव्य का त्याग कर दिया है किन्तु जिसने धन को आश्रयण किया है उसने सच्चे मार्ग का नाश ही कर दिया है ऐसा समझना चाहिये।।५२।।
दुध्र्यानार्थमवद्यकारणमहो निग्र्रन्थताहानये शय्याहेतुतृणाद्यपि प्रशमिनां लज्जाकरं स्वीकृतम् ।
यत्तत्विंâ न गृहस्थयोग्यमपरं स्वर्णादिवंâ साम्प्रतं निग्र्रन्थेष्वपि चैतदस्ति नितरां प्राय: प्रवष्टि: कलि: ।।५३।।
अर्थ—आचार्य कहते हैं निग्र्रंथमुनि शय्या के कारण यदि घास आदि को भी स्वीकार कर लें वह स्वीकार भी उनके खोटे ध्यान के लिये होता है तथा निन्दा का करने वाला और निग्र्रंथता में हानि पहुंचाने वाला होता है तथा लज्जा को करने वाला भी होता है तब वे निर्ग्रंथ यतीश्वर गृहस्थ के योग्य सुवर्ण आदि को कब रख सकते हैं ? यदि इस काल में निग्र्रंथ सुवर्ण आदि को रक्खे तो समझना चाहिये कि यह कलिकाल का ही महात्म्य है।।५३।।
आर्या छंद-
कादाचित्को बंध: क्रोधादे: कर्मण: सदा सङ्गात् ।
नात: क्वापि कदाचित्परिग्रहग्रहवतां सिद्धि: ।।५४।।
अर्थ—और भी आचार्य कहते हैं कि क्रोधादि कर्मों के द्वारा तो प्राणियों के कर्मों का बंध कभी—२ ही होता है किन्तु परिग्रह से प्रतिक्षण बंध होता रहता है अतएव परिग्रह धारियों को किसी काल में तथा किसी प्रदेश में भी सिद्धि नहीं होती। इसलिये भव्यजीवों को कदापि धनधान्य से ममता नहीं रखनी चाहिये।।५४।।
इंद्रवज्रा छंद-
मोक्षऽपि मोहादभिलाषदोषो विशेषतो मोक्षनिषेधकारी।
यतस्ततोऽध्यात्मरतो मुमुक्षुर्भवेत्किमत्र कृताभिलाष: ।।५५।।
अर्थ—स्त्री पुत्र आदि की अभिलाषा का करना तो दूर रहो यदि मोक्ष के लिये भी अभिलाषा की जावे तो वह दोषस्वरूप समझी जाती है तथा इसलिये वह मोक्ष की निषेध करने वाली होती है। इसीलिये जो मुनि अपनी आत्मा के रस में लीन हैं तथा मोक्ष के अभिलाषी हैं वे स्त्री पुत्र आदि में कब अभिलाषा कर सकते हैं।
भावार्थ—मोह के उदय से ही पदार्थों में इच्छा होती है तथा जब तक मोह रहता है तब तक मोक्ष कदापि नहीं हो सकती इसलिये मोक्ष के लिये भी अभिलाषा करना दोष है अत: मोक्षाभिलाषी मुनियों को आत्म रस में ही लीन रहना चाहिये।।५५।।
पृथ्वी छंद-
परिग्रहवतां शिवं यदि तदानतल: शीतलो यदीन्द्रियसुखं सुखं तदिह कालवूâट: सुधा ।
स्थिरा यदि तनुस्तदा स्थिरतरं तडिच्चाम्बरे भवेऽत्र रमणीयता यदि तदीन्द्रजालेऽपि च ।।५६।।
अर्थ—यदि परिग्रहधारियों को भी मुक्ति कही जावेगी तो अग्नि को भी शीतल कहना पड़ेगा तथा यदि इन्द्रियों से पैदा हुवे सुख को भी सुख कहोगे तो विष को भी अमृत मानना पड़ेगा और यदि शरीर को स्थिर कहोगे तो आकाश में बिजली को भी स्थिर कराना पड़ेगा तथा संसार में रमणीयता कहोगे तो इन्द्रजाल में भी रमणीयता कहनी पड़ेगी। इसलिये इसबात को मानो कि जिस प्रकार अग्नि शीतल नहीं होती उसी प्रकार परिग्रहधारियों को कदापि मुक्ति नहीं हो सकती और जिस प्रकार विष अमृत नहीं होता उसी प्रकार इन्द्रियसुख भी कदापि सुख नहीं हो सकता तथा जिस प्रकार बिजली स्थिर नहीं होती उसी प्रकार यह शरीर भी स्थिर नहीं हो सकता तथा जिस प्रकार इन्द्रजाल में रमणीयता नहीं होती उसी प्रकार संसार में भी रमणीयता नहीं हो सकती।।५६।।
मालिनी छंद-
स्मरमपि हृदि येषां ध्यानवन्हिप्रदीप्ते सकलभुवनमल्लं दह्यमानं विलोक्य।
कृतभिय इव नष्टास्ते कषाया न तस्मिन्पुनरपि हि समीयु: साधवस्ते जयन्ति।।५७।।
अर्थ—वे यतीश्वर सदा इसलोक में जयवंत है कि जिन यतीश्वरों के हृदय में ध्यानरूपी अग्नि के जाज्वल्यमान होने पर तीनों लोक के जीतने वाले कामदेवरूपी प्रबल योधा को जलते हुवे देखकर भयसेही मानों भागे गये तथा ऐसे भागे कि फिर न आ सके।
भावार्थ—जिन मुनियों के सामने कामदेव का प्रभावहत हो गया है तथा जो अत्यंतध्यानी है और कषायों कर रहित है उन मुनियों के लिये सदा मैं नमस्कार करता हूँ।।५७।।
अब आचार्य गुरूओं की स्तुति करते हैं।
उपेन्द्रवज्रा छंद-
अनघ्र्यरत्नत्रयसम्पदोऽपि निग्र्रंथताया: पदमद्वितीयम् ।
जयन्ति शान्ता: स्मरवैरिवध्वा: वैघव्यदास्ते गुरवो नमस्या:।।५८।।
अर्थ—अमूल्य रत्नत्रयरूपी संपत्ति के धारी होकर भी जो निर्गं्रथ पद के धारक हैं तथा शान्तमुद्रा के धारी होने पर भी जो काम देव रूपी वैरी की स्त्री को विधवा करने वाले हैं ऐसे वे उत्तम गुरू सदा नमस्कार करने योग्य हैं।
भावार्थ—इस श्लोक में विरोधा भास नामक अलंकार है इसलिये आचार्य विरोधाभास को दिखाते हैं कि जिसके अमूल्य रत्नत्रय मौजूद है वह परिग्रह करके रहित वैâसे हो सकता है। तथा जो शान्त है वह कामदेव की स्त्री को विधवा वैâसे बना सकता है इसलिये ऐसे चमत्कारी गुरू सदा वन्दनीक ही है।
सारांश—जो रत्नत्रय के धारी हैं तथा निग्र्रंथ हैं और शान्त मुद्रा के धारक हैं तथा कामदेव के जीतने वाले हैं उन गुरूओं को सदा मैं मस्तक झुकाकर नमस्कार करता हूं।।५८।।
आचार्य परमेष्ठी की स्तुति
शार्दूलविक्रीडित छंद-
ये स्वाचारमपारसौख्यसुतरोर्वीजं परं पञ्चधा सद्वोधा: स्वयमाचरन्ति च परानाचारयन्त्येव च ।
ग्रंथग्रंथिविमुक्तमुक्तिपदवीं प्राप्ताश्च यै: प्रापितास्ते रत्नत्रयधारिण:शिवसुखं कुर्वन्तु न: सूरय: ।।५९।।
अर्थ—जो सद्ज्ञान के धारक आचार्य अपार जो सौख्यरूपी वृक्ष उसको उत्पन्न करने वाले पांच प्रकार के आचार को स्वयं आचारण करते हैं तथा दूसरों को आचरण कराते हैं तथा जहां पर किसी प्रकार के परिग्रह का लेश नहीं ऐसी मुक्ति को स्वयं जाते हैं और दूसरों को पहुंचाते हैं इसलिये इस प्रकार निर्मलरत्नत्रय के धारी आचार्यवर हमारे लिये मोक्ष सुख को प्रदान करो।।५९।।
वसंततिलका छंद-
भ्रान्तिप्रदेषु वहुवत्र्मसु जन्मकक्ष्ये पन्थानमेकममृतस्य परं नयन्ति ।
ये लोकमुन्नतधिय: प्रणमामि तेभ्यस्तेनाप्यहं जिगमिषुर्गुरूनायकेभ्य: ।।६०।।
अर्थ—इस संसार में भ्रम के करने वाले अनेक मार्गों में से जो गुरूलोक को सुख के देने वाले एक मोक्षमार्ग को ले जाते हैं तथा स्वयं उच्चज्ञान के धारक हैं ऐसे उन श्रेष्ठ गुरूओं को उसी मार्ग में जाने की इच्छा करने वाला मैं भी मस्तक झुकाकर नमस्कार करता हूँ।।६०।।
उपाध्याय परमेष्ठी की स्तुति
शार्दूलविक्रीडित छंद-
शिष्याणामपहाय मोहपटलं कालेन दीर्घेण यज्जातं ‘ स्यात्पदलाञ्छितोज्वलवचो—दिव्याञ्चनेन ’ स्पुâटम् ।
ये कुर्वन्ति दृशं परामतितरां सर्वावलोके क्षमां लोके कारणमन्तरेण भिषजस्ते पान्तुनोऽध्यापका:।।६१।।
अर्थ—जो उपाध्यायपरमेष्ठी अनादिकाल से लगे हुवे मोह के परदे को स्याद्वाद से अविरोधी ऐसे अपने उपदेशरूपी दिव्य अंजन से हटाकर शिष्यों की दृष्टि को अत्यंत निर्मल तथा समस्त पदार्थों के देखने में समर्थ बनाते हैं ऐसे बिना कारण के ही वैद्य वे उपाध्याय मेरी इस संसार में रक्षा करो।।६१।।साधु परमेष्ठी की स्तुति
शार्दूलविक्रीडित छंद-
उन्मुच्यालयबंधलनादपि दृढात्कायेऽपि वीतस्पृहाश्चित्ते मोहविकल्पजालमपि यद्दुर्भेद्यमन्तस्तम: ।
भेदायास्य हि साधयन्ति तदहो ज्योतिर्जितार्वâप्रभं ये सद्वोधमयं भवन्तु भवंता ते साधव: श्रेयसे।।६२।।
अर्थ—जो साधु परमेष्ठी अत्यन्तकठिन भी गृहरूपी बंधन से अपने को छुड़ाकर तथा अपने शरीर में भी इच्छारहित होकर कठिनता से भेदने योग्य ऐसे मोह से पैदा हुवे विकल्पों के समूह रूप भीतरी अंधकार के नाश करने के लिये सूर्य की प्रभा को भी नीची करने वाली सम्यग्ज्ञान रूपी ज्योति को निरन्तर सिद्ध करते रहते हैं। ऐसे उन साधु परमेष्ठी के लिये नमस्कार है अर्थात् वे मेरे कल्याण के लिये होवे।।६२।।
वीतराग की महिमा का वर्णन
वसंततिलका छंद-
वङ्को पतत्यपि भयद्रुतविश्वलोकमुक्ताध्वनि प्रशमिनो न चलन्ति योगात् ।
बोधप्रदीपहतमोहमहान्धकारा: सम्यग्दृश: किमुत शेषपरीषहेषु।।६३।।
अर्थ– जिस व्रज के शब्द के भय से चकित होकर समस्तलोक मार्ग को छोड़ देते हैं ऐसे वङ्का के गिरने पर भी जो शान्तात्मामुनि ध्यान से कुछ भी विचलित नहीं होते तथा जिन्होंने सम्यग्ज्ञानरूपीदीपक से समस्त मोहान्धकार को नाश कर दिया है और जो सम्यग्दर्शन के धारी हैं वे मुनि परीषहों के जीतने में कब चलायमान हो सकते हैं ? अर्थात् परीषह उनका कुछ भी नहीं कर सकते।।६३।।
ग्रीष्मऋतु में पर्वत के शिखर पर ध्यानीमुनीश्वरों की स्तुति—
प्रोद्यत्तिग्मकरोग्रतेजसि लसच्चण्डानिलोद्यद्दिशि स्फारीभूतसुतप्तभूमिरजसि प्रक्षीणनद्यम्भसि।
ग्रीष्मे ये गुरुमेधनीध्रशिरसि ज्योतिर्निधायोरसि ध्वान्तध्वंसकरं वसन्ति मुनयस्ते सन्तु न: श्रेयसे।।६४।।
अर्थ—जिस ग्रीष्म ऋतु में अत्यंत तीक्ष्ण धूप पड़ती है तथा चारों दिशाओं में भयंकर लू चलती है तथा जिस ऋतु में अत्यंत संताप का देने वाला गरम रेता पैâला हुवा है तथा नदियों का पानी सूख जाता है ऐसी भयंकर ग्रीष्मऋतु में जो मुनि समस्त अन्धकार को नाश करने वाली सम्यग्ज्ञान रूपी ज्योति को अपने मन में रखकर अत्यंत ऊंचे पहाड़ की चोटी पर निवास करते हैं उन मुनियों के लिये मेरा नमस्कार हो अर्थात् वे मुनि मेरे कल्याण के लिये होवे।।६४।। वर्षाकाल में वृक्षों के नीचे स्थित मुनियों की स्तुति
शार्दूलविक्रीडित छंद-
ते व: पान्तु मुमुक्षव: कृतरवेरब्दै रतिश्यामलै: शश्वद्वारि वमद्भिरब्धिविषयक्षारत्वदोषादिव।
काले मज्जदिले पतद्गिरिकुले ‘धावद्धुनीसंकुले’ झंझावातविसंस्थुले तरुतले तिष्ठन्ति ये साधव:।।६५।।
अर्थ—जिस वर्षा काल में काले—२ मेघ भयंकर शब्द करते हैं तथा समुद्र के क्षार दोष से ही मानो जो जहां तहां जल वर्षाते हैं तथा जिस काल में जमीन नीचे को धसक जाती है तथा पर्वतों से बड़े—२ पत्थर गिरते हैं तथा जल की भरी हुई नदियाँ सब जगह दौड़ती फिरती हैं तथा जो वर्षाकाल वृष्टिसहित पवन से भयंकर हो रहा है ऐसे भयंकर वर्षाकाल में जो मोक्षाभिलाषी मुनि वृक्षों के नीचे बैठ कर तप करते हैं उन मुनियों के लिये नमस्कार है अर्थात् वे मुनि मेरी रक्षा करो।।६५।। शीतकाल में खुले हुवे मैदान में तप करने वाले यतीश्वरों की स्तुति
शार्दूलविक्रीडित छंद-
म्लायत्कोकनदे गलत्पिकमदे भ्रंश्यद्द्रुमौघच्छदे हर्षद्रोमदरिद्रके हिमऋतावत्यन्तदु:खप्रदे।
ये तिष्ठन्ति चतुष्पथे पृथुतप: सौधस्थिता: साधवो ध्यानोष्णप्रहितोग्रशीतविधुरास्ते मे विदध्यु:श्रियम् ।।६६।।
अर्थ— जिस शीतकाल में कमल कुम्हला जाते हैं तथा बन्दरों का मद गल जाता है और वृक्षों के पत्ते जल जाते हैं तथा जिस शीतकाल में वस्त्ररहित दरिद्रों के शरीर पर रोमांच खड़े हो जाते हैं और भी जो नानाप्रकार के दु:खों का देने वाला है ऐसे भयंकर शीतकाल में अत्यंत तपस्वी तथा ध्यानरूपी अग्नि से समस्त शीत को नाश करने वाले जो यतीश्वर खुले मैदान में निर्भयता से निवास करते हैं वे यतीश्वर मुझे अविनाशी लक्ष्मी प्रदान करो।।६६।।
और भी मुनिधर्म के स्वरूप को आचार्य दिखाते हैं।
वसंततिलका छंद-
कालत्रये वहिरवस्थितजातवर्षा शीतातपप्रमुखसंघटितोग्रदु:खे।
आत्मप्रबोधविकले सकलोऽपि कायक्लेशो वृथा वृतिरिवोज्झितशालिवप्रे।।६७।।
अर्थ—जो मुनि अपने आत्मज्ञान की कुछ भी परवा न कर बाहिर में रहकर वर्षा शीत गर्मी तीनों कालों में उत्पन्न हुवे दु:खों को सहन करते हैं उनका उस प्रकार का दु:ख सहना वैसा ही निरर्थक मालूम होता है जैसा कि धान्य के कट जाने पर खेत की बाड़ लगाना निरर्थक होता है इसलिये मुनियों को आत्मज्ञान पर विशेष ध्यान देना चाहिये।।६७।।
शार्दूलविक्रीडित छंद-
सम्प्रत्यस्ति न केवली किल कलौ त्रैलोक्सचूडामणि स्तद्वाच: परमासतेऽत्र भरतक्षेत्रे जगद्द्योतिका:।
सद्ररत्नत्रयधारिणो यतिवरास्तेषां समालंवनं तत्पूजा जिनवाचिपूजनमत: साक्षाज्जिन: पूजित:।।६८।।
अर्थ—यद्यपि इस समय इस कलिकाल में तीन लोक के पूजनीक केवली भगवान विराजमान नहीं हैं तो भी इस भरतक्षेत्र में समस्त जगत को प्रकाश करने वाली उन केवली भगवान की वाणी मौजूद हैं तथा उन वाणियों के आधार श्रेष्ठ रत्नत्रय के धारी मुनि हैं इसलिये उन मुनियों की पूजन तो सरस्वती की पूजन है तथा सरस्वती की पूजन साक्षात्केवली भगवान की पूजन है ऐसा भव्यजीवों को समझना चाहिये।।६८।।
शार्दूलविक्रीडित छंद-
स्पृष्टा यत्र मही तदंघ्रिकमलैस्तत्रैति सत्तीर्थतां तेभ्यस्तेपि सुरा: कृताञ्ञलिपुटा नित्यं नमस्कुर्वते।
तन्नामस्मृतिमात्रतोऽपि जनता निष्कल्मषा जायते ये जैना यतयश्चिदात्मनिरता ध्यानं समातन्वते।।६९।।
अर्थ—जो यतीश्वर आत्मा में लीन होकर ध्यान करते हैं उन जैनयतीश्वरों के चरण कमलों से सृष्ट भूमि उत्तमतीर्थ बन जाती है तथा उन यतीश्वरों को हाथ जोड़ मस्तक नवाकर बड़े—२ देव आकर नमस्कार करते हैं तथा उनके स्मरण मात्र से ही जीवों के समस्त पाप गल जाते हैं इसलिये यतीश्वरों को सदा ध्यान में लीन रहना चाहिये।।६९।।
शार्दूलविक्रीडित छंद-
सम्यग्दर्शनवृत्तवोधनिचित: शान्त: शिवैषी मुनि: मन्दै: स्यादवधीरितोऽपि विशद: साम्यं यदालम्ब्यते।
आत्मा तैर्विहतो यदत्र विषमध्वान्तश्रितो निश्चितं सम्पातो भवितोग्रदु:ख नरके तेषामकल्याणिनाम् ।।७०।।
अर्थ—सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान सम्यक्चारित्र का धारी तथा शांत और मोक्षाभिलाषी जो मुनि दुष्टों से अपमानित होकर भी स्वच्छ अंत:करण से समता को धारण करता है उसकी तो आत्मा शुद्ध ही होती है किन्तु जो उनकी निन्दा करने वाले हैं उन्होंने अपनी आत्मा का घात कर लिया क्योंकि वे दुष्ट कल्याणरहित पुरूष ऐसे नरक में गिरेंगे जो नरक भयंकर अंधकार से व्याप्त है। तथा कठिन दु:ख का स्थान है इसलिये मुनियों को चाहिये कि दुष्ट वैâसी भी निंदा करें तो भी उनको समता ही धारण करनी योग्य है।।७०।।
स्रग्धरा छंद-
मानुष्यं प्राप्य पुण्यात्प्रशममुपगता रोगवद्भोगजालं मत्वा गत्वा वनांतं दृशि विदि चरणे ये स्थिता: संगमुक्ता:।
कस्तोता वाक्पथातिक्रमणपटुगुणैरािंश्रतानांमुनीनांस्तोतव्यास्तेमहद्भिर्भुवि य इह तदंघ्रिद्वयेभक्तिभाज:।।
अर्थ—पुण्य योग से मनुष्य भव को पाय कर तथा शान्ति को प्राप्त होकर और भोगों को रोग तुल्य जानकर तथा वन में जाकर समस्त परिग्रह से रहित होकर जो यतीश्वर सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान सम्यक्चारित्र में स्थित होते हैं वचनागोचर गुणोंकर सहित उन मुनियों की प्रथम तो कोई स्तुति का करने वाला ही नहीं यदि कोई स्तुति कर सके भी तो वे ही पुरूष उनकी स्तुति कर सकते हैं जो उन मुनियों के चरण कमलों को आराधन करने वाले महात्मा पुरूष हैं।।७१।।
इस प्रकार धर्मोपदेशामृताधिकार में मुनिधर्म का वर्णन समाप्त हुवा।।
