रत्नकरण्ड श्रावकाचार में वर्णित श्रावक-व्रतों का वैशिष्ट्य
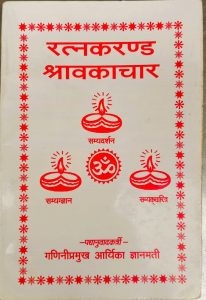
जैन धर्म केवल निवृत्तिमूलक दर्शन नहीं है, बल्कि उसके प्रवृत्त्यात्मक रूप में अनेक ऐसे तत्त्व विद्यमान हैं, जिनमें निवृत्ति और प्रवृत्ति का समन्वय होकर धर्म का लोकोपकारी रूप प्रकट हुआ है। इस दृष्टि से जैनधर्म जहाँ एक ओर अपरिग्रही, महाव्रतधारी अनगार धर्म के रूप में निवृत्तिप्रधान दिखाई देता है, तो दूसरी ओर मर्यादित प्रवृत्तियाँ करने वाले अणुव्रतधारी श्रावक धर्म की गतिविधियों में सम्यक् नियंत्रण करने वाला दिखाई देता है। समाज-रचना में राजनीति और अर्थनीति के धरातल पर यदि जैनदर्शन के अहिंसात्मक स्परूप का प्रयोग करे तो आधुनिक युग में समतावादी दृष्टिकोण को स्थापित किया जा सकता है। महात्मा गाँधी ने भी आर्थिक क्षेत्र में ट्रस्टीशिप का सिद्धान्त आवश्यकताओं से अधिक वस्तुओं का संचय न करना, शरीर श्रम, स्वादविजय, उपवास आदि के जो प्रयोग किये, उनमें जैनदर्शन के प्रभावों को सुगमता से रेखांकित किया जा सकता है। जैन दर्शन का मूल लक्ष्य वीतरागभाव अर्थात् राग-द्वेष से रहित समभाव की स्थिति प्राप्त करना है। समभाव रूप समता में स्थिर रहने को ही धर्म कहा गया है।समियाए धम्मे आरिएहिं पवेदिते – आचारांगसूत्र ५/३/४५ समता धर्म का पालन श्रमण के लिए प्रति समय आवश्यक है।मूलाचार ७/४२१ इसलिए जैन परम्परा में समता में स्थित जीव को ही श्रमण कहा गया है।
जब तक हृदय में या समाज में विषम भाव बने रहते हैं, तब तक समभाव की स्थिति प्राप्त नहीं की जा सकती। अत: यह आवश्यक है कि विषमता के जो कई स्तर, यथा-समाजिक विषमता, वैचारिक विषमता, दृष्टिगत विषमता, सैद्धान्तिक विषमता आदि प्राप्त होते हैं, उनमे व्यवहारिक रूप से समानता होनी चाहिए। लोभ और मोह पापों के मूल कहे गये हैं। मोह राग-द्वेष के कारण ही (जीव) व्यक्ति समाज में पापयुक्त प्रवृत्ति करने लगता है।प्रवचनसार १/८४ इसलिए इनके नष्ट हो जाने से आत्मा को समता में अधिष्ठित कहा गया है।मोहक्खोहविहीणो परिमाणे अप्पणो हु समो। – प्रवचनसार १/७ समाज में व्याप्त इस आर्थिक वैषम्य को जैनदर्शन में परिग्रह कहा गया है। यह आसक्ति, अर्थ-मोह या परिग्रह कैसे टूटे, इसके लिए जैनधर्म में श्रावक के लिए बारह व्रतों की व्यवस्था की गई है। जैन परम्परा में धर्म के दो रूप प्राप्त होते हैं – श्रमण धर्म एवं श्रावक धर्म। महाव्रत के सम्बन्ध में आचार्य समन्तभद्र लिखते हैं –
पञ्चानां पापानां हिंसादीनां मनोवच: कायै: ।
कृत- कारितऽनुमोदैस्त्यागस्तु महाव्रतं महताम् ।।
रत्नकरण्ड श्रावकाचार, ७२
अर्थात् मन, वचन, काय द्वारा कृत, कारित, अनुमोदन पूर्वक पांच पापों का पूर्णरूप से त्याग करना ही महाव्रत है। मुनिवर्ग महाव्रतों का पालन करते हैं तथा श्रावक वर्ग अणुव्रत सहित द्वादश व्रतों का पालन करते हैं। श्रावक धर्म का विस्तृत विवरण आचार्य समन्तभद्र ने रत्नकरण्डक श्रावकाचार नामक ग्रन्थ में दिया है तथा उसमें उन्होंने श्रावक के विभिन्न धर्मों को विवेचित किया है। श्वेताम्बर जैन आगमें में ज्ञाताधर्मकथा द्वादशांगी के अन्तर्गत परिगणित है। इसके पंचम अध्याय में शैलक का कथानक दिया गया है, जिसमें एक प्रसंग थावच्चा पुत्र एवं शुक के बीच हुए संवाद सहित यहाँ संवाद सहित यहाँ अपरिग्रह की प्रवृत्ति को दर्शाने के लिए दृष्टव्य है
मूल पाठ
‘सरिसवया ते भंते ! भक्खेया अभक्खेया ?
‘सुया ! सरिसवया भक्खेया वि अभक्खेया वि।’ से केणट्ठेणं भंते !
एवं वुच्चइ सरिसवया भक्खेय वि अभक्खेया वि ?‘
सुया ! सरिसवया दुविहा पण्णत्ता, तं जहा-मित्तसरिसवया धन्नसरिासवया य।
तत्थ णं जे ते मित्तसरिसवया ते तिविहा पण्णत्ता, तं जहा- सहजायया, सहविड्ढयया सहपंसुकीलियया। ते णं समणाणं निग्गंथाणं अभक्खेया।
तत्थं णं जे ते सत्थपरिणया ते दुविहा पन्नता, त जहा- फासुगा य असफासुगा य।
अफासुगा णं सुय! नो भक्खेया। तथ्य णंजे ते फासुया ते दुविहा पन्नत्ता, तं जहा जाइया य अजाइय।
तत्थं णं ते अजाइया ते अभक्खेया। तत्थ णं जे ते जाइया ते दुविहा पण्णत्ता, तं जहा- एसणिज्ज य अणेसणिज्जा य।
तत्थ णं जे ते अणेसणिज्ज ते णं अमकवेया।
तत्थ णं जेते एसणिज्ज ले दुविहा पन्नता, तं जहा- लद्धा स अलद्धाय।
तत्थ णं ते अलद्धा ते अभक्खेया।
तत्थ णं जे ते लद्धा ते निग्गंथाणं भक्खेय।
एएणं अट्ठेणं सुय!
एवं वुच्चइ सरिसवया भक्खेया वि अभक्खेया वि।
शुक परिव्राजक ने प्रश्न किया – ‘भगवन् ! आपके लिए सरिसवया’ भक्ष्य हैं या अभक्ष्य हैं’ थावच्चापुत्र ने उत्तर दिया – ‘हे शुक ! ‘सरिसवया’ हमारे लिए भक्ष्य भी हैं और अभक्ष्य भी हैं।’ शुक ने पुन: प्रश्न किया – ‘भगवन् ! किस अभिप्राय से ऐसा कहते हैं कि ‘सरिसवया (सृदश वय वाले मित्र) और धान्य-सरिसवया भक्ष्य भी हैं और अभक्ष्य भी हैं ? थावच्चापुत्र उत्तर देते हैं – ‘हे शु ! ‘सरिसवया’ दो प्रकार के कहे गये हैं- मित्र-सरिसवया (सृदश वय वाले मित्र) और धान्य-सरिसवया (सरसों)। इनमें जो मित्र-सरिसवया हैं वे तीन प्रकार के हैं।
१. साथ जन्मे हुए,
२. साथ बढ़े हुए,
३. साथ-साथ घूल में खेले हुए। यह तीन प्रकार के मित्र-सरिसवया श्रमण निर्ग्रन्थों के लिए अभक्ष्य हैं। जो धान्य- सरिसवया (सरसों) हैं, वो दो प्रकार हैं – शस्त्रपरिणत और अशस्त्रपरिणत। उनमें जो अशस्त्रपरिणत हैं अर्थात् जिनको अचित्त करने के लिए अग्नि आदि शास्त्रों का प्रयोग नहीं किया गया है, अतएव जो अचित्त नहीं है, वे श्रमण निग्र्रन्थों के लिए अभक्ष्य हैं। जो शस्त्रपरिणत हैं, वे दो प्रकार के हैं – प्रासुक और अप्रासुक। हे शुक। अप्रासुक भक्ष्य नहीं है। उनमें जो प्रासुक हैं, वे दो प्रकार के हैं – याचित (याचना किये हुए) और अयाचित (नहीं याचना किये हुए) उनमें जो अयाचित हैं, वे अभक्ष्य हैं। उनमें जो याचित हैं, वे दो प्रकार के हैं।
यथा- एषणीय और अनेषणीय। उनमें जो अनेषणीय हैं, वे अभक्ष्य हैं।
जो एषणीय हैं, वे दो प्रकार के हैं – लब्ध (प्राप्त) और अलब्ध (अप्राप्त)। उनमें जो अलब्ध हैं, वे अभक्ष्य हैं। जो लब्ध हैं वे निग्र्रन्थों के लिए भक्ष्य हैं। ‘हे शुक ! इस अभिप्राय से कहा है कि सरिसवया भक्ष्य भी हैं और अभक्ष्य भी हैं। ज्ञाताधर्मकथा के उक्त दृष्टांत में यद्यपि श्रमण के भक्ष्य का विवेचन किया गया है किन्तु विषय के आलोक में यहाँ यह विशेष रूप से कहा जा सकता है कि अभक्ष्य का त्याग अनावश्यक संग्रह ,एवं हिंसा के त्याग की भावना को व्यक्त करता है।
यदि व्यक्ति संयमपूर्ण आहार को ग्रहण करता है तो एक ओर स्वास्थ्य और धर्म आराधना का पालन तो होता ही है, साथ ही साथ आर्थिक दृष्टि से वह भी अपने आप को समृद्ध करता है। श्रावक शब्द – श्रा, व एवं क इन तीन शब्दों के योग से बनता है। जिसमें श्रा शब्द से श्रद्धा, व शब्द से विवेक तथा क शब्द से क्रिया का अर्थ प्रदर्शित होता है। अत: श्रावक का अर्थ विवेकवान विरक्तचित्त अणुव्रती अथवागृहस्थ होता है। जैन परम्परा में श्रावक के तीन भेद- पाक्षिक (निज धर्म का पक्ष मात्र करने वाला), नैष्ठिक (व्रतधारी गृहस्थ जो प्रतिमाएँ धारण करता है) तथा साधक (जो प्रतिक्षण अपनी साधना में लगा रहता है) प्राप्त होते हैं। जैन परम्परा में श्रावक धर्म का प्रतिपादन करने वाले ग्रन्थों में रत्नकरण्डक श्रावकाचार अतिप्राचीन ग्रन्थ है।
आचार्य वट्टकेर ने मूलाचार, शिवार्य ने भगवती आराधना नामक ग्रन्थ लिखकर श्रमणधर्म का प्रतिपादन किया वहीं पं. आशाधर जी ने सागार धर्मामृत एवं अनगारधर्मामृत नामक ग्रन्थों में दोनों धर्मों का प्रतिपादन किया। आचार्य वसुतिन्दि, अमितगत, जोइन्दु, सकलकीर्ति आदि आचार्यों ने श्रावकधर्म के ग्रन्थों की रचनाकर जैन साहित्य को समृद्ध किया। भगवान् महावीर ने जैनागमों में अगारधर्म बारह प्रकार का बतलाया है। श्रावकधर्म का प्रतिपादन आचार्य समन्तभद्र ने अपने ग्रन्थ रत्नकरण्ड श्रावकाचार में विस्तार से किया है। उन्होंने ७ अधिकारों-सम्यग्दर्शन अधिकारी (७८ गाथाएं), सम्यग्ज्ञान अधिकार (१४ गाथाएं), अणुव्रत अधिकार (४१ गाथाएं), गुणव्रत अधिकार (२४ गाथाएं), शिक्षाव्रत अधिकार (४४ गाथाएं), सल्लेखना अधिकार (२० गाथाएं), सदव्रतअधिकार (१७ गाथाएं) एवं अन्य १२ गाथाएँ केवल १५० गाथाओं में श्रावक धर्म का प्रतिपादन किया है।
रत्नकरण्डकश्रावकाचार में आचार्य समन्तभद्र ने श्रावक के चरित्र को परिभाषित करते हुए लिखा है –
गृहीणां त्रेधा त्रिष्टत्यणु-गुण-शिक्षा-वृतात्मकं चरणं ।
पंत्र-त्रि-चतुर्भेदं त्रयं यथासंख्यामाख्यातम् ।।५१।।
रत्नक.
अर्थात् श्रावक के तीन प्रकार का चरित्र होता है – पांच अणुव्रत, तीन गुणव्रत तथा चार शिक्षाव्रत। वे इस प्रकार हैं – पांच अणुव्रत इस प्रकार हैं
१. अहिंसाणुव्रत – स्थूल-मोटे तौर पर, अपवाद रखते हुए प्राणातिपात से निवृत्त होना।
२. सत्याणुव्रत – स्थूल मृषावाद से निवृत्त होना।
३. अचौर्याणुव्रत – स्थूल अदत्तादान से निवृत्त होना।
४. ब्रह्मचर्याणुव्रत – स्वदारसंतोष- अपनी परिणीता पत्नी तक मैथुन की सीमा करना।
५. अपरिग्रहाणुव्रत – इच्छा- परिग्रह की इच्छा का परिमाण या सीमाकरण करना। तीन गुणव्रत इस प्रकार हैं–
१. दिग्व्रत – विभिन्न दिशाओं में जाने के सम्बन्ध में मर्यादा या सीमाकरण।
२. अनर्थदंड विरमण – आत्मा के लिए अहितकर या आत्मगुणघातक निरर्थक प्रवृत्ति का त्याग।
३. उपभोग- परिभोग-परिणाम व्रत उपभोग जिन्हें अनेक बार भोगा जा सके, ऐसी वस्तुएँ जैसे– वस्त्र आदि परिभोग जिन्हें एक ही बार भोगा जा सके जैसे –भोजन आदि, इनका परिमाण-सीमाकरण। चार शिक्षाव्रत इस प्रकार हैं
१. सामायिक – समता या समत्वभाव की साधना के लिए एक नियत समय। (न्यूनतम) एक मूहूर्त- ४५ मिनट में किया जाने वाला अभ्यास।
२. देशावकाशिक – नित्य प्रति अपनी प्रवृत्तियों में निवृत्ति-भाव की बुद्धि का अभ्यास।
३. पोषधोपवास – यथाविधि आहार, अब्रह्मचर्य आदि का त्याग। तथा
४. वैयावृत्य – गुणों में अनुराग से संयमी अथवा तपस्वी जनों के खेद को दूर करना वैयावृत्य है।
श्रावकव्रतों का वैशिष्ट्य
आचार्य समन्तभद्र रत्नकरण्डक श्रावकाचार में प्रत्येक व्रत के स्वरूप एवं फल पर विचार करते हैं। अणुव्रतों को धारण करने का फल बतलाते हुए कहते हैं –
पञ्चाणुव्रतनिधयो, निरतिक्रमणा फलन्ति सुरलोकं ।
यत्रावधिरष्टगुणा, दिव्यशरीरं च लभ्यन्ते ।।६३।।
रत्न.क.
आचार्य इस गाथा में अणुव्रत के धारण करने के चार फल दिखा रहे हैं। अर्थात् जो अणुव्रतों का निरतिचार पूर्वक पालन करता है, उसे
१ देव पर्याय की प्राप्ति
२ अवधिज्ञान की प्राप्ति
३ अष्ट-लब्धियों की प्राप्ति
४ दिव्य शरीर की प्राप्ति होती है।
यह श्रावक के अणुव्रत धारण करने का ही फल है जो अणुव्रतों के वैशिष्ट्य को उजागर करता है। अनर्थदण्ड विरमणव्रत :
अभ्यन्तरदिगवधेरपार्थकेभ्य: सपापयोगेभ्य: ।
विरमणमर्नदण्डव्रतं विदुव्र्रतधराग्रण्य: ।।७४।।
रतनक.
अर्थात् दिशाओं की मर्यादा के भीतर बिना प्रयोजन पापबन्ध के कारणभूत कार्यों से विरक्त होना ही अनर्थदंड विरमण व्रत है। उक्त गाथा में अप् एवं अर्थक शब्द को सन्धि करके अपार्थक शब्द का प्रयोग किया है, जिसका अर्थ है–निष्प्रयोजन। यही शब्द इस व्रत की भावना को व्यक्त करता है कि निष्प्रयोजन की गई पापरूप प्रवृत्ति का त्याग आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है। जैन परम्परानुसार त्रियोग सम्पन्न अशुभ उपयोग रूप प्रवृत्ति ही दण्ड है, जिसका त्याग किया जाना व्रत की परिधि में आता है। यह जैन श्रावक व्रतों का ही वैशिष्ट्य है कि दण्ड के विधान का त्याग किया जाना एक व्रत की कोटि के अन्तर्गत समाहित है। इसीलिए आचार्य समन्तभद्र रत्नकरण्डकश्रावकाचार में मुनिराज को अदण्डधर- अशुभ उपयोगरूप मन,वचन, काय की प्रवृत्ति करने से रहित, कहते हैं।
पापो देशहिंसादानापध्यान दु:श्रुती पंच ।
प्राहु: प्रमादचर्यानर्थदण्डधरा ।।७५।।
रत्नक.
अर्थात् अशुभ- उपयोगरूप दण्ड को धारण नहीं करने वाले (अदण्डधरा) गणधरादिदेव५ हेतुओं को अनर्थदण्ड कहते हैं। वे हैं- पापोदेश, हिंसादान, अपध्यान, दु:श्रुति, प्रमाद। इन्हीं पांचों के संदर्भ में आचार्य विवेचन करते हुए इस प्रकार कहते हैं – पापोदेश : तिर्यञ्चों को कष्ट देना, ठगना, हिंसा को बढ़ाने वाली कथाओं का प्रसंग उपस्थित करना पापोदेश है। हिंसादान : मनुष्यों, तिर्यञ्चों की हिंसा के साधन-फरसा, कृपाण, कुदारी, बन्दुक, तोप आदि अस्त्र-शस्त्र, सांकल आदि का देना हिंसा दान है। (रत्नक. ७६) अपध्यान : राग-द्वेष से परस्त्री तथा परपुत्रादिकों के मारण, बन्धन, छेदन आदि हो जाये, ऐसा चिन्तवन करना अपध्यान है। (रत्नक. ७७) दु:श्रुति : आरम्भ, परिग्रह, साहस, मिथ्यात्व, राग-द्वेष, अहंकार, इन्द्रिय-विषय-वासना से मन को संक्लेशित करने वाले शास्त्रों का श्रवण दु:श्रुति है। (रत्नक. ७९) प्रमाद : निष्प्रयोजन पृथ्वी को कुरेदना, जल को छींटना या उछालना, अग्नि जलाना-बुझाना, वायु या पंखा झलना तथा वनस्पति छेदना आदि आरम्भपूर्ण क्रियाएँ करना प्रमाद है। (र.क. ८०) रत्नकरण्डक श्रावकाचार में व्रतों के वैशिष्ट्य को उजागर करने में आचार्य समन्तभद्र की दृष्टि और भी स्पष्ट दिखाई देती है, जब वे अणुव्रतों का पालन करने वालों की कथाओं के माध्यम से दृष्टान्त देते हैं।
उन्होंने अहिंसाणुव्रत का पालन करने वाले यमपाल नामक चाण्डाल की कथा, सत्याणुव्रत का पालन करने वाले धनदेव की कथा, अचौर्याणुव्रत का पालन करने वाले राजकुमार वारिषेण की कथा, ब्रह्मचर्याणुव्रत का पालन करने वाली नीली वणिक पुत्री की कथा और परिग्रह परिमाणव्रत का पालन करने वाले जय राजा, जो उत्तम-पूजातिशय को प्राप्त हुए, की कथा देकर अणुव्रतों के वैशिष्ट्य को उद्धृत किया है। इसी क्रम में अतीचार पूर्वक क्रमश: हिंसा आदि पांच पापों में संलग्न धनश्री की कथा, सत्यघोष पुरोहित की कथा, वत्स्य देश के एक तपस्वी की कथा, यमदण्ड कोतवाल की कथा तथा श्मश्रुनवनीत वणिक की कथा के माध्यम से भी श्रावक व्रतों का वैशिष्ट्य उजागर हुआ है। रतनकरण्डक श्रावकाचार में आचार्य समन्तभद्र ने द्वादशव्रतों का विवेचन, उसके लक्षण, फल, अतीचार तथा उनके पालन करने वालों की कथाओं को दद्धृत करते हुए, किया है। व्रतों के उक्त वैशिष्ट्य के साथ-साथ आधुनिक समाजिक दृष्टि से भी इनका महत्वपूर्ण स्थान व वैशिष्ट्य उजागर होता है। अत: जैनदर्शन के संदर्भ में श्रावक के व्रतों की व्यवस्था में निम्नांकित बिन्दुओं को रेखांकित किया जा सकता है।
१. अहिंसा की व्यावहारिकता
२. श्रम की प्रतिष्ठा
३. दृष्टि की सूक्ष्मता
४. आवश्यकताओं का स्वैच्छिक परिसीमन
५. साधन-शुद्धि पर बल
६. अर्जन का विर्सजन
१. अहिंसा की व्यावहारिकता
अहिंसा के संदर्भ में आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने कहा है –
अप्रादुर्भाव: खलु रागादीनां भवत्यहिंसेति ।
तेषामेवोत्पत्तिहिसेति जिनागमस्य संक्षेप: ।।४४।।
पुरुषार्थसिद्धयुपाय
अर्थात् जहाँ रागादि भावों का अभाव होगा, वहीं अहिंसा का प्रादुभार्व हो सकता है। भगवान महावीर स्वामी ने समता के साध्य को प्राप्त करने के लिए अहिंसा को साधन रूप बाताया है। अहिंसा मात्र नकारात्मक शब्द नहीं है, बल्कि इसके विविध रूपों में सर्वाधिक महत्त्व सामाजिक होता है। वैभवसंपन्नता, दानशीलता, व्यावसायिक कुशलता, ईमानदारी, विश्वसनीयता प्रामाणिकता जैसे विभिन्न अर्थ प्रधान क्षेत्रों में अहिंसा की व्यावहारिकता को अपनाकर श्रेष्ठता का मापदण्ड सिद्ध किया जा सकता है। अहिंसा की मूल भावना यह होती है कि अपने स्वार्थों, अपनी आवश्यकताओं को उसी सीमा तक बढ़ाओं, जहाँ तक वे किसी प्राणी के हितों को चोट नहीं पहुँचाती हों। अत: अहिंसा व्यक्ति-संयम भी है और सामाजिक-संयम भी।
२. श्रम की प्रतिष्ठा साधना के क्षेत्र में श्रम की भावना सामाजिक स्तर पर समाधुत हुई। इसीलिए महावीर ने कर्मणा श्रम की व्यवस्था को प्रतिष्ठापित करते हुए कि व्यक्ति कर्म से ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश् और शुद्र बनता है।उत्तराध्ययनसूत्र २५/३३ उन्होंने जन्मना जाति के स्थान पर कर्मणा जाति को मान्यता देकर श्रम के सामाजिक स्तर को उजागर किया, जहां से श्रम अर्थ-व्यवस्था से जुड़ा ओर कृषि गोपालन, वाणिज्य आदि की प्रतिष्ठा बढ़ी। जैन मान्यतानुसार सभ्यता का प्रारम्भिक अवस्था में जब कल्पवृक्षादि साधनों से आवश्यकताओं की पूर्ति होना संभव न रहा, तब भगवान् ने असि और कृष रूप जीविकोपार्जन की कला की और समाज की स्थापना में प्रकृति-निर्भरता से श्रम-जन्य आत्मा-निर्भरता के सूत्र दिए। यही श्रमजन्य आत्मनिर्भरता जैन परम्परा में आत्म-पुरुषार्थ और आत्म-पराक्रम के रूप में फलित हुई है। अत: साधना के क्षेत्र में श्रम एवं पुरुषार्थ की विशेष प्रतिष्ठा है। यही कारण है कि व्यक्ति श्रम से परमात्म दशा प्राप्त कर लेता है। उपासकदशांगसूत्र में भगवान् महावीर और कुम्भकार सद्दालपुत्र का जो संसार वर्णित है, उससे स्पष्ट होता है कि गोशालक का आजीवक मत नियतिवाद है तथा भगवान् महावीर का मत श्रमनिष्ठ आत्म-पुरुषार्थ और आत्मपराक्रम को ही अपना उन्नति का केन्द्र बनाता है।
३. दृष्टि की सूक्ष्मता धर्म के तीन लक्षण मने गये हैं – अहिंसा, संयम और तप। ये तीनों दु:ख के स्थूल कारण पर न जाकर दु:ख के सूक्ष्म कारण पर चोट करते हैंं मेरे दु:ख का कारण कोई दूसरा नहीं, स्वयं मैं ही हूँ। अत: दूसरे को चोट पहुंचाने की बात न सोचूँ- यह अहिंसा है। मित्ती में सव्वभूएसुसमणसुतं – ८६ इसे सार्वजनिक बनाना होगा। अपने को अनुशासित करूँ- यह संयम है। अत: दु:खों से उद्वेलित होकर अविचारपूर्वक होने वाली प्रतिक्रिया न करूँ- इसे परीषहजय भी कहते हैं तथा दु:ख के प्रति हमारी प्रवृत्तिसमरूप रहे। अपने आपको प्रतिकूल परिस्थितियों की दासता से मुक्त बनाये रखें और सब प्रकार की परिस्थितियों में अपना समभाव बना रहें, क्यों समया धम्ममुदाहरे मुणी अर्थात् अनुकूलता में प्रफूल्लित न होना और प्रतिकूलता में विचलित न होना समता है। ऐसी सूक्ष्म दृष्टि रखने पर सामाजिक प्रवृत्ति समतापूर्वक की जा सकती है।
४. आवश्यकताओं का स्वैच्छिक परिसीमन आधुनिक समाज की रचना श्रम पर आधारित होते हुए भी संघर्ष और असंतुलन पूर्ण हो गयी है। जीवन में श्रम की प्रतिष्ठा होने पर जीवन-निर्वाह की आवश्यक वस्तुओं का उत्पाद और विनिमय प्रारंभ हुआ। अर्थ-लोभ ने पूंजी को बढ़ावा दिया। फलत: औद्योगीकरण, यंत्रवाद, यातायात, दूरसंचार तथा अत्याधुनिक भौतिकवाद के हावी हो जाने से उत्पादन और वितरण में असंतुलन पैदा हो गया। समाज की रचना में एक वर्ग ऐसा बन गया, जिसके पास आवश्यकता से अधिक पूंजी और भौतिक संसाधन जमा हो गये तथा दूसरा वर्ग ऐसा बना, जो जीवन-निर्वाह की आवश्यकता को भी पूरी करने में असमर्थ रहा।
फलस्वरूप श्रम के शोषण बढ़े वर्ग-संघर्ष की मुख्य समस्या ने अन्तर्राष्ट्रीय समस्या का रूप ले लिया।दशवैकालिक १/१ इस समस्या के समाधान में समाजवाद, साम्यवाद जैसी कई विचारधाराएँ आयीं, किन्तु सबकी अपनी-अपनी सीमाएं हैं। भगवान् महावीर ने आज के लगभग २५०० वर्ष पूर्व इस समस्या के समाधान के कुछ सूत्र दिए, जो अर्थ-प्रधान होते हुए भी जैन धर्म के साधना-सूत्र कहे जा सकते हैं। भगवान महावीर ने श्रावकवर्ग की आवश्यकताओं एवं उपयोग का चिंतन कर हर क्षेत्र में मर्यादा एवं परिसीमन पूर्वक आचरण करने के लिए बारह व्रतों का विधान किया है। इनके पालने से दैनिक जीवन में आवश्यकताओं का स्वैच्छिक परिसीमन हो जाता है। परिसीमन के निमन सूत्र है :-
(क) इच्छा परिणाम महावीर के अपरिग्रह का सिद्धान्त देकर आवश्यकताओं को मर्यादित कर दिया। सिद्धान्तानुसार समतावादी समाज रचना में यह आवश्यक हो गया कि आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संचय न करें। मनुष्य की इच्छाएं आकाश के समान अनन्त है।उत्तराध्ययनसूत्र ९/४८ और लोभ के साथ ही लोभ के प्रति आसक्ति बढ़ती जाती है, क्योंकि चांदी-सोने के कैलाश पर्वत भी व्यक्ति को प्राप्त हो जाएं, तब भी उसकी इच्छा पूरी नहीं हो सकती।उत्तराध्ययनसूत्र ९/४८ अत: इच्छा का नियमन आवश्यक है। इस दृष्टि से श्रावकों के लिए परिग्रह-परिणाम या इच्छा परिमाण व्रत की व्यवस्था की गयी है। अत: मर्यादा से व्यक्ति अनावश्यक स्रंहग और शोषण की प्रवृत्ति से बचता है। सांसारिक पदार्थों का परिसीमन जीवन-निर्वाह को ध्यान में रखते हुए किया गया है, वे हैं –
१. क्षेत्र (खेत आदि भूमि),
२. हिरण्य (चांदी),
३. वास्तु (निवास योग्य स्थान),
४. शयनासन,
५. धन (अन्य मूल्यवान पदार्थ)(ढले हुुए या घी, गुड़ आदि),
६. धान्य (गेहूँ, चावल, तिल आदि),
७. द्विपद (दो पैर वाले),
८. चतुष्पद (चार पैर वाले), कुप्य (वस्त, पात्र, औषधि आदि),
१०. भाण्ड (पीतल, तांबा, कांसा, लोहा, कांच, प्लास्टिक आदि)।
(क) तत्त्वार्थसूत्र -७-२९
(ख) रत्नकरण्ड श्रावकाचार, ६८
(ख) दिक्परिमाण व्रत भगवान महावीर का दूसरा सूत्र है- दिक्परिमाणव्रत। विभिन्न दशाओं में आने-जाने के सम्बन्ध में मर्यादा या निश्चय करना कि अमुक दिशा में इतनी दूरी से अधिक नहीं जाऊँगा।रत्नकरण्ड श्रावकाचार, ६८ इस प्रकार की मर्यादा से वृत्तियों के संकोच के साथ-साथ मन की चंचलता समाप्त होती है तथा अनावश्यक लाभ अथवा संग्रह के अवसरों पर स्वैच्छिक रोक लगती है। क्षेत्र सीमा का अतिक्रमण करना अतर्राष्ट्रीय कानून की दृष्टि में अपराध माना जाता है। अत: इस व्रत के पालन करने से दूसरे के अधिकार क्षेत्र में उपनिवेश बसा कर लाभ कमाने की या शोषण करने की वृत्ति से बचाव होता है। इस प्रकार के व्रतों से हम अपनी आवश्यकताओं का स्वैच्छिक परिसीमन कर समतावादी समाज-रचना में सहयोग कर सकते हैं।
(ग) उपभोग-परिभोग परिमाण व्रत दिक्परिमाणव्रत के द्वारा मर्यादित क्षेत्र के बाहर तथा वहां की वस्तुओं से निवृत्ति हो जाती है, किन्तु मर्यादित क्षेत्र के अन्दर और वहाँ की वस्तुओं के उपभोग (एक बार उपभोग), परिभोग (बार-बार उपभोग) में भी अनावश्यक लाभ और संग्रह की वृत्ति न हो, इसके लिए इस व्रत का विधान है। जैन आगम में वर्णित इस व्रत की मर्यादा का उद्देश्य यही है कि व्यक्ति का जीवन सादगीपूर्ण हो और वह स्वयं जीवित रहने के साथ-साथ दूसरों को भी जीवित रहने के अवसर और साधन प्रदान कर सकें। व्यर्थ के संग्रह और लोभ से निवृत्ति के लिए इन व्रतों का विशेष महत्व है।
(घ) देशावकाशिक व्रत दिकपरिमाण एवं उपभोग-परिभोग परिमाण के साथ-साथ देशावकाशिक व्रत का भी विधान श्रावक के लिए किया गया है, जिसके अंतर्गत दिन-प्रतिदिन उपभोग-परिभोग एवं दिक्परिमाण व्रत का और भी अधिक परिसीमन करने का उल्लेख किया गया है अर्थात् एक दिन-रात के लिए उसे मर्यादा को कभी घटा देना, आवागमन के क्षेत्र एवं भागोपभोग्य पदार्थों की मर्यादा कम कर देना, इस व्रत की व्यवस्था में है। श्रावक के लिए देशावकाशिक व्रत में १४ विषयों का चिंतन कर प्रतिदिन के नियमों में मर्यादा का परिसीमन किया गया है।
१. सचित्तवस्तु,
२. द्रव्य,
३. विगय,
४. जुते,
५. पान,
६. वस्त्र,
७. पुष्प,
८. वाहन,
९. शयन,
१०. विलेपन,
११. ब्रह्मचर्य,
१२. दिशा,
१३. स्नान,
१४. भोजन वे चौदह विषय हैं :-
सचित्त दव्व विग्गई, पन्नी, ताम्बूल वत्थ कुसुमेसु ।
वाहक सयल विलेवण, बम्भ दिसि नाहण भत्तेसु ।।१३
इन नियमों से व्रत विषयक जो मर्यादा रखी जाती है, उसका संकोच होता है और आवश्यकताएं उत्तरोत्तर सीमित होती हैं।
५. साधन- शुद्धि पर बल
जैनदर्शन में साधन-शुद्धि पर विशेष बल इसलिए दिया गया है कि उससे व्यक्ति का चरित्र प्रभावित होता है। बुरे साधनों से एकचित्र किया हुआ धन अन्तत: व्यक्ति को दुव्र्यसनों की ओर ले जाता है और उसके पतन का कारण बनता है। तप के बारह प्रकारों में अनशन, ऊनोदरी, भिक्षाचर्या और रस परित्याग भोजन से ही संबन्धित है। इसीलिए खाद्य शुद्धि-संयम प्रकारान्तर से साधन-शुद्धि के ही रूप बनते हैं। अहिंसा की व्यावहारिकता की तरह ही सत्याणुव्रत एवं अस्तेयाणुव्रत का साधन-शुद्धि के संदर्भ में महत्व है। ये विभिन्न व्रत साधन की पवित्रता के ही प्रेरक और रक्षक हैं। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अर्थार्जन करने में व्यक्ति को स्थूल हितों से बचना चाहिए। सत्याणुव्रत में सत्य के रक्षण और असत्य से बचाव पर बल दिया गया। व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए, कन्नालाए (कन्या के विषय में), गवालीए (गौ के विषय में), भोमालिए (भूमि के विषयमें), णासावहारे (अर्थात् धरोहर के विषय में झूठ न बोलें, तथा दूडसक्खिजे (झूठह साक्षी न दे) इनका उपयोग व उपभोग न करें।
अर्थ की दृष्टि से सत्याणुव्रत का पालन कोर्ट-कचहरी में झूठे दस्तावेजों में भ्रष्टााचार एवं रिश्वतखोरी में नहीं हो पाता, क्योंकि इन सभी क्षेत्रों में अर्थ की प्रधानता होने से असत्य का आश्रय लिया जाता है, जिससे समाज के मूल्य ध्वस्त हो जाते हैं। इसीलिए सत्याणुव्रत समाज-रचना का आधार बन सकता है। अस्तेय व्रत की परिपालना का भी साधन-शुद्धता की दृष्टि से विशेष महत्व है। मन, वचन और काय द्वारा दूसरों के हकों को स्वयं हरण करना और दूसरों से हरण करवाना चोरी है। आज चोरी के साधन स्थूल से सूक्ष्म बनते जा रहे हैं। खाद्य वस्तुओं में मिलावट करना, झूठा जमा-खर्च बताना, जमाखोरी द्वारा वस्तुओं की कीमत घटा या बढ़ा देना, ये सभी कर्म चोरी के हैं। इन सभी सूक्ष्म तरीकों की चौर्यवृत्ति के कारण ही मुद्रा-स्फीति का इतना प्रसार है और विश्व की अर्थव्यवस्था उससे प्रभावित हो रही है। अत: अर्थ व्यवस्था संतुलन के लिए आजीविका के जितने भी साधन हैं और पूंजी के जितने भी स्रोत हैं उनका और पवित्र होना आवश्यक है, तभी समतावादी समाज का निर्माण कर सकते हैंं इसी संदर्भ में भगवान् महावीर ने आजीविकोपार्जन के उन कार्यों का निषेध किया है जिनसे पापवृत्ति बढ़ती है। वे कार्य कर्मादान कहे गये हैं। अत: साधन-शुद्धि के अभाव में इन कर्मादानों को लोक में निन्द्य बताया गया है। इनको करने से सामाजिक प्रतिष्ठा भी समाप्त होती है। कुछ कर्मादान हैं, जैसे –
१. इंगालकर्म (जंगल जलाना)।
२. रसवाणिज्जे (शराब आदि मादक पदार्थों का व्यापार करना)।
३. विसवाणिज्ज (अफीम आदि का व्यापार)।
४. केसवाणित्ते (सुन्दर केशों वाली स्त्रियों का क्रय-विक्रय)।
५. दवग्गिदावणियाकमेन (वन जलाना)
६. असईजणणेसाणयाकम्मे (असामाजिक तत्त्वों का पोषण करना आदि)।
६. अर्जन का विसर्जन
अर्जन का विसर्जन नामक सिद्धान्त को जैनदर्शन में स्वीकार्य दान एवं त्याग तथा संविभाग के साथ जोड़ सकते हैं। महावीर ने अर्जन के साथ-साथ विसर्जन की बात कही। अर्जन का विसर्जन तभी हो सकता है, जब हम अपनी आवश्यकताओं को नियंत्रिण एवं मर्यादित कर लेते हैं। उपासकदशांग सूत्र में दस आर्दश श्रावकों का वर्णन है, जिसमें आनन्द, मन्दिनीपिता और सालिहीपिता की संपत्ति का विस्तृत वर्णन आता है। इससे यह स्पष्ट है कि महावीर ने कभी गरीबी का समर्थन नहीं किया। उनका प्रहार या चिंतन धन के प्रति रही हुई मूच्र्छावृत्ति पर है। वे व्यक्ति को निष्क्रिय या अकर्मण्य बनने को नहीं कहते, पर उनका बल अर्जित संपत्ति को दूसरों में बांटने पर है। उनका स्पष्ट उद्घोष है – असंविभागी ण हु तस्स मोक्खो अर्थात् जो अपने प्राप्त को दूसरों में बांटता नहीं है, उसकी मुक्ति नहीं होती। अर्जन के विसर्जन का यह भाव उदार और संवेदनशील व्यकित हृदय में ही जागृत हो सकता है।
