व्यवहारनय परमार्थ का प्रतिपादक है।
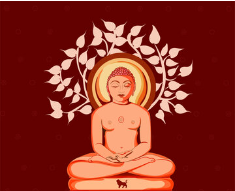
समयसार में आचार्य श्री कुन्दकुन्द स्वामी कहते हैं—
जो हि सुएणहिगच्छइ, अप्पाणमिणं तु केवलं सुध्दं।
तं सुयकेवलिमिसिणो, भणंति लोयप्पईवयरा।।९।।
जो सुयणाणं सव्वं, जाणई सुयकेविंल तमाहु जिणा।
णाणं अप्पा सव्वं, जम्हा सुयकेवली तम्हा।।१०।।
अर्थ
जो जीव निश्चय से श्रुतज्ञान के द्वारा इस केवल शुद्ध आत्मा को जानते हैं, लोक को प्रकाशित करने वाले ऋषिगण उनको श्रुतकेवली कहते हैं और जो संपूर्ण श्रुतज्ञान को जानते हैं जिनेन्द्रदेव उन्हें श्रुतकेवली कहते हैं क्योंकि सर्व ज्ञानमयी आत्मा ही है इसलिए वह श्रुतकेवली है।
परम पूज्य आचार्यदेव श्री अमृतचन्द्रसूरि इसी बात को स्पष्ट करते हुए ‘‘आत्मख्याति’’ टीका में लिखते हैं कि—‘‘यः श्रुतेन केवलं शुद्धमात्मानं जानाति सश्रुतकेवलीति इसकी ज्ञानज्योति हिन्दी टीका में पूज्य गणिनीप्रमुख श्री ज्ञानमती माताजी ने लिखा है कि ‘‘जो श्रुतज्ञान से केवल शुद्ध आत्मा को जानता है वह श्रुतकेवली है, इस प्रकार का कथन तो परमार्थ है और जो सम्पूर्ण श्रुतज्ञान (द्वादशांग) को जानता है वह श्रुतकेवली है इस प्रकार का कथन व्यवहार है।
अब प्रश्न यह होता है कि यहाँ पर निरूपित किया जाने वाला सर्व ही ज्ञान आत्मा है या अनात्मा ? अनात्मा तो कह नहीं सकते क्योंकि पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल में पाँचों द्रव्य अचेतन होने से ये सभी अनात्मा ही हैं अतः इनका ज्ञान के साथ तादात्म्य हो नहीं सकता है। इस कारण अन्य प्रकार का अभाव होेने से ज्ञान आत्मा ही है ऐसा सिद्ध हो जाता है, पुनः श्रुतज्ञान भी आत्मा ही है यह बात भी निश्चित हो जाती है और ऐसा सिद्ध हो जाने पर जो आत्मा को जानता है वह श्रुतकेवली है ऐसा जो कथन है सो परमार्थ ही है।
इस प्रकार से ज्ञान और ज्ञानी को भेद से कहने वाला जो व्यवहारनय है उसके द्वारा भी परमार्थ मात्र ही कहा जाता है किन्तु उससे अतिरिक्त कुछ नहीं कहा जाता। दूसरी बात यह है कि ‘‘जो श्रुतज्ञान के द्वारा केवल शुद्ध आत्मा को जानता है वह श्रुतकेवली है’’ इस प्रकार से परमार्थ का प्रतिपादन करना अशक्य होने से ‘‘जो सम्पूर्ण श्रुतज्ञान को जानता है वह श्रुतकेवली है’’ इस प्रकार का व्यवहार परमार्थ का प्रतिपादक होने से अपने स्वरूप को प्रतिष्ठित कराता है।
यह बात तो निश्चित ही है कि व्यवहारपूर्वक निश्चय होता है किन्तु निश्चयपूर्वक व्यवहार नहीं होता है अतएव यहाँ पर जो टीकाकार ने कहा है सो ठीक ही है। आज इस पंचमकाल में द्वादशांग श्रुतज्ञान उपलब्ध नहीं है उसका अंश रूप ही श्रुतज्ञान उपलब्ध है अतः जब कोई व्यवहार श्रुतकेवली ही नहीं हो सकते हैं तो पुनः निश्चय श्रुतकेवली कैसे हो सकते हैं ? द्वादशांग के वेत्ता श्रुतकेवली श्रीभद्रबाहु स्वामी अन्तिम श्रुतकेवली माने गए हैं। उनके बाद में सम्पूर्ण श्रुत के धारक ‘‘श्रुतकेवली’’ कोई नहीं हुए हैं।
स्वयं कुन्दकुन्ददेव भी श्रुतकेवली नहीं थे। इस कथन से जो यहाँ पर ऐसा कहा है कि ‘‘आत्मा को जानने वाले निश्चय श्रुतकेवली हैं ’’ उसका अभिप्राय यही है कि जो आत्मा का अनुभव करने वाले हैं, निवकल्प ध्यान में स्थित होकर जानने वाले हैं वे ही परमार्थ श्रुतकेवली हो सकते हैं अन्य सामान्य मुनि या श्रावक आदि नहीं। सारांश यह है कि छठे गुणस्थान में व्यवहार श्रुतकेवली होते हैं क्योंकि द्रव्यलिंगी मुनि को द्वादशांग का ज्ञान असम्भव है।
मात्र ग्यारह अंग तक का ज्ञान ही उन्हें हो सकता है अतः वे पूर्ण श्रुतज्ञान के अभाव में व्यवहार श्रुतकेवली नहीं हैं। श्रावक के व असंयत सम्यग्दृष्टि मनुष्य के अंग पूर्व रूप श्रुतज्ञान होता ही नहीं है अतः वे जब व्यवहार श्रुतकेवली ही नहीं हो सकते हैं तब निश्चय की बात तो बहुत ही दूर है। निश्चय श्रुतकेवली तो सातवें या आठवें गुणस्थान से माने जाते हैं चूँकि उन्हीं के शुक्लध्यानरूप भावश्रुतज्ञान होता है। इसी बात को श्री जयसेनाचार्य ने अपनी ‘‘तात्पर्यवृत्ति’’ टीका में भी सरल शब्दों में स्पष्ट किया है।
पूज्य गणिनीप्रमुख श्री ज्ञानमती माताजी ने इन दोनों आचार्यों की टीका को एक साथ समन्वयात्मक दृष्टि से हिन्दी टीका में प्रस्तुत किया है जिससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि दोनों के सिद्धान्तों में कोई अन्तर नहीं है, हाँ! केवल कठिन सरल भाषा का अन्तर जरूर है। हस्तिनापुर के दिगम्बर जैन त्रिलोक शोध संस्थान से प्रकाशित समयसार ग्रन्थ का स्वाध्याय ऐसी अनेक भ्रान्तियों का निवारण करने में अति सहायक सिद्ध होता है।
उसमें उपर्युक्त दोनों गाथाओं की टीका का उपसंहार करते हुए वर्णन आया है कि— ‘‘यहाँ दो बातें विशेष जानने योग्य हैं, एक तो उत्थानिका में कहा है कि ‘‘कथं व्यवहारस्य परमार्थ प्रतिपादकत्वमिति चेत्’’ व्यवहार नय परमार्थ का प्रतिपादक कैसे है ? ऐसा प्रश्न होने पर इन दो गाथाओं का अवतार हुआ है। इससे यह समझ में आता है कि द्रव्यश्रुत के आधार के बिना भावश्रुत नहीं हो सकता है।
व्याकरण में भी द्रव्य शब्द के ही भाव अर्थ में ‘‘त्व’’ या ‘‘ता’’ प्रत्यय लगता है जैसे सुवर्णस्य भावः ‘‘सुवर्णत्व’’ या ‘‘सुवर्णता’’ अर्थात् जब सुवर्ण होगा तभी उसका सुवर्णपना कहा जा सकेगा। श्री जयसेनाचार्य ने तो स्पष्ट कह दिया है कि ‘‘सुदणाणं द्रव्यश्रुताधारेणोत्पन्नं भावश्रुतज्ञानं आदा आत्मा भवति’’ अर्थात् द्रव्यश्रुतज्ञान के आधार से उत्पन्न हुआ भावश्रुतज्ञान ही आत्मा है इसलिए द्वादशांग के ज्ञाता द्रव्यश्रुतकेवली हुए बिना कोई भावश्रुतकेवली नहीं हो सकते हैं।
महाशास्त्र तत्त्वार्थसूत्र में भी कहा है ‘‘शुक्ले चाद्ये पूर्वविदः’’ आदि के दो शुक्लध्यान पूर्वविद्-ग्यारह अंग और चौदह पूर्व के ज्ञान श्रुतकेवली के ही होते हैं। दूसरी बात यह विशेष है कि यहाँ ‘‘यादृशं पूर्वपुरुषाणां शुक्लध्यानरूपं स्वसंवेदनज्ञानं तादृशमिदानीं नास्ति किन्तु धर्मध्यानं योग्यमस्तीत्यर्थः।’’ जैसा पूर्वपुरुष-मुनियों को शुक्लध्यानरूप स्वसंवेदनज्ञान था वैसा इस समय नहीं है किन्तु यथायोग्य धर्मध्यान है। इससे यह स्पष्ट है। कि पंचमकाल में धर्मध्यान के ध्याता साधु होते ही हैं, उनका निषेध नहीं किया जा सकता है।
