षट्खंडागम का सार
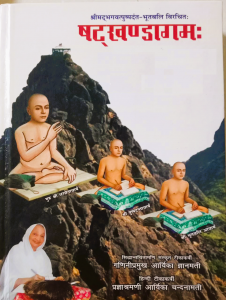
णमो अरिहंताणं, णमो सिद्धाणं, णमो आइरियाणं।
णमो उवज्झायाणं, णमो लोए सव्वसाहूणं।।१।।
षट्खण्डागम की प्रथम पुस्तक सत्प्ररूपणा में सर्वप्रथम ‘णमोकार महामंत्र’ से मंगलाचरण किया है। इसमें १७७ सूत्र हैं। इस ग्रंथ की रचना श्रीमत्पुष्पदंत आचार्य ने की है। इसके आगे के संपूर्ण सूत्र श्रीमद् भूतबलि आचार्य प्रणीत हैं।
इस मंगलाचरण की धवला टीका में पांचों परमेष्ठी के लक्षण बताये हैं।
यह मंत्र अनादि है या श्री पुष्पदन्ताचार्य द्वारा रचित सादि है ?
मैंने ‘सिद्धान्तचिन्तामणि’ टीका में इसका स्पष्टीकरण किया है। धवला टीका में इसे ‘निबद्धमंगल’ कहकर आचार्यदेव रचित ‘सादि’ स्वीकार किया है। इसी मुद्रित प्रथम पुस्तक के टिप्पण में जो पाठ का अंश उद्धृत है वह धवलाटीका का ही अंश माना गया है। उसके आधार से यह मंगलाचरण ‘अनादि’ है। आचार्य श्री पुष्पदंत द्वारा रचित नहीं है, ऐसा स्पष्ट होता है। इस प्रकरण को मैंने दिया है। यथा-
अयं महामंत्र: सादिरनादिर्वा ?
अथवा षट्खण्डागमस्य मु प्रतौ पाठांतरं।यथा-(मुद्रितमूलग्रन्थस्य प्रथमावृत्तौ)
‘‘जो सुत्तस्सादीए सुत्तकत्तारेण णिबद्धदेवदाणमोक्कारो तं णिबद्धमंगलं।
जो सुत्तस्सादीए सुत्तकत्तारेण कयदेवदाणमोक्कारो तमणिबद्धमंगलं’’१।
अस्यायमर्थ:-य: सूत्रस्यादौ सूत्रकर्त्रा निबद्ध:-संग्रहीत: न च ग्रथित: देवतानमस्कार: स निबद्ध: मंगलं।य: सूत्रस्यादौ सूत्रकर्त्रा कृत:-ग्रथित: देवतानमस्कार: स अनिबद्धमंगलं। अनेन एतज्ज्ञायते-अयं महामंत्र: मंगलाचरणरूपेणात्र संग्रहीतोऽपि अनादिनिधन:, न तु केनापि रचितो ग्रथितो वा।
उक्तं च णमोकारमंत्रकल्पे श्रीसकलकीर्तिभट्टारवै: –
महापंचगुरोर्नाम नमस्कारसुसम्भवम्। महामंत्रं जगज्जेष्ठ-मनादिसिद्धमादिदम्२।।६३।।
महापंचगुरूणां पंचत्रिंशदक्षरप्रमम्। उच्छ्वासैस्त्रिभिरेकाग्र-चेतसा भवहानये३।।६८।।
श्रीमदुमास्वामिनापि प्रोक्तम्-
ये केचनापि सुषमाद्यरका अनन्ता, उत्सर्पिणी-प्रभृतय: प्रययुर्विवर्त्ता:।
तेष्वप्ययं परतरं प्रथितं पुरापि, लब्ध्वैनमेव हि गता: शिवमत्र लोका:४।।३।।
यह महामंत्र सादि है अथवा अनादि ?
अथवा, मुद्रित मूल प्रति में (प्रथम आवृत्ति में) पाठान्तर है। जैसे-
जो सूत्र की आदि में सूत्रकर्त्ता के द्वारा देवता नमस्कार निबद्ध किया जाता है, वह निबद्धमंगल है और जो सूत्र की आदि में सूत्रकर्त्ता के द्वारा देवता नमस्कार किया जाता है-रचा जाता है, वह अनिबद्धमंगल है।
इसका अर्थ यह है-सूत्र ग्रंथ के प्रारंभ में ग्रंथकार जो देवता नमस्काररूप मंगल कहीं से संग्रहीत करते हैं, स्वयं नहीं रचते हैं वह तो निबद्धमंगल है और सूत्र के प्रारंभ में ग्रंथकर्त्ता के द्वारा जो देवता नमस्कार स्वयं रचा जाता है, वह अनिबद्धमंगल है। इससे यह ज्ञात होता है कि यह णमोकार महामंत्र मंगलाचरणरूप से यहाँ संग्रहीत होते हुए भी अनादिनिधन है, वह मंत्र किसी के द्वारा रचित या गूँथा हुआ नहीं है। प्राकृतिक रूप से अनादिकाल से चला आ रहा है।
‘‘णमोकार मंत्रकल्प’’ में श्री सकलकीर्ति भट्टारक ने कहा भी हैै-
श्लोकार्थ-नमस्कार मंत्र में रहने वाले पाँच महागुरुओं के नाम से निष्पन्न यह महामंत्र जगत में ज्येष्ठ-सबसे बड़ा और महान है, अनादिसिद्ध है और आदि अर्थात् प्रथम है।।६३।।
पाँच महागुरुओं के पैंतीस अक्षर प्रमाण मंत्र को तीन श्वासोच्छ्वासों में संसार भ्रमण के नाश हेतु एकाग्रचित्त होकर सभी भव्यजनों को जपना चाहिए अथवा ध्यान करना चाहिए।।६८।।
श्रीमत् उमास्वामी आचार्य ने भी कहा है-
श्लोकार्थ-उत्सर्पिणी, अवसर्पिणी आदि के जो सुषमा, दु:षमा आदि अनन्त युग पहले व्यतीत हो चुके हैं उनमें भी यह णमोकार मंत्र सबसे अधिक महत्त्वशाली प्रसिद्ध हुआ है। मैं संसार से बहिर्भूत (बाहर) मोक्ष प्राप्त करने के लिए उस णमोकार मंत्र को नमस्कार करता हूँ।।३।।
मैंने ‘सिद्धान्तचिन्तामणि टीका’ में सर्वत्र सूत्रों का विभाजन एवं समुदायपातनिका आदि बनाई हैं। यहाँ मैंने ‘समयसार’ ‘प्रवचनसार’ ‘पंचास्तिकाय’ ग्रंथों की ‘तात्पर्यवृत्ति’ टीका का अनुसरण किया है। श्री जयसेनाचार्य की टीका में सर्वत्र गाथासूत्रों की संख्या एवं विषयविभाजन से स्थल-अन्तरस्थल बने हुए हैं। उनकी टीका के अनुसार ही मैंने यहाँ स्थल-अन्तरस्थल विभाजित किये हैं।
सर्वत्र मंगलाचरण रूप में मैंने कहीं पद्य, कहीं गद्य का प्रयोग किया है। तीर्थ और विशेष स्थान की अपेक्षा से प्राय: वहाँ-वहाँ के तीर्थंकरों को नमस्कार किया है।
यहाँ पर उनके कुछ उदाहरण प्रस्तुत हैं-
जिनेन्द्रदेवमुखकमलविनिर्गत-गौतमस्वामिमुखकुण्डावतरित-पुष्पदंताचार्यादिविस्तारित-गंगाया: जलसदृशं ‘‘नद्या नवघटे भृतं जलमिव’’ इयं टीका सर्वजनमनांसि संतर्पिष्यत्येवेतिमया विश्वस्यते।
अथाधुना श्रीमत्पुष्पदन्ताचार्यदेवविनिर्मिते गुणस्थानादिविंशतिप्ररूपणान्तर्गर्भितसत्प्ररूपणा-नामग्रंथे अधिकारशुद्धिपूर्वकत्वेन पातनिका व्याख्यानं विधीयते। तत्रादौ ‘णमो अरिहंताणं’ इति पंचनमस्कार-गाथामादिं कृत्वा सूत्रपाठक्रमेण गुणस्थानमार्गणा-प्रतिपादनसूचकत्वेन ‘एत्तो इमेसिं’ इत्यादिसूत्रसप्तकं। तत: चतुर्दशगुणस्थाननिरूपणपरत्वेन ‘‘संतपरूवणदाए’’ इत्यादि-षोडशसूत्राणि। तत: परं चतुर्दशमार्गणासु गुणस्थानव्यवस्था-व्यवस्थापन-मुख्यत्वेन ‘‘आदेसेण गदियाणुवादेण’’ इत्यादिना चतु:पञ्चाशदधिक-एकशतसूत्राणि सन्ति। एवं अनेकान्तरस्थलगर्भित-सप्त-सप्तत्यधिक-एकशतसूत्रै: एते त्रयो महाधिकारा भवन्तीति सत्प्ररूपणाया: व्याख्याने समुदायपातनिका भवति।
अत्रापि प्रथममहाधिकारे ‘णमो’ इत्यादि मंगलाचरणरूपेण प्रथमस्थले गाथासूत्रमेकं। ततो गुणस्थानमार्गणा-कथनप्रतिज्ञारूपेण द्वितीयस्थले ‘एत्तो’ इत्यादि सूत्रमेकम्। ततश्च चतुर्दशमार्गणानां नामनिरूपणरूपेण तृतीयस्थले सूत्रद्वयं। तत: परं गुणस्थानप्रतिपादनार्थं अष्टानुयोगनामसूचनपरत्वेन चतुर्थस्थले ‘एदेसिं’ इत्यादिसूत्रत्रयं। एवं षट्खण्डागमग्रन्थराजस्य, सत्प्ररूपणाया: पीठिकाधिकारे चतुर्भिरन्तरस्थलै: सप्तसूत्रै: समुदायपातनिका सूचितास्ति।
अथ श्रीमद्भगवद्धरसेनगुरुमुखादुपलब्धज्ञानभव्यजनानां वितरणार्थं पंचमकालान्त्य-वीरांगजमुनिपर्यंतं गमयितुकामेन पूर्वाचार्यव्यवहारपरंपरानुसारेण शिष्टाचारपरिपालनार्थं निर्विघ्नसिद्धान्त-शास्त्रपरिसमाप्त्यादिहेतो: श्रीमत्पुष्पदन्ताचार्येण णमोकारमहामन्त्रमंगलगाथा-सूत्रावतार: क्रियते-
णमो अरिहंताणं, णमो सिद्धाणं, णमो आइरियाणं।
णमो उवज्झायाणं, णमो लोए सव्व-साहूणं।।१।।
जिनेन्द्रदेव के मुखकमल से निकलकर जो गौतमस्वामी के मुखरूपी कुण्ड में अवतरित-गिरी है तथा पुष्पदन्त आचार्य आदि के द्वारा विस्तारित गंगाजल के समान ‘‘नदी से भरे हुए नये घड़े के जल सदृश’’ यह टीका सभी प्राणियों के मन को संतृप्त करेगी, ऐसा मेरा विश्वास है।
अब यहाँ श्रीमान् पुष्पदन्त आचार्यदेव द्वारा रचित गुणस्थान आदि बीस प्ररूपणाओं में अन्तर्गर्भित इस सत्प्ररूपणा नामक ग्रंथ में अधिकारशुद्धिपूर्वक पातनिका का व्याख्यान किया जाता है। उसमें सबसे पहले ‘‘णमो अरिहंताणं’’ इत्यादि इस पञ्च नमस्कार गाथा को आदि में करके सूत्र पाठ के क्रम से गुणस्थान, मार्गणा के प्रतिपादन की सूचना देने वाले ‘‘एत्तो इमेसिं’’ इत्यादि सात सूत्र हैं। उसके बाद चौदह गुणस्थानों के निरूपण की मुख्यता से ‘‘ओघेण अत्थि’’ इत्यादि सोलह सूत्र हैं। पुन: आगे चौदह मार्गणाओं में गुणस्थान व्यवस्था की मुख्यता से ‘‘आदेसेण गदियाणुवादेण’’ इत्यादि एक सौ चौवन (१५४) सूत्र हैं। इस प्रकार अनेक अन्तस्थलों से गर्भित एक सौ सतहत्तर (१७७) सूत्रों के द्वारा ये तीन महाधिकार हो गए हैं। सत्प्ररूपणा के व्याख्यान में यह समुदायपातनिका हुई।
यहाँ भी प्रथम महाधिकार में ‘‘णमो’’ इत्यादि मंगलाचरण रूप से प्रथम स्थल में एक गाथा सूत्र है पुन: द्वितीय स्थल में गुणस्थान-मार्गणा के कथन की प्रतिज्ञा रूप से ‘‘एत्तो’’ इत्यादि एक सूत्र है और उसके बाद चौदह मार्गणाओं के नाम निरूपण रूप से तृतीय स्थल में दो सूत्र हैं। उसके आगे गुणस्थानों के प्रतिपादन हेतु आठ अनुयोग के नाम सूचना की मुख्यता से चतुर्थ स्थल में ‘एदेसिं’’ इत्यादि तीन सूत्र हैं।
इस प्रकार षट्खण्डागम ग्रंथराज की सत्प्ररूपणा के पीठिका अधिकार में चार अन्तरस्थलों के द्वारा सूत्रों में समुदायपातनिका सूचित-प्रदर्शित की गई है।
अब श्रीमत् भगवान धरसेनाचार्य गुरु के मुख से उपलब्ध ज्ञान को भव्यजनों में वितरित करने के लिए पंचमकाल के अन्त में वीरांगज मुनि पर्यन्त इस ज्ञान को ले जाने की इच्छा से, पूर्वाचार्यों की व्यवहार परम्परा के अनुसार, शिष्टाचार का परिपालन करने के लिए, निर्विघ्न सिद्धान्त शास्त्र की परिसमाप्ति आदि हेतु को लक्ष्य में रखते हुए श्रीमत्पुष्पदन्ताचार्य के द्वारा णमोकार महामंत्र मंगल गाथा सूत्र का अवतार किया जाता है-
णमो अरिहंताणं, णमो सिद्धाणं, णमो आइरियाणं।
णमो उवज्झायाणं, णमो लोए सव्वसाहूणं।।१।।
अतिशयक्षेत्र महावीर जी में मैंने ‘तृतीय महाधिकार’ प्रारंभ किया था अत: श्री महावीर स्वामी को नमस्कार किया है। यथा-
महावीरो जगत्स्वामी, सातिशायीति विश्रुत:।
तस्मै नमोऽस्तु मे भक्त्या, पूर्णसंयमलब्धये।।१।।
श्री वीरसेनाचार्य ने कहा है-
‘‘सुत्तमोदिण्णं अत्थदो तित्थयरादो, गंथदो गणहरदेवादोत्ति१।।
ये सूत्र अर्थप्ररूपणा की अपेक्षा से तीर्थंकर भगवान से अवतीर्ण हुए हैं और ग्रंथ की अपेक्षा श्री गणधर देव से अवतीर्ण हुए हैं।
अथवा ‘जिनपालित’ शिष्य को निमित्त कहा है।
श्री पुष्पदंताचार्य ने अपने भानजे ‘जिनपालित’ को दीक्षा देकर प्रारंभिक १७७ सूत्रों की रचना करके भूतबलि आचार्य के पास भेजा था। ऐसा ‘धवलाटीका’ में एवं श्रुतावतार में वर्णित है।
इस मंगलाचरण को सूत्र १ संज्ञा दी है। आगे द्वितीय सूत्र का अवतार हुआ है-
एत्तो इमेसिं चोद्दसण्हं जीवसमासाणं मग्गणट्ठदाए तत्थ इमाणि चोद्दस चेवट्ठाणाणि णादव्वाणि भवंति।।२।।
इस द्रव्यश्रुत और भावश्रुतरूप प्रमाण से इन चौदह गुणस्थानों के अन्वेषण रूप प्रयोजन के लिए यहाँ से चौदह ही मार्गणास्थान जानने योग्य हैं।
ऐसा कहकर पहले चौदह मार्गणाओं के नाम बताए हैं। यथा-गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, लेश्या, भव्यत्व, सम्यक्त्व, संज्ञी और आहार ये चौदह मार्गणा हैं।
पुन: पांचवें सूत्र में कहा है-
इन्हीं चौदह गुणस्थानों का निरूपण करने के लिए आगे कहे जाने वाले आठ अनुयोगद्वार जानने योग्य हैंं।।५।।
इन आठों के नाम-
| १. सत्प्ररूपणा | २. द्रव्यप्रमाणानुगम |
| ३. क्षेत्रानुगम | ४. स्पर्शनानुगम |
| ५. कालानुगम | ६. अन्तरानुगम |
| ७. भावानुगम और | ८. अल्पबहुत्वानुगम। |
आगे प्रथम ‘सत्प्ररूपणा’ का वर्णन करते हुए ओघ और आदेश की अपेक्षा निरूपण करने को कहा है।
इसी में ओघ की अपेक्षा चौदह गुणस्थानों का वर्णन है और आगे चौदह मार्गणाओं का वर्णन करके उनमें गुणस्थानों को भी घटित किया है। मार्गणाओं के नाम ऊपर लिखे गये हैं।
गुणस्थानों के नाम-
| १. मिथ्यात्व | २. सासादन |
| ३. मिश्र | ४. असंयतसम्यग्दृष्टि |
| ५. देशसंयत | ६. प्रमत्तसंयत |
| ७. अप्रमत्तसंयत | ८. अपूर्वकरण |
| ९. अनिवृत्तिकरण | १०. सूक्ष्मसांपराय |
| ११. उपशांतकषाय | १२. क्षीणकषाय |
| १३. सयोगिकेवली | १४. अयोगिकेवली ये चौदह गुणस्थान हैं। |
इस ग्रंथ में मैंने तीन महाधिकार विभक्त किये हैं। प्रथम महाधिकार में सात सूत्र हैं जो कि ग्रंथ की पीठिका-भूमिका रूप हैं। दूसरे महाधिकार सत्प्ररूपणा के अंतर्गत १६ सूत्रों में चौदह गुणस्थानों का वर्णन है एवं तृतीय महाधिकार में मार्गणाओं में गुणस्थानों की व्यवस्था करते हुए विस्तार से १५४ सूत्र लिए हैं।
इस प्रथम ग्रंथ में प्रारंभ में पंच परमेष्ठियों के वर्णन में एक सुन्दर प्रश्नोत्तर धवला टीका में आया है जिसे मैंने जैसे का तैसा लिया है। यथा-
‘‘संपूर्णरत्नानि देवो न तदेकदेश इति चेत् ?
न, रत्नैकदेशस्य देवत्वाभावे समस्तस्यापि तदसत्त्वापत्ते । इत्यादि।
शंका-संपूर्णरत्न-पूर्णता को प्राप्त रत्नत्रय ही देव है, रत्नों का एकदेश देव नहीं हो सकता है ?
समाधान-ऐसा नहीं कहना, क्योेंकि रत्नत्रय के एकदेश में देवपने का अभाव होने पर उसकी संपूर्णता में भी देवपना नहीं बन सकता है।
शंका-आचार्य आदि में स्थित रत्नत्रय समस्त कर्मों का क्षय करने में समर्थ नहीं हो सकते, क्योंकि उसमें एकदेशपना ही है, पूर्णता नहीं है ?
समाधान-यह कथन समुचित नहीं है, क्योंकि पलालराशि-घास की राशि को जलाने का कार्य अग्नि के एक कण में भी देखा जाता है इसलिए आचार्य, उपाध्याय और साधु भी देव हैं१।’’
यह समाधान श्री वीरसेनाचार्य ने बहुत ही उत्तम बताया है।
प्रथम पुस्तक ‘सत्प्ररूपणाग्रंथ’ की टीका को पूर्ण करते समय मैंने उस स्थान का विवरण दे दिया है। यथा-
‘‘वीराब्दे द्वाविंशत्यधिकपंचविंशतिशततमे फाल्गुनशुक्लासप्तम्यां ख्रिष्ट्राब्दे षण्णवत्यधि-कैकोनविंशतिशततमे पंचविशे दिनांके द्वितीयमासि (२५-२-१९९६) राजस्थानप्रान्ते ‘पिडावानाम-ग्रामे’ श्री पार्श्वनाथसमवसरणमंदिरशिलान्यासस्य मंगलावसरे एतत्सत्प्ररूपणाग्रन्थस्य ‘सिद्धान्त-चिन्तामणिटीकां’ पूरयन्त्या मया महान् हर्षोऽनुभूयते। टीकासहितोऽयं ग्रन्थो मम श्रुतज्ञानस्य पूर्त्यै भूयात्।’’
पुन: वीर निर्वाण संवत् पच्चीस सौ बाईसवें वर्ष में ही फाल्गुन शुक्ला सप्तमी तिथि को ईसवी सन् १९९६ के द्वितीय मास की २५ तारीख को राजस्थान प्रान्त के पिड़ावा ग्राम में श्रीपार्श्वनाथ समवसरण मंदिर के शिलान्यास के मंगल अवसर पर इस ‘सत्प्ररूपणा’ ग्रंथ की ‘सिद्धान्तचिन्तामणिटीका’ को पूर्ण करते हुए मुझे अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही है। टीका सहित यह सत्प्ररूपणा नामक ‘षट्खण्डागम’ ग्रंथ मेरे श्रुतज्ञान की पूर्ति के लिए होवे, यही मेरी प्रार्थना है। इसमें सूत्र १७७ तथा पृ. १६४ हैं।
पुस्तक २-आलाप अधिकार
यह द्वितीय ग्रंथ सत्प्ररूपणा के ही अंतर्गत है। इसमें सूत्र नहीं हैं।
‘‘संपहि संत-सुत्तविवरण-समत्ताणंतरं तेसिं परुवणं भणिस्सामो।’’
सत्प्ररूपणा के सूत्रों का विवरण समाप्त हो जाने पर अनंतर अब उनकी प्ररूपणा का वर्णन करते हैं-
शंका-प्ररूपणा किसे कहते हैं ?
समाधान-सामान्य और विशेष की अपेक्षा गुणस्थानों में, जीवसमासों में, पर्याप्तियों में, प्राणों में, संज्ञाओं में, गतियों में, इन्द्रियों में, कायों में, योगों में, वेदों में, कषायों में, ज्ञानों में, संयमों में, दर्शनों में, लेश्याओं में, भव्यों में, अभव्यों में, संंज्ञी-असंज्ञियों में, आहारी-अनाहारियों में और उपयोगों में पर्याप्त और अपर्र्याप्त विशेषणों से विशेषित करके जो जीवों की परीक्षा की जाती है, उसे प्ररूपणा कहते हैं। कहा भी है-
गुणस्थान, जीवसमास, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा, चौदह मार्गणाएँ और उपयोग, इस प्रकार क्रम से बीस प्ररूपणाएँ कही गई हैं।
इनके कोष्ठक गुणस्थानों के एवं मार्गणाओं के बनाये गये हैं।
गुणस्थान १४ हैं, जीवसमास १४ हैं-एकेन्द्रिय के बादर-सूक्ष्म ऐसे २, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय ऐसे ३, पंचेन्द्रिय के संज्ञी-असंज्ञी ऐसे २, ये ७ हुए, इन्हें पर्याप्त-अपर्याप्त से गुणा करने पर १४ हुए।
पर्याप्ति ६-आहार, शरीर, इन्द्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन।
प्राण १० हैं-पाँच इन्द्रिय, मनोबल, वचनबल, कायबल, आयु और श्वासोच्छ्वास।
संज्ञा ४ हैं-आहार, भय, मैथुन और परिग्रह। गति ४ हैं-नरकगति, तिर्यंचगति, मनुष्यगति और देवगति।
इन्द्रियाँ ५ हैं-एकेन्द्रियजाति, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पंचेन्द्रियजाति।
काय ६ हैं-पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति और त्रसकाय।
योग १५ हैं-सत्यमनोयोग, असत्यमनोयोग, उभयमनोयोग,अनुभयमनोयोग, सत्यवचनयोग, असत्यवचनयोग, उभयवचनयोग, अनुभयवचनयोग, औदारिककाययोग, औदारिकमिश्र, वैक्रियिक, वैक्रियिकमिश्र, आहारक, आहारकमिश्र और कार्मणकाय योग।
वेद ३ हैं-स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद।
कषाय ४ हैं-क्रोध, मान, माया, लोभ।
ज्ञान ८ हैं-मति, श्रुत, अवधि, मन:पर्यय, केवलज्ञान, कुमति, कुश्रुत और विभंगावधि।
संयम ७ हैं-सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहारविशुद्धि, सूक्ष्मसांपराय, यथाख्यात, देशसंयम और असंयम।
दर्शन ४ हैं-चक्षुर्दर्शन, अचक्षुर्दर्शन, अवधिदर्शन और केवलदर्शन।
लेश्या ६ हैं-कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म और शुक्ल।
भव्य मार्गणा २ हैं-भव्यत्व और अभव्यत्व।
सम्यक्त्व ६ हैं-औपशमिक, क्षायोपशमिक, क्षायिक, मिथ्यात्व, सासादन और मिश्र।
संज्ञी मार्गणा के २ भेद हैं-संज्ञी, असंज्ञी।
आहार मार्गणा २ हैं-आहार, अनाहार।
उपयोग के २ भेद हैं-साकार और अनाकार।
इस ग्रंथ को मैंने दो महाधिकारों में विभक्त किया है। इसमें कुल ५४५ कोष्ठक-चार्ट हैं। उदाहरण के लिए पाँचवें गुणस्थान का एक चार्ट दिया जा रहा है-
नं. १३
संयतासंयतों के आलाप
| गु. | जी. | प. | प्रा. | सं. | ग. | इं. | का. | यो. | वे. | क. | ज्ञा. | संय. | द. | ले. | भ. | स. | संज्ञि. | आ. | उ. |
| १
देश |
१
सं.प. |
६ | १० | ४ | २
म. ति. |
१
पंचे. |
१
त्रस. |
९
म.४ व. ४ औ.१ |
३ | ४ | ३
मति. श्रुत. अव. |
१
संयमा |
३
के.द. विना. शुभ. |
द्र.३
भा.३ |
१
भ. |
३
औ. क्षा. क्षायो. |
१
सं. |
१
आहार |
२
साकार अनाकार |
इनमें से संयतासंयत के कोष्ठक में-
गुणस्थान १ है-पाँचवां देशसंयत।
जीवसमास १ है-संज्ञीपर्याप्त।
पर्याप्तियाँ छहों हैं, अपर्याप्तियाँ नहीं हैं।
प्राण १० हैं।
संज्ञायें ४ हैं।
गति २ हैं-मनुष्य, तिर्यंच।
इंद्रिय १ है-पंचेन्द्रिय।
काय १ है-त्रसकाय।
योग ९ हैं-४ मनोयोग, ४ वचनयोग, १ औदारिक काययोग।
वेद ३ हैं।
कषाय ४ हैं।
ज्ञान ३ हैं-मति, श्रुत, अवधि।
संयम १ है-संयमासंयम।
दर्शन ३ हैं-केवलदर्शन के बिना।
लेश्या द्रव्य से-वर्ण से छहों हैं, भावलेश्या शुभ ३ हैं।
भव्यत्व १ है।
सम्यक्त्व ३ हैं-औपशमिक, क्षायिक और क्षायोपशमिक।
संज्ञीमार्गणा १ है-संज्ञी।
आहार मार्गणा १ है-आहारक।
उपयोग २ हैं-साकार और अनाकार।
यही सब चार्ट में दिखाया गया है। मेरे द्वारा लिखित पृ. ९० हैं। इस प्रकार यह दूसरी पुस्तक का सार अतिसंक्षेप में बताया गया है।
पुस्तक ३-द्रव्यप्रमाणानुगम-क्षेत्रानुगम
इस ग्रंथ में श्री भूतबलि आचार्य वर्णित सूत्र हैं अब यहाँ से संपूर्ण ‘षट्खण्डागम’ सूत्रों की रचना इन्हीं श्रीभूतबलि आचार्य द्वारा लिखित है। कहा भी है-
‘‘संपहि चोद्दसण्हं जीवसमासाणमत्थित्तमवगदाणं सिस्साणं तेसिं चेव परिमाणपडिबोहणट्ठं भूदबलियाइरियो सुत्तमाह१-’’
जिन्होंने चौदहों गुणस्थानों के अस्तित्व को जान लिया है, ऐसे शिष्यों को अब उन्हीं के चौदहों गुणस्थानों के-चौदहों गुणस्थानवर्ती जीवों के परिमाण-संख्या के ज्ञान को कराने के लिए श्रीभूतबलि आचार्य आगे का सूत्र कहते हैं-
इसमें प्रथम सूत्र-
‘‘दव्वपमाणाणुगमेण दुविहो णिद्देसो ओघेण आदेसेण य।।१।।
द्रव्यप्रमाणानुगम की अपेक्षा निर्देश दो प्रकार का है, ओघ निर्देश और आदेशनिर्देश। ओघ-गुणस्थान और आदेश-मार्गणा इन दोनों की अपेक्षा से उन-उन में जीवों का वर्णन किया गया है।
इस ग्रंथ में भी मैंने दो अनुयोगद्वार लिये हैंं-द्रव्यप्रमाणानुगम और क्षेत्रानुगम। अत: इन दोनों में चार महाधिकार किये हैं। द्रव्यप्रमाणानुगम में प्रथम महाधिकार में १४ सूत्र हैं एवं द्वितीय में १७८ हैं, ऐसे कुल सूत्र १९२ हैं। क्षेत्रानुगम में तृतीय महाधिकार में ४ सूत्र एवं चतुर्थ महाधिकार में ८८ सूत्र हैं, ऐसे कुल सूत्र ९२ हैं। दोनों अनुयोगद्वारों में सूत्र १९२+९२=२८४ हैं। पृ. १३० हैं।
चौदह गुणस्थानों में जीवों की संख्या बतलाते हैं-
प्रथम गुणस्थान में जीव अनंतानंत हैं। द्वितीय गुणस्थान में ५२ करोड़ हैं। तृतीय गुणस्थान में १०४ करोड़ हैं। चतुर्थ गुणस्थान में सात सौ करोड़ हैंं। पाँचवें गुणस्थान में १३ करोड़ हैं।
प्रमत्तसंयत नाम के छठे गुणस्थान से लेकर अयोगकेवली नाम के चौदहवें गुणस्थान के महामुनि एवं अरहंत भगवान ‘संयत’ कहलाते हैं। उन सबकी संख्या मिलाकर ‘तीन कम नव करोड़’ है। धवला टीका में कहा है-
‘‘एवं परुविदसव्वसंजदरासिमेकट्ठे कदे अट्ठकोडीओ णवणउदिलक्खा णवणउदिसहस्स-णवसद-सत्ताणउदिमेत्तो होदि१।’’
इसी तृतीय पुस्तक में दूसरा एक और मत प्राप्त हुआ है-
‘‘एदे सव्वसंजदे एयट्ठे कदे सत्तरसद-कम्मभूमिगद-सव्वरिसओ भवंति। तेसिं पमाणं छक्कोडीओ णवणउइलक्खा णवणउदिसहस्सा णवसयछण्णउदिमेत्तं हवदि२।’’ सर्वसंयतों की संख्या छह करोड़, निन्यानवे लाख, निन्यानवे हजार, नव सौ छ्यानवे है।
इन दोनों मतों को श्री वीरसेनाचार्य ने उद्धृत किया है।
वर्तमान में प्रसिद्धि में ‘तीन कम नव करोड़’ संख्या ही है।
इन सर्व मुनियों को नमस्कार करके यहाँ इस ग्रंथ का किंचित् सार दिया है। इसकी सिद्धान्तचिंतामणि टीका में मैंने अधिकांश गणित प्रकरण छोड़ दिया है, जो कि धवलाटीका में द्रष्टव्य है।
श्री वीरसेनाचार्य ने आकाश को क्षेत्र कहा है। आकाश का कोई स्वामी नहीं है, इस क्षेत्र की उत्पत्ति में कोई निमित्त भी नहीं है यह स्वयं में ही आधार-आधेयरूप है। यह क्षेत्र अनादिनिधन है और भेद की अपेक्षा लोकाकाश-अलोकाकाश ऐसे दो भेद हैं। इस प्रकार निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति और विधान से क्षेत्र का वर्णन किया है।
क्षेत्र में गुणस्थानवर्ती जीवों को घटित करते हुए कहा है-
‘‘ओघेण मिच्छाइट्ठी केवडि खेत्ते ? सव्वलोगे।।२।।
मिथ्यादृष्टि जीव कितने क्षेत्र में हैं ? सर्व लोक में हैं।।२।।
सासणसम्माइट्ठिप्पहुडि जाव अजोगिकेवलि त्ति केवडि खेत्ते ? लोगस्स असंखेज्जदिभाए।।३।।
सासादन सम्यग्दृष्टि से लेकर अयोगिकेवली पर्यंत कितने क्षेत्र में हैं ? लोक के असंख्यातवें भाग में हैं।।३।।
इसमें एक प्रश्न हुआ है-
लोकाकाश असंख्यातप्रदेशी है, उसमें अनंतानंत जीव वैâसे समायेंगे ?
यद्यपि लोक असंख्यात प्रदेशी है फिर भी उसमें अवगाहन शक्ति विशेष है जिससे उसमें अनंतानंत जीव एवं अनंतानंत पुद्गल समाविष्ट हैं। जैसे मधु से भरे हुए घड़े में उतना ही दूध भर दो, उसी में समा जायेगा१।
इस अनुयोगद्वार में स्वस्थान, समुद्घात और उपपाद ऐसे तीन भेदों द्वारा जीवों के क्षेत्र का वर्णन किया है।
इस ग्रंथ की पूर्ति मैंने मांगीतुंगी तीर्थ पर श्रावण कृ. १० को ईसवी सन् १९९६ में की है।
पुस्तक ४-स्पर्शन-कालानुगम
इस चतुर्थ ग्रंथ-पुस्तक में स्पर्शनानुगम एवं कालानुगम इन दो अनुयोगद्वारों का वर्णन है।
इन दोनों की सूत्र संख्या १८५+३४२=५२७ है।
स्पर्शनानुगम-इसमें भी मैंने गुणस्थान और मार्गणा की अपेक्षा दो महाधिकार किये हैं। यह स्पर्शन भूतकाल एवं वर्तमानकाल के स्पर्श की अपेक्षा रखता है। पूर्व में जिसका स्पर्श किया था और वर्तमान में जिसका स्पर्श कर रहे हैं, इन दोनों की अपेक्षा से स्पर्शन का कथन किया जाता है।
स्पर्शन में छह प्रकार के निक्षेप घटित किये हैं-नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावस्पर्शन।
‘तत्र स्पर्शनशब्द:’ नाम स्पर्शनं निक्षेप:, अयं द्रव्यार्थिकनयविषय:।
सोऽयं इति बुद्ध्या अन्यद्रव्येण सह अन्यद्रव्यस्य एकत्वकरणं स्थापनास्पर्शनं यथा घटपिठरादिषु अयं ऋषभोऽजित: संभवोऽभिनंदन: इति। एषोऽपि द्रव्यार्थिकनयविषय:१।’’
स्पर्शन शब्द नामस्पर्शन है। यह द्रव्यार्थिकनय का विषय है। यह वही है, ऐसी बुद्धि से अन्य द्रव्य के साथ अन्य द्रव्य का एकत्व करना स्थापनास्पर्शन निक्षेप है जैसे घट आदि में ये ऋषभदेव हैं, अजितनाथ हैं, संभवनाथ हैं, अभिनंदननाथ हैं इत्यादि। यह भी द्रव्यार्थिक नय का विषय है, इत्यादि निक्षेपों का वर्णन है।
पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा से प्ररूपणा करते हुए कहा है-
स्वस्थानस्वस्थान-वेदना-कषाय-मारणांतिक-उपपादगत मिथ्यादृष्टियों ने भूतकाल एवं वर्तमानकाल से सर्वलोक को स्पर्श किया है।
इसी प्रकार गुणस्थान और मार्गणाओं में जीवों के भूतकालीन, वर्तमानकालीन स्पर्शन का वर्णन किया है।
कालानुगम-इसमें भी गुणस्थान और मार्गणा की अपेक्षा दो महाधिकार कहे हैं। काल को नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव ऐसे चार भेद रूप से कहा है पुनश्च-‘नो आगमभावकाल’ से इस ग्रंथ में वर्णन किया है।
यह काल अनादि अनंत है, एक विध है, यह सामान्य कथन है। काल के भूत, वर्तमान और भविष्यत् की अपेक्षा तीन भेद हैं।
एक प्रश्न आया है-
स्वर्गलोक में सूर्य के गति की अपेक्षा नहीं होने से वहां मास, वर्ष आदि का व्यवहार कैसे होगा ?
तब आचार्यदेव ने समाधान दिया है-
यहाँ के व्यवहार की अपेक्षा ही वहाँ पर ‘काल’ का व्यवहार है। जैसे जब यहाँ ‘कार्तिक’ आदि मास में आष्टान्हिक पर्व आते हैं, तब देवगण नंदीश्वर द्वीप आदि में पूजा करने पहुँच जाते हैं इत्यादि।
नाना जीव की अपेक्षा मिथ्यादृष्टि का सर्वकाल है।।२।।
एकजीव की अपेक्षा किसी का अनादिअनंत है, किसी का अनादिसांत है, किसी का सादिसांत है। इनमें से जो सादि और सांत काल है, उसका निर्देश इस प्रकार है। एक जीव की अपेक्षा मिथ्यादृष्टि जीव का सादिसांत काल जघन्य से अंतर्मुहूर्त है१।।३।।
वह इस प्रकार है-
कोई सम्यग्मिथ्यादृष्टि अथवा असंयतसम्यग्दृष्टि अथवा संयतासंयत अथवा प्रमत्तसंयतजीव परिणामों के निमित्त से मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ। सर्वजघन्य अंतर्मुहूर्त काल रह करके, फिर भी सम्यक्त्व मिथ्यात्व को अथवा असंयम के साथ सम्यक्त्व को अथवा संयमासंयम को अथवा अप्रमत्तभाव के साथ संयम को प्राप्त हुआ। इस प्रकार से प्राप्त होने वाले जीव के मिथ्यात्व का सर्वजघन्य काल होता है२।
इस प्रकार यह कालानुगम का संक्षिप्त सार दिखाया है।
इस ग्रंथ की टीका मैंने मांंगीतुंगी क्षेत्र पर भाद्रपद शु. ३, वी.सं. २५२२, दिनाँक १५-९-१९९६ को लिखकर पूर्ण की है। इसमें पृ. १९० हैं।
पुस्तक ५-अन्तर-भाव-अल्पबहुत्वानुगम
इस ग्रंथ में अन्तरानुगम में ३९७ सूत्र हैं, भावानुगम में ९३ सूत्र हैं एवं अल्पबहुत्वानुगम में ३८२ सूत्र हैं। इस प्रकार ३९७+९३+३८२=८७२ सूत्र हैं।
अन्तरानुगम-इस ग्रंथ की सिद्धान्तचिन्तामणि टीका में मैंने दो महाधिकार विभक्त किये हैं। प्रथम महाधिकार में गुणस्थानों में अंतर का निरूपण है। द्वितीय महाधिकार में मार्गणाओं में अंतर दिखाया गया है।
नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव के भेद से छहविध निक्षेप हैं। अंतर, उच्छेद, विरह, परिणामान्तरगमन, नास्तित्वगमन और अन्यभावव्यवधान, ये सब एकार्थवाची हैं। इस प्रकार के अन्तर के अनुगम को अन्तरानुगम कहते हैं।
एक जीव की अपेक्षा जघन्य अन्तर काल अन्तर्मुहूर्त है।।३।।
जैसे एक मिथ्यादृष्टि जीव सम्यग्मिथ्यात्व, अविरतसम्यक्त्व, संयमासंयम और संयम में बहुत बार परिवर्तित होता हुआ परिणामों के निमित्त से सम्यक्त्व को प्राप्त हुआ और वहाँ पर सर्वलघु अंतर्मुहूर्त काल तक सम्यक्त्व के साथ रहकर मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ। इस प्रकार सर्वजघन्य अंतर्मुहूर्त प्रमाण मिथ्यात्वगुणस्थान का अंतर प्राप्त हो गया।
मिथ्यात्व का उत्कृष्ट अंतर कुछ कम दो छ्यासठ सागरोपम काल है।।४।।
इन ग्रंथों के स्वाध्याय में जो आल्हाद उत्पन्न होता है, वह असंख्यात गुणश्रेणी रूप से कर्मों की निर्जरा का कारण है। यहाँ तो मात्र नमूना प्रस्तुत किया जा रहा है।
भावानुगम-इसमें भी महाधिकार दो हैं। नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव इनकी अपेक्षा यह भाव चार प्रकार का है। इसमें भी भावनिक्षेप के आगमभाव एवं नोआगमभाव ऐसे दो भेद हैं। नोआगमभाव नामक भावनिक्षेप के औदयिक, औपशमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक और पारिणामिक ये पाँच भेद हैं।
असंयतसम्यग्दृष्टि में कौन सा भाव है ?
औपशमिकभाव भी है, क्षायिकभाव भी है और क्षायोपशमिक भाव भी है।।५।।
यहाँ सम्यग्दर्शन की अपेक्षा से ये भाव कहे हैं। यद्यपि यहाँ औदयिक भावों में से गति, कषाय आदि भी हैं किन्तु उनसे सम्यक्त्व उत्पन्न नहीं होता इसलिए उनकी यहाँ विवक्षा नहीं है।
अल्पबहुत्वानुगम-इस अनुयोगद्वार के प्रारंभ में मैंने गद्यरूप में श्री महावीर स्वामी को नमस्कार किया है। इसमें भी दो महाधिकार विभक्त किये हैं।
इस अल्पबहुत्व में गुणस्थान और मार्गणाओं में सबसे अल्प कौन हैं ? और अधिक कौन हैं ? यही दिखाया गया है। यथा-
सामान्यतया-गुणस्थान की अपेक्षा से अपूर्वकरण आदि तीन गुणस्थानों में उपशामक जीव प्रवेश की अपेक्षा परस्पर तुल्य हैं तथा अन्य सब गुणस्थानों के प्रमाण से अल्प हैं१।।२।।
और ‘मिथ्यादृष्टि सबसे अधिक अनंतगुणे हैें२।।१४।।
इस ग्रंथ में भी बहुत से महत्वपूर्ण विषय ज्ञातव्य हैं। जैसे कि-‘‘दर्शनमोहनीय का क्षपण करने वाले-क्षायिक सम्यक्त्व प्रगट करने वाले जीव नियम से मनुष्यगति में होते हैं।’’
जिन्होंने पहले तिर्यंचायु का बंध कर लिया है ऐसे जो भी मनुष्य क्षायिक सम्यक्त्व के साथ तिर्यंचों में उत्पन्न होते हैं उनके संयमासंयम नहीं होता है, क्योंकि भोगभूमि को छोड़कर उनकी अन्यत्र उत्पत्ति असंभव है३।’’
यह सभी सार रूप अंश मैंने यहाँ दिये हैं। अपने ज्ञान के क्षयोपशम के अनुसार इन-इन ग्रंथो का स्वाध्याय श्रुतज्ञान की वृद्धि एवं आत्मा में आनंद की अनुभूति के लिए करना चाहिए।
इस ग्रंथ की टीका की पूर्ति मैंने अंकलेश्वर-गुजरात में मगसिर कृ. ७, वीर नि. सं. २५२३, दिनाँक २-१२-१९९६ को की है। इसमें पृ. १९३ हैं।
पुस्तक ६-जीवस्थान चूलिका
इस ग्रंथ में चूलिका के नौ भेद हैं-
| १. प्रकृतिसमुत्कीर्तन, | २. स्थान समुत्कीर्तन |
| ३. प्रथम महादण्डक | ४. द्वितीय महादण्डक |
| ५.तृतीय महादण्डक | ६. उत्कृष्टस्थिति |
| ७. जघन्यस्थिति | ८. सम्यक्त्वोत्पत्ति एवं |
| ९. गत्यागती चूलिका। |
इसमें क्रमश: सूत्रों की संंख्या-४६+११७+२+२+२+४४+४३+१६+२४३=५१५ है। पृ. १८७ हैं।
चूलिका-पूर्वोक्त आठों अनुयोगद्वारों के विषय-स्थलों के विवरण के लिए यह चूलिका नामक अधिकार आया है।
१. प्रकृतिसमुत्कीर्र्तन-इस चूलिका में ज्ञानावरणीय आदि आठ प्रकृतियों का वर्णन करके उनके १४८ भेदों का भी निरूपण किया है।
२. स्थानसमुत्कीर्तन-स्थान, स्थिति और अवस्थान ये तीनों एकार्थक हैं। समुत्कीर्तन, वर्णन और प्ररूपण इनका भी अर्थ एक ही है। स्थान की समुत्कीर्तना-स्थान समुत्कीर्तन है।
पहले प्रकृति समुत्कीर्तन में जिन प्रकृतियों का निरूपण कर आए हैं, उन प्रकृतियों का क्या एक साथ बंध होता है ? अथवा क्रम से होता है ? ऐसा पूछने पर इस प्रकार होता है। यह बात बतलाने के लिए यह स्थान समुत्कीर्तन है।
वह प्रकृतिस्थान मिथ्यादृष्टि के अथवा सासादन के, सम्यग्मिथ्यादृष्टि के, असंयतसम्यग्दृष्टि के, संयतासंयत के और संयत के होता है। ऐसे यहाँ छह स्थान ही विवक्षित हैं क्योंकि ‘संयत’ पद से छठे, सातवें, आठवें, नवमें, दशवें, ग्यारहवें, बारहवें और तेरहवें गुणस्थानवर्ती संयतों को लिया है। अयोगकेवली गुणस्थान में बंध का ही अभाव है अत: उन्हें नहीं लिया है।
जैसे ज्ञानावरण की पाँचों प्रकृतियों का बंध छहों स्थानों में अर्थात् दशवें गुणस्थान तक संयतों में होता है इत्यादि।
३. प्रथम महादण्डक-प्रथमोपशम सम्यक्त्व को ग्रहण करने के लिए अभिमुख मिथ्यादृष्टि जीवों के द्वारा बंधने वाली प्रकृतियों का ज्ञान कराने के लिए यहाँ तीन महादण्डकों की प्ररूपणा आई है।
इसमें प्रथम महादण्डक का कथन सम्यक्त्व के अभिमुख जीवों के द्वारा बध्यमान प्रकृतियों की समुत्कीर्तना करने के लिए हुआ है।
विशेषता यह है कि-
‘‘एदस्सवगमेण महापावक्खयस्सुवलंभादो१।’’
क्योंकि इसके ज्ञान से महापाप का क्षय पाया जाता है।
४. द्वितीय महादण्डक-प्रकृतियों के भेद से और स्वामित्व के भेद से इन दोनों दण्डकों में भेद कहा गया है।
५. तृतीय महादण्डक-प्रथमोपशम सम्यक्त्व के अभिमुख ऐसा नीचे सातवीं पृथ्वी का नारकी मिथ्यादृष्टि जीव पाँचों ज्ञानावरण, नवों दर्शनावरण, साता वेदनीय, मिथ्यात्व, अनंतानुबंधी आदि १६ कषाय, पुरुषवेद, हास्य, रति, भय, जुगुप्सा इन प्रकृतियों को बांधता है इत्यादि।
६. उत्कृष्ट कर्मस्थिति-कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति को बांधने वाला जीव प्रथमोपशम सम्यक्त्व को नहीं प्राप्त करता है, इस बात का ज्ञान कराने के लिए कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति का निरूपण किया जा रहा है।
७. जघन्यस्थिति-उत्कृष्ट विशुद्धि के द्वारा जो स्थिति बंधती है, वह जघन्य होती है। इत्यादि का विस्तार से कथन है।
८. सम्यक्त्वोत्पत्ति चूलिका-जिन प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेशों को बाँधता हुआ, जिन प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेशों के द्वारा सत्त्वस्वरूप होते हुए और उदीरणा को प्राप्त होते हुए यह जीव सम्यक्त्व को प्राप्त करता है, उनकी प्ररूपणा की गई है।
‘‘प्रथमोपशम सम्यक्त्व को प्राप्त करने वाला जीव पंचेन्द्रिय, संज्ञी, मिथ्यादृष्टि, पर्याप्त और सर्वविशुद्ध होता है२।।४।।’’
आगे-‘‘दर्शनमोहनीय कर्म का क्षपण करने के लिए आरंभ करता हुआ यह जीव कहाँ पर आरंभ करता है ? अढाई द्वीप समुद्रों में स्थित पंद्रह कर्मभूमियों में जहाँ जिस काल में जिनकेवली और तीर्थंकर होते हैं, वहाँ उस काल में आरंभ करता है१।।११।।’’
ऐसे दो नमूने प्रस्तुत किये हैं।
९. गत्यागती चूलिका-इसमें सम्यक्त्वोत्पत्ति के बाह्य कारणों को विशेष रूप से वर्णित किया है-
प्रश्न हुआ-‘‘तिर्यंच मिथ्यादृष्टि कितने कारणों से सम्यक्त्व उत्पन्न करते हैं ?।।२१।।
तीन कारणों से-कोई जातिस्मरण से, कितने ही धर्मोपदेश सुनकर, कितने ही जिनबिंबों के दर्शन से।।२२।।
पुन: प्रश्न होता है-जिनबिंब दर्शन प्रथमोपशम सम्यक्त्वोत्पत्ति में कारण वैâसे है ? उत्तर देते हैं-
‘‘जिणबिंबदंसणेण णिधत्तणिकाचिदस्स वि मिच्छत्तादिकम्मकलावस्स खयदंसणादो।
तथा चोक्तं-दर्शनेन जिनेन्द्राणां पापसंघातकुंजरम्।
शतधा भेदमायाति गिरिर्वङ्काहतो यथा२।।१।।’’
जिनप्रतिमाओं के दर्शन से निधत्त और निकाचित रूप भी मिथ्यात्वादि कर्मकलाप का क्षय देखा जाता है, जिससे जिनबिंब का दर्शन प्रथम सम्यक्त्व की उत्पत्ति में कारण देखा जाता है। कहा भी है-जिनेन्द्रदेवों के दर्शन से पापसंघातरूपी कुंजरपर्वत के सौ-सौ टुकड़े हो जाते हैं, जिस प्रकार वङ्का के गिरने से पर्वत के सौ-सौ टुकड़े हो जाते हैं।
२१६ सूत्र की टीका में अन्य ग्रंथों के उद्धरण भी दिये गये हैं। नमूने के लिए प्रस्तुत हैं-
आत्मज्ञातृतया ज्ञानं, सम्यक्त्वं चरितं हि स:।
स्वस्थो दर्शनचारित्रमोहाभ्यामनुपप्लुत:३।।
इस प्रथमखण्ड ‘जीवस्थान’ की छठी पुस्तक की टीका मैंने अपनी दीक्षाभूमि ‘‘माधोराजपुरा’’ राजस्थान में पूर्ण की है। उसमें मैंने संक्षेप में तीन श्लोक दिये हैं-
देवशास्त्रगुरुन् नत्वा, नित्य भक्त्या त्रिशुद्धित:।
षट्खण्डागमग्रंथोऽयं, वन्द्यते ज्ञानवृद्धये।।१।।
द्वित्रिपंचद्विवीराब्दे, फाल्गुनेऽसितपक्षके।
माधोराजपुराग्रामे, त्रयोदश्यां जिनालये।।२।।
नम: श्रीशांतिनाथाय, सर्वसिद्धिप्रदायिने।
यस्य पादप्रसादेन, टीकेयं पर्यपूर्यत।।३।।
मैंने शरदपूर्णिमा को वी.सं.२५२१ में हस्तिनापुर में यह टीका लिखना प्रारंभ किया था। मुझे प्रसन्नता है कि फाल्गुन कृष्णा १३, वी. नि. सं. २५२३, दि. ७-३-१९९७ को माधोराजपुरा में मैंने यह प्रथम खंड की टीका पूर्ण की है। यह टीका मांगीतुंगी यात्रा विहार के मध्य आते-जाते लगभग ३६ सौ किमी. के मध्य में मार्ग में अधिक रूप में लिखी गई है।
मैंने इसे सरस्वती देवी की अनुकंपा एवं माहात्म्य ही माना है। इसमें स्वयं में मुझे ‘आश्चर्य’ हुआ है। जैसा कि मैंने लिखा है-
‘‘पुनश्च हस्तिनापुरतीर्थक्षेत्रे विनिर्मितकृत्रिमजंबूद्वीपस्य सुदर्शनमेर्वादिपर्वतामुपरि विराजमान-सर्वजिनबिंबानि मुहुर्मुहु: प्रणम्य यत् सिद्धान्तचिंतामणिटीकालेखनकार्यं एकविंशत्युत्तरपंचविंशतिशततमे मया प्रारब्धं, तदधुना मांगीतुंगी सिद्धक्षेत्रस्य यात्राया: मंगलविहारकाले त्रयोविंशत्युत्तरपंचविंशतिशततमे वीराब्दे मार्गे एव निर्विघ्नतया जिनदेवकृपाप्रसादेन महद्हर्षोल्लासेन समाप्यते। एतत् सरस्वत्या देव्य: अनुकंपामाहात्म्यमेव विज्ञायते, मयैव महदाश्चर्यं प्रतीयते१।’’
इस खंड में कुल सूत्र संख्या १७७+२८४+५२७+८७२+५१५=२३७५ है।
मेरे द्वारा लिखित पेजों की संख्या १६४+९०+१३१+१९०+१९३+१८७=९५५ है।
इस प्रकार ‘जीवस्थान’ नामक प्रथम खण्ड (अंतर्गत छह पुस्तकों) का यह संक्षिप्त सार मैंने लिखा है।
द्वितीय खण्ड-क्षुद्रकबंध
इसे प्राकृत भाषा में ‘खुद्दाबंध’ कहते हैं एवं संस्कृत भाषा में ‘क्षुद्रकबंध’ नाम है।
इसे क्षुद्रक बंध कहने का अभिप्राय यह है कि-
आगे स्वयं भूतबलि आचार्य ने ‘तीस हजार’ सूत्रों में ‘महाबंध’ नाम से छठा खण्ड स्वतंत्र बनाया है इसीलिए १५९४ सूत्रों में रचित यह ग्रंथ ‘क्षुद्रकबंध’ नाम से सार्थक है।
इस ग्रंथ की टीका को मैंने ‘पद्मपुरा’ तीर्थ पर प्रारंभ किया था अत: मंगलाचरण में श्रीपद्मप्रभ भगवान को नमस्कार किया है। यथा-
श्रीपद्मप्रभदेवस्य, विश्वातिशयकारिणे।
नमोऽभीप्सितसिद्ध्यर्थं, ते च दिव्यध्वनिं नुम:।।१।।
इस खण्ड में जीवों की प्ररूपणा स्वामित्वादि ग्यारह अनुयोगों द्वारा गुणस्थान विशेषण को छोड़कर मार्गणा स्थानों में की गई है।
इन ग्यारह अनुयोग द्वारों के नाम-
| १. एक जीव की अपेक्षा स्वामित्व | २. एक जीव की अपेक्षा काल |
| ३. एक जीव की अपेक्षा अन्तर | ४. नाना जीवों की अपेक्षा भंगविचय |
| ५. द्रव्यप्रमाणानुगम | ६. क्षेत्रानुगम |
| ७. स्पर्शनानुगम | ८. नाना जीवों की अपेक्षा काल |
| ९. नाना जीवों की अपेक्षा अन्तर | १०. भागाभागानुगम और |
| ११. अल्पबहुत्वानुगम। |
अंत में ग्यारहों अनुयोगद्वारों की चूलिका रूप से ‘महादण्डक’ दिया गया है। यद्यपि इसमें अनुयोगद्वारों की अपेक्षा ११ अधिकार ही हैं फिर भी प्रारंभ में प्रस्तावना रूप में ‘बंधक सत्त्वप्ररूपणा’ और अंत में चूलिका रूप में महादण्डक ऐसे १३ अधिकार भी कहे जा सकते हैं।
बंधक सत्त्वप्ररूपणा-इसमें ४३ सूत्र हैं। जिनमें चौदह मार्गणाओं के भीतर कौन जीव कर्मबंध करते हैं और कौन नहीं करते, यह बतलाया गया है।
१. एक जीव की अपेक्षा स्वामित्व-इस अधिकार में मार्गणाओं संबंधी गुण व पर्याय कौन से भावों से प्रगट होते हैं, इत्यादि विवेचन है।
२. एक जीव की अपेक्षा काल-इस अनुयोगद्वार में प्रत्येक गति आदि मार्गणा में जीव की जघन्य और उत्कृष्ट कालस्थिति का निरूपण किया गया है।
३. एक जीव की अपेक्षा अंतर-एक जीव का गति आदि मार्गणाओं के प्रत्येक अवान्तर भेद से जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल-विरहकाल कितने समय का होता है ?
४. नाना जीवों की अपेक्षा भंगविचय-भंग-प्रभेद, विचय-विचारणा, इस अधिकार में भिन्न-भिन्न मार्गणाओं में जीव नियम से रहते हैं या कभी रहते हैं या कभी नहीं भी रहते हैं, इत्यादि विवेचना है।
५. द्रव्यप्रमाणानुगम-भिन्न-भिन्न मार्गणाओं में जीवों का संख्यात, असंख्यात और अनंत रूप से अवसर्पिणी-उत्सर्पिणी आदि काल प्रमाणों की अपेक्षा वर्णन है।
६. क्षेत्रानुगम-सामान्यलोक, अधोलोक, ऊर्ध्वलोक, तिर्यक्लोक और मनुष्यलोक, इन पाँचों लोकों के आश्रय से स्वस्थानस्वस्थान, विहारवत्स्वस्थान, सात समुद्घात और उपपाद की अपेक्षा वर्तमान क्षेत्र की प्ररूपणा की गई है।
७. स्पर्शनानुगम-चौदह मार्गणाओं में सामान्य आदि पाँचों लोकों की अपेक्षा वर्तमान और अतीतकाल के निवास को दिखाया है।
८. नाना जीवों की अपेक्षा कालानुगम-नाना जीवोें की अपेक्षा अनादि अनंत, अनादिसांत, सादि अनंत और सादि सान्त काल भेदों को लक्ष्य करके जीवों की काल प्ररूपणा की गई है।
९. नाना जीवों की अपेक्षा अन्तरानुगम-मार्गणाओं में नाना जीवों की अपेक्षा बंधकों के जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल का निरूपण किया गया है।
१०. भागाभागानुगम-इसमें मार्गणाओं के अनुसार सर्व जीवों की अपेक्षा बंधकों के भागाभाग का वर्णन है।
११. अल्पबहुत्वानुगम-चौदह मार्गणाओं के आश्रय से जीवसमासों का तुलनात्मक प्रमाण प्ररूपित किया है।
अनन्तर चूलिका रूप ‘महादण्डक’ अधिकार में गर्भोपक्रांतिक मनुष्य पर्याप्त से लेकर निगोद जीवों तक के जीवसमासों का ‘अल्पबहुत्व’ निरूपित है।
इस प्रकार क्रमश: इस द्वितीय खण्ड में सूत्रों की संख्या-
४३+९१+२१६+१५१+२३+१७१+१२४+२७४+५५+६८+८८+२०५+७९=१५९४ है।
मेरे द्वारा सिद्धांतचिंतामणि टीका में पृष्ठ संख्या-२८५ है।
महत्त्वपूर्ण विषय-इस ग्रंथ में एक महत्त्वपूर्ण विषय आया है, जिसे यहाँ उद्धृत किया जा रहा है-
‘‘बादरणिगोदपदिट्ठिदअपदिट्ठिदाणमेत्थ सुत्ते वणप्फदिसण्णा
किण्ण णिद्दिट्ठा ?गोदमो एत्थ पुच्छेयत्वो।
अम्हेहि गोदमो बादरणिगोदपदिट्ठिदाणं
वणप्फदिसण्णं णेच्छदि त्ति तस्स अहिप्पाओ कहिओ१।’’
शंका-वनस्पति नामकर्म के उदय से संयुक्त जीवों के वनस्पति संज्ञा देखी जाती है। बादरनिगोद प्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित जीवों को यहाँ सूत्र में ‘वनस्पतिसंज्ञा’ क्यों नहीं निर्दिष्ट की ?
समाधान-‘गौतम गणधर से पूछना चाहिए।’ गौतम गणधरदेव बादर निगोद प्रतिष्ठित जीवों की वनस्पति संज्ञा नहीं मानते। हमने यहाँ उनका अभिप्राय व्यक्त किया है।
इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि जहाँ सूत्रों में जैन ग्रंथों में दो मत आये हैं, वहाँ टीकाकारों ने अपना अभिमत न देकर दोनों ही रख दिये हैं।
इस ग्रंथ की टीका का समापन मैंने हस्तिनापुर में ‘रत्नत्रयनिलय वसतिका’ में मगसिर शुक्ला त्रयोदशी, वीर नि. संवत् २५२४, दिनाँक-१२-१२-१९९७ को पूर्ण की है।
उसकी संक्षिप्त प्रशस्ति इस प्रकार है-
वीराब्दे दिग्द्विखद्वयंके, शांतिनाथस्य सन्मुखे।
रत्नत्रयनिलयेऽस्मिन्, हस्तिनागपुराभिधे।।१।।
षट्खण्डागमग्रंथेऽस्मिन्, खण्डद्वितीयकस्य हि।
क्षुद्रकबंधनाम्नोऽस्य, टीकेयं पर्यपूर्यत।।२।।
गणिन्या ज्ञानमत्येयं, टीकाग्रन्थश्च भूतले।
जीयात् ज्ञानर्द्धये भूयात् भव्यानां मे च संततम्।।३।।
तृतीय खण्ड-बंधस्वामित्वविचय
पुस्तक ८-
इस तृतीय खण्ड में नाम के अनुसार ही बंध के स्वामी के बारे में विचार किया गया है। यथा-
‘‘जीवकम्माणं मिच्छत्तासंजमकसायजोगेहि एयत्तपरिणामो बंधो१।’’
जीव और कर्मों का मिथ्यात्व, असंयम, कषाय और योगों से जो एकत्व परिणाम होता है, वह बंध है और बंध के वियोग को मोक्ष कहते हैं।
बंध के स्वामित्व के विचय-विचारणा, मीमांसा और परीक्षा ये एकार्थक शब्द हैं।
वर्तमान में जो साधु या विद्वान् मिथ्यात्व को बंध में ‘अकिंचित्कर’ कहते हैं उन्हें इन षट्खण्डागम की पंक्तियों पर ध्यान देना चाहिए। अनेक स्थलों पर आचार्यों ने कहा है-
‘‘मिच्छत्तासंजमकसायजोगभेदेण चत्तारि मूलपच्चया२।’’
मिथ्यात्व, असंयम कषाय और योग ये चार बंध के मूलप्रत्यय-मूलकारण हैं।
यहाँ भी गुणस्थानों में बंध के स्वामी का विचार करके मार्गणाओं में वर्णन किया गया है।
सूत्रों में बंध-अबंध का प्रश्न करके उत्तर दिया है। यथा-‘‘पाँच ज्ञानावरणीय, चार दर्शनावरणीय, यश:कीर्ति, उच्चगोत्र और पाँच अंतराय इनका कौन बंधक है और कौन अबंधक है ?३।।५।।
सूत्र में ही उत्तर दिया है-
‘‘मिथ्यादृष्टि से लेकर सूक्ष्मसांपरायिक शुद्धसंयत उपशमक व क्षपक तक पूर्वोक्त ज्ञानावरणादि प्रकृतियों के बंधक हैं। सूक्ष्मसांपरायिक काल के अंतिम समय में जाकर इन प्रकृतियों का बंध व्युच्छिन्न होता है। ये बंधक हैं, शेष अबंधक हैं४।।६।।
यहाँ पाँचवें प्रश्नवाचक सूत्र में टीकाकार ने इस सूत्र को देशामर्शक मानकर तेईस पृच्छायें की हैं-
१. यहाँ क्या बंध की पूर्व में व्युच्छित्ति होती है ?
२. क्या उदय की पूर्व में व्युच्छित्ति होती है ?
३. या क्या दोनों की साथ में व्युच्छित्ति होती है ?
४. क्या अपने उदय के साथ इनका बंध होता है ?
५. क्या पर प्रकृतियों के उदय के साथ इनका बंध होता है ?
६. क्या अपने और पर दोनों के उदय के साथ इनका बंध होता है ?
७. क्या सांतर बंध होता है ?
८. क्या निरंतर बंध होता है ?
९. या क्या सांतर-निरंतर बंध होता है ?
१०. क्या सनिमित्तक बंध होता है ?
११. या क्या अनिमित्तक बंध होता है?
१२. क्या गति संयुक्तबंध होता है ?
१३. या क्या गति संयोग से रहित बंध होता है ?
१४. कितनी गति वाले जीव स्वामी हैं ?
१५. और कितनी गति वाले स्वामी नहीं हैं ?
१६. बंधाध्वान कितना है-बंध की सीमा किस गुणस्थान से किस गुणस्थान तक है ?
१७. क्या अंतिम समय में बंध की व्युच्छित्ति होती है ?
१८. क्या प्रथम समय में बंध की व्युच्छित्ति होती है ?
१९. या अप्रथम अचरिम समय में बंध की व्युच्छित्ति होती है ?
२०. क्या बंध सादि है ?
२१. या क्या अनादि है ?
२२. क्या बंध ध्रुव ही होता है ?
२३. या क्या अध्रुव होता है ?
इस प्रकार ये २३ पृच्छायें पूछी गईं इस पृच्छा में अंतर्भूत हैं, ऐसा जानना चाहिए।
पुन: इनका उत्तर दिया गया है।
इस प्रकार इस ग्रंथ में कुल ३२४ सूत्र हैं।
इस ग्रंथ की संस्कृत टीका मैंने मार्गशीर्ष कृ. १३ को (दिनाँक १२-१२-९७) हस्तिनापुर में प्रारंभ की थी। उस समय ‘श्री ऋषभदेव समवसरण श्रीविहार’ की योजना बनाई थी। भगवान ऋषभदेव का धातु का एक सुंदर ८’²८’ फुट का समवसरण बनवाया गया था। इसके उद्घाटन की तैयारियाँ चल रही थीं। इसी संदर्भ में मैंने मंगलाचरण में तीन श्लोक लिखे थे। यथा-
सिद्धान् नष्टाष्टकर्मारीन्, नत्वा स्वकर्महानये।
बंधस्वामित्वविचयो, ग्रंथ: संकीर्त्यते मया।।१।।
श्रीमत्-ऋषभदेवस्य, श्रीविहारोऽस्ति सौख्यकृत्।
जगत्यां सर्वजीवाना-मतो देव! जयत्विह।।२।।
यास्त्यनन्तार्थगर्भस्था, द्रव्यभावश्रुतान्विता।
सापि सूत्रार्थयुङ्मान्ये! श्रुतदेवि! प्रसीद न:।।३।।
पुन: दिल्ली में मैंने द्वि. ज्येष्ठ शु. ५ श्रुतपंचमी वीर नि.सं. २५२५ को (दि. १८-६-१९९९ को) डेढ़ वर्ष में प्रीतविहार में श्रीऋषभदेव कमलमंदिर में पूर्ण किया है। इसमें मेरे लिखे पृ. २३० हैं।
इस ग्रंथ के अंत में मैंने ध्यान करने के लिए १४८ कर्मप्रकृतियों से विरहित १४८ सूत्र बनाये हैं। यथा-
‘‘मतिज्ञानावरणीयकर्मरहितोऽहं शुद्धचिन्मयचिन्तामणिस्वरूपोऽहम् ।।१।।
पूर्णता का अंतिम श्लोक-
ग्रन्थोऽयं बंधस्वामित्व-विचयो मंगलं क्रियात्।
श्री शांतिनाथतीर्थेश:, कुर्यात् सर्वत्र मंगलम् ।।८।।
इस प्रकार संक्षेप में इस तृतीय खण्ड का सार दिया है।
चतुर्थ-वेदना खण्ड
पुस्तक ९-
इस चतुर्थ और पंचम खण्ड में जो विषय विभाजित हैं, उनका विवरण इस प्रकार है-
अग्रायणीय पूर्व के अर्थाधिकार चौदह हैं-
| १. पूर्वांत | २. अपरान्त |
| ३. ध्रुव | ४. अधु्रव |
| ५. चयनलब्धि | ६. अध्रुवसंप्रणिधान |
| ७. कल्प | ८. अर्थ |
| ९. भौमावयाद्य, | १०. कल्पनिर्याण |
| ११. अतीतकाल | १२. अनागतकाल |
| १३. सिद्ध और | १४. बुद्ध१। |
यहाँ ‘चयनलब्धि’ नाम के पाँचवें अधिकार में ‘महाकर्म प्रकृतिप्राभृत’ संगृहीत है। उसमें ये चौबीस अनुयोगद्वार ज्ञातव्य हैं।
| १. कृति | २. वेदना |
| ३. स्पर्श | ४. कर्म |
| ५. प्रकृति | ६. बंधन |
| ७. निबंधन | ८. प्रक्रम |
| ९. उपक्रम | १०. उदय |
| ११. मोक्ष | १२. संक्रम |
| १३. लेश्या | १४. लेश्याकर्म |
| १५. लेश्या परिणाम | १६. सातासात |
| १७. दीर्घ-ह्रस्व | १८. भवधारणीय |
| १९. पुद्गलात्त | २०. निधत्तानिधत्त |
| २१. निकाचितानिकाचित | २२. कर्मस्थिति |
| २३. पश्चिमस्कंध और | २४. अल्पबहुत्व२। |
इन चौबीस अनुयोगद्वारों को षट्खण्डागम की मुद्रित नवमी पुस्तक से लेकर सोलहवीं तक में ‘वेदना’ और ‘वर्गणा’ नाम के दो खंडों में विभक्त किया है। वेदना खण्ड में ९, १०, ११ और १२ ऐसे चार ग्रंथ हैं।
इस नवमी पुस्तक में मात्र प्रथम ‘कृति’ अनुयोग द्वार ही वर्णित है। छियालिसवें सूत्र में कृति के सात भेद किये हैं-
१. नामकृति २. स्थापनाकृति ३. द्रव्यकृति ४. गणनकृति ५. ग्रन्थकृति ६. करणकृति और ७. भावकृति।
इन कृतियों का विस्तार से वर्णन करके अंत में कहा है कि-यहाँ ‘गणनकृति’ से प्रयोजन है१।
इस ग्रंथ में श्रीभूतबलि आचार्य ने ‘णमो जिणाणं’ आदि गणधरवलय मंत्र लिए हैं जो कि श्री गौतमस्वामी द्वारा रचित हैं। यहाँ ‘‘णमो जिणाणं’’ से लेकर ‘‘णमो वड्ढमाणबुद्धरिसिस्स’’ चवालीस मंत्र लिए हैं। अन्यत्र ‘पाक्षिक प्रतिक्रमण’ एवं ‘प्रतिक्रमणग्रन्थत्रयी’ टीका ग्रंथ तथा भक्तामर स्तोत्र ऋद्धिमंत्र आदि में अड़तालीस मंत्र लिये गये हैं।
इन ४८ मंत्रों को ‘श्रीगौतमस्वामी’ द्वारा रचित कृतियों में इसी ग्रंथ में दिया गया है।
इस नवमी पुस्तक में टीकाकार श्री वीरसेनाचार्य ने बहुत ही विस्तार से इन मंत्रों का अर्थ स्पष्ट किया है। अनंतर ‘सिद्धान्त ग्रंथों’ के स्वाध्याय के लिए द्रव्यशुद्धि, क्षेत्रशुद्धि, कालशुद्धि और भावशुद्धि का विवेचन विस्तार से किया है।
इस ग्रंथ की ‘सिद्धान्तचिन्तामणि’ टीका मैंने शरदपूर्णिमा वी.नि.सं. २५२५ को (२४-१०-९९ को) दिल्ली में राजा बाजार के दिगम्बर जैन मंदिर में प्रारंभ की थी।
श्री गौतमस्वामी के मुखकमल से विनिर्गत गणधरवलय मंत्रों की टीका लिखते समय मुझे एक अपूर्व ही आल्हाद प्राप्त हुआ है। इसकी पूर्णता मैंने आश्विन शु.१५-शरदपूर्णिमा वीर.नि.सं. २५२६ को (१३-१०-२००० को) दिल्ली में ही प्रीतविहार-श्रीऋषभदेव कमलमंदिर में की है। जिसका अंतिम श्लोक निम्नलिखित है-
अहिंसा परमो धर्मो, यावद् जगति वर्त्स्यते।
यावन्मेरुश्च टीकेयं, तावन्नंद्याच्च न: श्रियै।।९।।
इसमें ७६ सूत्र हैं एवं मेरे द्वारा लिखित पृ. १४० हैं।
इस प्रकार नवमी पुस्तक का किंचित् सार लिखा गया है।
पुस्तक १०-
इस ग्रंथ में ‘वेदना’ नाम का द्वितीय अनुयोगद्वार है। इस वेदनानुयोग द्वार के १६ भेद हैं-
| १. वेदनानिक्षेप | २. वेदनानयविभाषणता |
| ३. वेदनानामविधान | ४. वेदनाद्रव्यविधान |
| ५. वेदनाक्षेत्रविधान | ६. वेदनाकालविधान |
| ७. वेदनाभावविधान | ८. वेदनाप्रत्ययविधान |
| ९. वेदनास्वामित्वविधान | १०. वेदनावेदनाविधान |
| ११. वेदनागतिविधान | १२. वेदनाअनंतरविधान |
| १३. वेदनासन्निकर्षविधान | १४. वेदनापरिमाणविधान |
| १५. वेदनाभागाभागविधान और | १६. वेदनाअल्पबहुत्वविधान२। |
इस दशवीं पुस्तक में प्रारंभ के ५ अनुयोग द्वारों का वर्णन है। सूत्र संख्या ३२३ है। आगे ११वीं और १२वीं पुस्तक में सभी वेदनाओं का वर्णन होने से इस तृतीय खण्ड को वेदनाखण्ड कहा है।
यहाँ प्रथम ‘वेदना निक्षेप’ के भी नामवेदना, स्थापनावेदना, द्रव्यवेदना और भाववेदना ऐसे निक्षेप की अपेक्षा चार भेद हैं।
दूसरे ‘वेदनानयविभाषणता’ में नयों की अपेक्षा वेदना को घटित किया है। तीसरे ‘वेदनानामविधान’ के ज्ञानावरण आदि आठ कर्मों की अपेक्षा आठ भेद कर दिये हैं१।
वेदना द्रव्यविधान के तीन अधिकार किये हैं-पदमीमांसा, स्वामित्व और अल्पबहुत्व। इस ग्रंथ में इनका विस्तार से वर्णन है।
इस ग्रंथ में वेदनाक्षेत्रविधान के भी पदमीमांसा, स्वामित्व और अल्पबहुत्व ऐसे तीन भेद किये हैं।
आश्विन शु. १५-शरदपूर्णिमा (१३-१०-२०००) को दिल्ली में मैंने टीका लिखना प्रारंभ किया था पुन: इस ग्रंथ की टीका का समापन शौरीपुर भगवान नेमिनाथ की जन्मभूमि में वैशाख कृ. ७, वी.सं. २५२८, दिनाँक ३-५-२००२ को किया है। मेरे द्वारा लिखित पृ. संख्या ११८ हैं।
इस प्रकार संक्षिप्त सार दिया गया है।
पुस्तक नं. ११-
इस पुस्तक की टीका का प्रारंभ शौरीपुर में किया है। इस ११वें ग्रंथ में वेदनाकाल विधान और वेदनाभाव विधान का वर्णन है। सूत्र इसमें ५९३ हैं और पृ. संख्या २१२ है। इसके पूर्वार्द्ध की पूर्णता ‘‘तीर्थंकर ऋषभदेव तपस्थली प्रयाग’’ श्री ऋषभदेव दीक्षा तीर्थ पर की है एवं उत्तरार्ध को अर्थात् पूरे ग्रंथ का समापन पावापुरी-भगवान महावीर की निर्वाणभूमि पर श्रावण शु. ७, वी.सं. २५२९, दिनाँक ४-८-२००३ को किया है।
पुस्तक १२-
इस १२वीं पुस्तक की टीका लेखन का प्रारंभ मैंने श्रावण कृ. १०, वीर निर्वाण संवत् २५२९ (दिनाँक-२४-७-२००३) को कुण्डलपुर में प्रारंभ की।
इस ग्रन्थ में वेदनाअनुयोगद्वार के १६ भेदों में से ८वें से लेकर १६वें तक भेद वर्णित हैं-
| ८. वेदनाप्रत्ययविधान | ९. वेदनास्वामित्वविधान |
| १०. वेदनावेदनाविधान | ११. वेदनागतिविधान |
| १२. वेदना-अनंतरविधान | १३. वेदना-सन्निकर्षविधान |
| १४. वेदनापरिमाणविधान | १५. वेदनाभागाभागविधान और |
| १६. वेदनाअल्पबहुत्वविधान। |
इन नव वेदना अनुयोग द्वारों का इस ग्रन्थमें विस्तार से वर्णन है। इसमें सूत्र संख्या ५३३ है।
‘वेदनाप्रत्ययविधान’ में जीवहिंसा, असत्य आदि प्रत्यय-निमित्त से ज्ञानावरण आदि कर्मों की वेदना होती है। जैसे कि-
मुसावादपच्चए।।३।।
मिथ्यात्व, असंयम, कषाय और प्रमाद से उत्पन्न वचनसमूह असत् वचन है इत्यादि।
ऐसे संपूर्ण वेदनाओं का वर्णन किया गया है।
इसमें सूत्र ५३३ हैं, पृ. १७५ हैं।
इस ग्रंथ की टीका राजगृही में मार्गशीर्ष शु. १३, वीर निर्वाण संवत् २५३० में पूर्ण की। मैंने राजगृही सिद्धक्षेत्र पर ‘‘भगवान पार्श्वनाथ तृतीय सहस्राब्दि महोत्सव’’ मनाने के लिए प्रेरणा दी। इस संदर्भ में मैंने लिखा है-
पौषकृष्णैकादश्यां तिथौ काशीदेशे वाराणस्यां नगर्यां महानृपते: अश्वसेनस्य महाराज्ञ्य: वामादेव्यो गर्भात् भगवान् पार्श्वनाथो जज्ञे। उग्रवंशशिरोमणि: मरकतमणिसन्निभ: त्रयस्त्रिंशत्तमस्तीर्थंकरोऽयं अस्मात् वीरनिर्वाणसंवत्सरात् द्विसहस्र-अष्टशताशीतिवर्षपूर्वं अवततार।
उक्तं च तिलोयपण्णत्तिग्रंथे-अट्ठत्तरिअधियाए वेसदपरिमाणवासअदिरित्ते।
पासजिणुप्पत्तीदो उप्पत्तीवड्ढमाणस्स ।।५७७।।
भगवान पार्श्वनाथ की उत्पत्ति के २७८ वर्ष बाद वर्धमान भगवान की उत्पत्ति हुई है तथा भगवान महावीर को जन्म लिये २६०२ वर्ष हुए अत: २७८ में वह संख्या जोड़ देने से २७८ + २६०२ = २८८० वर्ष हो गये अत: मैंने यह घोषणा की थी कि आगे आने वाले पौष कृ. ११ (६-१-२००५) को भगवान पार्श्वनाथ का ‘तृतीय सहस्राब्दि महोत्सव’ प्रारंभ करें पुन: एक वर्ष तक सारे भारत में भगवान पार्श्वनाथ का गुणगान करें।
इस प्रकार इस बारहवीं पुस्तक का विषय संक्षेप में लिखा है।
पंचम खण्ड-वर्गणाखण्ड
पुस्तक १३-
नवमीं पुस्तक में चयनलब्धि के ‘महाकर्मप्रकृतिप्राभृत’ के ‘कृति, वेदना, स्पर्श, कर्म, प्रकृति आदि चौबीस अनुयोगद्वार कहे गये हैं। वेदना खण्ड में मात्र ‘कृति और वेदना’ ये दो अनुयोगद्वार आये हैं। शेष २२ अनुयोगद्वार इस ‘वर्गणाखण्ड’ नाम के पांचवें खण्ड में वर्णित हैं। इस खण्ड में भी १३वीं, १४वीं, १५वीं एवं १६वीं ऐसी चार पुस्तकें हैं। इस खण्ड में ‘बंधनीय’ का आलंबन लेकर वर्गणाओं का सविस्तार वर्णन किया गया है अत: इसे ‘वर्गणाखण्ड’ नाम दिया है।
इस ग्रंथ की टीका मैंने वीर निर्वाण संवत् २५३०, पौष कृ. ११ (दिनाँक-१९-१२-२००३) को भगवान महावीर की जन्मभूमि कुण्डलपुर में प्रारंभ की।
इस तेरहवीं पुस्तक में ‘स्पर्श, कर्म और प्रकृति’ इन तीन अनुयोगद्वारों का वर्णन है। सूत्र संख्या २०६ है।
इसमें ‘स्पर्श अनुयोगद्वार’ के सोलह अनुयोगद्वार ज्ञातव्य हैं-स्पर्शनिक्षेप, स्पर्शनयविभाषणता, स्पर्शनामविधान, स्पर्शद्रव्यविधान, स्पर्शक्षेत्रविधान, स्पर्शकालविधान, स्पर्शभावविधान, स्पर्शप्रत्ययविधान, स्पर्शस्वामित्वविधान, स्पर्शस्पर्शविधान, स्पर्शगतिविधान, स्पर्शअनंतरविधान, स्पर्शसन्निकर्षविधान, स्पर्शपरिमाणविधान, स्पर्शभागाभागविधान और स्पर्शअल्पबहुत्व।२
पुनश्च प्रथम भेद ‘स्पर्शनिक्षेप’ के १३ भेद किये हैं-नामस्पर्श, स्थापनास्पर्श, द्रव्यस्पर्श, एकक्षेत्रस्पर्श, अनंतरक्षेत्रस्पर्श, देशस्पर्श, त्वक्स्पर्श, सर्वस्पर्श, स्पर्शस्पर्श, कर्मस्पर्श, बंधस्पर्श, भव्यस्पर्श और भावस्पर्श३।
इस तेरहवें ग्रन्थ में सूत्र की टीका के अनंतर मैंने प्राय: ‘तात्पर्यार्थ’ दिया है। जैसे कि-स्पर्श अनुयोगद्वार में सूत्र २६ में टीका के अनंतर लिखा है।
‘‘अत्र तात्पर्यमेतत्-अष्टसु कर्मसु मोहनीयकर्म एव संसारस्य मूलकारणमस्ति। दर्शनमोहनीय-निमित्तेन जीवा मिथ्यात्वस्य वशंगता: सन्त: अनादिसंसारे परिभ्रमन्ति। चारित्रमोहनीयबलेन तु असंयता: सन्त: कर्माणि बध्नन्ति।
उक्तं च श्री पूज्यपादस्वामिना-
बध्यते मुच्यते जीव: समम: निर्मम: क्रमात्।
तस्मात् सर्वप्रयत्नेन निर्ममत्वं विचिन्तयेत्।।
एतज्ज्ञात्वा कर्मस्पर्शकारणभूतमोहरागद्वेषादिविभावभावान् व्यक्त्वा स्वस्मिन् स्वभावे स्थिरीभूय स्वस्थो भवन् स्वात्मोत्थपरमानंदामृतं सुखमनुभवनीयमिति।’’
कर्म अनुयोगद्वार में भी प्रथम ही १६ अनुयोगद्वार रूप भेद कहे हैं-कर्मनिक्षेप, कर्मनयविभाषणता, कर्मनाम विधान आदि। पुनश्च कर्मनिक्षेप के दश भेद किये हैं-नामकर्म, स्थापनाकर्म, द्रव्यकर्म, प्रयोगकर्म, समवदानकर्म, अध:कर्म, ईर्यापथकर्म, तप:कर्म, क्रियाकर्म और भावकर्म।
इसमें ‘तप:कर्म’ के बारह भेदों का विस्तार से वर्णन किया गया है। इसी प्रकार ‘क्रियाकर्म’ में-
‘‘तमादाहीणं पदाहीणं तिक्खुत्तं तियोणदं, चदुसिरं
बारसावत्तं तं सव्वं किरियाकम्मं णाम१।।२८।।’’
यह क्रियाकर्म विधिवत् सामायिक-देववंदना में घटित होता है। इसी सूत्र को उद्धृत करके अनगारधर्मामृत, चारित्रसार आदि ग्रंथों में साधुओं की सामायिक को ‘देववंदना’ रूप में सिद्ध किया है। इसका स्पष्टीकरण मूलाचार, आचारसार आदि ग्रंथों में भी है। ‘क्रियाकलाप’ जिसका संपादन पं. पन्नालाल सोनी ब्यावर वालों ने किया था उसमें तथा मेरे द्वारा संकलित (लिखित) ‘मुनिचर्या’ में भी यह विधि सविस्तार वर्णित है। इन प्रकरणों को लिखते हुए, पढ़ते हुए मुझे एक अद्भुत ही आनंद का अनुभव हुआ है।
तृतीय ‘प्रकृति’ अनुयोगद्वार में भी सोलह अधिकार कहे हैं-प्रकृतिनिक्षेप, प्रकृतिनयविभाषणता, प्रकृतिनामविधान, प्रकृतिद्रव्यविधान आदि।
इसमें प्रथम प्रकृतिनिक्षेप के चार भेद किये हैं-नामप्रकृति, स्थापनाप्रकृति, द्रव्यप्रकृति और भावप्रकृति।
इसमें द्रव्यप्रकृति के दो भेद हैं-आगमद्रव्यप्रकृति और नोआगमद्रव्यप्रकृति। नोआगमद्रव्यप्रकृति के भी दो भेद हैं-कर्मप्रकृति और नोकर्म प्रकृति।
कर्मप्रकृति के ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय कर्म प्रकृति।
इस तेरहवीं पुस्तक में प्रकृति अनुयोगद्वार में व्यंजनावग्रहावरणीय के ४ भेद किये हैं। धवला टीका में श्री वीरसेनस्वामी ने श्रोत्रेन्द्रिय के विषयभूत शब्दों के अनेक भेद करके कहा है-
‘‘सद्दपोग्गला सगुप्पत्तिपदेसादो उच्छलिय दसदिसासु
गच्छमाणा उक्कस्सेण जाव लोगंतं ताव गच्छंति।
कुदो एदं णव्वदे ?
सुत्ताविरुद्धाइरियवयणादो। ते किं सव्वे सद्दपोग्गला लोगंतं गच्छंति आहो ण सव्वे इति पुच्छिदे सव्वे ण गच्छंति, थोवा चेव गच्छंति।
जहण्णेण अंतोमुहुत्तकालेण लोगंतपत्ती होदि त्ति उवदेसादो२।’’
शब्द पुद्गल अपने उत्पत्ति प्रदेश से उछलकर दशों दिशाओं में जाते हुए उत्कृष्ट रूप से लोक के अंतभाग तक जाते हैं।
यह किस प्रमाण से जाना जाता है ?
यह सूत्र के अविरुद्ध व्याख्यान करने वाले आचार्यों के वचन से जाना जाता है।
क्या वे सब शब्दपुद्गल लोक के अंत तक जाते हैं या सब नहीं जाते ?
सब नहीं जाते हैं, थोड़े ही जाते हैं। यथा-शब्द पर्याय से परिणत हुए प्रदेश में अनंत पुद्गल अवस्थित रहते हैं। दूसरे आकाश प्रदेश में उनसे अनंतगुणे हीन पुद्गल अवस्थित रहते हैं।
इस तरह वे अनंतरोपनिधा की अपेक्षा वातवलय पर्यंत सब दिशाओं में उत्तरोत्तर एक-एक प्रदेश के प्रति अनंतगुणे हीन होते हुए जाते हैं।
आगे क्यों नहीं जाते ?
धर्मास्तिकाय का अभाव होने से वे वातवलय के आगे नहीं जाते हैं। ये सब शब्दपुद्गल एक समय में ही लोक के अंत तक जाते हैं, ऐसा कोई नियम नहीं है किन्तु ऐसा उपदेश है कि कितने ही शब्द पुद्गल कम से कम दो समय से लेकर अंतर्मुहूर्त काल के द्वारा लोक के अंत को प्राप्त होते हैं।
अष्टसहस्री ग्रंथ में भी शब्द पुद्गलों का आना, पकड़ना, टकराना आदि सिद्ध किया है क्योंकि ये पौद्गलिक हैं-पुद्गल की पर्याय हैं।
इन सभी प्रकरणों के अध्ययन से यह स्पष्ट है कि-
आज जो शब्द टेलीविजन-दूरदर्शन, रेडियो-आकाशवाणी, टेलीफोन-दूरभाष आदि के द्वारा हजारों किमी. दूर से सुने जाते हैं, टेलीफोन से कई हजार किमी. दूर से वार्तालाप किया जाता है, टेपरिकार्ड, वी.डी.ओ. आदि में भरे जाते हैं, महीनों, वर्षों तक ज्यों की त्यों सुने जाते हैं, यह सब पौद्गलिक चमत्कार है।
वास्तव में ये शब्द मुख से निकलने के बाद लोक के अंत तक पैâल जाते हैं इसीलिए इनका पकड़ना, दूर तक पहुँचाना, भेजना, यंत्रों में भर लेना आदि संभव है।
इन्हीं भावनाओं के अनुसार मैंने ३० वर्ष पूर्व भगवान ‘शांतिनाथ स्तुति’ में यह उद्गार लिखे थे। यथा-
सुभक्तिवरयंत्रत: स्फुटरवा ध्वनिक्षेपकात्।
सुदूरजिनपार्श्वगा भगवत:स्पृशन्ति क्षणात्।
पुन: पतनशीलतोऽवपतिता नु ते स्पर्शनात्।
भवन्त्यभिमतार्थदा: स्तुतिफलं ततश्चाप्यते१।।२०।।
हे भगवन्! आपकी श्रेष्ठ भक्ति वो ही हुआ ध्वनिविक्षेपण यंत्र, (रेडियो आदि) उससे स्फुट-प्रगट हुईं शब्द वर्गणाएं बहुत ही दूर सिद्धालय में-लोक के अग्रभाग में विराजमान आपके पास जाती हैं और वहाँ आपका स्पर्श करती हैं। पुन: पुद्गलमयी शब्दवर्गणायें पतनशील होने से यहाँ आकर-भक्त के पास आकर आपसे स्पर्शित होने से ही भव्य जीवों के मनोरथ को सफल कर देती हैं, यही कारण है कि इस लोक में स्तुति का फल पाया जाता है अन्यथा नहीं पाया जा सकता था।
इसमें ज्ञानावरण के अंतर्गत श्रुतज्ञानावरण के विषय में कहते हुए ‘श्रुतज्ञान’ के विषय में बहुत ही विस्तृत वर्णन किया है।
प्रश्न हुआ है-‘‘श्रुतज्ञानावरणीय कर्म की कितनी प्रकृतियाँ हैं ?
उत्तर दिया है-श्रुतज्ञानावरणीय कर्म की संख्यात प्रकृतियाँ हैं।
जितने अक्षर हैं और जितने अक्षर संयोग हैं उतनी प्रकृतियां हैं।२’’
पुनश्च-श्रुतज्ञानावरणीय कर्म के बीस भेद किये हैं-पर्यायावरणीय, पर्यायसमासावरणीय, अक्षरावरणीय, अक्षरसमासावरणीय, पदावरणीय, पदसमासावरणीय आदि से पूर्वसमासावरणीय पर्यंत ये बीस भेद हैं।१ इनसे पहले श्रुतज्ञान के बीस भेद हैं, जिनके ये आवरण हैं।
उन श्रुतज्ञान के नाम-
| पर्याय, | पर्यायसमास, |
| अक्षर, | अक्षरसमास, |
| पद, | पदसमास, |
| संघात, | संघातसमास, |
| प्रतिपत्ति, | प्रतिपत्तिसमास, |
| अनुयोगद्वार, | अनुयोगद्वारसमास, |
| प्राभृतप्राभृत, | प्राभृतप्राभृतसमास, |
| प्राभृत, | प्राभृतसमास, |
| वस्तु, | वस्तुसमास, |
| पूर्व और | पूर्वसमास, |
ये श्रुतज्ञान के बीस भेद हैं।
इस ग्रंथ की टीका के लेखन में मैंने जो परम आल्हाद प्राप्त किया है, वह मेरे जीवन में आfचन्त्य ही रहा है।
एक तो षट्खण्डागम रूपी परम ग्रंथराज, दूसरे श्रीभूतबलि महान आचार्य के सूत्र, तीसरे श्रीवीरसेनाचार्य की धवला टीका और चौथा भगवान महावीर तीर्थ त्रिवेणी का संगम। यही कारण है कि यह ग्रंथ मेरा यहाँ भगवान महावीर जन्मभूमि कुण्डलपुर, देशनाभूमि राजगृही एवं निर्वाणभूमि पावापुरी ऐसे-‘तीर्थ त्रिवेणी संगम’ में अतिशीघ्र मात्र नव माह में पूर्ण हुआ है।
इस ग्रंथ में श्री वीरसेनाचार्य ने अगणित रत्न भर दिये हैं।
यथा-‘श्रुतज्ञानमन्तरेण चारित्रानुत्पत्ते:।’’
‘‘द्वादशांगस्य सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राविनाभाविनो
मोक्षमार्गत्वेनाभ्युपगमात्।
श्रुतज्ञान के बिना चारित्र की उत्पत्ति नहीं होती है इसलिए चारित्र की अपेक्षा श्रुत की प्रधानता है।
सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र के अविनाभावी द्वादशांग को मोक्षमार्ग रूप से स्वीकार किया गया है।
यहाँ पर ५०वें सूत्र में श्रुतज्ञान के इकतालीस (४१) पर्याय शब्द बताये हैं। जैसे-प्रावचन, प्रवचनीय आदि।
इस ग्रंथ में श्रुतज्ञान के पर्याय, पर्यायसमास आदि बीस भेद किये हैं और उन्हीं का विस्तार किया है।
तब प्रश्न यह हुआ है कि-उन्नीसवां ‘पूर्व’ और बीसवां ‘पूर्वसमास’ भेद तो इन बीस भेदों में आ गया है पुन:-
अंगबाह्य चौदह प्रकीर्णकाध्याय, आचारांग आदि ग्यारह अंग, परिकर्म, सूत्र, प्रथमानुयोग और चूलिका, इनका किस श्रुतज्ञान में अन्तर्भाव होगा ?
तब श्रीवीरसेनस्वामी ने समाधान दिया है कि-
इनका अनुयोगद्वार और अनुयोगद्वारसमास में अंतर्भाव होता है अथवा प्रतिपत्तिसमास श्रुतज्ञान में इनका अंतर्भाव कहना चाहिए परंतु पश्चादानुपूर्वी की विवक्षा करने पर इनका ‘पूर्वसमास’ श्रुतज्ञान में अंतर्भाव होता है, ऐसा कहना चाहिए२।
इस प्रकार इस ग्रंथ में मति, श्रुत, अवधि, मन:पर्यय और केवलज्ञान का बहुत ही सुन्दर विवेचन है।
अनंतर सर्व कर्मों का वर्णन करके अंत में कहा है कि यहाँ ‘कर्म प्रकृति’ से ही प्रयोजन है।
यहाँ तक इन १३ ग्रंथों में ५६३० सूत्रों की मेरे द्वारा लिखित संस्कृत टीका के पृष्ठों की
संख्या-२८१+१९१+१४०+८३+१२४+२८७+२५७=१३५६+९४८=२३०४ है।
इस ग्रंथ की टीका मैंने द्वि. श्रावण शु. ७, वीर निर्वाण संवत् २५३०(दिनाँक २२-८-२००४) रविवार को कुण्डलपुर में की है।
इस प्रकार संक्षेप में इस ग्रंथ का सार दिया है।
पुस्तक १४-
इस ग्रंथ की टीका मैंने आश्विन शु. १५, वीर निर्वाण संवत् २५३० (दिनाँक २८-१०-२००४) को कुण्डलपुर में की है।
इस ग्रंथ में ‘कृति, वेदना’ आदि २४ अनुयोगद्वारों में से छठे बंधन अनुयोगद्वार का निरूपण है। सूत्र संख्या ७९७ है। इसमें बंध, बंधक, बंधनीय और बंधविधान ये भेद किये हैं। पुनश्च बंध के नामबंध, स्थापनाबंध, द्रव्यबंध और भावबंध ये चार भेद कहे हैं।
भावबंध के आगमभावबंध और नोआगमभावबंध दो भेद हैं।
आगम भावबंध के स्थित, जित, परिजित, वाचनोपगत, सूत्रसम, अर्थसम, ग्रंथसम, नामसम और घोषसम ये नव भेद हैं। इनके विषय में वाचना, पृच्छना, प्रतीच्छना, परिवर्तना, अनुपे्रक्षणा, स्तव, स्तुति, धर्मकथा तथा इनसे लेकर जो अन्य उपयोग हैं उनमें भाव रूप से जितने उपयुक्त भाव हैं, वे सब आगमभावबंध हैं।१
नोआगमभावबंध के भी दो भेद हैं-जीव भावबंध और अजीव भावबंध।
इनमें से जीवभावबंध के ३ भेद हैं-विपाकप्रत्ययिक जीवभावबंध, अविपाकप्रत्ययिक जीवभावबंध और तदुभयप्रत्ययिक जीवभावबंध।
इनमें देवभाव, मनुष्यभाव आदि विपाकप्रत्ययिक जीव भावबंध हैं।
अविपाकप्रत्ययिक जीवभावबंध के औपशमिक अविपाकप्रत्ययिक जीवभावबंध और क्षायिकअविपाक-प्रत्ययिक जीवभावबंध, ऐसे दो भेद हैं।
औपशमिक के उपशांत क्रोध, उपशांत मान आदि भेद हैं।
क्षायिक के क्षीणक्रोध, क्षीणमान आदि भेद हैं।
तदुभयप्रत्ययिक जीवभावबंध के क्षायोपशमिक एकेन्द्रियलब्धि, क्षायोपशमिक द्वीन्द्रियलब्धि आदि बहुत भेद हैं।
इस प्रकार सूत्र १३ से १९ तक इन सबका विस्तार है।
ऐसे ही अजीव भावबंध के भी तीन भेद हैं-विपाकप्रत्ययिक, अविपाकप्रत्ययिक और तदुभयप्रत्ययिक अजीवभावबंध। विपाकप्रत्ययिक अजीव भावबंध के प्रयोगपरिणतवर्ण, प्रयोगपरिणतशब्द आदि भेद हैं।
अविपाकप्रत्ययिक अजीव भावबंध के विस्रसापरिणतवर्ण आदि भेद हैं।
तथा तदुभयप्रत्ययिक अजीव भावबंध के प्रयोग परिणत वर्ण और विस्रसापरिणतवर्ण आदि भेद हैं।
इसके अनंतर द्रव्यबंध के आगम, नोआगम आदि भेद-प्रभेद किये हैं।
इस प्रकार ‘बंध’ भेद का प्ररूपण किया गया है।
अनंतर ‘बंधक’ अधिकार में मार्गणाओं में बंधक-अबंधक को विचार करने का कथन है।
अनंतर-
बंधनीय के प्रकरण में-वेदनस्वरूप पुद्गल है, पुद्गल स्कंधस्वरूप हैं और स्कंध वर्गणास्वरूप हैं२, ऐसा कहा है।
वर्गणाओं का अनुगमन करते हुए आठ अनुयोगद्वार ज्ञातव्य हैं-
वर्गणा, वर्गणाद्रव्य समुदाहार, अनंतरोपनिधा, परंपरोपनिधा, अवहार, यवमध्य, पदमीमांसा और अल्पबहुत्व।
वर्गणा के प्रकरण होने से यहां वर्गणा के १६ अनुयोगद्वार बताये हैं-
| १. वर्गणा निक्षेप | २. वर्गणानय-विभाषणता |
| ३. वर्गणाप्ररूपणा | ४. वर्गणानिरूपणा |
| ५. वर्गणाधु्रवाधु्रवानुगम | ६. वर्गणासांतरनिरंतरानुगम |
| ७. वर्गणाओजयुग्मानुगम | ८. वर्गणाक्षेत्रानुगम |
| ९. वर्गणास्पर्शनानुगम | १०. वर्गणाकालानुगम |
| ११. वर्गणाअनंतरानुगम | १२. वर्गणाभावानुगम |
| १३. वर्गणाउपनयनानुगम | १४. वर्गणापरिमाणानुगम |
| १५. वर्गणाभागाभागानुगम और | १६. वर्गणा अल्पबहुत्वानुगम। |
आगे इस ग्रंथ में ‘बंधनअनुयोगद्वार’ सूत्र ५८० हैं एवं इसकी चूलिका है जिसमें सूत्र २१७ हैं। कुल सूत्र ७९७ हैं।
बंधन अनुयोगद्वार की चूलिका के अंत में ७९७वें सूत्र में ‘बंध विधान’ के चार भेद किये हैं-प्रकृतिबंध, स्थितिबंध, अनुभागबंध और प्रदेशबंध।।७९७।।
इस सूत्र की टीका में श्री वीरसेनाचार्य ने कह दिया है कि-‘श्री भूतबलिभट्टारक’ ने ‘महाबंध’ खण्ड में इन चारों भेदों को विस्तार से लिखा है अत: मैंने यहाँ नहीं लिखा है। यथा-
यहाँ ‘भट्टारक’ पद से महान पूज्य अर्थ विवक्षित है। ये भूतबलि आचार्य महान दिगम्बर आचार्य थे, ऐसा समझना।
‘‘एदेसिं चदुण्णं बंधाणं विहाणं भूदबलिभडारएण महाबंधे सप्पवंचेण लिहिदं त्ति अम्मेहिं एत्थ ण लिहिदं। तदो सयले महाबंधे एत्थ परूविदे बंधविहाणं समप्पदि१।’’
इस ग्रंथ की टीका की पूर्णता मैंने फाल्गुन कृष्णा ११, वीर निर्वाण संवत् २५३२, भगवान ऋषभदेव के देशनादिवस (दिनाँक २४-२-२००६) को हस्तिनापुर में की है।
पुस्तक १५-
इस ग्रंथ की टीका मैंने हस्तिनापुर में फाल्गुन कृ. ११, वीर निर्वाण संवत् २५३२ (दिनाँक २४-२-२००६) के दिन प्रारंभ की है। इस ग्रंथ में चौबीस अनुयोगद्वारों में से ७वाँ निबंधन, ८वाँ प्रक्रम, ९वाँ उपक्रम, १०वाँ उदय और १२वाँ मोक्ष इन ५ अनुयोगद्वारों का कथन है। सूत्र संख्या ‘निबंधन’ अनुयोगद्वार तक है। कुल सूत्र २० हैं।
आगे प्रक्रम, उपक्रम, उदय और मोक्ष अनुयोगद्वारों में सूत्रसंख्या नहीं है।
इसमें मंगलाचरण में श्रीवीरसेनाचार्य ने प्रथम निबंधन अनुयोगद्वार में ‘श्री अरिष्टनेमि’ भगवान को नमस्कार किया है।
द्वितीय ‘प्रक्रम’ अनुयोगद्वार में श्री शांतिनाथ भगवान को, तृतीय ‘उपक्रम’ अनुयोगद्वार में श्री अभिनंदन भगवान को एवं चौथे ‘उदय’ अनुयोगद्वार में पुनरपि श्रीशांतिनाथ भगवान को नमस्कार किया है।
निबंधन-‘निबध्यते तदस्मिन्निति निबंधनम्’ इस निरुक्ति के अनुसार जो द्रव्य जिसमें संबद्ध है, उसे ‘निबंधन’ कहा जाता है। उसके नाम निबंधन, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावनिबंधन ऐसे छह भेद हैंं।
इनमें से नाम, स्थापना को छोड़कर शेष सब निबंधन प्रकृत हैं। यह निबंधन अनुयोगद्वार यद्यपि छहों द्रव्यों के निबंधन की प्ररूपणा करता है तो भी यहाँ उसे छोड़कर कर्मनिबंधन को ही ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि यहाँ अध्यात्म विद्या का अधिकार१ है।
प्रश्न-निबंधनानुयोगद्वार किसलिए आया है ?
उत्तर-द्रव्य, क्षेत्र, काल और योगरूप प्रत्ययों की भी प्ररूपणा की जा चुकी है, उनके मिथ्यात्व, असंयम, कषाय और योगरूप प्रत्ययों की भी प्ररूपणा की जा चुकी है तथा उन कर्मों के योग्य पुद्गलों की भी प्ररूपणा की जा चुकी है। आत्मलाभ को प्राप्त हुए उन कर्मों के व्यापार का कथन करने के लिए निबंधनानुयोग द्वार आया है२।
उनमें मूलकर्म आठ हैं, उनके निबंधन का उदाहरण देखिये-‘‘उनमें ज्ञानावरण कर्म सब द्रव्यों में निबद्ध है और नो कर्म सर्वपर्यायों में अर्थात् असर्वपर्यायों में-कुछ पर्यायों में वह निबद्ध है३।।१।।’’
यहाँ ‘सब द्रव्यों में निबद्ध है’ यह केवल ज्ञानावरण का आश्रय करके कहा गया है क्योंकि वह तीनों कालों को विषय करने वाली अनंत पर्यायों से परिपूर्ण ऐसे छह द्रव्यों को विषय करने वाले केवलज्ञान का विरोध करने वाली प्रकृति है। ‘असर्व-कुछ पर्यायों में निबद्ध है’ यह कथन शेष चार ज्ञानावरणीय प्रकृतियों की अपेक्षा कहा गया है।
इत्यादि विषयों का इस अनुयोग में विस्तार है।
२. प्रक्रम अनुयोगद्वार के भी नाम, स्थापना आदि की अपेक्षा छह भेद हैं। द्रव्य प्रक्रम के प्रभेदों में कर्म- प्रक्रम आठ प्रकार का है। नोकर्म प्रक्रम सचित्त, अचित्त और मिश्र के भेद से तीन प्रकार का है।
क्षेत्रप्रक्रम ऊर्ध्वलोक, अधोलोक और तिर्यग्लोकप्रक्रम के भेद से तीन प्रकार का है। इत्यादि विस्तार को धवला टीका से समझना चाहिए।
३. उपक्रम अनुयोगद्वार में भी पहले नाम, स्थापना आदि से छह भेद किये हैं पुन: द्रव्य उपक्रम के भेद में कर्मोपक्रम के आठ भेद, नो कर्मोपक्रम के सचित्त, अचित्त और मिश्र की अपेक्षा तीन भेद हैं पुन: क्षेत्रोपक्रम-जैसे ऊर्ध्वलोक उपक्रांत हुआ, ग्राम उपक्रांत हुआ व नगर उपक्रांत हुआ आदि।
काल उपक्रम में-बसंत उपक्रांत हुआ, हेमंत उपक्रांत हुआ आदि। यहाँ ग्रंथ में कर्मोपक्रम प्रकृत होने से उसके चार भेद हैं-बंधन उपक्रम, उदीरणा उपक्रम, उपशामना उपक्रम और विपरिणाम उपक्रम।
इसी प्रकार इन सबका इस अनुयोगद्वार में विस्तार है।
४. उदय अनुयोगद्वार में नामादि छह निक्षेप घटित करके ‘नोआगमकर्मद्रव्य उदय’ प्रकृत है, ऐसा समझना चाहिए।
वह कर्मद्रव्य उदय चार प्रकार का है-प्रकृति उदय, स्थिति उदय, अनुभाग उदय और प्रदेश उदय।
इन सभी में स्वामित्व की प्ररूपणा करते हुए कहते हैं। जैसे-
प्रश्न-पांच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण और पाँच अंतराय इनके वेदक कौन हैं ?
उत्तर-इनके वेदक सभी छद्मस्थ जीव होते हैं,४ इत्यादि। इस प्रकार से यहाँ संक्षेप में इन अनुयोगद्वारों के नमूने प्रस्तुत किये हैं।
५. मोक्ष-इसमें श्री मल्लिनाथ भगवान को नमस्कार करके टीकाकार ने मोक्ष के चार निक्षेप कहकर नोआगम द्रव्यमोक्ष के तीन भेद किये हैं-मोक्ष, मोक्षकारण और मुक्त।
जीव और कर्मों का पृथक् होना मोक्ष है। ज्ञान, दर्शन और चारित्र ये मोक्ष के कारण हैं। समस्त कर्मों से रहित अनंत दर्शन, ज्ञान आदि गुणों से परिपूर्ण, कृतकृत्य जीव को मुक्त कहा गया है।१
इस १५वें ग्रंथ की टीका को मैंने आश्विन शु. १५, वी.सं. २५३२ (दिनाँक ६-१०-२००६) को हस्तिनापुर में पूर्ण किया है।
पुस्तक १६-
इस ग्रंथ की टीका मैंने हस्तिनापुर में कार्तिक शु. १, नव संवत्सर के प्रथम दिवस वीर निर्वाण संवत् २५३३ (दिनाँक २३-१०-२००६) को प्रारंभ की है।
| १.‘कृति, | २.वेदना, |
| ३.स्पर्श, | ४.कर्म, |
| ५.प्रकृति, | ६.बंधन, |
| ७.निबंधन, | ८.प्रक्रम, |
| ९.उपक्रम, | १०.उदय और |
| ११.मोक्ष |
ये ग्यारह अनुयोगद्वार नवमी पुस्तक से पंद्रहवीं पुस्तक तक आ चुके हैं।
अब आगे के-
| १२. संक्रम, | १३. लेश्या, |
| १४. लेश्या कर्म | १५. लेश्या परिणाम |
| १६. सातासात | १७. दीर्घ-ह्रस्व, |
| १८. भवधारणीय, | १९. पुद्गलात्त |
| २०. निधत्तानिधत्त | २१. निकाचितानिकाचित |
| २२. कर्मस्थिति | २३. पश्चिमस्कंध और |
| २४. अल्पबहुत्व |
१३ अनुयोगद्वार शेष हैं। इस सोलहवीं पुस्तक में इन सबका वर्णन है।
इस ग्रंथ में सूत्र नहीं हैं, मात्र धवला टीका में ही इन अनुयोगद्वारों का विस्तार है।
१. संक्रम-अनुयोग द्वार के भी छह भेद करके पुन: कर्मसंक्रम के प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश संक्रम भेद किये हैं।
विस्तृत वर्णन करते हुए कहा है कि-चार आयु कर्मों का संक्रम नहीं होता है, क्योंकि ऐसा स्वभाव है, आदि।
२. लेश्या-इसके भी नामलेश्या, स्थापनालेश्या, द्रव्यलेश्या और भावलेश्या भेद किये हैं।
कर्म पुद्गलों के ग्रहण में कारणभूत जो मिथ्यात्व, असंयम और कषाय से अनुरंजित योग प्रवृत्ति होती है उसे नो आगमभाव लेश्या कहते हैं।२
भावलेश्या के कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म, शुक्ल ये छह भेद हैं।
३. लेश्याकर्म-इसमें छहों लेश्याओं के लक्षण-‘चंडो ण मुवइ वेरं’ इत्यादि बताये गये हैं।
४. लेश्यापरिणाम-कौन लेश्याएं किस स्वरूप से और किस वृद्धि अथवा हानि के द्वारा परिणमन करती हैं, इस बात के ज्ञापनार्थ ‘लेश्या परिणाम’ अनुयोगद्वार प्राप्त हुआ है।
इसमें ‘षट्स्थान पतित’ का स्वरूप कहा गया है।
५. सातासात अनुयोगद्वार-इसके समुत्कीर्तना, अर्थपद, परमीमांसा, स्वामित्व और अल्पबहुत्व, ऐसे पांच अवान्तर अनुयोगद्वार हैं। समुत्कीर्तना में-एकांत सात, अनेकांत सात, एकांत असात और अनेकांत असात।
अर्थ पद में-सातास्वरूप से बांधा गया जो कर्म संक्षेप व प्रतिक्षेप से रहित होकर सातास्वरूप से वेदा जाता है वह एकांतसात है। इससे विपरीत अनेकांत सात है३ इत्यादि।
६. दीर्घ-ह्रस्व-इन अनुयोगद्वार के भी चार भेद हैं-प्रकृतिदीर्घ, स्थितिदीर्घ, अनुभागदीर्घ और प्रदेशदीर्घ।
आठ प्रकृतियों का बंध होने पर प्रकृति दीर्घ और उनसे कम का बंध होने पर नो प्रकृतिदीर्घ होता है१।
ऐसे ही ह्रस्व में प्रकृति ह्रस्व, स्थिति ह्रस्व आदि चार भेद हैं।
एक-एक प्रकृति को बांधने वाले के प्रकृति ह्रस्व है इत्यादि।
७. भवधारणीय-इस अनुयोगद्वार में भव के तीन भेद हैं-ओघभव, आदेशभव और भवग्रहण भव।
आठ कर्मजनित जीव के परिणाम का नाम ओघभव है। चार गति नाम कर्मों को या उनसे उत्पन्न जीव परिणामों को आदेश भव कहते हैं।
भुज्यमान आयु को निर्जीण करके जिससे अपूर्व आयु कर्म उदय को प्राप्त हुआ है, उसके प्रथम समय में उत्पन्न ‘व्यंजन’ संज्ञा वाले जीव परिणाम को अथवा पूर्व शरीर के परित्यागपूर्वक उत्तर शरीर के ग्रहण करने को ‘भवग्रहणभव’ कहा जाता है। उनमें यहाँ भवग्रहण भव प्रकरण प्राप्त है।२
८. पुद्गलात्त-इस अनुयोगद्वार में नामपुद्गल, स्थापनापुद्गल, द्रव्यपुद्गल और भावपुद्गल ऐसे चार भेद हैं।
यहाँ आत्त-शब्द का अर्थ गृहीत है अत: यहाँ ‘पुद्गलात्त’ पद से आत्मसात् किये गये पुद्गलों का ग्रहण है। वे पुद्गल छह प्रकार से ग्रहण किये जाते हैं-ग्रहण से, परिणाम से, उपभोग से, आहार से, ममत्व से और परिग्रह से, इत्यादि।
९. निधत्तानिधत्त-इस अनुयोगद्वार में भी प्रकृतिनिधत्त, स्थितिनिधत्त, अनुभागनिधत्त और प्रदेशनिधत्त ऐसे चार भेद हैं।
जो प्रदेशाग्र निधत्तीकृत हैं अर्थात् उदय में देने के लिए शक्य नहीं है, अन्य प्रकृति में संक्रमण करने के लिए शक्य नहीं है किन्तु अपकर्षण व उत्कर्षण करने के लिए शक्य हैं ऐसे प्रदेशाग्र की निधत्त संज्ञा है। अनिवृत्तिकरण गुणस्थान में प्रविष्ट मुनि के सब कर्म अनिधत्त हैं, इत्यादि।
१०. निकाचितानिकाचित-इस अनुयोगद्वार में प्रकृति निकाचित आदि चार भेद हैं। जो प्रदेशाग्र, अपकर्षण, उत्कर्षण, संक्रमण और उदय में देने के लिए भी शक्य नहीं हैं, वे निकाचित हैं। अनिवृत्तिकरणवर्ती मुनि के सर्वकर्म अनिकाचित हैं, इत्यादि।
११. कर्मस्थिति-इस अनुयोग में जघन्य और उत्कृष्ट स्थितियों के प्रमाण की प्ररूपणा कर्मस्थिति ‘प्ररूपणा है, ऐसा श्री ‘नागहस्तीश्रमण’ कहते हैं किन्तु आर्यमंक्षु क्षमाश्रमण का कहना है कि-‘कर्मस्थिति संचित सत्कर्म की प्ररूपणा का नाम ‘कर्मस्थिति’ प्ररूपणा है। यहाँ दोनों उपदेशों के द्वारा प्ररूपणा करना चाहिए, ऐसा श्री वीरसेनस्वामी ने कहा३ है।
१२. पश्चिमस्कंध-इस अनुयोगद्वार में ओघभव, आदेशभव और भवग्रहणभव ऐसे तीन भेद करके यहाँ भवग्रहण भव प्रकरण प्राप्त है। जो अंतिम भव है उसमें उस जीव के सब कर्मों की बंधमार्गणा, उदयमार्गणा, उदीरणामार्गणा, संक्रममार्गणा और सत्कर्ममार्गणा ये पाँच मार्गणाएं पश्चिम स्कंध अनुयोगद्वार में की जाती हैं।
प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेशाग्र का आश्रय करके इन पांच मार्गणाओं की प्ररूपणा कर चुकने पर तत्पश्चात् पश्चिम भव ग्रहण में सिद्धि को प्राप्त होने वाले जीव की यह अन्य प्ररूपणा करना चाहिए४ इत्यादि।
१३. अल्पबहुत्व-इस अनुयोगद्वार में ‘नागहस्तिमहामुनि’ सत्कर्म की मार्गणा करते हैं और यह उपदेश प्रवाह स्वरूप से आया हुआ परंपरागत है। सत्कर्म चार प्रकार का है-प्रकृतिसत्कर्म, स्थिति सत्कर्म, अनुभाग सत्कर्म अौर प्रदेश सत्कर्म। इनमें से प्रकृति सत्कर्म के मूल और उत्तर की अपेक्षा दो भेद करके मूल प्रकृतियों के स्वामी को लेकर कहते हैं-‘‘पाँच ज्ञानावरणीय, चार दर्शनावरणीय और पांच अंतराय प्रकृतियों के सत्कर्म का स्वामी कौन है ? इनके सत्कर्म के स्वामी सब छद्मस्थ जीव हैं, इत्यादि रूप से अल्पबहुत्व का विस्तार से कथन किया गया है।१
इस प्रकार यहाँ सोलहवें ग्रंथ में इन उपर्युक्त कथित शेष १३ अनुयोगद्वारों को पूर्ण किया है।
उपसंहार यह है कि-कृति, वेदना, स्पर्श आदि चौबीस अनुयोगद्वारों में से ‘कृति और वेदना’ नाम के मात्र दो अनुयोगद्वारों में ‘वेदनाखण्ड’ नाम से चौथा खण्ड विभक्त है। पुनश्च ‘स्पर्श’ आदि से लेकर अल्पबहुत्व तक २२ अनुयोगद्वारों में ‘वर्गणाखण्ड’ नाम से पांचवां खण्ड लिया गया है। यहाँ तक पाँच खंडों को सोलह पुस्तकों में विभक्त किया है। छठे महाबंध खण्ड में सात पुस्तकें विभक्त हैं जो कि हिन्दी अनुवाद होकर छप चुकी हैं।
पूर्वाचार्यों द्वारा रचित षट्खण्डागम की टीकायें
इस ‘षट्खण्डागम’ ग्रंथराज पर छह टीकायें लिखी गई हैं, ऐसा आगम में उल्लेख है। उनके नाम-
१. श्री कुन्दकुन्ददेव ने तीन खण्डों पर ‘परिकर्म’ नाम से टीका लिखी है जो कि १२ हजार श्लोक प्रमाण थी।
२. श्री शामकुंडाचार्य ने ‘पद्धति’ नाम से टीका लिखी है जो कि संस्कृत, प्राकृत और कन्नड़ मिश्र थी, ये पांच खण्डों पर थी और १२ हजार श्लोकप्रमाण थी।
३. श्री तुंबुलूर आचार्य ने ‘चूड़ामणि’ नाम से टीका लिखी। छठा खण्ड छोड़कर षट्खण्डागम और कषायप्राभृत दोनों सिद्धान्त ग्रंथों पर यह ८४ हजार श्लोकप्रमाण थी।
४. श्री समंतभद्रस्वामी ने संस्कृत में पांच खण्डों पर ४८ हजार श्लोकप्रमाण टीका लिखी।
५. श्री वप्पदेवसूरि ने ‘व्याख्याप्रज्ञप्ति’ नाम से टीका लिखी, यह पांच खण्डों पर और कषायप्राभृत पर थी एवं ६० हजार श्लोकप्रमाण प्राकृत भाषा में थी।
६. श्री वीरसेनाचार्य ने छहों खण्डों पर प्राकृत-संस्कृत मिश्र टीका लिखी, यह ‘धवला’ नाम से टीका है एवं ७२ हजार श्लोकप्रमाण है।
वर्तमान में ऊपर कही हुई पांच टीकाएं उपलब्ध नहीं हैं, मात्र श्री वीरसेनाचार्य कृत ‘धवला’ टीका ही उपलब्ध है जिसका हिंदी अनुवाद होकर छप चुका है। इस ग्रंथ को ताड़पत्र से लिखाकर और हिंदी अनुवाद कराकर छपवाने का श्रेय इस बीसवीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती श्री शांतिसागर जी महाराज को है। उनकी कृपाप्रसाद से हम सभी इन ग्रंथों के मर्म को समझने में सफल हुये हैं।
यह ‘षट्खण्डागम’ कितना प्रामाणिक है, देखिए श्रीवीरसेनस्वामी के शब्दों में-
लोहाइरिये सग्गलोगं गदे आयार-दिवायरो अत्थमिओ। एवं बारससु दिणयरेसु भरहखेत्तम्मि अत्थमिएसु सेसाइरिया सव्वेसिमंगपुव्वाणमेगदेसभूद-पेज्जदोस-महाकम्मपयडिपाहुडादीणं धारया जादा। एवं पमाणीभूदमहारिसिपणालेण आगंतूण महाकम्मपयडिपाहुडामियजलपवाहो धरसेणभडारयं संपत्तो। तेण वि गिरिणयरचंदगुहाए भूदबलि-पुप्फदंताणं महाकम्मपयडिपाहुडं सयलं समप्पिदं। तदो भूदबलिभडारएण सुदणईपवाहवोच्छेदभीएण भवियलोगाणुग्गहट्ठं महाकम्मपयडिपाहुड-मुवसंहरिऊण छखंडाणि कयाणि। तदो तिकालगोयरासेसपयत्थवि-सयपच्चक्खाणंतकेवलणाण-प्पभावादो पमाणीभूदआइरियपणालेणागदत्तादो दिट्ठिट्ठविरोहाभावादो पमाणमेसो गंथो। तम्हा मोक्खकंखिणा भवियलोएण अब्भसेयव्वो। ण एसो गंथो थोवो त्ति मोक्खकज्जजणणं पडि असमत्थो, अमियघडसयवाणफलस्स चुलुवामियवाणे वि उवलंभादो१।
लोहाचार्य के स्वर्गलोक को प्राप्त होने पर आचारांगरूपी सूर्य अस्त हो गया। इस प्रकार भरतक्षेत्र में बारह सूर्यों के अस्तमित हो जाने पर शेष आचार्य सब अंग-पूर्वों के एकदेशभूत ‘पेज्जदोस’ और ‘महाकम्मपयडिपाहुड’ आदिकों के धारक हुए। इस प्रकार प्रमाणीभूत, महर्षि रूप प्रणाली से आकर महाकम्मपयडिपाहुड रूप अमृत जल-प्रवाह धरसेन भट्टारक को प्राप्त हुआ। उन्होंने भी गिरिनगर की चन्द्र गुफा में सम्पूर्ण महाकम्मपयडिपाहुड भूतबलि और पुष्पदन्त को अर्पित किया। पश्चात् श्रुतरूपी नदी प्रवाह के व्युच्छेद से भयभीत हुए भूतबलि भट्टारक ने भव्यजनों के अनुग्रहार्थ महाकम्मपयडिपाहुड का उपसंहार कर छह खण्ड (षट्खण्डागम) किये अतएव त्रिकालविषयक समस्त पदार्थों को विषय करने वाले प्रत्यक्ष अनन्त केवलज्ञान के प्रभाव से प्रमाणीभूत आचार्य रूप प्रणाली से आने के कारण प्रत्यक्ष व अनुमान से चूँकि विरोध से रहित है अत: यह ग्रंथ प्रमाण है। इस कारण मोक्षाभिलाषी भव्य जीवों को इसका अभ्यास करना चाहिए। चूँकि यह ग्रंथ स्तोक है अत: वह मोक्षरूप कार्य को उत्पन्न करने के लिए असमर्थ है, ऐसा विचार नहीं करना चाहिए; क्योंकि अमृत के सौ घड़ों के पीने का फल चुल्लूप्रमाण अमृत के पीने में भी पाया जाता है।
अत: यह ग्रंथराज बहुत ही महान है, इसका सीधा संबंध भगवान महावीर स्वामी की वाणी से एवं श्री गौतम स्वामी के मुखकमल से निकले ‘गणधरवलय’ आदि मंत्रों से है। इस ग्रंथ में एक-एक सूत्र अनंत अर्थों को अपने में गर्भित किये हुए हैं अत: हम जैसे अल्पज्ञ इन सूत्रों के रहस्य को, मर्म को समझने में अक्षम ही हैं। फिर भी श्रीवीरसेनाचार्य ने ‘धवला’ टीका को लिखकर हम जैसे अल्पज्ञों पर महान उपकार किया है।
इस धवला टीका को आधार बनाकर मैंने टीका लिखी है। इसमें कहीं-कहीं धवला टीका की पंक्तियों को ज्यों का त्यों ले लिया है। कहीं पर उनकी संस्कृत (छाया) कर दी है। कहीं-कहीं उन प्रकरणों से संबंधित अन्य ग्रंथों के उद्धरण भी दिये हैं। श्रीवीरसेनाचार्य के द्वारा रचित टीका में जो अतीव गूढ़ एवं क्लिष्ट सैद्धांतिक विषय हैं अथवा जो गणित के विषय हैं उनको मैंने छोड़ दिया है एवं ‘धवला टीकायां दृष्टव्यं’ धवला टीका में देखना चाहिए, ऐसा लिख दिया है अर्थात् इस धवला टीका के सरल एवं सारभूत अंश को ही मैंने लिया है। चूँकि यह श्रुतज्ञान ही ‘केवलज्ञान’ की प्राप्ति के लिए ‘बीजभूत’ है।
जो टीकाएं उपलब्ध नहीं हैं उनके रचयिता सभी टीकाकारों को मेरा कोटि-कोटि नमन है कि जिनके प्रसाद से श्रीवीरसेनस्वामी ने ज्ञान प्राप्त किया होगा। पुनश्च-
श्री वीरसेनस्वामी के हम सभी पर आज अनंत उपकार हैं कि जिनकी इस धवल-शुभ्र-उज्ज्वल-धवलाटीका के किंचित् मात्र अंश को मैंने समझा है।
इसमें पूर्वजन्म के संस्कार, वर्तमान में सरस्वती की महती कृपा, प्रथम क्षुल्लिका दीक्षागुरु श्री आचार्य देशभूषण जी एवं आर्यिका दीक्षा के गुरु के गुरु इस बीसवीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्रचक्रवर्ती श्री शांतिसागराचार्य एवं उनके प्रथम शिष्य पट्टाचार्य श्री वीरसागर जी महाराज (आर्यिका दीक्षा के गुरु) का मंगल आशीर्वाद ही मेरे इस श्रुतज्ञान में निमित्त है, ऐसा मैं मानती हूँ।
इस ग्रंथ की टीका-सिद्धान्तचिंतामणि को मैंने वैशाख कृ. २, वी.नि.सं. २५३३, दिनाँक ४-४-२००७ को पूर्ण की है। इस षट्खण्डागम के प्रथम खण्ड में २३७५, द्वितीय खण्ड में १५९४, तृतीय खण्ड में ३२४, चतुर्थ खण्ड में १५२५ और पाँचवें खण्ड में १०२३ ऐसे १६ ग्रंथों में कुल ६८४१ सूत्र हैं और मेरे द्वारा लिखित सिद्धांतचिंतामणि टीका के पृष्ठ लगभग ३१२५ हैं। आज (वैशाख कृ. २ को) मैंने अपनी आर्यिका दीक्षा के ५१ वर्ष पूर्ण कर इस चिंतामणि टीका को पूर्ण करके अपने आध्यात्मिक जीवन पर कलशारोहण किया है। भगवान शांतिनाथ की कृपाप्रसाद से साढ़े ग्यारह वर्ष में इस टीका को पूर्णकर आनंद का अनुभव करते हुए भावश्रुत की प्राप्ति के लिए ‘महाग्रंथराज षट्खण्डागम’ को अनंत-अनंत बार नमस्कार करती हूँ।
शान्तिकुंथ्वरतीर्थेशां, हस्तिनागपुरीं स्तुम:।
गर्भजन्मतपोज्ञानै:, पूतां तांश्च विशुद्धये।।१।।
