प्ररूपणा एवं गुणस्थान
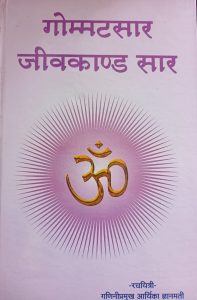
गुणस्थान
अथ श्रीनेमिचंद्र सैद्धान्तिक चक्रवर्ती गोम्मटसार ग्रंथ के लिखने के पूर्व निर्विघ्नसमाप्ति, नास्तिकतापरिहार, शिष्टाचार परिपालन और उपकारस्मरण इन चार प्रयोजनों से इष्टदेव को नमस्कार करते हुए इस ग्रंथ में जो कुछ वक्तव्य है उसके ‘सिद्ध’ इत्यादि गाथासूत्र द्वारा कथन करने की प्रतिज्ञा करते हैं-
।।मंगलाचरण।।
सिद्धं सुद्धं पणमिय, जिणिंदवरणेमिचंदमकलंकं।
गुणरयणभूसणुदयं, जीवस्स परूवणं वोच्छं।।१।।
सिद्धं शुद्धं प्रणम्य, जिनेन्द्रवरनेमिचंद्रमकलंकम्।
गुणरत्नभूषणोदयं, जीवस्य प्ररूपणं वक्ष्ये।।१।।
अर्थ—सिद्धावस्था या स्वात्मोपलब्धि को जो प्राप्त हो चुका है अथवा न्याय के प्रमाणों से जिसकी सत्ता सिद्ध है और जो घातिया द्रव्यकर्मों के अभाव से शुद्ध तथा मिथ्यात्वादि भावकर्मों के नाश से अकलंक हो चुका है एवं जिसके सदा ही सम्यक्त्वादि गुणरूपी रत्नों के भूषणों का उदय रहता है, इस प्रकार के श्री जिनेन्द्रवर नेमिचंद स्वामी को नमस्कार करके, जो उपदेश द्वारा पूर्वाचार्य परम्परा से चला आ रहा है इसलिए सिद्ध और पूर्वापर विरोधादि दोषों से रहित होने के कारण शुद्ध और दूसरे की निन्दा आदि न करने के कारण तथा रागादि का उत्पादक न होने से निष्कलंक है और जिससे सम्यक्त्वादि गुणरूपी रत्नभूषणों की प्राप्ति होती है—जो विकथा आदि की तरह राग का कारण नहीं है, इस प्रकार के जीवप्ररूपणा नामक ग्रन्थ को अर्थात् जिसमें अशुद्ध जीव के स्वरूप, भेद-प्रभेद आदि दिखाये गये हैं इस प्रकार के ग्रंथ को कहूँगा।
भावार्थ—प्रकृत गाथा का अर्थ संस्कृत टीका में २४ तीर्थंकर, श्री वर्धमान भगवान, सिद्ध परमेष्ठी, आत्मा, सिद्ध समूह, पंचपरमेष्ठी, नेमिनाथ भगवान, जीवकाण्ड ग्रंथ और श्री नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती इन सभी के नमस्कारपरक किया गया है। वह विशेष जिज्ञासुओं को वहीं देखना चाहिए।
प्ररूपणाएँ कितनी हैं?
गुण जीवा पज्जत्ती, पाणा सण्णा य मग्गणाओ य।
उवओगो वि य कमसो, वीसं तु परूवणा भणिदा।।२।।
गुण-जीवा: पर्याप्तय: प्राणा: संज्ञाश्च मार्गणाश्च।
उपयोगो पि च क्रमश: विंशतिस्तु प्ररूपणा भणिता:।।२।।
<
अर्थ—गुणस्थान, जीवसमास, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा, चौदह मार्गणा और उपयोग इस प्रकार ये बीस प्ररूपणा पूर्वाचार्यों ने कही हैं।
भावार्थ—इनको इसलिये प्ररूपणा कहा है कि इन्हीं के द्वारा अथवा इन विषयों का आश्रय लेकर इस ग्रंथ में जीवद्रव्य का प्ररूपण किया जाएगा। इनका लक्षण उस-उस अधिकार में स्वयं आचार्य यद्यपि करेंगे फिर भी संक्षेप में इनका स्वरूप प्रारंभ में यहाँ पर भी लिख देना उचित प्रतीत होता है। मोह और योग के निमित्त से होने वाली आत्मा के सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र गुण की अवस्थाओं को गुणस्थान कहते हैं। जिन सदृश धर्मों के द्वारा अनेक जीवों का संग्रह किया जा सके, उन सदृश धर्मों का नाम जीवसमास है। गृहीत आहारवर्गणाओं को खल, रस भाग आदि के रूप में परिणत करने की शक्ति विशेष की पूर्णता को पर्याप्ति कहते हैं। जिनका संयोग रहने पर ‘‘यह जीता है’’ और वियोग होने पर ‘‘यह मर गया’’ इस तरह का जीव में व्यवहार हो, उनको प्राण कहते हैं। आहारादि की वांछा को संज्ञा कहते हैं। जिनके द्वारा विवक्षित अनेक अवस्थाओें में स्थित जीवों का ज्ञान हो, उनको मार्गणा कहते हैं। बाह्य तथा अभ्यन्तर कारणों के द्वारा होने वाली आत्मा के चेतना गुण की सामान्य—निराकार अथवा विशेष—साकार परिणति विशेष को उपयोग कहते हैं।
भावार्थ—इस गाथा में तीन ‘‘च’’, एक ‘‘अपि’’ और एक ‘‘तु’’ का जो उल्लेख है, उनमें से संज्ञा के साथ आया हुआ पहला ‘‘च’’ शब्द अपने पूर्व की गुणस्थानादि पाँचों ही प्ररूपणाओं का समुच्चय अर्थ सूचित करता है, क्योंकि ये समुच्चय रूप एक-एक प्ररूपणा हैं। ‘‘मार्गणा’’ शब्द बहुवचनान्त है और उसके साथ भी ‘‘च’’ का प्रयोग है। अतएव एक ही मार्गणामहाधिकार की १४ गति आदि प्ररूपणा हैं। उनमें से प्रत्येक का अधिकार रूप से यहाँ समुच्चय रूप में प्ररूपण किया गया है, ऐसा समझना चाहिए। उपयोग शब्द के साथ ‘‘अपि’’ और ‘‘च’’ का प्रयोग है, यह इस बात को सूचित करता है कि यह भी एक स्वतंत्र प्ररूपणाधिकार है और अन्य गुणस्थानादि १९ अधिकारों की अपेक्षा जीव अथवा आत्मा का लक्षण होने से अपनी असाधारणता रखता है, क्योंकि मृग्य जीवों के मार्गयिता तत्त्व श्रद्धालु भव्य जीव के लिए मार्गण—अन्वेषण में मार्गणाएँ करण या अधिकरण हैं किन्तु उपयोग सभी जीवों में पाया जाने वाला असाधारण लक्षण होने से मार्गणा का सामान्य एवं महान उपाय है।
‘‘तु’’ शब्द इस बात को सूचित करता है कि सामान्य से तो एक ही प्ररूपणा है परन्तु विशेषापेक्षा उसके संक्षिप्त रुचि वालों की अपेक्षा दो भेद हैं और मध्यम रुचि वालों की अपेक्षा से ये बीस भेद हैं। दो भेदों में बीस का अन्तर्भाव किस तरह हो जाता है यह आगे बताया जाएगा।
इस गाथा में कही गई ये बीस प्ररूपणाएँ वे ही हैं जिनके कि आशय को गर्भित करके पुष्पदंताचार्य ने षट्खंडागम की रचना को प्रारंभ किया था और जिनपालित को पहले दीक्षा देकर फिर अपने रचित ‘‘संतसुत्तविवरण’’ को पढ़ाकर अपने साध्यायी मुनिपुंगव भगवान भूतबलि के पास भेजा था ” जिस पर से कि श्री भूतबलि द्वारा पूर्ण षट्खंडागम की रचना हुई जो कि इस जीवकाण्ड का भी मूल आधार है।
गुणस्थान व मार्गणा के पर्यायवाची नाम
संखेओ ओघो त्ति य, गुणसण्णा सा च मोहजोगभवा।
वित्थारादेसो त्ति य, मग्गणसण्णा सकम्मभवा।।३।।
संक्षेप ओघ इति, गुणसंज्ञा सा च मोहयोगभवा।
विस्तार आदेश इति च, मार्गण संज्ञा स्वकर्मभवा।।३।।
अर्थ—संक्षेप और ओघ यह गुणस्थान की संज्ञा है और वह मोह तथा योग के निमित्त से उत्पन्न होती है। इसी तरह विस्तार तथा आदेश यह मार्गणा की संज्ञा है और वह भी अपने-अपने योग्य कर्मों के उदयादि से उत्पन्न होती है। यहाँ पर चकार का ग्रहण है इससे गुणस्थान की सामान्य और मार्गणा की विशेष यह भी संज्ञा समझनी चाहिए।
यहाँ पर यह शंका हो सकती है कि मोह तथा योग के निमित्त से गुणस्थान उत्पन्न होते हैं, न कि ‘गुणस्थान’ यह संज्ञा, फिर संज्ञा को ‘मोहयोगभवा’ (मोह और योग से उत्पन्न) क्यों कहा ? इसका उत्तर यह है कि यद्यपि परमार्थ से मोह और योग के द्वारा गुणस्थान ही उत्पन्न होते हैं न कि गुणस्थान संज्ञा तथापि यहाँ पर वाच्य-वाचक में कथंचित् अभेद मानकर उपचार से संज्ञा को भी ‘‘मोहयोगभवा’’ कह दिया है।
भावार्थ—यद्यपि मोक्षमार्ग सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र इस तरह रत्नत्रयरूप है किन्तु गुणस्थानों के निर्माण में सम्यग्दर्शन और सम्यक्चारित्र दो प्रधान हैं जैसा कि ‘‘मोहयोगभवा’’ इस लक्षण पद से मालूम होता है।
गुणस्थान का सामान्य लक्षण
जेिंह दु लक्खिज्जंते, उदयादिसु संभवेहिं भावेहिं।
जीवा ते गुणसण्णा, णिद्दिट्ठा सव्वदरसीहिं।।४।।
यैस्तु लक्ष्यन्ते उदयादिषु सम्भवैर्भावै:।
जीवास्ते गुणसंज्ञा निर्दिष्टा: सर्वदर्शिभि:।।४।।
अर्थ—दर्शनमोहनीय आदि कर्मों की उदय, उपशम, क्षय, क्षयोपशम आदि अवस्था के होने पर होने वाले जिन परिणामों से युक्त जो जीव देखे जाते हैं उन जीवों को सर्वज्ञदेव ने उसी गुणस्थान वाला और उन परिणामों को गुणस्थान कहा है।
भावार्थ—जिस प्रकार किसी जीव के दर्शनमोहनीय कर्म की मिथ्यात्वप्रकृति के उदय से मिथ्यात्व (मिथ्यादर्शन) रूप परिणाम हुए तो उस जीव को मिथ्यादृष्टि और उस मिथ्यादर्शन रूप परिणाम को मिथ्यात्व गुणस्थान कहा जाएगा। गुणस्थान यह अन्वर्थ संज्ञा है, क्योंकि विवक्षित कर्मों के उदयादि से होने वाले पाँच प्रकार के जीव के भाव गुणशब्द से अभिप्रेत हैं। उन्हीं के स्थानों को गुणस्थान कहते हैं। यहाँ पर मुख्यतया मोहनीय कर्म के उदय आदिक से होने वाले भाव ही लिए हैं। मोहनीय के दो भेद हैं—दर्शनमोहनीय और चारित्रमोहनीय। इनमें से किन-किन गुणस्थानों में दर्शनमोहनीय के उदयादि की और किन-किन में चारित्र मोहनीय के उपशमादि की अपेक्षा है यह बात मूल ग्रंथ में गाथा नं. ११ से १४ तक में बताई गई है।
विवक्षित पाँच भावों का स्वरूप संक्षेप में इस प्रकार है—कर्मों के उदय से होने वाले औदयिक, उपशम से होने वाले औपशमिक, क्षय से होने वाले क्षायिक, क्षयोपशम से होने वाले क्षायोपशमिक और जिनमें उदयादिक चारों ही प्रकार के कर्म की अपेक्षा न हो, वे पारिणामिक भाव हैं, इन्हीं को गुण कहते हैं। तत्त्वार्थ सूत्र की दूसरी अध्याय में इन्हीं को जीव के स्वतत्त्व नाम से बताया है।
गुणस्थानों के नाम
मिच्छो सासण मिस्सो, अविरदसम्मो य देसविरदो य।
विरदा पमत्त इदरो, अपुव्व अणियट्टि सुहमो य।।५।।
मिथ्यात्वं सासन मिश्र अविरतसम्यक्त्वं च देशविरतश्च।
विरता: प्रमत्त इतर: अपूर्व: अनिवृत्ति: सूक्ष्मश्च।।५।।
अर्थ—
१. मिथ्यात्व
२. सासादन
३. मिश्र
४. अविरतसम्यग्दृष्टि
५. देशविरत
६. प्रमत्तविरत
७. अप्रमत्तविरत
८. अपूर्वकरण
९. अनिवृत्तिकरण
१०. सूक्ष्म साम्पराय।
इस सूत्र में चौथे गुणस्थान के साथ जो अविरत शब्द है वह अन्त्यदीपक है अतएव पहले के तीनों गुणस्थानों में भी अविरतपना समझना चाहिए। इसी प्रकार छट्ठे प्रमत्त गुणस्थान के साथ जो विरत शब्द है वह आदि दीपक है इसलिये यहाँ से लेकर सम्पूर्ण गुणस्थान विरत ही होते हैं, ऐसा समझना चाहिए।
उवसंत खीणमोहो, सजोगकेवलिजिणो अजोगी य।
चउदस जीवसमासा, कमेण सिद्धा य णादव्वा।।६।।
उपशान्त: क्षीणमोह: सयोगकेवलिजिन: अयोगी च।
चतुर्दश जीवसमासा: क्रमेण सिद्धाश्च ज्ञातव्या:।।६।।
अर्थ—
११. उपशांत मोह,
१२. क्षीणमोह,
१३. सयोगिकेवलिजिन और
१४. अयोगिकेवली जिन ये चौदह जीवसमास (गुणस्थान) हैं और सिद्ध इन जीवसमासों-गुणस्थानों से रहित हैं।
भावार्थ—इस सूत्र में क्रमेण शब्द जो पड़ा है उससे यह सूचित होता है कि जीव के सामान्यतया दो भेद हैं—एक संसारी, दूसरा मुक्त। मुक्त अवस्था संसारपूर्वक ही हुआ करती है। संसारियों के गुणस्थानों की अपेक्षा चौदह भेद हैं। इसके अनंतर क्रम से गुणस्थानों से रहित मुक्त या सिद्ध अवस्था प्राप्त होती है। इस प्रकार क्रमेण शब्द के द्वारा एक ही जीव की क्रम से होने वाली दो—संसार और सिद्ध—मुक्त अवस्थाओं के कथन से यह भी सूचित हो जाता है कि जो कोई ईश्वर को अनादि मुक्त बताते हैं अथवा आत्मा को सदा कर्मरहित या मुक्तस्वरूप मानते हैं या मोक्ष में जीव का निरन्वय विनाश कहते हैं, सो ठीक नहीं है।
इस गाथा में सयोग शब्द अन्त्यदीपक है इसलिये पूर्व के मिथ्यादृष्ट्यादि सब ही गुणस्थानवर्ती जीव योग सहित होते हैं। ‘‘जिन’’ शब्द मध्यदीपक है इससे असंयत सम्यग्दृष्टि से लेकर अयोगीपर्यन्त सभी जिन होते हैं। केवली शब्द आदि दीपक है अतएव सयोगी, अयोगी तथा सिद्ध तीनों ही केवली होते हैं, यह सूचित होता है।
मिथ्यात्वगुणस्थान का लक्षण
मिच्छोदयेण मिच्छत्तमसद्दहणं तु तच्च अत्थाणं।
एयंतं विवरीयं, विणयं संसयिदमण्णाणं।।७।।
मिथ्यात्वोदयेन मिथ्यात्वमश्रद्धानं तु तत्त्वार्थानाम्।
एकान्तं विपरीतं विनयं संशयितमज्ञानम्।७।।
अर्थ —मिथ्यात्व प्रकृति के उदय से होने वाले तत्त्वार्थ के अश्रद्धान को मिथ्यात्व कहते हैं। इसके पाँच भेद हैं—एकान्त, विपरीत, विनय, संशयित और अज्ञान।
अनेक धर्मात्मक पदार्थ को किसी एक धर्मात्मक मानना, इसको एकांत मिथ्यात्व कहते हैं। जैसे वस्तु सर्वथा क्षणिक ही है अथवा नित्य ही है, वक्तव्य ही है अथवा अवक्तव्य ही है।
धर्मादिक के स्वरूप को विपर्ययरूप मानना, इसको विपरीत मिथ्यात्व कहते हैं। जैसे यह मानना कि हिंसा से स्वर्गादिक की प्राप्ति होती है।
सम्यग्दृष्टि और मिथ्यादृष्टि देव, गुरु तथा उनके कहे हुए शास्त्रों में समान बुद्धि रखने और उनका समान सत्कारादि करने को विनय मिथ्यात्व कहते हैं। जैसे-जिन और बुद्ध तथा उनके धर्म को समान समझना तथा उनका समान सत्कारादि करना। इसके सिवाय सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्ररूप मोक्षमार्ग की अपेक्षा न रखकर केवल गुरुओं के विनय से ही मोक्ष होता है, ऐसा मानना भी विनय मिथ्यात्व है।
समीचीन तथा असमीचीन दोनों प्रकार के पदार्थों में से किसी भी एक पक्ष का निश्चय न होना इसको संशयमिथ्यात्व कहते हैं। जैसे—सग्रंथ लिंग मोक्ष का साधन है या यागादिकर्म, इसी तरह कर्मों के सर्वथा अभाव से प्रकट होने वाली अनंतगुण विशिष्ट आत्मा की शुद्ध अवस्था विशेष को मोक्ष कहते हैं, यद्वा बुद्धि-सुख-दु:खादि विशेष गुणों के उच्छेद को मोक्ष कहते हैं।
जीवादि पदार्थों को ‘यही है, इसी प्रकार से है’ इस तरह विशेष रूप से न समझने को अज्ञान मिथ्यात्व कहते हैं।
सासादन गुणस्थान का स्वरूप
आदिमसम्मत्तद्धा, समयादो छावली त्ति वा सेसे।
अणअण्णदरूदयादो, णासियसम्मो त्ति सासणक्खो सो।।८।।
आदिमसम्यक्त्वाद्वा, आसमयत: षडावलिरिति वा शेषे।
अनान्यतरोदयात्, नाशितसम्यक्त्व इति सासनाख्य: स:।।८।।
अर्थ—प्रथमोपशम सम्यक्त्व के अथवा यहाँ पर वा शब्द का ग्रहण किया है, इसलिये द्वितीयोपशम सम्यक्त्व के अंतर्मुहूर्त मात्र काल में से जब जघन्य एक समय तथा उत्कृष्ट छह आवली प्रमाण शेष रहे, उतने काल में अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ में से किसी के भी उदय में आने से सम्यक्त्व की विराधना होने पर सम्यग्दर्शन गुण की जो अव्यक्त अतत्वश्रद्धानरूप परिणति
मिश्रगुणस्थान का लक्षण
सम्मामिच्छुदयेणय, जत्तंतरसव्वघादिकज्जेण।
ण य सम्मं मिच्छं पि य, सम्मिस्सो होदि परिणामो।।९।।
सम्यग्मिथ्यात्वोदयेन च, जात्यन्तरसर्वघातिकार्येण।
न च सम्यक्त्वं मिथ्यात्वमपि च, सम्मिश्रो भवति परिणाम:।।९।।
अर्थ—जिसका प्रतिपक्षी आत्मा के गुण को सर्वथा घातने का कार्य दूसरी सर्वघाति प्रकृतियों से विलक्षण जाति का है, उस जात्यन्तर सर्वघाति सम्यग्मिथ्यात्व प्रकृति के उदय से केवल सम्यक्त्वरूप या मिथ्यात्वरूप परिणाम न होकर जो मिश्ररूप परिणाम होता है, उसको तीसरा मिश्रगुणस्थान कहते हैं।
शंका—यह तीसरा गुणस्थान बन नहीं सकता, क्योंकि मिश्ररूप परिणाम ही नहीं हो सकते। यदि विरुद्ध दो प्रकार के परिणाम एक ही आत्मा और एक ही काल में माने जाएँ तो शीत-उष्ण की तरह परस्पर सहानवस्थान लक्षण विरोध दोष आवेगा। यदि क्रम से दोनों परिणामों की उत्पत्ति मानी जाय, तो मिश्ररूप तीसरा गुणस्थान नहीं बनता ?
समाधान—यह शंका ठीक नहीं है क्योंकि मित्रामित्रन्याय से एक काल और एक ही आत्मा में मिश्ररूप परिणाम हो सकते हैं।
भावार्थ—जिस प्रकार देवदत्त नामक किसी मनुष्य में यज्ञदत्त की अपेक्षा मित्रपना और चैत्र की अपेक्षा अमित्रपना ये दोनों धर्म एक ही काल में रहते हैं और उनमें कोई विरोध नहीं है, उस ही प्रकार सर्वज्ञ निरूपित पदार्थ में स्वरूप के श्रद्धान की अपेक्षा समीचीनता और सर्वज्ञाभास कथित अतत्व श्रद्धान की अपेक्षा मिथ्यापना, ये दोनों ही धर्म एक काल और एक आत्मा में घटित हो
चतुर्थगुणस्थान का लक्षण
सम्मत्तदेसघादिस्सुदयादो वेदगं हवे सम्मं।
चलमलिनमगाढं तं, णिच्चं कम्मक्खवणहेदु ।।१०।।
सम्यक्त्वदेशघातेरुदयाद्वेदकं भवेत्सम्यक्त्वम्।
चलं मलिनमगाढं, तन्नित्यं कर्मक्षपणहेतु।।१०।।
अर्थ—सम्यग्दर्शनगुण को विपरीत करने वाली प्रकृतियों में से देशघाति सम्यक्त्व प्रकृति के उदय होने पर (तथा अनंतानुबंधिचतुष्क और मिथ्यात्व मिश्र इन सर्वघाति प्रकृतियों के आगामी निषेकों का सदवस्थारूप उपशम और वर्तमान निषेकों की बिना फल दिए ही निर्जरा होने पर) जो आत्मा के परिणाम होते हैं उनको वेदक या क्षायोपशमिक सम्यग्दर्शन कहते हैं। वे परिणाम चल, मलिन या अगाढ़ होते हुए भी नित्य ही अर्थात् जघन्य अंतर्मुहूर्त से लेकर उत्कृष्ट छ्यासठ सागर पर्यन्त कर्मों की निर्जरा के कारण हैं।
जिस प्रकार एक ही जल अनेक कल्लोलरूप में परिणत होता है, उस ही प्रकार जो सम्यग्दर्शन सम्पूर्ण तीर्थंकर या अर्हन्तों में समान अनंत शक्ति के होने पर भी ‘‘श्रीशांतिनाथ जी शांति के लिये और श्रीपार्श्वनाथ जी रक्षा करने के लिए समर्थ हैं’’ इस तरह नाना विषयों में चलायमान होता है उसको चल सम्यग्दर्शन कहते हैं। जिस प्रकार शुद्ध सुवर्ण भी मल के निमित्त से मलिन कहा जाता है, उस ही तरह सम्यक्त्व प्रकृति के उदय से जिसमें पूर्ण निर्मलता नहीं है उसको मलिन सम्यग्दर्शन कहते हैं। जिस तरह वृद्ध पुरुष के हाथ में ठहरी हुई भी लाठी काँपती है उस ही तरह जिस सम्यग्दर्शन के होते हुए भी अपने बनवाये हुए मंदिरादि में ‘‘यह मेरा मंदिर है’’ और दूसरे के बनवाये हुए मंदिरादि में ‘‘यह दूसरे का है’’ ऐसा भाव हो, उसको अगाढ़ सम्यग्दर्शन कहते हैं।
भावार्थ—उपशम के प्रशस्त और अप्रशस्त इस तरह दो प्रकार हैं। विवक्षित प्रकृति यदि उदय योग्य न हो और स्थिति, अनुभाग, उत्कर्षण, अपकर्षण तथा संक्रमण के योग्य हो तो उस उपशम को अप्रशस्त कहते हैं तथा जहाँ पर विवक्षित प्रकृति उदय योग्य भी न हो और उत्कर्षण, अपकर्षण एवं संक्रमणयोग्य भी न हो तो वहाँ प्रशस्त उपशम कहा जाता है। अनंतानुबंधी कषाय का अप्रशस्तोपशम अथवा विसंयोजन होने पर एवं दर्शनमोहनीय की मिथ्यात्व और मिश्र प्रकृति का प्रशस्त या अप्रशस्त उपशम अथवा क्षयोन्मुखता के होने पर और सम्यक्त्व प्रकृति के देशघाति स्पर्धकों का उदय होने पर जो तत्त्वार्थ श्रद्धानरूप परिणाम होते हैं, उनको ही वेदक या क्षायोपशमिक सम्यक्त्व कहते हैं। यहाँ पर जीव सम्यक्त्व प्रकृति के उदय का वेदन-अनुभवन करता है, इसलिये इसको वेदक कहते हैं।
गाथा में आए हुए नित्य शब्द का अभिप्राय अविनश्वर नहीं किन्तु अंतर्मुहूर्त से लेकर छ्यासठ सागर तक के काल के प्रमाण से है जैसा कि ऊपर बताया गया है अथवा इसका आशय ऐसा भी हो सकता है कि कर्मों के क्षपण का यह करण—असाधारण कारण है। यह बात केवल इस क्षायोपशमिक सम्यक्त्व के विषय में ही नहीं किन्तु वक्ष्यमाण औपशमिक एवं क्षायिक के विषय में भी समझनी चाहिए क्योंकि सम्यग्दर्शन के साहचर्य के बिना संवर निर्जरा नहीं हो सकती, यह ध्रुव नियम है। इस ध्रुव नियम को स्पष्ट करना ही नित्य शब्द का अभिप्राय हैै। इससे मोक्षमार्ग में सम्यग्दर्शन की असाधारणता सूचित हो जाती है तथा यह भी विशेषता व्यक्त होती है कि इस क्षायोपशमिक सम्यक्त्व के वेदक अथवा समल होते हुए भी वह कर्मक्षपण का कारण है। ध्यान रहे कि चतुर्थ गुणस्थान से लेकर ऊपर के सभी गुणस्थानों में होने वाली विशिष्ट निर्जरा का मूल कारण सम्यग्दर्शन ही है।
सम्माइट्ठी जीवो, उवइट्ठं पवयणं तु सद्दहदि।
सद्दहदि असब्भावं, अजाणमाणो गुरूणियोगा।।११।।
सम्यग्दृष्टिर्जीव उपदिष्टं, प्रवचनं तु श्रद्दधाति।
श्रद्दधात्यसद्भावमज्ञायमानो गुरुनियोगात्।।११।।
अर्थ—सम्यग्दृष्टि जीव आचार्यों के द्वारा उपदिष्ट प्रवचन का श्रद्धान करता है किन्तु अज्ञानतावश गुरु के उपदेश से विपरीत अर्थ का भी श्रद्धान कर लेता है।
भावार्थ—स्वयं के अज्ञानवश ‘अरिहंतदेव का ऐसा ही उपदेश’ है ऐसा समझकर यदि कदाचित् किसी पदार्थ का विपरीत श्रद्धान भी करता है तो भी वह सम्यग्दृष्टि ही है क्योंकि उसने अरिहंत का उपदेश समझकर उस पदार्थ का वैसा श्रद्धान किया है। परन्तु—
सुत्तादो तं सम्मं, दरसिज्जंतं जदा ण सद्दहदि।
सो चेव हवइ मिच्छाइट्ठी जीवो तदो पहुदी।।१२।।
सूत्रात्तं सम्यक् दर्शयन्तं, यदा न श्रद्दधाति।
स चैव भवति मिथ्यादृष्टिर्जीवस्तदा प्रभृति।।१२।।
अर्थ—गणधरादिकथित सूत्र के आश्रय से आचार्यादि के द्वारा भले प्रकार समझाए जाने पर भी यदि वह जीव उस पदार्थ का समीचीन श्रद्धान न करे तो वह जीव उस ही काल से मिथ्यादृष्टि हो जाता है।
भावार्थ—आगम दिखाकर समीचीन पदार्थ के समझाने पर भी यदि वह जीव पूर्व में अज्ञान से किए हुए अतत्वश्रद्धान को न छोड़े, तो वह जीव उस ही काल से मिथ्यादृष्टि कहा जाता है।
इसी चतुर्थ गुणस्थानवर्ती जीव के असंयत विशेषण की अपेक्षा को दृष्टि में रखकर उसके आशय को स्पष्ट करने के लिये विशेष स्वरूप दिखाते हैं।
णो इंदियेसु विरदो, णो जीवे थावरे तसे वापि।
जो सद्दहदि जिणुत्तं, सम्माइट्ठी अविरदो सो।।१३।।
नो इंद्रियेषु विरतो, नो जीवे स्थावरे त्रसे वापि।
य: श्रद्दधाति जिनोत्तं, सम्यग्दृष्टिरविरत: स:।।१३।।
अर्थ—जो इंद्रियों के विषयों से तथा त्रस-स्थावर जीवों कीहिंसा से विरक्त नहीं है किन्तु जिनेन्द्रदेव द्वारा कथित प्रवचन का श्रद्धान करता है वह अविरत सम्यग्दृष्टि है।
भावार्थ—संयम दो प्रकार का होता है—एक इंद्रिय संयम, दूसरा प्राणीसंयम। इंद्रियों के विषयों से विरक्त होने को इंद्रिय संयम और अपने तथा पर के प्राणों की रक्षा को प्राणीसंयम कहते हैं। इस गुणस्थान में दोनों संयमों में से कोई भी संयम नहीं होता, अतएव इसको अविरतसम्यग्दृष्टि कहते हैं। परन्तु इस गुणस्थान के लक्षण में जो अपि शब्द पड़ा है उससे सूचित होता है कि वह बिना प्रयोजन किसीहिंसा में प्रवृत्त भी नहीं होता क्योंकि यहाँ असंयम भाव से प्रयोजन अप्रत्याख्यानावरणादि कषाय के क्षयोपशम से पाँचवें आदि गुणस्थानों में पाए जाने वाले देशसंयम तथा आगे के संयमभाव के निषेध से है अतएव असंयत कहने का अर्थ यह नहीं है कि सम्यग्दृष्टि की प्रवृत्ति मिथ्यादृष्टि के समान अथवा अनर्गल हुआ करती है क्योंकि चतुर्थ गुणस्थान में ४१ कर्मप्रकृतियों के बंध का व्युच्छित्ति के नियमानुसार अभाव हो जाया करता है अतएव ४१ कर्मों के बंध की कारणभूत प्रवृत्तियाँ उसके न तो होती ही हैं और न उनका होना संभव ही है अतएव उसकी अंतरंग-बहिरंग प्रवृत्ति में नीचे के तीन गुणस्थान वालों की अपेक्षा महान अंतर हो जाया करता है।
देशविरत गुणस्थान का लक्षण
पच्चक्खाणुदयादो, संजमभावो ण होदि णविंर तु।
थोववदो होदि तदो, देसवदो होदि पंचमओ।।१४।।
प्रत्याख्यानोदयात्, संयमभावो न भवति नवरि तु।
स्तोकव्रतो भवति ततो, देशव्रतो भवति पंचम:।।१४।।
अर्थ—यहाँ पर प्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय रहने से पूर्ण संयम तो नहीं होता, किन्तु यहाँ इतनी विशेषता होती है कि अप्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय न रहने से एकदेश व्रत होते हैंं अतएव इस गुणस्थान का नाम देशव्रत या देशसंयम है। इसी को पाँचवाँ गुणस्थान कहते हैं।
भावार्थ—प्रत्याख्यान शब्द का अर्थ त्याग-पूर्णत्याग-सकलसंयम होता है। उसको आवृत करने वाली कषाय को प्रत्याख्यानावरण कहते हैं। नाम के एकदेश का उच्चारण करने पर पूरे नाम का बोध हो जाता है, इसी न्याय से यहाँ गाथा में प्रत्याख्यान शब्द का प्रयोग प्रत्याख्यानावरण के लिये किया गया है। यह हेतुवाक्य है। इससे एकदेश संयम और चारित्र की अपेक्षा यहाँ पाया जाने वाला क्षायोपशमिक भाव ये दो बातें सूचित होती हैं क्योंकि तृतीय कषाय के उदय का मुख्यतया उल्लेख नीचे की अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावरणचतुष्क इन आठ कषायों के उदय के अभाव को व्यक्त करता है।
छट्ठे गुणस्थान का लक्षण
संजलणणोकसायाणुदयादो संजमो हवे जम्हा।
मलजणणपमादो वि य, तम्हा हु पमत्तविरदो सो।।१५।।
संज्वलननोकषायाणामुदयात् संयमो भवेद्यस्मात्।
मलजननप्रमादो पि च तस्मात् खलु प्रमत्तविरत: स:।।१५।।
अर्थ—सकल संयम को रोकने वाली प्रत्याख्यानावरण कषाय का क्षयोपशम होने से पूर्ण संयम तो हो चुका है किन्तु उस संयम के साथ-साथ संज्वलन और नोकषाय का उदय रहने से संयम में मल को उत्पन्न करने वाला प्रमाद भी होता है अतएव इस गुणस्थान को प्रमत्तविरत कहते हैं।
भावार्थ—चौदह गुणस्थानों में यह छट्ठा गुणस्थान है परन्तु पूर्ण संयम जिनमें पाया जाता है, उनमें यह सबसे पहला है। यहाँ पर पूर्ण संयम के साथ प्रमाद भी पाया जाता है। यह प्रमाद संज्वलन कषाय के तीव्र उदय से हुआ करता है। आगे के गुणस्थानों में उसका मंद, मंदतर, मंदतम उदय हुआ करता है। संज्वलन के तीव्र उदय में भी प्रत्याख्यानावरण के अभाव से प्रकट हुए सकल संयम का घात करने की सामर्थ्य नहीं है, उससे प्रमादरूप मल ही उत्पन्न हो सकता है। इस गुणस्थान में भी औदयिकादि पाँच भावों में से चारित्र की अपेक्षा केवल क्षायोपशमिक भाव ही है किन्तु सम्यक्त्व की अपेक्षा पाँचवें गुणस्थान के समान औपशमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक इन तीन में से कोई भी एक भाव-सम्यग्दर्शन अवश्य पाया जाता है क्योंकि यहाँ द्रव्यसंयम की नहीं, अपितु भावसंयम की ही अपेक्षा है। यद्यपि यहाँ संज्वलन का उदय पाया जाता है फिर भी औदयिकभाव अभीष्ट-विवक्षित नहीं है क्योंकि सकल संयम जो यहाँ हुआ है, वह संज्वलन के उदय से नहीं किन्तु प्रत्याख्यानावरण के क्षयोपशम से हुआ है।
पंद्रह प्रमाद
विकहा तहा कसाया, इंदिय णिद्दा तहेव पणयो च।
चदु चदु पणमेगेगं, होंति पमादा हु पण्णरस।।१६।।
विकथास्तथा कषाया, इंद्रियनिद्रास्तथैव प्रणयश्च।
चतु: चतु: पंचैवैकं, भवन्ति प्रमादा: खलु पंचदश।।१६।।
अर्थ—चार विकथा—स्त्रीकथा, भक्तकथा, राष्ट्रकथा, अवनिपालकथा। चार कषाय—क्रोध, मान, माया, लोभ। पंच इंद्रिय—स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, श्रोत। एक निद्रा और एक प्रणय—स्नेह। इस तरह कुल मिलाकर प्रमादों के पंद्रह भेद हैं।
भावार्थ—संयम के विरोधी कथा या वाक्य प्रबंध को विकथा, इसी प्रकार जिससे संयम गुण का घात हो ऐसे क्रोध, मान, माया, लोभरूप परिणाम को कषाय, स्पर्शनादि इंद्रियों के द्वारा अपने-अपने स्पर्शादि विषय में रागभाव के होने को इंद्रिय, स्त्यानगृद्धि आदि तीन कर्मों के उदय से अथवा निद्रा और प्रचला के तीव्र उदय से अपने विषय में सामान्य ग्रहण को रोकने वाली जो जाड्यावस्था उत्पन्न होती है उसको निद्रा, बाह्य पदार्थों में ममत्व परिणाम को अथवा तीव्र हास्यादि नोकषायों के उदय से होने वाले संक्लेश परिणाम को प्रणय कहते हैं। ध्यान रहे कि यहाँ पर संज्वलन और तत्संबंधी नोकषाय के तीव्र उदय से होने वाले ही परिणाम प्रमाद शब्द से विवक्षित हैं। इन पंद्रह प्रमादों के कारण सम्यग्दर्शन या गुण, शील आदि कुशलानुष्ठान में असावधानी अथवा अनादर आदि भाव हो जाया करते हैं। यही प्रमाद है जो कि संयत को प्रमत्त बना देता है। यह दशा अन्तर्मुहूर्त से अधिक काल तक नहीं रहा करती, उसके बाद अप्रमत्त गुणस्थान१ हो जाया करता है और इन दोनों गुणस्थानों में इसी तरह हजारों बार परिवर्तन होता रहता है।
सप्तम गुणस्थान का स्वरूप
संजलणणोकसायाणुदओ मंदो जदा तदा होदि।
अपमत्तगुणो तेण य, अपमत्तो संजदो होदि।।१७।।
संज्वलननोकषायाणामुदयो मन्दो यदा तदा भवति।
अप्रमत्तगुणस्तेन च, अप्रमत्त: संयतो भवति।।१७।।
अर्थ—जब संज्वलन और नोकषाय का मंद उदय होता है तब सकल संयम से युक्त मुनि के प्रमाद का अभाव हो जाता है, इस ही लिये इस गुणस्थान को अप्रमत्तसंयत कहते हैं। इसके दो भेद हैं—स्वस्थानाप्रमत्त एवं दूसरा सातिशयाप्रमत्त।
छट्ठे गुणस्थान में संयत का प्रमत्त विशेषण अन्त्यदीपक है अतएव यहाँ तक के सभी गुणस्थान वाले जीव प्रमादसहित हुआ करते हैं और इससे ऊपर के गुणस्थान वाले सभी जीव प्रमादरहित ही होते हैंं। यही कारण है कि सातवें गुणस्थान का नाम अप्रमत्तसंयत है।
प्रश्न– हो सकता है कि जब ऊपर के यहाँ से आगे के सभी गुणस्थान संयत और अप्रमत्त हैं तब अप्रमत्तसंयत इस नाम से सभी गुणस्थानों का ग्रहण हो जाएगा, अतएव आठवें आदि गुणस्थानों के भिन्न-भिन्न नामनिर्देश की क्या आवश्यकता है ?
उत्तर—यद्यपि संज्वलन के तीव्र उदय के अभाव की अपेक्षा ऊपर के सभी गुणस्थान सामान्यरूप से अप्रमत्त हैं, फिर भी उन गुणस्थानों में होने वाले या पाए जाने वाले अन्य कार्यों का विशेषण रूप से उल्लेख करके उन-उनका भिन्न-भिन्न नाम निर्देश किया गया है।
अब अपूर्वकरण गुणस्थान को कहते हैं
अंतोमुहुत्तकालं, गमिऊण अधापवत्तकरणं तं।
पडिसमयं सुज्झंतो, अपुव्वकरणं समल्लियइ।।१८।।
अन्तर्मुहूर्त कालं गमयित्वा, अध: प्रवृत्तकरणं तत्।
पडिसमयं शुध्दयन्,अपुव्वकरणं समाश्रयति ||१८
अर्थ—जिसका अंतर्मुहूर्त मात्र काल है, ऐसे अध:प्रवृत्तकरण को बिताकर वह सातिशय अप्रमत्त जब प्रतिसमय अनंतगुणी विशुद्धि को लिये हुए अपूर्वकरण जाति के परिणामों को करता है, तब उसको अपूर्वकरणनामक अष्टमगुणस्थानवर्ती कहते हैं।
भावार्थ—यहाँ विशुद्धि शब्द उपलक्षण मात्र होने से प्रशस्त प्रकृतियों के चतु:स्थानी अनुभाग की अनंतगुणी वृद्धि, अप्रशस्त प्रकृतियों के द्विस्थानी अनुभाग की अनंतगुणी हानि तथा
नवमें गुणस्थान का स्वरूप
एकह्मि कालसमये, संठाणादीहिं जह णिवट्टंति।
ण णिवट्टंति तहावि य, परिणामेहिं मिहो जेहिं।।१९।।
होंति अणियट्टिणो ते, पडिसमयंजेस्सिमेक्कपरिणामा।
विमलयरझाणहुयवहसिहाहिं णिद्दड्ढकम्मवणा।।२०।।।।जुम्मम्।।
एकस्मिन् कालसमये, संस्थानादिभिर्यथा निवर्र्तन्ते।
न निवर्तन्ते तथापि च परिणामैर्मिथो यै:।।१९।।
भवन्ति अनिवर्तिनस्ते प्रतिसमयं येषामेकपरिणामा:।
विमलतरध्यानहुतवहशिखाभिर्निर्दग्धकर्मवना:।।२०।।युग्मम्।।
अर्थ—अंतर्मुहूर्तमात्र अनिवृत्तिकरण के काल में से आदि या मध्य या अंत के एक समयवर्ती अनेक जीवों में जिस प्रकार शरीर की अवगाहना आदि बाह्य कारणों से तथा ज्ञानावरणादिक कर्म के क्षयोपशमादि अंतरंग कारणों से परस्पर में भेद पाया जाता है, उस प्रकार जिन परिणामों के निमित्त से परस्पर में भेद नहीं पाया जाता, उनको अनिवृत्तिकरण कहते हैं। अनिवृत्तिकरण गुणस्थान का जितना काल है उतने ही उसके परिणाम हैं। इसलिए उसके काल के प्रत्येक समय में अनिवृत्तिकरण का एक ही परिणाम होता है तथा ये परिणाम अत्यंत निर्मल ध्यानरूप अग्नि की शिखाओं की सहायता से कर्मवन को भस्म कर देते हैं।
भावार्थ—यहाँ पर एक समयवर्ती नाना जीवों के परिणामों में पाई जाने वाली विशुद्धि में परस्पर निवृत्ति—भेद नहीं पाया जाता अतएव इन परिणामों को अनिवृत्तिकरण कहते हैं। अनिवृत्तिकरण का जितना काल है उतने ही उसके परिणाम हैं इसलिये प्रत्येक समय में एक ही परिणाम होता है। यही कारण है कि यहाँ पर भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणामों में सर्वथा विसदृशता और एक समयवर्ती जीवों के परिणामों में सर्वथा सदृशता ही पाई जाती है। इन परिणामों से ही आयुकर्म को छोड़कर शेष सात कर्मों की गुणश्रेणी निर्जरा, गुणसंक्रमण, स्थितिखण्डन एवं अनुभागखण्डन होता है और
दशवें गुणस्थान का स्वरूप
धुदकोसुंभयवत्थं, होहि जहा सुहमरायसंजुत्तं।
एवं सुहमकसाओ, सुहमसरागोत्ति णादव्वो।।२१।।
धौतकौसुम्भवस्त्रं, भवति यथा सूक्ष्मरागसंयुक्तम्।
एवं सूक्ष्मकषाय: सूक्ष्मसराग इति ज्ञातव्य:।।२१।।
अर्थ—जिस प्रकार धुले हुए कसूमी वस्त्र में लालिमा—सुर्खी सूक्ष्म रह जाती है उसी प्रकार जो जीव अत्यन्त सूक्ष्म राग-लोभ कषाय से युक्त हैं उनको सूक्ष्म-साम्पराय नामक दशम गुणस्थानवर्ती कहते हैं।
भावार्थ—जहाँ पर पूर्वोक्त तीन करण के परिणामों से क्रम से लोभ कषाय के बिना चारित्रमोहनीय कर्म की बीस प्रकृतियों का उपशम अथवा क्षय हो जाने पर सूक्ष्म कृष्टि को प्राप्त केवल लोभ कषाय का ही उदय पाया जाए, उसको सूक्ष्मसाम्पराय नाम का दशवां गुणस्थान कहते हैं।
उपशांतकषाय गुणस्थान का स्वरूप
कदग फलजुदजलं वा, सरए सरवाणियं व णिम्मलयं।
सयलोवसंतमोहो, उवसंतकसायओ होदि।।२२।।
कतक-फल-युतजलं वा, शरदि सर: पानीयं व निर्मलम्।
सकलोपशान्तमोह ,उपशांतकषायको भवति ||२२||
अर्थ—निर्मली फल से युक्त जल की तरह अथवा शरद ऋतु में ऊपर से स्वच्छ हो जाने वाले सरोवर के जल की तरह सम्पूर्ण मोहनीय कर्म के उपशम से उत्पन्न होने वाले निर्मल परिणामों को उपशांतकषाय नाम का ग्यारहवाँ गुणस्थान कहते हैं।
भावार्थ—इस गुणस्थान का पूरा नाम ‘‘उपशांतकषाय वीतराग छद्मस्थ’’ है। छद्म शब्द का अर्थ है—ज्ञानावरण, दर्शनावरण। जो जीव इनके उदय की अवस्था में पाये जाते हैं वे सब छद्मस्थ हैं। छद्मस्थ भी दो तरह के हुआ करते हैं—एक सराग, दूसरे वीतराग। ग्यारहवें, बारहवें गुणस्थानवर्ती जीव वीतराग और इनसे नीचे के सब सराग छद्मस्थ हैं। कर्दम सहित जल में निर्मली डालने से कर्दम नीचे बैठ जाता है और ऊपर स्वच्छ जल रह जाता है। इसी प्रकार इस गुणस्थान में मोहकर्म के उदयरूप कीचड़ का सर्वथा उपशम हो जाता है और ज्ञानावरण का उदय रहता है इसलिए इस गुणस्थान का यथार्थ नाम उपशांतकषाय वीतराग छद्मस्थ है।
यहाँ पर चारित्र की अपेक्षा केवल औपशमिक भाव और सम्यक्त्व की अपेक्षा औपशमिक और क्षायिक इस तरह से दो भाव पाये जाते हैं।
बारहवें गुणस्थान का स्वरूप
णिस्सेसखीणमोहो, फलिहामलभायणुदयसमचित्तो।
खीणकसाओ भण्णदि, णिग्गंथो वीयरायेहिं।।२३।।
नि:शेषक्षीणमोह: स्फटिकामलभाजनोदकसमचित्त:|
क्षीणकसायो भण्यते ,निर्ग्रन्थो वीतरागैः ||२३||
अर्थ—जिस निर्ग्रन्थ का चित्त मोहनीय कर्म के सर्वथा क्षीण हो जाने से स्फटिक के निर्मल पात्र में रखे हुए जल के समान निर्मल हो गया है उसको वीतराग देव ने क्षीणकषाय नामक बारहवें गुणस्थानवर्ती कहा है।
भावार्थ—जिस छद्मस्थ की वीतरागता के विरोधी मोहनीय कर्म के द्रव्य एवं भाव दोनों ही प्रकारों का अथवा प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेशरूप चारों ही भेदों का सर्वथा बंध, उदय, उदीरणा एवं सत्व की अपेक्षा क्षय हो जाता है वह बारहवें गुणस्थान वाला माना जाता है इसलिए आगम में इसका नाम क्षीणकषाय वीतराग छद्मस्थ ऐसा बताया है। यहाँ छद्मस्थ शब्द अन्त्यदीपक है और वीतराग शब्द नाम, स्थापना और द्रव्यरूप वीतरागता की निवृत्ति के लिए है तथा यहाँ पर पाँच भावों में से मोहनीय के सर्वथा अभाव की अपेक्षा से एक क्षायिक भाव ही माना गया है।
तेरहवें गुणस्थान का वर्णन
केवलणाणदिवायर, किरण-कलावप्पणासियण्णाणो।
णवकेवललद्धुग्गम, सुजणियपरमप्पववएसो।।२४।।
केवलज्ञानदिवाकर,-किरणकलापप्रणाशिताज्ञान:।
नवकेवललब्ध्युद्गमसुजनितपरमात्मव्यपदेश:।।२४।।
अर्थ—जिसका केवलज्ञानरूपी सूर्य की अविभागप्रतिच्छेदरूप किरणों के समूह से (उत्कृष्ट अनंतानंत प्रमाण) अज्ञान अंधकार सर्वथा नष्ट हो गया हो और जिसको नव केवललब्धियों के (क्षायिक सम्यक्त्व, चारित्र, ज्ञान, दर्शन, दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य) प्रकट होने से परमात्मा यह व्यपदेश (संज्ञा) प्राप्त हो गया है, वह इंद्रिय, आलोक आदि की अपेक्षा न रखने वाले ज्ञान-दर्शन से युक्त होने के कारण केवली और योग से युक्त रहने के कारण सयोग तथा घाति कर्मों से रहित होेने के कारण जिन कहा जाता है ऐसा अनादिनिधन आर्ष आगम में कहा है।
भावार्थ—बारहवें गुणस्थान का विनाश होते ही जिसके तीन१ घाति कर्म और अघाति कर्मों की १६ प्रकृति, इस तरह कुल मिलाकर ६३ कर्म प्रकृतियों के नष्ट होने से अनंत चतुष्टय-अनंतज्ञान, अनंतदर्शन, अनंतसुख और अनंत वीर्य तथा केवललब्धि प्रकट हो चुकी हैं किन्तु साथ ही जो योग से भी युक्त है उस अरिहंत परमात्मा को तेरहवें गुणस्थानवर्ती कहते हैं।
चौदहवें अयोगकेवली गुणस्थान का वर्णन
सीलेसिं संपत्तो, णिरुद्धणिस्सेसआसवो जीवो।
कम्मरयविप्पमुक्को, गयजोगो केवली होदि।।२५।।
शीलैश्यं संप्राप्तो, निरुद्ध नि:शेषास्रवो जीव:।
कर्मरजोविप्रमुक्तो, गतयोग: केवली भवति।।२५।।
अर्थ—जो अठारह हजार शील के भेदों का स्वामी हो चुका है और जिसके कर्मों से आने का द्वाररूप आस्रव सर्वथा बंद हो गया है तथा सत्व और उदयरूप अवस्था को प्राप्त कर्मरूप रज की सर्वथा निर्जरा होने से जो उस कर्म से सर्वथा मुक्त होने के सम्मुख है उस योगरहित केवली को चौदहवें गुणस्थानवर्ती अयोगकेवली कहते हैं।
भावार्थ—आगम में शील के जितने भेद या विकल्प कहे हैं उन सबकी पूर्णता यहीं पर होती है इसलिये वह शील का स्वामी है और पूर्ण संवर तथा निर्जरा का सर्वोत्कृष्ट एवं अंतिम पात्र होने से मुक्तावस्था के सम्मुख है। काययोग से भी वह रहित हो चुका है। इस तरह के जीव को ही चौदहवें गुणस्थान वाला अयोगकेवली कहते हैं।
सिद्धों का लक्षण
अट्ठविहकम्मवियला, सीदीभूदा णिरंजणा णिच्चा।
अट्ठगुणा किदकिच्चा, लोयग्गणिवासिणो सिद्धा।।२६।।
अष्टविधकर्मविकला: शीतीभूता निरंजना नित्या:।
अष्टगुणा कृतकृत्या लोकाग्रनिवासिन: सिद्धा:।।२६।।
अर्थ—जो ज्ञानावरणादि अष्ट कर्मों से रहित हैं, अनंतसुखरूपी अमृत के अनुभव करने वाले शांतिमय हैं, नवीन कर्मबंध के कारणभूत मिथ्यादर्शनादि भावकर्मरूपी अंजन से रहित हैं, सम्यक्त्व, ज्ञान, दर्शन, वीर्य, अव्याबाध, अवगाहन, सूक्ष्मत्व, अगुरुलघु ये आठ मुख्य गुण जिनके प्रकट हो चुके हैं, कृतकृत्य हैं—जिनको कोई कार्य करना बाकी नहीं रहा है, लोक के अग्रभाग में निवास करने वाले हैं, उनको सिद्ध कहते हैं।
भावार्थ—संसारावस्था का विनाश हो जाने पर भी आत्मद्रव्य का विनाश नहीं होता, उसका अस्तित्व रहता है किन्तु वह अस्तित्व किस रूप में रहता है यह इस गाथा के द्वारा बताया गया है।
गुणस्थानसार
इन बीस प्ररूपणाओं द्वारा अथवा इन बीस प्रकरणों का आश्रय लेकर यहाँ जीवद्रव्य का प्ररूपण किया जाता है। ‘‘जीवट्ठाण’’ नामक सिद्धांतशास्त्र में अशुद्ध जीव के १४ गुणस्थान, १४ मार्गणा और १४ जीवसमास स्थानों का जो वर्णन है वही इसका आधार है। संक्षेप रुचि वाले शिष्यों की अपेक्षा से इन बीस प्ररूपणाओं का गुणस्थान और मार्गणा इन दो ही प्ररूपणाओं में अंतर्भाव हो जाता है अतएव संग्रहनय से दो ही प्ररूपणा हैं अर्थात् गुणस्थान यह एक प्ररूपणा हुई और चौदह मार्गणाओं में जीवसमास, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा और उपयोग इन पाँचों प्ररूपणाओं का अंतर्भाव हो जाता है। जैसे— इंद्रिय मार्गणा और कायमार्गणा में जीवसमास गर्भित हो जाते हैं इत्यादि। इसलिये अभेद विवक्षा से गुणस्थान और मार्गणा ये दो ही प्ररूपणा हैं किन्तु भेद विवक्षा से बीस प्ररूपणाएँ होती हैं।
‘‘संक्षेप’’ और ‘‘ओघ’’ ये गुणस्थान के पर्यायवाची नाम हैं तथा ‘‘विस्तार’’ और ‘‘आदेश’’ ये मार्गणा के पर्यायवाची नाम हैं। मोह तथा योग के निमित्त से होने वाले आत्मा के परिणामों का नाम गुणस्थान है और अपने-अपने कर्म के उदय से होने वाली मार्गणाएं हैं।
गुणस्थान का सामान्य लक्षण—दर्शनमोहनीय आदि कर्मों की उदय, उपशम, क्षय, क्षयोपशम आदि अवस्था के होने पर होने वाले जीव के परिणाम गुणस्थान कहलाते हैं।
गुणस्थान के १४ भेद हैं। उनके नाम—मिथ्यात्व, सासादन, मिश्र, अविरतसम्यग्दृष्टि, देशविरत, प्रमत्तविरत, अप्रमत्तविरत, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, सूक्ष्मसांपराय, उपशांतमोह, क्षीणमोह, सयोगकेवली और अयोगकेवली।
गुणस्थानों का संक्षिप्त लक्षण—
१. मिथ्यात्व के उदय से होने वाले तत्वार्थ के अश्रद्धान को मिथ्यात्व कहते हैं। इसके पाँच भेद हैं—एकांत, विपरीत, विनय, संशय और अज्ञान अथवा गृहीत और अगृहीत के भेद से मिथ्यात्व के दो भेद भी होते हैं। इन्हीं में संशय को मिला देने से तीन भेद भी हो जाते हैं। विशेष रूप से ३६३ भेद होते हैं यथा—क्रियावादियों के १८०, अक्रियावादियों के ८४, अज्ञानवादियों के ६७ और वैनयिकवादियों के ३२, मिथ्यादृष्टि जीव के परिणामों की अपेक्षा विस्तार से मिथ्यात्व के असंख्यात लोकप्रमाण तक भेद हो जाते हैं।
मिथ्यादृष्टि जीव को सच्चा धर्म नहीं रुचता है। वह सच्चे गुरुओं के उपदेश का श्रद्धान नहीं करता है किन्तु आचार्याभासों से उपदिष्ट वचनों का श्रद्धान कर लेता है। इस गुणस्थान का काल संख्यात, असंख्यात या अनंत भव होता है।
२. उपशम सम्यक्त्व का जघन्य और उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त है। किसी सम्यग्दृष्टि के इस अंतर्मुहूर्त काल में से जब जघन्य एक समय तथा उत्कृष्ट छ: आवली प्रमाण काल शेष रहे और उसी काल में अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ में से किसी एक के उदय आ जाने से सम्यक्त्व की विराधना होने पर जो अव्यक्तरूप अतत्व श्रद्धान की परिणति है उसे सासादन गुणस्थान कहते हैं। इसका काल अति अल्प होने से हम और आप के द्वारा जाना नहीं जाता है। यह जीव सम्यक्त्वरूपी रत्नपर्वत से गिरा और मिथ्यात्वरूपी भूमि पर नहीं पहुँचा, मध्य के काल का नाम सासादन है। इसका काल जघन्य एक समय और उत्कृष्ट ६ आवली मात्र है।
३. दर्शनमोहनीय की सम्यक्त्वमिथ्यात्व नामक प्रकृति के उदय से सम्यक्त्व या मिथ्यात्वरूप परिणाम न होकर जो मिश्र परिणाम होते हैं, उसे मिश्र गुणस्थान कहते हैं। जैसे—दही और गुड़ के मिश्रण का स्वाद मिश्ररूप है वैसे ही यहाँ मिश्र श्रद्धान है। इस गुणस्थान में संयम, देशव्रत और मारणांतिक समुद्घात नहीं होता है तथा मृत्यु भी नहीं है। पहले जिस गुणस्थान में आयु बाँधी थी, उसी गुणस्थान में जाकर मरण करता है। इस गुणस्थान का काल अंतर्मुहूर्त मात्र है।
४. अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व और सम्यक्त्व प्रकृति इन सात प्रकृतियों के उपशम से उपशम सम्यक्त्व, क्षय से क्षायिक सम्यक्त्व एवं सम्यक्त्व प्रकृति के उदय से वेदक सम्यक्त्व होता है। इस वेदक सम्यक्त्व में चल, मलिन और अगाढ़ दोष होते रहते हैं। यह सम्यक्त्व भी नित्य ही अर्थात् जघन्य अंतर्मुहूर्त से लेकर उत्कृष्ट छ्यासठ सागर पर्यंत कर्मों की निर्जरा का कारण है। शंका आदि पच्चीस मल दोषों को दूर करने वाला सम्यग्दृष्टि जिनेन्द्र भगवान के वचनों पर श्रद्धान करता है। कदाचित् अज्ञानी आदि गुरु के वचनों को अर्हंत के वचन समझकर श्रद्धान कर लेता है फिर भी सम्यग्दृष्टि है। यदि पुन: किसी गुरु ने उसे सूत्रादि ग्रंथ दिखाकर कहा कि यह गलत है और वह हठ को नहीं छोड़ता है तो उसी समय से वह मिथ्यादृष्टि बन जाता है। यह जीव इंद्रियों के विषयों से, त्रस-स्थावर कीहिंसा से विरत नहीं है फिर भी अनर्गल रूप से इंद्रिय विषयों का सेवन या हिंसादि कार्य नहीं कर सकता है अत: जिनेन्द्र भगवान के वचनों पर श्रद्धान करने से अविरत सम्यग्दृष्टि कहलाता है। उपशमसम्यक्त्व का जघन्य एवं उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त है। वेदक का जघन्य अंतर्मुहूर्त एवं उत्कृष्ट छ्यासठ सागर प्रमाण है और क्षायिक का अनंतकाल है। यह सम्यक्त्व केवली या श्रुतकेवली के पादमूल में ही होता है और तीन या चार भव में जीवों को मोक्ष पहुँचाकर वहाँ शाश्वत विद्यमान रहता है।
५. यहाँ पर प्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय रहने से पूर्ण संयम नहीं होता किन्तु अप्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय रहने से एक देशव्रत होते हैं अत: इस पंचम गुणस्थान का नाम देशसंयम है। इसमें त्रसवध से विरति और स्थावर वध से अविरति ऐसे विरताविरत परिणाम एक समय में रहते हैं अत: यह संयमासंयम गुणस्थान है। इसका उत्कृष्ट काल कुछ अधिक आठ वर्ष कम एक कोटि पूर्व वर्ष प्रमाण है।
६. यहाँ सकल संयम घातक प्रत्याख्यानावरण कषाय के क्षयोपशम से पूर्ण संयम हो चुका है किन्तु संज्वलन और नोकषाय के उदय से मल को उत्पन्न करने वाले प्रमाद के होने से इसे प्रमत्तविरत कहते हैं। यह साधु सम्पूर्ण मूलगुण और शीलों से सहित, व्यक्त, अव्यक्त प्रमाद के निमित्त से चित्रल आचरण वाला होता है। स्त्रीकथा, भक्तकथा, राष्ट्रकथा, अवनिपालकथा, ४ कषाय, पंचेन्द्रिय विषय, निद्रा और स्नेह ये १५ प्रमाद हैं। इन्हें परस्पर में गुणा करने से प्रमाद के ८० भेद हो जाते हैं।
यथा—४x४x५x१x१=८०
७. संज्वलन और नोकषाय के मंद उदय से सकल संयमी मुनि के प्रमाद नहीं है अत: ये अप्रमत्तविरत कहलाते हैं। इसके दो भेद हैं—स्वस्थान अप्रमत्त, सातिशय अप्रमत्त। जब तक चारित्र मोहनीय की २१ प्रकृतियों का उपशमन, क्षपण कार्य नहीं है किन्तु ध्यानावस्था है तब तक स्वस्थान अप्रमत्त हैं। जब २१ प्रकृतियों का उपशमन या क्षपण करने के लिए मुनि होते हैं तब वे सातिशय अप्रमत्त कहलाते हैं। ये श्रेणी चढ़ने के सम्मुख होते हैं। इस गुणस्थान का काल अंतर्मुहूर्त है। चारित्र मोहनीय की २१ प्रकृतियों का उपशम या क्षय करने के लिए तीन प्रकार के विशुद्ध परिणाम होते हैं—अध:करण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण। करण नाम परिणामों का है। ये सातिशय अप्रमत्त मुनि अध:प्रवृत्तकरण को करते हैं।
८. अध:प्रवृत्तकरण में अंतर्मुहूर्त रहकर ये मुनि प्रतिसमय अनंतगुणी विशुद्धि को प्राप्त होते हुए एवं पूर्व में कभी भी नहीं प्राप्त हुए ऐसे अपूर्वकरण जाति के परिणामों को प्राप्त होते हैं। यहाँ पर एक समयवर्ती मुनियों के परिणामों में सदृशता और विसदृशता दोनों ही होती है। इसका काल भी अंतर्मुहूर्त है।
९. अनिवृत्तिकरण गुणस्थान में ध्यान में स्थित एक समयवर्ती अनेकों मुनियों के परिणामों में होने वाली विशुद्धि में परस्पर में निवृत्ति अर्थात् भेद नहीं पाया जाता है इसलिये इसे अनिवृत्तिकरण कहते हैं। इसका काल भी अंतर्मुहूर्त है।
१०. उपशमक या क्षपक मुनि सूक्ष्मलोभ का अनुभव करते हुए सूक्ष्मसांपराय कहलाते हैं। यहाँ यथाख्यातचारित्र से किंचिन्न्यून अवस्था रहती है।
११. इस गुणस्थान में मोहनीय कर्म की सम्पूर्ण प्रकृतियों का उपशम हो जाने से परिणाम पूर्णतया निर्मल हो जाते हैं और यथाख्यात चारित्र प्रगट हो जाता है अतएव यहाँ उपशांत वीतरागछद्मस्थ कहलाते हैं।
१२. मोहनीय कर्म के सर्वथा नष्ट हो जाने से क्षीणकषाय मुनि निर्ग्रन्थ वीतराग कहलाते हैं।
भावार्थ—सातिशय अप्रमत्त गुणस्थान वाले कोई मुनि उपशम श्रेणी में चढ़ते हुये २१ प्रकृतियों को उपशम करते हुए आठवें, नवमें, दशवें और ग्यारहवें तक जाते हैं वहाँ से गुणस्थान का अंतर्मुहूर्त काल पूर्ण कर नियम से नीचे गिरते हैं क्योंकि उपशम की गई २१ कषाय प्रकृतियों में से किसी का उदय आ जाता है अथवा मरण हो जाता है। जो मुनि २१ प्रकृतियों का नाश करते हुये क्षपक श्रेणी पर चढ़ते हैं वे नियम से ग्यारहवें में न जाकर बारहवें में जाते हैं और वहाँ अंत समय में ज्ञानावरणादि का नाश कर केवली बन जाते हैं।
१३. यहाँ तेरहवें गुणस्थान में केवलज्ञान प्रगट हो जाता है और क्षायिक भावरूप नवकेवललब्धियाँ प्रकट हो जाती हैं। ये परमात्मा अर्हंत परमेष्ठी कहलाते हैं। कुछ अधिक आठ वर्ष कम एक कोटिपूर्व वर्ष तक इस गुणस्थान में केवली भगवान रह सकते हैं ।
१४. सयोगकेवली योग निरोध कर चौदहवें गुणस्थान में अयोगी-केवली कहलाते हैं।
पहले, दूसरे, तीसरे गुणस्थान तक बहिरात्मा, चौथे से बारहवें तक अंतरात्मा एवं तेरहवें, चौदहवें में परमात्मा कहलाते हैं।
आयु कर्म के बिना शेष सात कर्मों की गुणश्रेणी निर्जरा का क्रम—सातिशयमिथ्यादृष्टि, सम्यग्दृष्टि, श्रावक, विरत, अनंतानुबंधी के विसंयोजक, दर्शनमोह के क्षपक, कषायों के उपशामक, उपशांत कषाय, कषायों के क्षपक, क्षीणमोह, सयोगी और अयोगी इन ग्यारह स्थानों में कर्मों की निर्जरा क्रम से असंख्यातगुणी-असंख्यातगुणी अधिक-अधिक होती जाती है।
चौदहवें गुणस्थान के अंत में सम्पूर्ण कर्मों से रहित होकर सिद्ध परमेष्ठी हो जाते हैं। वे नित्य, निरंजन, अष्टगुण सहित, कृतकृत्य हैं और लोक के अग्रभाग में विराजमान हो जाते हैं। आत्मा से सम्पूर्ण कर्मों का छूट जाना ही मोक्ष है। ये सिद्ध परमेष्ठी गुणस्थानातीत कहलाते हैं।
इनमें अविरत सम्यग्दृष्टि चतुर्थ गुणस्थानवर्ती, पहली प्रतिमा से लेकर ग्यारहवीं प्रतिमा तक अणुव्रतों का पालन करने वाले देशव्रती पंचमगुणस्थानवर्ती एवं सर्व आरंभ-परिग्रह त्यागी मुनिराज महाव्रती षष्ठ गुणस्थानवर्ती होते हैं।
