कायमार्गणा
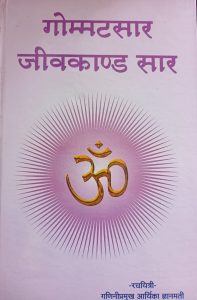
(अष्टम अधिकार)
काय का स्वरूप
जाईअविणाभावी, तसथावरउदयजो हवे काओ।
सो जिणमदम्हि भणिओ, पुढवीकायादिछब्भेयो।।५९।।
जात्यविनाभावित्रसस्थावरोदयजो भवेत् काय:।
स जिनमते भणित: पृथ्वीकायादिषड्भेद:।।५९।।
अर्थ—जाति नाम कर्म के अविनाभावी त्रस और स्थावर नामकर्म के उदय से होने वाली आत्मा की पर्याय को जिनमत में काय कहते हैं। इसके छह भेद हैं—पृथिवी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति और त्रस।
भावार्थ यद्यपि काय शब्द का अर्थ शरीर होता है और निरुक्ति के अनुसार यह अर्थ भी संगत है। फिर भी यहाँ यह निरुक्तार्थ गौण एवं उपचरित है, मुख्य नहीं है। इसीलिये आचार्य ने काय का लक्षण बताते हुए यहाँ पर इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि मार्गणा के प्रकरण में काय का अर्थ जाति नाम कर्म के उदय से अविनाभावी त्रस एवं स्थावर नाम कर्म के उदय होने से होने वाली जीव की पर्याय विशेष है। शरीर नाम कर्म के उदय से होने वाला कार्य यहाँ पर काय शब्द से अभीष्ट नहीं है। इस तरह के शरीर में स्थित जीव की पर्याय ही वास्तव में काय शब्द से यहाँ अभिप्रेत है। यदि निरुक्ति अर्थ को शरीर रूप मुख्य माना जायेगा तो आगम के अनेक विषय विसंगत हो जाएंगे। वायुकायिक आदि को स्थावर नहीं कहा जा सकेगा, क्योंकि वे स्थानशील नहीं है—सदा ही चलते रहते हैंं तथा सब स्थावरों को भी त्रस कहा जा सकेगा, क्योंकि वे भी उद्वेग को प्राप्त हैं, इत्यादि।
सामान्यतया जाति नामकर्म के एकेन्द्रिय से लेकर पंचेन्द्रिय तक पाँच भेद होते हैं। फिर भी इनके त्रस और स्थावर नाम कर्म के उदय के संबंध से दो भेद किये गये हैं—एकेन्द्रिय और द्वीन्द्रिय से लेकर पंचेन्द्रिय तक। जिन जीवों के एकेन्द्रिय जाति नामकर्म का उदय पाया जाता है उनके स्थावर नामकर्म का भी उदय हुआ करता है और जिनके द्वीन्द्रिय से लेकर पंचेन्द्रिय तक की किसी भी जाति का उदय होता है उनके त्रस नामकर्म का उदय हुआ करता है क्योंकि त्रस स्थावर कर्मों का उदय जाति का अविनाभावी—उससे अविरुद्ध बताया गया है। जिस तरह गति से अविरुद्ध जाति कर्म का उदय हुआ करता है। उसी प्रकार जाति से अविरुद्ध—अविनाभावी स्थावर और त्रस नामकर्मों का उदय हुआ करता है। शरीर कर्म के उदय से आगत नोकर्मवर्गणाओं की रचना इन्हीं जात्यविनाभावी त्रस या स्थावर नामकर्म के उदय के अनुसार हुआ करती है। ऐसा नहीं है कि शरीर के अनुसार इन जीव विपाकी जात्यादि कर्मों का उदय होता हो। जैसा कि गाथा के पूर्वार्ध से विदित होता है तथा देखा जाता है कि विग्रह गति में शरीर के उदय और कार्य के पूर्व त्रस-स्थावर कर्मोदय के अनुसार जीव की वह पर्याय और संज्ञाभिधान माना गया है। अतएव यहाँ पर काय से शरीर का ग्रहण करके कोई भ्रम में न पड़े इसीलिए जीव विपाकी कर्मों के उदय से जन्य जीव-पर्याय रूप काय का लक्षण ग्रंथकारों ने स्पष्टतया बता दिया है।
पृथ्वी आदि चार स्थावर का स्वरूप
पुढवी आऊ तेऊ, वाऊ कम्मोदयेण तत्थेव।
णियवण्णचउक्कजुदो, ताणं देहो हवे णियमा।।६०।।
पृथिव्यप्तेजोवायुकर्मोदयेन तत्रैव।
निजवर्णचतुष्कयुतस्तेषां देहो भवेन्नियमात्।।६०।।
अर्थ—पृथ्वी, अप्—जल, तेज—अग्नि, वायु, इनका शरीर नियम से अपने-अपने पृथ्वी आदि नामकर्म के उदय से अपने-अपने योग्य रूप, रस, गंध, स्पर्श से युक्त पृथ्वी आदिक में बनता है।
भावार्थ —पृथ्वी आदि नामकर्म के उदय से पृथ्वीकायिक आदि जीवों के अपने-अपने योग्य रूप, रस, गंध, स्पर्श से युक्त पृथ्वी आदि पुद्गलस्कंध शरीर रूप परिणत हो जाते हैं अर्थात् शरीर योग्य प्राप्त नोकर्मवर्गणाओं का परिणाम और रचना जात्यविनाभावी स्थावर या त्रस नामकर्म एवं उनके अवान्तर भेदरूप जीव विपाकी कर्म के उदय के अनुरूप हुआ करती है।
शरीर के भेद और उनके लक्षण
बादरसुहुमुदयेण य, बादरसुहुमा हवन्ति तद्देहा।
घादसरीरं थूलं, अघाददेहं हवे सुहुमं।।६१।।
बादरसूक्ष्मोदयेन च बादरसूक्ष्मा भवन्ति तद्देहा:।
घातशरीरं स्थूलमघातदेहं भवेत् सूक्ष्मम्।।६१।।
अर्थ—बादरनामकर्म के उदय से बादर और सूक्ष्म नामकर्म के उदय से सूक्ष्म शरीर हुआ करता है। जो शरीर दूसरे को रोकने वाला हो अथवा जो स्वयं दूसरे से रुके उसको बादर—स्थूल कहते हैं और जो दूसरे को न तो रोके और न स्वयं दूसरे से रुके उसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं।
भावार्थ —नामकर्म के भेदों में जाति, स्थावर, त्रस ये तीन भेद जिस तरह जीव विपाकी कर्मों के भेद हैं, जो कि काय की उत्पत्ति या व्यपदेश में मुख्य अन्तरंग कारण हैं। उसी प्रकार शरीर के दो प्रकार बादर और सूक्ष्म होने में भी नामकर्म के दो जीवविपाकी ही कर्म-बादर और सूक्ष्म कारण हैं। जो जीव बादर नामकर्म के उदय से युक्त हैं उनके शरीर नामकर्म के उदय से संचित नोकर्म वर्गणाओं की बादर शरीर रूप रचना हुआ करती है और जो जीव सूक्ष्म नामकर्म के उदय से युक्त हैं उनके शरीर नाम कर्म के उदय से प्राप्त शरीर योग्य नोकर्मवर्गणाओं से सूक्ष्म शरीर का परिणमन हुआ करता है। अतएव आशय इस प्रकार समझना चाहिए कि जिनका शरीर बादर है वे बादर जीव हैं और जिनका शरीर सूक्ष्म है वे जीव सूक्ष्म हैं क्योंकि कार्य कारण का ज्ञापक हुआ करता है।
वनस्पतिकाय का स्वरूप और उसके भेद
उदये दु वणप्फदिकम्मस्स य जीवा वणप्फदी होंति।
पत्तेयं सामण्णं, पदिट्ठिदिदरेत्ति पत्तेयं।।६२।।
उदये तु वनस्पतिकर्मणश्च जीवा वनस्पतयो भवन्ति।
प्रत्येकं सामान्यं प्रतिष्ठितेतरे इति प्रत्येकम्।।६२।।
अर्थ—स्थावर नामकर्म का अवान्तर विशेष भेद जो वनस्पति नामकर्म है उसके उदय से जीव वनस्पति होते हैं। उनके दो भेद हैं—एक प्रत्येक दूसरा साधारण। प्रत्येक के भी दो भेद हैं—प्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित।
भावार्थ —जो एक ही जीव प्रत्येक वनस्पति नामकर्म के उदय से युक्त होकर पूरे एक शरीर का मालिक हो उस जीव को प्रत्येक वनस्पति कहते हैं। जिस एक ही शरीर में अनेक जीव समानरूप से रहें उस शरीर को साधारण शरीर कहते हैं और इस तरह के साधारण शरीर के धारण करने वाले उन जीवों को साधारण वनस्पति जीव कहते हैं क्योंकि इनके साधारण-वनस्पति नामकर्म का उदय पाया जाता है। प्रत्येक वनस्पति के भी दो भेद हैं—एक प्रतिष्ठित दूसरा अप्रतिष्ठित। प्रतिष्ठित प्रत्येक उसको कहते हैं कि जिस एक ही जीव के उस विवक्षित शरीर में मुख्य रूप से व्यापक होकर रहने पर भी उसके आश्रय से दूसरे अनेक निगोदिया जीव भी रहें किन्तु जहाँ पर यह बात नहीं है, एक जीव के मुख्यतया रहते हुए भी उसके आश्रय से दूसरे निगोदिया जीव नहीं रहते उनको अप्रतिष्ठित प्रत्येक कहते हैं।
वनस्पति जीवों के अवान्तर भेद
मूलग्गपोरबीजा,कंदा तह खंदबीज बीजरुहा।
सम्मुच्छिमा य भणिया, पत्तेयाणंतकाया य।।६३।।
मूलाग्रपर्वबीजा, कन्दास्तथा स्कन्धबीजबीजरुहा:।
सम्मूर्छिमाश्च भणिता: प्रत्येकानंतकायाश्च।।६३।।
अर्थ—जिन वनस्पतियों का बीज, मूल, अग्र, पर्व, कंद अथवा स्कंध है अथवा जो बीज से उत्पन्न होती हैं यद्वा जो सम्मूच्र्छन हैं वे सभी वनस्पतियाँ सप्रतिष्ठित तथा अप्रतिष्ठित दोनों प्रकार की होती हैं।
भावार्थ —वनस्पति अनेक प्रकार की होती हैं। कोई तो मूल से उत्पन्न होती हैं, जैसे—अदरख, हल्दी आदि। कोई अग्र से उत्पन्न होती हैं, जैसे— गुलाब, उदीची आदि। कोई पर्व-पंगोली से उत्पन्न होती हैं, जैसे—ईख, बेंत आदि। कोई कंद से उत्पन्न होती हैं, जैसे—पिंडालू, सूरण आदि। कोर्ई स्कंध से उत्पन्न होती हैं, जैसे—सल्लकी, कटकी, पलाश, ढाक आदि। कोई अपने-अपने बीज से उत्पन्न होती हैं, जैसे—गेहूूँ, चना, धान आदि। कोई सम्मूर्च्छन-मिट्टी जल आदि के संबंध से ही उत्पन्न हो जाती हैं, जैसे—घास आदि। ये सब ही वनस्पति सप्रतिष्ठित प्रत्येक और अप्रतिष्ठित प्रत्येक इस तरह दोनों प्रकार की हुआ करती हैं
यह बात भी ध्यान में रहनी चाहिए कि यहाँ पर बताए गए वनस्पति के भेदों में एक भेद सम्मूर्च्छन भी बताया है वह वनस्पति के अनेक कारणजन्य प्रकारों में से एक प्रकार है। जिसका आशय इतना ही है कि उसकी उत्पत्ति का कोई बीज निश्चित नहीं है। जैसा कि अन्य वनस्पतियों के मूल आदि निश्चित हैं। जन्म के तीन (सम्मूर्च्छन, गर्भ, उपपाद) प्रकारों में से एक सम्मूर्च्छन भेद है। वह तो एकेन्द्रिय जीवों से लेकर संसारी जीवों में चतुरिन्द्रिय तक सभी जीवों का तथा किन्हीं-किन्हीं पंचेन्द्रिय जीवों का भी हुआ करता है। दोनों ही सम्मूर्च्छन में सामान्य विशेष का अंतर है। सम्मूर्च्छन जन्म सामान्य है और यह भेद विशेष है।
सप्रतिष्ठित प्रत्येक और अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति की पहचान
गूढसिरसंधिपव्वं, समभंगमहीरुहं च छिण्णरुहं।
साहारणं सरीरं, तव्विवरीयं च पत्तेयं।।६४।।
गूढशिरासन्धिपर्वं समभंगमहीरुकं च छिन्नरुहम्।
साधारणं शरीरं तद्विपरीतं च प्रत्येकम्।।६४।।
अर्थ—जिनकी शिरा—बहि:स्नायु, सन्धि—रेखाबंध और पर्व—गाँठ अप्रकट हों और जिसका भंग करने पर समान भंग हो और दोनों भंगों में परस्पर हीरुक—अन्तर्गत सूत्र—तन्तु न लगा रहे तथा छेदन करने पर भी जिसकी पुन: वृद्धि हो जाए उनको सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति कहते हैं। और जो विपरीत हैं—इन चिन्हों से रहित हैं वे सब अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति कही गयी हैं।
भावार्थ —यद्यपि वनस्पति के जो दो भेद गिनाये हैं उनमें प्रत्येक से साधारण भेद भिन्न ही है। परन्तु यहाँ पर साधारण जीवों से आश्रित होने के कारण उपचार से ताल, नालिकेर, तिंतिणीक आदि प्रत्येक वनस्पति के भेदों को भी साधारण शब्द से कह दिया है।
साधारण जीवों का स्वरूप
साहारणमाहारो, साहारणमाणपाणगहणं च।
साहारणजीवाणं, साहारणलक्खणं भणियं।।६५।।
साधारणमाहार: साधारणमानपानग्रहणं च।
साधारणजीवानां साधारणलक्षणं भणितम्।।६५।।
अर्थ—इन साधारण जीवों का साधारण अर्थात् समान ही तो आहार होता है और साधारण—समान अर्थात् एक साथ ही श्वासोच्छ्वास का ग्रहण होता है। इस तरह से साधारण जीवों का लक्षण परमागम में साधारण ही बताया है।
भावार्थ —साथ ही उत्पन्न होेने वाले जिन अनंतानंत साधारण जीवों की आहारादि पर्याप्ति और उनके कार्य सदृश तथा समान काल में होते हों उनको साधारण जीव कहते हैं।
जत्थेक्क मरइ जीवो, तत्थ दु मरणं हवे अणंताणं।
वक्कमइ जत्थ एक्को, वक्कमणं तत्थ णंताणं।।६६।।
यत्रैको म्रियते जीवस्तत्र तु मरणं भवेदनन्तानाम्।
प्रक्रामति यत्र एक: प्रक्रमणं तत्रानन्तानाम्।।६६।।
अर्थ—साधारण जीवों में जहाँ पर एक जीव मरण करता है वहाँ पर अनंत जीवों का मरण होता है और जहाँ पर एक जीव उत्पन्न होता है वहाँ अनंत जीवों का उत्पाद होता है।
भावार्थ —साधारण जीवों में उत्पत्ति और मरण की अपेक्षा भी सादृश्य है। प्रथम समय मेंं उत्पन्न होने वाले साधारण जीवों की तरह द्वितीयादि समयों में भी उत्पन्न होने वाले साधारण जीवों का जन्म-मरण साथ ही होता है। यहाँ इतना विशेष समझना कि एक बादर निगोद शरीर में या सूक्ष्म निगोद शरीर में साथ ही उत्पन्न होने वाले अनंतानंत साधारण जीव या तो पर्याप्तक ही होते हैं या अपर्याप्तक ही होते हैं किन्तु मिश्ररूप नहीं होते क्योंकि उनके समान कर्मोदय का नियम है।
एक निगोद शरीर में जीव कितने हैं
एगणिगोदसरीरे, जीवा दव्वप्पमाणदो दिट्ठा।
सिद्धेहिं अणंतगुणा, सव्वेण विदीदकालेण।।६७।।
एकनिगोदशरीरे जीवा द्रव्यप्रमाणतो दृष्टा:।
सिद्धैरनन्तगुणा: सर्वेण व्यतीतकालेन।।६७।।
अर्थ—समस्त सिद्ध राशि का और सम्पूर्ण अतीत काल के समयों का जितना प्रमाण है द्रव्य की अपेक्षा से उनसे अनंतगुणे जीव एक निगोद शरीर में होते हैं।
भावार्थ —यहाँ पर काल के आश्रय से एक शरीर में पाये जाने वाले जीवों की संख्या बताई गई है। क्षेत्र तथा भाव की अपेक्षा से उनकी संख्या आगम के अनुसार जानी जा सकती है।
नित्यनिगोद का स्वरूप
अत्थि अणंता जीवा, जेिंह ण पत्तो तसाण परिणामो।
भावकलंकसुपउरा, णिगोदवासं ण मुंचंति।।६८।।
सन्ति अनंता जीवा यैर्न प्राप्त: त्रसानां परिणाम:।
भावकलंकसुप्रचुरा निगोदवासं न मुंचन्ति।।६८।।
अर्थ—ऐसे अनंतानंत जीव हैं कि जिन्होेेंने त्रसों की पर्याय अभी तक कभी भी नहीं पाई है और जो निगोद अवस्था में होने वाले दुर्लेश्यारूप परिणामों से अत्यंत अभिभूत रहने के कारण निगोदस्थान को कभी नहीं छोड़ते।
भावार्थ —निगोद के दो भेद हैं—एक नित्य निगोद दूसरा चतुर्गति निगोद। जिसने कभी त्रस पर्याय को प्राप्त कर लिया हो उसको चतुर्गति निगोद कहते हैं और जिसने अभी तक कभी भी त्रस पर्याय को न पाया हो अथवा जो भविष्य में भी कभी त्रस पर्याय को नहीं पावेगा उसको नित्यनिगोद कहते हैं, क्योंकि नित्य शब्द के दोनों ही अर्थ होते हैं एक तो अनादि दूसरा अनादि अनंत। इन दोनों ही प्रकार के जीवों की संख्या अनंतानंत है।
गाथा में आया हुआ ‘प्रचुर’ शब्द प्राय: अथवा आभीक्ष्ण्य अर्थ को सूचित करता है। अतएव छह महीना आठ समय में छह सौ आठ जीवों के उसमें से निकल कर मोक्ष को चले जाने पर भी कोई बाधा नहीं आती।
निगोदिया से रहित कौन हैं ?
पुढवीआदिचउण्हं, केवलिआहारदेवणिरयंगा।
अपदिट्ठिदा णिगोदेहिं पदिट्ठिदंगा हवे सेसा।।६९।।
पृथिव्यादिचतुर्णा केवल्याहारदेवनिरयांगानि।
अप्रतिष्ठितानि निगोदै: प्रतिष्ठितांगा भवन्ति शेषा:।।६९।।
अर्थ—पृथ्वी, जल, अग्नि और वायुकायिक जीवों का शरीर तथा केवलियों का शरीर, आहारकशरीर और देव-नारकियों का शरीर बादर निगोदिया जीवों से अप्रतिष्ठित है। शेष वनस्पतिकाय के जीवों का शरीर तथा द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, पंचेन्द्रिय तिर्यंच और मनुष्यों का शरीर निगोदिया जीवों से प्रतिष्ठित है।
स्थावर और त्रस जीवों का आकार
मसुरंबुबिंदुसूई, कलावधयसण्णिहो हवे देहो।
पुढवीआदिचउण्हं, तरुतसकाया अणेयविहा।।७०।।
मसूराम्बुबिंदुसूचीकलापध्वजसन्निभो भवेद्देह:।
प्रथिव्यादिचतुर्णा तरुत्रसकाया अनेकविधा:।।७०।।
अर्थ—मसूर (अन्न विशेष), जल की बिन्दु, सुइयों का समूह तथा ध्वजा इनके सदृश क्रम से पृथ्वी, अप्, तेज, वायुकायिक जीवों का शरीर होता है और वनस्पति तथा त्रसों का शरीर अनेक प्रकार का होता है।
भावार्थ —जिस तरह का मसूरादिक का आकार है उस ही तरह का पृथ्वीकायिकादिक का शरीर होता है किन्तु वनस्पति और त्रसों का शरीर अनियत संस्थान होेने से एक प्रकार का नहीं किन्तु अनेक प्रकार की भिन्न-भिन्न आकृतियों वाला ही हुआ करता है। ध्यान रहे, पृथ्वीकायिकादि के जो दृष्टिगोचर शरीर हैं वे अनेकों जीवों के शरीर के समूहरूप हैं, अतएव उनका नियत संस्थान घनांगुल के असंख्यातवें भाग प्रमाण होने से दिखाई नहीं पड़ता।
कायमार्गणा से रहित सिद्धों का स्वरूप बताते हैं-
जह कंचणमग्गिगयं, मुंचइ किट्टेण कालियाए य।
तह कायबंधमुक्का, अकाइया झाणजोगेण।।७१।।
यथा कंचनमग्निगतं मुच्यते किट्टेन कालिकया च।
तथा कायबन्धमुक्ता अकायिका ध्यानयोगेन।।७१।।
अर्थ—जिस प्रकार मलिन भी सुवर्ण अग्नि के द्वारा सुसंस्कृत होकर बाह्य और अभ्यन्तर दोनों ही प्रकार के मल से रहित हो जाता है उस ही प्रकार ध्यान के द्वारा यह जीव भी शरीर और कर्मबंध दोनों से रहित होकर सिद्ध हो जाता है।
भावार्थ -जिस प्रकार सोलह ताव के द्वारा तपाये हुए सुवर्ण में बाह्य किट्टिका और अभ्यंतर कालिका इन दोनों ही प्रकार के मल का बिल्कुल अभाव हो जाने पर फिर किसी दूसरे मल का संबंध नहीं होता उस ही प्रकार महाव्रत और धर्मध्यानादि से सुसंस्कृत एवं सुतप्त आत्मा में से एक बार शुक्लध्यान रूपी अग्नि के द्वारा बाह्य मल काय और अन्तरंग मल कर्म के संबंध के सर्वथा छूट जाने पर फिर उनका बंध नहीं होता और वे सदा के लिए काय और कर्म से रहित होकर सिद्ध हो जाते हैं। इस तरह से इस गाथा में आचार्य ने कायमार्गणा के वर्णन का वास्तविक प्रयोजन बता दिया है।
काय मार्गणासार
जाति नामकर्म के अविनाभावी त्रस और स्थावर नामकर्म के उदय से आत्मा की जो पर्याय होती है उसे काय कहते हैं। उसके छह भेद हैं—पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति और त्रसकाय।
पृथ्वी आदि नामकर्म के उदय से जीव का पृथ्वी आदि शरीर में जन्म होता है।
पाँच स्थावर काय के बादर और सूक्ष्म की अपेक्षा दो-दो भेद हो जाते हैंं। विशेष यह है कि वनस्पतिकाय के साधारण और प्रत्येक ये दो भेद होते हैं उसमें साधारण के बादर, सूक्ष्म दो भेद होते हैं, प्रत्येक वनस्पति के नहीं होते।
बादर नामकर्म के उदय से होने वाला शरीर बादर है। यह शरीर दूसरे का घात करता है और दूसरे से बाधित होता है।
सूक्ष्म नामकर्म के उदय से होेने वाला शरीर सूक्ष्म है। यह न स्वयं दूसरे से बाधित होता है और न दूसरे का घात करता है। इन दोनों के शरीर की अवगाहना घनांगुल के असंख्यातवें भाग प्रमाण है। इनमें बादर जीव आधार से रहते हैं और सूक्ष्म जीव सर्वत्र तिल में तेल की तरह व्याप्त हैं अर्थात् सारे तीन लोक में भरे हुए हैं, ये अनंतानंत प्रमाण हैं।
वनस्पतिकाय के विशेष भेद
वनस्पतिकाय के दो भेद हैं—प्रत्येक और साधारण।
प्रत्येक के भी दो भेद हैं—सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित।
जिनकी शिरा, संधि और पर्व अप्रगट होें, तोड़ने पर समान भंग हों, तन्तु न लगा रहे, छेदन करने पर भी पुन: वृद्धि हो जावे वे सप्रतिष्ठित वनस्पति हैं। सप्रतिष्ठित वनस्पति के आश्रित अनंत निगोदिया जीव रहते हैं। जिनमें से निगोदिया जीव निकल गये हैं वे वनस्पति अप्रतिष्ठित कहलाती हैं। आलू, अदरक, तुच्छ फल, कोंपल आदि सप्रतिष्ठित हैं। आम, नारियल, ककड़ी आदि अप्रतिष्ठित हैं अर्थात् प्रत्येक वनस्पति का स्वामी एक जीव रहता है किन्तु उसके आश्रित जीवों से सप्रतिष्ठित जीवों का आश्रय न रहने से अप्रतिष्ठित कहलाती है।
साधारण वनस्पति—साधारण नामकर्म के उदय से जिस शरीर के स्वामी अनेक जीव होते हैं उसे साधारण वनस्पति कहते हैं। इन साधारण जीवों का साधारण ही आहार, साधारण ही श्वासोच्छ्वास होता है, इस साधारण शरीर में अनंतानंत जीव रहते हैं। इनमें जहाँ एक जीव मरता है वहाँ अनंतानंत जीवों का मरण हो जाता है और जहाँ एक जीव का जन्म होता है वहाँ अनंतानंत जीवों का जन्म होता है। एक निगोद शरीर में जीव द्रव्य की अपेक्षा सिद्धराशि से अनन्तगुणी हैं और निगोद शरीर की अवगाहना घनांगुल के असंख्यातवें भाग प्रमाण (सुई की नोंक के असंख्यातवें भाग) है।
निगोद के भेद—निगोद के नित्य निगोद और इतर निगोद से दो भेद हैं। जिसने अभी तक त्रस पर्याय नहीं पाई है अथवा भविष्य में भी नहीं पाएंगे वे नित्य निगोद हैं। किन्हीं के मत से अभी तक त्रस पर्याय नहीं पाई है किन्तु आगे पा सकते हैं अत: छह महीने आठ समय में उसमें से ही छह सौ आठ जीव निकलते हैं और यहाँ से इतने ही समय में इतने ही जीव मोक्ष चले जाते हैं। जो निगोद से निकलकर चतुर्गति में घूम पुन: निगोद में गये हैं वे इतर या चतुर्गति निगोद हैं।
त्रस जीव—द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पंचेन्द्रिय जीव त्रस हैं। उपपाद जन्म वाले और मारणांतिक समुद्घात वाले त्रस को छोड़कर बाकी के त्रस जीव त्रस नाली के बाहर नहीं रहते हैं।
किन-किन शरीर में निगोदिया जीव रहते हैं—पृथ्वी, जल, अग्नि, वायुकायिक, केवली, आहारक, देव और नारकियों के शरीर में बादर निगोदिया जीव नहीं रहते हैं। शेष वनस्पतिकायिक, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, पंचेन्द्रिय तिर्यंच और मनुष्यों के शरीर में निगोदिया जीव भरे रहते हैं।
षट्कायिक जीवों का आकार—पृथ्वीकायिक का शरीर मसूर के समान, जलकायिक का जल बिन्दु सदृश, अग्निकायिक जीव का सुइयों के समूह सदृश, वायुकायिक का ध्वजा सदृश होता है। वनस्पति और त्रसों का शरीर अनेक प्रकार का होता है।
जिस प्रकार कोई भारवाही पुरुष कावड़ी के द्वारा भार ढोता है उसी प्रकार यह जीव कायरूपी कावड़ी के द्वारा कर्मभार को ढो रहा है।
यथा मलिन स्वर्ण अग्नि द्वारा सुसंस्कृत होकर बाह्य और अभ्यन्तर दोनों प्रकार के मल से रहित हो जाता है तथैव ध्यान के द्वारा यह जीव भी शरीर और कर्मबंध दोनों मल से रहित होकर सिद्ध हो जाता है।
यद्यपि यह काय मल का बीज और मल की योनि स्वरूप अत्यंत निंद्य है, कृतघ्न सदृश है फिर भी इसी काय से रत्नत्रय रूपी निधि प्राप्त की जा सकती है अत: इस काय को संयम रूपी भूमि में बो करके मोक्ष फल को प्राप्त कर लेना चाहिए। स्वर्गादि अभ्युदय तो भूसे के सदृश स्वयं ही मिल जाते हैं। इसलिये संयम के बिना एक क्षण भी नहीं रहना चाहिए।
