आचार्य श्री के अनुशासन
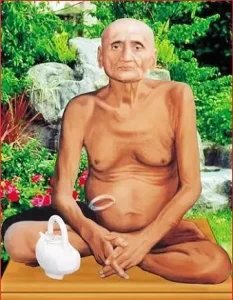
(ज्ञानमती_माताजी_की_आत्मकथा)
दूसरे दिन संघ की एक वृद्धा आर्यिका ने पूछा- ‘‘वीरमती! तुम प्रतिक्रमण करती हो?’’ मैंने कहा-‘‘हाँ माताजी! दोनों समय करती हूँ।’’ उस समय संघ में प्रातःकाल ही प्रतिक्रमण की पद्धति थी, सायंकाल में नहीं होता था।
उन्होंने कहा-‘‘प्रातःकाल ७ बजे मेरे पास प्रतिक्रमण बोलना’’ मैंने प्रातःकाल उन्हीं के पास विधिवत् पूरा प्रतिक्रमण पढ़कर सुना दिया। वे सारा प्रतिक्रमण पाठ मुझे कंठाग्र हुआ देखकर बहुत ही प्रसन्न हुई और आश्चर्य करने लगीं पुनः तीन दिन बाद आचार्य महाराज जी ने उनसे पूछा- ‘‘इस क्षुल्लिका वीरमती की चर्या कैसी है? संघ के अनुकूल है या नहीं?’’ उन माताजी ने कहा-‘‘महाराज जी! इसका ज्ञान बहुत अच्छा है। प्रतिक्रमण पाठ, सारी भक्तियाँ सब कंठाग्र याद हैं।
उच्चारण बहुत शुद्ध है। विनय भी अच्छा करती है। परन्तु ।’’ आचार्यश्री ने पूछा-‘‘परन्तु क्या?’’ माताजी ने कहा-‘‘इसने अपने मन से ही क्षुल्लिका का चिन्ह ऐसा दुपट्टा छोड़ दिया है, आर्यिकाओं के समान करपात्र में आहार करती है तथा चावल के सिवाय सभी अन्न का त्याग कर रखा है। इसकी ये मनचाही-स्वच्छंद प्रवृत्तियाँ ठीक नहीं हैं।’’ मैं पास ही बैठी थी, एकदम सहम गई और मन में सोचने लगी-‘‘भगवन्! यह क्या? यहाँ तो अच्छे को भी बुरा कहा जा रहा है।’’ इतने में आचार्यश्री बहुत ही वात्सल्यपूर्ण शब्दों में बोले- ‘‘बाई ! क्षुल्लिका को कटोरे में या थाली में ही आहार लेना चाहिए तथा उत्तरीय वस्त्र अवश्य होना चाहिए। मैंने हाथ जोड़कर विनम्रता से निवेदन किया- ‘‘महाराज जी! कुछ दिनों पूर्व मैंने क्षुल्लिका विशालमती माताजी से बार-बार आर्यिका दीक्षा लेने की भावना व्यक्त की थी।
उनकी आज्ञा से चारित्रचक्रवर्ती आचार्यश्री के पास प्रार्थना की। आचार्यश्री ने कहा-तुम नेमिसागर, वर्धमानसागर या वीरसागर जी के पास में दीक्षा ले लो अब मैं दीक्षा नहीं देता हूँ। उसके अनंतर मैं उनकी सल्लेखना देखने के लिए उधर ही रह गई। मेरे भावों की अति उत्कटता देखकर मुझे विशालमती अम्मा ने कहा-‘‘तुम करपात्र में आहार लेओ, चूँकि वसुनंदि-श्रावकाचार और चारित्रसार में क्षुल्लक के लिए भी करपात्र में आहार का विधान आया है अतः मैंने अपने गुरु देशभूषण जी महाराज के द्वारा दी गई कटोरी को त्याग दिया और हाथ में ही आहार लेने लगी। उन्हीं के कहने से मैंने दुपट्टा भी छोड़ दिया है।’’ इतना सुनकर पास में बैठी एक-दो आर्यिकाएँ हँसने लगीं परन्तु आचार्यश्री ने गंभीर मुद्रा में कहा-‘‘तुम्हें वापस कटोरी भी लेना होगा और उत्तरीय वस्त्र भी, तभी आर्यिका दीक्षा मिलेगी।’’
इतना कहकर महाराज जी चुप हो गये, चूँकि वे बहुत ही कम बोलते थे पुनः आर्यिकायें बोल पड़ीं- ‘‘महाराज जी! इन्होंने अन्न छोड़ रक्खा है सो यह त्याग संघ में नहीं निभ सकता है।’’ आचार्यश्री ने पूछा-‘‘बाई! तुमने अन्न क्यों त्यागा है?’’ मैंने इस बारे में भी बतला दिया कि- ‘‘कुंथलगिरि में आचार्यदेव की सल्लेखना के बाद त्याग भावना से प्रेरित हो मैंने अन्न त्याग दिया है।’’ आचार्यश्री ने पूछा-‘‘कितने दिन के लिए?’’ मैंने सहसा हड़बड़ा कर कह दिया-‘‘दो वर्ष तक के लिए।’’ आचार्य महाराज कुछ गुस्सा होकर बोले-‘‘यह त्याग बहुत गलत है।
इतने बड़े संघ में श्रावकों के यहाँ तुम्हें फल, दूध आदि भरपेट कैसे मिल सकता है? प्रतिदिन अल्प आहार करके शरीर और संयम की रक्षा कैसे हो सकती है? मैं साधुओं के अन्न त्याग के बारे में पसंद नहीं करता हूँ। श्रावक उनके लिए अलग से खटपट करें। देखो, गेहूँ और दूध साधुओं को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। यह प्रत्येक श्रावकों के घर में सुलभ है। तुम्हें यह मनचाहा त्याग खत्म कर अन्न लेना चाहिए।’’ मैं चुप रही, कुछ देर बाद वहाँ से वापस अपने स्थान पर आ गई।
अब संघ में प्रायः यत्र-तत्र मेरी चर्चा चलने लगी। संघ के ब्रह्मचारी सूरजमल जी ने आकर मुझे समझाना शुरू किया- ‘‘माताजी! अभी आपकी उम्र बहुत छोटी है। आचार्य महाराज जो कुछ कहते हैं, उनकी आज्ञा के अनुसार प्रवृत्ति करो तभी तुम्हें संघ में आर्यिका दीक्षा मिलेगी।……गुरु की आज्ञा से मन से किये गये त्याग को छोड़ने में तुम्हें क्या दोष है? उसके जिम्मेवार तो गुरु ही हैं। यदि गुरु कहें अग्नि में कूद पड़ो तो कूद पड़ना चाहिए। इसी का नाम गुरुभक्ति है।’’
इत्यादि प्रकार से ब्रह्मचारी जी ने समझाया, किन्तु उस समय ये सब कुछ मेरे गले नहीं उतरा। वहीं जयपुर में एक मंदिर में वज्रकीर्ति मुनिराज अपने संघ सहित ठहरे हुए थे। वे गिरनार की यात्रा करने जाने वाले थे। मैं उनके दर्शन करने गई थी। उन्होंने कहा- ‘‘माताजी! तुम मेरे साथ गिरनार यात्रा चलो, मैं तुम्हें आर्यिका दीक्षा देऊँगा।’’
मैंने महाराज जी की सारी चर्या बारीकी से देखी। वे श्रावकों के लिए यज्ञोपवीत लेने के बारे में पक्षपाती नहीं थे। यह बात मुझे खटक गई। मैंने यह कुछ कहा नहीं, मात्र इतना ही कहकर वापस आ गई कि-‘‘महाराज जी! मैं विचार करूँगी।’’ अब इस संघ में मैं लिये गये नियम को छोड़ने के विषय में बहुत ही ऊहापोह में पड़ गई। एक आर्यिका ने कहा-‘‘महाराज जी! इनके पास कु. प्रभावती और सौ. सोनूबाई ये दो शिष्यायें हैं जिनको ये पढ़ाती हैं। वे इन्हीं के पास रहती हैं। यह गलत है इन्हें अपनी दोनों शिष्याओं को संघ में बड़ी माताजी आर्यिका वीरमती जी के पास छोड़ देना चाहिए।’’
दूसरी आर्यिका ने कहा-‘‘इन्होंने ही कु. प्रभावती को दस प्रतिमा के व्रत दिये हैं। सो यह मान्य नहीं है। उसे वापस आचार्य महाराज से सप्तम प्रतिमा के व्रत दिलाने चाहिए। उसे दस प्रतिमा से नीचे उतार देना चाहिए।’’ इस बारे में संघ के ही कुछ साधु वर्ग पक्ष में नहीं थे कि प्रभावती को इनके द्वारा दिये गये व्रतों से नीचे उतार कर आचार्यश्री से पुनः सप्तम प्रतिमा दिलाई जाये। इन सभी संघर्षों के बीच एक दिन मुझे सभी के बीच एक आर्यिका ने अपमानित भी कर दिया किन्तु उस प्रसंग पर एक मुनि, जो कि करुणाशील और प्रौढ़ थे,
वेदी में जाकर रो पड़े और मुझसे बोले- ‘‘माताजी! तुम्हारा धैर्य बहुत ही प्रशंसनीय है जो तुम्हारे अश्रु नहीं आये। इस प्रसंग पर यदि और कोई होता, वह या तो रो पड़ता या हल्ला-गुल्ला मचाने लगता किन्तु आप में सहनशीलता कमाल की है।’’ मैंने कहा-‘‘महाराज जी! मैंने जब घर छोड़ा तब कितने संघर्ष झेले हैं उनके आगे यह सब तो कुछ भी नहीं हैं। मुझे तो आर्यिका दीक्षा लेनी है, बस इतना ही लक्ष्य है। कोई क्या कहते हैं मुझे उस पर इतना विचार नहीं होता। हाँ, आचार्यश्री ने जो कटोरी और दुपट्टा वापस लेने को कहा है और अन्न भी लेने को कहा है।
सो उसमें ही मुझे चिंता हो रही है, क्योंकि त्याग की हुई वस्तु लेना संभव नहीं है। मैं क्या करूँ? सो बुद्धि काम नहीं कर रही है।’’ वैसे वे साधु भी इस पक्ष में नहीं थे कि त्याग किये हुए को ग्रहण कराया जाये, लेकिन वे कर क्या सकते थे? जयपुर के सेठ रामचन्द्र जी कोठारी पहले से ही मेरे परिचित थे तथा जब सन् १९५४ में मैंने आचार्यश्री देशभूषण जी के साथ जयपुर में चातुर्मास किया था तब से पंडित इन्द्रलाल जी शास्त्री निकटता से परिचय में थे अतःइस समय भी ये दोनों महानुभाव मेरे पास आते रहते थे और मैं इन्हीं से समयोचित बातचीत किया करती थी।
इस मेरे त्याग की चर्चा में मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं पुनः कैसे ग्रहण कर लूँ! पंडित इन्द्रलाल जी ने भी अनेक उपायों से मेरे गले उतारने की कोशिश की और कहते रहे कि- ‘‘माताजी! आपको इतने बड़े आचार्य महाराज के कहने पर कटोरी आदि लेने में कोई दोष नहीं है। जो कुछ भी हो आचार्य महाराज स्वयं सोचें, तुम्हें जो कहते हैं सो तुम करो।’’ मेरे प्रति पं. इन्द्रलाल जी, रामचन्द्र जी आदि का सौहार्द भाव बहुत ही विशेष था अतः ये दोनों मेरे बारे में आचार्य महाराज जी से भी प्रार्थना किया करते थे कि- ‘‘महाराज जी! इनकी बुद्धि बहुत ही तीक्ष्ण है।
ये आगम के विषय में बहुत ही दृढ़ हैं। इनका चारित्र बहुत ही उज्ज्वल है। आप इन्हें दीक्षा अवश्य दीजिये। आपके संघ के लिए ये भूषण हैं, रत्न हैं।’’ तब एक दिन आचार्यश्री ने कहा कि-‘‘इनके गुरु देशभूषण जी की अनुमति आये बगैर मैं किसी के शिष्य को कैसे दीक्षा दे सकता हूँ?’’ मैंने कहा-‘‘महाराज जी! उन्होंने अनेक बार कहा था कि आचार्य वीरसागर जी के संघ में ही तुम आर्यिका दीक्षा लेओ, चूंकि वहाँ वयोवृद्ध आर्यिकायें भी हैं और संघ के साधु विहार भी हमारे समान २०-२० मील का नहीं करते हैं तथा ‘गुरूणां गुरु’ चारित्र चक्रवर्ती आचार्यश्री शांतिसागर महाराज जी के ही आदेश से इस समय मैं यहाँ आई हूँ ।’’
फिर भी महाराज जी की आज्ञा से मैंने अपने दीक्षागुरु आचार्य देशभूषण जी के पास आर्यिका दीक्षा की स्वीकृति के लिए पत्र डाल दिया तथा रामचन्द्र जी ने भी पत्र डाल दिया। इसी मध्य एक आर्यिका ने कहा कि- इनके साथ जो बाइयाँ हैं वे अच्छे घराने की हैं या नहीं? कौन जाने? किसके यहाँ से या कहाँ से इन्हें भगाकर ले आई हैं? इनका भी परिचय मालूम करना चाहिए, तभी ये संघ में रह सकती हैं। मैंने उसी समय सेठ रामचन्द्र जी से सोनूबाई के पति लालचन्द्र को और म्हसवड़ के प्रमुख सेठ केवलचन्द्र जी शाह को तथा कु. प्रभावती के भाई शांतिलाल को पत्र लिखा दिया।
उन सभी के संतोषप्रद पत्र आ गये, तब आचार्य महाराज और संघस्थ सभी साधु-साध्वी प्रसन्न हुए। इसके पूर्व भी आचार्यश्री ने इन किन्हीं बातों को महत्त्व नहीं दिया था। वे बराबर प्रारंभ से ही सौ. सोनूबाई से आहार ले रहे थे। उन्होंने मात्र तीन बातों में ही बंधन लगाया था। पुनरपि आचार्यश्री ने मुझे समझाया और कहा- ‘‘बाई! देखो, तुमने अपने गुरु के द्वारा दी गई कटोरी का विशालमती जी के कहने से त्याग कर दिया है तो तुम पुनः कटोरी ग्रहण कर अपने पास मत रखो किन्तु श्रावक के घर में ही उन्हीं की कटोरी लेकर उसमें आहार करके उसे वहीं छोड़कर आ जाओ।
दुपट्टा भी आहार के समय ही ले लो क्योंकि दुपट्टा बगैर आर्यिकाओं की समानता हो जाती है तथा तुमने चावल को तो खुला ही रखा है, उसका मांड लेती हो तो पुनः चावल लेने में कोई हानि नहीं है।’’ इस पर महाराज जी ने एक उदाहरण भी सुनाया, वे बोले- ‘‘एक बार एक सज्जन आये, वे बहुत ही धर्मात्मा, स्वाध्यायी विद्वान् थे। वे मुझसे सप्तम प्रतिमा लेना चाहते थे। दिवस निश्चित हो गया पुनः वे आकर बोले-महाराज जी! मैं प्रतिमा लेने के पूर्व आपसे एकांत में बात करना चाहता हूँ।
मैं उनकी बात समझ गया कि वे क्या कहना चाहते हैं? मैंने पूछा-पंडित जी! यह बताओ कि आप हमें गुरु बनाना चाहते हैं या हमारे गुरु बनना चाहते हैं? पंडित जी समझ गये कि यहाँ कुछ शर्त नहीं चलेगी, अतः उन्होंने मुझसे व्रत नहीं लिया। मुझे भी ऐसे शिष्यों का लोभ नहीं है। वे पंडित जी पंथवाद की शर्त के लिए आये थे कि मैं आपके आम्नाय से न चलकर अपने तेरापंथ आम्नाय के अनुसार ही चलूँगा, ऐसी ही उनकी मनोभावना थी जो कि अन्य शब्दों से स्पष्ट हो चुकी थी।
इसलिए शिष्य वही है जो गुरू को समर्पित हो। इत्यादि।’’ इतना सब सुनकर भी मैं चुप रही, पुनः मंदिर में आकर भगवान् के सामने बैठ गई और सोचने लगी- ‘‘हे भगवन्! अब मैं क्या करूँ? इतने विशाल संघ के नायक आचार्यदेव को गुरू बनाने का लोभ भी नहीं छूट रहा है और उनका अनुशासन भी कठिन प्रतीत हो रहा है।
सोचते-सोचते भगवान् की प्रतिमा को मैं एकटक निहार रही थी और मानों उनसे यह पूछ ही रही थी कि अब क्या करना? प्रभो! आप ही मेरे मन को समाधान दो जिसमें मेरा हित हो, आगम की रक्षा हो, मर्यादा की रक्षा हो और धर्म की रक्षा हो वही उपाय बताओ ।
इतने में ही मेरी अंतरात्मा से यही आवाज उठी कि-‘‘कुछ भी हो जो गुरु कहते हैं वही करना चाहिए। गुण दोष सब उन्हीं के ऊपर छोड़ देना चाहिए। आज लगभग १०-१५ दिन हो गये हैं। अपना मस्तिष्क फटा जा रहा है। अब गुरु की शरण ही सब कुछ है।……’’ इतना सोचकर वेदी से बाहर आई और मंदिर के आंगन में अपने स्वाध्याय की पुस्तक लेकर बैठ गई। इसी मध्य पं. इन्द्रलाल जी शास्त्री आ गये। उन्हें मैंने कहा था कि ‘‘पंडित जी! मुझे कोई ऐसा प्रमाण दिखाओ कि जिसमें स्वयं के लिए हुए नियम गुरु की आज्ञा से छोड़े जा सकते हों।’’
‘पंडित जी उस समय भगवती आराधना टीका सहित लेकर आये थे। उन्होंने मुझे उसमें से ‘असत्यमृषा’ भाषा के प्रकरण को खोल कर दिखाया जो कि यह था-
‘‘पच्चक्खाणी नाम केनचिद् गुरुमननुज्ञाप्य इदं क्षीरादिकं इयंतं कालं मया प्रत्याख्यातं इत्युत्तं कार्यान्तरमुद्दिश्य तत्कुर्वित्युदितं गुरूणा प्रत्याख्यानावधिकालो न पूर्ण इति नैकान्ततः सत्यता गुरुवचनात्प्रवृत्तो न दोषायेति मृषैकान्तः१।’’
प्रत्याख्यानी नाम की अनुभय भाषा का लक्षण करते हुए कहते हैं कि किसी ने गुरू की आज्ञा लिए बगैर यह दूध आदि वस्तु मैंने इतने दिन के लिए त्याग दिया है ऐसा प्रत्याख्यान-त्याग ले लिया पुनः अन्य कार्य का उद्देश्य करके गुरु ने कहा कि तुम यह ग्रहण करो। उसके त्याग की अवधि का काल पूर्ण नहीं हुआ इसलिए यह बात एकान्त से सत्य नहीं है और उस शिष्य ने गुरू की आज्ञा से उस त्यागी हुई वस्तु के ग्रहण करने में प्रवृत्ति की है इसलिए दोष न होने से यह एकान्त झूठ भी नहीं है।
यहाँ पर इस अनुभय भाषा के प्रत्याख्यानी भाषा के लक्षण में यही बात समझने की है कि प्रत्याख्यान की अवधि पूर्ण न होने पर भी यदि गुरू की आज्ञा से शिष्य उस वस्तु को ग्रहण कर लेता है तो दोष नहीं है। इसे देखकर मेरा मन प्रसन्न हुुआ और मैंने आचार्यश्री के पास जाकर उनकी आज्ञा पालन करने के लिए स्वीकृति दे दी। आचार्यश्री की आज्ञा से एक आर्यिका माताजी ने मुझे एक नया दुपट्टा मँगाकर दे दिया। मैंने वह दुपट्टा धोकर सुखा दिया। दूसरे दिन मैं वह दुपट्टा ओढ़कर आहार के लिए निकली, सेठ रामचन्द्र जी के यहाँ मेरा पड़गाहन हो गया। मुझे उन्होंने एक कटोरी दी।
उसमें आहार लिया साथ में चावल भी ले लिया। कटोरी वहीं छोड़कर आ गई। मंदिर आकर आचार्यश्री के सामने ज्यों की त्यों सारी बातें निवेदित कर दीं। पुनः आचार्य महाराज ने रामचंद्र से भी पूछा- ‘‘क्यों रामचन्द्र जी! इन्होंने कटोरी में आहार लिया है?’’ रामचन्द्र जी ने कहा-‘‘हाँ, महाराज जी! इन जैसा पात्र आपको मुश्किल से मिलेगा, आप तो संघ में सभी को प्रेरणा दे देकर मुनि, आर्यिका बनाते हो। एक ये हैं कि जो स्वयं दीक्षा माँग रही हैं और आप टाल रहे हैं।’’
महाराज जी प्रसन्न मुद्रा में मुस्करा दिये। गुरू की प्रसन्नता और शुभाशीर्वाद प्राप्त कर कृतकृत्य होती हुई मैं अपने स्थान पर आ गई। मैंने समझा कि-‘‘अब मेरी दीक्षा हो जायेगी।’’ किन्तु आचार्य महाराज का यह कहना था कि कम से कम छह महीने संघ में रहना चाहिए, तब दीक्षा देंगे। सो मैं भी गुरू की आज्ञानुसार संघ की सभी क्रियाओं में भाग ले रही थी और अपने पठन-पाठन में लगी हुई थी। यद्यपि मेरी भावना इतनी उत्कट थी कि मुझे दीक्षा बिना एक-एक दिन भी वर्ष के समान लग रहे थे फिर भी शांति के सिवाय उपाय क्या था।
मैं सोचने लगी- ‘‘देखो, मैंने जल्दबाजी में क्षुल्लिका विशालमती अम्मा की नहीं मानी और श्रवण-बेलगोला के बाहुबली की यात्रा छोड़कर आ गई। यहाँ तो दिसंबर १९५५ निकल गया और १९५६ की जनवरी, फरवरी भी निकली जा रही है। सच है, ‘उतावला सो बावला, ऋतु आये फल होय।’ इस सूक्ति के अनुसार ‘‘जब योग होगा तभी दीक्षा मिलेगी।’’
आचार्यश्री ने संघ सहित जयपुर से विहार कर दिया। संघ ‘माधोराजपुरा’ में आ गया।
