अतिशय क्षेत्र महावीर जी के दर्शन
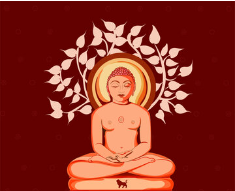
आचार्य संघ यहाँ आकर भगवान् महावीर मंदिर के नीचे कटरा की धर्मशाला में ही ठहरा हुआ था। यहाँ दर्शन करके हम लोगों ने शांतिवीरनगर जाकर, वहाँ मंदिर के दर्शन किये। कमलाबाई आदर्श विद्यालय में जिनमंदिर के दर्शन किये और ब्र. कृष्णाबाई के मुमुक्षु महिलाश्रम के मंदिर जाकर वहाँ भी दर्शन किये।
क्षेत्र-परिचय
यहाँ का मंदिर चांदनपुर गांव के अति निकट है। इस क्षेत्र का अतिशय इस प्रकार प्रसिद्ध है कि बहुत समय पहले एक गाय एक टीले पर खड़ी हो जाती और उसके स्तनों से दूध झर जाता। ग्वाले ने छिपकर यह सब देखा पुन: ग्वाले ने उस टीले को खोदकर भगवान् महावीर की मूर्ति को प्राप्त कर लिया।
भगवान् के प्रगट होने का समाचार चारों ओर फैलते ही हजारों जैन आ गये। तभी जैन श्रावकों ने वहाँ मंदिर निर्माण कराकर जिनप्रतिमा को वेदी में विराजमान करा दिया। भूगर्भ से निकले भगवान् के स्थान पर छतरी बनाकर चरण विराजमान कर दिये गये हैं। इस क्षेत्र का दर्शन करने के लिए लाखों अजैन आते हैं। इधर के मीना-गूजर लोग इन्हें ही अपना आराध्य देव मानते हैंं।
यह स्थान आमेर गद्दी के मूलसंघ आम्नाय के दिगम्बर जैन भट्टारकों का केन्द्र रहा है। आज इस क्षेत्र पर जो कुछ वैभव दिख रहा है, वह सारे भारत के दिगम्बर जैन बंधुओं की श्रद्धा का फल है। यहाँ क्षेत्र पर यह एक विशाल मंदिर है। दो मंदिर आश्रम में हैं और शांतिवीरनगर में एक विशालकाय २८ फुट ऊँची खड्गासन भगवान् शांतिनाथ की प्रतिमा का ही पंचकल्याणक होने वाला था।
यहाँ क्षेत्र पर छह धर्मशालायें हैं। औषधालय आदि कई सेवाभावी संस्थायें हैं। वहीं पर ब्र. श्रीलालजी काव्यतीर्थ ने एक प्रिंटीग प्रेस लगाकर कई वर्षों तक अनेक जैनग्रंथों को छपवाया है।
मध्यलोक चैत्यालय की रूपरेखा
आचार्यश्री शिवसागर जी महाराज ने एक दिन मुझसे कहा- ‘‘माताजी! जहाँ पंचकल्याणक प्रतिष्ठा के लिए मंच और पंडाल बन रहा है, वहीं पर आपके मध्यलोक चैत्यालय की रचना बनवायेंगे। यहाँ जगह भी विस्तृत है, विस्तार से काम होगा।’’ पुनः वे बोले- ‘‘अब मेरी इच्छा कुछ दिन यहीं रहने की है। इसके एक कोने में एक कमरा गुफा के समान होगा जिसमें मैं रहूंगा और दूसरे कोने में मुनिश्री श्रुतसागरजी रहेंगे।’’
पुनः कुछ क्षण बाद उनके मुख से शब्द निकले- ‘‘मेरे आचार्य अवस्था के बारह वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। जैसे बारह बजे तक सूर्य ऊपर चढ़ता है, पुनः ढलता जाता है, ऐसे ही मेरे भी बारह वर्ष तक उन्नति के थे-ऊपर चढ़ते हुए थे, अब ढलते हुए रहेंगे।’’ पता नहीं क्यों? आचार्यश्री के मुख से वहाँ क्षेत्र पर ये शब्द कई बार निकले और कई साधुओं के सामने निकले थे।
अथवा यों कहिये- ‘‘जैसी होनहार होती है, वैसे ही शब्द कभी-कभी मुख से निकल जाते हैं।’’ जब से फाल्गुन शुक्ला छठ से दशमी तक पंचकल्याणक का मुहूर्त निकला था तभी से एक प्रतिष्ठाचार्य ने संघ में एक माताजी के पास सूचना भेजी थी कि यह मुहूर्त प्रमुख के लिए हानिप्रद है लेकिन जैनशास्त्रानुसार होलाष्टक (फाल्गुन शुक्ला अष्टमी से पूर्णिमा तक को होलाष्टक कहते हैं) का कोई उल्लेख नहीं है।
कहते हैं कि बावनगजा में भी होलाष्टक में प्रतिष्ठा थी, उसी में आचार्य कल्पश्री चन्द्रसागर जी महाराज गये थे और उनकी समाधि हो गई थी। जो भी हो, सन् १९८५ की प्रतिष्ठा में पहले फाल्गुन शुक्ला अष्टमी तक का मुहूर्त था। आचार्यश्री धर्मसागरजी ने कुछ विकल्प (वहम) किया था, तभी उनकी और मुनिश्री श्रुतसागरजी की आज्ञानुसार उसे बढ़ाकर वैशाख में कर दिया गया था।
उसके बाद भी मैं आषाढ़ से अगले चैत्र मास तक बहुत बीमार हुई थी। खैर! इस सन् १९८७ की प्रतिष्ठा का मुहूर्त आचार्यश्री विमलसागर जी की आज्ञा से फाल्गुन शुक्ला ७ से ग्यारस (११) तक था। चूँकि ये आचार्य महाराज होलाष्टक नहीं मानते हैं। अन्यत्र भी कुंभोज आदि में फाल्गुन की आष्टान्हिका में प्रतिष्ठायें हुई हैं अतः इस विषय में मुझे विशेष ज्ञान नहीं है, मुहूर्तज्ञ ही जानें।
पंचकल्याणक प्रतिष्ठा
यहाँ इस समय आचार्य संघ के आने पर भगवान् शांतिनाथ की पंचकल्याणक प्रतिष्ठा की जोरदार तैयारियाँ चल रही थीं। प्रतिष्ठा का मुहूर्त फाल्गुन की आष्टान्हिका में था।
झंडारोहण
माघ शु. १५ के दिन सर्व संघ के सानिध्य में प्रतिष्ठा के लिए झंडारोहण किया गया। ध्वजा ऊपर लहराते ही उसकी नोक किसी गलत दिशा में चली गई अतः मुनिश्री श्रेयांससागर जी आदि दो-चार साधु-साध्वियों ने आपस में कुजबुज करना शुरू की। आर्यिका विशुद्धमतीजी ने भी मुझसे कहा- ‘‘माताजी! कुछ अशुभ दिखता है, उपाय सोचना चाहिए।’’ मैंने भी ब्रह्मचारी सूरजमल से कहा- ‘‘बाबाजी! कुछ शांतिविधान करा दीजिये।’’
किन्तु जो होनहार होती है सो भला कैसे टल सकती है? उसी दिन सायंकाल के प्रतिक्रमण के समय आचार्यश्री शिवसागर जी और बड़ी आर्यिका श्री वीरमती जी से जरा सी बात में आपस में अशांति हो गई। दोनों ही संघ में बड़े थे और दोनों में ही उग्रता आ जाने से कोई रोक भी न पाये। कुछ क्षण बाद माहौल शांत हो गया। नित्य की भांति दैवसिक प्रतिक्रमण हुआ।
हम सभी अपने-अपने स्थान पर आ गये किन्तु उस अशांति से कई साधु-साध्वियों के मानसपटल पर प्रतिष्ठा के अशुभ का आभास समझकर, विषाद की रेखाएँ खिंच गर्इं। संघ का वातावरण कुछ उदास सा दिखने लगा।
आचार्यश्री अस्वस्थ
आचार्यश्री को अष्टमी (फाल्गुन कृ. ८) को बुखार आ गया। एक-दो दिन मध्यान्ह में आचार्यश्री ने मोतीचंद से वैयावृत्ति करवाई, तेल मालिस करवाई, जबकि उससे पहले कभी भी शरीर पर तेल नहीं लगवाया था। एक बार बोले- ‘‘मोतीचंद! पता नहीं क्यों? मेरे जीवन में मुझे कभी भी ऐसी कमजोरी और ऐसी हाथ-पैरों में दर्द नहीं हुई है।
इन दिनों न जाने कैसा शरीर गिरा-गिरा सा लगता है?’’ मोतीचंद ने आकर मुझे बताया-‘‘मुझे भी मन में बहुत ही चिंता हो गई। क्या करना? समझ में नहीं आया।’’ आचार्यश्री को आहार लेने में भी कंठ में कुछ तकलीफ हो रही थी। साधारण सी कुछ दवा दी गयी होगी।
वैद्यों ने मुनिश्री श्रुतसागरजी आदि से एकांत में कुछ शंका व्यक्त कर दी। इधर-उधर की बातें करते हुए कई एक प्रमुख साधु एवं श्रावकों ने आचार्यश्री से पूछा-‘‘महाराज जी! यदि आप इतनी दूर पांडाल में नहीं जा सके, तो दीक्षाएँ कौन देंगे? ।’’ आचार्यश्री ने कहा-‘‘नहीं, नहीं, मैं स्वस्थ हो जाऊँगा, मैं चलूँगा।’’
दीक्षा हेतु प्रार्थना
कई दिन पूर्व मैं आचार्यश्री के समक्ष कई शिष्य-शिष्याओं को दीक्षा हेतु प्रार्थना कराने ले गई थी। क्षुल्लिका अभयमती को आर्यिका बनना था। क्षुल्लक संभवसागर मुनि बनना चाहते थे। यशवंत कुमार मुनि बनना चाहते थे, गेंदीबाई भी क्षुल्लिका दीक्षा लेना चाहती थीं। ब्र. अशर्फी बाई, ब्र. विद्याबाई आर्यिका बनना चाहती थीं।
आचार्य श्री ने इन सबको दीक्षा देने के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी थी और अतीव वात्सल्य से बार-बार मेरी ओर देखकर खुश हो रहे थे पुनः बोले- ‘‘माताजी! मोतीचंद को भी दीक्षा दिलावो, वह बहुत योग्य है ।’’ मैंने कहा-‘‘महाराज जी! मैंने बहुत प्रेरणा दे दी, किन्तु वे अभी तैयार नहीं हैं।’’
पुनः बोले-‘‘दीक्षार्थियों को तैयार करना तुम्हारा काम है और दीक्षा देना मेरा काम है।’’ ‘‘कौन जानता था कि निकट भविष्य में ही क्या होने वाला है?’’
साधुओं में ऊहापोह
‘‘हम सभी साधुओं में ऊहापोह चल रहा था कि आचार्यश्री कैसे स्वस्थ हों? क्या किया जाये?।’’
मेरी अपनी धुन थी, कलकत्ता टेलीफोन करके वैद्यराज केशवदेव को बुलाया जाये। चूँकि हैदराबाद में आकर वे मेरा इलाज कर चुके थे और श्रवणबेलगोल में आर्यिका आदिमती, क्षुल्लिका अभयमती का इलाज कर चुके थे। हालांकि मेरी कोई सुनने वाला नहीं था। वास्तव में वैद्य भाग्य नहीं हैं और न भगवान ही हैं। मेरी छटपटाहट देखकर मोतीचंद बोले-‘‘माताजी! आप मुझे जो भी उपदेश दोद्ध मैं करने को तैयार हूँ।’’
तब मैंने मोतीचंद से कहा-‘‘तुम कलकत्ता फोन करो।’’ इधर आचार्य श्री की हालत बहुत नाजुक होती जा रही थी। मैंने यह भी नहीं सोचा कि ‘‘कब कलकत्ते फोन होगा? कब वैद्य यहाँ पहुँचेंगे? और कब उनकी दवा आचार्यश्री के पेट में जायेगी?.’’ इधर फाल्गुन कृष्णा अमावस्या ने अपना प्रभाव दिखाया।
आचार्य शिवसागरजी की समाधि
मध्यान्ह सामायिक के बाद आचार्यश्री लघुशंका के लिए उठे, मध्य में ही गड़बड़ हो गई, आचार्यश्री ने बहुत ही खेद की मुद्रा बनाकर मौनपूर्वक ही खेद व्यक्त किया, शुद्धि करके आकर कमरे में बैठ गये। आर्यिका विशुद्धमती जी आदि कई साधु-साध्वियाँ उनके सानिध्य में थे। मुझे भी समाचार मिलते ही मैं भी ऊपर आ गई।
कुछ ही क्षण बाद आचार्यश्री ध्यानमुद्रा में बैठ गये और हम सभी साधुवर्ग महामंत्र का उच्चारण करते रहे। आचार्यश्री ने इस नश्वर शरीर को छोड़कर, दिव्य वैक्रियक शरीर प्राप्त कर लिया। इधर एकदम हाहाकर मच गया। हम लोगों के हृदय पर मानों व्रजपात ही हो गया हो।
बिजली सी खबर सारे क्षेत्र में पहुँच गई। जयपुर आदि शहरों में भी फोन से समाचार पहुँचा दिये गये। उसी दिन सायंकाल करीब ५ बजे शांतिवीर नगर में आचार्यश्री के पार्थिव शरीर की अंतिम संस्कार क्रिया की गयी।
मुनिश्री धर्मसागर संघ
मुनिश्री धर्मसागर जी सन् १९५८ में ब्यावर से विहार कर अलग चले गये थे। इस प्रतिष्ठा के अवसर पर यहाँ अपने संघ सहित आये हुए थे। वे भी इस समय यहीं संघ में विराजमान थे। यद्यपि मुनि-आर्यिका आदि साधुओं को शोक नहीं करना चाहिए। हम लोग तो श्रावकों को ऐसे इष्टवियोग-मरण आदि के अवसर पर शिक्षा देते हैं, संबोधित करते हैं, रोने से रोकते हैं और कहते हैं- ‘‘दुखशोकतापाव्रंदनवधपरिदेवनान्यात्मपरोभयस्थान्यसद्वेद्यस्य।’’
दुख करना, शोक करना, पश्चात्ताप करना, करुण व्रंदन करके रोना, वध करना, ऐसा रोना कि दूसरे भी रो पड़ें, यह सब शोकादि स्वयं करना, दूसरे में उत्पन्न करना अथवा स्वयं और पर दोनों में करना इनसे असातावेदनीय कर्म का आस्रव होता है। दूसरी बात यह है कि मृत्यु के आगे किसी की नहीं चलती है। ‘‘अलंघ्यशक्ति-र्भवितव्यतेयं’’ भवितव्यता यानी होनहार अलंघ्य है-टाले नहीं टलती है। सब कुछ जानते हुए भी संघ के सभी साधुवर्ग अपने आपको ही मानों भूल गये थे, सभी रो रहे थे।
शायद ही एक-दो साधु कोई बचे हों कि जिनकी आंखों से अश्रु न आये हों, तो भी उन सबका ही अन्तःकरण शोक को प्राप्त हो गया था। चूँकि यह अकस्मात् समाधि हो गई थी और प्रतिष्ठा के इस अवसर पर जबकि प्रतिष्ठा प्रारंभ के मात्र ६ दिन शेष रह गये थे। और भी खास बात यह थी कि-
‘‘आचार्य बनने के समय किसी को ऐसा नहीं लगता था कि ये मुनिराज सभी साधु-साध्वियों के मन पर ऐसा छा जायेंगे, ऐसा वात्सल्य रखेंगे और सभी के गुरु बन जायेंगे।’’ महाराज जी अनुशासन में कठोर भी थे और वात्सल्य में कुशल मातृत्व भावना भी रखते थे इसी वजह से पूरे संघ में सभी को हितैषी दिख रहे थे तथा यही कारण था कि उनका अभाव इस समय सभी के लिए दुःखद बन गया।
आचार्य पट्ट की चर्चा
संघ में योग्य और संघ संचालन में कुशल मुनिश्री श्रुतसागरजी ही थे अतः चतुर्विध संघ में उन्हीं को आचार्य बनाने की बात हुई। इसी मध्य मुनिश्री धर्मसागर जी चार मुनियों के साथ यहाँ पधारे हुए थे। चूँकि आचार्यश्री वीरसागर जी महाराज के शिष्यों में इनका द्वितीय नम्बर था अतः उनके संघ के मुनिवर्ग जो कि श्रीनिर्मलसागर जी, श्री संयमसागर जी, श्रीबोधिसागर जी एवं श्री दयासागर जी थे, उनके माध्यम से यह चर्चा आई कि-
‘‘जिस समय मुनिश्री धर्मसागर जी से छोटे मुनिश्री श्रुतसागर जी को आचार्य पट्ट दिया जायेगा, तो मुनिश्री धर्मसागर जी उसी समय विहार कर जायेंगे।’’ अब संघ के मुनियों, आर्यिकाओं, ब्रह्मचारियों और प्रमुख श्रावकों में इस चर्चा ने विशेष रूप ले लिया। दिन-रात ऊहापोह शुरू हो गया। कुछ साधु-साध्वी तटस्थ थे, कोई भी आचार्य बने हमें क्या करना?
किन्तु हम जैसे साधु-साध्वी उस विषय में पूर्णतया अपनी सहमति-असहमति में लगे हुए थे। इस ऊहापोह में सेठ हीरालाल जी पाटनी, निवाई वालों ने बार-बार हम लोगों के स्थान पर आकर चर्चायें शुरू कर दींं और निर्णय लेने का प्रयास करने लग गये.।
सभी मुनि-आर्यिकाओं की भी सभा बैठी, उसमें खास-खास ब्रह्मचारी और श्रेष्ठी बैठे अन्ततोगत्वा आचार्य पद के लिए मुनिश्री धर्मसागर जी का नाम घोषित हो गया। उस समय फाल्गुन शुक्ला अष्टमी को भगवान् के तपकल्याणक के दिन आचार्यपट्ट होकर, नूतन आचार्य से ग्यारह दीक्षाएँ होना निश्चित हो गया।
पंचकल्याणक प्रतिष्ठा प्रारंभ
इधर शांतिवीरनगर में पंचकल्याणक प्रतिष्ठा शुरू हो गई। भगवान के गर्भ, जन्म कल्याणक सम्पन्न हुए और तप कल्याणक का दिन आ गया।
माता-पिता का आगमन
टिकैतनगर में कैलाश जी ने दुकान से घर आकर संघ से आया हुआ एक पत्र सुनाया, जिसे मोतीचंद ने लिखा था। उसमें यह समाचार था कि- ‘‘संघ यहाँ महावीर जी क्षेत्र पर विराजमान है, फाल्गुन सुदी में शांतिवीर नगर में भगवान शांतिनाथ की विशालकाय प्रतिमा का पंचकल्याणक महोत्सव होने जा रहा है।
इस अवसर पर अनेक दीक्षाओं के मध्य क्षुल्लिक अभयमती जी की आर्यिका दीक्षा अवश्य होगी अतः आप माँ और पिताजी को अंतिम बार उनकी इस दीक्षा के माता-पिता बनने का लाभ न चुकावें, अवश्य जा जावें। उस समय यद्यपि पिताजी को पीलिया के रोग से काफी कमजोरी चल रही थी, वे प्रवास में जाने के लिए समर्थ नहीं थे फिर भी माँ ने आग्रह किया कि- ‘‘यह अंतिम पुण्य अवसर नहीं चुकाना है। भगवान महावीर स्वामी की कृपा से आपको स्वास्थ लाभ होगा। हिम्मत करो, भगवान, तीर्थ और गुरुओं की शरण में जो होगा, सो ठीक ही होगा ।’’
कैलाशचंद जी ने भी साहस किया। रुग्णावस्था में भी पिता को साथ लेकर माँ की मनोकामना पूर्ण करने के लिए महावीर जी आ गये। वहाँ आकर देखते हैं-बड़ा ही गमगीन वातावरण है। अकस्मात् फाल्गुन कृष्णा अमावस्या की मध्यान्ह में आचार्यश्री शिवसागर जी महाराज की समाधि हो गई है। सभी साधु-साध्वियों के चेहरे उदास दिख रहे हैं और यहाँ अब आचार्य पट्ट मुनिश्री धर्मसागर जी महाराज को दिया जाये या मुनि श्रुतसागर जी महाराज को ?’’
साधुओं की सभा में यह जटिल समस्या चल रही है। खैर! उन्हें इन बातों से क्या लेना-देना था? वे वहाँ कटरा में ही धर्मशाला में ठहर गये। माँ ने सभी साधुओं के दर्शन किये किन्तु पिता कहीं नहीं जा सके। वे अपने कमरे से ही दरवाजे में पलंग पर बैठे-बैठे दूर से साधुओं का दर्शन कर लेते थे।
वे पीलिया रोग से उस समय काफी परेशान थे। कई बार उन्होंने मेरे दर्शन के लिए सुपुत्र कैलाश से भावना व्यक्त की। कैलाश ने मुझसे प्रार्थना भी की किन्तु मैं कुछ धार्मिक आयोजनों में व्यस्त भी रहा करती थी तथा कुछ संकोचवश वहाँ नहीं गई।
मां मोहिनी की मनोभावना पूर्ण हुई
इधर फाल्गुन शुक्ला अष्टमी को भगवान के तपकल्याणक दिवस मुनि श्री धर्मसागर जी को चतुर्विध संघ के समक्ष आचार्य पद प्रदान किया गया और नवीन आचार्य के करकमलों से उसी दिन ग्यारह दीक्षाएँ हुर्इं। कैलाशचंद जी इतनी भीड़ में भी पिता को सभा में ले आये। उन्होंने क्षुल्लिका अभयमती की आर्यिका दीक्षा में माता-पिता के पद को स्वीकार कर, उनके हाथ से पीताक्षत, सुपारी, नारियल आदि भेंट में प्राप्त किये।
इस लाभ से वे बहुत ही प्रसन्न हुए। इस दीक्षा के अवसर पर मेरी प्रेरणा से सनावद के यशवन्त कुमार ने मुनि दीक्षा ली थी। ब्र. अशर्फीबाई और ब्र. विद्याबाई ने भी आर्यिका दीक्षा ली थी। क्षुल्लिका अभयमती का नाम अभयमती ही रहा। ब्र. अशरफीबाई का नाम आर्यिका गुणमती प्रसिद्ध हुआ और विद्याबाई का नाम आर्यिका विद्यामती रखा गया।
इन दीक्षाओं को सम्पन्न कराने में मैंने बड़े उत्साह से भाग लिया था। इसके बाद प्रतिष्ठा के शेष दो कल्याणक भी सानंद सम्पन्न हुए। प्रतिष्ठा के बाद भीड़ कम हो गई, तब माँ मोहिनी ने वहाँ कुछ दिन और रहकर धर्मलाभ लेने का निर्णय किया।
श्रीमान् छोटेलाल जी को मेरे अंतिम दर्शन
गृहस्थाश्रम के पिताजी पीलिया से परेशान थे। बार-बार कैलाशचंद से मुझे बुलाने के लिए कहते थे और कैलाशचंद आकर मुझसे प्रार्थना किया करते किन्तु पता नहीं क्यों? मैं टाल दिया करती थी। एक दिन मैं कैलाशचंद के साथ उनके कमरे में गई। पिताजी देखते ही रो पड़े और बोले- ‘‘माताजी! अब हमें इस जीवन में आपके दर्शन नहीं होंगे।’’
मैं वहाँ दो मिनट के लिए खड़ी हुई, आशीर्वाद दिया और बोली- ‘‘घबराते क्यों हो ?’’ बाद में मैं जल्दी ही वापस चली आई। पता नहीं, मुझे वहाँ बैठकर पिता को कुछ शब्दों में शिक्षा देने में क्यों संकोच रहा?’’ पिताजी चाहते थे कि आर्यिका ज्ञानमती जी मेरे पास कुछ देर बैठकर कुछ कहें, बोलें, सुनावें किन्तु उनकी इच्छा पूरी नहीं हो पाई । दो-चार दिनों में ही घर वापस जाने का कार्यक्रम बन गया।
क्षुल्लिका विशालमती से मिलन
सन् १९५५ में क्षुल्लिका विशालमती जी से आज्ञा लेकर मैं म्हसवड़ से आचार्यश्री वीरसागर जी के संघ में आ गई थी। क्षुल्लिका विशालमतीजी का मेरे प्रति इतना वात्सल्य था कि उनको शब्दों में कहना शक्य नहीं है। उन्होंने सोचा भी नहीं था, न मैंने ही सोचा था कि- ‘‘हम दोनों का इतनी जल्दी वियोग हो जायेगा।’’
किन्तु दो चातुर्मास के बाद ही वियोग हो गया। मैंने आर्यिका दीक्षा लेने का निर्णय बनाया, तभी उन्होंने अच्छी शिक्षायें और प्रेरणा देकर मेरी इच्छानुसार मुझे इधर संघ में भेज दिया था पुनः फरवरी १९५६ में इधर रैनवाल में संघ के दर्शनार्थ और मुझसे मिलने हेतु-सुख-दुख पूछने हेतु आ गई थीं। तभी वे मेरी संतुष्टि देखकर कुछ कडुवे-मीठे अनुभव लेकर ५-७ दिन रहकर चली गई थीं।
खास बात यह हुई थी कि यहाँ संघ में एक वयोवृद्ध सुमतिमती माताजी ने कहा कि- ‘‘ये क्षुल्लिका विशालमती रेल-मोटर पर बैठती हैं, इनके साथ अब तुम आहार नहीं करना।’’ मैंने कहा-‘‘ठीक है।’’ इधर क्षुल्लिका विशालमती जी पूर्वप्रेम से मेरे साथ आहार को आना चाहती थीं।
मैंने टाल दिया किन्तु भय के कारण उनसे वास्तविक स्थिति नहीं बताई कि मुझे यहाँ संघ में मना किया गया है। इसके अतिरिक्त भी वे जिस-जिस चौके में जाती थीं प्रायः संघ के साधु वहाँ से निकल जाते थे इससे भी इन्हें दुःख होता था। आज मैं समझती हूूँ कि उस समय मुझे एकांत में संघ की इस मर्यादा और कठोरता का परिचय दे देना चाहिए था।
खैर! इस व्यवहार से वे शायद मेरे प्रति भी उपेक्षित हुर्इं और चली गर्इं। ‘‘मेरे जीवन में ऐसे अनेक प्रकार के प्रसंग आये हैं और साधुओं में या श्रावकों में मैंने वास्तविक स्थिति का खुलासा न कर मौन रखा। इससे मेरे प्रति अनेक भ्रांत धारणाएँ लोगों में बनती रहीं और मुझे कष्टों का सामना भी करना पड़ा, ऐसा मैंने स्वयं अनुभव किया है।
अब मैं समझती हूँ कि यह ‘‘सहनशीलता’’ न होकर मेरे में बहुत बड़ी कमी थी, आज भी प्रायः यह कमी मौजूद है।’’ उसके बाद पुनः यहाँ पर (महावीर जी) सन् १९६९ में ये क्षुल्लिका विशालमती आई थीं। मैं इन्हें देखते ही उनसे चिपट गई, उन्होंने भी मुझे बड़ा मानकर आर्यिका पद में देखकर ‘वंदामि’ किया, रत्नत्रय कुशल पूछा।
रात्रि में वे मेरे पास ही सोई, अनेक बातें हम दोनों की आपस में हुर्इं, उस समय आचार्यपट्ट की समस्या यहाँ उलझी हुई थी अतः मेरा मस्तिष्क विक्षिप्त सा था। प्रातः बिना आहार किये वे कब चली गर्इं इसका मुझे बहुत ही दुःख हुआ। शायद वे रैनवाल की पुरानी घटना ‘‘मेरे साथ कोई आहार नहीं करेगा’’ ऐसा स्मरण कर ही चली गई होंगी।
इसका मुझे बहुत दुःख हुआ फिर भी क्या उपाय था? इसके बाद मेरे जीवन में उनका मिलन या वार्तालाप या पत्रों द्वारा विचारों का आदान-प्रदान कुछ भी नहीं हो सका, अब तो वे स्वर्गस्थ हो चुकी हैं। हां! शायद स्वर्ग में मिलना हो सकता है।
व्याकरण का अध्यापन
आर्यिका विशुद्धमती जी की काफी दिनों से इच्छा थी, कहा करती थीं कि- ‘‘माताजी! जैनेंद्रप्रक्रिया व्याकरण पढ़ाइये।’’ उस समय यहाँ महावीरजी में प्रातः सामायिक के बाद ही व्याकरण पढ़ाने का समय निश्चित किया गया था।
उसमें कई आयिकायें बैठती थीं, मोतीचन्द भी बैठते थे। यह व्याकरण की कक्षा बहुत ही अच्छी चल रही थी किन्तु अकस्मात् आचार्यश्री शिवसागर जी महाराज की सल्लेखना हो जाने से छूट गई पुनः वहाँ नहीं चल पाई।
आचार्यश्री विमलसागर जी संघ दर्शन
आचार्यश्री विमलसागर जी महाराज अपने विशाल संघ सहित यहाँ महावीर जी क्षेत्र पर पधारे। दोनों संघों का अच्छा मिलन हुआ। इस समय यहाँ पचहत्तर साधु-साध्वी मयूरपिच्छिकाधारी हो गये थे। आपस में अच्छा सौहार्द था। मैं आचार्यश्री विमलसागर जी से विशेष निकटता होने से विशेष प्रसन्न थी। मैंने मोतीचंद से कहा- ‘‘मोतीचंद! देखो, इतने विशाल मुनि-आर्यिकाओं के संघ का एक जगह मिलना कम संभव है अतः तुम एक पूरे साधू समूह का फोटो ले लो पुनः मुनि समूह और आर्यिका समूह के अलग-अलग दो फोटो ले लो।’’
चूँकि मोतीचन्द को फोटो खींचने का बहुत ही शौक था अतः मेरी आज्ञा शिरोधार्य कर इन्होंने यह कार्य हाथ में लिया। इसमें इन्हें बहुत ही मेहनत पड़ी। कहीं कोई आर्यिका नहीं आ रही हैं, नाराजगी व्यक्त कर रही हैं। कहीं कोई साधु चिढ़ रहे हैं तो कहीं कोई नहीं आ रहे हैंं। कुल मिलाकर समूह में सबको बिठाकर साधुओं का फोटो खींचना कितना कठिन काम है।
मोतीचंद बहुत परेशान हो गये, हिम्मत हारकर बोले- ‘‘माताजी! मेरे वश का नहीं है।’’ फिर भी मेरी विशेष प्रेरणा होने से उन्होंने यह सामूहिक फोटो खींचा। उस समय के बाद शायद इन्होंने कैमरा रख दिया, फोटो ही नहीं खींचा है। मेरा कहना यही था कि- ‘‘यह एक इतिहास बनता है कि अमुक सन, संवत् में अमुक स्थान पर, इतने मुनियों का समुदाय एकत्रित हुआ था।
उसमें इतने मुनि और इतनी आर्यिकायें थीं इत्यादि और मेरा इसमें भला क्या स्वार्थ था? मुझे वह उदाहरण भी अच्छी तरह याद था कि जब आचार्य शिरोमणि गुरुणां गुरु चारित्रचक्रवर्ती श्रीशांतिसागरजी महाराज दिल्ली के चाँदनी चौक आदि स्थलोें पर अकेले जा-जाकर किसी श्रावक से कहकर अपना फोटो खिंचवाते थे, तब किसी ने कहा-
‘‘महाराज! आपको फोटो खिंचवाने का शौक क्यों? तब महाराज जी ने कहा था-‘‘भईया! हमें दिगम्बर मुुद्रा में फोटो खिंचवाने का शौक नहीं है, प्रत्युत् इसमें यह रहस्य है कि भविष्य में दिल्ली राजधानी जैसे शहरों में दिगम्बर मुनियों का विहार निराबाध होता रहे, इसके लिए ये फोटो साक्षी रहेंगे कि दिगम्बर मुनि अमुक सन्-संवत् में भी दिल्ली के चांदनी चौक आदि स्थानों में निराबाध विहार करते रहते थे।’’
खैर! मोतीचन्द द्वारा खींचे गये वे मुनि और आर्यिका समूह के फोटो आज अनेक मंदिरों में व अनेक मुनिभक्तों के घरों में लगे हुए दिखते हैं।
महावीर जी का वार्षिक मेला
यहाँ चैत्र सुदी तेरस से लेकर वैशाख बदी पंचमी तक बहुत बड़ा मेला लगता है। भगवान् महावीर स्वामी की रथयात्रा निकलती है। उस दिन हजारों जैन तो आते ही हैं, अजैन लोगों की संख्या अधिक रहती है। उसमें इस इलाके के खास मीणा-गूजर लोग बहुत रहते हैं। ये खूब नाचते-गाते हैं, खूब भक्ति करते रहते हैं। यहाँ मेला की भीड़ देखी, अनंतर यहाँ से विहार का कार्यक्रम बनाया गया।
महावीर जी से विहार
अजमेर से बहुत से श्रावक आचार्यश्री को श्रीफल चढ़ाकर अजमेर चातुर्मास के लिए प्रार्थना करने लगे। आचार्यश्री का आश्वासन पाकर अजमेर से भक्तगण ७-८ चौके लेकर आ गये। आचार्यश्री ने संंघ सहित जयपुर के लिए विहार कर दिया। संघ पद्मपुरी तीर्थ के दर्शन कर जयपुर खानिया में पहुँचा।
वहाँ आचार्यश्री वीरसागर जी की निषद्या के दर्शन किये, मंदिरों के दर्शन किये और आचार्यश्री वीरसागर जी के चातुर्मास के संस्मरण याद कर गुरु के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित किये। यहाँ पर गर्मी में संघ ठहर गया और अजमेर के श्रावकों को आचार्यश्री ने वापस अजमेर भेज दिया।
संघ विच्छेद
यहाँ खानिया से मुनिश्री श्रुतसागर जी ने अलग विहार कर दिया। उनके साथ में मुनिश्री अजितसागरजी, मुनिश्री सुबुद्धिसागरजी आदि कई मुनि गये थे और आर्यिका विशुद्धमती जी आदि कई आर्यिकायें भी गई थीं। हालांकि उस समय उनके अलग होने के प्रसंग में बहुत संघर्ष हुए थे। इसके बाद आचार्य संघ खजांची की नशिया में आकर ठहरा था। यहाँ से मुनिश्री श्रेयांससागर जी, आर्यिका अरहमतीजी, आर्यिका श्रेयांसमती आदि भी अलग विहार कर गये।
इधर जयपुर के कई पंडितों ने और श्रावकों ने आकर मुझसे निवेदन किया- ‘‘माताजी! सभी संघ ने मिलकर इन्हें आचार्यश्री शांतिसागर जी का तृतीय पट्टाधीश बनाया है। संघ में प्रमुख-प्रमुख मुनि वर्ग विहार कर अलग हो गये हैं। अब यदि आप भी अलग विहार कर जावेंगी तो संघ में खास साधु रहेंगे ही कौन? अतः आपको संघ में ही रहकर आचार्य परम्परा की मर्यादा संभालनी चाहिए।’’
मैं भी यही सोच रही थी कि ‘‘अब क्या करना?’’ फिर भी आचार्यश्री धर्मसागर जी की आज्ञा न होने से मैंने अपने विहार का विचार बदल दिया। महाराज जी को प्रसन्नता रही। इधर जयपुर के लोग आचार्य संघ का चातुर्मास यहीं कराना चाहते थे। आचार्यश्री ने बक्शीजी के चौक में पदार्पण किया। यहाँ मंदिर जी में मुनिसंघ ठहरा और धर्मशाला में आर्यिकाएँ ठहर गर्इं।
सबसे बड़ी आर्यिका वीरमती जी भी संघ में ही थीं। महाराज जी ने श्रावकों से कहा- ‘‘यहाँ गुरुकुल की स्थापना करनी चाहिए, तभी हम चातुर्मास करेंगे।’’ लोगों ने मंजूर कर लिया। रुपये इकट्ठे कर गुरुकुल खोला भी गया था किन्तु वह अधिक दिन चल नहीं सका था। यहाँ जयकुमार छाबड़ा अच्छे महानुभाव थे जो कि आचार्यश्री के कहे गये हर कार्यों में रुचि लेते थे और अनेक श्रावक, श्राविकाएँ भक्ति में रत थे। चातुर्मास यहीं करना निश्चित हो गया।
श्रावकों को बहुत ही प्रसन्नता हुई। साथ ही अजमेर के श्रावक कई बार बस लेकर आ चुके थे और यहाँ से विहार कराना चाहते थे अतः उन्हें दुःख हुआ। एक बार अजमेर से श्रावकगण बस में बैठकर आ रहे थे अकस्मात् बस का एक्सीडेंट हो जाने से कई लोगों को गहरी चोटें आर्इं, मुनिभक्त महेंद्रकुमार बोहरा को भी हड्डी में चोट आ गई,
काफी दिनों तक ये लोग अस्वस्थ रहे, फिर भी इन लोगों ने मुनियों के प्रति उपेक्षा नहीं की है, प्रत्युत् पूर्ववत् ही भक्त बने रहे हैं। आजकल कुछ श्रावक ऐसी घटनाओं से धर्म को ही छोड़ बैठते हैं, उनके लिए ऐसे-ऐसे भक्त ही उदाहरण बन जाते हैं।
वर्षायोग स्थापना
यहाँ आषाढ़ शुक्ला चौदस के दिन पूर्वरात्रि में वर्षायोग स्थापना की गई।
सांवत्सरिक प्रतिक्रमण
पहले आचार्यश्री वीरसागर जी सांवत्सरिक प्रतिक्रमण दीपावली के दिन करते थे। आचार्यश्री शिवसागर जी महाराज भी ऐसे करते आये थे। यहाँ सन् १९६९ में जयपुर में मैंने आचार्य श्री धर्मसागर जी महाराज को अनगारधर्मामृत की पंक्तियाँ दिखाई और प्रार्थना की कि- ‘‘महाराज जी! यह सांवत्सरिक प्रतिक्रमण शास्त्राधार से आषाढ़ मास की चतुर्दशी को ही होना चाहिए।’’ यथा-‘‘आषाढ़ान्त सांवत्सरी।’’
आचार्यश्री मुस्कराये और बोले- ‘‘ठीक है’’ पुनः उन्होंने आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी को ही सांवत्सरिक प्रतिक्रमण किया। इससे पूर्व मैंने आर्यिका वीरमती माताजी को ग्रन्थ-प्रमाण दिखाकर पक्ष में ले लिया था। तभी से लेकर सन् १९८६ के चातुर्मास तक आचार्यश्री यह बड़ा सांवत्सरिक प्रतिक्रमण आषाढ़ में ही करते आये हैं।
युग प्रतिक्रमण
ऐसे ही अनगार धर्मामृत में लिखा है पाँच वर्ष के बाद युग प्रतिक्रमण करना चाहिए। यथा- ‘‘तथा पंचसंवत्सरांते विधेया यौगान्ती प्रतिक्रमणा।’’ पाँच वर्ष के अंत में किया जाने वाला ‘यौगांत’ प्रतिक्रमण है।
इसे ही युग प्रतिक्रमण कहते हैं। यह भावना मैंने सन् १९८५ की प्रतिष्ठा के समय आचार्यश्री धर्मसागर जी से कहलाई थी उन्होंने स्वीकार भी कर लिया था किन्तु अत्यधिक कमजोर हो जाने से वे नहीं आ सके। बाद में सन् १९८७ की प्रतिष्ठा में आचार्यश्री विमलसागर जी ने यहाँ हस्तिनापुर से यह युग प्रतिक्रमण प्रारम्भ कर दिया है।
वर्षायोग स्थापना काल
ऐसे ही आचार्यश्री वीरसागर जी और आचार्यश्री शिवसागर जी महाराज वर्षायोग प्रतिष्ठापन क्रिया दिन में ही कर लेते थे। मैंने सुना था कि आचार्यकल्प श्री चन्द्रसागर जी महाराज और आचार्य श्री महावीरकीर्ति जी महाराज रात्रि में ही वर्षायोग प्रतिष्ठापना करते थे। आचार्यश्री देशभूषण जी महाराज ने भी जयपुर में रात्रि में ही प्रतिष्ठापन क्रिया की थी। अनगार धर्मामृत शास्त्र में लिखा है-
ततश्चतुर्दशीपूर्वरात्रे सिद्धमुनिस्तुती।
चतुर्दिक्षु परीत्याल्पाश्चैत्भक्तिगुरुस्तुतिं।।६६।।
शांतिभत्तिं च कुर्वाणैर्वर्षायोगस्तु गृह्यताम् ।
ऊर्जकृष्ण चतुर्दश्यां पश्चाद्रात्रौ च मुच्यताम् ।।६६।।१
मैंने आचार्यश्री धर्मसागर जी महाराज से कहा- महाराज जी ने भी कहा कि- ‘‘हाँ, आचार्यकल्प श्री चंद्रसागर जी महाराज भी रात्रि में ही स्थापना करते थे अतः ठीक है।’’ ऐसा कहकर उन्होंने जयपुर से ही रात्रि में वर्षायोग स्थापना करना शुरू कर दी। उसी प्रकार दीपावली के दिन अर्थात् कार्तिक वदी चौदश की पिछली रात्रि में वर्षायोग निष्ठापन क्रिया करते थे।
आर्यिकायें भी स्थापना के दिवस रात्रि मेेंं वहीं मंदिर में सायंकाल से ही आ जाती थीं और निष्ठापना के दिन पहले से ही आचार्य संघ के निकट स्थानों में रहकर पिछली रात्रि में आचार्यश्री के सानिध्य में आ जाती थीं। सन् १९७४ में आचार्यश्री धर्मसागर जी ने दिल्ली में भी चातुर्मास स्थापना लाल मंदिर में रात्रि में ही की थी और समापन क्रिया-दरियागंज के बालाश्रम में पिछली रात्रि में ही सम्पन्न की थी।
प्रकाशचंद को गुरुदर्शन
जयपुर में सन् १९६९ में प्रकाशचंद अपनी पत्नी ज्ञानादेवी को, बच्चों को, बहन माधुरी और भतीजी मंजू को साथ लेकर संघ के दर्शनार्थ आ गये। सन् १९६३ में मेरे संघ को सम्मेदशिखर पहुँचाने के बाद प्रकाशचंद छह वर्ष बाद संघ के दर्शनार्थ आये थे। यहाँ वे लोग कुछ दिन ठहरे थे।
यहाँ पर मोतीचंद ने मेरे द्वारा रचित ‘‘उषावंदना’’ पुस्तिका दस हजार प्रति छपाने का निर्णय किया और प्रकाशचंद के परिवार से ही व्यवस्था करा ली तथा एक ‘जैन ज्योतिर्लोक’ पुस्तक भी छपा रहे थे जिसको प्रकाश ने पिताजी के नाम से कर दिया। प्रकाशचंद ने कहा-मैं घर जाकर रुपये भेज दूँगा।
माधुरी पर संस्कार
== यहाँ पर मेरे पास कु. सुशीला, शीला, कला आदि गोम्मटसार जीवकाण्ड पढ़ रही थीं और कातन्त्र व्याकरण भी पढ़ती थीं। मैंने कु. माधुरी की बुद्धि कुशाग्र देखकर उसे वही गोम्मटसार और व्याकरण पढ़ाना शुरू कर दिया, साथ ही यह भी समझाना शुरू कर दिया कि- ‘‘तुम कुछ दिन यहाँ रहकर धार्मिक अध्ययन कर लो, फिर घर चली जाना।’
एक बार माधुरी और मंजू के मन में भी यह बात जंच गई पुनः वे प्रकाशचंद के जाते समय संघ में नहीं रह सकीं और साथ ही साथ घर चली गर्इं। उस समय माधुरी की उम्र १०-११ वर्ष की थी। घर पहुँचते ही पिता ने माधुरी को छाती से चिपका लिया और बोले- ‘‘बिटिया! तुम माताजी के पास नहीं रहीं, बहुत अच्छा किया ।
वहाँ संघ में मैं मध्यान्ह १ बजे से ४ बजे तक मुनिश्री दयासागरजी, श्री अभिनंदनसागर जी, श्री संयमसागर जी, श्री बोधिसागरजी, श्री निर्मलसागरजी, श्री महेन्द्रसागर जी, श्री संभवसागर जी और श्री वर्धमानसागर जी को गोम्मटसार जीवकांड, कल्याणमंदिर आदि ग्रंथों का स्वाध्याय कराती थी, इसमें आर्यिकायें भी बैठती थीं तथा मोतीचंद भी बैठते थे।
आहार के बाद अपने स्थान पर कुछ आर्यिकाओं को प्राकृत व्याकरण पढ़ाती। प्रतिदिन प्रातः ७ बजे से ९.३० बजे तक मुनिश्री अभिनन्दनसागरजी, श्री वर्धमानसागर जी आदि को तथा आर्यिका आदिमती जी, अभयमती जी को और मोतीचन्द को तत्त्वार्थ राजवार्तिक और अष्टसहस्री पढ़ाती। मेरी सारी दिनचर्या बहुत ही व्यस्त रहती।’’
टिकैतनगर में जब माधुरी ने मेरे पास पढ़ी हुई गोम्मटसार की ३४ गाथाएँ आचार्य सुबलसागरजी को कंठाग्र सुनाई, तो वे हर्षविभोर हो गये और बोले- ‘‘इन माता मोहिनी की कूख से जन्म लिये सभी संतानों को बुद्धि का क्षयोपशम विरासत में ही मिला है। प्रत्येक पुत्र-पुत्रियों की बुद्धि बहुत ही तीक्ष्ण है।’’
इस प्रकार आचार्य सुबलसागरजी महाराज माधुरी से प्रतिदिन गोम्मटसार की वे ३४ गाथाएँ कंठाग्र सुना करते थे और गद्गद हो जाया करते थे।
अष्टसहस्री अनुवाद
यहाँ मोतीचंद से मैंने बम्बई परीक्षालय की शास्त्री परीक्षा का फार्म भरा दिया था और कलकत्ता की बंगीय संस्कृत शिक्षा परिषद परीक्षालय से न्यायतीर्थ का फार्म भरा दिया था। इन दोनों कोर्स में अष्टसहस्री ग्रंथ था। यह न्याय का उच्चतम ग्रंथ था। इसकी संस्कृत भी बहुत कठिन थी। मोतीचन्द ने कई बार कहा-
‘‘माताजी! इस ग्रंथ को मूल से पढ़कर मैं परीक्षा नहीं दे सकता हूँ।’’ मैंने उस ग्रंथराज की हिन्दी करना शुरू कर दिया। प्रारंभ में कुछ ही पृष्ठों का हिन्दी अनुवाद हुआ था। देखकर मोतीचन्द तो प्रसन्न हुए ही, साथ ही पं. भंवरलालजी न्यायमूर्ति, जो कि ‘जिनस्तवनमाला’ आदि मेरी स्तुतिरचना की पुस्तक को अपनी प्रेस में छाप रहे थे, आते-जाते रहते थे, ये बहुत ही प्रसन्न हुए।
यहाँ के संस्कृत विद्यालय के प्राचार्य पं. गुलाबचन्द जैन दर्शनाचार्य बहुत ही प्रसन्न हुए। पं. इन्द्रलालजी शास्त्री भी मेरे पास आते रहते थे। कुल मिलाकर जयपुर के ७-८ विद्वानों ने आकर मेरा अनुवाद देखा और बार-बार प्रार्थना करने लगे- ‘‘माताजी! इस ग्रंथ का हिन्दी अनुवाद आपसे बढ़िया कोई नहीं कर सकता है। अब आप इसे छोड़ना नहीं, इसको पूर्ण करके ही छोड़ना।
यह एक महान् कार्य होगा।’’ मैं अपने अनुवाद किये हुए हिन्दी के पेजों से इन लोगों को पढ़ाकर, सुविधा से अर्थ हृदयंगम करा देती थी। सन् १९७० में टोंक चातुर्मास के बाद मैंने टोडारायसिंह गांव में पौष शुक्ला १२ को इस ग्रंथ के अनुवाद को पूरा किया था, उसी समय मैंने इस ग्रंथ के साररूप में चौवन सारांश बनाये थे, जिनको पढ़कर सन् १९७२ में त्रिशला, माधुरी, मालती, रवीन्द्रकुमार मोतीचन्द आदि सभी शिष्यों ने शास्त्री की परीक्षाएँ उतीर्ण की थीं।
इस ग्रंथ के अनुवाद के मध्य मुझे जुकाम, खांसी वर्षों रहा है। डाक्टर, वैद्यों का कहना था कि ‘‘माताजी को झुककर लिखना, मस्तिष्क से इतना अधिक काम लेना बंद कर देना चाहिए। तभी जुकाम नियंत्रण में आयेगा।’’ किन्तु मैंने किसी की भी न सुनकर इस ग्रंथ का अनुवाद पूरा करके ही चैन ली थी।
उसमें कारण यही था कि अष्टसहस्री ग्रंथ के अनुवाद के समय मुझे एक विशेष ही आनंद का अनुभव हो रहा था। सम्यग्दर्शन की निर्मलता के साथ-साथ श्रीजिनेन्द्रदेव के प्रति महान अनुराग बढ़ता ही जाता था जो कि शब्दों में लिखना अशक्य ही है।
जैन ज्योतिर्लोक शिविर
यहाँ जैन दर्शन विभाग के प्राचार्य पं. गुलाबचंद जैन मेरे निकट आते रहते थे। इन्हें जैन भौगोलिक विषय से अच्छा प्रेम था। अनेक चर्चायें और शंका समाधान किया करते थे। कई एक विद्वानों की इच्छा से यहाँ मैंने आचार्यश्री की आज्ञा लेकर पन्द्रह दिन का ‘जैन ज्योतिर्लोक’ पर शिक्षण शिविर का आयोजन किया।
सभी विद्वान् और श्रेष्ठीवर्ग कापी-पेन लेकर बैठते थे। मैं मुख्यतया ‘लोक विभाग’ नामक ग्रंथ के आधार से इस ज्योतिर्लोक के विषय में शिक्षण देती थी। लोगों को जैन शास्त्राधार से सूर्य, चंद्र, नक्षत्र आदि के विमान, गमन आदि का ज्ञान प्राप्त कर बड़ा आनंद आ रहा था। इस विषय को शिविर में मोतीचन्द ने भी अच्छी तरह से समझा था तथा अपनी कापी में लिखा था।
शिविर के बाद मैंने उस कापी का संशोधन करके इसे पुस्तक का रूप बना दिया तभी मोतीचन्द ने उसको ‘जैन ज्योतिर्लोक’ नाम से छपाया था। उसके कवर का चित्र नक्षत्र, तारामंंडल और चंद्रमा से सुन्दर बनवाया था। उसका दूसरा संस्करण भी दिल्ली में छप चुका है। यह पुस्तक अत्यधिक लोकप्रिय रही है।
दशलक्षण पर्व
दशलक्षणपर्व में श्रावकोें ने उसी बक्सी के चौक में पांडाल बनवाया, वहीं प्रतिदिन आचार्यश्री का प्रवचन रखा गया था। पर्व के पूर्व आचार्यश्री ने मुझे बुलाकर कहा- ‘‘माताजी! आप राजवार्तिक पढ़ाती हैं इसलिए दशों दिन आप तत्त्वार्थ सूत्र की एक-एक अध्याय का अर्थ सहित विवेचन करें। मैं एक-एक धर्म पर प्रवचन करूँगा।’’
मैंने कहा-‘‘ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा हो वैसा ही मैं करूँगी।’’ इस निर्णय से यहाँ के अनेक विद्वान् बहुत ही प्रसन्न हुए और मेरे पास आकर बोले- ‘‘माताजी! हम सभी विद्वान् आपके मुख से तत्त्वार्थसूत्र का प्रवचन सुनना चाहते हैं। चूँकि आप राजवार्तिक, श्लोकवार्तिक आदि ग्रंथों के आधार से अधिकरूप में सिद्धान्त, न्याय और भूगोल, खगोल पर प्रकाश डालेंगी।’’
उज्जैन के पं. सत्यंधर कुमार जी आदि भी आये हुए थे, वे भी यहाँ पर्व में रुकने को तैयार हो गये। इधर एक महानुभाव (ब्रह्मचारी जी) ने आकर आचार्यश्री से कहा-‘‘महाराज जी! आप तत्त्वार्थसूत्र पर प्रवचन करें और एक-एक साधु-साध्वियों से एक-एक धर्म पर प्रवचन करावें। ज्ञानमती जी से ही तत्त्वार्थसूत्र पर प्रवचन नहीं कराना है’’
आचार्यश्री सरल स्वभावी थे अतः उन महानुभाव की भी बात मान ली। मैंने जरा भी चिंता या ऊहापोह नहीं किया। विद्वान वर्ग को ऐसा निर्णय बदला गया मालूम होते ही वे कई लोग मिलकर मेरे पास आकर निवेदन करने लगे- ‘‘माताजी! हम लोग अन्य किसी मंदिर में आपका तत्त्वार्थ सूत्र पर प्रवचन कराना चाहते हैं.।’’
मैंने उन्हें प्रेम से समझाकर मना कर दिया और कहा- आप लोग आचार्यश्री के मुख से सूत्र का प्रवचन सुनें। इनका अनुभव ज्ञान मेरी अपेक्षा भी विशेष है, मेरा तो कोरा न्याय और व्याकरण में शाब्दिक ज्ञान है इत्यादि।’’ पुनः इन विद्वानों में से शायद ही कोई एक-दो विद्वान किसी दिन आये हों। बल्कि ये लोग यह कहने लगे- ‘‘अकारण ही ईष्र्यालु लोगों ने हम लोगों के लिए अंतराय का काम कर दिया ।’’
शांतिबाई की दीक्षा
खानिया में एक कन्या कु. शांतिबाई मुजफ्फरनगर की मेरे पास आई थी। वह ब्रह्मचर्यव्रत धारण किये हुए थी। मेरे पास रहकर अध्ययन करना चाहती थी। मैंने आचार्यश्री से आज्ञा लेकर उसे अपने पास रखा। अध्ययन कराना शुरू कर दिया। इसका क्षयोपशम अच्छा था। धीरे-धीरे उसे वैराग्य की ओर मोड़ दिया।
तब वह इसी चातुर्मास में दीक्षा लेने के लिए तैयार हो गई। आचार्यश्री ने स्वीकृति दे दी। यहाँ की समाज ने उस ब्रह्मचारिणी का अच्छा सम्मान किया, उसकी बिंदोरी-शोभायात्रा भी कई दिन तक निकाली गई। अच्छी प्रभावना हुई। उसकी आर्यिका दीक्षा हुई और नामकरण ‘जयमती’ किया गया। ये आर्यिका जयमती कई वर्ष मेरे पास रही हैं, धार्मिक अध्ययन किया है। तपश्चर्या की शक्ति अच्छी थी।
८-८ उपवास करके सीढ़ियाँ चढ़ना, जोर-जोर से बोलना देखकर मैं सोचती- ‘‘इसका पूर्व पुण्य है। मैं तो एक उपवास करके ही सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाती हूँ, बोलने की शक्ति घट जाती है।’’ ये आर्यिका सन् १९७१ में मुनिश्री सुपार्श्वसागर जी के संघ के साथ सम्मेदशिखर की यात्रा के लिए गई थीं पुनः आ गई थीं। यहाँ सन् १९७४ में उसी संघ के साथ वापस आकर संघ में शामिल हो गई थीं पुनः सन् १९७५ में इधर अलग होकर विहार करने लगीं जो कि हम लोगों को इष्ट नहीं था क्योंकि संघ में अनुशासन में रहने से ही आत्महित होता है।
इधर कहीं विहार के समय मार्ग में बस की टक्कर से एक्सीडेंट हो जाने से वे बहुत घायल हो गई थीं तब इनकी दीक्षा छूट गई थी, मुजफ्फरनगर में इलाज चलता रहा था। बाद में स्वस्थ होने पर पुनः मुनिश्री जयसागर जी से आर्यिका दीक्षा ले ली है। अभी सन् १९८८ में जनवरी में मैंने सुना कि ये आर्यिका यहाँ हस्तिनापुर में बड़े मंदिर पर आकर ठहरी हुई हैं। इधर न जंबूद्वीप के दर्शन करने आर्इं और न मेरे पास ही आर्इं।
किसी ने बताया कि चोट आने के बाद उनके मस्तिष्क में कुछ कमी हो गई है। कुछ भी हो- ‘‘ऐसी बीमारी या आपत्ति विशेष में स्थितीकरण, उपगूहन, संरक्षण आदि के लिए ही तो आचार्यों ने साधुओं को-मुनियों को संघ में रहने का आदेश दिया है, एकाकी रहने का सर्वथा विरोध किया है पुनः आर्यिकाओं के लिए तो एकाकी विहार करने की आज्ञा कथमपि नहीं है और जो इस आज्ञा का पालन नहीं करते हैं उनको ऐसे ही प्रसंग प्राप्त होते हैं। ऐसे-ऐसे उदाहरण देखकर मन में बहुत ही दुख होता है किन्तु क्या उपाय है?
इस कलिकाल में गुरुजनों के अनुशासन में रहने वाले विरले ही पुण्यशाली जीव हैं, ऐसा समझना चाहिए। गुरुआज्ञा को उल्लंघन करने का दुष्परिणाम एक मुझे स्मरण में आ जाता है तो रोमांच हो जाता है। एक बाल विधवा महिला सन् १९५७ में खानिया में आई। वह संघ में रहकर पढ़ना चाहती थी। आचार्यश्री वीरसागर जी ने मुझे बुलाकर कहा-इसे अपने पास रखो और पढ़ाओ तथा अनुशासन में रखो। मैंने प्रेम से उसे छहढाला, तत्त्वार्थसूत्र आदि पढ़ाना शुरू किया।
दशलक्षण पर्व में वह दश उपवास करना चाहती थी। मैंने दो उपवास गुरुदेव से दिला दिये। अगले दिन चर्चा हुई, उसने कहा-मैं व्रत या उपवास में कुल्ला नहीं करूँगी। यह बात संघस्थ वयोवृद्धा आर्यिका श्री सुमतिमती माताजी को मालूम हुई। उन्होंने कहा- बिना कुल्ला किये न भगवान का अभिषेक-पूजन कर सकती हो, न आहारदान।
वह महिला जिद पर अड़ी रही, बात बढ़ गई। आर्यिका श्री वीरमती माताजी आदि ने, ब्र. सूरजमलजी ने भी समझाया। सभी बोले- देखो बाई! तुम्हारी छोटी उम्र है, अनुशासन में रहो, आज्ञा पालो, तब तो इहभव व परभव सुधरेगा अन्यथा पुनः डूब जावोगी। उसने किसी की न मानी, तब बात दोनों आचार्यों तक गई।
आचार्यश्री वीरसागर जी और आचार्य श्री महावीरकीर्तिजी ने भी समझाया। उसे आगम प्रमाण भी दिखाये गये, किन्तु वह महिला दुराग्रह में ही अटल रही। अन्ततोगत्वा आचार्यश्री ने कहा कि- ‘‘इसे संघ से निकाल दो।’’ उसे संघ से निकाल दिया गया। कुछ दिन बाद उसने एक तेरहपंथी मुनिराज से क्षुल्लिका दीक्षा ले ली। कुछ दिन बाद एकल विहारी हो गई।
उसने दीक्षा छोड़ दी थी, अब साधारण महिला के रूप में रहती है। अभी सन् १९८७ में यहाँ हस्तिनापुर आई थी। बड़े मंदिर पर ठहरी थी। यहाँ आई, मैंने पहचान लिया। वह बहुत दुःखी होकर बोली- ‘‘माताजी, मेरी बहुत बड़ी दुरावस्था है।’’ मैंने पूछा-कहाँ रहती हो? उसने कहा-‘‘जबलपुर।’’ मैंने पूछा-‘‘खाने-पीने की व्यवस्था क्या है?’’
उसने बताया-‘‘वहीं बच्चों के लिए गोलियाँ बेचकर कुछ पैसे कमाकर, अपना उदर पोषण करती हूँ।’’ इत्यादि करुण कथा सुनकर मेरा हृदय करुणा से भर आया और पुरानी स्मृति आकर दुराग्रह का दुष्परिणाम सामने दिखने लगा। मैं कुछ भी नहीं बोल सकी, सोचती ही रह गई। देवपूजन, दान करने वाले श्रावक-श्राविकाओं के लिए सागारधर्मामृत व सोमदेवसूरि कृत यशस्तिलकचंपू में आचमन-कुल्ला करने के-मुख शुद्धि के प्रमाण हैं।
आप्लुतः संप्लुतस्वान्तः शुचिवासो विभूषितः।
मौनसंयमसंपन्नः कुर्याद्देवार्चनाविधिम् ।।४३८।।
दंतधावनशुद्धास्यो मुखवासोचिताननः।
असंजातान्यसंसर्गः सुधीर्देवानुपाचरेत् ।।४३९।।(यशस्तिलक चंपू)
तात्पर्य यह है कि-स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहने और चित्त को वश में करके मौन तथा संयमपूर्वक जिनेंन्द्रदेव की पूजा करे। दंतधावन से मुख शुद्ध करके दूसरों को न छूकर जिनेंद्रदेव की पूजा करे। आचार्य श्री वीरसागर जी महाराज कहते थे- उपवास में भी कुल्ला करके ही पूजन करना चाहिए, मंजन या दातोन नहीं करना चाहिए।
मुनिगण आहार के बाद बैठकर मुख शुद्धि करते हैं। अंतराय के बाद पानी नहीं पीते हैं किन्तु मुखशुद्धि-कुल्ला करते हैं अतः कुल्ला करने से पानी पीने का दोष नहीं आता है। आचार्य श्री शिवसागर जी, आचार्यश्री धर्मसागर जी, आचार्यश्री महावीर कीर्तिजी, आचार्यश्री विमलसागर जी आदि आचार्यश्री शान्तिसागर जी की परम्परा के साधु-साध्वियों की यही मान्यता है।
मेरी तथा आर्यिका सुपार्श्वमती जी एवं आर्यिका विजयमती जी की भी यही मान्यता है।
एक ब्राह्मण वैद्य
जयपुर में संघ में किसी भी साधु-साध्वी की बीमारी में प्रायः मुझे वैद्यों को बुलाकर औषधि उपचार कराना होता था। एक बार एक साधु की बीमारी से एक जैन वैद्य ने ‘कामदुधा’ रस दवा बतलाई। मैं प्रारंभ से साधुओंं की दवाई के बारे में दवाई का नाम और उसमें क्या-क्या चीजे हैं? कैसे बनी हैं? इत्यादि समझे वगैर किसी को दवा नहीं दिलाती थी अतः कुछ-कुछ दवाइयों के नाम और इसमें क्या-क्या है? इत्यादि का थोड़ा सा ज्ञान मुझे भी था।
मैंने उसी क्षण कहा- ‘‘वैद्य जी! इसमें कौड़ी और सीप की भस्म पड़ती है अतः यह दवा जैन साधुओं के काम नहीं आ सकती।’’ इतनी सी बात पर बता नहीं क्यों, वे वैद्यजी खूब ही गरम हो गये, तब से मैंने उन वैद्य को बुलाना ही बंद कर दिया। वहाँ जयपुर में एक वैद्य ब्राह्मण थे, उनका नाम था ‘रामदयाल जी’। वे बहुत ही सरल स्वभावी थे।
प्रायः औषधि का नुसखा लिख देते, संघस्थ ब्रह्मचारी अथवा श्रावक उन दवाइयों को लाकर देख-शोध कर कूट-पीस कर साधु-साध्वियों के आहार में पहुँचा देते थे। उनमें एक विशेषता यह थी, वह यहाँ ज्ञातव्य है- खानिया में एक बार एक ब्रह्मचारिणी को गर्मी के दिनों में लघुशंका नहीं हुई। दो दिन बाद रात्रि में जब उसका पेट फूल गया, तब छटपटाने लगी और मुझे सूचना मिली, तब मैंने रात्रि में ही जैसे-तैसे प्रयास करके वैद्य रामदयाल को बुलवाया।
ये वैद्यजी आये और बोले- ‘‘भक्तामरस्तोत्र का पाठ शुरू करो, सब लोग भक्तामर बोलो।’’ मुझे बड़ा अटपटा लगा। मैं मन में सोचने लगी- ‘‘हम लोग पाठ तो इतनी देर से बोल ही रहे थे, इन्हें तो उपचार के लिए बुलाया है।…’’
फिर मैंने कहा-‘‘वैद्यजी! कुछ इलाज बताओ, पाठ तो हम लोग सुना ही रहे हैं। वे बोले-‘‘कुछ नहीं, सबसे बड़ी दवा तो भक्तामर ही है’’ और वे स्वयं भक्तामर बोलने लगे। उनका उच्चारण बहुत शुद्ध था और उन्हें यह पूरा कंठाग्र था। बाद मेें उन्होंने उस लड़की को पानी से भरे ‘टब’ में बैठाया। चूँकि रात्रि में कुछ खाने की दवा दे नहीं सकते थे अतः कुछ पेट पर लेप भी कराया। उस ब्रह्मचारिणी बालिका को लघुशंका हो गई। कुछ शांति आ गई।
ऐसे कई बार इनके मुख से भक्तामर सुनकर एक दिन मैंने पूछ ही लिया- ‘‘वैद्य जी! आप तो ब्राह्मण हैं, आपको भक्तामर स्तोत्र के प्रति इतनी श्रद्धा कैसे हुई है?’’ उन्होंने कहा-‘‘मुझे विरासत में यह स्तोत्र मिला है। मेरे पिताजी को यह स्तोत्र बहुत ही प्रिय था। इसको पढ़कर मैं किसी भी रोगी को दवा देता हूँ तो उसे अवश्य ही लाभ करती है।
इसलिए मेरी औषधि की आज इतनी प्रसिद्धि हो रही है.।’’ इन वैद्य को मैंने सन् १९७६ में खतौली में आर्यिका रत्नमती माताजी के इलाज के लिए भी बुलाया था। अब तो वे स्वर्गस्थ हो चुके हैं। उनके उस प्रसंग से मुझे बहुत प्रसन्नता हुई थी। वैसे पहले से ही मैं हर किसी डॉक्टर को, जो कि अपने निकट आते थे, उन्हें शिक्षा दिया करती थी कि-‘‘
आप लोग रोगी को ‘ॐ नमः’ मंत्र दिया करो, चूँकि यह ‘लघुमंत्र’ सर्वसम्प्रदाय मान्य है और महाशक्तिशाली है। इसके साथ मेरा कहना यह रहा है कि- ‘‘आप डाक्टर-वैद्य आदि रोगी को यह कह दो कि मांस, मछली, अण्डे खाने से या शराब पीने से आपका यह रोग ठीक नहीं हो सकता है, तब वे रोगी अवश्य ही इन वस्तुओं का त्याग करने को तैयार हो जायेंगे।’’
मेरी यह शिक्षा दिल्ली में कई जैन डॉक्टरों ने मानी है और यह नियम लिया है कि ‘‘मैं औषधि के लिए भी अण्डे अथवा शराब का प्रयोग नहीं बतलाऊँगा ।’’ यहाँ पर अनेक धर्मप्रभावनात्मक कार्यों के साथ चातुर्मास संपन्न हो गया। उसके बाद आचार्यश्री दीवानजी की नशिया में आ गये। कुछ दिनों यहीं पर ठहरे थे।
