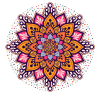बड़ी जयमाला
-दोहा-
अति अद्भुत लक्ष्मी धरें, समवसरण प्रभु आप।
तुम धुनि सुन भविवृन्द नित, हरें सकल संताप।।१।।
-शंभु छंद-
जय जय त्रिभुवनपति का वैभव, अन्तर का अनुपम गुणमय है।
जो दर्श ज्ञान सुख वीर्यरूप, आनन्त्य चतुष्टय निधिमय है।।
बाहर का वैभव समवसरण, जिसमें असंख्य रचना मानीं।
जब गणधर भी वर्णन करते, थक जाते मनपर्यय ज्ञानी।।२।।
यह समवसरण की दिव्यभूमि, इक हाथ उपरि पृथ्वीतल से।
द्वादश योजन उत्कृष्ट कही, इक योजन हो घटते क्रम से।।
यह भूमि कमल आकार कही, जो इन्द्रनीलमणि निर्मित है।
है गंधकुटी इस मध्य सही, जो कमल कर्णिका सदृश है।।३।।
पंकज के दल सम बाह्य भूमि, जो अनुपम शोभा धारे है।
इस समवसरण का बाह्य भाग, जो अनुपम शोभा धारे है।।
सब बीस हजार हाथ ऊँचा, यह समवसरण अतिशय शोभे।
एकेक हाथ ऊँची सीढ़ी, सब बीस हजार प्रमित शोभे।।४।।
पंगू अन्धे रोगी बालक, औ वृद्ध सभी जन चढ़ जाते।
अंतर्मुहूर्त के भीतर ही, यह अतिशय जिनआगम गाते।।
इसमें शुभ चार दिशाओं में, अति विस्तृत महावीथियाँ हैं।
वीथी में मानस्तम्भ कहे, जिनकी कलधौत पीठिका हैं।।५।।
इक योजन से कुछ अधिक तुँग, बारह योजन से दिखते हैं।
इनमें हैं दो हजार पहलू, स्फटिक मणी के चमके हैं।।
उनमें चारों दिश में ऊपर, सिद्धों की प्रतिमाएँ राजें।
मनस्तम्भों की सीढ़ी पर लक्ष्मी की मूर्ति अतुल राजें।।६।।
ये अस्सी कोशों तक सचमुच, अपना प्रकाश पैâलाते हैं।
जो इनका दर्शन करते हैं, वे निज अभिमान गलाते हैं।।
ये प्रभु का सन्निध्य पा करके, ही मान गलित कर पाते हैं।
अतएव सभी अतिशय भगवन्! तेरा ही गुरुजन गाते हैं।।७।।
प्रभु समवसरण में द्वादश गण, बैठे क्रम से ध्वनि सुनें सभी।
पहले में गणधर गण मुनिगण, दूजे में कल्पवासि देवी।।
तीजे में आर्यिका श्राविकायें, चौथे में भवनवासि देवी।
पंचम में व्यंतरनी, छट्ठे में बैठी ज्योतिष्की देवी।।८।।
सप्तम में भावनसुर, अष्टम में व्यंतर, नवमें ज्योतिष सुर।
दशवें में कल्पवासि सुर हैं, ग्यारहवें चक्री श्रावक नर।।
बारहवें में पशुगण बैठे, सब बाधा रहित बैठते हैं।
संख्यात मनुज तिर्यंच, असंख्याते सुरवृंद तिष्ठते हैं।।९।।
अठरह महाभाषा सातशतक, क्षुद्रक भाषामय दिव्य धुनी।
उस अक्षर अनक्षरात्मक को, संज्ञी जीवों ने आन सुनी।।
तीनों संध्या कालों में वह, त्रय त्रय मुहूर्त स्वयमेव खिरे।
गणधर चक्री अरु इन्द्रों के, प्रश्नोंवश अन्य समय भि खिरे।।१०।।
भव्यों के कर्णों में अमृत, बरसाती शिवसुखदानी है।
चैतन्य सुधारस की झरणी, दुखहरणी यह जिनवाणी है।।
जन चार कोश तक उसे सुनें, निज निज के सब कर्त्तव्य गुने।
नित ही अनंत गुण श्रेणिरूप परिणाम शुद्ध कर कर्म हने।।११।।
छह द्रव्य पाँच है अस्तिकाय, अरु तत्त्व सात नव पदार्थ भी।
इनको कहती ये दिव्यध्वनि, सब जन हितकर शिवमार्ग सभी।।
आनन्त्य अर्थ के ज्ञान हेतु जो बीज पदों का कथन करे।
अतएव अर्थकर्ता जिनवर उनकी ध्वनि मेघ समान खिरे।।१२।।
उन बीजपदों में लीन अर्थ प्रतिपादक बारह अंगों को।
गणधर गूँथे अतएव ग्रंथकर्ता मानें वंदूँ उनको।।
जिन श्रुत ही महातीर्थ उत्तम, उसके कर्ता तीर्थंकर हैं।
वे सार्थक नाम धरें जग में, इससे तिरते भवसागर हैं।।१३।।
जय जय प्रभुवाणी कल्याणी, गंगाजल से भी शीतल है।
जय जय शमगर्भित अमृतमय, हिमकण से भी अति शीतल है।
चंदन अरु मोतीहार चंद्रकिरणों से भी शीतलदायी।
स्याद्वादमयी प्रभु दिव्यध्वनी, मुनिगण को अतिशय सुखदायी।।१४।।
वस्तू में धर्म अनंत कहे, उन एक एक धर्मों को जो।
यह सप्तभंगि अद्भुत कथनी, कहती है सात तरह से जो।।
प्रत्येक वस्तु में विधि निषेध, दो धर्म प्रधान गौण मुख से।
वे सात तरह से हों वर्णित, नहिं भेद अधिक अब हो सकते।।१५।।
प्रत्येक वस्तु है अस्तिरूप, अरु नास्तिरूप भी है वो ही।
वो ही है उभयरूप समझो, फिर अवक्तव्य भी है वो ही।।
वो अस्तिरूप अरु अवक्तव्य, फिर नास्ति अवक्तव भंग धरे।
फिर अस्तिनास्ति अरु अवक्तव्य, ये सात भंग हैं खरे खरे।।१६।।
इस सप्तभंगमय सिंधू में, जो नित अवगाहन करते हैं।
वे मोह राग द्वेषादि रूप, सब कर्म कालिमा हरते हैं।।
वे अनेकांतमय वाक्य सुधा, पीकर आतमरस चखते हैं।
फिर परमानंद परमज्ञानी होकर, शाश्वत सुख भजते हैं।।१७।।
मैं निज अस्तित्व लिये हूँ नित, मेरा पर में अस्तित्व नहीं।
मैं चिच्चैतन्य स्वरूपी हूँ, पुद्गल से मुझ नास्तित्व सही।।
इस विध निज को निज के द्वारा, निज में ही पाकर रम जाऊँ।
निश्चयनय से सब भेद मिटा, सब कुछ व्यवहार हटा पाउँ।।१८।।
भगवन्! कब ऐसी शक्ति मिले, श्रुतदृग से निज को अवलोवूँ।
फिर स्वसंवेद्य निज आतम को, निज अनुभव द्वारा मैं खोजूँ।।
संकल्प विकल्प सभी तज के, बस निर्विकल्प मैं बन जाऊँ।
फिर केवल ‘ज्ञानमती’ से ही, निज को अवलोवूँâ सुख पाऊँ।।१९।।
—दोहा—
जिनवर समवसरण अतुल, अतिशय गंगा तीर्थ।
इसमें अवगाहन करूँ, बन जाऊँ जग तीर्थ।।२०।।
ॐ ह्रीं अर्हं समवसरणविभूतिमंडिताय श्रीऋषभदेवतीर्थंकराय जयमाला पूर्णार्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा।
शांतये शांतिधारा। दिव्य पुष्पांजलि:।
—नरेन्द्र छंद—
ऋषभदेव के समवसरण को, जो जन पूजें रुचि से।
मनवांछित फल को पा लेते, सर्व दुखों से छुटते।।
धर्मचक्र के स्वामी बनते, तीर्थंकर पद पाते।
केवल ‘ज्ञानमती’ किरणों से भविमन ध्वांत नशाते।।१।।
।।इत्याशीर्वाद:।।
प्रशस्ति
-शंभु छंद-
श्री ऋषभदेव को वंदन कर, श्री वीरप्रभू के चरण नमूँ।
श्री गौतम गणधर देव नमूँ, श्री सरस्वती माँ को प्रणमूँ।।
श्री ऋषभदेव की जन्मभूमि, वरतीर्थ अयोध्या को प्रणमूँ।
प्रभु दीक्षा अरु वैâवल्यभूमि, शुभ जैन प्रयाग तीर्थ प्रणमूँ।।१।।
फाल्गुन कृष्णा एकादशि को, वैâवल्यज्ञान से धन्य किया।
इस युग में पहला समवसरण, धनपति ने रचकर पुण्य लिया।।
वटवृक्ष तले केवलज्ञानी, अक्षयवटवृक्ष प्रसिद्ध हुआ।
शत इंद्र भरत चक्री श्रोता, गणधर गुरु वंदित तीर्थ हुआ।।२।।
श्री ऋषभदेव जिन तपस्थली, यह जैन तीर्थ जग मान्य बना।
द्वादशवर्षीय महाकुंभ, मस्तकाभिषेक सब मान्य घना।।
श्री ऋषभदेव का समवसरण, पूजा विधान सुंदर रचना।
सब करो करावो भव्यवृंद, पावोगे इच्छित सौख्य घना।।३।।
श्री मूलसंघ में कुंदकुंद आम्नाय सरस्वति गच्छ कहा।
विख्यात बलात्कारगण से, गुरु आम्नायों में मुख्य रहा।।
इस परम्परा के आचार्यों का, मैं नित वंदन करती हूँ।
बीसवीं सदी के प्रथम सूरि, श्री शांतिसिंधु को नमती हूँ।।४।।
उन पट्टाचार्य सुशिष्य प्रथम, श्री वीरसागराचार्य हुए।
गुरुवर्य आर्यिका दीक्षा दे मुझ ज्ञानमती१ को धन्य किये।।
वीराब्द पच्चीस सौ उनतालिस२, वर माघ शुक्ल दशमी तिथि में।
‘ऋषभेश्वर समवसरणविधान’ रचना को पूर्ण किया मैंने।।५।।
-दोहा-
हस्तिनागपुर में हुए, शांतिनाथ भगवान।
कुंथुनाथ अरनाथ के, चार-चार कल्याण।।६।।
तीनों तीर्थंकर प्रभू, कामदेव चक्रीश।
तीन तीन पद के धनी, नमूँ नमूँ नत शीश।।७।।
जब तक जग में रवि शशी, तब तक श्री जिनधर्म।
यह विधान कृति जगत को, देवे शिवपथ मर्म।।८।।