स्याद्वाद चन्द्रिका में उद्धरण-वैभव
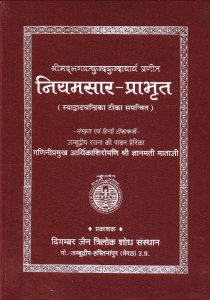
लोक में जैसे धन, ऐष्वर्य वैभव किसी व्यक्ति की प्रतिश्ठा में चार चांद लगा देते हैं तथा उसका जीवन सुसंस्कृत एवं श्रेयस्कर रूप में समृद्ध होता है, उसी प्रकार किसी रचनाकार की साहित्य रचना में विवक्षित अर्थ के पोशक उद्धरणों का वैभव उसकी श्री वृद्धि करता है। जैन वाङ्मय परम्परा में टीका की विधाओं में प्रायः पूर्व ग्रंथों के अंषों का प्रस्तुतीकरण बडे़ सुन्दर ढंग से किया जाता रहा है। नियमसार की प्रस्तुत स्याद्वाद चन्द्रिका टीका में भी इसी प्रणाली का सम्यक् निर्वाह किया गया है।
इसी ग्रंथ की आचार्य पझप्रभमल धारी देव की तात्पर्य वृत्ति यद्यपि सारार्थ व्यक्त करने वाली कृति है, तथापि उसमें भी कतिपय आगमिक उद्धरण प्राप्त होते हैं। पू० माता जी की इस टीका में तो उद्धरणों की बहुलता है जिनके कारण यह महनीय कृति मूल ग्रंथ सरीखा ही जान पड़ती है। टीका कत्र्री ने शास्त्रों का सम्यक् आलोढन करके 62 ग्रंथों का इसमें उपयोग किया है। वे उद्धरण मूल गद्य ग्रंथों के, टीकाग्रंथों के, पद्यग्रंथों के एवं सूत्रों के अनुवाद स्थलों के अनेकों रूपों में प्राप्त होते हैं।
प्राकृत और संस्कृत दोनों भाशाओं के उत्कृश्ट चयनित अंषों को इसमें समाविश्ट किया गया है। प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग एवं द्रव्यानुयोग सभी का वैभव इस टीका में दृश्टिगत होता है। इसमें जहां विधिपरक सामान्य उद्धरण “शोभित है वहीं “शंका समाधान के रूप में भी प्रकट किये गये हैं जिससे टीका का सौंदर्य द्विगुणित हो गया है।
इन उद्धरणों से, प्रायः न्याय, आचरण, सिद्धान्त, दर्षन, अध्यात्म, वैराग्य एवं शंत रस तथा भूगोल आदि का परिपाक विलसित रूप में हुआ है। अपने नाम के अनुरूप ही इस टीका में अनेकान्त एवं स्याद्वाद के निरूपक ग्रंथों के महत्वपूर्ण अंषों को सर्वाधिक स्थान दिया गया है। सूक्तियां, कहावतें और मुहावरों का प्रयोग भी टीका को मुखरित करता हुआ विदित होता है। कुल मिलाकर इस उपरोक्त प्रणाली को सफल शैली कहा जा सकता है। इसके द्वारा ही सामान्य जनों को भी सरलता से ग्रंथ का विशय हृदयंगम कराया जा सकता है।
माता जी ने स्वयं ही गाथा क्रमांक 185 के अंतर्गत कहा है कि उन्होंने जिनागम सूत्र रूपी मणियों को चुन चुनकर इस टीका में प्रयुक्त किया है। मणि तो सर्वत्र सौंदर्य-कारक होती है, प्रकाषक होती है तिमिरनाषक होती है एवं अलंकार रूप होती है। उद्धरणों का यही रूप प्रस्तुत टीका में पद-पद पर इसे अलंकृत करता प्रतीत होता है। मैं समझता हूं कि यदि इस टीका से उद्धरणों को पृथक कर दिया जाय तो यह अधूरी एवं श्री न्यून ही कही जायेगी। आचार्यों के कोई वचन स्वयं तो बोलते नहीं हैं
वे तो स्वयं वाच्य मात्र हैं। वक्ता ही उनका प्रयोग करता है। यदि यथास्थान उनका प्रयोग होता है तो वे सुषोभित होते हैं एवं प्रकृत रचना को “शोभा प्रदान करते हं। इसमें प्रयोजक की मुख्य भूमिका, प्रयोग हेतु सावधानी की होती है। पू० माता जी ने बडे़ कौषल से यथा प्रकरण प्रासंगिक रूप में उनको प्रस्तुत किया है। यह उनकी मनीशा, कुषाग्रबुद्धि और कुषलता है।
रचना पर दृश्टिपात करने से ज्ञात होता है कि मानो उनके सामने स्वयं शास्त्रांष अपेक्षित रूप में आकर कहते हों कि हमें प्रयोग करो, हमें प्रयोग करो। इस स्थिति में तो टीका में उद्धरणों की प्रचुरता होना अवष्यंभावी है ही इसमें माता जी का अगाध, समन्वित एवं बहुआयामी शास्त्र ज्ञान ही सहायक सिद्ध हुआ है। जो उनके ज्ञानमती नाम की सार्थकता को प्रकट करता है ज्ञान के लिए भी तो निमित्त कारणों की अपेक्षा रहती है सो उद्धरण ही मानो ज्ञान के सम्मुख निमित्त रूप में उपस्थित हो जाते हैं। यह विभिन्न प्रकार के उद्धरणों का रूप उनके अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग का प्रतीक है।
उनकी स्वाध्याय शीलता एवं कण्ठस्थीकरण स्वभाव का परिपाक प्रस्तुत टीका में सर्वत्र हुआ है। किसी विद्यालय में विधिवत् षिक्षा प्राप्त न करके भी इस प्रकार की विचक्षणता का गौरव उनके त्याग तपस्या का परिणाम है जिसे अति प्रषस्त ही कहा जा सकता है। ज्ञानावरण का क्षयोपषम अथवा क्षय चारित्र से ही होता है। आगम में प्रसिद्ध है कि चारित्र से, संयम से मोहनीय के नाषपूर्वक ही केवलज्ञान प्रकट होता है न कि केवलज्ञान से मोहनीय कर्म का नाष।
उद्धरणों की अपनी प्रकृति (स्वभाव ) होती है, विशय होता है। वे भी मानों खोज में रहते हैं कि उन्हें भी समुचित समादरणीय स्थान पर सुषोभित किया जाय इसी में उनकी गरिमा है। केवल रचयिता के ग्रंथ में ही सुशुप्त अवस्था में स्थानगत होने में उन्हें न आनंद है, न संतोश ही।
वे अपने मुखरित उपादान को लिए आमंत्रण हेतु आतुर, लालायित रहते हैं, उनकी यह स्थिति और प्रयोक्ता की अपनी आवष्यकता, ज्ञानाभ्यास और उन वाङ्मय की विभिन्न सूक्ति मणियों से परिचय का जब सुमेल होता है एवं प्रकृत विशय-गत अपेक्षा तथा तत्तत् ग्रंथांष की प्रकृति का संगम होता है तभी उद्धरणों का वैभव सुश्ठु रूप में प्रकट होकर रचना का वरण एवं अलंकरण करता है। इसमें लेखक या प्रयोक्ता की शोधपूर्ण दृश्टि भी प्रधान कारण है।
स्याद्वाद चन्द्रिका वस्तुतः एक ऐसी रचना बन गई है जिस पर आगमोक्त सूक्ति रूपी मणियां विशय को शोभित एवं सज्जायुक्त करती हुई, बल प्रदान करती हुई आसीन हो गई हैं। प्रस्तुत टीका पर सम्यक् दृश्टिपात करने से विदित होता है कि इन उद्धरणों ने इसे उपयोगी बनाने में, चार चांद लगाने में बहुमूल्य योगदान किया है ‘उक्तं च’ तथा ‘प्रोक्तं,’ ‘तदेव दृष्यताम्’, पष्यतु, ‘आचार्याः ऊचुः’, तथाहि आदि उत्थानिकांष रूप “शब्दों के द्वारा आर्यिका ज्ञानमती ने उन गद्यांषों एवं पद्यांषों को प्रयुक्त कर उन प्रकृत ग्रंथों को महिमामंडित किया है। उन ग्रंथों के लेखक महान पूर्व परम्पराचार्यों को अपनी विनयांजलि ही दी है। गुरूओं का गुण गौरव उन्हें सदैव अभीश्ट रहा है।
यहां हम टीका के हार्द को प्रकाषित करने हेतु एवं पाठकों के ज्ञानवद्र्धन हेतु कतिपय उद्धरणों को प्रस्तुत करना आवष्यक समझते हैं। प्रस्तुत शोधालेख में यह अति उपयोगी रहेगा। इन्हीं के द्वारा टीका का विशय पूर्ण हुआ है एवं सौश्ठव प्रकट हुआ है। टीकाकत्र्री ने 62 गंरथों का उपयोग प्रस्तुत कृति में किया है। उद्धरणों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो उन ग्रंथों ने अपने प्रतिनिधियों के रूप में उन्हें पे्रशित किया है तथा उनके प्रतीक रूप वाड्मय के वे ग्रंथ रत्न प्रस्तुत टीका में प्रतिबिम्बित ही हो रहे हैं।
स्याद्वाद चन्द्रिका में प्रथम ही नियमसार की मंगलाचरण-गाथा में प्रयुक्त पद ‘जिणं’ की टीका में मात्र एक वाक्य ‘‘अनन्तभवप्रापणहेतून् समस्तमोहरागद्वेशादीन् जयतीति जिनः।’’ जिनेन्द्र के लक्षण रूप लिखा गया है तथा आचार्य पूज्यपाद देव कृत एक अनुप्रास से अलंकृत महनीय आर्या छन्द उस लक्षण की पुश्टि हेतु प्रस्तुत किया है, दृश्टव्य है-
जितमदहर्शद्वेशा जितमोहपरीशहा जितकशायाः।
जितजन्ममरणरोगाः जितमात्सर्याः जयन्तु जिनाः।।
टीकागत वाक्य का हिन्दी अनुवाद है, ‘जो अनन्त भवों को प्राप्त कराने में कारण ऐसे सम्पूर्ण मोह-राग-द्वेश आदि को जीतते हैं वे जिन कहलाते हैं। यह प्रकृत जिन का अर्थ संक्षिप्त है। टीकाकत्र्री को अनुभव हुआ होगा कि पाठक गण को और अधिक अर्थ के निकट पहुंचाया जाय।
इस स्थल पर उन्होंने अपनी अन्य “ाब्दावली का प्रयोग न कर अपने से भी श्रेश्ठ एवं सारभूत संक्षिप्त किन्तु विस्तृत अर्थ वाले अलंकार युक्त प्रवाहमय उक्त उद्धरण को रखकर टीका की “ाोभा को वृद्धिंगत किया है।’’ जिन्होंने मद, हर्श और द्वेश को जीत लिया है मोह और परीशहों पर विजय प्राप्त की है कशायों को जीत लिया है, जन्म-मरण और रोगों को जीत लिया है एवं मात्सर्य को विजित किया है (जीतने की विषेशता होने के कारण) ऐसे जिनदेव सदा जयषील होवें। छन्द में इस अभिप्राय के सम्मिलन से विषेश स्पश्टीकरण हुआ है।
मूलग्रंथ की गाथा क्रमांक 3 निम्न प्रकार है
मग्गो मग्गफलं ति य दुविहं जिणसासणे समक्खादं।
मग्गो मोक्ख उवायो तस्स फलं होइ णिव्वाणं।।
इसकी व्याख्या करते हुए माता जी ने नियमसार प्राभ्त के अध्ययन के अधिकारीपने के प्रकरण में उल्लिखित किया है कि मुख्य रूप से मुनि हैं एवं गौण रूप से पाक्षिक, नैश्ठिक और साधक श्रावक भी हैं। श्रावक के अधिकार को सिद्ध करने हेतु उन्होंने श्रावक की मुनिधर्म, अनुरागिता को कारण मानकर उस निम्न उद्धरण में प्रकट किया है-
अथ नत्वाऽर्हतोक्षूणचरणान् श्रमणान् अपि।
तदधर्मरागिणां धर्मः सागाराणं प्रचक्ष्यते।।
इस उद्धरण की सुशमा प्रस्तुत कर टीकाकत्र्री यह प्रकट करना चाहती हैं कि कुन्दकुन्द स्वामी के निष्चय नय प्रधान समयसार, नियमसार आदि आध्यात्मिक ग्रंथों को जो लोग मुनिधर्म के प्रति भक्ति, अनुराग से रहित होकर पढ़ते हैं वे व्यवहार को सर्वथा हेय जानकर ‘इतोभ्रश्टास्ततो भ्रश्टाः’ होकर कुगति के पात्र होते हैं।
जो विशय कशायों में आकण्ठ डूबे हैं व्यवहार नय परक शास्त्रों से विमुख हैं यदि उनको पाप पुण्य की समानता जोकि आपेक्षिक है, विशयक उपदेष मिलता है तो वे पुण्य को छोड़कर पापों में और लिप्त हो जाते हैं, समस्त भोगों का सेवन करते हुए भी उनसे अपने को पृथक, अस्पृश्ट एवं शुद्ध मानते हुए भ्रमित होकर पापपंक में अत्यधिक मग्न हो जाते हैं। अतः सर्वप्रथम व्यवहार धर्म का आलम्बन चाहिए। मुनिधर्म का भक्ति रूप गृहस्थ धर्म का आचरण पाप से निवृत्ति रूप होना चाहिए तभी वे अध्यात्म ग्रंथों के मूल तत्व को यथार्थ हृदयंगम कर सकेंगे।
पू० माता जी ने स्याद्वाद चन्द्रिका की सुशमा वृद्धि हेतु गौतम गणधर देव, आचार्य पुष्पदन्त, भूतबलि, आ० कुन्दकुन्द, समन्तभद्र, उमास्वामी, पूज्यपाद, भट्टाकलंक देव, यतिवृशभ, देवसेन, आ० वीरसेन, जिनसेन आदि महान परम्पराचार्यों को उनके उद्धरणों की प्रस्तुति के माध्यम से विनयपूर्वक स्मरण किया है। तत्वार्थ राजवात्र्तिक और “लोक वार्तिक में वर्णित मोक्षमार्ग की रत्नत्रयात्मकता के प्रतिपादन हेतु एक स्थल पर उन्होंने उल्लेख किया है-
‘‘त्रयमेतत् संगतं मोक्षमार्गों नैकषो द्विषो वा इति। नहि त्रितयमन्तरेण मोक्ष- प्राप्तिरस्ति रसायनवत्।तथा न मोक्षमार्ग ज्ञानादेव मोक्षेणाभिसम्बन्धो दर्षन- चारित्राभावात्…………………..।’’
दर्षन, ज्ञान, चारित्र ये तीनों ही मिलकर मोक्षमार्ग हैं। एक-एक अथवा दो-दो मोक्षमार्ग नहीं हैं, क्योंकि इन तीनों के बिना मोक्षमार्ग नहीं है। रसायन के समान………………………..।
प्रस्तुत उद्धरण सूत्रार्थ(अगले पृश्ठ पर) में से है यह उन एकान्तनयावलम्बियों, मिथ्यावासित बुद्धि रोग वालों के लिए स्वयं रसायन रूप है जो केवल एक से ही मोक्षमार्ग मानते हों, वर्तमान में मात्र शास्त्र ज्ञान से ही सिद्धि मानने वालों का एक पृथक समुदाय ही बन गया है जो चारित्र से शुन्य है, व्रतों को आस्रव बन्ध का ही कारण समझ कर उनसे एवं संयमी जनों से दूर हो रहा है। माता जी की दूर दृश्टि उनके अभिप्राय तक पहुंची और उनके लिए उन्होंने इन उद्धरणों के माध्यम से हितोपदेष होकर यथोक्त मार्ग में लगाने की चेश्टा की है।
टीकाकत्र्री आर्यिका ज्ञानमती विवक्षित प्रकरण की पुश्टि करने की अभ्यासी है। कभी जैन दर्शन एवं धर्म की प्रभावना के प्रसंग में अन्य मत की समीक्षा एवं निरसन आवष्यक हो जाता है। इस विशय में उन्होंने अन्य मतावलम्बी ग्रंथों के उद्धरणों के माध्यम से अपने उद्देष्य की सिद्धि की है। स्याद्वाद चन्द्रिका में भी कई स्थलों पर दार्षनिक एवं आचरण विशयक जैनतर साहित्य के अंषों को भी प्रस्तुत किया है। जैनागम का मूल अहिंसा, अनेकान्त एवं पूर्वापर अविरोध को सिद्ध करने हेतु यह प्रयास किया गया है।
समीचीन और असमीचीन शास्त्रों के अंतर को स्पश्ट करने हेतु भी यह पद्धति अपनाई गई है। उन्होंने कहा है कि जो सर्व को प्रकाषित करने वाले ‘स्यात्’ पद मुद्रा से चिन्हित नहीं है ऐसे शास्त्रों में पूर्वापर- विरोध दोश पाया जाता है। जाबालिक मत के ग्रंथों में इस दोश को प्रकट करने हेतु उन्होंने नियमसार मूल की गाथा क्रमांक 8 की टीका के अंतर्गत उसके निम्न दो “लोक उद्धृत किए हैं-
गंगाद्वारे कुषावर्ते बिल्वके नीलपर्वते। स्नात्वा कनखले तीर्थे संभेवन्न पुनर्भवः।।
दुश्टमन्तर्गतं चित्तं तीर्थस्नानान्न शुद्ध्यति। शतषोऽपि जलैर्धौतं सुराभाण्डमिवाषुचिः।।
गंगाद्वार में, कुषावत्र्त में, बिल्वक में, नीलपर्वत के तीर्थ में और कनखल तीर्थ में स्नान करने से पुनर्जन्म नहीं होता है। पुनः लिखते हैं, जिनका अंतरंग मन दुश्ट है वह तीर्थ स्नान से शुद्ध नहीं होता है, जैसे “शराब के भांड को सैकड़ों बार भी जल से धोने पर भी वह पवित्र नहीं होता है। इस प्रकार के (अन्य मत के) आगम में एकरूपता नहीं है, पूर्वापरविरोध है, अतः वह आगम नहीं हो सकता। इस विधि से माता जी ने उद्धरण द्वारा प्रकरण की चर्चा की है।
आ० कुन्दकुन्द स्वामी ने नियमसार की गाथा क्रमांक 11 के अंतर्गत अतीन्द्रिय केवलज्ञान को स्वभावज्ञान घोशित कर विवेचित किया है। टीकाकत्र्री ने प्रस्तुत केवलज्ञान की अपेक्षित विस्तार से मीमांसा की है। उसके स्वरूप प्रकाषन हेतु उन्होंने आ० गृद्धपिच्छ के ही अन्य गं्रथ प्रवचनसार प्राभृत की गाथाओं को भी उद्धृत किया है। यद्यपि अपने “शब्दों के द्वारा भी विशय प्रतिपादित किया जा सकता है परन्तु जो प्रामाणिकता आगमोक्त अंषों को भी साथ ही प्रस्तुत कर देने से आती है उनके अभाव में वह न्यून रूप में होती है।
दूसरे, मन में अनिन्हव गुण होने के कारण भी लेखिका को इस प्रकार का उद्यम करने का अवष्य भाव उत्पन्न हुआ होगा। वे समस्त श्रेय परम्पराचार्यों को ही देना चाहती हैं। उन्होंने अनेक स्थलों पर यह भाव प्रकट किया भी है कि उनका कुछ नहीं है सब आगम का है। उक्त गाथा की टीका में प्रस्तुत प्रवचनसार की अनेक गाथाओं में से एक यहां उद्धृत करता हूं जिससे केवलज्ञान के स्वरूप पर सम्यक् प्रकाष पड़ता है-
अपदेसं सपदेसं मुत्तममुत्तं च पज्जयमजादं।
पलयं गयं च जाणदि तं णाणमणिदियं भणियं।।
जो ज्ञान अप्रदेष, सप्रदेष, मूर्त और अमूर्त ऐसे सभी पदार्थों को तथा अतीत और अनागत सभी पर्यायों को जानता है वह ज्ञान अनिन्द्रिय कहा गया है। वही केवलज्ञान है। आगे अविद्यमान पर्यायें भी केवलज्ञान का विशय है इसे सिद्ध करने हेतु उद्धरण दिये गये हैं।
आचार्य परम्परा में आचार्य यतिवृशभ एक महान प्रामाणिक आचार्य हुए हैं, उन्होंने कशाय पाहुड़ पर चूर्णि सूत्रों की रचना का महनीय कार्य किया है। तिलोयपण्णत्ती उनका महान ग्रंथ है। उनके द्वारा रचित गाथाओं को भी माता जी ने यथास्थान संयोजित किया है, जिससे टीका का विशय पूर्ण होने में सहायता मिली है। यहां तिलोयपण्णत्ती की उद्धृत निम्न गाथा अवलोकनीय है-
छब्बीस जुदेक्कसयप्पमाण भोगक्खिदीण सुहमेक्कं।
कम्मखिदीसु णराणं हवेदि सोक्खं च दुक्खं च।।
एक सौ छब्बीस भोगभूमियों में सुख ही है और कर्मभूमियों में सुख और दुख दोनों ही हैं। वर्तमान युग भौतिकता एवं आपाधापी का युग है। प्रायः स्वाध्याय की परिपाटी का अभाव ही हो रहा है। कुछ लोग स्वाध्याय के प्रति रुचिवान हैं भी, किन्तु उनके पास भी अधिक समय नहीं है। क्षयोपषम कम है, अल्पज्ञता है अतः समस्त अपेक्षित ग्रंथों का पारायण करने मंे असमर्थ हैं। विद्वान लोग भी अब गम्भीरतापूर्वक अध्ययन करते नजर नहीं आते।
उनको भी जीविकोपार्जन से अवकाष नहीं है। ऐसी स्थिति में यदि एक ही ग्रंथ में अन्य अनेकों ग्रंथों के उद्धरण प्रस्तुत किए जायें तो उनका रसास्वादन भी कम परिश्रम में ही हो जाता है। साथ ही यदि उन अंषों के पढ़ने से ग्रंथों के प्रति जिज्ञासा एवं रूचि जागृत हो जावे तो वह बहुत लाभकारी सिद्ध हो सकता है इस दृश्टि से स्याद्वाद चन्द्रिका टीका स्वाध्याय सम्बन्धी लोभ की पे्ररक प्रमाणित होगी।
नियमसार की गाथा क्रमांक 18 निम्न प्रकार है-
कत्ता भोत्ता आदा पोग्गलकम्मस्स होदि ववहारा।
कम्मजभावेणादा कत्ता भोत्ता दु णिच्छयदो।। 18।।
प्रस्तुत गाथा में कहा गया है कि जीव व्यवहार नय से पुद्गल कर्मों का कर्ता है, भोक्ता है तथा निष्चय नय से कर्मज भावों रागद्वेश आदि का कर्ता भोक्ता है। प्रस्तुत प्रकरण की पुश्टि विभिन्न दृश्टिकोणों से करने हेतु माता जी ने गोम्मटसार एवं बृहद् द्रव्य संग्रह की प्रसिद्ध गाथाओं को उद्धृत किया है। यह भी प्रकट किया है कि यहां निष्चय नय का अर्थ अषुद्ध निष्चय नय लेना चाहिए। पाठक उक्त प्रकरण को अवष्य अवलोकित करें।
प्रमाण और नय विशयक चर्चाओं को सजाने हेतु स्याद्वाद चन्द्रिका में अनेकों उद्धरणों की सुशमा प्रायः दृश्टिगत होती है जोकि इस टीका के नाम के अनुरूप ही है। नयचक्र, अश्टसहस्री, तत्वार्थ राजवार्तिक, “लोकवार्तिक आलापपद्धति, न्यायकुमुदचन्द्र आदि अनेकों ग्रंथों की पंक्तियों को लेखिका ने यथास्थान स्थापित किया है जिससे टीका का विशय सज संवर गया है। उन अंषों के अभाव में टीका प्रस्तुत सुंदर स्वरूप में उपलब्ध नही होती ऐसा मैं मानता हूं। यहां आ० विद्यानन्दि महोदय की निम्न उद्धृत उक्ति प्रकट है-
अर्थस्यानेकरूपस्य घीः प्रमाणं तदंषधीः।
नयो धर्मान्तरापेक्षी दुर्णयस्तन्निराकृतिः।
अनेक रूप (धर्मों) वाले पदार्थ का, अनेकान्तात्मक पदार्थ का ज्ञान प्रमाण है, उसके एक अंष का ज्ञान नय है। यह अन्य (विरोधी) धर्मों की अपेक्षा रखने वाला है और अन्य धर्मों का निराकरण करने वाला (अमान्य करने वाला) दुर्नय है।
नय चक्र का भी एक उदाहरण दृश्टव्य है-
कम्माणं मज्झगयं जीवं जो गहइ सिद्धसंकासं।
भण्णइ सो सुद्ध णओ खलु कम्मोवाहि णिरवेक्खो।। 18।।
जो नय कर्मों के मध्य स्थित जीव को भी सिद्ध के समान शुद्ध कहता है वह कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध नय है।
कारण परमाणु और कार्य परमाणु का स्वरूप वर्णन प्रस्तुत करते समय पृश्ठ 87 पर टीकाकत्र्री ने यहां अकलंकदेव कृत तत्वार्थ राजवार्तिक के अंषों को प्रस्तुत किया है जो उचित ही है उससे यथेश्ट प्रभाव पड़ता है।
आचार्य अमृतचन्द्र जी ने समयप्राभृत पर कलष काव्य लिखकर आत्मख्याति टीका पूर्ण की है। समयसार कलष अध्यात्म पे्रमियों के लिए अत्यंत प्रिय ग्रंथ है। पू० ज्ञानमती माता जी ने स्याद्वाद चन्द्रिका में बहुलता से उसके कलषों का उपयोग किया है। इससे टीका के अध्यात्मिक स्वरूप को स्थिर रखने में बड़ी सहायता मिली है यहां हम प्रतिनिधि रूप में मात्र एक कलष को उद्धृत कर रहे हैं।
अस्मिन्ननादिनि महत्यविवेकनाट्ये वर्णादिमान् नटति पुद्गल एव नान्यः।
रागादिपुद्गलविकारविरूद्धषुद्ध-चैतन्यधातुमयमूर्तिरयं च जीवः।। 44।।
इस अनादिकालीन अविवेक रूप नाटक में वर्णादि वाला पुद्गल ही नृत्य कर रहा है, अन्य नहीं। यह जीव तो रागादि पौद्गलिक विकारों से विरूद्ध, शुद्ध चैतन्यधातुमय मूर्ति रूप है।
प्रस्तुत विशय में यह कहना असंगत न होगा कि उक्त कलष का प्रायः सभी विद्वानों ने यही हिन्दी अर्थ किया है जो मुझे अपूर्ण लगता है तथा खटकता है। संभव है कि यह मेरी अल्पज्ञता हो। इस विशय में निम्न बिन्दुओं पर ध्यान दिलाना चाहूंगा। यह अध्यात्म क्षेत्र में व्यवहार नय का विशय है। अषुद्ध नय प्रयोग है।
- 1- यहां अविवेक नाट्य कहा गया है सो विवेक और अविवेक तो जीव में है, पुद्गल में नहीं वह तो जड़ है। अविवेक नाट्य में जीव और पुद्गल दोनों ही नृत्य कर रहे हैं। दोनों में क्रियावती एवं वैभाविक शाक्ति है। नाट्य का फल जीव को ही मिलता है तो कर्ता भी जीव ही है। उसके निमित्त कारण मात्र पुद्गल का नाट्य कहना, आपेक्षिक दृश्टि से ठीक होते हुए भी उस अपेक्षा का स्पश्टीकरण न करके पुद्गल मात्र का नाट्य कहना संगत नहीं लगता। भ्रमोत्पादक प्रतीत होता है।
- 2- कलष के उत्तर अद्र्धांष में रागादिपुद्गलविकार से रहित एवं शुद्ध चैतन्य से युक्त कहा गया है सो शुद्ध नय से है। शुद्ध नय में तो किसी का भी नाट्य या भ्रमण ही सिद्ध नहीं होता।
- 3- शुद्ध नय की दृश्टि से तो पुद्गल भी शुद्ध है। वह भी नाट्य नहीं करता। इस नय से तो जीव और पुद्गल दोनों ही नाट्य रहित शुद्ध रूप में हैं।
- 4- अन्य शास्त्रों के अनेकों स्थलों पर दोनों का ही इस लोकावास में नृत्य बताया है।
- 5- आचार्य अमृतचन्द्र जी ने ‘च’ “शब्द का प्रयोग किया है न कि ‘तु’ का। ‘तु’ लिखने से न तो मात्रा बढ़ती और न कोई हानि होती। ‘तु’ लिखने से तथाकथित अर्थ ही सिद्ध होता। ‘च’ तो यहां योग का वाचक ही कहें, जोकि प्रसिद्ध ही है, तो अर्थ ठीक भासित होगा।
- 6- जीव के चतुर्गति भ्रमण की ही सिद्धि है न कि पुद्गल की।
मैं विद्वानों के द्वारा कथित उपरोक्त हिन्दी अर्थ का निशेध करने का साहस तो जुटा नहीं सकता तथा अनेकान्त में तो किसी भी धर्म की विधि की जा सकती है। किन्तु मैं निम्न प्रकार से कलष का अन्वय करके हिन्दी अर्थ प्रस्तुत करना चाहूँगा, विद्वद्गण एवं पू० माता जी का ध्यान आकर्शित कर रहा हूं।
‘‘अस्मिन्ननादिनि महत्यविवेकनाट्ये वर्णादिमान् पुद्गलः
रागादिपुद्गलविकार विरूद्धशुद्धचैतन्यधातुमयमूर्तिरयं जीवष्च नटति नान्यः। 44।।
अर्थ – इस अनादिकालीन महान अविवेकरूप नाट्य में वर्णादिमान् पुद्गल नाट्य करता है तथा शुद्ध नय से रागादि पुद्गल विकारों से रहित चैतन्य धातुमय मूर्ति (होकर भी अषुद्ध नय से) जीव भी नाट्य करता है अन्य नहीं।
यहां पर दोनों के लिए पृथक-पृथक एक वचन का प्रयोग करना भी रूढ़ि अर्थ में असंगत नहीं होगा। जैसे राम जाता है और “याम जाता है (इनके अतिरिक्त) अन्य नहीं।
पुनष्च आचार्य श्री अमृतचन्द्र जी का निम्न कलष भी दृश्टव्य है-
परपरिणतिहेतोर्मोहनाम्नोऽनुभावाद-विरतमनुभाव्यव्याप्तिकल्माशितायाः,
ममपरमविषुद्धिर्षुद्धचिन्मात्रमूर्ते-र्भवतु समयसारव्याख्ययैवानुभूतेः।।
यहां पर शुद्ध नय से परमविषुद्ध शुद्ध चैतन्यमूर्ति होने पर भी अषुद्ध नय से पर-परिणति से कल्माशितता स्वीकार की है उसी प्रकार कलष क्रमांक 44 में भी शुद्ध नय से रागादि पुद्गल विकार रहित जीव का भी नाटक (भ्रमण) अषुद्ध नय से स्वीकार करना योग्य होगा।
जिनागम में प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग एवं द्रव्यानुयोग ये चार अनुयोग प्रसिद्ध हैं। प्रथमानुयोग का उद्गम दृश्टिवाद अंग के प्रथमानुयोग भेद से, ज्ञातृधर्मकथांग से, अनुत्तरोपपादिक दषांग से एवं अन्तःकृद्दषांग से हुआ है। करणानुयोग का श्रोत दृश्टिवाद के अंग परिकर्म, अग्रायणीय पूर्व तथा ज्ञानप्रवाद पूर्व आदि है। चरणानुयोग आचारांग तथा उपासकाध्ययनांग का रूप है तथा द्रव्यानुयोग अग्रायणीय पूर्व तथा ज्ञानप्रवाद पूर्व से संबंधित है।
यहां यह स्पश्ट है कि द्रव्यानुयोग और करणानुयोग दोनों मिलकर चलते हैं। द्रव्यानुयोग के ग्रंथों का पारायण करने से ज्ञात होता है कि उसमें सदैव करणानुयोग की अपेक्षा स्पश्ट झलकती है। यदि करणानुयोग की उपेक्षा करके मात्र द्रव्यानुयोग का अध्ययन किया जाय तो परिणाम भ्रम रूप ही निकलता है।
नियमसार की टीका लिखते समय टीकाकत्र्री ने करणानुयोग की सापेक्षता का ध्यान रखा है। विवक्षित विशय को गति देने हेतु उन्होंने करणानुयोग के ग्रंथों के उद्धरण देकर सुश्ठ प्रयत्न किया है। गणित करणानुयोग का मुख्य विशय है। नियमसार गाथा क्रमांक 31 में कालद्रव्य के विशय में आचार्य कुन्दकुन्द स्वामी ने कहा है-
समयावलिभेदेण दु दुवियप्पं अहव होइ तिवियप्पं।
तीदो संखेज्जावलि हद संठाण (सिद्धाण) प्पमाणं तु।। 31।।
जीवादु पुग्गलादोऽणंतगुणा भावि(चावि)संपदी समया
लोयायासे संति य परमट्ठो सो हवे कालो।। 32।।
समय और आवलि के भेद से काल दो प्रकार का है अथवा तीन प्रकार का है। अतीत काल संख्यात आवलि से गुणित संस्थान प्रमाण है। जीव और पुद्गल से अनंत गुणा भविश्यत् काल है और वर्तमान काल समय मात्र है। जो लोकाकाष के एक एक प्रदेष पर स्थित है वे कालाणु परमार्थ काल है।
इसकी टीका आर्यिका ज्ञानमती जी ने विस्तार से की है और विशय को स्पश्ट किया है। गाथागत ‘हदसंठाणं’ के स्थान पर ‘हदसिद्धाणं’ की सम्यक्ता भी प्रकट की है ताकि अन्य आचार्य परम्परा के अनुसार भी अर्थ किया जा सके। आचार्य पद्मप्रभ ने भी गाथा में ‘हदसिद्धाणं’ पद स्वीकार किया है। साथ ही उन्होंने टीका में ‘संस्थान’ पदगत अर्थ भी प्रकट किया है।
पू० माता जी ने दोनों पदों में से निशेध किसी का भी न करके प्रस्तुत गाथा 31 के सम्भावित सभी अर्थ प्रकट किए हैं, तथा पाठ भेद और उसका प्रभाव स्पश्ट किया है। यह उनकी टीका की विषेशता ही कही जायेगी। प्रस्तुत पाठ भेद की स्थिति में पद ‘हदसिद्धाणं’ की प्रबलता सिद्ध करने हेतु उन्होंने मिलती जुलती आ० नेमिचन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्ती देव की निम्न गाथायें उद्धृत की हैं जिससे प्रकृत विशय पर उपयोगी प्रकाष पड़ता है, अवलोकनीय है-
ववहारो पुण तिविहो तीदोवट्टंतगो भविस्सोदु।
तीदोसंखेज्जावलि हदसिद्धाणं पमाणं तु।।
समओ दु वट्टमाणो जीवादो सव्वपुग्गलादोवि।
भावी अणंतगुणिदो इदि ववहारो हवे कालो।। 579।।1
यहां प्रस्तुत जीवकांड की गाथाओं के उद्धरण का मुख्य उद्देष्य टीकाकत्र्री का यह रहा है कि कुन्दकुन्द स्वामी की गाथा में गोम्मटसार के समान ही ‘हदसिद्धाणं’ पद स्वीकार किया जाय। ठीक ही है परम्पराचार्यों के मंतव्यों की परस्पर अनुसारता ही हमें प्रमाण मानना चाहिए।
इसी स्थल पर माता जी ने आचार्य पद्मप्रभमलधारी देव की तात्पर्यवृत्ति टीका का अंष उद्धृत कर प्रकट किया है-
‘‘अत्र श्री कुन्दकुन्ददेवस्य गाथायां ‘‘तीदोसंखेज्जावलिहदसंठाणप्पमाणं तु’’ एतत्पाठो लभ्यते,तस्य टीकायामपि श्री पद्मप्रभमलधारिदेवैः कथ्यते,यत् ‘‘अतीतसिद्धानांसिद्धपर्यायप्रादुर्भावसमयात् पुरागतो ह्यावल्यादिव्यवहारकालः, सकालस्यैषां संसारावस्थायां यानि संस्थानानि गतानि तैः सदृषत्वादनन्तः।
अनागतकालोऽप्यनागतसिद्धानामनागतषरीराणि यानि तैः सदृष इत्यामुक्तेः सकाषादित्यर्थः।’’
आसां पंक्तीनामर्थः स्पश्टतया न प्रतिभासते………….।’’
माता जी ने कहा है कि उपरोक्त पंक्तियों का अर्थ उन्हें स्पश्ट प्रतिभासित नहीं हो रहा है। साथ ही मूल गाथा में मलधारिदेव ने ‘हदसिद्धाणं’ पाठ लिखा है और अर्थ ‘हदसंठाणं’ का किया है। इस विशय में मैं अपनी समझ के अनुसार (आवष्यक नहीं है वह युक्त हो) अभिमत प्रकट करना चाहूंगा। इस हेतु निम्न बिन्दु विचारणीय है-
- 1- आ० पद्मप्रभमलधारिदेव ने सिद्धों के संसारावस्था में व्यतीत “शरीराकारों के बराबर अतीतकाल को अनन्त प्रमाण लिखा है।
- 2- “शरीरों के संस्थान या आकार आत्मप्रदेषाकार ही होते हैं।
- 3- प्रतिसमय कर्मोदय की भिन्नता स्वरूप संस्थान या आकार बदलना स्वाभाविक है जैसे गर्भस्थ षिषु के आकार से लेकर प्रति समय, प्रति आवली प्रतिदिन वृद्धिगत अवस्था होती है इसी प्रकार पूरे जीवन में भी परिवर्तित होती है। वृद्धावस्था में “शरीराकार की हानिगत अवस्था होती है।
- 4- “शरीर संस्थान व्यंजन पर्याय है और इनके अंतर्भूत अर्थपर्यायें हैं।
- 5- अर्थपर्याय प्रति समय ‘शट्स्थान पतित हानिवृद्धि रूप होती है।
- 6- प्रति समय हानिवृद्धि का तात्पर्य “शरीराकारों का भी प्रति समय परिवर्तन है।
अतः सिद्धों के सिद्ध पर्याय प्रकट होने से पूर्व संसारावस्था में जितने समय समय प्रति भिन्न “ारीराकार हुए उतने ही प्रमाण समय रूप अतीत व्यवहार काल हैं। “शरीराकार समय और समयों का विवक्षित समूह सभी अनंत प्रमाण है। इसी प्रकार से अनागत काल भी विवक्षित अनन्तता के प्रमाण है। आ० पद्मप्रभ की टीकांष का यह तात्पर्य संभव है।
उपरोक्त प्रसंग में माता जी का ध्यान आ० कुन्दकुन्द और नेमिचन्द्र जी की पद समानता पर गया और इसी हेतु उन्होंने उपरोक्त दो गाथायें गोम्मटसार की उद्धृत कर हमें यथेश्ट अर्थ की ओर पे्ररित किया है। इससे प्रकट है कि उद्धरणों की कितनी उपयोगिता है तथा अनेक “शास्त्रों के स्वाध्याय का क्या लाभ है। इसी हेतु वक्ता को सभी “शास्त्रों में पारंगत होना आवष्यक होता है। आ० गुणभद्र ने वक्ता के लक्षण प्रकट करते हुए कहा है-
प्राज्ञः प्राप्तसमस्तषास्त्रहृदयः प्रज्ञप्तलोकस्थितिः।
प्रास्ताषः प्रतिभापरः प्रषमवान् प्रागेवदृश्टोत्तरः।।
प्रायः प्रष्नसहः परमनोहारी परानिन्दया।
ब्रूयात् धर्मकथां गणीगुणनिधिः प्रस्पश्टमिश्टाक्षरः।।
समस्त “शास्त्रों के रहस्य का ज्ञाता, लोकस्थिति से अवगत, आषारहित, प्रतिभा सम्पन्न, मंदकशाय, प्रष्न से पूर्व ही उत्तर का ज्ञाता, प्रष्नों को सहन करने वाला, दूसरों की निन्दा न करने से सभी को प्रिय, गुणी तथा स्पश्ट और मिश्टभाशी आचार्य धर्मकथा का उपदेष करें।
माता जी तो स्वयं संयमी एवं गणिनी पद से विभूशित हैं, दीक्षा और षिक्षा में कुषल हैं तथा सभी अनुयोगों के “ाास्त्रों की मर्मज्ञ विदुशी हैं। उक्त सभी लक्षण उनमें घटित होते हैं। उपदेष हों या आलेखन सभी में उनकी समान रूप से योग्य गति है। उन्होंने बहुषास्त्रविद् होने के आलम्बन से ही नियमसार टीका में उद्धरणों की बहुआयामी शोभा प्रकट की है।
पू० ज्ञानमती माता जी ने नियमसार के ही पूर्व तात्पर्यवृत्ति टीकाकार आ० पद्मप्रभ का भी यथास्थान आवष्यकता अनुभव कर उपयोग किया है। अतः अन्य 62 गंरथों के रचयिताओं के साथ ही वे प्रस्तुत आचार्य से भी उपकृत हैं। उनकी मात्र वृत्तिरूप प्रथम टीका भी बहुत सुंदर एवं अध्यात्म रसिकों का सदियों से कण्ठहार बनी हुई हैं। उसके सौंदर्य का उपयोग करने से स्याद्वाद चन्द्रिका का सौश्ठव वृद्धिगत हुआ है। इससे माता जी के गुणग्राहकता गुण का परिचय मिलता है। साधु तो वैसे भी हंस के समान होते हैं क्षीर को ग्रहण करने के समान वे अवष्य गुणग्राही होते हैं।
भट्टाकलंक देव महान प्रभावक आचार्य के रूप में बहुविख्यात हैं। उनके गंभीर आर्श अर्थ को समाहित करने वाले स्याद्वाद न्याय युक्त परिवेष वाले एवं जिनधर्मप्रभावक वचनों का उदाहरण देने में परवर्ती आचार्यों एवं विद्वानों को बडे़ गौरव का अनुभव हुआ है। तत्वार्थ राजवार्तिक उनका वाङ्मयदर्पणवत् महनीय टीका ग्रंथ है।
आर्यिका ज्ञानमती ने स्याद्वाद चन्द्रिका में उसका भरपूर प्रयोग किया है। जैसे कोई व्यक्ति आभूशणों का संग्रह कर अपने व्यक्तित्व का अलंकरण करता है, तथैव उन्होंने अपनी प्रस्तुत टीका रचना को तत्वार्थवार्तिक के वार्तिकों के उद्धरणों से सजाया है। गाथा क्रमांक 36 की टीका में प्रदेषों का व्याख्यान करते हुए माता जी ने तत्वार्थ वार्तिक के अध्याय 5 सूत्र 8 के वार्तिक संख्या 15 व 16 प्रस्तुत किए हैं, पठनीय हैं-
जिनका आषय यह है कि अर्हन्त भगवान के आगम से चलाचल प्रदेषों पर स्थित अनन्तानन्त कई प्रदेषों का उक्त वार्तिकों के अनुसार स्वरूप जानना चाहिए। इन उद्धरणों से टीका की प्रामाणिकता का विस्तार हुआ है। इसके अतिरिक्त भी कर्म सिद्धान्त के विशय में माता जी ने पचास्तिकाय, गोम्मटसार, तत्वार्थसूत्र, धवला, द्रव्यसंग्रह टीका आदि के उद्धरण प्रचुर मात्रा में दिये हैं जो स्याद्वाद चन्द्रिका की श्री में स्पश्ट रूप से वृद्धि करते हैं।
अध्यात्म के गौरव को प्रतिश्ठित करने हेतु टीकाकत्र्री ने प×चास्तिकाय, गोम्मटसार, समयसार, समयसार कलष, समाधिषतक, अश्टपाहुड़, परमात्मप्रकाष, इश्टोपदेष,ज्ञानार्णव,आत्मानुषासन आदि ग्रंथों के अवतरणों को प्रयोग कर नियमसार के अध्यात्म विशयक तत्व को प्रकाषित व पल्लवित किया है। नियमसार की गाथा क्रमांक 37 निम्न प्रकार हैं-
पुग्गलदव्वं मुत्तं मुत्तिविरहिया हवंति सेसाणि।
चेदणभावो जीवो चेदणगुणवज्जिया सेसा।। 37।।
पुद्गल द्रव्य मूर्तिक है, द्रव्य अमूर्तिक हैं। जीव चैतन्य स्वभाव वाला है “ द्रव्य चेतना गुण रहित हैं। माता जी ने अपने “शब्दों में प्रस्तुत गाथा की विषद व्याख्या की है। यदि प्रस्तुत गाथा के हार्द को प्रकट करने वाला कोई सुंदर, गाथा का प्रतीक रूप संक्षिप्त, बोधगम्य एवं भावार्थ रूप वाक्य किन्हीं आचार्य का मिल जावे तो उसे प्रयुक्त करना श्रेयस्कर रहेगा इस उद्देष्य से टीकाकत्र्री को अपने स्वाध्यायार्जित ज्ञानकोष में आ०पूज्यपादका निम्न पद दृश्टिगोचर हुआ जो उन्होंने यथास्थान टीका को सुबोध, सुपाच्य बनाने हेतु प्रयुक्त करना योग्य समझा, दृश्टव्य है-
‘‘अचेतनमिदं दृष्यमदृष्यं चेतनं ततः।
जो दृष्यमान है वह सब अचेतन है और जो नहीं दिखता वह जीव है (जोकि अनुभव का विशय है)
आर्यिका ज्ञानमती की विषाल एवं स्वनामानुरूप ज्ञान दृश्टि के उदाहरण सर्वत्र अपने प्रमेयत्व गुण का प्रयोग करते हुए अर्थात अपने आकार अस्तित्व को फेंकते हुए दृश्टिगत होते हैं। यह उनकी टीका की विषेशता एवं सफलता है।
पूज्य माता जी पर आचार्य पद्मनन्दी कृत ‘पचविंषतिका’ का सर्वप्रथम एवं महनीय उपकार है जिसके प्रति वे कृतज्ञ हैं ऐसा उन्होंने स्याद्वाद चन्द्रिका में व्यक्त किया है। उस ग्रंथ के अध्यात्म विशयक निष्चय पचाषत् अधिकार में बडे़ सुन्दर स्वरूप सम्बोधक मंत्र रूप वाक्य हैं। मैं यहां माता जी के द्वारा उसमें से उद्धृत कतिपय अध्यात्म सूक्ति मणियों का प्रकाष करने हेतु उन्हें प्रस्तुत करने का लोभ संवरण नहीं कर पा रहा हूं। पाठक ध्यान देवें,
मयि चेतः परजातं तच्च परं कर्म विकृतिहेतुरतः।
किं तेन निर्विकारः केवलमहममलबोधात्मा।।
त्याज्या सर्वाचिंतेति बुद्धिराविश्करोति तत्तत्त्वम्।
चन्द्रोदयायते यच्चैतन्यमहोदधौ झगिति।।
मेरा जो चित्त है वह पर से उत्पन्न हुआ है और वह जो पर है उसे कर्म कहते हैं। वह कर्म विकृति का हेतु है। इसलिए उस विकृति से मुझे क्या प्रयोजन है? मैं तो निर्विकार हूं, केवल (असहाय) हूँ और अमल ज्ञान स्वरूप हूं। इसलिए सभी चिन्ता त्याग करने योग्य है, ऐसी बुद्धि उस तत्व को उत्पन्न करती है जो चैतन्य रूपी महासमुद्र को बढ़ाने के लिए शीघ्र ही चन्द्रमा के उदय समान आचरण करती है।
आ० पद्मनन्दी की यह अध्यात्म पद रूप मणियां माता जी की प्रस्तुत टीका संज्ञक आभूशण को अलंकृत कर उसे गौरव प्रदान करती दृश्टिगत हो रही है।
मूलाचार आचार्य कुन्दकुन्द की साधुचर्या प्ररूपक महनीय कृति है उसमें अध्यात्म गवेशणा में प्रयुक्त निष्चय सामायिक का स्वरूप विस्तार से वर्णित है नियमसार में उसी को परम समाधि के रूप में वर्णित किया गया है। माता जी ने इस अधिकार की टीका में गाथा संख्या 127 के अंतर्गत मूलाचार से निम्न उद्धरण दिया है जो उपयोगी एवं प्रकृत अर्थ का पोशक है।
सम्मतणाणसंजम तवेहिं जं तं पसत्थसमगमणं।
समयं तु तं तु भणिदं तमेव सामाइयं णाम।।
सम्यक्त्व, ज्ञान, संयम और तप के साथ जो प्रषस्त समागम है वह समय है। उसे ही तुम सामायिक जानो। यहां चार आराधनाओं में संसक्त मन की ध्यान रूप अवस्था है उसे सामायिक कहा है यही नियमसार गाथा संख्या 127 में “शब्दषः वर्णन है। दोनों गाथायें समानान्तर एवं समानार्थक है। पू० माता जी के द्वारा दिया गया सन्दर्भ पाठकों के लिए ज्ञान विस्तार का उपाय है। टीका में समानार्थक आगमांषों को प्रस्तुत करना भी उपयोगी माना गया है।
नियमसार-अजीवाधिकार में गाथा क्रमांक 39 एवं 41 निम्न प्रकार है,
णो खलु सहावठाणा णो माणवमाणभावठाणा वा।
णो हरिसभावठाणा णो जीवस्साहरिसभावठाणा वा।।
णो खइयभावठाणा णो खउवसमसहावठाणा वा।
ओदइय भावठाणा णो उवसमणे सहावठाणा वा।।
जीव के (निष्चय से) स्वभाव स्थान, मान अपमान भाव स्थान नहीं है। हर्श भाव और विशादभाव स्थान भी नहीं है।। 39।।
जीव के निष्चय से क्षायिक भावस्थान नहीं है, क्षायोपषमिक स्वभाव स्थान नहीं है, औदयिक भावस्थान नहीं है तथा औपषमिक स्वभाव स्थान नहीं है। यह विवेचन नास्ति स्वभाव की अपेक्षा है।
यहां गाथा क्रमांक 39 में स्वभावस्थान और 41 में ‘स्वभावस्थान’ “शब्द के अर्थों में क्या एकता अथवा क्या अनेकता है इसकी गवेशणा में ज्ञानमती जी ने अनेकता, भिन्नता स्वीकार कर टीका का विस्तार किया है। यह उचित ही है। प्रथम ‘सहावठाणा’’ की टीका में स्वभाव “शब्द का अर्थ कर्म प्रकृति के उदय से होने वाला जीवों का भाव, परिणाम रूप स्वभाव किया है। इस अर्थ की सिद्धि हेतु गोम्मटसार अथवा धवला टीका की निम्न पंक्तियां उद्धृत की हैं-
पयडीसील सहावो जीवंगाणं अणाइ संबंधो।
कणगोवले मलं वा ताणत्थित्तं सयं सिद्धं।।
कर्मोदय जन्य स्वभाव स्थान शुद्ध निष्चय से आत्मा में नहीं है इसके समर्थन हेतु आ० पद्मप्रभमलधारि देव की टीका का, ”त्रिकालनिरूपाधिस्वरूपस्थ शुद्ध जीवास्तिकायस्य खलु विभावस्वभावस्थानानि“, यह वाक्य भी उद्धृत किया है। एवंविध ही आचार्य कुन्दकुन्द स्वामी के प×चास्तिकाय की गाथा क्रमांक 65 को भी प्रस्तुत किया है जिसमें यह निरूपित है कि आत्मा और पुद्गल स्वभाव रूप से कई रूप परिणमन करते हैं।
आत्मा भाव कर्म के रूप में तथा पुद्गल द्रव्यकर्म के रूप में परस्पर अन्योन्य अवगाहन एवं निमित्त नैमित्तिक भाव द्वारा परिणमन करते हैं। टीका में माता जी ने उपरोक्त उद्धरणों के माध्यम से पाठकों को अवगत कराया है कि कुन्दकुन्द स्वामी ने जिस स्वभाव “शब्द का गाथा क्रमांक 39 के अंतर्गत प्रयोग किया है वह कर्मोदय जन्म विभाव स्वभाव है। इस रूप आत्मा तन्मय होता है यह आत्मा का ही परिणाम है। समयसार कलष में आ० अमृतचन्द्र जी ने यह भाव व्यक्त किया है जिसे यहां प्रस्तुत करना उपयुक्त होगा-
यः परिणमति स कर्ता यः परिणामो भवेत्तु तत्कर्म।
या परिणतिः क्रिया सा त्रयमपि भिन्नं न वस्तुतया।।
जो परिणमन करता है वह कर्ता है जो परिणाम होता है वह कर्म है तथा जो परिणति है वह क्रिया है, ये तीनों वस्तुरूप से भिन्न नहीं है अर्थात एक ही हैं।
नियमसार की उपर्युक्त गाथा सं. 41 में स्वभाव “शब्द का अर्थ औदयिक भाव के साथ ही मोक्षमार्ग में उपयोगी औपषमिक, क्षायोपषमिक और क्षायिक भावों के रूप में भी लिया है। क्षायिक भाव को भी कर्म की अपेक्षा होने के कारण शुद्ध जीव के अस्तित्व में परमभावग्राहीषुद्धद्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा निशेध किया है। यहां जैनाभासों के ‘‘औदारिकषरीरस्य कि×िचन्यून कोटिवर्शस्थितिः कवलाहारमन्तेरण कथं संभवति? कथन के उद्धरण द्वारा उस शंका का समाधान किया है। निरसन किया है। क्षायिक भोग भाव की स्थिति में कवलाहार की आवष्यकता ही नहीं है यह स्पश्ट किया है।
स्याद्वाद चन्द्रिका की लेखिका ज्ञानमती माँ मूल जैन सिद्धान्त ग्रंथों की मर्मज्ञ विदुशी हैं। विशय के यथेश्ट प्रतिपादन हेतु उन्होंने गौतम गणधर देव के द्वादषांग से साक्षात् संबंधित कशायपाहुड़, ‘ट्खण्डागम, समयप्राभृत, मूलाचार, तिलोयपण्णती आदि तथा स्वयं गणधर स्वामी द्वारा रचित प्रतिक्रमण के सूत्रों काउद्धृत कर टीका को अत्यंत महत्वपूर्ण एवं श्री समृद्ध बना दिया है। क्षयोपषम सम्यग्दर्षन के प्रकरण में पृश्ठ 161 पर कशाय पाहुड की गाथा संख्याक1 107 और उसकी अनुसारी लब्धिसार की गाथा सं. 105 की प्रस्तुति द्वारा वेदक सम्यक्त्व के स्वरूप पर आ० कुन्दकुन्द स्वामी के आषय को स्पश्ट किया है। पाठकों को इसका रसास्वादन अवष्य करणीय है।
नियमसार की गाथा नं० 62 की टीका के अंतर्गत भाशा समिति के विशय में गौतम गणेष के प्रतिक्रमण से निम्न अंष उद्धृत किया गया है। इससे व्यवहार चारित्र के प्रति निरतिचार संयम पालन हेतु मुमुक्षु की सदिच्छा का प्रकटीकरण हुआ है-
‘‘तत्थ भासासमिदी कक्कसा कडुआ णिट्ठुरा परकोहिणी मज्झंकसा अइमाणिणी अणयंकरा छेयंकरा भूयाणवहंकरो चेदि दसविहा भासा भासिया भासिज्जंतो विसमणुमणिदो तस्स मिच्छा मे दुक्कडं।’’
साधक प्रतिक्रमण करते समय भगवान से यह प्रार्थना करता है कि मैंने कर्कष, कठोर, निश्ठुर, पर को क्रोध उत्पन्न कराने वाली, हृदय में भी प्रवेष कर जाये ऐसे कठोर “शब्दरूप मध्यकषा, अति मानकारी, नयों से विरूद्ध अथवा सर्वथा एकान्त रूप, हृदय को छेदने वाली और जीवों की वधकारी इस प्रकार की भाशा बोली हो, बुलवाई हो अनुमोदना की हो वह मेरा दुश्कृत दोश मिथ्या होवे। इस प्रकार भाशा समिति के दोशों को दूर करने वाला यह प्रतिक्रमण है।
प्रस्तुत उद्धरण से विविध भाशा विकारों को जानकर उन पर विजय प्राप्त करने का भाव जागृत होता है। यह हम सभी लोगों के लिए उपयोगी है।
जैन वाङ्मय का मूल प्रारूप प्राकृत भाशा में है। स्याद्वाद चन्द्रिका कत्र्री का मूलग्रंथों के स्वाध्याय से उनके प्रति विषेश श्रद्धा एवं रूचि से प्राकृत (अद्र्धमागधी) का प्रयोग करने का विषेश अभ्यास है। वे संस्कृत की भी अधिकारी विद्वान हैं। प्राकृत के उद्धरणों के साथ ही उन्होंने संस्कृत के वाक्यों में नियमसार के मूल रहस्य को खोलने हेतु सुंदर से सुंदर प्रकृत विशयोपयोगी उद्धरणों को चुन चुनकर रखा है। इससे टीका में आकर्शण, रमणीयता, कोमलता का संचार होता प्रतीत होता है।
टीका के क्षेत्र में आचार्य वीरसेन कृत ‘ट्खण्डागम की धवला टीका एक प्रसिद्ध एवं बहुसम्माननीय टीका है। इसमें आचार्य देव ने प्राकृत एवं संस्कृत मिश्रित भाशा में अत्यंत प्रभावकारी “शैली में ‘ट्खण्डागम सूत्रों का विशय विस्तार एवं स्पश्टीकरण किया है। यह धवला टीका स्वयं में एक मूल ग्रंथ सदृष प्रतीत होता है।
ज्ञानमती माता जी ने प्रस्तुत नियमसार की संस्कृत टीका में धवला से प्राकृत के उद्धरणों के अतिरिक्त संस्कृत उद्धरणों का बहुलता से उपयोग किया है। इसकी अत्यंत महत्वपूर्ण पंक्तियों का उपयोग अर्थ की निश्पत्ति हेतु अपेक्षित स्थलों पर किया है।
णमोकार महामंत्र, जोकि ‘ट्खण्डागम का मंगलाचरण रूप है, में सिद्धों से प्रथम ही मात्र घातियों कर्मों का नाष करने वाले अर्हंत भगवान को नमस्कार किया गया है। सम्यग्दृश्टि निश्पक्ष होता है तथापि क्या यह पक्षपात नहीं है एतद्विशयक प्रसंग की उपस्थिति में स्याद्वाद चन्द्रिका में उपर्युक्त धवला का निम्न उदाहरण विलोकनीय है-
‘‘न पक्षपातो दोशाय “शुभपक्षवृत्तेः श्रेयोहेतुत्वात्, अद्वैतप्रधाने गुणीभूतद्वैते द्वैतनिबन्धनस्य पक्षपातस्यानुपपत्तेष्च।
आप्तश्रद्धाया आप्तागमपदार्थविशयश्रद्धाधिक्यनि- बन्धनत्वख्यापनार्थं वार्हतामादौ नमस्कारः।’’
शुभ पक्ष के वत्र्तन में किया गया पक्षपात दोश के लिए नहीं है, क्योंकि वह मोक्ष का हेतु है। जहां अद्वैत प्रधान है वहां द्वैत गौण हो जाता है। ऐसे अद्वैत प्रधान में द्वैत निमित्तक पक्षपात नहीं बन सकता अथवा आप्त की श्रद्धा में आप्त आगम और पदार्थ विशयक
श्रद्धा की अधिकता हेतु है ऐसा बतलाने के लिए भी अर्हन्तों को पहले नमस्कार किया है।
उक्त उद्धरण से स्याद्वाद चन्द्रिका में गुणगरिश्ठता एवं प्रामाणिकता स्वयं मुखरित हो उठी है।
किसी भी टीका रचना का मूल उद्देष्य मूल ग्रंथ के विशय का प्रकाषन ही होता है। उद्धरणों के प्रस्तुतीकरण के निम्न उद्देष्य संभावित होते हैं-
- 1. मूल ग्रंथ का अर्थ स्पश्टीकरण एवं श्रद्धा का जागरण।
- 2. मूल ग्रंथ का विशय विस्तार।
- 3. तद्विशयक शंकाओं और जिज्ञासाओं का समाधान।
- 4. कालक्रम से विच्छिन्न परम्परा का दृढ़ीकरण, मार्ग प्रभावना।
- 5. प्रवचनवत्सलत्व तथा जिनवाणी मां एवं पूर्वाचार्यों का गुण स्मरण तथा साहित्य रचना उपकार रूप ऋण का विमोचन।
- 6. टीकाग्रंथ का अलंकरण साज सज्जा।
- 7. मन्द क्षयोपषम की स्थिति में उदाहरणों द्वारा अर्थावगम।
- 8. अपने स्वयं के अर्जित ज्ञान को अविच्छिन रखने तथा वृद्धिगत करने का लक्ष्य।
- 9. उपयोग की चंचलता को रोककर आगमाभ्यास के इस साधन से उसका स्थितिकरण तथा स्थिरीकरण।
- 10. अप्रसिद्ध एवं भूले बिसरे प्रकरणों को भी प्रस्तुत करना।
- 11. स्वाध्याय तप के पांचों अंगों वाचना, पृच्छना, आम्नाय, अनुपे्रक्षा एवं उपदेषों का एक ही पद्धति के अंतर्गत लाभ।
नियमसार की प्रस्तुत व्याख्या में टीकाकत्र्री ने उपरोक्त सभी उद्देष्यों की पूर्ति हेतु ग्रंथ में सर्वत्र प्रयास किया है। उनकी टीका में यथोक्त उद्धरण इन्द्र- धनुशीय सुशमा को बिखेरते हुए सुषोभित हो रहे हैं। उद्धरणों का वैभव कहें या टीका का वैभव एक ही अर्थ का द्योतन करते हुए प्रतीत होते हैं।
इस टीका में 62 ग्रंथों के 354 उद्धरण प्रस्तुत कर माता जी ने एक विषिश्ट कार्य किया है। अन्य टीकाओं पर दृश्टिपात करने से ज्ञात होता है कि टीका के कलेवर के अनुसार अपेक्षाकृत प्रायः कम ही उद्धरण देखने को मिलते हैं स्याद्वाद चन्द्रिका के समस्त उद्धरणों का पृथक संग्रह किया जावे तो एक रोचक संकलन ग्रंथ ही बन जावेगा।
नियमसार मूल में कुल 187 गाथायें, आर्या छंद हैं उनमें कुछ अनुश्टप भी हैं। प्रस्तुत टीका में प्रति गाथा 2 उद्धरण औसतन प्राप्त होते हैं यह एक उत्कृश्ट मानदण्ड ही ज्ञात होता है। मेरे देखने में इतना उद्धरण वैभव अन्यत्र देखने में नहीं आया। टीकागत लगभग 5000 पदों में 354 उद्धरणों से टीका इस प्रकार सुषोभित है जैसे आभूशणों से कामिनी सज्जित होती है।
ज्ञानमती माता जी बहुमुखी प्रतिभा की धनी, कुषल एवं सिद्धहस्त लेखिका हैं। काव्य प्रतिभा की परिचायक भक्तिरस से ओतप्रोत उनकी रचनाओं का संग्रह जिनस्तोत्रसंग्रह के नाम से प्रकाषित हुआ है। इसमें हिन्दी संस्कृत आदि भाशाओं में उनकी दिव्य लेखनी अपनी ही किसी कृति के अंषों का पद्य अनुवाद रूप भी है।
उसमें जिनस्तवन माला “ाीर्शक के अंतर्गत तीर्थंकरों के प्रति उन्होंने अपने गुणानुराग को व्यक्त किया है। यह प्रायः दृश्टिगोचर नहीं ही होता है कि कोई लेखक अपनी ही किसी कृति के अंषों को स्वयं के लेखन में उद्धृत करे। नियमसार की टीकाकत्र्री ने स्याद्वाद चन्द्रिका में कतिपय स्थलों पर अपना ही काव्य उद्धृत कर टीका को आकर्शक बनाया है।
नियमसार प्राभृत में निष्चय प्रत्याख्यान अधिकार अध्यात्म का प्रतिपादक एवं विषुद्ध ध्यानमूलक महा अध्याय है। इसमें कुन्दकुन्द स्वामी ने आत्मस्वरूप का निरूपण करने के साथ जीव के एकत्व भाव का भी निरूपण किया है।
गाथा क्रमांक 101 में उन्होंने निरूपित किया है कि जीव अकेला ही मरता है, अकेला ही जन्म लेता है, अकेला ही जीवित रहता है और अकेला ही कर्मरज रहित होकर सिद्ध होता है। यह चिंतन मुमुक्षु को उपयोगी एवं आवष्यक बताया है। इसी अर्थ का प्रतिपादन स्वरचित जिन स्तवन माला के स्वरूप सम्बोधक एवं वैराग्यपरक सुन्दर काव्य के उद्धरण द्वारा टीकाकत्र्री ने किया है, ध्यान देने योग्य है-
“शरीरी प्रत्येकं भवति भुवि वेधा स्वकृतितः।
विधत्ते तानाभूपवनजलवन्हिदु्रमतनुम्।
त्रसो भूत्वा भूत्वा कथमपि विधायात्र कुषलम्।
स्वयं स्वस्मिन्नास्ते भवति कृतकृत्यः षिवमयः।।
प्रत्येक “शरीरधारी प्राणी इस संसार में स्वयं अपने कर्मों से अपना विधाता होता है। यह अनेक प्रकार के पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और वनस्पति के “ारीर को धारण करता रहता है। कभी त्रस होकर बड़ी मुष्किल से कुछ पुण्य करके स्वयं ही अपने में स्थित हो जाता है तब यह षिवरूप होकर कृतकृत्य भगवान हो जाता है। पाठक इस प्रकार के उद्धरणों से अवष्य भावबोध को प्राप्त होता है।
आगम में निष्चय प्रत्याख्यान का साधक व्यवहार प्रत्याख्यान कहा है। भोजन संबंधी इच्छाओं का परित्याग कर आत्मस्वरूप में लीन होना निष्चय प्रत्याख्यान है। स्याद्वाद चन्द्रिका में निष्चय प्रत्याख्यान के अंतर्गत टीकाकत्र्री ने भोजन सम्बंधी प्रत्याख्यान के 10 भेदों का सलक्षण उल्लेख आचार्य वसुनन्दि की मूलाचार टीका से उद्धृत करके किया है।
| 1- अनागत | 2- अतीत | 3- कोटिसहित | 4- विखंडित |
| 5- साकार | 6- अनाकार | 7- परिमाणगत | 8- अपरिषेश |
| 9- अध्वानगत | 10- सहेतुक |
इन 10 प्रत्याख्यानों का स्वरूप इस टीका में लिखा गया है। प्रायः पाठक को ज्ञान की अल्पता, अवकाष की कमी, अनभिज्ञता आदि कारणों से बडे़ बडे़ ग्रंथों को देखने पढ़ने का योग नहीं मिलता। इस अभाव की पूर्ति स्याद्वाद चन्द्रिका में समाविश्ट उद्धरणों से अपेक्षित रूप में संभावित है।
बाह्य तप अर्थात व्यवहार प्रत्याख्यान, अंतरंग तप अर्थात निष्चय प्रत्याख्यान का कारण जैनागम में उल्लिखित है। इस पर माता जी ने प्रस्तुत टीका में सम्यक् प्रकाष डालकर सिद्धि की है। इसी की अपेक्षायुक्त आगम प्रमाण के रूप में निम्न उद्धरण टीका मंे आषय को स्पश्ट कर सुषोभित हो रहा है-
वाह्यं तपः परमदुष्चरमाचरस्त्वं आध्यात्मिकस्य तपसः परिवृंहणार्थम्।
ध्यानं निरस्य कलुशद्वयमुत्तरस्मिन् ध्यानद्वये ववृतिशेतिषयोपपन्ने।।83।।
हे भगवान! आध्यात्मिक तप की वृद्धि के लिए अपने कठोर बाह्य तप का आचरण किया है एवं आर्त रौद्र इन दो कलुशित ध्यानों का निरसन कर धर्मषुक्लध्यान रूप अतिषय ध्यानद्वय की प्राप्ति की है।
यहां स्याद्वाद चन्द्रिका की एतद्विशयक कतिपय पंक्तियों को उद्धृत करना उपयोगी होगा। ये पंक्तियां मार्ग की प्रतिश्ठापक ही हैं। अर्हंत भगवान के दिव्योपदेष की सारभूत ही है-
‘‘ये केचिद् भव्योतमा जैनेष्वरीं दीक्षामादाय सुश्ठुतया स्वाचरणविधिं ज्ञात्वा मूलाचारमया भवन्ति त एव प्रत्याख्यानेन परिणता सन्तो निष्चय नियमसारा भविश्यन्ति न चान्ये।’’
जो कोई भव्योत्तम जैनेष्वरी दीक्षा को लेकर अच्छी तरह से अपने आचार की विधि को जानकर मूलाचार मय हो जाते हैं, वे ही प्रत्याख्यान रूप परिणत होते हुए निष्चय नियमसार हो जाते हैं अन्य नहीं।’’
आषय यह है कि मूलाचार के अनुसार बाह्य तप धारण कर मुनि अवस्था अंगीकार करने के पष्चात् ही निष्चय मोक्षमार्ग की प्राप्ति होती है। गृहस्थ अवस्था से नहीं।
जिनकथित मोक्षमार्ग में भावविषुद्धि मूलतत्व निरूपित की गई है। भाव- विषुद्धि, चित्त की निर्मलता से ही ध्यान की सिद्धि, आत्मसाक्षात्कार होता है।
बन्ध मोक्ष का उपादान मन ही है। कहा भी है-
‘‘मनः एव मनुश्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः।’’
आचार्य कुन्दकुन्द ने परम आलोचना अधिकार के अंतर्गत नियमसार में निम्न गाथा प्रस्तुत की है-
मदमाणमायलोहविवज्जिय भावो दु भावसुद्धि त्ति।
परिकहियं भव्वाणं लोयालोयप्पदरिसीहिं।। 118।।
लोकालोक के प्रदर्षी अर्हन्त भगवान ने भव्यों के लिए मद मान माया लोभ से रहित भाव को ही भावषुद्धि कहा है।
टीकाकत्र्री ने प्रस्तुत गाथा की टीका के अंतर्गत आ० पद्मनन्दीकृत पंचविंषतिका के निष्चय प×चाषत् अधिकार से निम्नलिखित आर्या छन्द उद्धृत कर गृद्धपिच्छाचार्य के आषय को सुश्ठु प्रकट किया है।
चित्तेन कर्मणा त्वं बद्धो यदि बध्यते त्वया तदतः।
प्रतिबन्दीकृतमात्मन्! मोचयति त्वां न सन्देहः।। 37।।
हे आत्मन् तुम मन के द्वारा कर्म से बांधे गये हों यदि तुम उस मन को बांध लेते हो वष में कर लेते हो तो इससे वह प्रतिबन्दीस्वरूप होकर तुमको छुड़ा देगा इसमें सन्देह नहीं।
वस्तुतः कुन्दकुन्द स्वामी के अनुसार मन को रागद्वेश से रहित करना, भाव विषुद्धि करना ही मन का वषीकरण है। मन को कहीं अन्दर या बाहर ले जाकर बन्द कर देना बन्दीकरण नहीं है अपितु उसकी प्रकृति के विकार राग, द्वेश, (क्रोध, मान, माया, लोभ) का समापन ही मन का निरोध या प्रतिबन्दीकरण है।
चित्त की शुद्ध हेतु साधु के विधायी कर्तव्य की पे्ररणा करने के उद्देष्य से परम आलोचना अधिकार में ही आ० पद्मनन्दी के इसी आलोचना नामक प×चविंषतिका के अधिकार में से एक गाथा माता जी ने उद्धृत की है उससे यह सिद्ध होता ह
कि मुनिपद में व्यवहार आलोचना के द्वारा निष्चय आलोचना संभव है। आ० पद्मनन्दी ने कहा है-
आश्रित्य व्यवहारमार्गमथवा मूलोत्तराख्यान् गुणान्।
साधोर्धारयतो मम स्मृतिपथप्रस्थायि यद् दूशणम्।
“शुद्धर्थं तदपि प्रभो! तव पुरः सज्जोहमालोचितुम्।
निःषल्यं हृदयं विधेयमजडैर्भव्यैर्यतः सर्वथा।। 9।।
यहां साधुओं को “शल्यरहित हृदय से आत्मालोचन, आत्ममन्थन करने का उपदेष दिया गया है।
उपरोक्त प्रकार स्याद्वाद चन्द्रिका में उद्धृत कतिपय उद्धरणों से पाठकों को ज्ञात हो जायेगा कि प्रस्तुत टीका अति समृद्ध है। विशय विस्तार के भय से यहां संक्षिप्त प्रस्तुतीकरण किया है।
जिन 62 गंरथों के उद्धरणों को इस टीका में स्थान दिया गया है उनकी सूची यहां उपयोगी जानकर प्रस्तुत की जा रही है।
| 1- लोकवात्र्तिक | 2- तिलोयपण्णत्ती भाग-1 | 3- तिलोयपण्णत्ती भाग-2 | 4- तत्वार्थ सूत्र |
| 5- तत्वार्थ वात्र्तिक | 6- गोम्मटसार जीवकाण्ड | 7- गोम्मटसार कर्मकाण्ड | 8- प×चास्तिकाय |
| 9- अश्टसहस्री | 10- नयचक्र | 11- आलाप पद्धति | 12- मोक्षप्राभृत |
| 13– समयसार कलष | 14- नियमसार टीका (आ० पद्मप्रभकृत) | 15- बृहद्द्रव्य संग्रह (टीका श्री ब्रह्मदेव सूरि) | 16- कशायपाहुड सूत्र |
| 17- लब्धिसार | 18- भगवती आराधना | 19- धवला पुस्तक-6 | 20- सर्वार्थसिद्धि |
| 21- मूलाचार | 22- प्रवचनसार | 23- जयधवला पुस्तक-1 | 24- श्री कुन्दकुन्द कृतभक्ति संग्रह |
| 25- धवला पुस्तक-1 | 26- आचार सार | 27- दषभक्ति | 28- यतिप्रतिक्रमण |
| 29- अनगार धर्मामृत | 30- पद्मनन्दीप×चविंषति | 31- परमात्मप्रकाष | 32- समाधिषतक |
| 33- भावसंग्रह | 34- कातन्त्रव्याकरण | 35- भद्रबाहुचरित्र | 36- द्वात्रिंषतिका |
| 37- सामायिक भाश्य | 38- प्रतिक्रमण ग्रंथत्रयी | 39- ज्ञानार्णव | 40- क्रियाकलाप |
| 41- आदिपुराण | 42- इश्टोपदेष | 43- हरिवंषपुराण | 44- धवला पुस्तक-1 |
| 45- पुरूशार्थसिद्ध्युपाय | 46- परीक्षामुख | 47- लधीयस्त्रय | 48- धवला पुस्तक-8 |
| 49- रत्नकरण्ड श्रावकाचार | 50- पात्रकेसरि स्तोत्र | 51- त्रिलोकसार | 52- जैनेन्द्रव्याकरण |
| 53- कल्याणमंदिर स्तोत्र | 54- आप्त मीमांसा | 55- द्रव्यसंग्रह | 56- वसुनन्दि श्रावकाचार |
| 57- परमानंद स्तोत्र | 58- समयसार | 59- चन्द्रप्रभस्तुति | 60- आत्मानुषासन |
| 61- स्वयंभूस्तोत्र | 62- एकीभाव स्तोत्र |
प्रस्तुत उद्धरण वैभव अध्याय का सारांष यह है कि स्याद्वाद चन्द्रिका का प्राणतत्व आगम के प्रमुख अंषों से परिपुश्ट है। यह तो पाठक जानते ही हैं कि टीका का अभिप्रेत स्वयं टीकाकार का न होकर मूलग्रंथकर्ता का ही होता है। उस कथ्य को पाठक तक सुरक्षित रूप में कैसे पहुंचाया जाय ताकि वह अर्थ को हृदयंगम भी कर ले और विशयान्तर भी न हो, इस हेतु उद्धरणों का बड़ा सहारा होता है।
टीकाकत्र्री ने इस उद्धरण प्र्रस्तुतीकरण विद्या का भरपूर प्रयोग कर नियमसार के विशय को पल्लवित कर हम तक सफलतापूर्वक पहुंचाया है। वे साधुवाद की पात्र हैं उनका प्रयत्न भगीरथ प्रयत्न के समान जिनवाणी रूप गंगा की “ाीतलता एवं सुखद स्पर्ष को चतुर्दिक प्रस्तारित करता हुआ स्तुत्य है।
