तत्त्वार्थ सूत्र प्रवचन ( प्रथम अध्याय )
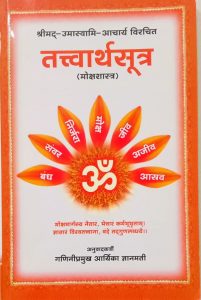
प्रवचन कर्त्री -आर्यिका चंदनामती माताजी
मंगलाचरण
सिद्धेर्धाममहारिमोहहननं कीर्ते: परं मंदिरम्।
मिथ्यात्वप्रतिपक्षमक्षयसुखं संशीतिविध्वंसनम्।।
सर्वप्राणिहितं प्रभेन्दुभवनं सिद्धिप्रमालक्षणम्।
संतश्चेतसि चिन्तयंतु सुधिय: श्रीवर्धमानं जिनम्।।
भगवान् महावीर द्वारा प्रतिपादित सम्पूर्ण द्वादशांग के सार को अपने में समाहित किए हुए ग्रन्थराज तत्त्वार्थसूत्र अनेकान्त वाणी को प्रतिपादित करने वाला है इसीलिए उसे मोक्षशास्त्र भी कहा जाता है। इस ग्रन्थ के मंगलाचरण का प्रथम पद ही मोक्ष शास्त्र की सार्थकता को बतलाता है। उमास्वामी आचार्य ने सूक्ष्म चिंतनपूर्वक ही इस ग्रंथ में समस्त सार रहस्य को गागर में सागर सदृश भर दिया है। इसके दश अध्यायों में क्रमशः सात तत्त्वों का वर्णन पाया जाता है। उन्हीं में से प्रथम अध्याय का कुछ सार यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है। सर्वप्रथम ग्रन्थकर्ता आचार्य श्री उमास्वामी द्वारा किए गए मंगलाचरण को आपको जानना है–
मोक्षमार्गस्य नेतारं, भेत्तारं कर्मभूभृताम्।
ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां, वन्दे तद्गुण लब्धये।।१।।
अर्थ — जो मोक्षमार्ग के नेता है, कर्मरूपी पर्वतों का भेदन करने वाले हैं और विश्व के समस्त तत्त्वों के ज्ञाता–जानने वाले हैं, ऐसे किसी परमात्मपद को मैं उनके गुणों की प्राप्ति हेतु नमस्कार करता हूं। देखिए न ! स्वार्थपरता की पराकाष्ठा, भगवान् के नमस्कार में भी भक्त का कितना स्वार्थ छिपा है। शायद स्वार्थ के बिना कोई किसी को पूछता ही नहीं है किन्तु किसी की समूलचूल वस्तु को मांगते हुए नमस्कार करने का तो कोई ढंग नहीं समझ में आता ? यदि किसी सेठ साहूकार के पास जाकर कोई सेवक खूब नमस्कार करे और उसकी सम्पूर्ण सम्पत्ति की माँग करे तो क्या सेठजी उसे अपनी सारी सम्पत्ति देने को राजी हो जायेंगे ? नहीं, वे तो कभी नहीं देने वाले, जिस सम्पत्ति को खून पसीना एक करके उन्होंने कमाया है, अपने प्राणों से अधिक उसकी रक्षा की है, स्वयं के भोगों में तो सोच-सोच कर एक-एक पैसा निकालते हैं तो भला कैसे उस सम्पत्ति को दूसरे के लिए दे देंगे। यदि बहुत उदारता भी दिखाएंगे तो थोड़ा बहुत दानस्वरूप तो दे सकते हैं किन्तु सारी सम्पत्ति न तो वह दे ही सकते हैं और न मांगने वाला स्वयं इतनी हिम्मत ही कर सकता है। लेकिन ध्यान दीजियेगा कि हमारे जिनेन्द्र भगवान अत्यन्त उदार हैं उनसे आप उनकी पूरी सम्पत्ति भी मांग लेवें तो वे प्रतिक्षण देने को तैयार रहते हैं। शर्त यह है कि आपको उन जैसी मुद्रा स्वीकार करनी पड़ेगी और अपना सर्वस्व समर्पण करना पड़ेगा। समर्पण करना कोई कठिन बात भी नहीं है। चाहे गुरु हों या भगवान्, यदि उनके प्रति आप सर्मिपत हो गए तो कोई भी पद या गुण की प्राप्ति दुर्लभ नहीं है अन्यथा कितनी भी ज्ञानाराधना करें, पूजा करें किन्तु समर्पित भावना नहीं है तो आपकी पदोन्नति नहीं हो सकती है।
एक संक्षिप्त उदाहरण आपको बताती हूँ— एक असहाय बालक दर-दर की ठोकरें खाता था। एक दिन किसी सेठ ने उसे देखा तो करुणावश उसको अपने घर लाकर सेठानी को सौंप दिया और बोले कि इसे भी पुत्रवत् स्नेह देकर अपने घर में रखना है। पति की आज्ञावश न चाहते हुए भी सेठानी को उसका पालन पोषण करना पड़ता था। सेठ ने बालक से कहा—आज से हम लोग तुम्हारे माता—पिता हैं और तुम हमारे पुत्र हो। बालक प्रसन्नतापूर्वक सेठ के घर में रहने लगा किन्तु सेठानी अपने कर्कश स्वभाववश उस बालक को बहुत कष्ट देती। उससे दिन भर खूब काम करवाती, फटकारती, मारती तथा रात्रि को सेठजी के समाने प्यार जताती। यही क्रम प्रतिदिन चल रहा था।
तभी एक दिन— प्रात:काल बालक ग्वाले के यहाँ से दूध लेकर आ रहा था अकस्मात् रास्ते में ठोकर खाकर गिरने से सारा दूध गिर गया। बेचारा बालक बहुत सहम गया कि कैसे घर जाऊँ, क्या कहूँ ? सेठानी तो वैसे ही रोज मुझे डाँटती मारती है, आज जाने क्या होगा ? किसी तरह डरते-डरते वह घर आया किन्तु जो सोचा था उससे कहीं ज्यादा अनुभव अया। मार-मार कर सारी चमड़ी लाल कर दी सेठानी ने और घर से बाहर निकालकर दरवाजा बन्द कर लिया। एक वृक्ष के नीचे बेचारा उदास बालक बैठा था। मार्ग से एक बाबाजी निकले, उन्होंने पूछा—रेलवे स्टेशन किधर है? इतना सुनते ही बालक उसके साथ ही स्टेशन की ओर चल दिया। रास्ते में दोनों का वार्तालाप हुआ। बालक को बहुत दुखी देखकर बाबाजी ने उससे पूछा—बेटे! तुम उस सेठानी को क्या कहकर सम्बोधित करते थे ? बालक बोला—वह तो सेठानी है इसलिए मैं उसे सेठानी ही कहता था और वह मुझे नौकर समझकर सारा कार्य कराती थी। बाबा बोले—कभी तुमने प्यार से उसे माँ कहकर पुकारा होता तो वह भी तुम्हें पुत्रवत् स्नेह देती। खैर! जो हुआ उसे जाने दो। मेरी मानो एक बार जाकर तुम उसे माँ कहकर समर्पित हो जाओ वह भी तुम्हें पुत्र ही मानेगी।
बालक के बहुत मना करने पर भी बाबाजी ने उसे घर भेज दिया और बोला—यदि फिर भी तुम वहाँ न रह सको तो वापस आना, मैं तुम्हें अपने साथ ले चलूंगा। मार्ग में अनेकों विचारों में झूलता उतराता है बालक! सोचता है कि सच बात तो है, जब मैने उसे माँ नहीं समझा तो वह भला मुझे पुत्र वैâसे समझती। बस! उसने निर्णय कर लिया और दौड़ा—दौड़ा घर की ओर चल पड़ा। दोनों ओर की भावनाओं का तारतम्य देखिए। इधर सेठानी भी दरवाजे पर खड़ी पुत्र का मानो इन्तजार ही कर रही थी। बालक आते ही सेठानी के पैरों में लिपट गया और बोला—माँ! मुझे माफ कर दो, तुम्हारे सिवाय तो संसार में मेरा कोई नहीं है। अश्रुपूरित नेत्रों से माँ ने बेटे को पुचकारा और नहलाकर भोजन कराया, सुख दुख पूछा। समर्पित भावों से एक असहाय बालक को अपनी माँ मिल गई और सेठानी के अन्दर असली मातृत्त्व भी जाग उठा। वह सोचती है कि मुझसे बड़ी गलती हुई।
यदि मेरे पुत्र से ही दूध गिर जाता तो………… इन उदाहरणों से प्रत्येक मानव को शिक्षा लेनी चाहिए। माता-पिता की सम्पत्ति, गुरु का स्नेह, प्रभु की गुण सम्पत्ति सभी पुत्र, शिष्य और भक्त को सर्मिपत भावनाओं से स्वयं प्राप्त हो जाते हैं। उन्हें मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यदि उनकी आज्ञा की अवहेलना होती रहे, भक्त के स्थान पर बगुला भगत बनकर मात्र भक्ति ही करते रहे, पीठ पीछे उनके अनादर की प्रबल भावना रही तो सिवाय पाप बन्ध के कोई गुण या सम्पत्ति प्राप्त नहीं होती। आचार्य श्री उमास्वामी ने भी ‘वन्दे तद्गुणलब्धये’ कहकर प्रभु की वंदना की है क्योंकि उन्होंने स्वयं दिगम्बर मुनि दीक्षा धारण कर स्वयं को प्रभू के हवाले कर दिया था। निरीहवृत्तिपूर्वक अयाचकवृत्ति से इस मोक्षशास्त्र की रचना प्रारम्भ करते हुए अपने से महान व्यक्तित्व के प्रति शीश झुकाया था। उनका यह मंगलाचरण ही इतना महान है कि जिसके ऊपर अनेकों आचार्यों ने बड़ी-बड़ी टीकाएं लिख डालीं। श्री विद्यानन्दि स्वामी ने इस मंगलाचरण के ऊपर ‘आप्तपरीक्षा’ नामक ग्रन्थ लिखकर उसकी स्वोपज्ञ टीका लिखी है। श्री समन्तभद्र स्वामी ने इस मंगलाचरण की टीका करते हुए ‘आप्तमीमांसा’’ नामक स्तोत्र ग्रंथ को ११४ कारिकाओं में रच डाला है। इसी स्तोत्र पर श्री भट्टाकलंक देव ने आठ सौ श्लोक प्रमाण ‘अष्टशती भाष्य’ बनाया है, अनंतर श्री विद्यानन्दि स्वामी ने आप्तमीमांसा की कारिका सहित इस अष्टशती को लेकर आठ हजार श्लोक प्रमाण ‘अष्टसहस्री’ ग्रंथ की रचना कर डाली है; जिसे न्यायदर्शन का उच्चतम ग्रंथ माना जाता है। इस ग्रंथ के बारे में वर्णन करते हुए स्वयं विद्यानन्दि महोदय ने इसे ‘कष्टसहस्री’ शब्द से सम्बोधित किया है।
अष्टसहस्री के विषय में एक जर्मन के न्यायदर्शनविज्ञ ने कहा है— ‘‘जिसने जैनकुल में जन्म लेकर अष्टसहस्री ग्रंथ नहीं पढ़ा वह जैन नहीं और जो अष्टसहस्री पढ़कर जैन नहीं बना तो समझो उसने अष्टसहस्री पढ़ी ही नहीं।’’ अर्थात् अनेकांत स्याद्वाद का झण्डा फहराने वाला यह एकमात्र ग्रंथ है। इसी अष्टसहस्री ग्रंथ का हिन्दी में अनुवाद किया था वर्तमान की परम विदुषी, सरस्वती की प्रतिमूर्ति, गणिनी आर्यिका श्री ज्ञानमती माताजी ने सन् १९७० में, जो प्रकाशित होकर भक्तों को न्याय का उच्च कोटि का विद्वान बनाने में सहायक सिद्ध हो रहा है। कुछ वर्ष पूर्व यह चर्चा उठी थी कि यह मंगलाचरण आचार्य उमास्वामी कृत नहीं है प्रत्युत् सर्वार्थसिद्धि ग्रंथ के प्रारम्भ में उपलब्ध होने से यह सर्वार्थसिद्धि का मंगलाचरण है। इस पर अनेक विद्वानों ने इसे श्री उमास्वामी कृत घोषित किया है। आचार्य उमास्वामी आचार्य श्री कुन्दकुन्ददेव के पट्टशिष्य थे जिसका वर्णन श्रवलबेलगोला स्थित एक शिलालेख में है कि—
अभूदुमास्वाति मुनि: पवित्रे वंशे तदीये सकलार्थवेदी।
सूत्रीकृतं येन जिनप्रणीतं शास्त्रार्थजातं मुनिपुङ्गवेन।।
स प्राणिसंरक्षणसावधानो बभार योगी किल गृद्धपिच्छान्।
तदा प्रभृत्येव बुधा यमाहुराचार्यशब्दोत्तरगृद्धपिच्छम्।।
आचार्य कुन्दकुन्द की वंश परम्परा में गृद्धपिच्छाचार्य (उमास्वाति आचार्य) हुए जिनके समान इस धरती पर आगम का कोई ज्ञात नहीं था। उन्होंने तत्त्वार्थसूत्र का मंगलाचरण रचकर उसमें बहुत सार भर दिया। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें किसी व्यक्ति विशेष को नमस्कार न करके ऐसे गुणों को नमस्कार किया है जो किसी भी व्यक्ति में घटित हो सकते हैं। यहाँ एक प्रमाण मैं और प्रस्तुत कर रही हूँ। आप्तमीमांसा की ११४ वीं कारिका की टीका में अष्टसहस्री ग्रंथकार श्री विद्यानन्दि स्वामी क्या कहते हैं—
‘‘शास्त्रारम्भेभिष्टुतस्याप्तस्य मोक्षमार्गप्रणेतृतया
कर्मभूमृद्भोत्तृतया विश्वतत्त्वानां ज्ञातृतया च
भगवदर्हत् सर्वज्ञस्यैवान्ययोगव्यवच्छेदेन
व्यवस्था-पनपरा परीक्षेयं विहिता।’’
अर्थात् शास्त्र के प्रारम्भ में स्तुति को प्राप्त जो आप्त हैं, वे मोक्षमार्ग के प्रणेता, कर्म पर्वत के भेत्ता और विश्वतत्त्व के ज्ञाता इन तीन विशेषणों से युक्त भगवान अर्हंत सर्वज्ञ ही हैं, अन्य कोई नहीं हो सकते हैं। इस प्रकार अन्य योग का व्यवच्छेद करके भगवान् अर्हंत में ही इन विशेषणों की व्यवस्था को करने में तत्पर यह परीक्षा की गई है। यह है सारे अष्टसहस्री ग्रंथ का अन्तिम उपसंहार। यह मंगलाचरण उमास्वामी आचार्यकृत ही है, इस बात को सिद्ध करने के लिए इससे बढ़कर सबल प्रमाण और क्या हो सकता है ? श्लोकवार्तिकालंकार ग्रंथ में भी श्री विद्यानंदि महोदय ने कई स्थलों पर इसी बात को स्पष्ट किया है। जब एक मंगलाचरण के ऊपर आप्तमीमांसा, अष्टशती, अष्टसहस्री जैसे जैनदर्शन के सर्वोपरि ग्रंथ बन गये तब उस ग्रंथ की जितनी भी गौरवगाथाएं गाई जावें, थोड़ी ही हैं। यही कारण है कि आज भी भारतवर्ष में दक्षिण-उत्तर आदि प्रान्तों में सर्वत्र नर-नारी इस तत्त्वार्थसूत्र का पाठ बड़ी भक्ति से करते हैं और एक उपवास करने का फल प्राप्त करते हैं। बहुत सी महिलाओं का तो नियम ही रहता है कि ‘‘तत्त्वार्थसूत्र’’ सुने बिना भोजन नहीं करना। कहा भी है—दशाध्याये परिच्छिन्ने, तत्त्वार्थे पठिते सति।
फलं स्यादुपवासस्य, भासितं मुनिपुंगवै:।।दश अध्याय से परिपूर्ण इस तत्त्वार्थसूत्र को पढ़ने पर एक उपवास का फल प्राप्त होता है ऐसा श्री मुनियों में श्रेष्ठ मुनियों ने कहा है। इस ग्रंथ का यह मंगलाचरण सच्चे आप्त–देव को सिद्ध करने में सर्वोपरि मान्य अमोघ उपाय है ऐसा समझना चाहिए। अब प्रथम अध्याय के प्रथम सूत्र का अवतार होता है— सम्यग्दर्शन ज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्ग:।।१।।
अर्थ — सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यव्चाचरित्र इन तीनों की एकतारूप रत्नत्रय मोक्ष का मार्ग है। संसार सागर में डूबते हुए संसारी प्राणियों के उद्धार की पुण्य भावना से मोक्षमार्ग का निरूपण करने वाले इस सूत्र की रचना आचार्य श्री उमास्वामी महाराज ने की है। इन तीन रत्नों की व्याख्या तत्त्वार्थराजर्वाितक के कत्र्ता श्री भट्टाकलंक स्वामी ने निम्न प्रकार से की है— दर्शनमोह कर्म के उपशम, क्षय या क्षयोपशम रूप अंतरंग कारण से होने वाले तत्त्वार्थ श्रद्धान को सम्यग्दर्शन कहते हैं। प्रमाण और नयों के द्वारा जीवादि तत्त्वों का संशय, विपर्यय और अनध्यवसाय से रहित यथार्थ बोध सम्यग्ज्ञान कहलाता है।
संसार के कारणभूत राग—द्वेषादि की निवृत्ति के लिए कृतसंकल्प विवेकी पुरुष का शरीर और वचन की बाह्य क्रियाओं से तथा अभ्यंतर मानस क्रियाओं से विरक्त होकर स्वस्वरूप स्थिति का प्राप्त करना सम्यक्चारित्र है। पूर्ण यथाख्यात चारित्र वीतरागी-ग्यारहवें और बारहवें गुणस्थान में तथा जीवनमुक्त केवली के होता है। उससे नीचे विविध प्रकार का चारित्र श्रावकों को तथा दसवें गुणस्थान तक के साधुओं को होता है। इसके अतिरिक्त सर्वार्थसिद्धि, तत्त्वार्थवृत्ति आदि अनेकानेक ग्रंथों के अन्दर यही बताया है कि इन तीनों की एकता ही मोक्षमार्ग का दिग्दर्शन कराने वाली है। केवल सम्यग्दर्शन आपको मोक्ष प्रदान नहीं करेगा। only the right knowledge cannot, Only the right conduct cannot, but the mixture of all will take us to salvation केवल सम्यग्ज्ञान अथवा केवल सम्यक्चारित्र ही आपको मोक्ष प्रदान नहीं कर सकते अपितु इन तीनों का जहाँ पूर्ण रूप से एकीकरण—समावेश हो जाता है वहीं मोक्षमार्ग साकार होता है। यद्यपि मोक्ष साक्षात् रूप में दिखता नहीं है फिर भी उसका कथन किया गया है क्योंकि बहुत सी चीजें प्रत्यक्ष नहीं भी दिखती हैं तो भी उका अस्तित्त्व स्वीकार करना पड़ता है। कर्मोदय की निवृत्ति होने पर चतुर्गति का चक्र रुक जाता है और उसके रुकने से संसार रूपी घटीयन्त्र का परिचलन समाप्त हो जाता है, इसी का नाम मोक्ष है। चूँकि प्राणी अनादिकाल से कर्मों के बन्धन में जकड़ा हुआ है। जैसे जेल में पड़ा हुआ व्यक्ति यदि अपने मुक्त होने का समाचार जान लेता है तो आश्वस्त होकर संसार से मुक्त होने का प्रयास करने लगता है। जैन सिद्धान्त में आचार्यों ने सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र इनको रत्न की संज्ञा दी है, जो प्रत्येक प्राणी में विद्यमान रहते हैं। व्यवहार में रत्नों को रखने वाला ‘जौहरी’ कहलाता है इसलिए आप सभी जौहरी हैं ऐसा श्रद्धान रखें। जौहरी अपने रत्नों को खूब संभालकर रखता है। आपने देखा होगा कि जब आप किसी ज्वैलर्स की दुकान पर जाकर किसी रत्न को दिखाने की मांग करते हैं तो वह एक मजबूत अलमारी खोलता है। अलमारी के अन्दर भी लॉकर खोलता है और उसमें से रत्नों का डिब्बा निकालता है। इतना ही नहीं, डिब्बे के अन्दर डिब्बी, डिब्बी में लाल कागज की पुड़िया में रुई में लिपटा नगीना निकाल कर बड़े सुरक्षित ढंग से ग्राहक के समक्ष प्रस्तुत करता है। उसी प्रकार आपकी तिजोरी में भी तीन-तीन अनमोल रत्न बड़े सुरक्षित रखे हैं आप उन्हें प्रगट कर अपने शहर के जौहरी ही नहीं तीन लोक के सर्वोत्तम जौहरी बन सकते हैं। जहां आपके पास मांगने वाले भक्तों (ग्राहकों) की भीड़ लग जाएगी। पूज्य गणिनीप्रमुख श्री ज्ञानमती माताजी ने अपने तीनलोक मण्डल विधान पूजन की एक जयमाला में बड़े सुन्दर भाव संजोए हैं
— दोहा—
तीर्थंकर गुणरत्न को, गिनत न पावें पार।
तीन रत्न के हेतु मैं, नमूँ अनन्तों बार।।
वीतरागी तीर्थंकर भगवान् कुछ देते—लेते नहीं हैं किन्तु भक्त अपनी प्रबल भक्ति के वश उन रत्नाधिपति की स्तुति करके उन वेशकीमती रत्नों को प्राप्त कर लेता है इसीलिए उपर्युक्त पंक्तियों में यह भावना निहित है कि हे भगवन् ! मैं तीन रत्नों को पाने हेतु आपको तीन बार नहीं अनन्त बार नमस्कार करता हूँ। यदि तीनों में से एक की भी कमी रह गई तो मोक्ष नहीं मिल सकता। श्रद्धा, ज्ञान, आचरण ये तीनों अभिन्न रूप से जब आत्मा में प्रगट होंगे तभी मोक्षमार्ग प्रशस्त होगा अन्यथा नहीं। न तो केवल सम्यग्दर्शन मोक्ष दिला सकता है, न ज्ञान और न अकेला चारित्र, अन्यथा वह मोक्ष धरती पर ही साकार हो जाता। मोक्ष तो उस चरम अवस्था का नाम है जहां तीनों इकट्ठे होकर भी आत्मा के एक रूप में पूर्ण हो जाते हैं। इसीलिए तीनों के मिलन का नाम मोक्षमार्ग बताया है न कि मोक्ष। यह रत्नत्रय अग्नि के उष्ण स्वभाव और जल के शीतल स्वभाव की भांति चैतन्य आत्मा का स्वभाव है क्योंकि आत्मा के उष्ण स्वभाव है क्योंकि आत्मा को छोड़कर अन्य द्रव्यों के साथ इसका सम्बन्ध नहीं पाया जाता है। आचार्य श्री उमास्वामी की निर्दोष लेखनी द्वारा द्वितीय सूत्र का अवतार हुआ—
‘‘तत्त्वार्थश्रद्धानं सम्यग्दर्शनम्’’।।२।।
अर्थ—तत्त्वार्थ का श्रद्धान सम्यग्दर्शन है।दर्शन शब्द ‘दृष्टि’ धातु से बना है और दृशि धातु का अर्थ देखना है। वैसे एक धातु के अनेक अर्थ भी होते हैं अतः प्रकरण के अनुसार यहां दर्शन का अर्थ श्रद्धान लिया जाएगा ‘‘तस्य भाव: तत्त्वम्’’ तत्त्वार्थ का अर्थ है कि जो पदार्थ जिस रूप से स्थित है उसका उसी रूप से ग्रहण करना। तात्पर्य यह है कि जिसके होने पर तत्त्वार्थ अर्थात् वस्तु का यथार्थ ग्रहण हो उसे सम्यग्दर्शन कहते हैं। राजर्वाितककार ने सम्यग्दर्शन के सराग और वीतराग नाम से दो भेद बताये हैं। प्रशम, संवेग, अनुकम्पा और आस्तिक्य से जिसका स्वरूप अभिव्यक्त होता है वह सराग सम्यग्दर्शन है। मोहनीय की सात कर्म प्रकृतियों का पूर्ण नाश होने पर आत्मविशुद्धि रूप वीतराग सम्यग्दर्शन है। वीतराग सम्यक्त्व की प्राप्ति में सरागसम्यक्त्व साधन होता है। सम्यग्दर्शन कैसे उत्पन्न होता है ? तीसरे सूत्र में बताते हैं
‘‘तन्निसर्गादधिगमाद्वा’’।।३।।
अर्थ — सम्यग्दर्शन निसर्ग (स्वभाव) और अधिगम (परोपदेश) दो प्रकार से उत्पन्न होता है। दोनों ही सम्यग्दर्शनों में अंतरंग कारण तो दर्शनमोह का उपशम, क्षय या क्षयोपशम समान है। इसके होने पर जो सम्यग्दर्शन बाह्योपदेश के बिना प्रगट होता है वह निसर्गज है तथा जो पर के उपदेश से होता है वह अधिगमज है। जैसे किसी ने पूर्वभव में गुरु का उपदेश ग्रहण किया था अत: आगे जाकर अगले भव में बिना उपदेश के पूर्व संस्कारवश अन्य कोई कारण मिलने से सम्यग्दर्शन उत्पन्न हो जाता है तो उसे निसर्गज कहते हैं। इसमें वर्तमान भव का परोपदेश विवक्षित न होकर पूर्वभव का परोपदेश कार्यकारी माना जाता है। वर्तमान भव में गुरु के उपदेश से ग्रहण किया गया सम्यक्त्व अधिगमज कहलाता है। यह दोनों ही सम्यग्दर्शन देशनालब्धि के बिना किसी को नहीं होते। चाहे देशना इस भव में प्राप्त हो या अगले भव में। वर्तमान युग में इस सम्यग्दर्शन के विषय में ही विवाद चल रहा है, और आश्चर्य इस बात का है कि वह विवाद अपने को दिगम्बर जैन मानने वाले दिगम्बर ‘सम्प्रदाय’ के भीतर ही चल रहा है। इसलिए सम्यग्दर्शन के बारे में ही भली प्रकार से जान लेना आवश्यक हो जाता है। वह सम्यग्दर्शन किसको, कब और कैसे होता है ? ये तीन बातें ही मुख्यतया ज्ञातव्य हैं। पूज्य ज्ञानमती माताजी ने ‘प्रवचन निर्देशिका’ नामक ग्रंथ में लिखा है— ‘वह भव्य जीव को ही होता है, अभव्य को नहीं। काललब्धि आदि के मिलने पर ही होता है, उसके बिना नहीं और अन्तरंग तथा बहिरंग कारणों से ही होता है बिना कारण के नहीं। हम और आप भव्य हैं या अभव्य ? काललब्धि आई है या नहीं ? इसका निर्णय तो सर्वज्ञ देव के सिवाय अन्य कोई कर नहीं सकता क्योंकि कोई अभव्य जीव ग्यारह अंग का ज्ञानी और निर्दोष-निरतिचार चारित्र का पालन करने वाला महातपस्वी मुनि होकर ही नवमें ग्रैवेयक में जा सकता है। हम और आप जैसे साधारण मनुष्य नहीं। उनमें किस रूप से मिथ्यात्व रहता है उसका निर्णय आप नहीं कर सकते, वह तो सर्वज्ञ गम्य ही है।’ यहाँ एक बात यह विशेष ध्यान देने की है कि जिस प्रकार से हमें श्री कुन्दकुन्द आचार्य के वचन प्रमाण हैं उसी प्रकार से श्री गुणधर आचार्य, श्री पुष्पदन्त भूतबलि आचार्य के वचन भी प्रमाण होने चाहिए। धवला, जयधवला आदि सिद्धान्तग्रंथों की टीका करने वाले आचार्य श्री वीरसेन स्वामी ने धवला की छठी पुस्तक में सम्यग्दर्शन का लक्षण बताते हुए कहा है—
सम्माइट्ठी जीवो उवइट्ठं पवयणं तु सद्दहदि।
सद्दहदि असब्भावं अजाणमाणो गुरुणियोगा।।१०।।
इसका अर्थ यह है कि सम्यग्दृष्टि जीव सर्वज्ञ के द्वारा उपदिष्ट प्रवचन का तो नियम से श्रद्धान करता ही है किन्तु कदाचित् अज्ञानवश सद्भूत अर्थ को स्वयं नहीं जानता हुआ गुरु के नियोग—निमित्त से असद्भूत अर्थ का भी श्रद्धान करता है अर्थात् गुरु यदि अज्ञानी है तो उसके द्वारा बताए गए गलत अर्थ का श्री श्रद्धान शिष्य करता है तो भी वह सम्यग्दृष्टि होता है। उसके आगे की गाथा में भी क्या बताते हैं ?
सुत्तादो तं सम्मं दरसिज्जंतं जदा ण सद्दहदि।
सो चेव हवइ मिच्छाइट्ठी जीवो तदो पहुदी।।
इसका अर्थ यह है कि गुरु के ऊपर श्रद्धान करके गलत अर्थ का जानने वाला जो सम्यग्दृष्टि जीव है वह पुन: सूत्रग्रंथों से सही अर्थ को दिखाने पर भी यदि श्रद्धान नहीं करता है तो उसी समय वह मिथ्यादृष्टि तो है ही। निश्चय सम्यग्दर्शन का थर्मामीटर तो केवली के सिवाय किसी के पास नहीं है। आज के युग में तो व्यवहार सम्यग्दर्शन सही सलामत बना रहे यह महान् पुण्य और सौभाग्य की बात है किन्तु अपने को सम्यग्दर्शन का खिताब देने वाले लोग हमारे गुरुओं की निन्दा करते हैं। वे भला सम्यग्दृष्टि हो सकते हैं क्या ? यह विचारणीय विषय है। गुरुनिन्दा और सम्यग्दर्शन का आपस में सर्प और नेवला जैसा सम्बन्ध है। हमारा स्याद्वाद जैनधर्म कर्मसिद्धान्त पर टिका हुआ है। प्रत्येक व्यक्ति अपने—अपने कर्मों के अनुसार फल को भोगता है अत: मुनि को अपने कर्त्तव्य पर छोड़ दीजिए, आप अपने कर्त्तव्य का पालन करिए। आचार्य श्री सोमदेव सूरि ने कहा है—
भुक्तिमात्र प्रदाने तु, का परीक्षा तपस्विनाम्।
ते सन्त: सन्त्वसन्तो वा, गृही दानेन शुद्धयति।।
तपस्वी मुनियों को तो आप श्रावक केवल आहार ही देते हैं उस आहार मात्र को प्रदान करने हेतु उनकी परीक्षा करने का आपको क्या अधिकार है ? वे साधु हों या असाधु अर्थात् सम्यग्दृष्टि हों या नहीं हों, श्रावक तो उन्हें दान देने मात्र से शुद्ध हो जाते हैं। सम्यग्दर्शन कोई साधारण वस्त्र जैसी चीज नहीं है जो बाहर से खरीदकर अपने पास रखी जा सके, वह तो आत्मा का स्वभाव है उसे प्रगट करना अपना धर्म है। यदि परनिन्दा से कलुषित आत्मा के परिणाम हैं तो उसमें सम्यग्दर्शन कैसे प्रगट हो सकता है ? यदि आचार्य कुन्दकुन्द स्वामी के समयसार की दुहाई देते हुए आप उनकी एक निश्चयपरक गाथा को स्वर्णाक्षरों में अंकित करें और एक व्यवहारपरक गाथा को मद्देनजर कर देवें तो उस सम्यग्दर्शन का क्या नाम है ? आगम में यह बात कहीं दृष्टिगत नहीं हुई है। इस विषय में भगवती आराधना में आचार्य श्री शिवकोटि की यह गाथा ध्यान देने योग्य है—
पदमक्खरं च एक्वं पि जो ण रोचेदि सुत्तणिद्दिट्ठं।
सेसं रोचंतो वि हु मिच्छाइट्ठी मुणेयव्वो।।३९।।
अत्यन्त रहस्योद्घाटित है इस गाथा का अभिप्राय कि जो जीव सूत्रनिर्दिष्ट समस्त वाङ्मय का श्रद्धान करता हुआ भी ‘यदि एक पद का श्रद्धान नहीं करता है जो वह समस्त श्रुत की रुचि करता हुआ भी मिथ्यादृष्टि है।’’ आप स्वयं सोचें कि एक पद मात्र के प्रति अश्रद्धान करने पर जब आचार्य मिथ्यादृष्टि की डिग्री दे रहे हैं तो अपनी मनमानी गाथाओं को लेकर उसकी शेष गाथाओं को नहीं मानने वाले तो केवल सम्यग्दर्शन का पोपडम रचते हैं किन्तु वास्तविक सम्यग्दर्शन तो उनसे बहुत दूर है। इसका अर्थ यह है कि हमारे लिए जितना उपादेय समयसार है उससे कहीं अधिक उपादेय रयणसार और मूलाचार भी है क्योंकि जब तक मनुष्य का आचरण शुद्ध नहीं होगा तब तक वह समयसार को पढ़ने—सुनने का अधिकारी नहीं हो सकता है। चारों ही गतियों में अपने—अपने कारणों के मिलने पर सम्यग्दर्शन उत्पन्न हो सकता है। आचार्यों ने सम्यग्दर्शन उत्पत्ति में सर्वाधिक प्रबल कारण ‘‘जिनबिम्बदर्शन’’ को बतलाया है। इस अचेतन बाह्य निमित्त से आत्मा के अन्तरंग दर्शनमोहनीय कर्मों का भी उपशम, क्षय और क्षयोपशम होकर औपशमिक, क्षायिक और क्षायोपशमिक नाम के सम्यग्दर्शन उत्पन्न हो जाते हैं किन्तु जिनेन्द्र भगवान् के दर्शन करने वाले सभी प्राणियों को सम्यग्दर्शन की उत्पत्ति हो जावे यह आवश्यक नहीं है क्योंकि यह निश्चित है कि— ‘‘कार्य की उत्पत्ति कारण से ही होती है किन्तु कारण के होने पर कार्य की उत्पत्ति हो ही जावे यह जरूरी नहीं है।’’ फिर भी जिनबिम्ब दर्शन कभी निरर्थक नहीं हो सकता है। इससे कदाचित् सम्यक्त्व उत्पन्न नहीं भी होवे तो भी अनंत—अनंत जन्म के संचित पाप कर्म समूह का नाश होकर महान् पुण्य कर्म का संचय तो हो ही जाता है। आचार्य श्री वीरसेन स्वामी ने धवला पुस्तक ६ के पृष्ठ ४२७ पर कहा है— ‘‘जिनबिम्ब के दर्शन से निधत्त और निकाचित रूप मिथ्यात्व आदि कर्मों का क्षय देखा जाता है, जिससे जिनबिम्ब का दर्शन प्रथम सम्यक्त्व की उत्पत्ति का कारण होता है। कहा भी है—
‘‘दर्शनेन जिनेन्द्राणां पापसंघातवुंजरम्।
शतधा भेदमायाति गिरिर्वङ्काहतो यथा।।’’
अर्थात् जिनेन्द्र के दर्शन से पापसंघातरूपी वुंजर के सौ टुकड़े हो जाते हैं, जिस प्रकार वङ्का के आघात से पर्वत के सौ टुकड़े हो जाते हैं। चारों ही गतियों के जीवों में सम्यग्दर्शन की उत्पत्ति होती है। जैसे नरक में नारकी जीवों के जातिस्मरण, वेदनानुभव और धर्मोपदेश इन तीन कारणों से सम्यक्त्व की प्राप्ति हो सकती है। तिर्यञ्चों में एकेन्द्रिय, दो इन्द्रिय, तीन इन्द्रिय, चार इन्द्रिय और असंज्ञी पंचेन्द्रिय इनके सम्यक्त्व उत्पन्न नहीं होता है तथा सम्मूर्च्छन तिर्यंचों के भी प्रथम उपशम सम्यक्त्व प्राप्त करने की योग्यता नहीं है अत: गर्भ से जन्म लेने वाले पर्याप्तक संज्ञी पंचेन्द्रिय तिर्यंच ही इस सम्यक्त्व को उत्पन्न करते हैं। वे बहुत से तिर्यंच दिवस पृथक्त्व के व्यतीत हो जाने पर तीन कारणों से सम्यक्त्व प्राप्त कर सकते हैं। कितने ही जाति स्मरण से, कितने ही धर्मोपदेश सुनकर और कितने ही जिनबिम्बों के दर्शन करके सम्यक्त्व को उत्पन्न करते हैं। मनुष्यगति में भी इन्हीं तीन कारणों से सम्यक्त्व उत्पन्न होता है। देवों में पर्याप्त मिथ्यादृष्टि देव अन्तर्मुहूर्त काल से लेकर ऊपर कभी भी प्रथम सम्यक्त्व प्राप्त कर सकते हैं, अन्तर्मुहूर्त से पहले नहीं। देव चार कारणों से सम्यक्त्व उत्पन्न करते हैं—कितने ही जातिस्मरण से, कितने ही धर्मोपदेश सुनकर, कितने ही जिनमहिमा देखकर और कितने ही देवों की ऋद्धि देखकर सम्यक्त्व प्राप्त करते हैं। निसर्गज सम्यक्त्व के लिए भी जातिस्मरण अथवा जिनबिम्बदर्शन निमित्त होना ही चाहिये अन्यथा यह सम्यक्त्व भी प्रगट नहीं हो सकता। हाँ ! इसमें केवल धर्मोपदेश की अपेक्षा नहीं है क्योंकि धर्मोपदेश के निमित्त से होने वाला सम्यक्त्व अधिगमज कहलाता है। ये तो बहिरंग निमित्त बताए हैं एवं अंतरंग निमित्त तो दर्शनमोहनीय कर्म का उपशम, क्षय और क्षयोपशम होना ही चाहिए। तत्त्वार्थ सूत्र के चतुर्थ सूत्र का अवतरण करते हुए सात तत्त्वों के नाम बताए गए हैं—
जीवाजीवास्रवबंधसंवरनिर्जरामोक्षास्तत्त्वम्।।४।।
अर्थ — जीव, अजीव, आस्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष ये सात तत्त्व हैं। तत्त्वार्थराजवार्तिक ग्रन्थ में आचार्य श्री अकलंक देव ने किसी शिष्य की ओर से यह प्रश्न उठाया है कि सभी तत्त्व जीव और अजीव के मिलाप से ही संभव होते हैं अत: केवल इन में ही आस्रव, बंध आदि तत्त्वों का अन्तर्भाव हो जायेगा, इनको अलग से कहने की क्या आवश्यकता थी ? इसका उत्तर स्वयं श्री अकलंकदेव देते हुए कहते हैं— जीव और अजीव का पारस्परिक संश्लेश संसार का प्रधान कारण है और इन दोनों का पृथक्—पृथक् हो जाना मोक्ष का प्रधान कारण है अत: संसार और मोक्ष के प्रधान कारणों के प्रतिपादन के लिए सात तत्त्व का विभाग किया है। जैसे—यहाँ मोक्षमार्ग का प्रकरण है और उसका फल ‘मोक्ष’ है अत: वह मोक्ष किसके होता है ? जीव के होता है इसलिए जीव का ग्रहण उचित है। मोक्ष संसारपूर्वक ही होता है और संसार अजीव के होने पर जीव के होता है इसलिए अजीव का ग्रहण किया है। संसार का प्रधान कारण आस्रव और बंध है तथा मोक्ष का प्रधान कारण संवर और निर्जरा है इसलिए सूत्र में इन सभी का ग्रहण करना परम आवश्यक है क्योंकि इन तत्त्वों के ज्ञान के बिना मोक्ष का ज्ञान भी नहीं हो सकता है। इनका विस्तृत विवरण सर्वार्थसिद्धि, राजवार्तिक आदि ग्रन्थों से अवगन्तव्य है। अब इन तत्त्वों को तथा सम्यग्दर्शन आदि के व्यवहार के कारणों को कैसे जानें, उसके लिए आचार्यश्री ने सूत्र बताया—
नामस्थापनाद्रव्यभावतस्तन्न्यास:।।५।।
अर्थ — नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव से जीवादि पदार्थों का न्यास करना चाहिये। जैसे—तद्रूप गुणों के अभाव में भी किसी व्यक्ति का नाम सम्यग्दर्शन या महावीर आदि रख देना नाम निक्षेप है। किसी वस्तु आदि का किसी में प्रतिनिधित्व करना स्थापना निक्षेप है। जैसे इन्द्राकार प्रतिमा में ‘यह इन्द्र है’ ऐसी स्थापना तदाकार कहलाती है एवं शतरंज की मोहरों में हाथी, घोड़े की कल्पना करना अतदाकार स्थापना होती है। अनागत परिणाम विशेष के प्रति अभिमुख को द्रव्य कहते हैं अर्थात् जो आगामी पर्याय की योग्यता वाला है, उसको वर्तमान में उस रूप कह देना द्रव्यनिक्षेप है। जो होता है वह भाव है अर्थात् वर्तमान की उस—उस पर्याय का ग्रहण करने वाला भाव निक्षेप है। सूत्र में ‘तत् शब्द का ग्रहण इसलिए किया है कि सम्यग्दर्शन और जीव तत्त्व के साथ—साथ अजीवादि तत्त्वों में एवं सम्यग्ज्ञान और चारित्र में भी नामादि निक्षेपों का कथन होना चाहिए। अब आगे प्रमाण, नय, सम्यग्दर्शनादि तथा तत्त्वों को जानने के उपाय का वर्णन करते हैं—
प्रमाणनयैरधिगम:।।६।।
अर्थ — प्रमाण और नयों के द्वारा जीवादि तत्त्वों का अधिगम—ज्ञान होता है। समुदाय को विषय करने वाला प्रमाण कहलाता है और अवयव को विषय करने वाला नय होता है। राजवार्तिक के अनुसार— ‘‘सकलादेश: प्रमाणाधीनो विकलादेशो नयाधीन:’’ अर्थात् प्रमाण सकलादेशी है और नय विकलादेशी। सकलादेश सम्पूर्ण पदार्थ को जानना प्रमाणाधीन है और विकलादेश एक—एक अंश को जानना नयाधीन है। अनेकान्तमयी स्याद्वाद शासन में वस्तु तत्त्व का कथन सप्तभंगी के द्वारा किया जाता है। सप्तभंगी किसे कहते हैं ?
‘‘प्रश्नवशादेकस्मिन् वस्तुन्यविरोधेन विधिप्रतिषेधकल्पना सप्तभंगी’’
प्रश्न के अनुसार एक ही वस्तु में प्रमाण से अविरुद्ध विधिप्रतिषेध (अस्ति, नास्ति आदि) धर्मों की कल्पना करना सप्तभंगी है। जैसे एक ही जीव तत्त्व को सात प्रकार से कह रहे हैं— # स्यात् जीव # स्यात् अजीव # स्यात् उभय—जीव—अजीव # स्यात् अवक्तव्य # स्यात् जीव अवक्तव्य # स्यात् अजीव अवक्तव्य # स्यात् उभय अवक्तव्य—जीव—अजीव अवक्तव्य। यहाँ ‘स्यात्’ शब्द का अर्थ ‘कथंचित्’ है अर्थात् कथञ्चित् जीव तत्त्व स्वात्मा से स्वरूप की अपेक्षा जीव है और पर की अपेक्षा वही जीव कथञ्चित् अजीव भी है क्योंकि अनादिकाल से वह जीव तत्त्व अजीव पुद्गल के साथ संसार में भ्रमण कर रहा है अत: इन सात प्रकार की कथन शैली को स्याद्बाद शब्द से सम्बोधित किया गया है, यही नयव्यवस्था भी कहलाती है। इस प्रमाण के दो भेद हैं—प्रत्यक्ष प्रमाण और परोक्ष प्रमाण। जिस ज्ञान के द्वारा किसी बाह्य निमित्त की सहायता के बिना ही आत्मा पदार्थों को स्पष्ट रूप से जाने उसे प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं और इन्द्रिय तथा प्रकाश आदि की सहायता से पदार्थों को एकदेशरूप से जाने उसे परोक्ष प्रमाण कहते हैं। जो पदार्थों के एकदेश को विलय करे वह नय है उसके द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक ऐसे दो भेद हैं। जो मुख्य रूप से द्रव्य को विषय करे उसे द्रव्यार्थिक तथा जो मुख्य रूप से पर्याय को विषय करे उसे पर्यायार्थिक नय कहते हैं। जैसे बात करने भी अपनी—अपनी शैली है। मान लीजिए कि कोई जीव सूक्ष्म रुचि वाले हैं उन्हें थोड़ी सी बात कहने पर समझ में आ जाता है और जो विस्तार वाले हैं उन्हें नय और छोटे—छोटे वाक्यों के माध्यम से समझाना पड़ता है यही नय प्रणाली कहलाती है। अब जीवादि तत्त्वों को जानने के अन्य और भी उपाय बताते हैं—
निर्देशस्वामित्त्व साधनाधिकरणस्थितिविधानत:।।७।।
अर्थ — निर्देश—सामान्य नाममात्र कथन या स्वरूप का निश्चय, स्वामित्व— अधिकारी, साधन—कारण, अधिकरण—आधार, स्थिति—कालमर्यादा, विधानत:—भेद प्रभेद से भी जीवादि तत्त्वों का ज्ञान होता है। अर्थ के स्वरूप की अवधारणा—निश्चय निर्देश कहलाता है। अधिपति—आधिपत्य को बतलाने वाला स्वामी है। सम्यग्दर्शनादि उत्पत्ति के निमित्त को साधन कहते हैं। सम्यग्दर्शनादि के आधार को अधिकरण कहते हैं। कालकृत व्यवस्था का नाम स्थिति है। सम्यग्दर्शनादि के भेद—प्रभेदों को विधान कहते हैं। यह छह अनुयोग कहलाते हैं। जो शास्त्र रूप हैं वे तो ४ अनुयोग होते हैं जिनके अन्दर द्वादशांग वाणी निबद्ध है लेकिन छह अनुयोग वे हैं जिनके द्वारा जीवादि तत्त्वों का एवं सम्यग्दर्शन आदि का अधिगम होता है। कुछ और उपाय भी बतलाते हैं—
सत्संख्याक्षेत्रस्पर्शनकालान्तरभावाल्पबहुत्त्वैश्च।।८।।
अर्थ — सत्, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अन्तर, भाव और अल्पबहुत्त्व के द्वारा भी जीवादि का अधिगम होता है। शिष्यों के आशयवश ही तत्त्वज्ञान के इन कारणों का व्याख्यान आचार्यश्री उमास्वामी ने किया है। जितने प्रश्न हैं उन सबका परिहार करने के लिए कहते हैं कि तत्त्वाधिगम के विभिन्न भेदों का कथन शिष्य की योग्यता, अभिप्राय और जिज्ञासा की शान्ति के लिए किया जाता है। कोई शिष्य अति संक्षेप में समझ लेते हैं, कोई विस्तार से और कोई मध्यम रीति से। अन्यथा ‘‘प्रमाण’’ इस संक्षिप्त पद के ग्रहण से ही समस्त आयोजन सिद्ध हो जाते, अन्य उपायों का कथन करने की आवश्यकता ही नहीं थी। देखो ! शिवभूति मुनिराज को ‘‘तुषमास भिन्नं’’ इस अल्पज्ञान से ही केवलज्ञान की प्राप्ति हो गई थी जबकि वे श्रुत के प्रति बिलकुल अल्पज्ञानी थे फिर भी आचार्य श्री कुन्दकुन्द स्वामी ने उनका नाम अपनी गाथा में उल्लेख किया है—
‘‘तुसमासं घोसतो शिवभूदी केवली जादो’’
उनके विषय में ऐसा कथन आता है कि उनकी स्मरण शक्ति बहुत कमजोर थी। गुरु के द्वारा बार—बार बतलाने पर भी शिवभूति मुनिराज को कोई भी पाठ याद नहीं होता था अत: गुरुदेव ने उन्हें समझाया कि तुम तो इतना ध्यान रखो कि ‘मा रुष मा तुष’’ अर्थात् राग मत करो, द्वेष मत करो इतने मात्र से तुम्हारा कल्याण होगा। वे मुनिराज यही वाक्य रटते—रटते एक दिन उसे भी भूल गए, तब उन्हें बड़ा दु:ख हुआ किन्तु ज्ञानावरण कर्म का तीव्र उदय, वे बेचारे कर भी क्या सकते थे, किंकर्तव्यविमूढ़ थे। वे यत्र—तत्र विहार कर रहे थे आखिर एक दिन वह शुभ दिवस भी आया जब वे एक गांव से निकल रहे थे। अकस्मात् उनकी दृष्टि एक महिला पर पड़ी जो अपने घर के बाहर बैठी हुई उड़द की दाल धो—धो कर छिलका अलग कर रही थी इस दृश्य को देखते ही उनकी अन्तरात्मा जागृत हो गई। अज्ञान का आवरण हटा और स्मृतिपटल पर गुरुदेव के शब्द प्रस्फुटित हो गए। चिन्तन चला कि मेरे गुरु ने शायद यही तो बताया था जो महिला कर रही है अर्थात् उन्होंने रटना शुरू कर दिया—‘‘तुषमाषभिन्नं’’ माष का अर्थ होता है—उड़द और तुष का अर्थ—छिलका। उन मुनिराज ने समझ लिया कि जैसे उड़द की दाल से छिलका अलग किया जाता है उसी प्रकार से मैंने अपनी चैतन्य आत्मा से शरीर को पृथक् करने के लिए जैनेश्वरी दीक्षा धारण की है। अनन्तर वही क्रिया उनके आत्मकल्याण में प्रेरणास्रोत बनी और इसी का चिन्तन करते—करते एक दिन वे शुक्लध्यान में आरूढ़ हो गये और उन्हें केवलज्ञान की प्राप्ति भी हो गई। इसीलिए कहा जाता है कि आत्मगत श्रुतज्ञान चाहे आत्मार्थी को किञ्चित् ही क्यों न हो किन्तु आत्मगत ज्ञान और चारित्र मोक्षप्राप्ति में प्रबल निमित्त है। इसी प्रकार से कभी—कभी अतिसंक्षिप्त व्याख्यान के द्वारा भी शिष्यों को जीवादि तत्वों एवं सम्यग्दर्शनादि का ज्ञान हो जाता है। अब नवमें सूत्र का अवतार करते हुए ज्ञान के नाम और भेद बताते हैं—
मतिश्रुतावधिमन:पर्ययकेवलानि ज्ञानम्।।९।।
अर्थ — मति, श्रुत, अवधि, मन:पर्यय और केवलज्ञान ये पाँच सम्यग्ज्ञान के भेद हैं। पाँचों इन्द्रियों और मन के द्वारा पदार्थों का जो ज्ञान होता है उसे मतिज्ञान कहते हैं। मतिज्ञान से जाने हुए पदार्थ से सम्बन्ध रखने वाले किसी दूसरे पदार्थ के ज्ञान को श्रुतज्ञान कहते हैं। जैसे मतिज्ञान के द्वारा किसी पुस्तक का ज्ञान हो जाने पर अपनी बुद्धि से यह जानना कि यह पुस्तक ज्ञान प्राप्त कराने में साधनभूत है अथवा उसके समान अन्य पुस्तकाकार वस्तु देखकर अन्य बहुत सी पुस्तकों का ज्ञान प्राप्त करना श्रुतज्ञान है। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की मर्यादा को लिए हुए रूपी पदार्थों को जानने वाले ज्ञान को अवधिज्ञान कहते हैं। प्राणीमात्र के मन में स्थित सरल या जटिल रूपी—मूर्तिक पदार्थों को जानने वाला मन:पर्यय ज्ञान कहलाता है। समस्त द्रव्य की समस्त पर्यायों को एक साथ स्पष्ट जानने वाले ज्ञान को केवलज्ञान कहते हैं। अब प्रमाण का लक्षण और उनके भेद बताए हैं—
तत्प्रमाणे।।१०।।
अर्थ — ऊपर कहे गए मति आदि ज्ञान ही प्रमाण हैं, अन्य कोई प्रमाण नहीं हैं। सूत्र में द्विवचन का प्रयोग इसलिए किया गया है कि उस प्रमाण के भी दो भेद हैं—प्रत्यक्ष प्रमाण और परोक्ष प्रमाण। इन पाँच ज्ञानों में कौन से ज्ञान प्रत्यक्ष और कौन से परोक्ष प्रमाण हैं इसको जानने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं—
आद्ये परोक्षम्।।११।।
अर्थ — इन पाँच ज्ञानों में आदि के दो ज्ञान—मतिज्ञान और श्रुतज्ञान परोक्ष प्रमाण हैं। ये ज्ञान इन्द्रिय, मन, उपदेश, प्रकाश आदि पर की सहायता से उत्पन्न होते हैं इसलिए परोक्ष कहलाते हैं। अभी आपके और हमारे दोनों के मति और श्रुत, यह दोनों ही ज्ञान हैं और इन दोनों ज्ञानों को परोक्ष कहा गया है। हम यह पुस्तक देख रहे हैं यह हमारा परोक्ष ज्ञान है। आप कहेंगे—कैसे ? हम तो स्पष्ट देख रहे हैं, प्रत्यक्ष देख रहे हैं तो परोक्ष कैसे हुआ ? इस बात का उत्तर आगे देंगे कि जिसमें किसी का अवलम्बन होता है वह परोक्ष कहलाता है। इस परोक्ष ज्ञान को न्याय की शैली में परीक्षामुख, न्यायदीपिका के अन्दर सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष भी कहा है। इस बात को जब शिष्य स्वीकार नहीं करता और कहता है कि—भगवन्! मैं तो सामने देख रहा हूँ कि यह चीज है और आप इसको कहते हैं परोक्ष ज्ञान है तब उन आचार्य ने कहा—परोक्ष आगम वालों की दृष्टि से परोक्ष है क्योंकि इसमें इन्द्रिय और मन की सहायता लेनी पड़ती है और चूँकि हमको व्यवहार में सब प्रत्यक्ष दिख रहा है इसलिये उसका नाम दिया है सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष। अब प्रत्यक्ष प्रमाण के भेद बताते हैं—
प्रत्यक्षमन्यत्।।१२।।
अर्थ — मति, श्रुत ज्ञान के अतिरिक्त शेष अवधि, मन:पर्यय और केवलज्ञान ये तीन प्रत्यक्ष ज्ञान होते हैं। अक्ष नाम आत्मा का है। जो ज्ञान आत्मा से ही उत्पन्न होता है, इन्द्रिय आदि पर की अपेक्षा नहीं होती उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। प्रत्यक्ष के दो भेद हैं—देश प्रत्यक्ष और सकल प्रत्यक्ष। अवधि और मन:पर्यय ये दो ज्ञान देशप्रत्यक्ष हैं अर्थात् इनकी कुछ सीमा होती है कि इतनी सीमा तक यह रूपी पदार्थों को देखेंगे परन्तु केवलज्ञान रूपी, अरूपी सभी सीमित, असीमित पदार्थों को अर्थात् लोक से सब पदार्थों को देख लेता है इसलिए सकल प्रत्यक्ष कहलाता है। मंतिज्ञान के और भी नाम हैं जिसको बताते हुए आगे सूत्र का अवतार होता है—
मति: स्मृति: संज्ञा चिन्ताऽभिनिबोधइत्यनर्थान्तरम्।।१३।।
अर्थ — मति, स्मृति, संज्ञा, चिन्ता, अभिनिबोध ये मतिज्ञान के ही नामान्तर हैं क्योंकि ये पाँचों ही मतिज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से उत्पन्न होते हैं। भावार्थ—मति, स्मृति, संज्ञा, चिन्ता और अभिनिबोध ये एक—दूसरे के पर्यायवाची ही नाम हैं। इनमें एक का कथन करें तो दूसरे का कथन समझ लेना चाहिये। मन और इन्द्रियों से वर्तमान काल के पदार्थों का जानना मति है। पहले जाने हुये पदार्थों का वर्तमान में स्मरण आना कहलाता है स्मृति। वर्तमान में किसी पदार्थ को देखकर ‘यह वही है’ इस प्रकार स्मरण और प्रत्यक्ष के जोड़रूप ज्ञान को संज्ञा कहते हैं। इसी का दूसरा नाम ‘प्रत्यभिज्ञान’ है। जहाँ—जहाँ धुआँ है वहाँ—वहाँ अग्नि अवश्य ही होती है, जैसे—रसोईघर में धुएँ को देखकर अग्नि का अनुमान लगाया जाता है इस प्रकार के व्याप्तिज्ञान को चिन्ता कहते हैं। साधन से साध्य का ज्ञान होने को अभिनिबोध कहते हैं। जैसे—‘उस पहाड़ में अग्नि है क्योंकि उस पर धुआँ है’ इसी का दूसरा नाम अनुमान है। मतिज्ञान के कारण और स्वरूप को बताते हैं—
तदिन्द्रियानिन्द्रियनिमित्तम्।।१४।।
अर्थ — वह मतिज्ञान पाँचों इन्द्रिय और अनिन्द्रिय—मन की सहायता से होता है। इन्द्र अर्थात् आत्मा। आत्मा के चिन्ह विशेष को इन्द्रिय कहते हैं। अभिप्राय यहाँ यह है कि जानने की शक्ति तो आत्मा में स्वभाव से ही है किन्तु ज्ञानावरण कर्म का उदय रहते हुये वह बिना बाह्य सहायता के स्वयं नहीं जान सकता अत: जिन अपने चिह्नों के द्वारा वह पदार्थों को जानता है उन्हें इन्द्रिय कहते हैं। यहाँ मन को अनिन्द्रिय शब्द से सम्बोधित किया गया है, जिसका अर्थ है—ईषत् इन्द्रिय अर्थात् मन पूरी तरह से इन्द्रिय नहीं है क्योंकि इन्द्रियों का तो स्थान भी निश्चित है और विषय भी निश्चित है किन्तु मन का न तो कोई निश्चित स्थान ही है और न कोई निश्चित विषय ही है। मन को अन्त:करण भी कहते हैं क्योंकि एक तो वह आँख वगैरह की तरह बाहर में दिखाई नहीं देता। दूसरी बात मन का प्रधान कार्य गुण दोष का विचार तथा स्मरण आदि है उसमें वह इन्द्रियों की सहायता नहीं लेता अत: उसे अन्त:करण भी कहते हैं। मतिज्ञान में इन्द्रिय और मन की सहायता लेनी पड़ती है, तब जाकर मतिज्ञान होता है। दोनों चीजें इसलिये कही हैं कि एकेन्द्रिय से लेकर चार इन्द्रिय तक के प्राणियों के मन नहीं होता लेकिन फिर भी उनके भी मति और श्रुत दोनों ज्ञान मौजूद हैं। जितने भी जीव हैं चाहे वह एक निगोदिया जीव ही क्यों न हों उनके भी यह दोनों ज्ञान मौजूद हैं इसलिए कि उनके आत्मा है और साथ में कम से कम एक इन्द्रिय लगी हुई है, बिना ज्ञान के ये जीव जड़ हो जाता है। मतिज्ञान के भेदों को बताया है—
अवग्रहेहावायधारणा:।।१५।।
अर्थ — अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा ये चार मतिज्ञान के भेद हैं। # अवग्रह — सत्तामात्र अवलोकन स्वरूप दर्शन के पश्चात् जो पदार्थ का प्रथम ग्रहण रूप ज्ञान होता है उसे अवग्रह कहते हैं। जैसे—चक्षु से किसी सफेद वस्तु को जानना। # ईहा — अवग्रह से जाने हुए पदार्थ में विशेष जानने की इच्छा का होना ईहा है। जैसे—यह सफेद रूप वाली वस्तु क्या है ? यह बगुलों की पंक्ति है या पताका। # अवाय — विशेष चिन्हों द्वारा यथार्थ वस्तु का निर्णय कर लेना अवाय है। जैसे—पंखों के हिलने से तथा ऊपर—नीचे होने से यह निर्णय हो गया कि यह तो बगुलों की ही पंक्ति है। # धारणा — अवाय से जानी हुई वस्तु को कालान्तर में भी नहीं भूलना धारणा है। मतिज्ञानावरण कर्म का जैसा—जैसा क्षयोपशम आत्मा में होता जाता है वैसी—वैसी धारणा शक्ति वृद्धिंगत हो जाती है। किन्हीं— किन्हीं प्राणी विशेष में यह धारणा शक्ति इतनी मजबूत हो जाती है कि अनेक भवों के पश्चात् भी उन्हें पूर्व जन्मों की बात ज्यों की त्यों स्मृति में आ जाती है। इस अवर्सिपणी काल में मनुष्यों की आयु, बुद्धि आदि सभी का ह्रास होता जा रहा है यही कारण है कि आज कई—कई बार धर्मगुरुओं की प्रेरणा मिलने पर भी मानव आत्मज्ञान से विमुख होता जा रहा है। परम पूज्य गणिनीप्रमुख आर्यिकारत्न श्री ज्ञानमती माताजी अनेकों बार प्रवचन में कहा करती हैं कि ‘‘गुरु उपदेश जीवन में कभी भी व्यर्थ नहीं जाता’’ आज भले ही आपको वह स्मरण न रहे किन्तु किसी न किसी भव में दु:ख—सुख का अनुभव करते हुए अवश्य याद आवेगा और वह सम्यग्दर्शन की उत्पत्ति में निमित्त भी बन सकता है। देखो! इसी पंचमकाल में श्री अकलंक और निकलंक जैसे एकपाठी और दो पाठी भी हुए हैं जिसमें अकलंक मात्र एक बार गुरुमुख से अध्ययन करके जीवन में कभी नहीं भूलते थे और निकलंक दो बार किसी बात को सुनने के पश्चात् पुन: नहीं भूलते थे यह उनकी धारणा शक्ति की ही विशेषता थी। इसी शताब्दी के महान विद्वान श्रीमद्राजचंद्र, जिनके नाम से आप सभी परिचित हैं वे शतावधानी थे। एक साथ सौ प्रश्नों को सुनकर क्रमश: धारावाहिक उत्तर देते थे। मैंने स्वयं पूज्य ज्ञानमती माताजी के बारे में अनुभव किया है कि उन्होंने आज से ५०—६० वर्ष पूर्व भी जिन ग्रंथों का स्वाध्याय किया था उन ग्रन्थों में कहाँ क्या वर्णन है उन्हें ज्यों का त्यों स्मरण रहता है। ज्ञान तो सभी की आत्मा में विद्यमान है किन्तु बादलों की तरह ज्यों—ज्यों उस पर से आवरण हटता जाता है त्यों—त्यों ज्ञान प्रगट होता है और एक दिन वही ज्ञान पूर्ण निरावरण होकर केवलज्ञान सूर्य को प्रगट कर देता है अत: अपने ज्ञान को समीचीन करने का सतत् प्रयास करना चाहिये। अवग्रह आदि के विषयभूत पदार्थ क्या हैं ? सो ही बताते हैं—
बहुबहुविधक्षिप्रानि:सृतानुक्तध्रुवाणां सेतराणाम्।।१६।।
अर्थ — बहु, बहुविध, क्षिप्र, अनि:सृत, अनुक्त, ध्रुव और इनके प्रतिपक्षी अल्प, अल्पविध, अक्षिप्र, अनि:सृत, उक्त और अध्रुव इन बारहों के अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा चारों ही ज्ञान होते हैं अर्थात् बारह को चार से गुणा करने पर मतिज्ञान के ४८ भेद हो जाते हैं। बहुत वस्तुओं के ग्रहण करने को बहुज्ञान कहते हैं। बहुत तरह की वस्तुओं के ग्रहण करने को बहुविधज्ञान कहते हैं। जैसे—सेना या वन को एक समूह रूप में जानना बहुज्ञान है और हाथी, घोड़े आदि या आम, महुआ आदि भेदों को जानना बहुविध ज्ञान है। वस्तु के एक भाग को देखकर पूरी वस्तु को जान लेना अनि:सृृत ज्ञान है। जैसे—जल में डूबे हुए हाथी की सूंड को देखकर हाथी को जान लेना। शीघ्रता से जाती हुई वस्तु को जानना क्षिप्र ज्ञान है। जैसे—तेज चलती हुई रेलगाड़ी को या उसमें बैठकर बाहर की वस्तुओं को जानना। बिना कहे अभिप्राय से ही जान लेना अनुक्त ज्ञान है। बहुत काल तक जैसा का तैसा निश्चल ज्ञान होना या पर्वत वगैरह स्थिर पदार्थ को जानना ध्रुव ज्ञान है। एक प्रकार की वस्तुओं का ज्ञान होना एकविध ज्ञान है। धीरे—धीरे चलते हुए घोड़े आदि को जानना अक्षिप्र ज्ञान है। सामने विद्यमान पूरी वस्तु को जानना नि:सृत ज्ञान है। कहने पर जानना उक्त ज्ञान है। चंचल बिजली वगैरह को जानना अध्रुव ज्ञान है। इस प्रकार से बारह प्रकार का अवग्रह, बारह प्रकार की ईहा, बारह प्रकार का अवाय और बारह प्रकार का धारणा ज्ञान होता है तथा इनमें से प्रत्येक ज्ञान पांच इन्द्रिय और मन के द्वारा होता है अत: ४८ को ६ से गुणा करने पर मतिज्ञान के २८८ भेद होते हैं।
अर्थस्य।।१७।।
अर्थ — यह बहुविध आदि अर्थ—पदार्थ के विशेषण हैं अर्थात् बहुत से पदार्थ और बहुत तरह के पदार्थ इस तरह बारहों भेद पदार्थ के विशेषण हैं। आगे बतलाते हैं कि सभी पदार्थों से अवग्रह आदिक चारों ज्ञान होते हैं या उसमें कुछ अन्तर होता है—
व्यञ्जनस्यावग्रह:।।१८।।
अर्थ — व्यंजन अर्थात् अस्पष्ट शब्द आदि का केवल अवग्रह ही होता है ईहा आदि नहीं होती। व्यञ्जन यानी अस्पष्ट, जैसे—कुछ स्वर होते हैं और कुछ व्यंजन होते हैं क, प, त ये जितने भी व्यंजन हैं उनमें जब तक स्वर नहीं लगता तब तक वह बिल्कुल अस्पष्ट होते हैं क्योंकि खाली व्यंजन का उच्चारण नहीं हो पाता। जैसे खाली व्यंजन का उच्चारण नहीं हो पाता, ऐसे ही अस्पष्ट पदार्थ वगैरह का अर्थात् व्यंजनावग्रह का केवल अवग्रह हो जाता है, ज्ञान हो जाता है ईहा आदिक ज्ञान उनके नहीं होते। अवग्रह के दो भेद होते हैं—अर्थावग्रह और व्यञ्जनावग्रह। स्पष्ट पदार्थ के अवग्रह को अर्थावग्रह कहते हैं और अस्पष्ट पदार्थ के अवग्रह को व्यंजनावग्रह कहते हैं। जैसे—कान में एक हल्की सी आवाज सुनाई पड़ी उसके बाद फिर कुछ भी नहीं जान पड़ा कि क्या था ? ऐसी अवस्था में केवल व्यंजनावग्रह ही होकर रह जाता है किन्तु यदि धीरे—धीरे वह आवाज स्पष्ट हो जाती है तो व्यंजनावग्रह के बाद अर्थावग्रह और फिर ईहा आदि ज्ञान भी होते हैं अत: अस्पष्ट पदार्थ का केवल अवग्रह ज्ञान ही होता है और स्पष्ट पदार्थ के चारों ज्ञान होते हैं। अब आचार्य श्री उमास्वामी कहते हैं कि—
न चक्षुरनिन्द्रियाभ्याम्।।१९।।
अर्थ — नेत्र और मन से व्यञ्जनावग्रह नहीं होता है। चक्षु और मन से व्यंजनावग्रह नहीं होता क्योंकि चक्षु और मन पदार्थ को दूर से ही जानते हैं उसको छूकर नहीं। जैसे चक्षु अपने आँख में लगे हुए अंजन को नहीं देख सकता किन्तु दूर के पदार्थों को देख सकता है इसी तरह मन भी जिन पदार्थों का विचार करता है वे उससे दूर ही होते हैं। इसी से जैन सिद्धान्त में चक्षु और मन को अप्राप्यकारी माना है। शेष चारों इन्द्रियाँ अपने विषय को उससे छूकर ही जानती हैं अत: व्यंजनावग्रह चार ही इन्द्रियों से होता है। इस प्रकार से बहु आदि बारह विषयों की अपेक्षा व्यंजनावग्रह के ४८ भेद होते हैं तथा पहले गिनाये हुये २८८ भेदों में इन ४८ भेदों को मिला देने से मतिज्ञान के ३३६ भेद हो जाते हैं। यथाक्रम से जिसमें जिस ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम होता है उसके वह ज्ञान प्रगट हो जाया करता है। इस प्रकार से यहाँ पर मतिज्ञान का स्वरूप और उसके भेद कहे हैं। अब आगे श्रुतज्ञान का लक्षण और उसके भेद कहते हैं—
श्रुतं मतिपूर्वं द्वयनेकद्वादशभेदं।।२०।।
अर्थ — श्रुतज्ञान मतिज्ञानपूर्वक होता है। उसके दो भेद हैं—अंगप्रविष्ट और अंगबाह्य। उनमें से अंगप्रविष्ट के बारह भेद हैं और अंगबाह्य के अनेक भेद हैं। किसी भी जीव के सबसे पहले मतिज्ञान होता है उसके बाद श्रुतज्ञान होता है। बिना मतिज्ञान हुए श्रुतज्ञान कभी नहीं होता। उस श्रुतज्ञान के जो अंगप्रविष्ट नाम का भेद है उसके बारह भेद हैं—आचारांग, सूत्रकृतांग, स्थानांग, समवायांग, व्याख्याप्रज्ञप्तिअंग, ज्ञातृधर्मकथांग, उपासकाध्ययनांग, अंतकृद्दशांग, अनुत्तरोप—पादिकदशांग, प्रश्नव्याकरणांग, विपाकसूत्रांग और दृष्टिवाद अंग। तीर्थंकर भगवान जब चार घातिया कर्मों का नाश करके केवलज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तब लोकालोक के समस्त पदार्थों को जानकर अपनी दिव्यध्वनि द्वारा सारे संसारी प्राणियों को उपदेश देते हैं। उनके उपदेश को गणधर देव अपनी स्मृति में रखकर बारह अंगों में संकलित कर देते हैं। यही ज्ञान अंग प्रविष्ट श्रुतज्ञान कहा जाता है। यह अंगग्रंथ अत्यन्त महान् और गंभीर अर्थ को लिए हुए होते हैं। वर्तमान में द्वादशांग में से कोई भी अंग के पूर्ण ग्रन्थ उपलब्ध नहीं हैं, उनके अंश अवश्य आज शास्त्रों में निबद्ध हैं। आचार्यों ने अल्पबुद्धि शिष्यों पर दया करके उनके आधार पर जो ग्रन्थ रचे हैं वे अंगबाह्य कहलाते हैं। यह सब अक्षरात्मक श्रुतज्ञान के भेद हैं। आज से लगभग २००० वर्ष पूर्व आचार्य श्री धरसेन स्वामी ने श्रुतज्ञान का ह्रास होते देखा तब उन्हें विशेष चिन्ता हुई कि श्रुत की अविच्छिन्न परम्परा कैसे चलेगी ? अत: उन्होंने पुष्पदन्त और भूतबलि नाम के दो दिगम्बर मुनि शिष्यों को अपना श्रुतज्ञान वितरित किया जिसके फलस्वरूप आज तक धवल जयधवल, महाधवल आदिक सूत्रग्रन्थ देखे जाते हैं तथा हमारी जिनवाणी जो कि चार अनुयोगों में निबद्ध है उसके भी बहुमात्रा में ग्रन्थ उपलब्ध हैं। आचार्य श्री कुन्दकुन्द स्वामी ने भी जैन वाङ्मय का बहुत विस्तार किया है। मति और श्रुतज्ञान परोक्ष प्रमाण हैं और प्रत्यक्ष प्रमाण के तीन भेद हैं—अवधिज्ञान, मन:पर्ययज्ञान और केवलज्ञान। अवधिज्ञान का वर्णन करते हुए कहते हैं—
भवप्रत्ययोऽवधिर्देवनारकाणाम्।।२१।।
अर्थ — भवप्रत्यय अवधिज्ञान देव और नारकियों के होता है। अवधिज्ञान अवधिज्ञानावरण और वीर्यान्तराय कर्म के क्षयोपशम से होता है और क्षयोपशम व्रत, नियम आदि के आचरण से होता है किन्तु देवों और नारकियों में व्रत, नियम आदि नहीं होते अत: उनमें देव और नारकी का भव पाना ही क्षयोपशम के होने में कारण होता है। इसी से उनमें होने वाला अवधिज्ञान भवप्रत्यय—जिसके होने में भव ही कारण है, कहा जाता है अर्थात् जो देव और नारकियों में जन्म लेता है उसके अवधि ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम हो ही जाता है अत: वहां क्षयोपशम के होने में भव ही मुख्य कारण है। इतना विशेष है कि मिथ्यादृष्टियों के कुअवधि ज्ञान होता है। देव और नारकियों का अवधिज्ञान भवप्रत्यय है क्योंकि यह भव अर्थात् पर्याय के कारण उत्पन्न हुआ है और जो किसी पर्याय विशेष की अपेक्षा न रखकर अवधिज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से होवे उसको कहते हैं गुणप्रत्यय अवधिज्ञान या क्षयोपशमनिमित्तक अवधिज्ञान। स्मरण रखने योग्य बात यहाँ यह बतायी गयी है कि भवप्रत्यय अवधिज्ञान में भी अवधिज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम होता है पर वह क्षयोपशम देव और नरक पर्याय में नियम से प्रकट हो जाता है। तीर्थंकरों के भी भवप्रत्यय अवधिज्ञान होता है। अब क्षयोपशमनिमित्तक अवधिज्ञान के भेद एवं स्वामी के बार में बताते हैं—
क्षयोपशमनिमित्त: षड्विकल्प: शेषाणाम्।।२२।।
अर्थ — क्षयोपशम के निमित्त से होने वाला अवधिज्ञान छ: प्रकार का होता है और वह मनुष्य तथा तिर्यञ्चों के होता है। अवधि ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम जिसमें निमित्त है उसे क्षयोपशमनिमित्तक अवधिज्ञान कहते हैं। यद्यपि सभी अवधिज्ञान क्षयोपशम के निमित्त से होते हैं फिर भी इस अवधिज्ञान का नाम क्षयोपशमनिमित्तक इसलिए रखा गया कि इसके होने में क्षयोपशम ही प्रधान कारण है, भव नहीं। इसी से इसे गुण प्रत्यय भी कहते हैं; इसके छ: भेद हैं—अनुगामी, अननुगामी, वर्धमान, हीयमान, अवस्थित, अनवस्थित। जो अवधिज्ञान अपने स्वामी—जीव के साथ—साथ जाता है उसे अनुगामी कहते हैं। इसके तीन भेद हैं—क्षेत्रानुगामी, भवानुगामी और उभयानुगामी। जिस जीव के जिस क्षेत्र में अवधिज्ञान प्रकट हुआ वह जीव यदि दूसरे क्षेत्र में जाय तो उसके साथ जाय और छूटे नहीं, उसे क्षेत्रानुगामी कहते हैं। जो अवधिज्ञान परलोक में भी अपने स्वामी जीव के साथ जाता है वह भवानुगामी है। जो अवधिज्ञान अन्य क्षेत्र में भी साथ जाता है और अन्य भव में भी साथ जाता है वह उभयानुगामी है। जो अवधिज्ञान अपने स्वामी जीव के साथ नहीं जाता है वह अननुगामी है। इसके भी तीन भेद हैं जो पूर्वोक्त तीन भेदों से उल्टे हैं। विशुद्ध परिणामों की वृद्धि होने से जो अवधिज्ञान बढ़ता ही जाता है उसे वर्धमान कहते हैं। संक्लेश परिणामों की वृद्धि होने से जो अवधिज्ञान घटता ही जाता है उसे हीयमान कहते हैं। जो अवधिज्ञान जिस मर्यादा को लेकर उत्पन्न हुआ हो उसी मर्यादा में रहे, न घटे और न बढ़े, उसे अवस्थित कहते हैं और जो घटे—बढ़े उसे अनवस्थित कहते हैं। दूसरी प्रकार से अवधिज्ञान के देशावधि, परमावधि और सर्वावधि ऐसी तीन भेद भी बताये हैं। इनमें देशावधि चारों गतियों में हो सकता है परन्तु परमावधि और सर्वावधि अवधिज्ञान चरमशरीरी मुनियों को ही होता है। मन:पर्ययज्ञान के भेदों को बताते हैं—
ऋजुविपुलमती मन:पर्यय:।।२३।।
अर्थ — मन:पर्ययज्ञान ऋजुमति और विपुलमति के भेद से दो प्रकार का होता है। मन:पर्यय का मतलब क्या है ? दूसरे के मन में स्थित सूक्ष्म से सूक्ष्म तत्त्वों को जानने वाला मन:पर्ययज्ञानी कहलाता है और यह नियम है कि यह मन:पर्यय ज्ञान किसी श्रावक को नहीं हो सकता, मुनि को ही होगा। अवधिज्ञान के लिए बताया है कि अवधिज्ञान तो श्रावक को हो सकता है लेकिन मन:पर्ययज्ञान तपस्वी ऋद्धिधारी मुनियों को ही होगा। उस मन:पर्यय ज्ञान के दो भेद हैं—१. ऋजुमति और २. विपुलमति।
दूसरे के मन में सरल रूप में स्थित रूपी पदार्थ को जो ज्ञान प्रत्यक्ष जानता है उसे ऋजुमति मन:पर्यय कहते हैं और दूसरे के मन में सरल अथवा जटिल रूप में स्थित रूपी पदार्थ को जो ज्ञान प्रत्यक्ष जानता है, उसे विपुलमति मन:पर्यय कहते हैं। देव, मनुष्य, तिर्यंच सभी के मन में स्थित विचार को मन:पर्यय ज्ञान जानता है किन्तु वह विचार रूपी पदार्थ अथवा संसारी जीव के विषय में होना चाहिए। अमूर्त्तिक द्रव्यों और मुक्तात्माओं के विषय में जो चिन्तन किया गया होगा, उसे मन:पर्यय नहीं जान सकता तथा उन्हीं जीवों के मन की बात जान सकता है जो मनुष्य लोक की सीमा के अन्दर हों। इतना विशेष है कि मनुष्यलोक तो गोलाकार है किन्तु मन:पर्यय ज्ञान का क्षेत्र गोलाकार न होकर पैंतालिस लाख योजन लम्बा चौड़ा चौकोर है। उसके दो भेदों में से ऋजुमति तो केवल उसी वस्तु को जान सकता है जिसके बारे में सरल रूप से विचार किया गया हो अथवा मन, वचन और काय की चेष्टा के द्वारा जिसे स्पष्ट कर दिया गया हो किन्तु विपुलमति मन:पर्यय चिन्तित और
चिन्तित को भी जान लेता है।।२३।।
अर्थ —अब मन:पर्यय के दोनों भेदों में विशेषता बतलाते हैं—
विशुद्ध्यप्रतिपाताभ्यां तद्विशेष:।।२४।।
अर्थ — परिणामों की विशुद्धता और अप्रतिपात—केवलज्ञान होने से पहले नहीं छूटना, इन दो बातों से ऋजुमति और विपुलमति ज्ञान में विशेषता है। ऋजुमति और विपुलमति में विशुद्धि और अप्रतिघात की अपेक्षा से विशेषता है। मन:पर्यय ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से जो आत्मा में उज्ज्वलता होती है वह विशुद्धि है और संयम परिणाम की वृद्धि होने से गिरावट का न होना अप्रतिपात है। ऋजुमति से विपुलमति अधिक विशुद्ध होता है तथा ऋजुमति होकर छूट भी जाता है किन्तु विपुलमति वाले का चारित्र वर्धमान ही होता है अत: वह केवलज्ञान उत्पन्न होने तक बराबर बना रहता है।।२४।। आगे अवधिज्ञान और मन:पर्यय ज्ञान में विशेषता बतलाते हैं—
विशुद्धिक्षेत्रस्वामिविषयेभ्योऽवधिमन:पर्ययो:।।२५।।
अर्थ — अवधिज्ञान और मन:पर्यय ज्ञान में विशुद्धि, क्षेत्र, स्वामी और विषय की अपेक्षा से अन्तर है। अवधिज्ञान जिस रूपी द्रव्य को जानता है उसके अनन्तवें भाग सूक्ष्म रूपी द्रव्य को मन:पर्यय ज्ञान वाला जानता है अत: अवधिज्ञान से मन:पर्यय ज्ञान विशुद्ध है। अवधिज्ञान की उत्पत्ति का क्षेत्र समस्त त्रसनाली है किन्तु मन:पर्यय ज्ञान मनुष्य लोक में ही उत्पन्न होता है। अवधिज्ञान के विषय का क्षेत्र समस्त लोक है किन्तु मन:पर्यय ज्ञान के विषय का क्षेत्र पैंतालिस लाख योजन में स्थित मनुष्य या देव के मन में स्थित विषय को जानने का है। इतने क्षेत्र में स्थित अपने योग्य विषय को ही ये ज्ञान जानते हैं तथा अवधिज्ञान चारों गतियों के सैनी पंचेन्द्रिय पर्याप्तक जीवों के होता है किन्तु मन:पर्यय ज्ञान कर्मभूमि के गर्भज मनुष्यों के ही होता है उनमें भी संयमियों के ही होता है, संयमियों में भी वर्धमान चारित्र वालों के ही होता है, हीयमान चारित्र वालों के नहीं होता। वर्धमान चारित्र वालों में भी सात प्रकार की ऋद्धियों में से एक—दो ऋद्धियों के धारी मुनियों के ही होता है और ऋद्धिधारियों में भी किसी के ही होता है, सभी के नहीं होता। इस तरह अवधि और मन:पर्यय ज्ञान में विशुद्धि आदि की अपेक्षा भेद जानना चाहिए। अब ज्ञानों का विषय बतलाते हुए प्रथम मतिज्ञान और श्रुतज्ञान का विषय बताते हैं—
मतिश्रुतयोर्नबन्धो द्रव्येष्वसर्वपर्यायेषु।।२६।।
अर्थ — मतिज्ञान और श्रुतज्ञान के विषय का नियम द्रव्यों की कुछ पर्यायों में है। अर्थात् ये दोनों ज्ञान द्रव्यों की कुछ पर्यायों को जानते हैं, सब पर्यायों को नहीं जानते। इस सूत्र में ‘‘विषय’’ शब्द नहीं है अत: ‘‘विशुद्धि क्षेत्र’’ आदि सूत्र से विषय शब्द ले लेना चाहिए तथा ‘‘द्रव्येषु’’ शब्द बहुवचन का रूप है इसलिए जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल सभी द्रव्यों का ग्रहण करना चाहिए। इन द्रव्यों में से एक—एक द्रव्य की अनन्त पर्यायें होती हैं। उनमें से कुछ पर्यायों को ही मति, श्रुत ज्ञान जानते हैं। अब यह शंका हुई कि धर्म, अधर्म आदि द्रव्य तो अमूर्तिक हैं। वे मतिज्ञान के विषय नहीं हो सकते अत: सब द्रव्यों को मतिज्ञान जानता है ऐसा कहना ठीक नहीं है? उसका समाधान करते हुए बताते हैं कि यह आपत्ति ठीक नहीं है, क्योंकि मन की सहायता से होने वाला मतिज्ञान अमूर्तिक द्रव्यों में भी प्रवृत्ति कर सकता है और मनपूर्वक अवग्रह आदि ज्ञान होने पर पीछे श्रुतज्ञान भी अपने योग्य पर्यायों को जान लेता है अत: कोई दोष नहीं है।।२६।। यह दोनों ज्ञान रूपी, अरूपी सभी द्रव्यों को जानते हैं पर उनकी सभी पर्यायों को नहीं जान पाते, कुछ पर्यायों को ही जानते हैं। यहाँ तक कि अपनी पीठ में क्या—क्या है, अपनी पीठ पीछे की वस्तु को हम नहीं जान सकते हैं। अपने शरीर के अवयवों की गणना हम नहीं कर सकते हैं। हमारा ज्ञान इतना स्थूल है कि वह कुछ ही पर्यायों को ग्रहण कर सकता है सारी पर्यायों को नहीं ग्रहण कर सकता। सारी पर्यायों को ग्रहण करने वाला तो केवलज्ञानी ही होता है। अवधिज्ञान का विषय बताते हैं—
रूपिष्ववधे:।।२७।।
अर्थ — अवधिज्ञान रूपी पदार्थों को जानता है अर्थात् रूप, रस, गन्ध, स्पर्श वाले पुद्गल ही अवधिज्ञान के विषय होते हैं वह क्षायिक भाव तथा धर्म, अधर्म आदि अरूपी द्रव्यों को नहीं जानता। अवधिज्ञान रूपी पदार्थों को ही जानता है। रूपी का मतलब क्या होता है? जिसका रूप है, जिसके अन्दर स्पर्श, रस, गंध, वर्ण पाया जाता है। चाहे रूपी कह लीजिये चाहे र्मूितक कह लीजिये, आत्मा केवल अरूपी है और हमारा शरीर पुद्गल रूपी है। छ: द्रव्य हैं—जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश व काल। इनमें से कितने द्रव्य र्मूितक हैं और कितने अर्मूितक हैं ? इनमें एक पुद्गल द्रव्य र्मूितक है बाकी के सभी द्रव्य अर्मूितक हैं। आकाश की कोई र्मूित नहीं दिखती। आप सोचते हैं कि यह नीला—नीला आकाश दिख रहा है, यह आकाश नहीं हैं हर जगह आकाश है, हमारे चारों ओर आकाश है और वह आकाश अर्मूितक है। यह तो पुद्गल के परमाणु हैं जिनको हमने आकाश मान लिया है। यह बादल हैं, आकाश नहीं हैं। शेष पाँच द्रव्य हैं—धर्म, द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य और जीव द्रव्य यह सब अर्मूितक हैं। जिसमें पूरण और गलन स्वभाव होता है वही कहलाता है र्मूितक और र्मूितक या रूपी पदार्थों को जानने वाला ही अवधिज्ञान है। मन:पर्ययज्ञान का विषय बताया है—
तदनन्तभागे मन:पर्ययस्य।।२८।।
अर्थ — सर्वावधिज्ञान के विषयभूत रूपी द्रव्य के सूक्ष्म अनन्तवें भाग में मन:पर्यय ज्ञान की प्रवृत्ति होती है। सारांश यह है कि अवधिज्ञान से मन:पर्ययज्ञान अत्यन्त सूक्ष्म पदार्थ को जानने की शक्ति रखता है। मन:पर्यय ज्ञान उन रूपी पदार्थों में भी उसके अनन्तवें पदार्थ को भी जान सकता है लेकिन इतनी सब विशेषता होते हुए भी अरूपी पदार्थ को नहीं जान पाता। विज्ञान ने इतनी प्रगति कर ली लेकिन जब इस प्राणी के शरीर से निकलकर आत्मा जाने लगती है तो कोई वैज्ञानिक, कोई मशीनरी उसको पकड़ नहीं पाई, इतनी उपलब्धियाँ हो गयीं लेकिन अर्मूितक आत्मा को कोई भी आज तक देख नहीं पाया, जान नहीं पाया। अगर पकड़ पाये हैं, जान पाये हैं, अनुभव कर पाये हैं तो केवलज्ञानी और ध्यानी आत्मा ही उसका अनुभव कर पाये हैं जिसके बल पर उन्होंने सिद्धशिला को प्राप्त किया है। वह केवल एक केवलज्ञान ही है, केवलदर्शन ही है जिसने उस अरूपी आत्मा को देखा है, जाना है और अनुभव किया है। उस केवलज्ञान का विषय क्या है? यह जिज्ञासा होने पर आचार्य कहते हैं—
सर्वद्रव्यपर्यायेषु केवलस्य।।२९।।
अर्थ —केवलज्ञान सभी द्रव्यों की समस्त पर्यायों को विषय करता है अर्थात् लोक और अलोक में त्रिकालविषयक जितने अनंतानंत द्रव्य और पर्याय हैं उन सभी में केवलज्ञान की प्रवृत्ति होती है। जितना यह लोक है उतने यदि अनंत भी लोक हों तो उन्हें भी केवलज्ञान जान सकता है। समस्त द्रव्य की समस्त पर्यायों को केवलज्ञान विषय करता है। उससे कोई भी चीज अछूती नहीं रह सकती। चाहे आप कमरे में छिपकर कोई काम कर रहे हों, चाहे आप अंधरी रात में कोई काम कर ले, केवलज्ञानी सब कुछ जानता है, उसकी फिल्म बराबर चल रही है, वह फिल्म कभी रुकती नहीं हैं। केवलज्ञान ऐसा है कि वह बराबर देखता ही रहता है, इसलिये उसकी विशेषता बताई है कि वह सभी द्रव्य की त्रिकालवर्ती समस्त पर्यायों को जानने में सक्षम होता है। इतना सुनते—सुनते जब शिष्य थक गया तो उसने कहा कि महाराज! मेरे हित की बात बताइए। मुझे तो आप यह बताइए कि एक प्राणी एक साथ कितने ज्ञानों को धारण कर सकता है ? आपके मन में भी जिज्ञासा होगी कि क्या मुझे भी केवलज्ञान मिल सकता है ? उस शिष्य ने भी पूछा—महाराज! इतना विस्तारपूर्वक तो आपने बता ही दिया। अब मुझे बताइए कि मैं कितने ज्ञान प्राप्त कर सकता हूँ ? तब आचार्यश्री बताते हैं कि एक जीव के एक साथ कितने ज्ञान हो सकते हैं—
एकादीनि भाज्यानि युगपदेकस्मिन्नाचतुभ्र्य:।।३०।।
अर्थ —एक साथ एक आत्मा में एक को आदि लेकर चार ज्ञान तक हो सकते हैं। एक आत्मा में दो ज्ञान—मति और श्रुत, तीन ज्ञान—मति, श्रुत, अवधि या मति, श्रुत, मन:पर्यय, चार ज्ञान—मति, श्रुत, अवधि, मन:पर्यय ज्ञान होंगे। पाँच ज्ञान कभी एक साथ नहीं होंगे। केवलज्ञान एक अकेला ही होता है। केवलज्ञान क्षायिक और परम विशुद्ध है अत: सकलज्ञानावरण कर्म के विनाश होने पर ही प्रगट होता है। अब आपको पुरुषार्थ करना है कि आपको दो ज्ञान प्राप्त करना है, एक ज्ञान प्राप्त करना है या चार ज्ञान प्राप्त करने हैं। यह निर्णय मैं आपके ऊपर ही छोड़ देती हूँ। और अब आगे का सूत्र आता है—
मतिश्रुतावधयो विपर्ययश्च।।३१।।
अर्थ —मति, श्रुत, अवधि ये तीनों ज्ञान मिथ्या भी होते हैं और सम्यव्â भी। मिथ्यादृष्टि जीव के मिथ्यादर्शन के साथ रहने के कारण इन ज्ञानों में मिथ्यात्व आ जाता है। जैसे—कड़वी तूमड़ी में रखा हुआ दूध कड़वा हो जाता है उसी तरह मिथ्यादृष्टि रूप आधारदोष से ज्ञान में मिथ्यात्व आ जाता है। यहाँ पर यह शंका करना उचित नहीं है कि जैसे—मणि, सुवर्ण आदि मलस्थान में गिरकर भी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते वैसे ही ज्ञान को भी नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि पारिणामिक अर्थात् परिणमन कराने वाले की शक्ति के अनुसार वस्तुओं में परिणमन होता है। कड़वी तूमड़ी के समान मिथ्यादर्शन में ज्ञान रूपी दूध को बिगाड़ने की शक्ति है। यद्यपि मलस्थान से मणि आदि में बिगाड़ नहीं होता पर अन्य धातु आदि के सम्बन्ध से सुवर्ण आदि भी विपरिणत हो ही सकते हैं। सम्यग्दर्शन के होते ही मति आदि ज्ञानों का मिथ्याज्ञानत्व हटकर उनमें सम्यग्ज्ञानत्व आ जाता है और मिथ्यादर्शन के उदय से ये ही मति आदि ज्ञान कुमति, कुश्रुत, कुअवधि रूप बन जाते हैं। आज विज्ञान ने कितनी-कितनी उन्नति कर ली लेकिन आज के युग के अन्दर भी जब हमारी भारतीय संस्कृति को अमेरिकन देखते हैं तो इस बात का अनुभव करते हैं कि वास्तव में हमने यन्त्रों की उपलब्धि कर ली, हमने विज्ञान के सहारे न जाने कितने यन्त्र बना लिये, सब कुछ खोज कर ली लेकिन आत्मा की खोज, अध्यात्म की खोज करने में आज भी हम असफल हैं। बैलगाड़ी के युग से यह मानव मिसाइल के युग में, कम्प्यूटर के युग में तो आ गया लेकिन आत्मा की खोज नहीं कर पाया, अध्यात्म की खोज नहीं कर पाया इसलिये वह खोखला का खोखला रह गया। शायद इसीलिये एक कवि ने ऐसे ही
सभा में बैठे हुए अनेक श्रोताओं से कहा—चेहरे पर चेहरे हैं, बड़े-बड़े गहरे हैं। पर त्याग के नाम पर, आप गूंगे और बहरे हैं।।यही कारण है कि हम अध्यात्म की खोज नहीं कर पाते। हम बाह्य चकाचौंध में पड़कर न जाने कितनी-कितनी खोज करने में लगे हुए हैं लेकिन हमें गूंगे और बहरे नहीं बनना है। अगर आप गूंगे और बहरे होते तो न तो मेरी बात का जवाब दे सकते थे और न आप उसको पढ़ ही सकते थे, न मानव पर्याय की सार्थकता को समझ सकते थे। मैं समझती हूँ कि आप लोग बहुत चतुर हैं और आपमें जो अनादिकालीन गूँगा और बहरापन है उसको समाप्त करने का आपने बीड़ा उठाया है यही कारण है कि आप आज यहाँ इस महान ग्रंथराज की वाचना सुनने और गुनने के लिये आये हैं। मोक्षशास्त्र जैसे महान ग्रन्थ को सबका शिरमौर्य कहा जाए कि जो कुछ भी निकला है वह इस तत्त्वार्थ सूत्र से निकला है तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। तत्त्वार्थ सूत्र चारों अनुयोगों का प्रतिपादन करने वाला द्वादशांग जिनवाणी का प्रतीक है। आपसे कोई पूछे कि आपके जैनधर्म का मूलग्रन्थ कौन-सा है ? तो आपको बताना चाहिये कि तत्त्वार्थ सूत्र हमारा मूलग्रन्थ है। आपके जैनधर्म का मूलमन्त्र कौन-सा है ? आपको बताना चाहिये कि णमोकार महामन्त्र हमारे जैनधर्म का मूलमन्त्र है। इस सूत्र में बताया है कि यह तीनों ज्ञान संसर्ग की अपेक्षा से, मिथ्यात्व कर्म की अपेक्षा से मिथ्या भी हो सकते हैं, सम्यक्त्व की अपेक्षा से सम्यक् भी हो सकते हैं। अगर आपको सम्यग्दर्शन है तो आप निश्चित मानिये कि आपको मति और श्रुतज्ञान हैं, आज हमारे पास थर्मामीटर नहीं है कि हम आपको बिल्कुल निश्चित रूप से बता सवेंâ कि आप सम्यग्दृष्टि हैं कि मिथ्यादृष्टि हैं। देव, शास्त्र, गुरु के प्रति श्रद्धान है तो नियम से व्यवहार सम्यग्दृष्टि हैं। निश्चय सम्यग्दर्शन की बात तो जाने दीजिये, हमें प्रयास करना है कि अगर हमारे जीवन के अन्दर कभी अवधिज्ञान भी उपज जाये तो वह कुअवधिज्ञान न बनने पावे क्योंकि पंचमकाल के अन्दर अवधिज्ञान का निषेध नहीं किया है।
पंचमकाल के अन्त में भी वीरांगज मुनिराज को अवधिज्ञान होगा और वह जान जाएंगे कि अब धर्म के ह्रास का समय है। मैं एक शास्त्र का उदाहरण आपको बताती हूँ कि किस प्रकार से अवधिज्ञान के अन्दर भी विपरीतता आती है। शास्त्र की पौराणिक कथा है— एक राजा था, उसको एक बार दाह ज्वर हो गया। बहुत दवाइयाँ कीं, बहुत चन्दन लगाया, बहुत सारी शीतल दवाइयाँ भी लीं लेकिन उसका दाह ज्वर शान्त नहीं हुआ, बड़ा परेशान था वह राजा। एक दिन वह कमरे में लेटा हुआ था। दरवाजे से छिपकली की पूंछ कटकर एक बूँद खून उसके शरीर पर पड़ गया। जहाँ हाथ पर आ करके खून की बूँद पड़ी, वहीं पर थोड़ी शांति उसे महसूस हुई। तब राजा को तुरन्त कुअवधि उत्पन्न हो गयी। उसने सोचा कि इस खून की बूँद के गिरने से ही इस जगह का मेरा दाह ज्वर शान्त हुआ है इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैं खून की बावड़ी में स्नान कर लूँ तो मेरा दाह ज्वर शान्त हो सकता है। उसने एकदम सोचा—इतने पशु कहाँ पर मिलेंगे ? उनको वैâसे मारा जायेगा ? वैâसे खून की बावड़ी तैयार की जायेगी ? कुअवधिज्ञान का बटन ऑन हो गया और उसको अपने शहर के बाहर का जंगल दिखने लगा। उस जंगल के अन्दर असंख्यातों हिरण थे, गाय थीं, तमाम सारे पशु थे वह दिखने लग गये। वह सोचने लगा कि अगर इतने सारे पशुओं को मारकर इनकी खून की बावड़ी तैयार कर दी जाए, मैं उसके अन्दर डुबकी लगा लूँ तो निश्चित ही मेरा ज्वर शान्त हो जायेगा।
अपने बेटे को बुलाकर वह राजा कहता है कि बेटा! तू मेरा आज्ञाकारी पुत्र है, तू मेरे दीर्घजीवन की कामना करता है, तूने न जाने कितने वैद्यों-हकीमों से मेरी दवा करा ली लेकिन मेरा दाह ज्वर शान्त नहीं हुआ। आज मुझे अनुभूति हुई है कि अगर खून की बावड़ी तैयार कर दी जाए तो मेरा यह दाह ज्वर उसमें डुबकी लगाने से शान्त हो सकता है और तू ही मेरी इच्छा की पूर्ति कर सकता है। बेटा! मेरे शहर के पास में जो जंगल है, जा देख! वहाँ बहुत सारे पशु हैं, उनमें से सारे पशुओं में केवल हिरण को ही ला करके, तू उनको मारकर खून की बावड़ी तैयार कर लेगा तो मेरे दाह ज्वर की उपशांति हो जाएगी। बेटा! मुझे विश्वास है कि तू जरूर मेरी आज्ञा को निभाएगा। बेटा एकदम किंकर्तव्यविमूढ़! मैं क्या करूँ ? पिताजी को क्या हुआ है ? लेकिन बोला कुछ नहीं। जंगल में गया, देखा, वास्तव में यहाँ तो बहुत पशु हैं। जाते-जाते जंगल के एक छोर से दूसरे छोर को नाप आया। तभी उसने वहीं जंगल के बीच में एक शिलातल पर एक दिगम्बर मुनिराज को देखा, वे ध्यान लगाकर बैठे हैं। महाराज के पास गया। नमस्कार करके महाराज से पूछता है कि महाराजश्री! मेरे पिताजी को क्या हो गया है ? मेरे पिताजी ने इस जंगल को देखा है और यह कहा है कि सारे पशुओं को मारकर खून की बावड़ी तैयार कर दो। मुनिवर! मैं क्या करूँ? मुझे कुछ उपाय बताइये कि कत्र्तव्य का निर्वाह भी हो जाए, आज्ञा का पालन भी हो जाए, हिंसा का दोष भी नहीं लगे और पिताजी भी ठीक हो जावें। महाराज ने कहा—बेटा! तेरे पिता को कुअवधिज्ञान उत्पन्न हो गया है। इसकी पहचान क्या है गुरुवर ? उनको यहाँ जो कुछ है, सब दिख रहा है। क्या उन्हें दिव्यज्ञान हो गया है ? पुत्र के ऐसा पूछने पर महाराज बोले कि—बेटा! उनको तो मिथ्याज्ञान हो गया है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो जाकर तुम अपने पिता से पूछना कि उस जंगल के अन्दर दिगम्बर मुनिराज भी आपको दिखते हैं क्या ? उस बेटे ने जाकर पिता से पूछा कि—पिताजी! उस जंगल के अन्दर एक सन्त बैठे हुए ध्यान कर रहे हैं, वह भी आपके ज्ञान में दिखते होंगे ? पिता बोले—कोई मुनि नहीं हैं, कोई सन्त नहीं हैं, मुझे तो वहाँ पर सारे पशु दिख रहे हैं। मेरी एक ही आज्ञा है कि उन सबको लाकर मौत के घाट उतारकर उनकी खून की एक बावड़ी तैयार करो। उसने मन्त्रियों से परामर्श किया कि मैं क्या करूँ ? इतना बड़ा धर्म संकट है।
तब एक मन्त्री ने सलाह दी—युवराज! आप ऐसा करें कि पिताजी की आज्ञा का पालन भी हो जाए और हिंसा भी न हो, आप लाख को पिघलाकर जो बावड़ी तैयार करेंगे वह बिल्कुल खून जैसी दिखने लग जाएगी। बहुत अच्छी युक्ति समझ में आ गयी उसको और उस बेटे ने लाख की बावड़ी तैयार की। जब लाख ठण्डा हो गया तब जाकर पिताजी से कहा—पिताजी! बावड़ी तैयार है, आप उसमें डुबकी लगाइए। पिताजी ने उसे कोटि-कोटि आशीर्वाद दिया—बेटा! मुझे तुझसे यही आशा थी। आखिर कौन बेटा होगा जो अपने पिता के दीर्घ जीवन को नहीं चाहता होगा और डुबकी लगाते-लगाते जाने कितने आशीर्वाद अपने बेटे के लिए देता रहा कि मैं तो तुझे ही सारा राज्य वैभव देने वाला हूँ, तुझे ही राजमुकुट देने वाला हूँ, तुझे ही अपार सम्पत्ति देने वाला हूँ, तुझे ही राजा बनाने वाला हूँ और इतना कहते-कहते एकदम बावड़ी के बीच में आ गया। उसकी एकदम इच्छा हुई और उसने आनन्दविभोर होकर मँह में जैसे ही खून का कुल्ला भरा कि कितना सुन्दर खून तैयार किया है बेटे ने, लेकिन मुँह के अन्दर जाते ही वह सारा का सारा प्रेम क्रोध में परिवर्तित हो गया। जो शब्द कोटि-कोटि आशीर्वाद दे रहे थे वे ही शब्द उसे दुराशीष दे रहे थे। तूने मेरे साथ विश्वासघात किया है, तू तो होते ही मर जाता तो अच्छा था। कितना कपूत है, वैâसा है, तूने किस प्रकार से मेरी आज्ञा का पालन किया है? मेरे साथ में इतना बड़ा धोखा किया है। तूने लाख की बावड़ी तैयार की है और एकदम से अपनी कमर से तलवार खींच कर चल पड़ा अपने बेटे को मारने के लिए, लेकिन चूँकि लाख के खून से सराबोर था, अकस्मात् जैसे ही बावड़ी से निकलता है, पैर फिसलता है और उसकी तलवार छूट कर उसको ही लग जाती है और वह मरकर नरक चला जाता है।
मुनिराज ने बता दिया था—बेटा! तेरे पिता के मिथ्यात्व कर्म का उदय आया है, नरक आयु का बन्ध हो गया है यही कारण है कि जंगल में केवल पशु ही पशु दिख रहे हैं। कुअवधिज्ञान का प्रभाव है कि यहाँ बैठे हुए जैन सन्त, उनका यह धर्मध्यान, कुछ भी दिखता नहीं है। यह कुअवधिज्ञान की महिमा है कि जैसे खराब पात्र होता है तो उसमें रखा हुआ दूध भी खराब हो जाता है, ऐसे ही अगर हमारे अन्दर हमारा मनरूपी पात्र खराब है, उसके अन्दर मिथ्यात्व का कचरा लगा है तो हमारा ज्ञान मिथ्याज्ञान हो जाएगा। अवधि कुअवधि हो जाएगी, दर्शन कुदर्शन बन जाएगा इसलिये यह समझना है कि मति, श्रुत और अवधिज्ञान ये मिथ्या और सम्यक् दोनों होते हैं। आपने इन्हीं शास्त्रों में महासती मैनासुन्दरी की कथा पढ़ी होगी कि किस प्रकार उसने कर्मसिद्धान्त को प्रबल मानकर अपने सम्यग्दर्शन में दृढ़ रहते हुए उन्होंने अपने कुष्टी पति राजा श्रीपाल और उनके ५०० कुष्टी साथियों का कुष्ट रोग सिद्धचक्र के पाठ के माहात्म्य से दूर कर दिया, यह सब तो शास्त्रों में लिखित सत्य कथानक और जिनधर्म के चमत्कार हैं परन्तु आज भी अगर आपका सम्यग्दर्शन दृढ़ है तो प्रत्यक्ष चमत्कार देखने में आता है, एक ऐसा ही सम्यग्दर्शन की दृढ़ता का चमत्कार परम पूज्य गणिनीप्रमुख श्री ज्ञानमती माताजी के जीवन में घटित हुआ जब बचपन से ही ग्रन्थों के स्वाध्याय के कारण सम्यग्दर्शन में दृढ़ उन ७—८ वर्ष की वय वाली कु. मैना के दो छोटे भाइयों प्रकाश और सुभाष को भयंकर चेचक हो गई, उस समय लोग शीतला माता का प्रकोप मानकर नाना प्रकार के मिथ्यात्व करते थे तब उस छोटी सी कन्या ने भगवान शीतलनाथ की दृढ़ भक्ति कर सभी को आश्चर्यचकित कर दिया और उस गांव से ही नहीं अपितु पूरे अवध प्रांत से मिथ्यात्व को हटाकर जिनधर्म का माहात्म्य पैâला दिया। उस समय की उनके जीवन की वह घटना सुनकर पूरा शरीर रोमांचित हो उठता है कि किस प्रकार उन्होंने सारे गांव का संघर्ष झेलकर भी जिनधर्म पर दृढ़ श्रद्धा रखी, भगवान शीतलनाथ के अभिषेक का गंधोदक लाकर प्रतिदिन उन बच्चों को लगाया और उस भक्ति की शक्ति का चमत्कार हुआ, उनके दोनों भाई स्वस्थ हो गए और मिथ्यात्व को पूजने वालों के बच्चे कालकवलित हो गए। अतएव इन कथानकों के माध्यम से हमें अपने सम्यग्दर्शन को दृढ़ से दृढ़तर बनाना है, हमें यह पुरुषार्थ करना है कि हमारा ज्ञान सम्यक्ज्ञान ही बना रहे, हमारा दर्शन सम्यक्दर्शन ही बना रहे, हमारा चारित्र सम्यक्चारित्र ही बना रहे ताकि हम मोक्षमहल की सीढ़ी चढ़ने में सक्षम हो सवें। सम्यग्दर्शन के बारे में आचार्यों ने कहा है कि—मोक्षमार्ग की परथम सीढ़ी या बिन ज्ञान चरित्ता। आगे का सूत्र बताता है कि ज्ञान मिथ्या क्यों हो जाते हैं—
सदसतोरविशेषाद्यदृच्छोपलब्धेरुन्मत्तवत्।।३२।।
अर्थ — अपनी इच्छानुसार जैसा-तैसा जानने के कारण सत् और असत् पदार्थों में विशेष ज्ञान न होने से पागल पुरुष के ज्ञान की तरह मिथ्यादृष्टि का ज्ञान मिथ्याज्ञान ही होता है। जैसे हम यह देखते हैं कि यह पुस्तक है, यह सिद्धक्षेत्र है, यह मन्दिर है, यह पार्श्वनाथ भगवान हैं ऐसा का ऐसा ही मिथ्यादृष्टि भी देखता है लेकिन चूँकि अन्दर में उसके मिथ्यात्व कर्म का उदय है इसलिये उसका ज्ञान मिथ्याज्ञान कहलाता है। जैसे यूँ समझिये कि कोई पागल पुरुष है वह पागल अवस्था में अपनी स्त्री को माता कहने लगता है, माता को स्त्री कहने लगता है लेकिन जब उसका दिमाग सही होता है तो माता को माता, स्त्री को स्त्री, बहन को बहन कितना भी कहता है लेकिन इतना कहने मात्र से ही उसकी पागल संज्ञा खत्म हो जाती है क्या ? नहीं, ना। है तो पागल ही। उसको जो पागलपन की दवाई दी जा रही है वह तो दी ही जाती है, ऐसा ही पागलपन बताया है कि जब इस जीव ने मोह और मिथ्यात्व रूपी मदिरा को पी रखा है, तो यह पागल व्यक्ति सही से सही भी कहेगा तो भी वह पागल के समान मिथ्यादृष्टि ही कहलायेगा। यही बात इसके अन्दर बतलाई है कि चूँकि वस्तुस्वरूप का सच्चा ज्ञान उसको नहीं हो पाता है इसलिये ऊपर से कोई भी भेद न होते हुए भी चूँकि अन्दर से भेद है इसलिये मिथ्याज्ञान और सम्यक्ज्ञान में यह अन्तर होता है। अब इस अध्याय का अन्तिम सूत्र अवतरित करते हुए आचार्यश्री कहते हैं—
नैगमसंग्रह व्यवहारर्जुसूत्रशब्दसमभिरूढैवम्भूता नया:।।३३।।
अर्थ — नयो के सात भेद हैं—नैगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजुसूत्र, शब्द, समभिरूढ़ और एवंभूत नय। प्रमाण के द्वारा प्रकाशित अनेक धर्मात्मक पदार्थ के धर्म विशेष को ग्रहण करने वाला ज्ञान नय है। उसके मूल में द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक ये दो भेद हैं तथा नैगम आदि सात भेद भी हैं।
१. अर्थ के संकल्प मात्र को ग्रहण करने वाला नैगमनय है। जैसे—प्रस्थ बनाने के निमित्त जंगल से लकड़ी लेने के लिए जाने वाले फरसाधारी किसी पुरुष से पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं ? तो वह उत्तर देता है कि प्रस्थ के लिए जा रहा हूँ। इस उदाहरण में नैगमनय के अनुसार भविष्य में बनने वाले प्रस्थ का संकल्प निहित है अत: उसे व्यवहार से कह दिया गया है।
२. अपने अविरोधी सामान्य के द्वारा उन—उन पदार्थों का संग्रह करने वाला संग्रह नय है। जैसे—सत् कहने से सत्ता सम्बन्ध के योग्य द्रव्य गुण कर्म आदि सभी शक्तियों का ग्रहण हो जाता है।
३. संग्रह नय के द्वारा संग्रहीत पदार्थों में विधिपूर्वक विभाजन करना व्यवहार नय है। जैसे—सर्व संग्रहनय ने ‘सत्’ ऐसा सामान्य ग्रहण किया था पर इससे तो व्यवहार नहीं चल सकता था अत: भेद किया जाता है कि जो सत् है वह द्रव्य है या गुण ? द्रव्य भी जीव है या अजीव ? जीव और अजीव सामान्य से भी व्यवहार नहीं चलता था अत: उसके भी देव, नारक, मनुष्य आदि और घट—पट आदि भेद लोकव्यवहार के लिए किये जाते हैं।
४. जिस प्रकार सरल सूत डाला जाता है उसी तरह ऋजुसूत्र नय एक समयवर्ती वर्तमान पर्याय को विषय करता है। अतीत और अनागत चूँकि विनष्ट और अनुत्पन्न हैं अत: उनसे व्यवहार नहीं हो सकता। इस ऋजुसूत्र नय का विषय एक क्षणवर्ती वर्तमान पर्याय है।
५. जिस व्यक्ति ने संकेत ग्रहण किया है उसे अर्थबोध कराने वाला शब्दनय होता है।
६. अनेक ग्रंथों को छोड़कर किसी एक अर्थ में मुख्यता से रूढ़ होने का समभिरूढ़ नय कहते हैं। जैसे किसी ने पूछा कि ‘आप कहाँ हैं ? तो समभिरूढ़ नय उत्तर देगा—अपने स्वरूप में।’ क्योंकि अन्य पदार्थ की अन्यत्र वृत्ति नहीं हो सकती अन्यथा ज्ञानादि और रूपादि की भी आकाश में वृत्ति होनी चाहिए।
७. जिस समय जो पर्याय या क्रिया हो उस समय तद्वाची शब्द के प्रयोग को ही एवंभूतनय स्वीकार करता है।
जैसे—गौ जिस समय चलती है उसी समय गौ है, न तो बैठने की अवस्था में और न सोने की अवस्था में। पूर्व और उत्तर अवस्थाओं में वह पर्याय नहीं रहती अत: उस शब्द का प्रयोग ठीक नहीं है। ये नय उत्तरोत्तर सूक्ष्मविषयक तथा पूर्वहेतुक हैं अत: इनका कथन क्रम के अनुसार किया है। गौण मुख्य विवक्षा से परस्पर सापेक्ष होकर ये नय सम्यग्दर्शन के कारण होते हैं और पुरुषार्थ क्रिया में समर्थ होते हैं। इस प्रकार तत्त्वार्थ सूत्र की प्रथम अध्याय के अन्दर आचार्य श्री उमास्वामी ने रत्नत्रय का सुन्दर वर्णन करते हुए प्रमाण और नयों का वर्णन किया है। उसी का समापन करते हुए मुझे एकमात्र यही बात कहना हैज्ञान के लिये, सच्चा ग्रन्थ चाहिये।
सिद्धि के लिये, सच्चा पंथ चाहिये।।
भटके हैं संसार में, अनादि से हम।
अब तिरने के लिए, सच्चा सन्त चाहिये।।वही ग्रन्थ, वही पंथ, वही संत आपको प्राप्त हुए हैं, उन सन्तों की वाणी को सुनकर दस धर्मों को अपने जीवन में उतारें तथा इनकी अमृतवाणी सदैव आपको प्राप्त होती रहे जिसके द्वारा आप सब अपने इस अमूल्य मानव जीवन को सार्थक कर सवें यही मंगल भावना है।।
इति तत्त्वार्थाधिगमे मोक्षशास्त्रे प्रथमोऽध्याय: समाप्त:।।

 प्रवचन कर्त्री -आर्यिका चंदनामती माताजी
प्रवचन कर्त्री -आर्यिका चंदनामती माताजी

