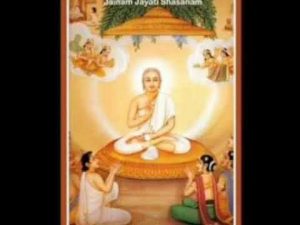श्रीगौतमस्वामी प्रणीत प्रतिक्रमण पाठ में परिवर्तन
विचारणीय विषय
णमो अरिहंताणं, णमो सिद्धाणं, णमो आइरियाणं।
णमो उवज्झायाणं, णमो लोए सव्वसाहूणं।।
गणधरवलय मंत्र
णमो जिणाणं । णमो ओहिजिणाणं।।
णमो परमोहिजिणाणं। णमो सव्वोहिजिणाणं।।
णमो अणंतोहिजिणाणं। णमो कोट्ठबुद्धीणं।।
णमो बीजबुद्धीणं। णमो पादाणुसारीणं।।
णमो संभिण्णसोदाराणं। णमो सयंबुद्धाणं।।
णमो पत्तेयबुद्धाणं। णमो बोहियबुद्धाणं।
णमो उजुमदीणं। णमो विउलमदीणं।।
णमो दसपुव्वीणं। णमो चउदसपुव्वीणं।।
णमो अट्ठंग- महा- णिमित्त-कुसलाणं।।
णमो विउव्व- इड्ढि- पत्ताणं।।
णमो विज्जाहराणं। णमो चारणाणं।।
णमो पण्णसमणाणं। णमो आगास-गामीणं।।
णमो आसीविसाणं। णमो दिट्ठिविसाणं।।
णमो उग्गतवाणं। णमो दित्ततवाणं।।
णमो तत्ततवाणं। णमो महातवाणं।
णमो घोरतवाणं, णमो घोरगुणाणं।।
णमो घोर परक्कमाणं। णमो घोरगुण-बंभयारीणं।।
णमो आमोसहि-पत्ताणं। णमो खेल्लोसहि-पत्ताणं।।
णमो जल्लोसहि—पत्ताणं। णमो विप्पोसहिपत्ताणं।।
णमो सव्वोसहिपत्ताणं। णमो मणबलीणं।।
णमो वचिबलीणं । णमो कायबलीणं।।
णमो खीरसवीणं। णमो सप्पिसवीणं।।
णमो महुरसवीणं। णमो अमियसवीणं।।
णमो अक्खीण-महाणसाणं। णमो वड्ढमाणाणं।।
णमो सिद्धायदणाणं। णमो भयवदो
महदि-महावीर-वड्ढमाण-बुद्धरिसीणो चेदि।
जस्संतियं धम्मपहं णियच्छे, तस्संतियं वेणयियं पउंजे।
काएण वाचा मणसा वि णिच्चं, सक्कारए तं सिरपंचमेण।।
गणधरवलय मंत्र का पद्यानुवाद
शंभु छंद
मैं नमूँ जिनों को जो अर्हन्, अवधीजिन मुनि को नमूँ नमूँ।
परमावधि जिन को नमूँ तथा, सर्वावधि जिन को नमूँ नमूँ।।
मैं नमूँ अनंतावधि जिन को, अरु कोष्ठबुद्धियुत साधु नमूँ।
मैं नमूँ बीजबुद्धीयुत मुनि, पादानुसारियुत साधु नमूँ।।१।।
संभिन्नश्रोतृयुत साधु नमूँ, मैं स्वयंबुद्ध मुनिराज नमूँ।
प्रत्येकबुद्ध ऋषिराज नमूँ, पुनि बोधितबुद्ध मुनीश नमूँ।।
ऋजुमति मनपर्यय साधु नमूँ, मैं विपुलमतीयुत साधु नमूँ।
मैं नमूँ अभिन्न सुदशपूर्वी, चौदशपूर्वी मुनिराज नमूँ।।२।।
अष्टांगमहाणिमित्तकुशली, नमूँ नमूँ विक्रियाऋद्धि प्राप्त।
विद्याधरऋषि को नमूँ नमूँ, मैं संयत चारणऋद्धि प्राप्त।।
मैं प्रज्ञाश्रमण मुनीश नमूूँ, आकाशगामि मुनिराज नमूँ।
आशीविषयुत ऋषिराज नमूँ, दृष्टीविषयुत मुनिराज नमूँ।।३।।
मैं उग्रतपस्वी नमूँ दीप्ततप, नमूँ तप्ततपसाधु नमूँ।
मैं नमूँ महातपधारी को, अरु घोरतपोयुत साधु नमूँ।।
मैं नमूँ घोरगुणयुत साधू, मैं घोरपराक्रम साधु नमूँ।
मैं नमूँ घोरगुणब्रह्मचारि, आमौषधि प्राप्त मुनीश नमूँ।।४।।
क्ष्वेलौषधि प्राप्त मुनीश नमूँ, जल्लौषधि प्राप्त मुनीश नमूँ।
विप्रुष औषधियुत साधु नमूँ, सर्वौषधि प्राप्त मुनीश नमूँ।।
मैं नमूँ मनोबलि मुनिवर को, मैं वचनबली ऋद्धीश नमूँ।
मैं कायबली मुनिनाथ नमूँ, मैं क्षीरस्रावि मुनिराज नमूँ।।५।।
मैं घृतस्रावी मुनिराज नमूँ, मैं मधुस्रावी मुनिराज नमूँ।
मैं अमृतस्रावी साधु नमूँ, अक्षीणमहानस साधु नमूँ।।
मैं वर्धमान ऋद्धीश नमूँ, मैं सिद्धायतन समस्त नमूँ।
मैं भगवन् महति महावीर, श्री वर्धमान बुद्धर्षि नमूँ।।६।।
शेर छंद
जिसके निकट में धर्मपथ को प्राप्त किया हूँ।
उनके निकट ही विनयवृत्ति धार रहा हूँ।।
नित काय से, वचन से और मन से उन्हीं को।
पंचांग नमस्कार करूँ भक्ति भाव सों।।
मंगलाचरण
य: सर्वाणि चराचराणि विधिवद्-द्रव्याणि तेषां गुणान्।
पर्यायानपि भूतभाविभवत:, सर्वान् सदा सर्वदा।।
जानीते युगपत् प्रतिक्षणमत:, सर्वज्ञ इत्युच्यते।
सर्वज्ञाय जिनेश्वराय महते, वीराय तस्मै नम:।।१।।
पद्यानुवाद
जो विधिवत् सब लोक चराचर, द्रव्यों को उनके गुण को।
भूत भविष्यत् वर्तमान, पर्यायों को भी नित सबको।।
युगपत समय-समय प्रति जाने, अतः हुए सर्वज्ञ प्रथित।
उन सर्वज्ञ जिनेश्वर महति, वीरप्रभू को नमूँ सतत।।१।।
धर्मतीर्थ की उत्पत्ति
‘‘वर्धमान भगवान ने तीर्थ की उत्त्पत्ति की है।१’’ अठारह भाषा और सात सौ क्षुद्र भाषा स्वरूप द्वादशांगात्मक उन अनेक बीज पदों के प्ररूपक अर्थकर्ता हैं’’ तथा बीजपदों में लीन अर्थ के प्ररूपक बारह अंगों के कर्ता गणधर भट्टारक ग्रंथकर्ता हैं।।२’’
संपहि वड्ढमाणतित्थगंधकत्तारो वुच्चदे—
दिव्यध्वनि का वर्णन तिलोयपण्णत्ति ग्रंथ में आया है।
जोयणपमाणसंट्ठिद—तिरियामरमणुवणिवहपडिबोधो।
मिदमधुरगभीरतरा — विसदविसयसयलभासाहिं।।६०।।
अट्ठरस महाभासा खुल्लयभासा वि सत्तसयसंखा।
अक्खरअणक्खरप्पय सण्णीजीवाण सयलभासाओ।।६१।।
एदािंस भासाणं तालुवंदतोट्ठकंठवावारं।
परिहरिय एक्ककालं भव्वजणाणंदकरभासो।।६२।।३
एक योजन प्रमाण तक स्थित तिर्यंच देव और मनुष्यों के समूह को बोध प्रदान करने वाली भगवान की दिव्यध्वनि होती है। यह दिव्यध्वनि मृदु—मधुर, अतिगंभीर और विशद—स्पष्ट विषयों को कहने वाली संपूर्ण भाषामय होती है। यह संज्ञी जीवों की अक्षर और अनक्षररूप अठारह भाषा और सात सौ लघु भाषाओं में परिणत होती हुई, तालु—ओंठ—दाँत तथा कंठ के हलन—चलनरूप व्यापार से रहित होकर एक ही समय में भव्य जीवों को आनंदित करने वाली होती है ऐसी दिव्यध्वनि के स्वामी तीर्थंकर भगवान होते हैं।।६०-६१-६२।।
अब वर्धमान जिनके तीर्थ में ग्रंथकर्ता को कहते हैं—
‘‘उक्त पाँच अस्तिकायादिक क्या हैं ?’’ ऐसे सौधर्मेन्द्र के प्रश्न से सन्देह को प्राप्त हुए, पाँच सौ, पाँच सौ शिष्यों से सहित तीन भ्राताओं से वेष्टित, मानस्तंभ के देखने से गर्व रहित हुए, बुद्धि को प्राप्त होने वाली विशुद्धि से संयुक्त वर्धमान भगवान के दर्शन करने पर असंख्यात भवों में अर्जित महान् कर्मों को नष्ट करने वाले, जिनेन्द्रदेव की तीन प्रदक्षिणा करके पाँच अंगों द्वारा भूमिस्पर्शपूर्वक वंदना करके एवं हृदय से जिनभगवान का ध्यान कर संयम को प्राप्त हुए, विशुद्धि के बल से मुहूर्त के भीतर उत्पन्न हुए समस्त गणधर के लक्षणों से संयुक्त तथा जिनमुख से निकले हुए बीजपदों के ज्ञान से सहित ऐसे गौतमगोत्र वाले इन्द्रभूति ब्राह्मण द्वारा चूँकि आचारांग आदि बारह अंगों तथा सामायिक, चतुा वशतिस्तव, वंदना, प्रतिक्रमण, वैनयिक, कृतिकर्म, दशवैकालिक, उत्तराध्ययन, कल्पव्यवहार, कल्पाकल्प, महाकल्प, पुण्डरीक, महापुण्डरीक व निषिद्धिका,
इन अंगबाह्य चौदह प्रकीर्णकों की श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में युग की आदि में प्रतिपदा के पूर्व दिन में रचना की थी अतएव इन्द्रभूति गणधर देव भट्टारक श्री वर्धमान स्वामी के तीर्थ में ग्रंथकर्ता हुए। कहा भी है—
वासस्स पढममासे पढमे पक्खम्मि सावणे बहुले।
पडिवदुपुव्वदिवसे तित्थुप्पत्ती दु अभिजिम्मि।।४०।।
‘‘वर्ष के प्रथम मास व प्रथम पक्ष में श्रावण कृष्णा प्रतिपदा के पूर्व दिन में अभिजित् नक्षत्र में तीर्थ की उत्पत्ति हुई१।
षट्खंडागम ग्रंथ में श्रीवीरसेनस्वामी कहते हैं—
‘‘तेण महावीरेण केवलणाणिणा कहिदत्थो तम्हि चेव काले तत्थेव खेत्ते खयोवसम—जणिदचउ—रमलबुद्धिसंपण्णेण ब्रह्मणेण गोदमगोत्तेण सयलदुस्सुदि—पारएण जीवाजीवविसयसंदेह—विणासणट्ठमुवगयवड्ढमाण-पादमूलेण इंदिभूदिणावहारिदो२।।२।।
इस प्रकार केवलज्ञानी भगवान महावीर के द्वारा कहे गये पदार्थ को उसी काल में और उसी क्षेत्र में क्षयोपशम विशेष से उत्पन्न चार प्रकार के—मति, श्रुत, अवधि, मन:पर्ययरूप निर्मल ज्ञान से युक्त संपूर्ण अन्य मतावलंबी वेद-वेदांग में पारंगत, गौतमगोत्रीय ऐसे इन्द्रभूति ब्राह्मण ने जीव-अजीवविषयक संदेह को दूर करने के लिए श्रीवर्द्धमान भगवान के चरणकमल का आश्रय लेकर ग्रहण किया अर्थात् प्रभु की दिव्यध्वनि को सुना।
इसीलिए भगवान महावीर ‘अर्थकर्ता’ कहलाये हैं।
‘पुणो तेणिंदभूदिणा भावसुदपज्जय—परिणदेण बारहंगाणं चोद्दसपुव्वाणं च गंथाणमेक्केण चेव मुहुत्तेण रयणा कदा।।३
पुन: उन इन्द्रभूति गौतमस्वामी ने भावश्रुत पर्याय से परिणत होकर बारह अंग और चौदह पूर्वरूप ग्रंथों की रचना एक ही मुहूर्त में कर दी।
सारांश यह है कि आज से पच्चीस सौ सत्तर (२५७०)४ वर्ष पूर्व श्रावण कृष्णा प्रतिपदा को राजगृही के विपुलाचल पर्वत पर भगवान महावीर की दिव्यध्वनि खिरी थी यही प्रथम देशना दिवस—‘वीरशासन जयंती’ के नाम से प्रसिद्ध है। उसी दिन श्री गौतमस्वामी ने गणधर पद प्राप्त करके द्वादशांग श्रुत की रचना की थी जो कि मौखिक मानी गई है उसे लिपिबद्ध नहीं किया जा सकता है।
दिगम्बर जैन ग्रंथों के अनुसार आज कोई भी द्वादशांग या अंगबाह्य के ग्रंथ नहीं हैं क्योंकि इनको लिपिबद्ध नहीं किया जा सकता था। परम्परागत आचार्यों ने जो कुछ मौखिक श्रुतज्ञान गुरुवों से प्राप्त किया, कालांतर में श्रीधरसेनाचार्य के शिष्य पुष्पदंत—भूतबलि नाम के दो आचार्यों ने षट्खंडागम ग्रंथ को लिपिबद्ध करके रचना की है। ऐसा इन्द्रनंदि आचार्य आदि ने श्रुतावतार आदि ग्रंथों में लिखा है।
इसी प्रकार श्रीगौतमस्वामी के मुखकमल से विनिर्गत ये महान रचनायें आज वर्तमान में भी उपलब्ध हैं। चैत्यभक्ति, प्रतिक्रमणदण्डकसूत्रादि। ये ग्रंथ मौखिक रूप से आचार्यों को प्राप्त होते रहे हैं पुन: किन्हीं महान आचार्यों ने इन्हें लिपिबद्ध करके हमें और आप सभी भव्यात्माओं के लिये सुरक्षित रखा है।
पाक्षिक प्रतिक्रमण में ‘‘णमो जिणाणं’’ आदि गणधरवलयमंत्र हैं एवं दैवसिक—पाक्षिक प्रतिक्रमण में ‘‘य: सर्वाणि चराचराणि’’ वीरभक्ति पाठ है। इन ‘णमो जिणाणं’ आदि गणधरवलय मंत्रों को श्रीभूतबलि आचार्यदेव ने षट्खंडागम के अंतर्गत तृतीय ‘वेदनाखंड’ के रचते समय मंगलाचरण रूप में लिया है। जिनकी विस्तृत टीका (पुस्तक नवमी में) टीकाकार श्री वीरसेनाचार्यदेव ने की है।
एवं श्री प्रभाचंद्राचार्य ने भी चैत्यभक्ति व प्रतिक्रमण दण्डकसूत्रों की संस्कृत टीका की है।
महामंत्र णमोकार मंत्र
णमो अरिहंताणं, णमो सिद्धाणं, णमो आइरियाणं।
णमो उवज्झायाणं, णमो लोए सव्व साहूणं।।१।।
इस महामंत्र को णमोकार मंत्र, अपराजित मंत्र, अनादि मंत्र व सार्वभौम मंत्र भी कहते हैं।
आज के उपलब्ध सम्पूर्ण जैन वाङ्मय में दो ही मंत्र अनादिनिधन मान्य हैं-
१. णमोकार महामंत्र,
२. चत्तारि मंगल पाठ।
श्रीमान् उमास्वामी आचार्य ने कहा है—
ये केचनापि सुषमाद्यरका अनन्ता, उत्सर्पिणी-प्रभृतय: प्रययुर्विवर्त्ता:।
तेष्वप्ययं परतरं प्रथितं पुरापि, लब्ध्वैनमेव हि गता: शिवमत्र लोका:।।३।।
श्लोकार्थ—उत्सर्पिणी, अवसर्पिणी आदि के जो सुषमा, दु:षमा आदि अनन्त युग पहले व्यतीत हो चुके हैं, उनमें भी यह णमोकार मंत्र सबसे अधिक महत्त्वशाली प्रसिद्ध हुआ है। मैं संसार से बहिर्भूत (बाहर) मोक्ष प्राप्त करने के लिए उस णमोकार मंत्र को नमस्कार करता हूँ।
‘णमोकार मंत्रकल्प’ में श्री सकलकीर्ति भट्टारक ने भी कहा है—
महापंचगुरोर्नाम, नमस्कारसुसम्भवम्।
महामंत्रं जगज्जेष्ठ-मनादिसिद्धमादिदम्।।६३।।
महापंचगुरूणां, पंचत्रिंशदक्षरप्रमम्।
उच्छ्वासैस्त्रिभिरेकाग्र-चेतसा भवहानये।।६८।।
श्लोकार्थ-नमस्कार मंत्र में रहने वाले पाँच महागुरुओं के नाम से निष्पन्न यह महामंत्र जगत में ज्येष्ठ—सबसे बड़ा और महान है, अनादिसिद्ध है और आदि अर्थात् प्रथम है।।६३।।
पाँच महागुरुओं के पैंतीस अक्षर प्रमाण मंत्र को तीन श्वासोच्छ्वासों में संसार भ्रमण के नाश हेतु एकाग्रचित्त होकर सभी भव्यजनों को जपना चाहिए अथवा ध्यान करना चाहिए।।६८।।
श्री गौतमस्वामी ने पाक्षिक प्रतिक्रमण में कुछ पंक्तियाँ ऐसी रखी हैं,जिनसे भी स्पष्ट है कि यह महामंत्र व चत्तारिमंगल पाठ अनादिकालीन है। यथा—
‘‘काऊण णमोक्कारं, अरहंताणं तहेव सिद्धाणं।
आइरिय-उवज्झायाणं, लोयम्मि य सव्वसाहूणं।।’’
‘‘णमोक्कारपदे अरहंतपदे सिद्धपदे आयरियपदे उवज्झायपदे साहुपदे मंगलपदे लोगोत्तमपदे सरणपदे।।’’ (पाक्षिक प्रतिक्रमण)
पद्यानुवाद
अरिहंतों को कर नमस्कार सिद्धों को नमस्कार करके।
आचार्य उपाध्याय को व लोक में सर्वसाधु को भी नमते।।
नमस्कार पद अर्हत् पद अरु सिद्धपदाचार्य पद में।
उपाध्याय साधूपद मंगल-लोकोत्तम शरणं पद में।।
‘णमोक्कारपदे’ आदि दण्डक सूत्रों में णमोकार पद में अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधुपद ये पांच पद हैं तथा मंगलपद, लोकोत्तमपद व शरणपद से चत्तारि मंगल पाठ आ जाता है क्योंकि चत्तारि मंगल पाठ में—चत्तारि मंगलं, चत्तारि लोगुत्तमा और चत्तारिसरणं पद ही मुख्य है।
षट्खण्डागम धवला टीका पुस्तक ९ में कालशुद्धि में साधुओं के लिए श्वासोच्छ्वासपूर्वक महामंत्र जपने का विधान है। इससे भी स्पष्ट होता है कि इस महामंत्र को श्वासोच्छ्वासपूर्वक जपने की विधि अनादि है।
महामंत्र को १०८ बार जपने से ३०० (३२४) श्वासोच्छ्वास हो जाते हैं। इस एक जाप्य से एक उपवास का फल प्राप्त होता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है।
चत्तारिमंगल पाठ
चत्तारि मंगलं-अरिहंत मंगलं, सिद्ध मंगलं, साहु मंगलं, केवलि पण्णत्तो धम्मो मंगलं।
चत्तारि लोगुत्तमा-अरिहंत लोगुत्तमा, सिद्ध लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवलिपण्णत्तो धम्मो लोगुत्तमा।
चत्तारि सरणं पव्वज्जामि-अरिहंत सरणं पव्वज्जामि, सिद्ध सरणं पव्वज्जामि, साहु सरणं पव्वज्जामि, केवलि पण्णत्तो धम्मो सरणं पव्वज्जामि। ह्रौं शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। अनादि सिद्धमंत्र:।
(हस्तलिखित वसुनंदि प्रतिष्ठासार संग्रह)
इसलिए ये महामंत्र और चत्तारि मंगल पाठ अनादिनिधन है, ऐसा स्पष्ट है।वर्तमान में विभक्ति लगाकर ‘चत्तारिमंगल पाठ’-नया पाठ पढ़ा जा रहा है, जो कि विचारणीय है। यह पाठ कुछ वर्षों से अपनी दिगम्बर जैन परम्परा में आया है। देखें प्रमाण-‘ज्ञानार्णव’ जैसे प्राचीन ग्रंथ में बिना विभक्ति का प्राचीन पाठ ही है। यह विक्रम सम्वत् १९६३ से लेकर कई संस्करणों में वि.सं. २०५४ तक में प्रकाशित है। पृ. ३०९ पर यही प्राचीन पाठ है। प्रतिष्ठातिलक जो कि वीर सं. २४५१ में सोलापुर से प्रकाशित है, उसमें पृष्ठ ४० पर यही प्राचीन पाठ है।
आचार्य श्री वसुविंदु अपरनाम जयसेनाचार्य द्वारा रचित ‘प्रतिष्ठापाठ’ जो कि वीर सं. २४५२ में प्रकाशित है, उसमें पृ. ८१ पर प्राचीन पाठ ही है। हस्तलिखित ‘श्री वसुनंदिप्रतिष्ठापाठ संग्रह’ में भी प्राचीन पाठ है। प्रतिष्ठासारोद्धार जो कि वीर सं. २४४३ में छपा है, उसमें भी यही पाठ है। ‘क्रियाकलाप’ जो कि वीर सं. २४६२ में छपा है, उसमें भी तथा जो ‘सामायिकभाष्य’ श्री प्रभाचंद्राचार्य द्वारा ‘देववंदना’ की संस्कृत टीका है, उसमें भी अरहंत मंगलं—अरहंत लोगुत्तमा,……. अरहंत सरणं पव्वज्जामि यही पाठ है पुन: यह संशोधित नया पाठ क्यों पढ़ा जाता है ? क्या ये पूर्व के आचार्य व्याकरण के ज्ञाता नहीं थे ? इन आचार्यों की कृति में परिवर्तन, परिवर्धन व संशोधन कहाँ तक उचित है ?
नया पाठ-
चत्तारि मंगलं-अरहंता मंगलं, अरहंता लोगुत्तमा, अरहंते सरणं पव्वज्जामि, सिद्धे सरणं पव्वज्जामि ।
यह पाठ कुछ वर्षों से ही अनुमानत: श्वेताम्बर परम्परा से नया आया है, ऐसा पं. पन्नालाल जी साहित्याचार्य आदि विद्वानों ने कहा था। जो भी हो, हमें और आपको प्राचीन पाठ ही पढ़ना चाहिए। सभी पुस्तकों में प्राचीन पाठ ही छपाना चाहिए व मानना चाहिए। नया परिवर्द्धित पाठ नहीं पढ़ना चाहिए।
श्री गौतमस्वामी प्रणीत कृतियों का परिचय
१. चैत्यभक्ति—यह श्रीगौतमस्वामी के मुखकमल से विनिर्गत है।
२. निषीधिका दण्डक—इस दैवसिक प्रतिक्रमण के अन्तर्गत प्रतिक्रमण भक्ति में ‘‘निषीधिका दण्डक’’ आता है। इसमें प्रथम पद जो ‘‘णमो णिसीहियाए’’ है, उसका अर्थ टीकाकार ने १७ प्रकार से किया है।इस निषीधिका दण्डक में श्रीगौतमस्वामी ने अष्टापदपर्वत, सम्मेदशिखर, चम्पापुरी, पावापुरी आदि की भी वंदना की है।
जब चार ज्ञानधारी सर्वऋद्धि समन्वित गौतम गणधर इन तीर्थक्षेत्रों की वंदना करते हैं, तब आज जो अध्यात्म की नकल करने वाला कोई यह कहे कि ‘‘यदि साधु के तीर्थ वंदना का भाव हो जाये तो उसे प्रायश्चित लेना चाहिए। ऐसा कथन सर्वथा अनुचित है।
३. वीरभक्ति—सर्वज्ञ का लक्षण, धर्म का लक्षण आदि इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हैं।
४.गणधरवलय मन्त्र—बड़ा प्रतिक्रमण जो कि पाक्षिक, चातुर्मासिक और वार्षिक रूप में किया जाता है।
उसकी टीका के प्रारम्भ में टीकाकार कहते हैं—‘‘वृहत्प्रतिक्रमणलक्षणमुपायं विदधानस्तदादौ मंगलार्थमिष्टदेवताविशेषं नमस्कुर्वन्नाह णमो जिणाणमित्यादि।।’’
‘श्रीगौतमस्वामी दैवसिकादिप्रतिक्रमणादिभिर्निवारार्तुमशक्यानां दोषानां निराकरणार्थं वृहत्प्रतिक्रमण—लक्षणमुपायं विदधानस्तदादौ मंगलाद्यर्थमिष्टदेवता-विशेषं नमस्कुर्वन्नाह णमो जिणाणमित्यादि’’।
ये ‘‘णमो जिणाणं, णमो ओहिजिणाणं’’ आदि ४८ मंत्र गणधरवलय मन्त्र कहे जाते हैं।। बृहत्प्रतिक्रमणपाठ में प्रतिक्रमणभक्ति में इनका प्रयोग है।
इन मंत्रों का मंगलाचरण धवला की नवमी पुस्तक में है—
एवं दव्वट्ठिय जणाणुग्गहट्ठं णमोक्कारं गोदमभडारओ महाकम्म—पयडिपाहुडस्स आदिम्हि काऊण पज्जवट्ठियाणुग्गहट्ठमुत्तर सुत्ताणि भणदि।१
दूसरे सूत्र की उत्थानिका में विशेष स्पष्टीकरण हो रहा है।
इस प्रकार द्रव्यार्थिक नय से जनों के अनुग्रहार्थ गौतम भट्टारक महाकर्मप्रकृतिप्राभृत के आदि में नमस्कार करके पर्यायार्थिकनय युक्त शिष्यों के अनुग्रहार्थ उत्तर सूत्रों को कहते हैं—
णमो ओहिजिणाणं।।२।।
ये मंत्र आदि श्रीगौतमस्वामी द्वारा रचित ही हैं। इसके लिये षट्खंडागम आदि के प्रमाण देखिये।
षट्खंडागम में ये मंत्र ४४ हैं और प्रतिक्रमण पाठ में ४८ हैं।
(४८) णमो वड्ढमाणबुद्धरिसिस्स।।४४।
वर्धमान बुद्ध ऋषि को नमस्कार हो।।४४।।
शंका—जबकि वर्धमान भगवान् को पूर्व में नमस्कार किया जा चुका है तो फिर यहाँ दोबारा नमस्कार किसलिए किया गया है ?
समाधान—
जस्संतियं धम्मपहं णिगच्छे, तस्संतियं वेणयियं पउंजे।
कायेण वाचा मणसा वि णिच्चं, सक्कारए तं सिरपंचमेण१।।
‘जिनके समीप धर्मपथ प्राप्त हो, उनके निकट विनय का व्यवहार करना चाहिये तथा उनका सिर झुकाकर पांच अंग—पंचांग एवं काय, वचन और मन से नित्य ही सत्कार—नमस्कार करना चाहिये।’ इस आचार्य परंपरागत नियम को बतलाने के लिये पुन: नमस्कार किया गया है।
प्रतिक्रमणग्रंथत्रयी में यह मंत्र ऐसा है—
णमो भयवदो महदिमहावीर वड्ढमाणबुद्धरिसिणो चेदि।
जो भगवान सहज विशिष्ट मति, श्रुत, अवधि इन तीन ज्ञान के धारी और पूजा के अतिशय को प्राप्त हैं, महतिमहावीर और वर्धमान नाम के धारक अंतिम तीर्थंकर हैं, बुद्धर्षि—प्रत्यक्षवेदी—केवलज्ञान के धारी हैं। रुद्र के द्वारा किये गये उपसर्ग को जीतने से ‘महतिमहावीर’ यह नाम प्रसिद्ध हुआ है। इन अंतिम तीर्थंकर के वर्धमान, वीर, महावीर, सन्मति और महतिमहावीर ऐसे पांच नाम विख्यात हैं। ऐसे वर्धमान भगवान को नमस्कार होवे।
५. सुदं मे आउस्संतो—इसमें मुनिधर्म एवं श्रावक धर्म का वर्णन है।
६. श्रावक प्रतिक्रमण—इसमें पाक्षिक श्रावक से लेकर उत्कृष्ट श्रावक क्षुल्लक, ऐलक तक की ग्यारह प्रतिमाओं का प्रतिक्रमण है।
७. दैवसिक प्रतिक्रमण—मुनि-आर्यिका आदि जिस प्रतिक्रमण को प्रतिदिन प्रात: और सायंकाल में करते हैं वह दैवसिक-रात्रिक प्रतिक्रमण है।
८. पाक्षिक प्रतिक्रमण—पन्द्रह दिन में होने वाला या चार महीना या वर्ष में होने वाला बड़ा प्रतिक्रमण है। अष्टमी क्रिया में होने वाली आलोचना—ये तीनों प्रतिक्रमण श्री गौतमस्वामी द्वारा रचित हैं। यह रचनायें साक्षात् उनके मुखकमल से विनिर्गत हैं।
पाक्षिक प्रतिक्रमण में एक स्थल पर स्वयं श्रीगौतमस्वामी ने अपने नाम को संबोधित किया है। यथ—
‘‘जो सारो सव्वसारेसु, सो सारो एस गोदम।
सारं झाणं त्ति णामेण, सव्वबुद्धेिंह देसिदं।।
श्री गौतम ! सर्वसारों में भी जो सार है वह सार ‘ध्यान’ इस नाम से कहा गया है ऐसा सभी सर्वज्ञ भगवंतों ने कहा है।
दैवसिक प्रतिक्रमण की टीका करते हुए श्री प्रभाचन्द्राचार्य कहते हैं—
‘‘श्री गौतमस्वामी—मुनीनां दुष्षमकाले दुष्परिणामादिभि: प्रतिदिन—मुपार्जितस्य कर्मणो विशुद्ध्यर्थं प्रतिक्रमणलक्षणमुपायं विदधानस्तदादौ मंगलार्थमिष्ट-देवताविशेषं नमस्करोति—
‘श्रीमते वर्धमानाय नमो’’ इत्यादि।
इस उद्धरण से भी ये रचनायें श्रीगौतमस्वामी के मुखकमल से विनिर्गत हैं। ऐसा स्पष्ट हो जाता है।
श्री गौतमस्वामी द्वारा प्रणीत प्रतिक्रमण पाठ के प्रमाण
(प्रतिक्रमण ग्रंथत्रयी से)
श्रीगौतम स्वामी विरचित प्रतिक्रमण ग्रंथत्रयी ग्रंथ में श्री प्रभाचन्द्राचार्य ने संस्कृत टीका में अनेक स्थानों पर श्री गौतमस्वामी का नाम लिया है उनके प्रमाण इस ग्रंथ में देखिए। यह ग्रंथ वीरसंवत् २४७३ (सन् १९४७) में श्री १०८ चारित्रचक्रवर्ती आचार्य शांतिसागर दिगम्बर जैन जिनवाणी जीर्णोद्धारक संस्था से प्रकाशित है।
(१)श्री प्रभाचन्द्राचार्य विरचित टीकयाऽलङ्कृता प्रतिक्रमणग्रंथत्रयी
जीवे प्रमादजनिता: प्रचुरा: प्रदोषा यस्मात्प्रतिक्रमणत: प्रलयं प्रयान्ति।।
तस्मात्तदर्थममलं मुनिबोधनार्थं वक्ष्ये विचित्रभवकर्मविशोधनार्थम्।।१।।
श्रीगौतमस्वामी मुनीनां दुष्षमकाले दुष्परिणामादिभि: प्रतिदिनमुपार्जितस्य कर्मणो विशुद्ध्ध्यर्थं प्रतिक्रमणलक्षणमुपायं विदधानस्तदादौ मङ्गलार्थमिष्टदेवता—विशेषं नमस्करोति—
श्रीमते वर्धमानाय नमो नमितविद्विषे।
यज्ज्ञानान्तर्गतं भूत्वा त्रैलोक्यं गौष्पदायते।।१।।
टीका—नमो नमस्करोऽस्तु। कस्मै ? वर्धमानाय अन्तिमतीर्थंकरदेवाय (प्रतिक्रमण ग्रंथत्रयी पृ. १)
(२)ये रात्रौ दिवसे पथि प्रयततां दोषा यतीनां कृतोऽ—
प्रयायाता: प्रलये तु हेतुरमलस्तेषामयं दर्शित:।।
श्रीमद्गौतमनामभिर्गणधरैर्लोकत्रयोद्योतवै:।
युव्यक्त: सकलोऽप्यसौ यतिपतेर्ज्ञात: प्रभाचन्द्रत:।।
।।इति—श्रीगौतमस्वामी—विरचित—दैवसिकादि—प्रतिक्रमणायाष्टीका श्रीमत्प्रभाचन्द्र—पण्डितेन कृतेति मंगलमहा।।
इतिश्री—अष्टोत्तरशतगुणगणालंकृतचारित्रचक्रवर्त्याचार्य—शांतिसागर—दिगंबरजैन—जिनवाणीजीर्णोद्धारक-संस्थया प्राकाश्यं नीताया: प्रतिक्रमणग्रंथत्रय्या: प्रथमो ग्रंथ: समाप्त:।।(प्रतिक्रमण ग्रंथत्र्यी पृ. ८७—८८)
(३)बृहत्प्रतिक्रमणम्
दोषा दैवसिकप्रतिक्रमणतो नश्यन्ति ये नो नृणां
तन्नाशार्थमिमां ब्रवीति गणभृच्छ्रीगौतमो निर्मलाम्।
सूक्ष्मस्थूलसमस्तदोषहननीं सर्वात्मशुद्धिप्रदां
यस्मान्नास्ति बृहत्प्रतिक्रमणतस्तन्नाशहेतु: पर:।।१।।
श्री गौतमस्वामी दैवसिकादिप्रतिक्रमणादिभिर्निराकर्तुमशक्यानां दोषाणां निराकणार्थं बहुत्प्रतिक्रमणलक्षणमुपायं विदधानस्तदादौ मंगलार्द्यर्थमिष्टदेवता— विशेषं नमस्कुर्वन्नाह णमो जिणाणमित्यादि। (प्रतिक्रमण ग्रंथत्रयी पृ. ८९)
(४)सुधम्मे इत्यादि श्रीगौतमस्वामी—
इष्टोपयोगसंबोधेनेन भव्यान्संबोधयन् सुधम्मे इत्याद्याह। आउस्संतो। आयुष्मन्तो भव्या मे मया सुदं श्रुतम्। इह भरतक्षेत्रे खलु स्फुटं भयवदा भगवताहिसादीनि व्रतानि सम्मं धम्मोति सम्यग्धर्म इति—उवदेसिदाणि उपदिष्टानि। (प्रतिक्रमण ग्रंथत्रयी पृ. ९७)
(५)कायं व्युत्सृजामि त्यजामि तत्रोदासीनो भवामि। कथं भूतं कायं ? पावकम्मं। पापकर्म यस्मात् पापाय वा कर्म व्यापारो यस्य।। दुच्चरियं।। दुष्टं दुर्गतिप्रापकं चरितं यस्य।
यत्पापं प्रचुरं प्रदुष्टमनसा जीवै: पुरोपार्जितं।
तत्सद्य: प्रलयं प्रयाति निखिलं तेषां प्रतिक्रामतां।।
मत्वेदं गणभृत्प्रतिक्रमणया तन्नाशमासूक्तवान्।
व्याख्याता तदियं प्रभेंदुमुनिना सद्धीधनैर्भाव्यतां।।
।।इति—श्रीगौतमस्वामि—विरचित—बृहत्प्रतिक्रमणायाष्टीका श्रीमत्प्रभाचंद—पंडितेन कृतेति।।
इतिश्री—अष्टोत्तरशतगुणगणालंकृतचारित्रचक्रवर्त्याचार्य—शांतिसागर—दिगंबरजैनजिनवाणीजीर्णोद्धारकसंस्थया प्राकाश्यं नीताया: प्रतिक्रमणग्रंथत्रय्या: द्वितीयो ग्रंथ: समाप्त:।। (प्रतिक्रमण ग्रंथत्रयी पृ. १५२)
(६)आलोचना
पंचाचारविशोधनार्थममलामालोचनामुक्त्वा—
नष्टम्यादिदिनावधिर्गणनया श्रीगौतमो मादृशं।
स्पष्टार्थै: प्रवरै: प्रसन्नवचनै: सर्वप्रबोधप्रदै—
स्तां व्याख्यातुमशेष—तोऽमलवपु: प्रारभ्यते प्रक्रम:।।१।।
श्री गौतमस्वामी मुनीनां दुष्षमकाले दुष्परिणामादिभि: प्रतिदिनमुपार्जितस्य पंचाचारगोचरस्यातीचारस्य दिनगणनया विशुद्ध्यर्थमालोचनालक्षणमुपायमुप—दर्शयन्नाहठच्छामीत्यादि।। भंते।। भगवन् इच्छामि।। कि कर्तुं ? आलोचेदुं।। आलोचयितुं।। आलोचनांविशुद्धिं कर्तुं।। क्व ? अट्ठमियम्हि।। आष्टमिके। अष्टम्यामष्टसंख्यावच्छिन्नदिनगणनायां भवो ज्ञानाचाराद्यतीचार आष्टमिक:। तस्मिन्।। अट्ठमियमालोचेदुमिति।। पाठे त्वष्टसंख्यावच्छिन्नदिनगणनाप्रभवं तदतीचारमालोचयितुमिच्छामीत्यर्थ:। (प्रतिक्रमण ग्रंथत्रयी पृ. १५३)
(७)सम्मत्तमरणं। सम्यक्त्वयुक्तस्यापरित्यक्तसम्यक्त्वस्य मरणं।। होउ मज्झं।। भवतु मम।। पंडितमरणं।। भक्तप्रत्याख्यानेंगिनीपादोपयानमरण—भेदात् त्रिविधं पंडितमरणं मम भवतु।। वीरियमरणं।। वीर्ययुक्तस्याक्लीबस्य मरणं मम भवतु।। दुक्खक्खओ।। दु:खाना चातुर्गतिकानां क्षयो विनाश:। कम्मक्खओ।। कर्मणां ज्ञानावरणादीनां क्षय: प्रलयो भवतु।। बोहिलाहो।। बोधे: रत्नत्रयस्य लाभो मम भवतु।। सुगइगमणं।। शोभनायां गतौ मोक्षगतौ गमनं मम भवतु।। जिणगुणसंपत्ति।। जिनस्य प्रक्षीणाशेषकर्मणो भगवतो गुणा अनंतज्ञानादय:। तेषां संप्राप्तिर्मम भवतु।।
यन्नो वैश्चिदपि प्रसन्नवचनैर्नि: शेषशुद्धिप्रदं।
व्याख्यातं प्रवरं प्रतिक्रमणसद्गं्थत्रयं धीमतां।।
तद्येन प्रकटीकृतं भवहरं शब्दार्थतो निर्मलं।
स श्रीमान्निखिलोपकारनिरतो जीयात्प्रभेंदुर्जिन:।।
पेटलापट्के श्रीचंद्रप्रभदेवपादानामग्रे श्रीगौतमस्वामीकृत—प्रतिक्रमणात्रयस्य टीकात्रयं—श्री प्रभाचंद्रपंडितेन कृतमिति।।१।।
।।श्री।।श्री।।श्री।। ।।श्रीपार्श्वनाथाय नम:।।
इतिश्री—अष्टोत्तरशतगुणगणालंकृतचारित्रचक्रवर्त्याचार्यशांतिसागर—दिगंम्बर—जैनजिनवाणीजीर्णोद्धारक-संस्थया प्राकाश्यं नीताया: प्रतिक्रमण—ग्रंथत्रय्या: तृतीयो ग्रंथ: समाप्त।। (प्रतिक्रमण ग्रंथत्रयी पृ. १९४, १९५)
चैत्यभक्ति के विषय में उद्गार
पं. श्री लालाराम जी के
पूज्यवर आचार्यश्री १०८ शांतिसागर जी महाराज ने अपने मुनिसंघ सहित वीर निर्वाण संवत् २४५७ का चातुर्मास देहली नगर में किया था। उनके पुण्यमय दर्शन करने के लिए मैं भी देहली गया था।
उस संघ में मुनिराज श्री १०८ श्रुतसागर जी भी हैं। इन समस्त मुनिराजों को इन भक्तियों से सदा काम पड़ता रहता है कितनी ही भक्तियाँ तो प्रतिदिन बोलनी पड़ती हैं तथा कितनी ही विशेष-विशेष समय पर पढ़ी जाती हैं। इन भक्तियों के पढ़ते समय यदि इनका अर्थज्ञान हो, तो फिर और भी विशेष आनन्द आता है इसीलिए इनके अर्थ जानने की मुनिराज श्री १०८ श्रुतसागर जी की प्रबल इच्छा थी। मुनियों की इच्छाएँ और प्रवृत्तियाँ सब धार्मिक ही होती हैं इसीलिए इन इच्छाओं की पूर्ति करना विशेष पुण्य का कारण समझा जाता है। यही समझकर मैंने वहाँ से आकर अपनी तुच्छ बुद्धि के अनुसार यह हिन्दी टीका लिखी है।
इन भक्तियों में अधिकतर भक्तियाँ आचार्यश्री १०८ पूज्यपाद स्वामी की लिखी हुई हैं। आचार्य पूज्यपाद स्वामी कितने प्रौढ़ और प्राचीन उद्भट विद्वान् आचार्य थे, यह बात प्राय: समाज के समस्त जनसाधारण तक जानते हैं।
इन भक्तियों की एक संस्कृत टीका है जो आचार्य श्री प्रभाचंद्र स्वामी की बनाई हुई है। उस टीका में चैत्यभक्ति की टीका के प्रारंभ में लिखा है कि—
श्री वर्द्धमानस्वामिनं प्रत्यक्षीकृत्य गौतमस्वामी ‘‘जयति भगवान्’’ इत्यादि स्तुतिमाह।
अर्थ—गौतम स्वामी ने भगवान् महावीर स्वामी के प्रत्यक्ष दर्शन कर ‘जयति भगवान्’ इन शब्दों से प्रारंभ करते हुए स्तुति की।
वृहद्द्रव्यसंग्रह की संस्कृत टीका में भी लिखा है :—
ततश्च जयति भगवान् इत्यादि नमस्व्ाâारं कृत्वा जिनदीक्षां गृहीत्वा कचलोचनानन्तरमेव चतुर्ज्ञानसप्तर्द्धिसम्पन्नास्त्रयोपि (गौतम अग्निभूत वायुभूत नामान:) गणधरदेवा: संजाता:। गौतमस्वामी भव्योपकारार्थं द्वादशांगश्रुतरचनां कृतवान्।
तदनन्तर गौतम, अग्निभूति, वायुभूति इन तीनों विद्वानों ने ‘‘जयति भगवान्’’ इत्यादि शब्दों से स्तुति करते हुए भगवान महावीर स्वामी को नमस्कार किया। जिनदीक्षा ग्रहण की और केशलोंच करने के अनन्तर ही मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान और मन:पर्ययज्ञान चारों ज्ञान उनको प्रगट हो गये तथा सातों प्रकार की ऋद्धियाँ प्रगट हो गईं। इस प्रकार वे तीनों ही मुनि उसी समय भगवान् महावीर स्वामी के गणधर हुए। उनमें से गौतम स्वामी ने भव्य जीवों का उपकार करने के लिए द्वादशांग श्रुतज्ञान की रचना की।
इन दोनों कथनों से यह निर्विवाद सिद्ध हो जाता है कि इन भक्तियों में से चैत्यभक्ति भगवान् महावीर स्वामी के मुख्य गणधर भगवान् गौतम स्वामी की बनाई हुई है। इससे इसकी प्राचीनता और प्रौढ़ प्रमाणता भी स्वयं सिद्ध हो जाती है।
इस स्तुति में कृत्रिम-अकृत्रिम चैत्यालयों का भी वर्णन है। जिसमें भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी, कल्पवासी आदि सब देवों के चैत्यालयों का तथा मध्यलोक के अकृत्रिम चैत्यालयों का भी वर्णन है। इससे सिद्ध होता है कि यह मूर्ति पूजा जैनियों ने ब्राह्मणों से नहीं ली है किन्तु अनादिकाल से चली आ रही है। जो लोग मूर्तिपूजा आदि को ब्राह्मणों से ली हुई बतलाते हैं, उनको इससे शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। साथ में जो लोग जैन भूगोल को अप्रमाण और टीलों पर बैठकर लिखे हुए बतलाते हैं, उन्हें भी अपने नेत्र खोल लेने चाहिए।
इस ऊपर के कथन से यह भी सिद्ध हो जाता है कि यह चैत्यभक्ति महावीर स्वामी के केवलज्ञान के समय की बनी हुई है अर्थात् चतुर्थकाल में जब तेंतीस वर्ष साढ़े आठ महीना शेष रह गये थे, उस समय की यह रचना है। ऐसी-ऐसी चतुर्थकाल की रचनाएँ न जाने कितनी हैं, जो अज्ञानता के कारण हमें मालूम नहीं हैं। बहुत से लोग कहा करते हैं कि ‘‘वर्तमान के समस्त शास्त्र पंचमकाल के बने हुए हैं इसलिए उनमें कहा हुआ विषय भगवान महावीर स्वामी का कहा हुआ नहीं माना जा सकता’’ ऐसे लोगों को भी अनर्गल बोलना बंद कर कुछ दिन तक जानकार विद्वानों से अध्ययन करना चाहिए।
यह हिन्दी टीका मैंने संस्कृत टीका के आधार से की है तथापि प्रमादवश या अज्ञानवश इसमें जो कुछ स्खलन हुआ हो, उसे विद्वानों को सुधार कर बांच लेना चाहिए।
फाल्गुन शु. १२, वी. नि. सं. २४५८
-लालाराम जैन शास्त्री, मोरेना (म.प्र.)
श्री गौतमस्वामी प्रणीत प्रतिक्रमण पाठ में तथा
अन्य ग्रंथों में समानता व अन्तर
श्री गौतमस्वामी प्रणीत प्रतिक्रमण पाठ में जो ‘‘नव पदार्थ’’, ‘‘द्वादशतप’’, ‘‘बंध के कारण’’, ‘‘श्रावक के बारह व्रत’’ व पच्चीस भावनाएँ वर्णित हैं। इन्हीं के अनुसार षट्खण्डागम ग्रंथ व श्री कुंदकुंददेव द्वारा विरचित समयसार, प्रवचनसार, मूलाचार आदि ग्रंथों में समानता है। आगे के ‘‘तत्त्वार्थसूत्र’’ आदि गं्रंथों से अन्तर आया है। उसे यहाँ दिखाते हैं—
१. नव पदार्थ—
श्री गौतमस्वामी कथित नवपदार्थ—
से अभिमद-जीवाजीव-उवलद्ध-पुण्णपाव-आसव-संवर-णिज्जर-बंधमोक्ख-महिकुसले१।
इसमें अभिमत जीव रु अजीव उपलब्ध पुण्य अरु पाप कहे।
आस्रव संवर निर्जर व बंध अरु मोक्ष कुशल नव तत्त्व रहें।।
षट्खण्डागम धवला टीका पुस्तक १३ में नव पदार्थ—
‘‘जीवाजीवपुण्ण-पाव-आसव-संवर-णिज्जर-बंध-मोक्खेहि णवहि पयत्थेहि वदिरित्तमण्णं ण किं पि अत्थि, अणुवलंभादो।’’
जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आस्रव, संवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष, इन नौ पदार्थों के सिवाय अन्य कुछ भी नहीं है क्योंकि इनके सिवाय अन्य कोई पदार्थ उपलब्ध नहीं होता।
यहाँ इन्हें नौ पदार्थ कहा है।
समयसार में श्री कुंदकुंददेव ने कहा है-
(१५ ज.) भूयत्थेणाभिगदा जीवाजीवा य पुण्णपावं च।
आसवसंवरणिज्जर बंधो मोक्खो य सम्मत्तं३।।१३ अ.।।
भूतार्थेनाभिगता जीवाजीवौ च पुण्यपापं च।
आस्रवसंवरनिर्जरा बंधो मोक्षश्च सम्यक्त्वम्।।१३।।
पद्यानुवाद-शेर छंद-
(१५ ज.) भूतार्थ से जाने गए जो जीवाजीव हैं।
जो पुण्य पाप आस्रव संवर भी तत्त्व हैं।।
निर्जर व बंध मोक्ष ये सम्यक्त्व कहे हैं।
व्यवहार से ये मुक्ति के साधक भी हुए हैं।।१२ अ.।।
उत्थानिका-शुद्धनय से जानना ही सम्यक्त्व है, ऐसा सूत्रकार कहते हैं-
अन्वयार्थ-(भूतार्थेन अभिगता: जीवाजीवौ च पुण्यपापं च आस्रवसंवर-निर्जरा: बंध: च मोक्ष: सम्यक्त्वं) भूतार्थ से जाने हुए जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आस्रव, संवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष ये नव तत्त्व ही सम्यक्त्व हैं।।१२।।
आत्मख्याति-अमूनि हि जीवादीनि नवतत्त्वानि भूतार्थेनाभिगतानि सम्यग्दर्शनं संपद्यंत एवामीषु तीर्थप्रवृत्तिनिमित्तभूतार्थनयेन व्यपदिश्यमानेषु जीवाजीवपुण्यपापास्रवसंवरनिर्जराबंधमोक्षलक्षणेषु नवतत्त्वेष्वेकत्वद्योतिना भूतार्थनयेनैकत्वमुपानीय शुद्धनयत्वेन व्यवस्थापितस्यात्मनोनुभूतेरात्मख्याति-लक्षणाया: संपद्यमानत्वात्।
आत्मख्याति-ये जीव आदि नवतत्त्व भूतार्थनय से जाने हुए सम्यग्दर्शन ही हो जाते हैं क्योंकि तीर्थ प्रवृत्ति के लिए अभूतार्थनय से कहे गये जो जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आस्रव, संवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष लक्षण वाले ये नवतत्त्व हैं। उन तत्त्वों में एकत्व को प्रकट करने वाले, भूतार्थनय से एकत्व को प्राप्त कर शुद्धनय से व्यवस्थापित जो आत्मा है उसकी आत्मख्याति लक्षण वाली अनुभूति उत्पन्न हो जाती है अर्थात् शुद्धनय से नवतत्त्वों को जानने से आत्मा की ही अनूभूति होती है।
भूमिका-अथ कश्चिदासन्नभव्य: पीठिकाव्याख्यानमात्रेणैव हेयोपादेयतत्त्वं परिज्ञाय विशुद्धज्ञान-दर्शनस्वभावं निजस्वरूपं भावयति। विस्तररुचि: पुनर्नवभिरधिकारै: समयसारं ज्ञात्वा पश्चाद्भावनां करोति। तद्यथा—विस्तररुचिशिष्यं प्रति जीवादिनवपदार्थाधिकारै: समयसारव्याख्यानं क्रियते।
उत्थानिका-तत्रादौ नवपदार्थाधिकारगाथाया आर्त्तरौद्रपरित्यागलक्षण-निर्विकल्पसामायिक-स्थितानां यच्छुद्धात्मरूपस्य दर्शनमनुभवनमवलोकनमुप-लब्धि: संवित्ति: प्रतीति: ख्यातिरनुभूतिस्तदेव निश्चयनयेन निश्चयचारित्रा—विनाभावि निश्चयसम्यक्त्वं भण्यते। तदेव च गुणगुण्यभेदरूपनिश्चनयेन शुद्धात्मस्वरूपं भवतीत्येका पातनिका। अथवा नवपदार्था भूतार्थेन ज्ञाता: संतस्त एवाभेदोपचारेण सम्यक्त्वविषयत्वाद् व्यवहारसम्यक्त्वनिमित्तं भवंति, निश्चयनयेन तु स्वकीयशुद्धपरिणाम एव सम्यक्त्वमिति द्वितीया चेति पातनिकाद्वयं मनसि धृत्वा सूत्रमिदं प्ररूपयति–
भूदत्थेणाभिगदा, जीवाजीवा य पुण्णपावं च।
आसवसंवरणिज्जर-बंधो मोक्खो य सम्मत्तं।।१५।।
भूतार्थेनाऽभिगता जीवाऽजीवौ च पुण्यपापं च।
आस्रव-संवर-निर्जरा-बंधो मोक्षश्च सम्यक्त्वम्।।१५।।
तात्पर्यवृत्ति-भूदत्थेण भूतार्थेन निश्चयनयेन शुद्धनयेन अभिगदा अभिगता निर्णीता निश्चिता ज्ञाता: संत:। के ते। जीवाजीवा य पुण्यपावं च आसवसंवर-णिज्जरबंधो मोक्खो य जीवाजीव-पुण्यपापास्रवसंवर-निर्जराबंधमोक्षस्वरूपा नवपदार्था: सम्मत्तं त एवाभेदोपचारेण सम्यक्त्वविषय-त्वात्कारणत्वात्सम्यक्त्वं भवंति। निश्चयेन परिणाम एव सम्यक्त्वमिति।१
भूमिका-कोई आसन्नभव्य जीव इस पीठिका के व्याख्यानमात्र से ही हेय-उपादेय तत्त्वोें को जानकर विशुद्ध ज्ञानदर्शन स्वभाव वाले अपने स्वरूप की भावना करता है उसका अनुभव करता है किन्तु पुन: विस्तार रुचि वाला कोई शिष्य आगे कहे जाने वाले नव अधिकारों के द्वारा समयसारस्वरूप अपनी शुद्ध आत्मा को समझकर अनंतर उसकी भावना करता है। उसी विस्तार रुचि वाले शिष्य के प्रति जीवादि नव पदार्थ के नव अधिकारों से इस समयसार का व्याख्यान किया जा रहा है।
उत्थानिका-उनमें सर्वप्रथम नव पदार्थ के अधिकाररूप गाथा में आर्त, रौद्रध्यान के परित्याग लक्षण, निर्विकल्पसामायिक में जो स्थित हैं, ऐसे मुनियों के जो शुद्ध आत्मा के स्वरूप का दर्शन है, अनुभवन है, अवलोकन है, उपलब्धि है, संवित्ति है, प्रतीति है, ख्याति है और अनुभूति है वही निश्चयनय से निश्चयचारित्र के साथ अविनाभाव संबंध रखने वाला ऐसा निश्चयसम्यक्त्व या वीतरागसम्यक्त्व कहलाता है और वही सम्यक्त्व गुण-गुणी में अभेद को कहने वाले ऐसे निश्चयनय से शुद्धात्मा का स्वरूप है। इस प्रकार से यह एक पातनिका अर्थात् उत्थानिका हुई।
अथवा भूतार्थ से जाने गये जो जीवादि नव पदार्थ हैं वे ही अभेदोपचार से सम्यक्त्व का विषय होने से व्यवहारसम्यक्त्व के निमित्त होते हैं किन्तु निश्चयनय से अपनी आत्मा का शुद्ध परिणाम ही सम्यक्त्व है, इस प्रकार से यह दूसरी उत्थानिका हुई। इस तरह इन दोनों उत्थानिकाओं को मन में रखकर आगे का सूत्र प्ररूपित करते हैं-
अन्वयार्थ-(भूयत्थेण अभिगदा जीवाजीवा य पुण्णपावं च आसव-संवरणिज्जर बंधो य मोक्खो सम्मत्तं) भूतार्थ से—अशुद्ध निश्चयनय से जाने गये जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आस्रव, संवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष ये ही सम्यक्त्व हैं।।१५।।
तात्पर्यवृत्ति-भूतार्थ अर्थात् निश्चयनय या शुद्धनय, इस शुद्धनय के द्वारा निर्णय किये गये—निश्चित किये गये—जाने गये जो जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आस्रव, संवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष ये नव पदार्थ हैं वे ही अभेद के उपचार के द्वारा सम्यक्त्व होते हैं क्योंकि ये नव पदार्थ ही सम्यक्त्व के विषय हैं और सम्यक्त्व के लिए कारण हैं। निश्चयनय से आत्मा का श्रद्धान रूप परिणाम ही सम्यक्त्व है।
इसी गाथा को श्री कुंदकुंद स्वामी ने अपने मूलाचार ग्रंथ में लिया है-
भूयत्थेणाभिगदा जीवाजीवा य पुण्णपावं च।
आसवसंवरणिज्जरबंधो मोक्खो य सम्मत्तं१।।२०३।।
गोम्मटसार जीवकाण्ड के अनुसार देखें-
णव य पदत्था जीवाजीवा ताणं च पुण्णपावदुगं२।
आसवसंवरणिज्जरबंधा मोक्खो य होंतित्ति।।६२१।।
जीवदुगं उत्तत्थं जीवा पुण्णा हु सम्मगुण सहिदा।
वदसहिदा वि य पावा तव्विवरीया हवंतित्ति।।६२२।।
जीवा अजीवा: तेषां पुण्यपापद्वयं आस्रव: संवरो निर्जरा बन्धो मोक्षश्चेति नवपदार्था भवन्ति। पदार्थशब्द: सर्वत्र सम्बन्धनीय:,-जीवपदार्थ: इत्यादि:।।६२१।।
जीवाजीवपदार्थौ द्वौ पूर्व जीवसमासे षड्द्रव्याधिकारे चोक्तार्थौ। पुण्यजीवा: सम्यक्त्वगुणयुक्ता व्रतयुक्ताश्च स्यु:। तद्विपरीतलक्षणा: पापजीवा: खलु नियमेन।।६२२।।
तत्त्वार्थसूत्र ग्रंथ में इनका क्रम बदला है। सर्वार्थसिद्धि ग्रंथ में देखिए—
तत्त्वार्थश्रद्धानं सम्यग्दर्शनमित्युक्तम्। अथ किं तत्त्वमित्यत इदमाह—
जीवाजीवास्रवबन्धसंवरनिर्जरामोक्षास्तत्त्वम्३।।४।।
तत्र चेतनालक्षणो जीव:। सा च ज्ञानादिभेदादनेकधा भिद्यते। तद्विपर्ययलक्षणोऽजीव:। शुभाशुभकर्मागमद्वाररूपं आस्रव:। आत्म-कर्मणोरन्योऽन्यप्रदेशानुप्रवेशात्मको बन्ध:। आस्रवनिरोधलक्षण: संवर:। एकदेशकर्मसंक्षयलक्षणा निर्जरा। कृत्स्नकर्म वियोगलक्षणो मोक्ष:। एषां प्रपञ्च उत्तरत्र वक्ष्यते। सर्वस्य फलस्यात्माधीनत्वादादौ जीवग्रहणम्। तदुपकारार्थ त्वात्तदनन्तरमजीवाभिधानम्। तदुभयविषयत्वात्तदनन्तरमास्रवग्रहणम्। तत्पूर्वत्वातदनन्तरं बन्धाभिधानम्। संवृतस्य बन्धाभावात्तत्प्रत्यनीक-प्रतिपत्त्यर्थं तदनन्तरं संवरवचनम्। संवरे सति निर्जरोपपत्तेस्तदन्तिके निर्जरावचनम्। अन्ते प्राप्यत्वान्मोक्षस्यान्ते वचनम्।
इह पुण्यपापग्रहणं कर्त्तव्यम्। ‘नवपदार्था:’ इत्यन्यैरप्युक्तत्वात्। न कर्त्तव्यम् आस्रवे बंधे चान्तर्भावात्।
जीवादि पदार्थों का श्रद्धान करना सम्यग्दर्शन है। अब तत्त्व कौन-कौन हैं, इस बात को बतलाने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं-
जीव, अजीव, आस्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष ये तत्त्व हैं।।४।।
इनमें से जीव का लक्षण चेतना है जो ज्ञानादिक के भेद से अनेक प्रकार की है। जीव से विपरीत लक्षण वाला अजीव है। शुभ और अशुभ कर्मों के आने के द्वार रूप आस्रव है। आत्मा और कर्म के प्रदेशों का परस्पर मिल जाना बंध है। आस्रव का रोकना संवर है। कर्मों का एकदेश अलग होना निर्जरा है और सब कर्मों का आत्मा से अलग हो जाना मोक्ष है। सब फल जीव को मिलता है अत: सूत्र के प्रारंभ में जीव का ग्रहण किया है। अजीव जीव का उपकारी है यह दिखलाने के लिए जीव के बाद अजीव का कथन किया है। आस्रव जीव और अजीव दोनों को विषय करता है अत: इन दोनों के बाद आस्रव का ग्रहण किया है। बंध आस्रवपूर्वक होता है इसलिए आस्रव के बाद बंध का कथन किया है। संवृत जीव के बंध नहीं होता, अत: संवर बंध का उलटा हुआ इस बात का ज्ञान कराने के लिए बंध के बाद संवर का कथन किया है। संवर के होने पर निर्जरा होती है इसलिए संवर के पास निर्जरा कही है। मोक्ष अन्त में प्राप्त होता है इसलिए उसका अन्त में कथन किया है।
तत्त्वार्थराजवार्तिक के कतिपय अंश-
त्रिकालविषयजीवनानुभवनात् जीव:१।।७।।
दशसु प्राणेषु यथोपात्त-प्राणापर्यायेण त्रिषु कालेषु जीवनानुभवनात् ‘जीवति, अजीवीत्, जीविष्यति’ इति वा जीव। तथा सति सिद्धानामपि जीवत्वं सिद्धं जीवितपूर्वत्वात्। संप्रति न जीवन्ति सिद्धा:, भूतपूर्वगत्या जीवत्वमेषाम् इत्यौपचारिकत्वं स्यात्, मुख्यं चेष्यते:, नैष दोष:, भावप्राणज्ञानदर्शनानुभवनात् सांप्रतिकमपि जीवत्वमस्ति। अथवा रूढिशब्दोऽयम्। रूढौ च क्रिया व्युत्पत्त्यर्थेवेति कदाचित्कं जीवनमपेक्ष्य सर्वदा वर्तते गोशब्दवत्।
तद्विपर्ययोऽजीव:।।८।।
यस्य जीवनमुक्तलक्षणं नास्त्यसौ तद्विपर्ययाद् अजीव इत्युच्यते।
आस्रवत्यनेन आस्रवणमात्रं वा आस्रव:।।९।।
येन कर्मास्रवति यद्वा आस्रवणमात्रं वा स आस्रव:।
बध्यतेऽनेन बंधनमात्रं वा बन्ध:।।१०।।
बध्यते येन अस्वतन्त्रीक्रियते येन, अस्वतन्त्रीकरणमात्रं वा बन्ध:।
संव्रियतेऽनेन संवरणमात्रं वा संवर:।।११।।
येन संव्रियते येन संरुध्यते, संरोधनमात्रं वा संवर:।
निर्जीर्यते यया निर्जरणमात्रं वा निर्जरा।।१२।।
निर्जीर्यते निरस्यते यया, निरसनमात्रं वा निर्जरा।
मोक्ष्यते येन मोक्षणमात्रं वा मोक्ष:।।१३।।
मोक्ष्यते अस्यते येन असनमात्रं वा मोक्ष:।
द्रव्यसंग्रह में देखिए-
जीवो उवओगमओ, अमुत्तिकत्ता सदेहपरिमाणो।
भोत्ता संसारत्थो, सिद्धो सो विस्ससोड्ढगई१।।२।।
-शंभुछंद—(पद्यानुवाद)-
जो जीता है सो जीव कहा, उपयोगमयी वह होता है।
मूर्ती विरहित कर्ता स्वदेह, परिमाण कहा औ भोक्ता है।।
संसारी है औ सिद्ध कहा, स्वाभाविक ऊर्ध्वगमनशाली।
इन नौ अधिकारों से वर्णित, है जीव द्रव्य गुणमणिमाली।।२।।
अर्थ-प्रत्येक प्राणी जीव है, उपयोगमयी है, अमूर्तिक है, कर्ता है, स्वदेह परिमाण रहने वाला है, भोक्ता है, संसारी है, सिद्ध है और स्वभाव से ऊर्ध्वगमन करने वाला है। ये जीव के नव विशेष लक्षण हैं।
अज्जीवो पुण णेओ, पुग्गल धम्मो अधम्म आयासं।
कालो पुग्गल मुत्तो, रूवादिगुणो अमुत्ति सेसादु।।१५।।
पुद्गल औ धर्म, अधर्म तथा, आकाश काल ये हैं अजीव।
इन पाँचों में पुद्गल मूर्तिक, रूपादि गुणों से युत सदीव।।
बाकी के चार अमूर्तिक हैं, स्पर्श वर्ण रस गंध रहित।
चैतन्य प्राण से शून्य अत:, ये द्रव्य अचेतन ही हैं नित।।१५।।
अर्थ—पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल ये अजीव द्रव्य पाँच प्रकार का है ऐसा जानो। इनमें से पुद्गल द्रव्य मूर्तिक है क्योंकि वह रूप, रस, गंध और स्पर्श गुण वाला है, बाकी शेष द्रव्य अमूर्तिक हैं।
आसव बंधणसंवर-णिज्जरमोक्खा सपुण्णपावा जे।
जीवाजीव-विसेसा, तेवि समासेण पभणामो।।२८।।
हैं जीव अजीव इन्हीं दो के, सब भेद विशेष कहे जाते।
वे आस्रव बंध तथा संवर, निर्जरा मोक्ष हैं कहलाते।।
ये सात तत्त्व हो जाते हैं, इनमें जब मिलते पुण्य पाप।
तब नौ पदार्थ होते इनको, संक्षेप विधि से कहूँ आज।।२८।।
अर्थ-जीव और अजीव के विशेष भेद रूप आस्रव, बन्ध, संवर, निर्जरा और मोक्ष होते हैं। ये पुण्य और पाप से सहित भी हैं। इन सबको हम संक्षेप से कहते हैं।
श्रीगौतमस्वामी प्रणीत प्रतिक्रमण पाठ में
परिवर्तन-परिवर्धन उचित नहीं है।
(१) करोम्यहं—आजकल कुछ साधु-साध्वियां ‘‘कुर्वेऽहं’’ क्रिया को पढ़ने लगे हैं किंतु मुझे यह संशोधन नहीं जँचा है अत: मैंने यहाँ ‘‘करोम्यहं’’ ऐसा आचार्य प्रणीत प्राचीन पाठ ही सर्वत्र रखा है।
सिद्धांतचक्रवर्ती श्रीवीरनंदि आचार्य ने आचारसार ग्रंथ में ‘‘करोम्यहं’’ पाठ ही लिया है।
यथा-‘‘क्रियायामस्यां व्युत्सर्गं भक्तेरस्या: करोम्यहं१।’’अनगार धर्मामृत में पाक्षिक प्रतिक्रमण के लक्षण की स्वोपज्ञटीका में ‘‘करोम्यहं’’ क्रिया का प्रयोग पंद्रह बार आया है। उदाहरण के लिये देखिये—
‘‘सर्वातिचारविशुद्ध्यर्थं पाक्षिकप्रतिक्रमणक्रियायां सिद्धभक्तिकायोत्सर्गं करोम्यहं२।’’ इत्यादि।
क्रियाकलाप में देववंदना, दैवसिक प्रतिक्रमण, पाक्षिकप्रतिक्रमण एवं अन्य क्रियाओं की प्रयोगविधि में ‘‘करोम्यहं’’ पाठ ही उपलब्ध है।
चारित्रसार ग्रंथ में भी—‘‘चैत्यभक्तिकायोत्सर्गं करोमीति विज्ञाप्य इत्यादि पाठों में ‘‘करोमि’’ क्रिया ही है। ऐसा ही सामायिक भाष्यग्रंथ एवं प्रतिष्ठातिलक ग्रंथ में भी ‘‘करोमि, करोम्यहं’’ पाठ ही उपलब्ध हो रहे हैं। कुल मिलाकर सभी ग्रंथों में इस परस्मैपदी ‘‘करोमि’’ क्रिया ही उपलब्ध हो रही है पुन: इसे बदलकर ‘‘कुर्वेऽहं’’ पाठ क्यों रखा गया ? यह विचारणीय है।
(२) ‘‘णाणाणं दंसणाणं चरित्ताणं’ पाठ सामायिक दण्डक में है यहाँ ‘तवाणं’ पाठ बढ़ाया है सो उचित नहीं है देखिये प्रमाण—
‘‘णाणाणमित्यादि—ज्ञानदर्शनचारित्राणां सदा करोमि क्रियाकर्म। गुणानामानन्त्य—संभवेऽपि रत्नत्रयस्य प्राधान्येन मोक्षोपायभूतत्वात्तदेव स्तुतम्।’’
(क्रियाकलाप पृ. १४६)
इससे स्पष्ट है कि ‘तवाणं’ पद मूल में नहीं है। टीकाकारों ने भी नहीं माना है।
(३) ऐसे ‘‘कीरंतं पि ण समणुमणामि’’ पाठ के स्थान पर—
‘‘अण्णं करंतं पि ण समणुमणामि’’ पाठ श्री गौतमस्वामी की कृति में सुधारना सर्वथा अनुचित है।
(४) इसी प्रकार—
‘‘वंदामि रिट्ठणेिंम’’ पाठ ही थोस्सामि स्तव में सर्वत्र मान्य है।
श्रमणचर्या के प्रथम संस्करण में—
‘वंदाम्यरिट्ठणेमिं’ किया है, पुन: द्वितीय संस्करण में ‘‘वंदे अरिट्ठणेिंम’’ किया है।
इस परिवर्तन पाठ को पढ़ना उचित नहीं है।
(५) सामायिक भाष्य में चैत्यभक्ति की अंचलिका की टीका में देखिए—
‘‘अंचेमि अर्चामि। पूजेमि पूजयामि। वंदामि स्तौमि। णमंसामि नमस्यामि प्रणिपतामि।’’ (सामायिक भाष्य पृ. १७५)
टीकाकार ने भी प्राचीन पाठ ही लिया ‘अंचेमि’ आदि। अत:—
श्रमणचर्या में पृ. १०२ पर—
‘‘अच्चेमि पुज्जेमि वंदामि णमस्सामि।’’ पाठ सुधारना कहाँ तक उचित है।
(६) इसी तरह ‘‘सल्लेहणामरणं’’ के अनंतर ‘‘तिदियं अब्भोवस्साणं चेदि’’ पाठ हटाकर ‘‘इच्चेदाणि चत्तारि सिक्खावदाणि’’ बढ़ाना उचित नहीं है। मूल पाठ जो ‘क्रियाकलाप’ आदि ग्रंथों में चला आ रहा है, उसे ही पढ़ना चाहिये।
(७) ‘जो एदाइं वदाइं धरेइ सावया सावियाओ वा खुड्ढय खुड्ढियाओ वा अट्ठदहभवण-वासिय-वाणविंतरजोइसियसोहम्मीसाणदेवीओ वदिक्कमित्तउवरिम-अण्णदर-महड्ढियासु देवेसु उववज्जंति।’
जो श्रावक या श्राविका अथवा क्षुल्लक या क्षुल्लिका इन उपर्युक्त बारह व्रतों को या ग्यारह प्रतिमाओं को धारण करते हैं वे अठारह स्थान को, भवनवासी, वान व्यंतर, ज्योतिषी और सौधर्म—ईशान स्वर्ग की देवियों को छोड़कर ऊपर के स्वर्गों में से किसी भी स्वर्ग में महर्द्धिक देवों में उत्पन्न होते हैं।
सन् १९५८ में एक विद्वान ने कहा कि ‘अट्ठदह’ पाठ का अर्थ समझ में नहीं आता है अत: इसके स्थान में ‘णट्ठदेहा’ पाठ हो सकता है।’
कुछ पुस्तकों में उन्होंने ऐसा संशोधन करा दिया किन्तु उनसे कहा गया कि—पंडित जी! श्रावक-श्राविका और क्षुल्लक-क्षुल्लिका ‘नष्टदेहा:’—देहरहित तो होते नहीं हैं अत: यह संशोधन मुझे संगत नहीं लगता है। चर्चा के प्रसंग में ऐसी बात आई—
‘अठारह स्थान ऐसे ढूंढने चाहिये जहाँ व्रती नहीं जाता हो तथा उन अठारह स्थानों में ये भवनत्रिक और सौधर्म-ईशान की देवियाँ नहीं आनी चाहिए चूँकि इन्हें पृथक् से लिया है। तभी उमास्वामी श्रावकाचार के दो श्लोक स्मृतिपथ में आ गये, वे ये हैं—
सम्यक्त्वसंयुत: प्राणी, मिथ्यावासेन जायते।
द्वादशेषु च तिर्यक्षु, नारकेषु नपुँसके।।८८।।
स्त्रीत्वे च दुष्कृताल्पायु-दारिद्य्रादिकवर्जित:।
भवनत्रिषु षट्भूषु, तद्देवीषु न जायते।।८९।।
सम्यक्त्व से सहित जीव मिथ्यात्व के निम्न स्थानों में नहीं जाता है—
१. पृथ्वीकायिक
२. जलकायिक
३. अग्निकायिक
४. वायुकायिक
५. वनस्पतिकायिक
६. दो इंद्रिय
७. तीन इंद्रिय
८.चार इंद्रिय
९. निगोद
१०. असंज्ञीपंचेन्द्रिय
११. कुभोगभूमि और
१२. म्लेच्छखंड,
मिथ्यात्व के इन बारह स्थानों में उत्पन्न नहीं होता है तथा
१३. तिर्यचों में
१४. नरकों में
१५. नपुंसक में और
१६. स्त्रीवेद में उत्पन्न नहीं होता है।
पुन: पापी, अल्पायु, दारिद्रादि से वर्जित रहता है। यह सम्यग्दृष्टी भवनत्रिकों में, प्रथम नरक से अतिरिक्त छह नरकभूमियों में व स्वर्ग की देवियों में भी नहीं जाता है।
चर्चा में यह बात और आई कि यहाँ प्रतिक्रमण में तो व्रतिक श्रावकों के लिए कथन है अत: व्रतीजन तो सुभोगभूमि और मनुष्य पर्याय में भी नहीं जाते हैं क्योंकि गाथा है कि—
अणुवदमहव्वदाइं ण लहइ देवाउगं मोत्तुं। (गोम्मटसार कर्मकांड)
अणुव्रती और महाव्रती तो देवायु के सिवाय अन्य किसी आयु का बंध ही नहीं कर सकता है इसलिये उपर्युक्त
१६ स्थानों में,
१७. सुभोगभूमि और
१८. मनुष्य।
इन दो स्थानों को मिला देने से अठारह स्थान हो जाते हैं। व्रतिक व क्षुल्लक-क्षुल्लिका इनमें नहीं जाते हैं।
ये अठारह स्थान आचार्य श्री शिवसागरजी महाराज को भी बहुत ही संगत प्रतीत हुये थे। तब विद्वान द्वारा संशोधित पाठ ‘णट्ठदेहा’ हटा दिया गया था।
उसके बाद वह चर्चा वहीं समाप्त हो गई थी।
कुछ दिन पूर्व श्रमणचर्या में ‘अट्ठदह’ पाठ को उलट कर ‘दहअट्ठ’ पाठ लिया गया जिसका अर्थ यह निकाला गया-‘दश प्रकार के भवनवासी और आठ प्रकार के वानव्यंतर। पुन: ‘श्रमणचर्या’ में छपा है—‘दह-अट्ठ-पंच’ जिसे भवनवासी, वानव्यंतर और ज्योतिषी देवों के भेदरूप से माना गया।
जो भी हो मेरी विचारधारा तो यही है कि यदि कुछ पाठ संशोधित भी करना है तो पुराने विद्वानों के समान उस मूलपाठ को न हटाकर टिप्पण में ‘संभावित है’ ऐसा लिखकर उसे देना चाहिए।
ऐसे ही एक पाठ परिवर्तन और है जो कि अतीव विचारणीय है—मूल पाठ है-‘से अभिमदजीवाजीव-उवलद्धपुण्णपाव-आसवसंवरणिज्जरबंधमोक्खमहिकुसले।’
अब इसे बदल कर ऐसा पाठ रखा गया है—‘से अभिमदजीवाजीवउवलद्ध-पुण्णपावआसवबंध-संवरणिज्जरमोक्खमहिकुसले।’
मूलपाठ में नव तत्त्वों का क्रम यह था-जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आस्रव, संवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष।
परिवर्तित पाठ का क्रम ऐसा हो गया है जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आस्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष।
विचार करने से यह समझ में आता है कि—इस मूलपाठ के क्रम के अनुसार ही कुंंदकुंददेव ने समयसार में गाथा रखी है—
भूयत्थेणाभिगदा जीवाजीवा य पुण्णपावं च।
आसवसंवरणिज्जरबंधो मोक्खो य सम्मत्तं।।१३।।
और इसी गाथा के क्रम के अनुसार ही श्रीकुंदकुंददेव ने समयसार में अधिकार विभक्त किये हैं। जीवाजीवाधिकार के बाद पुण्य-पापाधिकार है पुन: आस्रव अधिकार, संवर अधिकार, निर्जरा अधिकार लेकर तब बंध अधिकार है इसके बाद मोक्ष अधिकार है।
(८) क्रियाकलाप पृ. श्रमणचर्या पृ.
देवा वि तस्स पणमंति ६६ देवा वि तं णमंसंति ४०
प्रतिक्रमणग्रंथत्रयी में टीकाकार ने यही क्रियाकलाप वाला पाठ रखकर इसी की टीका की है। जैसे—
‘‘देवा वि तस्स पणमंति-देवा अपि तस्य प्रणमंति।’’ इस प्रकार अनेक संशोधन वर्तमान में किये जा रहे हैं किन्तु विचार करने की बात है कि इन टीकाकार श्री प्रभाचंद्राचार्य तक तो यह प्राचीन पाठ ही प्रमाणभूत माना गया है और श्रीटीकाकार भी प्राकृत-संस्कृत व्याकरण व छंद शास्त्रादि के ज्ञाता अवश्य थे फिर भी उन्होंने यह पाठ नहीं बदला है। आजकल ऐसे ही अनेक संशोधन हुये हैं जो कि हमें इष्ट नहीं हैं।