स्याद्वाद चन्द्रिका :- टीका का स्वरूप
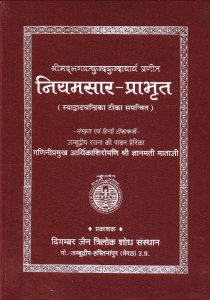
पू० ज्ञानमती माता टीका क्षेत्र की सिद्धहस्त लेखिका हैं। उनके द्वारा रचित यह टीका नियमसार के हार्द खोलने हेतु समर्थ टीका है। किसी भी ग्रन्थ की टीका हेतु जितनी योग्यतायें अपेक्षित है उनका सामावेष प्रस्तुत कृति में पाया जाता है। आचार्य जयसेन स्वामी ने समयसार, प्रवचनसार, पंचास्तिकाय ग्रन्थों की तात्पर्यवृत्ति टीकाओं में एवं ब्रहादेव सूरि ने परमात्मप्रकाष एवं बृहद्द्रव्य संग्रह में जो टीका नैपुण्य समाहित किया है वही रूप माता जी ने प्रस्तुत किया है इसे वृत्ति रूप संज्ञा देना अनुचित न होगा।
आ० पद्मप्रभ कृत नियमसार की टीका को भी वृत्ति संज्ञा है किन्तु वह सामान्य रूप से तात्पर्य को, भावार्थ को प्रस्तुत करने रूप है। अतः वह अध्यात्म की प्रखर प्रस्तुति होने पर भी सामान्य टीका ही कही जा सकती है। इससे भिन्न पू० आर्यिका ज्ञानमती कृत स्याद्वाद चन्द्रिका विषेश वर्णन करती है।
नियमसार के मूल में गुप्त अथवा समाविश्ट अभीश्ट तत्वों केा स्पश्ट करने मे यह समर्थ है। आगे तुलना में यह स्पश्ट करेंगे। स्याद्वाद चन्द्रिका में ‘ट्खण्डागम की प्रष्नोत्तर परक शैली तथा सिद्धान्त प्रस्तुतीकरण शैली के दर्षन भी होते हैं। माता जी सिद्धान्त के गूढ़ रहस्यों को सामान्यजनों को अवगत कराने में रूचिवान् प्रतीत होती हैं। टीका के पारायण से ही इसके समग्र रूप से गुणों का परिज्ञान हो सकता है। यहाँ हम निम्न टीकांष और उसका हिन्दी अनुवाद पाठकों हेतु उद्धृत करते हैं। उत्थानिका एवं मूल गाथा भी प्रस्तुत है।
”कस्य क्रियाऽवष्यकननाम्ना कथ्यते किंच तस्य कार्यमित्याषंकायामाचार्य देवा ब्रुवन्ति -‘जो ण हवदि अण्णवसो तस्स दु कम्मं भणंति आवासं। कम्मविणासणजोगो णिव्वुदिमग्गो ति पिज्जुत्तो’।।141।।
”जो अण्णवसो ण हवदि पिच्छिकमण्डलुमात्रसहितो यो महातपोधनोऽन्येशां पचेन्द्रियविशयाणं कशायाणां च वषे न भवति स एवानन्यवष तस्स दु कम्मं आवासं भणन्ति तस्य महामुनेस्तु कर्मक्रियाप्रवृत्तिष्च आवष्यकमिति भणन्ति।
के ते भणन्ति ? श्री गौतम प्रभृतिगणधरदेवा। पुनः इदमावष्यकं किं करोति ? कम्मविणासणजोगा णिव्वुदिमग्गो कर्मणां।
विनाषने क्षमो यः कष्चिद् योगो मनोवाक्कायप्रवृतिः परमसमा- धिलक्षणनिर्विकल्पध्यानं वा स एव निवृत्ति मार्गो मोक्षप्राप्त्युपायो भवति।
इमाष्च व्यवहारक्रियाभिः साध्या निष्चयावष्यकक्रिया एवं कर्मविनाषन कुषलास्ततो मोक्षमार्गोऽपि ता एव। ‘त्ति पिज्जुत्तो’ इत्यनेन प्रकारेण गणधरादिदेवै प्ररूपितो न च रथ्यापुरुशः।
इतो विस्तरः – अहोरात्रं साधुभिरवष्यमेव कत्र्तव्याः याः काष्चित् क्रियास्ताः एवावष्यक क्रियाः कथ्यन्ते।
इमाः ‘शट्प्रकाराः भवन्ति।
उक्तं च मूलाचारे –
सामाइय चउवीसत्थव वंदणयं पडिक्कमणं।
पच्चक्खाणं च तहा काओसग्गो छवदि छठ्ठो।।
सर्वसत्वेशु समभावं धारयित्वा त्रिकालदेववन्दनाकरणं सामायिकक्रियाकृति- कर्मविधेरन्तर्गतचतुर्विषतितीर्थकराणां “थोस्सामि” इत्यादिना स्तवनं स्तवक्रिया, देवश्रुतगुर्वादीनां जयति ‘भगवान् हेमाम्भोज’ इत्यादि वंदनकरणं वंदनाक्रिया,
दैवसिकरात्रिकादिसप्तविधप्रतिक्रमणे “जीवे प्रमादजनिताः” इत्यादिना तत्करणं प्रतिक्रमण क्रिया, प्रतिदिनमाहारानन्तरं चतुर्विधाहारस्तपोभावनयायस्यापि वस्तुनस्त्यागः प्रत्याख्यान क्रिया, तथा वीरभक्तिस्वाध्यायवन्दनादिक्रियाकरणे सप्तविंषत्या- द्युच्छ्वासगणनया महामन्त्रजपनं कायोत्सर्ग क्रिया। ‘
एतां व्यवहारावष्यकक्रिया यथासमयं विदधानस्य साधोर्मूलगुणैः साद्र्धमावष्यकापरिहाणिनामधेया भावनापि जायते या च तीर्थंकर प्रकृतिबन्धकारणभूता भवति।
तथापीमाः पचपरमेश्ठिश्रुततीर्थादीनाश्रित्य वत्र्ततेऽतएव क्रिया उच्यन्ते। किन्च,निष्चयक्रियाः सर्वथा स्वाश्रया एव भवन्ति।
इत्थमववुद्ध्यैदंयुगीनैः साधुभिरपि निष्चयपरमावष्यकसिद्धध्यर्थं स्वस्वपदानुसारेणा- वष्यकं कत्र्तव्यमेव”।।141।।
स्वोपज्ञ हिन्दी अनुवाद
किनकी क्रिया आवष्यक नाम से कहलाती है और उसका कार्य क्या है ? ऐसी आषंका होने पर आचार्य देव कहते हैं।
अन्वयार्थ
(जो अण्णवसो ण हवदि) जो अन्य के वंष में नहीं है, (तस्स दु कम्मं आवासं भणन्ति) उनकी क्रिया आवष्यक कही जाती है। (कम्मविणासण जोगो) कर्मका विनाष करने वाला जो योग है, (णिव्वुदिमग्गो त्ति पिज्जत्तो) वही निर्वाण का मार्ग है, ऐसा प्रतिपादित किया गया है। जो पिच्छी कमण्डलु मात्र परिकर सहित महातपोधन अन्य पन्चेन्द्रियों के विशय पर कशायों के वष में नहीं होते हैं, वे ही अन्य के वष नहीं है। उन महामुनि का कर्म, क्रिया और प्रवृत्ति आवष्यक इस नाम से कही जाती है।
“शंका– कौन ऐसा कहते हैं ?
समाधान– श्री गौतम स्वामी आदि गणधर देवां ने ऐसा कहा है।
“शंका– पुनः ये आवष्यक क्रियायें क्या करती है?
समाधान– कर्मो के विनाषन में समर्थ जो कोई योग अर्थात् मन-वचन- काय की प्रवृत्ति, अथवा परमसमाधि लक्षण निर्विकल्प ध्यान है, वही निर्वाणकार्य, मोक्ष की प्राप्ति का उपाय है और ये व्यवहार आवष्यक क्रियाओं से साध्य निष्चय आवष्यक क्रियायें ही कर्मविनाषन में कुषल हैं, इसलिए मोक्षमार्ग भी ये ही हैं। इस प्रकार से गणधर देव आदि ने प्ररुपण किया है न कि रास्ता चलते पुरुशों ने।
इसी प्रकार विस्तार करते हैं-अहोरात्र साधुओं के द्वारा अवष्य ही करने योग्य जो क्रियायें कहलाती हैं। ये छः प्रकार की होती हैं। मूलाचार में कहा है – सामायिक, चतुर्विंषतिस्तव, वन्दना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, कायोत्सर्ग ये छः क्रियायें हैं।
सभी जीवों में समता भाव धारण करके त्रिकाल देव वन्दना ‘सामायिक‘ क्रिया है। कृतिकर्म विधि के अन्तर्गत 24 तीर्थकरों की ‘‘थोस्सामि’’ इत्यादि रूप से ‘स्तवक्रिया’ है। देव, श्रुत, गुरु आदि का ‘जयतु’ भगवान् हेमाम्भोज’ इत्यादि पढ़ते हुए वन्दना करना वन्दना क्रिया है।
दैवसिक, रात्रिक, आदि सात प्रकार के प्रतिक्रमण में ‘जीवे प्रमादजनिता‘ इत्यादि रुप से पाठ का करना ‘प्रतिक्रमण’ क्रिया है। प्रतिदिन आहार के अनन्तर चतुर्विध आहार का त्याग करना और तप की भावना से अन्य भी वस्तु का त्याग करना ‘प्रत्याख्यान’ क्रिया है तथा वीरभक्ति में, स्वाध्याय और वन्दना आदि क्रिया के करने में 27 उच्छ्वास की गणना से महामंत्र का जाप करना ‘कायोत्सर्ग’ क्रिया है।
इन व्यवहार आवष्यक क्रियायें को समय के अनुसार करने वाले साधु के मूलगुणों के साथ ‘‘आवष्यकापरिहाणि’’ नाम की भावना भी होती है, जो कि तीर्थकर प्रकृति के बन्ध में कारण भूत हो जाती है। फिर भी ये क्रियायें पंचपरमेश्ठी श्रुत और तीर्थ आदि के आश्रय से होती हैं। इसलिए ये
व्यवहार क्रियायें कहलाती हैं क्योंकि निष्चय क्रियायें सर्वथा अपनी आत्मा के आश्रित ही होती हैं। ऐसा जानकर आजकल के साधुओं को भी निष्चयपरमआवष्यक की सिद्धि के लिए अपने पद के अनुसार आवष्यक क्रियायें करते ही रहना चाहिए।’’
टीका के स्वरूप को उक्त उदाहरण से सामान्य रुप से हृदयंगम किया जा सकता है। कहीं इसमें संक्षेप शैली के, किन्हीं स्थालों पर मध्यम शैली के तथा यत्र कुत्र अपेक्षित विस्तार के दर्षन होते है। कहीं विषेश वर्णन से दीर्घ विस्तृत है।
स्याद्वाद चन्द्रिका में खण्डान्वय (पदखण्डना रूप) और दण्डान्वय (सम्पूर्ण पद के अन्वय रूप) पद्धति यथा आवष्यक अपनाई गई है। किन्हीं स्थलों पर करने हेतु शब्दार्थ, लक्षण, व्युत्पत्ति आदि समाविश्ट किये गये हैं। किन्ही स्थलों पर संस्कृत छाया सान्वय करते हुए उसके “ाब्दार्थ मात्र को सरल रीत्या स्पश्ट किया गया है।
अन्यत्र शब्दों की विषेश व्याख्या कर विशय को सुबोध किया गया है। संस्कृत छाया सर्वत्र ही दृश्टिगोचर होती है। इस प्रकार प्रक्रिया के पष्चात् ‘इतो विस्तर’ इत्यादि पद से टीका अपने अपेक्षित सभी गुणों के साथ लिखी गई है। यह आगम सिद्धान्त और अध्यात्म के उपयोगी सभी पाष्र्वों का स्पर्ष करती है।
स्याद्वाद चन्द्रिका को व्याकरण सम्मत शैली से युक्त एवं शब्दार्थ के विषेश रूप युक्त कहा जा सकता है। निम्न स्थल दृश्टव्य है।
णमिऊण जिणं वीरं अणंतवरणाणदंसणसहावं
वोच्छामि णियमसारं केवलि सुद केवली भणिदं ।। 1 ।।
टीका – णमिऊण इत्यादि पदखण्डनारूपेण व्याख्यानं क्रियते। णमिऊण नत्वा। कं ? वीरं-अन्तिमतीर्थšरं।
कथम्भूतं जिणं-जिनं पुनरपि कथं अणंतवरणाणदंसणसहावं, अनन्तवरज्ञानदर्षनस्वभावं एवं पूर्वाद्धेन नमस्कारं कृत्वा अपराद्र्धेन प्रतिज्ञां कुर्वन्ति। वोच्छामि-वक्ष्यामि।
कं ? णियमसारं-नियमसारं। कथम्भूतं ? केवली भणिदं-‘केवलीश्रुतकेवलीभणित’ इति क्रिया कारक सम्बन्धः।
एक अन्य स्थल पर दृश्टिपात करणीय है।
चलमलिणमगाढत्त विवज्जिय सद्दहणमेव सम्मत्तं।
अधिगमभावो णाणं हेयोपादेय तच्चाणं ।। 52।।
टीका- ‘चलमलिनमगाढत्त विवज्जिय सट्टहणमेव सम्मत्तं’ चलमलिनगाढत्व- विवर्जितश्रद्धान एव सम्यक्त्वं चलमलिनागाढ दोशै रहितमेव श्रद्धान एव सम्यक्त्वं- चलमलिनागाढ दोशै रहितमेव श्रद्धानं सम्यक्त्वं ‘हेयोपादेय तच्चाणं अधिगम भावो णाणं’ हेयोपादेय तत्वानामधिगमभावो ज्ञानमिति।
अन्वयार्थ के पष्चात ”इतो विस्तर“, ”तद्यथा“ “शब्द से प्रारम्भ करके विस्तार रूप व्याख्यान किया गया है। जैसे कदलीपत्र के अन्तर्गत पत्र पर पत्र निकलते जाते हैं। उसी प्रकार इसमें विषेशता के साथ अर्थ पर अर्थ निकलते जाते दृश्टिगत होते हैं। अर्थ को पुश्ट करने हेतु दृश्टान्तों एवं उदाहरणों का उपयोग भरपूर किया गया है। उपरोक्त गाथा की विस्तृत टीका दृश्टव्य है,
इतो विस्तर :- यथा एकमेव जलं नानाकल्लोलरूपेण परिणमति तथैव सर्वतीर्थकराणामहर्तां वा समानानन्तषक्तौ सत्यामापि शन्तिजिनेष्वरः शन्तिं करोति पाष्र्वनाथष्च कश्टं निवारयति नानाविशयेशु चलः चंचलः परिणामः स एव चलदोशः।
यथा शुद्धोऽपि स्वर्णः मलसंसर्गेण मलिनमुच्यते तथैव शकादिदोशेशु अन्यतमदोशेण पूर्णं निर्मलत्वं अस्ति स मलदोशो निगद्यते यथा वृद्धपुरुशस्य हस्तगतं दण्ड कम्पते तथैव स्वनिर्मापितजिनमन्दिरे ममेदं परनिर्मापिते च परस्येदं इति भाव अगाढदोशः कथ्यते एतच्चलमलिनागाढदौशै रहितं यत् श्रद्धानं तत् निर्दोश सम्यग्दर्षनमुच्यते।
विस्तृत व्याख्यान के पष्चात अभिप्राय भावार्थ या तात्पर्य प्रस्तुत किया गया है। इसमें स्पश्ट मार्गदर्षन झलकता है। क्या करणीय है, अकरणीय है भावार्थ में सार रूप में निर्दिश्ट किया गया है।
- उदाहरणार्थ 1- गाथा क्रमांक 25 की टीका का अन्तिम पद ‘एतज्ज्ञात्वा ज्ञानदर्षन-गुणप्रधाने निजषुद्धात्मन्येव रुचिः कर्तव्या इति।’
- 2- एतज्ज्ञात्वा शुद्धनयेन स्वं पर्यायष्च शुद्धमेवेति श्रद्दधानः शुद्धसिद्ध परमात्मनो भक्तिं प्रकुर्वाणष्च व्यवहारनयेन निजात्मा पवित्री कर्तव्यः।
- अर्थ–1– यह जानकर ज्ञानदर्षन प्रधान निजषुद्धात्मा में ही रुचि करना चाहिए।
- 2- यह जानकर शुद्धनय से अपनी आत्मा व पर्याय शुद्ध ही है ऐसा श्रद्धान करते हुऐ शुद्ध सिद्ध परमात्मा की भक्ति करते हुए व्यवहार नय से अपनी आत्मा को पवित्र करना चाहिये।
स्याद्वाद चन्द्रिका में परम्परावादिता पूर्णरूपेण प्रकट होती है। माता जी आर्श परम्परा की दृढ़ श्रद्धानी है। उन्होंने प्रस्तुत स्याद्वाद चन्द्रिका में आगमिक शब्दों का प्रयोग भरपूर किया है।
पू० माता जी का कथनकौषल प्रस्तुत कृति में प्रौढ़ता को प्राप्त हुआ है। विशय को सुबोध और रुचिकर बनाने हेतु उनका प्रयास रहा है कि छोटे छोटे पद और वाक्य प्रयुक्त हों परन्तु आवष्यकता का अनुभव कर उन्होंने सामान्य समासित पदों का भी प्रयोग किया है। विभक्तियों के होने वाले विस्तार से बचने हेतु उन्होंने सन्धियुक्त पदों को आवष्यकतानुसार स्थान दिया है। इससे टीका का आकर्शक सौन्दर्य प्रकट किया है। एक स्थल पर गौर करें।
”षुद्धबुद्धनित्यनिरजनज्ञानदर्षनसुखवीर्यगुणमणितनिजपरमात्मतत्त्वसम्यक्श्रद्धानज्ञानानुचरणरूपनिष्चयरत्नत्रयपरिणतपरमसमाधौ
इस टीका में दीर्घवाक्यों की आवली भी दृश्टव्य है। कतिपय वाक्य तो आ० पद्मप्रभ की तात्पर्यवृत्तिगत वाक्यों से भी लम्बे हैं,
उदाहारणार्थ
वचनरचनारूपद्रव्यप्रतिक्रमणविवर्जितरागादिभावरहितव्रतविराधनारहितचतुर्विधाराधनासहितस्वषुद्धात्माराधनापरिण
तानाचारविवर्जितयत्याचारपरिणतोन्मार्गरहितजिनमार्गस्थितत्रिषल्यविवर्जितनिः “शल्यभावास्थितागुप्तिस्वरूपोऽहम्।
किसी भी ग्रन्थ की टीका में सर्वप्रथम शब्दार्थ का अति महत्व है। शब्दार्थ ज्ञान करके ही तद् विशय को हृदयंगम करने की येाग्यता आती है। किसी शब्द का मात्र अर्थ जैसे पद्मप्रभ कमल ही पर्याप्त नही होता अपितु उस शब्द की परिभाशा लक्षण, निरुक्ति व्युत्पत्ति आदि भी आवष्यक तत्व है।
विषेश तोर से टीका क्षेत्र में स्याद्वाद चन्द्रिका में यह सर्वत्र ध्यान दिया गया है कि पाठक को शब्द का पारायण करते समय ही उस शब्द के वाच्य का चित्र भी उसके समक्ष प्रकट हो जाये। इससे शब्द की वाचक शक्ति का मूल्य भी प्रकट होता है। संस्कृतच्छाया करके शब्द को व्याख्यायित किया गया है।
असरीरा अविणासा अणिंदिया णिम्मला विसुद्धा।
जह लोयग्गे सिद्धा तह जीवा संसिदी णेया ।।गाथा-48।।
‘जह लोयग्गेसिद्धा तह संसिदी जीवा णेया’ – यथा लोकाग्रे सिद्धा राजन्ते तथा संसृतौ संसारे जीवाः ज्ञेयाः संसारिणो जीवाः ज्ञातव्या इति। कथम्भूतास्ते सिद्धाः असरीरा अषरीराः औदारिकादिपचविध“शरीररहिता ज्ञान“शरीराष्च पुनः कथम्भूताः ?
अविणासा-अविनाषाः, अविनष्वराः नरनरकादि रूपेण जन्ममरणाभावात् शष्वताः नित्याः।
पुनरपि कथम्भूताः ? अण्ंिदिया-अनिन्द्रियाः अतीन्द्रियाः वा क्षायोपषमिक- जन्यभावेन्द्रियाभावात् आत्मोत्थसकलविमलकेवलज्ञानदर्षनलोचनाभ्यां युगपत् लोकालोकव्यापिसकलपदार्थावलोकनसमर्था अतीन्द्रियाः।
आर्यिका ज्ञानमती किसी भी विशय का संक्षेप, मध्यम एवं विस्तार रूप से व्याख्यान करने में पटु हैं। चारों अनुयोगों में निश्णात होने, भाशा पर अधिकार रखने, भाशा विज्ञान के ज्ञाता होने, प्रस्तुतीकरण की अदभुत क्षमता होने से उनकी लेखनी निर्बाध गति से चलती है। भाव विषुद्धि अर्थात चारित्र के द्वारा हृदय की निर्मल परिणति भी इसका कारण है।
स्याद्वाद चन्द्रिका में गाथा क्रमांक 187 की टीका एवं समापन विशयक विवेचन एवं अपनी स्थति का प्रकाषन आदि का सांगोपोग वर्णन 17 पृश्ठों में किया गया है। गाथा के हार्द को खेालने हेतु प्रायः सभी सम्बन्धित विशयों को इसमे समाहित किया गया है। इसी प्रकार गाथा संख्या 175 की 10 पृश्ठों में व्याख्या की गई है अन्य भी अनेक अति विस्तार के निरूपण पाये जाते हैं।
विषेशता यह है कि आगम के श्रद्धालु व्यक्ति को इसमें कही एक शब्द भी अनर्थक ज्ञात नही होता है। नियमसार मुख्य रूप से द्रव्यानुयोग का ग्रन्थ है अतः रुचिवान पाठक इसमें अति आनन्द का अनुभव करता है। गाथा क्रमांक 187 की टीका में निम्न प्रस्तुत अंष कुन्कुन्द स्वामी के व्यक्तित्व विशयक निश्कर्श है जो अवष्य ही ध्यान देने योग्य है। इससे यह विदित होता है कि टीका का विस्तार किस पद्धति से माता जी ने किया है।
अनेन निष्चीयते यद् इमे आचार्याः ‘ाड्मुहूत्र्तादधिकमपि कालं युगपद् ग्रन्थरचनां चक्रुः।
तथा च ‘ाश्ठसप्तमगुणस्थानयोः कालमन्तमुहूर्तमेवातो ग्रन्थलेखनकुर्वता सतामेशां सूरीणां स्वात्मामिमुखसंवित्तिलक्षणनिज“शुद्धात्मतत्वस्य सविकल्पध्यानं भवन्नासीत्, न च सातिषयाप्रमत्त-योग्यं निर्विकल्पध्यानं।
तत एते महाचार्या अपि अध्यात्मस्वरूप- निजतत्व भावनां भावयन्तः सन्त एवासीत्।
अद्यत्वेऽपि चारित्रक्रियाकुषला केचिद् जिनमुद्राधराः मुनिवराः संघसंचालनपरा अपि निर्विकल्पसमाधिध्येयरूपां कृत्वा निजषुद्धत्मतत्त्वं भावयन्ति अग्रे दुश्शमकालान्तं भावयिश्यन्त्येव।“
अर्थ-इससे यह निष्चय होता है। कि ये आचार्य छः मुहूर्त से अधिक काल तक भी एक साथ ग्रन्थ रचना करते होगें और छठे सातवें गुणस्थान का काल अन्तर्मुहूर्त मात्र ही है। इसलिए ग्रन्थ लिखते हुए भी इन आचार्य को अपने आत्मा के अभिमुख होने से हुआ स्वसंवेदन लक्षण निज शुद्धात्मतत्व का सविकल्प ध्यान होता ही रहता था किन्तु इन्हें भी सातिषय अवस्था के योग्य निर्विकल्प ध्यान नहीं होता था।
इसलिए ये महान् आचार्य भी अध्यात्मस्वरूप निज आत्मतत्व को ही भाते रहते थे। आज भी चारित्र और क्रियाओं मे कुषल कोई जिनमुद्राधारी मुनिराज संघ संचालन मे तत्पर रहते हुए भी निर्विकल्प समाधि को ध्येय रूप करके निज शुद्ध आत्मतत्व की भावना करते रहते हैं और आगे पंचम काल के अन्त तक करते रहेंगे।
स्पश्टीकरण
स्याद्वाद चन्द्रिका में विशय का स्पश्टीकरण अति सुन्दर रूप से हुआ है। विशय के अन्तस्तत्व को खोलने हेतु पाँच प्रकार के अर्थ की आवष्यकता होती है।
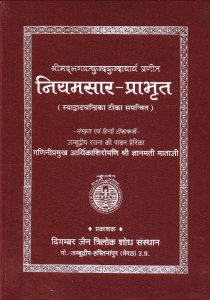
1. “शब्दार्थ,
2. नयार्थ,
3. मतार्थ,
4. आगमार्थ,
5. भावार्थ
प्रस्तुत कृति में प्राय सर्वत्र यह ध्यान रखा गया है उपरोक्त सभी पाँचों अर्थों का नामोल्लेख सर्वत्र न होने पर भी उनके दर्षन हमें सामान्यतः सर्वत्र होते हैं। कहीं कहीं विषेश रूप से इन पाँचों के द्धारा ही कथन किया गया है। गाथा क्रमांक 4 में यह बात स्पश्ट रूप से झलकती है।
प्रस्तुत गाथा के अपेक्षित शब्द मोक्ष का भाव एवं द्रव्य मोक्ष सहित अर्थ करके पुनः नयार्थ प्रस्तुत किया गया है। व्यवहार नय से क्षीण कशायी मुनि के अंतिम समय का परिणाम मोक्ष हेतु है तथा निष्चय नय से अयोग केवली का अंतिम समयवर्ती परिणाम (रत्नत्र्ाय) मुक्ति का हेतु, यह निरूपित किया है। अनन्तर आ० अकलंक देव, आ० विद्यानन्द, आ० अमृतचन्द्र सूरि के उदाहरणों द्धारा आगमार्थ प्रस्तुत किया है। पुनः निम्न वाक्य में मतार्थ भी प्रस्तुत किया है।
”किच ये केचिद् श्रद्धानषून्या रत्नत्रयमध्ये केनचिदेकेन द्वाभ्यां वामार्गो मन्यन्ते ते मिथ्यादृश्टयः ………………….।“
टीका के अन्त में तात्पर्यमेतत् कथन द्वारा सारांष (भावार्थ) प्रस्तुत किया है। इस प्रकार स्पश्टीकरण की आकर्शक शैली के दर्षन स्याद्वाद चन्द्रिका मे होते हैं। पूरे ग्रन्थ का पारायण सम्यक्रीत्या सामथ्र्य होने से स्वयं अथवा किन्ही विज्ञजनों के मार्र्गदर्षन में किया जावे तो भलीभाँति ज्ञानार्जन हो सकता है।
टीकागत विषेशताओं को दृश्टिगत कर यहाँ हम प्रस्तुत प्रकाषित टीका की प्रस्तावना में डा० लालबहादुर “शस्त्री के शब्दों को उद्धृत करने का लोभ सवंरण नहीं कर पा रहें हैं इनसे इस टीका पर गौरवमय प्रकाष पड़ता है।
”मूलग्रन्थ की अपेक्षा उसकी टीका करने में टीकाकार को जो श्रम, अनुसन्धान, शब्द और अर्थ की संगति और तात्पर्य की ओर ध्यान देना पड़ता है वह अत्यन्त कश्ट साध्य है। इसमं संस्कृत टीका करना तो और भी कठिन है वहाँ प्रत्येक शब्द की व्युत्पत्ति का ध्यान रखना पड़ता है साथ ही मूलग्रन्थ के रचयिता के अभिप्रायों को टटोलना पड़ता है ग्रन्थान्तरों के उद्धरण भी खेाजने पड़ते है। स्याद्वाद चन्द्रिका टीका को देखकर लगता है कि पूज्य माता जी ने इसमें कठोर श्रम किया है।
टीका में वे सभी बातें है जो प्रबुद्ध टीकाकार को स्मरण रखना चाहिये टीका की विषेशता है कि खण्डान्वय और दण्डान्वय को लेकर पहले तो सामान्य अर्थ किया गया है बाद में उसी गाथा का विस्तार से अर्थ किया है। प्रत्येक शब्द की व्याकरण सम्मत व्युत्पत्ति दी गई है। अर्थ के समर्थन में ग्रन्थान्तरों के प्रमाण दिये गये हैं। टीका की भाशा शैली भी प्राचीन आचार्यों जैसी ही है।
आर्यिका ज्ञानमती जी ही एक ऐसी महिला है जिन्होंने नियमसार की संस्कृत टीका लिखकर नारी जगत को एक महान उच्चासन पर बैठा दिया है यदि इस टीका को नारी के मस्तक का टीका कहा जाय तो कोई अत्युक्ति न होगी।“
स्याद्वाद चन्द्रिका व्याकरण सम्मत टीका है। अब तक कई विद्धानों ने इस टीका का पारायण किया है। यह समीक्षाओं से भी प्रकाषित हुई है वे समीक्षायंे प्रषंसात्मक ही है। स्वयं माता जी व्याकरण पटु हैं कातन्त्र की तो वे विषिश्ट ज्ञाता हैं। उसका तो उन्होंने अनेकों बार अध्यापन भी किया है अतः व्याकरण विशयक स्खलन का तो कोई प्रष्न ही नही हैं।
सन्धि, समास, विभक्ति, रूप, लिंग, कारक, वचन आदि सभी पक्षों की समरसता शद्धता सर्वत्र दृश्टिगोचर होती है। कहीं से व्याकरण विशयक कोई प्रकाषन-उपरान्त संषोधन अद्यावद्यि प्रस्तावित नहीं किया गया है। पाठक टीका के पारायण से व्याकरण सौश्ठव का अनुभव कर सकते हैं।
टीका में स्वरचित “लोक जो मंगलाचरण एवं प्रषास्ति के अन्तर्गत माता जी ने लिखे है वे उनके काव्य रचना कौषल को प्रकट करते हैं। टीका के प्रारम्भ में प्रथम मंगल “लोक से काव्य की निर्दाशता का दर्षन करें, रसास्वादन करें ।
वन्दे वागीष्वरीं नित्यं जिनवक्त्राब्जनिर्गताम्।
”वाक“दध्यै नयसिदध्ये च स्याद्वादामृतगर्भिणीम्।।2।।
मैं स्याद्वाद रूपी अमृत से गर्भित जिनेन्द्र देव के मुख कमल से निकली हुई वागीष्वरी नामक सरस्वती देवी की अपने वचनों की “शुद्धि एवं नयसिद्धि हेतु वन्दना करती हूँ।
यह “लोक तो उनके ग्रन्थ की निर्दोशता अर्थात वाक्यों की “शुद्धि और नय (सम्यक्नय)की सिद्धि को मानों प्रतीक ही है। प्रारम्भ में ही उन्होंने जो यह भाव व्यक्त किया है वह उनके शुद्धि संकल्प एवं प्रयत्न तथा नय सिद्धि की कामना का द्योतक है। उन्हें इसमें सफलता भी प्राप्त हुई। प्रषस्ति का भी एक “लोक उनकी निर्दोश काव्य रचना के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत करना चाहूँगा।
येशां चित्तस्य च प्राप्तेऽनुकूलत्वेऽलिखं कृतिम्।
वाह्यानां प्रतिकूलत्वं नैकान्तेन हि बाधते । प्रषस्ति-19।।
(जिनकी) संघस्थों की और अपने चित्त की अनुकूलता के प्राप्त होने पर मैंने यह कृति (टीका) लिखी है, क्योंकि बाह्य लोगों की या वाह्य वातावरण की प्रतिकूलता एकान्त से कार्य में बाधक नहीं है। अर्थात संघ की आर्यिका षिश्यवर्गों का आज्ञा पालन वैयावृत्ति आदि अनुकूलता रहने से लेखन कार्य आदि होते हैं। बाहर के लोग चाहे अनूकूल हो या निन्दा करते रहें उससे लेखन आदि कार्य में बाधा नहीं भी आती है।
व्युत्पत्ति वैभव
किसी भी वाचक पद के वाच्य को पूर्णरीत्या स्पश्ट करने के लिए व्युत्पत्ति का बहुत महत्व है। स्याद्वाद चन्द्रिका में व्युत्पत्तियाँ विषिश्ट रूप से टीकाकार ने समाहित की है। व्युत्पत्ति-लभ्यर्थ स्पश्ट हो जाने से पाठक भाव को सुश्ठु रूप से हृदयंगम कर लेता है यहाँ एक उदाहरण के माध्यम से व्युत्पत्ति कौषल को समझने का प्रयास करते हैं यथा,
वीर निम्न चार व्युत्पत्तियाँ दृश्टव्य हैं।
- 1- “वि” विषिश्टा ई लक्ष्मीः अन्तरंगानन्तचतुश्टयविभूतिबहिरंगसमवसरणादि रूपा च सम्पत्तिः, तां राति ददातीति वीरः।
- 2- (अथवा) विषिश्टेन ईरते सकलपदार्थसमूहं प्रत्यक्षीकरोतीति वीरः।
- 3- (अथवा) वरीयते “रयते विक्रामति कर्मारातीन् विजयते इति वीरः श्री वद्र्धमानः सन्मतिनाथोऽतिवीरो महति महावीर इति पचाभिधानैः प्रसिद्धःसिद्धार्थस्यात्मजः पष्चिमतीर्थšर इत्यर्थः।
- 4- (अथवा) ”कटपयपुरस्थवर्णैं नव नव पचाश्टकल्पितैः क्रमषः। स्वरनषून्यं संख्यामात्रोपरिमाक्षरं त्याज्यम्।” इति सूत्र नियमेन वकारेण चतुर ‘र’“ब्देन च द्यšस्तथा ‘अंकानां वामतो गतिः’ इति न्यायेन चतुर्विंषत्यंकेन (24) वृशभादि महावीर पर्यन्तचतुविंषति तीर्थकराणामपि ग्रहणं भवति।
सामान्य पाठकों के ज्ञानार्थ यहाँ हिन्दी अनुवाद प्रस्तुत है
वीर निम्न चार व्युत्पत्तियाँ दृश्टव्य हैं।
- 1- “वि” विषिश्ट ‘ई’ लक्ष्मी, अर्थात् अंतरंग अनंत चतुश्टय विभूति और बहिरंग समवसरण आदि संपत्ति यही विषिश्ट लक्ष्मी है इसको जोदेते हैं वे ‘वीर’ हैं।
- 2- अथवा जो विषेश रीति से ‘ईर्ते’ अर्थात जानते हैं। सम्पूर्ण पदार्थों को प्रत्यक्ष करते हैं वे वीर हैं।
- 3- अथवा वीरता करते हैं – विक्रमषील हैं अर्थात कर्म “शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते हैं वे वीर हैं। ये वीर भगवान श्री वद्र्धमान, सन्मति, अतिवीर और महति महावीर इन पाँचों से प्रसिद्ध श्री सिद्धार्थ महाराज के पुत्र अन्तिम तीर्थंकर हैं।
- 4- अथवा वीर शब्द का चैथा अर्थ करते हैं – ‘कटपय’ इत्यादि “लोक का अर्थ है क से झ तक अक्षरों में से क्रम से 1 आदि से 9 तक लेना। ट से भ तक भी क्रम से 1 से 9 तक लेना। प वर्ग से क्रमषः पाँच तक अंक लेना और या ‘य, र, ल, व, स, ह इन आठ से क्रमषः 8 तक अंक लेना। इस सूत्र के नियम से ‘वीर’ शब्द के वकार से 4 अंक और रकार से 2 अंक लेना।
तथा ‘अंकाना वामतो गतिः’ इस सूत्र के अनुसार अंकों को उलटे से लिखना होता है। इसलिए 24 अंक आ गया। वीर शब्द से इस 24 अंक से आदिनाथ से लेकर महावीर पर्यन्त 24 तीर्थंकरों का भी ग्रहण हो जाता है जिससे 24 तीर्थंकरों से को भी नमस्कार किया गया है।
यहाँ टीकाकत्र्री ने अत्यन्त कुषाग्र बुद्धि का परिचय दिया है। गोम्मटसार एवं उसकी केषववर्णी कृत टीका से उपयोगी अंष लेकर यहाँ गणित प्रकरण से जो व्युत्पत्ति दी गई है वह तथा अन्य तीन व्युत्पत्तियाँ उनकी अर्थ करने की सूझ-बूझ का प्रतिनिधित्व करतीं हैं। स्वर-व्यंजन रूप वर्ण अंक विद्या-अंक वर्ग का प्रतीकत्व कर सकते हैं तथा वर्ण (बीज), अथवा बीजाक्षरों में गणितीय तत्व अथवा अंकत्व समाहित हो सकता है इसका प्रकटीकरण माता जी ने इस स्थल पर कर अर्थ पद्वति का अतिषय प्रस्तुत किया है।
व्युत्पत्ति के विशय में वे आ० पप्रभ मलधारीदेव से आगे हैं। प्रकृत ‘वीर’ शब्द की उन्होंने मात्र दो व्युत्पत्तियाँ दी हैं। किन्तु माता जी ने 4 की संख्या में लिखी है। दोनों टीकाकारों की व्युत्पत्ति के संख्या के अंकों 2 व 4 को निकटस्थ करने से 24 संख्या निश्पन्न होती है। संयोग से वह 24 तीर्थंकरों का बहुमान प्रस्तुत करती है।
इसी प्रकार से अन्य भी व्युत्पत्तियों द्वारा अर्थ के प्रकटीकरण से टीका की जो समृद्धि हुई है वह पाठकों को पारायण से दृश्टिगत होगी। यहाँ तो संकेत मात्र एक उदाहरण दिया है। वस्तुतः यह टीका अर्थ के विहंगम स्वरूप को अपने अन्तस् में समाहित किये वर्तमान का एक चमत्कार ही है।
यहाँ व्युत्पत्तीकरण की व्यापकता का निम्न उदाहरण प्रस्तुत है जिससे टीका की विस्तृत अर्थता का सूचन होता है। मंगलाचरण की टीका में ‘जिन’ शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार की है,
”अनन्तभवप्रापणहेतून् समस्तमोहरागद्वेशादीन् जयतीति जिनः।”
अर्थात अनन्तभवों को प्राप्त कराने में कारणभूत समस्त मोह रागद्वेश को जो जीतते है वे जिन हैं।
इसके अनन्तर आचार्य पूज्यपाद कृत निम्न व्युत्पत्तिपरक “लोक उद्धृत कर मणिकांचन योग अवतरित कर दिया है।
जितमदहर्शद्वेशा जितमोहपरीशहा जितकशायाः।
जितजन्ममरणरोगाः जितमात्सर्याः जयन्तु जिनाः। (दषभक्ति)
समस्त विकारी भावों पर विजय प्राप्त कराने वाले जिन जयषील हो। यहाँ विषेश ध्यान देने योग्य है कि टीकाकत्र्री ने पाठकों के लिए आचार्यों की व्युत्पत्तियों को भी प्रासंगिकता के साथ उनके नाम से उद्धृत कर टीका को सुगम एवं सरल बना दिया।
सुगठित शब्दावली एवं पद-विन्यास की दृश्टि से भी यह कृति प्रषसंनीय है भाशा की दृश्टि मधुर से भी और आकर्शक है। प्रस्तुत शधालेख में अनेकों उदाहारणों के पारायणों से यह बात स्पश्टरीत्या दृश्टिगत की जा सकती है। विशय विस्तार के भय से यहाँ किन्ही अन्य अंष को प्रस्तुत नहीं कर पा रहा हूँ। टीका शैली सर्वत्र परिमार्जित भाशा सहित सरल एवं नियन्त्रित है। इसमें पूर्व कालीन आचार्यों की टीका शैली के दर्षन भी होते हैं। वस्तुतः यह समृद्ध टीका है।
डा० जय कुमार जैन मुजफ्फर नगर वालों की निम्न पंक्ति इस कृति की प्रषंसा में प्रस्तुत करना उचित ही होगा।
”स्याद्वाद चन्द्रिका जैन साध्वी द्वारा विरचित प्रथम संस्कृत टीका होते हुए भी अपनी सरलता, प्रासादिकता, प्रभावकता एवं प्रात्र्जलता के कारण संस्कृत टीका साहित्य में निष्चित ही महत्वपूर्ण पद पर प्रतिश्ठित होगी।“
