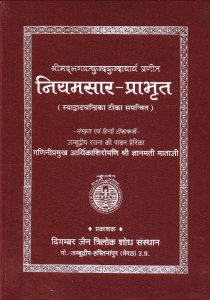स्याद्वाद चन्द्रिका में दार्षनिक दृश्टि
ज्ञानमती माता जी दर्षन विशयक अगाध ज्ञान की धनी है। जैन एवं जेनेतर सांख्य, बौद्ध, नैयायिक, वैषेशिक, मीमांसक और वेदान्त, चार्वाक आदि की मान्यताओं का स्पश्टीकरण स्याद्वाद चन्द्रिका में भी उन्होंने किया है। जैन धर्म का अध्यात्म उसकी न्याय अथवा दार्षनिक अकाट्य दृश्टि पर टिका हुआ है।
आ० कुन्दकुन्द के वाड्मय में निरूपित अध्यात्म को आ० समन्तभद्र देव, अकलंकदेव, विद्यानन्द, प्रभाचन्द्र और वादिराज आदि आचार्यों ने बल प्रदान कर उसे स्थायित्व रूप पद पर आसीन किया है तभी वह जैन-जैनेतर जनों में अपना प्रभाव जमा सका है।
दार्षनिक क्षेत्र में न्याय, तर्क, प्रमाण, हेतुविद्या, आन्वीक्षिकी आदि एकार्थ वाची हैं जो तत्त्वों के विशय-ज्ञान का प्रतिनिधित्व करते हैं। अर्थ का निर्णय करने हेतु न्याय अति आवष्यक है। इसमें प्रमाता, प्रमेय, प्रमाण, और प्रमाण का फल आदि का विस्तार से निरूपण किया जाता है।
प्रमाण के भेदों प्रत्यक्ष, परोक्ष, प्रत्यक्ष के भेदों परमार्थ और सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष का स्वरूप वर्णित करते हुए प्रत्यक्ष, आगम अनुमान का विशय इसमें गर्भित किया जाता है। परोक्ष प्रमाण के अंतर्गत स्मृति, प्रत्यभिज्ञान (अनुमान) तर्क (आगम, श्रुत) का विशय भी स्पश्ट किया जाता है। जैनाचार्यों ने स्वार्थानुमान के अन्तर्गत पूर्ववत्, शशवत्, सामान्यतोदृश्ट तथा परार्थानुमान में प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन आदि का निरूपण जैनेतर मान्यताओं से संगति बिठाते हुए उनकी मिथ्या अवधारणाओं को निरसित करने हेतु किया है।
‘सम्यग्ज्ञानं प्रमाणं’ सम्यग्ज्ञान को प्रमाण संज्ञा प्राप्त है। स्वार्थ प्रमाण, परार्थ प्रमाण, स्वतः प्रमाण, परतः प्रमाण आदि के विकल्पों से जैन दर्षन की मान्यताओं की प्रभावना ‘हेतु विद्या’ में की जाती है। प्रमाण का विशय अति विस्तृत है। इसमें अन्य दर्षनों की मान्यताओं की जो कि ऐकान्तिक हैं, सापेक्ष नयों से स्वीकार करते हुए उसमें छिपे एकान्त अथवा दुराग्रह को निरसित करने का अभ्यास कराया जाता है। आप्त मीमांसा, अश्टषती, अश्टसहस्री, प्रमेय कमल मार्तण्ड आदि सैकड़ों ग्रन्थों में यह विशय समाहित है जिनके अभ्यास से तर्क में निपुणता प्राप्त कर जैन दर्षन की प्रभावना की जाती है।
पू० माता जी के तर्क शस्त्र या प्रमाणज्ञान का प्रमाण उनके द्वारा रचित अश्टसह का हिन्दी भाशा में विषेश अनुवाद है। अश्ट सहस्री को कश्ट सहस्री नाम से उल्लिखित किया जाता है तथा पूर्व में कोई हिन्दी अनुवाद न होने के कारण इस विशय के परिज्ञान से सामान्य तो क्या विद्वज्जन भी प्रायः अपरिचित ही थे। अश्टसहस्री का अनुवाद तो वस्तुतः लोहे के चने चबाने के समान ही कहा जावेगा। माता जी ने अपने न्याय विशयक अगाध ज्ञान का उपयोग स्याद्वाद चन्द्रिका में भी किया है इसके दर्षन अनेक स्थलों पर होते हैं।
न्याय शस्त्रां में चार प्रकार की कथायें या विद्याओं का अति महत्व है। माता जी आक्षेपिणी, विक्षेपिणी, संवेगिनी एवं निर्वेदिनी इन सभी में अति दक्ष हैं। विक्षेपिणी शैली का प्रयोग वे बहुत विमर्ष के साथ करती हैं ताकि पाठक की श्रद्धा जैनधर्म से पलायित न हो तथा परमत का भी निरसन हो। लेखिका ने अश्ट सह के अन्तर्गत विशयानुसार खण्डन – मण्डन विधि को स्वयं अपनाया भी है किन्तु नियमसार के जैन अध्यात्म विशय में कोमल शैली का प्रयोग किया है जो अति वांछनीय ही है। ऊपर उल्लिखित चार कथाओं के लक्षण निम्न हैं –
आक्षेपिणी – जैन धर्म की समर्थक उक्तियों का प्रकाषन।
विक्षेपिणी – अन्य दर्षनों द्वारा, उनके मान्य तत्त्वों का दिग्दर्षन कराते हुए, जैन दर्षन का, खण्डन कर उसके विरोधी वक्तव्य का प्रस्तुतीकरण एवं स्वमत मण्डन ताकि इस प्रकार का अवसर निर्माण कर जैन वादी को शस्त्रार्थ में विजय प्राप्त हो सके।
संवेगिनी – धर्म एवं धर्म के फल में अनुराग उत्पन्न करने वाली कथा।
निर्वेदिनी – संसार, शरीर और भोगों से विरक्ति उत्पन्न (निर्वेगिनी) कर त्याग मार्ग की रुचि उत्पन्न करने वाला वचन समूह।
स्याद्वाद चन्द्रिका में उपरोक्त चारों प्रकार की शैली से माता जी ने भव्यों को अपेक्षित सम्बोधन कर यथेश्ट मार्गदर्षन किया है किन्तु विक्षेपिणी पद्धति का प्रयोग अल्प रूप में ही विहित समझा है, यह उचित भी है। प्रायः जैन दर्षन की मान्यताओं को समीचीन पद्धति से पुश्ट किया है। ‘नियमसार’ के रत्नत्रय रूप विशय को इससे बल मिला है।
पू० माता जी जैन न्याय की प्रखर वेत्ता व वक्ता है। स्याद्वाद चन्द्रिका में अधिकांषतः जैन न्याय सम्मत गवेशणाओं के आधार पर नियमसार का हार्द खोला गया है। उसमें पगपग पर जैन न्याय से विशय का स्पश्टीकरण एवं पुश्टिकरण किया गया है। यहाँ जैन न्याय के प्रायः मूल तत्व पल्लवित रूप में दृश्टिगत किए जा सकते हैं। माता जी न्याय प्रभाकर जैसी सर्वोच्च उपाधि से विभूशित हैं उनका न्याय कौषल ‘स्याद्वाद चन्द्रिका’ में दृश्टव्य है। हम यहाँ न्याय विशयक एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं –
यदि आत्मा परपदार्थसार्थमेव प्रकाषयति जानाति तर्हि दर्षनं तु स्वप्रकाषकत्वेन तेनात्मना पृथगेव भविश्यति।
ततः कारणात् तद्दर्षनं किमपि परद्रव्यस्वरूप-ज्ञेयवस्तु ज्ञातुं न “शक्नोति।
अन्यच्चात्मापि स्वात्मानं न ज्ञास्यति नैयायिकमतेऽपि आत्मात्मानं न जानाति तर्हि
आत्मनो ज्ञानं कथं भविश्यतीति शकायां एतद् ज्ञातव्यं यत् नैयायिका समवायग्रहणेनात्मनि ज्ञानगुणसम्बन्धं मन्यन्ते न तथा जैनमतेऽस्ति।
तात्पर्यमेतत् अनेकान्तमते नयचक्रं सम्यगवबुदध्यात्मतत्वस्य ज्ञानदर्षनयोष्च स्वरूपमवबोद्धव्यं।
अर्थ – (उसे ही कहते हैं) यदि आत्मा पर पदार्थ के समूह को ही जानता है प्रकाषित करता है तो दर्षन स्वप्रकाषक होने से उस आत्मा से पृथक ही रहेगा। इस कारण से वह दर्षन कुछ भी पर द्रव्यस्वरूप ज्ञेय वस्तु को जानने में समर्थ नहीं होगा। पुनः आत्मा भी अपने आपको नहीं जानेगा। नैयायिक मत में भी आत्मा स्वयं को नहीं जानता है, तो फिर आत्मा का ज्ञान कैसे होवगा। ऐसी आषंका होने पर ऐसा जानना कि नैयायिक लोग समवाय गुण से आत्मा में ज्ञान गुण का सम्बन्ध मानते हैं वैसा जैनमत में नहीं है। तात्पर्य यह हुआ कि अनेकान्त मत में नय समूह को अच्छी तरह जानकर आत्मतत्त्व का और ज्ञान दर्षन का स्वरूप समझना चाहिए।
स्याद्वाद चन्द्रिकाकत्र्री ने कहा है।
”सिद्धान्तग्रन्थन्यायग्रन्थयोर्दर्षनज्ञानलक्षणं पृथक् पृथक् वर्तते।“
सिद्धान्त ग्रन्थ और न्याय ग्रन्थ मे दर्षन और ज्ञान का लक्षण पृथक् पृथक् है। आगे कहा है कि ‘ट्खण्डागम जो कि सिद्धान्त ग्रन्थ है उसकी धवला टीका में श्री वीरसेन आचार्य देव ने कहा है कि अपने से भिन्न वस्तु को जानने वाला ज्ञान है और अपने से अभिन्न वस्तु को जानने वाला दर्षन है इसलिए इन दोनों में एकत्व नहीं है।
शंका – ज्ञान और दर्षन की युगपत् प्रवृत्ति क्यों नहीं होती ?
समाधान – क्यों नहीं होती। होती ही है। आवरण कर्म के नश्ट हो जाने पर दोनों की एक साथ प्रवृत्ति पाई जाती है।
आगे माता जी ने स्पश्ट किया है। कि संसारी जीवों में ज्ञान-दर्षन की युगपत् प्रवृत्ति नहीं होती क्योंकि आवरण कर्म के उदय से (ज्ञानावरण-दर्षनावरण के उदय से) छद्मस्थ जीवों के ज्ञानदर्षन की युगपत् प्रवृत्ति की शक्ति रुक जाती है। यह प्रष्न उपस्थित होने पर कि स्वसंवेदन से रहित आत्मा पदार्थ की तो उपलब्धि नहीं होती, माता जी ने समाधान दिया है कि बहिरंग पदार्थों की उपयोग रूप अवस्था में अन्तरंग पदार्थ का उपयोग (स्वसंवेदन) का अभाव ही है।
यहाँ भी स्पश्ट किया है कि अनन्त त्रिकाल गोचर वाह्य पदार्थ में प्रस्तुत होने वाला केवलज्ञान है और तीनों कालों की विशयभूत, ऐसी अपनी आत्मा में प्रवृत्त होने वाला केवल दर्षन है। यह सब व्याख्यान माता जी ने सिद्धान्तग्रन्थ धवला का उद्धरण प्रस्तुत कर किया है। आगे तर्कषास्त्र का कथन माता जी ने प्रस्तुत कर कहा है, दृश्टव्य है।
किन्तु तर्कषास्त्रेऽन्यदेव कथितं वत्र्तते – ”स्वापूर्वार्थव्यवसायात्मकं ज्ञानं प्रमाणं“ अपना और अपूर्व पदार्थ का निष्चय करने वाला सविकल्प ज्ञान है तथा सत्तावलोकन मात्र निर्विकल्प दर्षन है। सभी न्याय ग्रन्थों मे स्वपर के सामान्य को ग्रहण करने वाला दर्षन है और स्वपर के विषेश को ग्रहण करने वाला ज्ञान है, यह निरूपण है। इन दोंनो सिद्धान्त और न्याय की मान्यता में अपेक्षा से दोश नहीं आता।
आगे बृहद् द्रव्यसंग्रहगत सन्मतितर्क के अभिप्राय का विस्तार कर विषेश ऊहापोह द्वारा तर्क और सिद्धान्त के साम×जस्य का प्रस्तुतीकरण करते हुए कहा है,
तर्क ग्रन्थ के अभिप्राय से सत्तावलोकन दर्षन कहा गया है उसके ऊपर सिद्धान्त के अभिप्राय से कहते हैं। जैसे उत्तर ज्ञान की उत्पति में जो प्रयत्न है उस रूप में जो अपनी आत्मा का परिच्छेदन या अवलोकन है वह दर्षन कहलाता है इसके अनन्तर वाह्य विशय में विकल्प रूप से पदार्थ का ग्रहण है वह ज्ञान है ऐसा वार्तिक है।
शंका – यदि आत्मा का ग्राहक दर्षन है और पर का ग्राहक ज्ञान है तो जैसे नैयायिक के मत में ज्ञान आत्मा को नहीं जानता है वैसे ही जैन मत में भी ज्ञान आत्मा को नहीं जानेगा। यह बहुत बड़ा दूशण आ जावेगा।
समाधान – नैयायिक मत में ज्ञान पृथक् और दर्षन पृथक् ऐसे दो गुण नहीं है इस कारण उनके यहाँ आत्मा का ज्ञान नहीं होना यह दूशण आता हैै, किन्तु जैन मत में तो ज्ञानगुण से परद्रव्य को जानते हैं और दर्षन गुण से आत्मा को जानते हैं। इसलिए आत्मा को नहीं जानने रूप दूशण नहीं आता। दूसरी बात यह है कि सामान्य ग्राहक दर्षन और विषेश ग्राहक ज्ञान है जब ऐसा कहा जावेगा तो वह ज्ञान प्रमाणता को नहीं प्राप्त होगा।
शंका – ऐसा क्यों।
समाधान – सो ही बताते है। वस्तु को ग्रहण करने वाला प्रमाण है। वह वस्तु सामान्य विषेशात्मक है। पुनः ज्ञान ने वस्तु का एकदेष विषेश ही ग्रहण किया है न कि वस्तु को। सिद्धान्त से गुण-गुणी अभिन्न है और विपर्यय और अनध्यवसाय रहित वस्तु को जानने वाला ज्ञान स्वरूप आत्मा ही प्रमाण है। वह प्रदीप के समान, स्वपर के समान और विषेश को जानता है इस कारण अभेद रूप से वह आत्मा ही प्रमाण है।
अधिक कहने से क्या यादि कोई भी तर्क के अर्थ को और सिद्धान्त के अर्थ को जानकर एकान्त दुराग्रह का त्याग करके नय विभाग से मध्यस्थ वृत्ति से व्याख्यान करता है, तब दोंनो ही घटित हो जाते हैं। तर्कषास्त्र में मुख्यता से पर समय का व्याख्यान है और सिद्धान्त में मुख्य रूप से स्वसमय का व्याख्यान है। यहाँ पर बृहद्द्रव्य संग्रह की टीका का संक्षेप में कुछ अवतरण दिया है। विषेश जिज्ञासुओं को वहीं से देख लेना चाहिये।“
यहाँ इसी विशय से सम्बन्धित एक महत्वपूर्ण चर्चा अप्रासंगिक न होगी। आ० कुन्दकुन्द ने नियमसार प्राभृत के अन्तर्गत शुद्ध उपयोगाधिकार का प्रारम्भ करते हुए कहा है –
जाणदि पस्सदि सव्वं वयवहार णयेण केवली भगवं ।’
केवलणाणी जाणदि पस्सदि णियमेण अप्पाणं ।।59।।
यह आर्या अत्यन्त उपयोगी है एवं दार्षनिक क्षेत्र के समाधान हेतु वरदान ही है। इसका अर्थ यह है कि केवली भगवान व्यवहार नय से समस्त ज्ञेयों को जानते देखते हैं (किन्तु) निष्चय नय से अपनी आत्मा को जानते और देखते हैं। इस सूत्र की टीका हुए आर्यिका ज्ञानमती स्याद्वाद चन्द्रिका में उल्लिखित करती हैं।
”अत्र गाथायां व्यवहारनयो भेदकारक एव गृहीतव्यो न च पराश्रितः।कि×च केवलिनां ज्ञानं पराश्रितं नास्ति प्रत्युत तज्ज्ञाने सर्व प्रतिविम्बी भवति दर्पणवत्।न ते भगवन्त ईहापूर्वकं जानन्ति मोहाभावात्।
अर्थ – यहाँ पर गाथा में भेद को करने वाला व्यवहार नय ग्रहण करना चाहिए न कि पराश्रित। क्योंकि केवली भगवान का ज्ञान पराश्रित नहीं है बल्कि उनके ज्ञान में सभी पदार्थ प्रतिविम्बित होते रहते हैं। दर्पण के समान1। वे भगवान इच्छापूर्वक कुछ नहीं जानते क्योंकि उनके मोह का अभाव हो गया है।
प्रस्तुत टीकांष का खुलासा इस प्रकार करना चाहूँगा। अपनी आत्मा को जानना-देखना व विष्व को जानना-देखना एक ही बात है। वह इस प्रकार किव्यवहार के कथन से यदि भगवान सर्वज्ञ है, तो सर्व में उनकी अपनी आत्मा भी सम्मिलित है। निष्चय नय कथानानुसार यदि भगवान आत्मज्ञ हैं तो उनकी आत्मा तो समस्त विष्व के (त्रिकाल एवं तीन लोक की समस्त पर्यायों सहित) आकार परिणत है।
उसमें सर्वजगत प्रतिविम्बित हो रहा है अतः सर्वज्ञता सहज ही सिद्ध होती है। विषेश यह है कि भगवान स्व को तन्मय होकर जानते देखते हैं पर को तन्मय होकर नहीं जानते। इससे निष्चय नय और व्यवहार नयों का प्रयोग कुन्दकुन्द स्वामी ने किया है।
यहाँ इन्ही आचार्य की एक गाथा उद्धृत करने का लोभ संवरण नहीं कर पा रहा है।
आदा णाणपमाणं णाणं णेयप्पमाणमुद्दिट्ठं।’
णेयं लोयालोयं तम्हा णाणं दु सव्वगयं ।।प्रवचन सार।।
आत्मा ज्ञान प्रमाण है ज्ञान ज्ञेय प्रमाण है, ज्ञेय लेाकालोक है अतः ज्ञान सर्वगत है। (आत्मा = ज्ञान = ज्ञेय सर्ववस्तु, अतः ज्ञान = सर्वगत स्ववस्तु)
इस गाथा से यह सिद्ध होता है कि आत्मज्ञता ही सर्वज्ञता है तथा सर्वज्ञता ही आत्मज्ञता है। यहाँ वेदान्त द्वारा मान्य सर्वव्यापकता को सर्वथा न स्वीकार कर, अर्थात् प्रदेषों की अपेक्षा सर्वस्थितियों में न स्वीकार कर ज्ञान की अपेक्षा सर्वगतपना, सर्वव्यापिपना किया है। हाँ केवली समुद्घात की अवस्था में प्रदेष तीनों लोकों में व्याप्त होने की वजह से प्रदेष एवं ज्ञान दोनों की अपेक्षा सर्वगतत्व सिद्ध होता है।
ज्ञान से सर्व को जानना अतन्मय होकर ही हो सकता है। अतः सर्वज्ञता तो व्यवहारनय का विशय है। आत्म प्रदेष ज्ञेयरूप परिणत न होकर ज्ञेयाकार रूप परिणत होते हैं वह परिणति आत्मतन्मयत्व है अतः आत्मज्ञता निष्चयनय का विशय है। परिणमन को ही निष्चय नय से कत्र्तृत्वपना कहा है। (समयसार कलष में यह दृश्टव्य है।)(कलष-51)1
जैन दर्षन की स्थापना हेतु परंपराचार्यों ने प्रत्यक्ष प्रमाण के दो भेद परमार्थ एवं सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष स्वीकार किये हैं। प्रमाण के पाँच भेद है।
1. मतिज्ञान 2. श्रुतज्ञान 3. अवधिज्ञान 4. मनः पर्ययज्ञान 5. केवलज्ञान।
इसमें अवधि, मनः पर्यय ये दो प्रत्यक्ष तथा केवलज्ञान सकल प्रत्यक्ष है। एवं मतिज्ञान–श्रुतज्ञान परोक्ष हैं, क्योंकि ये मन और इन्द्रियों की सहायता से पदार्थों को जानते हैं।
उपरोक्त विशय की चर्चा स्याद्वाद चन्द्रिका टीका में आर्यिका ज्ञानमती जी ने उठायी है यहाँ टीका की कतिपय पंक्तियाँ गाथा क्रमांक 12 के अन्तर्गत दृश्टव्य है।
अभ्यन्तरे मतिज्ञानावरणकर्मक्षयोपषमाद् वीर्यान्तरायक्षयोपषमाच्चबहिरंग-पचेन्द्रियमनोऽबलम्बाच्च मूत्र्तामूत्र्तवस्तु अस्पश्टतया यज्जनाति तन्मतिज्ञानम् परमार्थत परोक्षमपि इदं तर्क शस्त्रनुसारेण प्रत्यक्षं गीयते
अर्थ – अभ्यन्तर में मतिज्ञानावरण कर्म के क्षयोपषम, वीर्यान्तराय कर्म के क्षयोपषम से तथा बहिर› में पाँच इन्द्रियों और मन के अवलम्बन से जो मूत्र्त-अमूत्र्त वस्तु को अस्पश्ट रूप से जानता हो वह मतिज्ञान है। वह ज्ञान यद्यपि परमार्थ से परोक्ष है फिर भी तर्क शस्त्र के अनुसार सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष कहलाता है।
अभ्यन्तर में श्रुत ज्ञानवारण के क्षयोपषम से और मन के अवलम्बन से तथा बहिरं› में प्रकाष, उपाध्याय आदि सहकारी कारणों के मिलने से जो मूत्र्त-अमूत्र्त को अस्पश्ट जानता है वह श्रुतज्ञान है। उसमें से जो शब्द रूप श्रुत ज्ञान है वह परोक्ष ही है और जो जीव-अजीव आदि वाह्य पदार्थों के जानने रूप है वह भी परोक्ष है क्योकि अविषद है पुनः जो अभ्यन्तर ”मैं सुखी हूँ अथवा दुःखी हूँ“ इत्यादि विकल्प रूप से होते हैं अथवा ”मैं अनन्त ज्ञान आदि रूप हूँ“ इत्यादि प्रकार से होता है वह ईशत् परोक्ष है।
ओैर जो शुद्ध आत्मा की तरफ (अभिमुख) होकर उसके अनुभव रूप भाव श्रुतज्ञान है, वह उभय नय से ”आत्मा“ से वाच्य वीतराग चारित्र के साथ अविनाभावी निर्विकल्प संवेदन ज्ञान है यह प्रत्यक्ष कहलाता है क्योकि यह परम समाधि में लीन हुए मुनियो को संवेदन ज्ञान है। यह प्रत्यक्ष कहलाता है। क्योंकि यह परम प्रत्यक्ष कहलाता है क्योंकि यह परम समाधि में लीन हुए मुनियों को स्वानुभवगम्य हो रहा है।
यही ज्ञान, स्वभाव ज्ञान के लिए बीज भूत है। आगे ओैर भी चर्चा टीकाकत्र्री ने इस सम्बन्ध में की है पठनीय है।
जैन दर्षन अनेकान्त दर्षन है। इसी में सभी का हित है। इसे आ0 समन्तभद्र ने सर्वोदय तीर्थ की संज्ञा दी है। दृश्टव्य है।
सर्वान्तवत्तद् गुणमुरव्यकल्पंसर्वान्तषून्यं च मिथोऽनपेक्षं।
सर्वापदामन्तकरं निरन्तंसर्वोदयं तीर्थमिदं तवैव।।
हे भगवान, समस्त अन्तों (धर्म-स्वभावों-पहलुओं) का जिसमें समावेष है और गौण मुख्य की कल्पना से, विधि से जो सहित है। (वह समीचीन मत अनेकान्त है।) एवं जो सभी की समावेषता से शून्य है अनपेक्ष है वह मिथ्या मत है। आपका यही अनेकान्त समस्त आपत्तियों का नाषक है। तथा अनन्त काल तक के लिए स्थाई है। वह आपका ही सर्वोदय तीर्थ है। सबके लिए हितकर है।
पूज्य माता जी ने स्याद्वाद चन्द्रिका में अनेकान्त जैन दर्षन का विषेश वर्णन किया है। इसमें वर्णित अनेकान्त के मान्य तत्वों के सम्बन्ध में पृथक् अनेकान्त एवं स्याद्वाद नय निरूपण के अन्तर्गत चर्चा कर रहे हैं।