स्याद्वाद चन्द्रिका में गुणस्थान परिपाटी से प्रकरण-पुश्टि
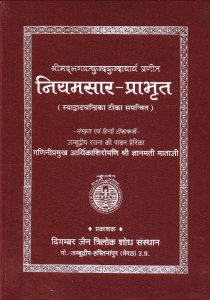
संसारी जीव को सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्र के द्वारा मोक्ष प्राप्त करने के प्रयत्न में जो परिणतियां प्राप्त होती हैं, जिस विकास क्रम से गुजरना होता है, जो कक्षायें उत्तीर्ण करनी होती हैं उन्हें गुणस्थान कहते हैं। ये गुण के स्थान अर्थात नियम (रत्नत्रय) रूप गुण के पद है।
आगे आगे गुण में विकास रूप स्थितियां हैं इसका अर्थ यह है कि जो गुण या क्वालिटी ;फनंसपजलद्ध, विषेशता आगे के गुणस्थान में वह पूर्व के गुणस्थान में नहीं है आगे के गुणस्थान में आस्रव, बन्ध न्यून एवं संवर, निर्जरा अधिक होती है इसका कारण वृद्धिगत होती हुई भाव विषुद्धि है।
इसी के बल से असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा होती है1। आगम में मोह और योग के निमित्त से होने वाली जीव की दषाओं को, जीव के परिणामों को, दर्जा या गुणस्थान कहा गया है2। इसमें मोहनीय कर्म के दो भेद दर्षन मोहनीय एवं चारित्र मोहनीय के उदय उपषम, क्षयोपषम, क्षय आदि दस करणों के माध्यम से अवस्थायें अपेक्षित होती हैं एवं मन-वचन-काय के निमित्त से होने वाले जो प्रभाव होते हैं उनका रूप समाविश्ट रहता है।
आदि के चार गुणस्थान दर्षन मोहनीय कर्म के निमित्त से एवं पाचवें गुणस्थान से बारहवें तक आठ गुणस्थान चारित्र मोहनीय कर्म के निमित्त से होते हैं। तेरहवां, चैदहवां गुणस्थान योग से निमित्त से होता है। जीव, अजीव, आस्रव, बन्ध, संवर, निर्जरा और मोक्ष इन सात तत्वों एवं नियम अर्थात् सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान एवं सम्यक्चारित्र इन रत्नत्रयों आदि का ज्ञान करने हेतु आगमकथित गुणस्थान एवं मर्णणास्थान का स्वरूपावबोध आवष्यक होता है। सिद्धान्त ग्रंथों में इन्हीं गुणस्थानों एवं मार्गणास्थानों के निरूपण क्रमषः सामान्य (ओघ) और विषेश (आदेष-विस्तार) निरूपण के नाम से प्रसिद्ध हैं। प्ररूपणायें 20 हैं। यथा-
गुणजीवापज्जत्ती पाणा सण्णा य मग्गणाओ य।
उवओगो वि य कमसो वीसं तु परूवणा भणिया ।। 2।।
गुणस्थान, जीव समास, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा, 14 मार्गणायें तथा उपयोग ये 20 प्ररूपणायें हैं। इनमें गुणस्थान भी चैदह हैं जो कि ‘ाट्खण्डागम सत्प्ररूपणा के 9 से 22वें तक सूत्रों में उल्लिखित हैं तथा धवला टीका के आधार पर गोम्मटसार जीवकांड में आचार्य नेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्ती देव ने निम्न गाथाओं में गुणस्थानों का नामोल्लेख किया है –
मिच्छो सासण मिस्सो अविरद सम्मो य देसविरदो य।
विरदा पमत्त इदरो अपुव्व अणियट्ठि सुहुमो य।। 9।।
उवसंत खीणमोहो सजोग केवलिजिणो अजोगी य।
चोद्दस जीवसमासा कमेण सिद्धा य णादव्वा।। 10।।
अर्थात् गुणस्थानों के नाम इस प्रकार हैं,
| 1-मिथ्यादृश्टि | 2-सासादन | 3-मिश्र | 4-अविरत सम्यग्दृश्टि |
| 5-देषविरत | 6-प्रमत्तविरत | 7-अप्रमत्त विरत | 8-अपूर्वकरण |
| 9-अनिवृत्तिकरण | 10-सूक्ष्म साम्पराय | 11-उपषान्तमोह | 12-क्षीणमोह |
| 13-सयोग केवली | 14-अयोग केवली। |
सिद्ध भगवान गुणस्थानातीत हैं। यहां ज्ञातव्य है कि आचार्य धरसेन स्वामी से ज्ञान प्राप्त कर आचार्य पुश्पदन्त और भूतबली महाराज ने ‘ट्खण्डागम की रचना की थी। यह सर्वप्रथम लिपिबद्ध आगम है श्रुत पंचमी (ज्येश्ठ “शुक्ल पंचमी) को यह पूर्ण हुआ था यह रचना काल लगभग 2000 वर्श पूर्व का है।
इस ‘ट्खण्डागम के जीवस्थान, क्षुल्लकबन्ध, बन्ध स्वामित्व, वेदना खण्ड, वर्गणा खण्ड और महाबन्ध ये छह खण्ड हैं। इस सिद्धान्त ग्रंथ पर आठवीं “शताब्दी में आ० वीरसेन स्वामी ने धवला टीका (पांच खण्डों पर) लिखी जो साठ हजार पद प्रमाण हैं। ‘ट्खण्डागम के सार रूप में 11वीं “शताब्दी में आ० नेमिचंद्र सिद्धान्त चक्रवर्ती देव ने गोम्मटसार जीवकांड एवं कर्मकांड की रचना की थी।
बडे़ हर्श का विपय है कि ‘ट्खण्डागम पर ही पू० आर्यिका ज्ञानमती माता जी ने धवला एवं गोम्मटसार के रहस्यों को समाविश्ट करते हुए वर्तमान में क्षयोपषम कम होने तथा एकान्त नयाभास प्रवृत्ति होने की स्थिति का अवलोकन कर सुपाच्यमान सर्वोपयोगी ‘‘सिद्धान्त चिन्तामणि’’ नाम की विषद टीका संस्कृत भाशा में की है इसका प्रथम खंड दि० जैन त्रिलोक “ाोध संस्थान से प्रकाषित हो चुका है। यह अवष्य पठनीय है।
उपर्युक्त 14 गुणस्थानों के स्वरूप को वर्णित करना यहां अभीश्ट होगा। यह करणानुयोेग एवं द्रव्यानुयोग के परिपे्रक्ष्य में यहां अति संक्षेप में किया जाता है।
1. मिथ्यात्व :- मिथ्यात्व प्रकृति के उदय से अतत्व श्रद्धान रूप आत्मा के परिणाम विषेश को मिथ्यात्व गुणस्थान कहते हैं।
2. सासादन :- सम्यक्त्व की आसादना (विराधना) सहित मिथ्यात्व के सम्मुख और अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ कर्मप्रकृति के उदय सहित परिणाम को सासादन कहते हैं यह गुणस्थान गिरने की अपेक्षा होता है।
3. मिश्र :- सम्यक्मिथ्यात्व प्रकृति के उदय से जीव के न तो सम्यक्त्व परिणाम होते हैं, न केवल मिथ्यात्व रूप परिणाम होते हैं। मिश्रित दही-गुड़ के समान मिश्र परिणाम को मिश्र गुणस्थान कहते हैं।
4. अविरत सम्यग्दृश्टि :- दर्षन मोहनीय की तीन एवं चारित्र मोहनीय की अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ इन चार प्रकृतियों, कुल सात कर्म प्रकृतियों के उपषम, क्षयोपषम या क्षय से और अप्रत्याख्यानावरण चतुश्क के उदय से व्रत रहित एवं सम्यक्त्व सहित परिणाम को अविरत सम्यग्दृश्टि गुणस्थान कहते हैं। आत्मनिन्दा सहित विशयभोगों का अनुभव इसमें होता है।
5. देषविरत :- प्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, लोभ के उदय से तथा अप्रत्याख्यानावरण चतुश्क के उपषम या क्षयोपषम से श्रावक व्रत रूप देषविरत या संयमासंयम गुणस्थान होता है।
6. प्रमत्त विरत :- संज्वलन और नोकशाय के तीव्र उदय से संयमभाव तथा मलजनक प्रमाद इन दोनों से युक्त संयमी मुनि के चित्रलाचरणी परिणाम को प्रमत्त विरत कहते हैं।
7. अप्रमत्त :- 15 प्रकार प्रमाद अर्थात् 4 कशाय, 4 विकथा, 5 इन्द्रिय विशय, 1 निद्रा, 1 स्नेह से रहित परिणाम (ध्यान अवस्था) को अप्रमत्त विरत कहते हैं। इसके स्वस्थान एवं सातिषय दो भेद हैं। स्वस्थान में साधु सातवें से छठवें और छठवें से सातवें में हजारों बार आता जाता है। सातिषय में श्रेणी आरोहण के सम्मुख होता है।
8. अपूर्वकरण :- श्रेणी का पहला गुणस्थान अपूर्वकरण होता है। यहां शुक्ल- ध्यान प्रारंभ होता है। जिस करण में उत्तरोत्तर अपूर्व ही अपूर्व परिणाम होते चले जाते हैं अर्थात् भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम सदा विसदृष ही हों और एक समयवर्ती जीवों के परिणाम सदृष भी हों उसे अपूर्वकरण कहते हैं।
9. अनिवृत्तिकरण :– जिस करण में भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम विसदृष हों और एक समयवर्ती जीवों के परिणाम सदृष ही हों उसे अनिवृत्तिकरण कहते हैं।
10. सूक्ष्मसाम्पराय:- अत्यंत सूक्ष्म अवस्था को प्राप्त लोभ कशाय के उदय को अनुभव करते हुए जीव के सूक्ष्म साम्पराय नाम का दसवां गुणस्थान होता है।
11. उपषान्तमोह :- चारित्र मोहनीय की प्रकृतियों का उपषम होने सयथाख्यात चारित्र को धारण करने वाले मुनि के परिणाम को उपषान्त मोह कहते हैं। इस गुणस्थान का काल समाप्त हो जाने पर मोहनीय के उदय से जीव निचले गुणस्थानों में आ जाता है।
12. क्षीणमोह :– मोहनीय कर्म के अत्यंत क्षय होने से स्फटिक भाजनगत शुद्ध जल की तरह अत्यंत निर्मल अविनाषी यथाख्यात चारित्रधारी मुनि के क्षीणमोह गुणस्थान होता है।
13. सयोग केवली:– घातिया कर्मों की 47 एवं अघातिया कर्मों की 16 प्रकृतियों कुल 63 प्रकृतियों के सर्वथा नाष होने से लोकालोक प्रकाषक केवल ज्ञान तथा मनोयोग, वचनयोग, काययोग के धारक अर्हन्त भट्टारक सयोगी परमात्मा के सयोग केवली गुणस्थान होता है।
14. अयोग केवली :– मन-वचन-काय योग से रहित केवल ज्ञान सहित अर्हन्त परमात्मा के यह गुणस्थान कहा गया है। यहां उपयोगी जानकर गुणस्थान का लक्षण निम्न गाथा में व्यक्त किया जाता है।
जे हिं लक्खिजन्ते उदयादिसु संभवेहिं भावेहिं।
जीवा ते गुणसण्णा णिद्दिट्ठा सव्व दरिसीहिं।।
अर्थ – मोहनीय आदि कमों के उदय, उपषम, क्षय, क्षयोपषम परिणाम रूप अवस्था विषेशों के होते हुए उत्पन्न होने वाले जिन भावों से अर्थात् जीव के मिथ्यात्व आदि परिणामों से जीव गुण्यन्ते अर्थात् देखे जाते हैं, पहचाने जाते हैं जीव के उन परिणामों की गुणस्थान संज्ञा होती है ऐसा सर्वज्ञदेव ने कहा है।
(टीका) नियमसार निष्चयरत्नत्रय प्रधान अध्यात्म का महान ग्रंथ है। कर्म सिद्धान्त एवं करणानुयोग से अपरिचित पाठक वर्णित विपय को इसके अंतर्गत पढ़कर निष्चयैकान्त से प्रभावित होकर भ्रमित हो सकता है, बजाय ज्ञान प्राप्ति के एकान्त मिथ्यात्व (नियतिवाद आदि) से अत्यधिक ग्रसित हो सकता है एवं यद्वा तद्वा अवस्था में शुद्ध आत्मानुभव मान लेता है जो कि असंभव है। अक्रियावादिता के ज्वर से ग्रसित हो सकता है।
यदि नियमसारप्राभृत की अध्यात्म गवेशणा में कर्मसिद्धान्त आदि उपयोगी समावेष कर गुणस्थान परिपाटी से अध्ययन किया जावे तो दृश्टि व्यापक रहती है एवं असंयम एवं सांख्यमतदूशण आदि से बच जाता है एवं सम्यक्त्व प्राप्त कर सकता है अथवा प्राप्त सम्यक्त्व को दृढ़ कर सकता है। यहां इस प्रकरण में उपयोगी जानकर पंडित प्रवर टोडरमल जी का निम्न दोहा प्रस्तुत है-
लब्धिसार को पायकैं करिकैं क्षपणासार।
हो है प्रवचनसार सौं समयसार अविकार।।
यहां स्पश्ट है कि लब्धिसार, क्षपणासार, प्रवचनसार के क्रम से नियमसार समयसार का पात्र होकर अविकारी होता है। इनमें करणानुयोग एवं गुणस्थान प्रक्रिया समाविश्ट हो जाती है। पूर्वाक्त गुणस्थान के महत्व संबंधी दृश्टिकोण को मन में रखकर पू० माता जी ने स्याद्वाद चन्द्रिका में यथास्थान गुणस्थान विवेचन से प्रकृत नियमसार के विशयों की पुश्टि की है।
यह एक महनीय कार्य है तथा प्रस्तुत टीका की प्रमुख विषेशताओं में है कतिपय जन भ्रम से अव्रती अवस्था में अपने को कारण समयसार रूप मानकर भ्रमित होते हैं। इस भ्रम के निवारणार्थ कारण समयसार या निष्चय रत्नत्रयस्वरूप मोक्षमार्ग का स्वरूप वर्णित करते हुए निम्न टीकांष माताजी ने लिखा है वह ज्ञातव्य है-
‘‘नियमो मोक्षोपायो यद्यपि व्यवहारनयेन क्षीणकशायान्त्यसमयपरिणाम- स्तथाप्यघातिकर्मवषेन केवलिनामपि चारित्रगुणेशु आनुशंगिकदोशाः सम्भवन्ति। तथा च व्युपरतक्रियानिवृत्तिलक्षणं ध्यानमपि उपचारेण तत्र कथ्यते। अतो निष्चयनयेन अयोगिकेवलिनामन्त्यसमयपरिणामोऽपि रत्नत्रययस्वरूपमोक्षमार्ग एव।
यह नियम नाम से जो मोक्ष का उपाय है अर्थात् रत्नत्रय है वह यद्यपि व्यवहारनय से क्षीणकशायी मुनि के अंतिम समय का परिणाम है, फिर भी अघाति कर्म के निमित्त से केवली भगवन्तों के चारित्र गुणों में आनुशंगिक दोश संभव है तथा व्युपरतक्रियानिवृत्ति नाम का चैथा शुक्लध्यान भी उनके वहां पर उपचार से कहा गया है इसलिए निष्चय नय से अयोगिकेवलियों के अंतिम समय का परिणाम भी रत्नत्रयस्वरूप मोक्षमार्ग ही है।
’’ यहां यह स्पश्ट है कि चैदहवें गुणस्थान तक भी जीव अपूर्ण है मोक्षमार्गी ही है नियममय ही है तो अव्रती तक गुणस्थानों में अपने को गुण से पूर्ण या मुक्त मान लेना निष्चयनय का दुरुपयोग ही है। नियमसार गाथा क्रमांक 18 के अंतर्गत कुन्दकुन्द स्वामी ने अध्यात्म भाशा में सम्यग्ज्ञान के चारों भेदों मति, श्रुत, अवधि, मनःपर्यय को विभाव ज्ञान कहा है। यहां पर विभाव से कर्मोपाधि सापेक्षता की ही विवक्षा है।
इस प्रकरण को पू० माता जी ने आगम की अपेक्षा भी समझने हेतु ज्ञान, अज्ञान का निरूपण किया है। आगम की अपेक्षा उपरोक्त चार क्षायोपषमिक ज्ञान सम्यक्ज्ञान माने जाते हैं कहा भी है-
णाणं अठवियप्पंमदिसुद ओही अणाणणाणाणि।
मणपज्जय केवलमवि पच्चक्ख परोक्ख भेयं च।।
ज्ञान आठ प्रकार का है, मति, श्रुत, अवधि ये तीन ज्ञान अर्थात् सम्यग्ज्ञान कुमति, कुश्रुत, विभंगावधि ये तीन मिथ्याज्ञान या अज्ञान, मनःपर्यय और केवलज्ञान कुल आठ हैं। इनमें मति-श्रुत, कुमति-कुश्रुत परोक्ष हैं क्योंकि इन्द्रिय एवं मन से उत्पन्न होते हैं तथा अवधि, विभंगावधि, मनः पर्यय और केवल ये प्रत्यक्ष हैं। इनका विषेश वर्णन तत्वार्थसूत्र आदि से जानना चाहिए।
आर्यिका ज्ञानमती जी के एतद्विशयक के निरूपण का हिन्दी अनुवाद यहां प्रस्तुत किया जाता है इससे आगम कथित सम्यग्ज्ञानों को भी कुन्दकुन्द स्वामी द्वारा विभाव ज्ञान कहने का स्पश्टीकरण हो जायेगा- ‘‘मिथ्यात्व और सासादन इन दो गुणस्थानों में तीनों अज्ञान रहते हैं। तीसरे मिश्र गुणस्थान में ज्ञान और अज्ञान (तीनों) मिश्रित रहते हैं।
असंयत सम्यग्दृश्टि गुणस्थान से लेकर बारहवें गुणस्थान तक मति, श्रुत और अवधि ये तीनों ज्ञान पाये जाते हैं। मनः पर्यय ज्ञान कुछ ऋद्धिसम्यक् वृद्धिंगत चारित्र वाले किन्हीं किन्हीं महामुनियों के ही होता है। (ये चारों ही ज्ञान सम्यग्ज्ञान होने से आगम अपेक्षा स्वभाव ज्ञान कहने में कोई दोश नहीं है।)
इनमें भावश्रुत ज्ञान तो पूर्ण स्वभाव ज्ञान केवलज्ञान का कारण कहा गया है। भावश्रुत ज्ञान द्रव्यश्रुतज्ञान के अवलम्बन से ही होता है अतः वह भी कार्यकारी है। स्वभाव का परम्परा कारण है। आ० कुन्दकुन्द देव के प्रस्तुत नियमसार प्राभृत की गाथा संख्याक 18 निम्न प्रकार है-
कत्ता भोत्ता आदा पोग्गलकम्मस्स होदि ववहारा।
कम्मजभावेणादा कत्ता भोत्ता दु णिच्छयदो।। 18।।
अर्थ – व्यवहार नय से आत्मा पुद्गल कर्मों का कर्ता भोक्ता होता है। किन्तु निष्चय नय से आत्मा कर्म से उत्पन्न हुए भावों (भाव कर्म) का कर्ता होता है। (यहां निष्चय नय से अषुद्ध निष्चय नय ग्रहण करना चाहिए)। यहां यह ज्ञातव्य है कि अध्यात्म में अषुद्ध निष्चय को व्यवहार ही निरूपित किया गया है। कुन्दकुन्द के टीकाकारों का मन्तव्य भी ऐसा ज्ञात होता है। किन्तु (अध्यात्म में भी) उपरोक्त गाथा में आचार्य कुन्दकुन्द ने रागद्वेश आदि कर्मज भावों के कर्तव्य को निष्चय से बताया है इससे विदित होता है कि आगम भाशा में जो द्रव्यार्थिक नय के शुद्ध और अषुद्ध दो भेद किए गये हैं, उनमें अषुद्ध द्रव्यार्थिक को अषुद्ध निष्चय नय के रूप में निष्चय नय ही मान्य किया गया है क्योंकि कर्मज भावों को आत्मा तन्मय होकर ही करता है।
वह तद्रूप परिणमन सत्यार्थ है भले ही त्रैकालिक तादात्म्य न हो। वर्तमान में कतिपय निष्चय पक्ष व्यामोही जन भ्रम से शुद्ध निष्चय नय के विशय को ही सत्यार्थ मानकर अपने को कर्म का अकर्ता, अभोक्ता मानकर स्वयं का तथा औरों को भी पापपंक में डुबो रहे हैं उन्हें उपरोक्त गाथा का लक्ष्य स्वीकार करना चाहिए।
पू० माता जी ने इस प्रकरण को स्पश्ट और पुश्ट करने हेतु गुणस्थानों में कर्म-कत्र्तृत्व अर्थात् बन्ध और भोक्तृत्व अर्थात् उदय का वर्णन प्रस्तुत गाथा की टीका में किया है जो अति उपयोगी है। माता जी की दूरदर्षिता यहां परिलक्षित होती है। यहां हम विस्तार भय से मुक्त होकर उनकी गोम्मटसार सिद्धान्तानुसार टीका का हिन्दी अनुवाद-गुणस्थान प्रकरण अक्षरषः प्रस्तुत करते हैं-
-सत्तरसेकग्गसयं चउसत्ततरि सगट्ठि तेवट्ठी।
बंधा णवट्ठवण्णा दुवीस सत्तारसेकोघे।।
गाथार्थ :- ‘‘यह जीव गुणस्थानों में पहले से लेकर क्रम से 117, 101, 74, 77, 67, 63, 59, 58, 22, 17, 1, 1, 1 और 0 इस तरह कर्म को बांधता है (कर्म का कर्ता होता है)। खुलासा इस प्रकार है- मिथ्यात्व गुणस्थान में 117 का बंध है, सासादन में 101 का, मिश्र में 74 का, असंयत सम्यग्दृश्टि में 77 का, देषविरत में 67, प्रमत्त संयत में 63 का, अप्रमत्त संयत में 59 का, अपूर्वकरण में 58 का, अनिवृत्तिकरण में 22 का, सूक्ष्मसाम्पराय में 17 का, उपषान्तमोह, क्षीणमोह और सयोगकेवली इन तीन गुणस्थानों में एक मात्र 1 सातावेदनीय प्रकृति का बन्ध करता है (अयोग केवली के बन्ध का अभाव है।)
और तो क्या आठवें गुणस्थानवर्ती महामुनि श्रेणी में चढ़कर भी 58 प्रकृतियों का बन्ध कर रहे हैं।
शंका:- वे कौन सी प्रकृतियां हैं?
समाधान :- ये 58 प्रकृतियां बंधती रहती हैं।
| 1- निद्रा | 2- प्रचला | 3- तीर्थंकर | 4- निर्माण |
| 5- प्रषस्त विहायोगति | 6- तैजस | 7- कार्माण | 8- आहारक शरीर |
| 9- आहारक अंगोपांग | 10- समचतुरस्र संस्थान | 11- देवगति | 12- देवत्यानुपूर्वी |
| 13- वैक्रियक शरीर | 14- वैक्रियक अंगोपांग | 15- स्पर्ष | 16- रस |
| 17- गन्ध | 18- वर्ण | 19- अगुरूलघु | 20- उपघात |
| 21- परघात | 22- उच्छ्वास | 23- त्रस | 24- बादर |
| 25- पर्याप्त | 26- प्रत्येक “शरीर | 27- स्थिर | 28- “ाुभ |
| 29- सुभग | 30- सुस्वर | 31- आदेय | 32- हास्य |
| 33- रति | 34- भय | 35- जुगुप्सा | 36- पुरुशवेद |
| 37- संज्वलन क्रोध | 38- संज्वलन मान | 39- संज्वलन माया | 40- संज्वलन लोभ |
| 41- मतिज्ञानावरण | 42- श्रुतज्ञानावरण | 43- अवधि ज्ञानावरण | 44- मनःपर्यय ज्ञानावरण |
| 45- केवल ज्ञानावरण | 46- चक्षुर्दर्षनावरण | 47- अचक्षुर्दर्षनावरण | 48- अवधि दर्षनावरण |
| 49- केवल दर्षनावरण | 50- दानान्तराय | 51- लाभान्तराय | 52- भोगान्तराय |
| 53- उपभोगान्तराय | 54- वीर्यान्तराय | 55- यषस्कीर्ति | 56- उच्चगोत्र |
| 57- पचेन्द्रिय जाति | 58- सातावेदनीय |
यह नाना जीवों की अपेक्षा कथन है। इसी प्रकार वीतराग छद्मस्थ महामुनि जोकि यथाख्यात चारित्र को प्राप्त कर चुके हैं ऐसे वे उपषान्तकशाय, क्षीणकशाय, गुणस्थानवर्ती तथा सयोग केवली भगवान, इनके भी एक सातावेदनीय का बन्ध होता रहता है। इसलिए ये जीव अपने अपने गुणस्थान के योग्य पुद्गल कर्म प्रकृतियों के कत्र्ता होते हैं। उसी प्रकार पुद्गल कर्मों के भोक्ता भी हैं, यहां भी माता जी ने निम्न गाथा उद्धृत कर निरूपण किया है-
सत्तरमेक्कार खचदुसहियसयं सगिगिसीदि छदु सदरी।
छावट्ठि सट्ठि णवसगवण्णास दुदारू वारूदया।।
अर्थ – मिथ्यादृश्टि गुणस्थान से लेकर अयोग केवली पर्यन्त जीव उन गुणस्थनों में क्रमषः 117, 111, 100, 104, 87, 81, 76, 72, 66, 60, 59, 58, 42 और 12 प्रकृतियों के उदय का अनुभव करते हैं। इसलिए ये सभी जीव अपने अपने गुणस्थान के योग्य उदय में आये हुए कर्मों के भोक्ता कहलाते हैं। यह सब कथन व्यवहार नय की अपेक्षा ही है।
’’ यही बात अ० कुन्दकुन्द स्वामी ने मूल गाथा में कही है ‘ववहारा’ शब्द का प्रयोग किया है। स्याद्वाद चन्द्रिका की इसी गाथा क्रमांक 18 की विस्तृत टीका में कर्तृत्व और भोक्तृत्व को सिद्ध करने हेतु माता जी ने सम्यक् रूप से स्पश्टीकरण दिया है। जीव इन उभय भावों से गुणस्थान परिपाटी से किस प्रकार मुक्त होता जाता है यह खुलासा करते हुए माता जी ने भाव व्यक्त किया है कि यह आत्मा जब तक मिथ्यादृश्टि है तब तक एकान्त से उनका (पुद्गल कर्मों का) कर्ता और उनके फलों का भोक्ता है। यह कर्तृत्व और भोक्तृत्व निमित्त मात्र से ही है उपादान रूप से नहीं, क्योंकि वह पुद्गल कर्म रूप परिणमन नहीं करता।
उपादान रूप से तो परिणमन करने वाले को ही कर्ता कहा जाता है। जोकि निष्चय नय का विशय है। जब यही जीव सम्यग्दृश्टि हो जाता है तब नय विभाग से अपने को पुद्गल कर्मों का कथंचित् कर्ता और भोक्ता मानता है वह शुद्ध निष्चय नय से तो ”मैं पर के कर्तृत्व और भोक्तृत्व से “शून्य हूँ।“ ऐसा चिंतवन करता है।
जब वही अप्रमत्त आदि गुणस्थानों में चढ़ता है, तब “शुभ-अषुभ मन, वचन, काय के व्यापार से रहित होने के कारण शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव से परिणमन करता हुआ वहां पर बुद्धिपूर्वक कर्ता, भोक्तापने का परिहार करता है अर्थात् वहां ध्यान में बुद्धिपूर्वक कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं रहता है। पुनः सूक्ष्म साम्पराय गुणस्थान के ऊपर यह कर्मों का कर्तृत्व भोक्तृत्व संभव ही नहीं क्योंकि आगे सम्पूर्ण मोहनीय कर्म के उदय का अभाव है अथवा पुद्गल कर्मों का कर्तापना रागद्वेशादि भावों के अभाव में संभव नहीं है। छठे गुणस्थान तक बुद्धिपूर्वक रागद्वेश आदि भाव है, वहां तक कर्तृत्व भी घटता है।
आगे सूक्ष्मसाम्पराय नामक दसवें तक बुद्धिपूर्वक रागद्वेश आदि का अभाव है और कशाय के उदय का सद्भाव है। अतः कथंचित् कर्तृत्व है किन्तु आगे के गुणस्थानों में कशाय नहीं रहते हैं। केवली भगवान के भी साता वेदनीय प्रकृति का बन्ध होता रहता है। अतः वहां उनके भी कर्म का कर्तृत्व है, किन्तु वह उपचार मात्र से ही है।
(एक समयवर्ती स्थिति मात्र है)। इसी प्रकार साता असाता आदि शुभ-अषुभ कर्मों के उदय से हुए सुख दुखों का भोक्तापन अर्थात हर्श विशाद आदि रूप फल का अनुभव करना छठे गुणस्थान तक ही है। आगे अप्रमत्त आदि गुणस्थानों में मोहनीय के रति अरति से होने वाले रागद्वेशादि का अभाव हो जाने से वहां वे महामुनि निर्विकार स्वसंवेदन ज्ञान के बल से रागरहित अपनी आत्मा से उत्पन्न हुए सुख का अनुभव करते हैं।
इसलिए वहां बुद्धिपूर्वक कर्मों का भोक्तृत्व नहीं घटता है। हां, सूक्ष्मसाम्पराय गुणस्थान पर्यन्त उन मुनियों के कथंचित् अबुद्धिपूर्वक कर्मफल भोक्तृत्व घटित होता है, क्योंकि वहां पर भी सूक्ष्म लोभ का सद्भाव है। इसके आगे क्षीणकशाय तक यद्यपि ज्ञान, दर्षन, सुख और वीर्य ये क्षायोपषमिक रूप हैं फिर भी उनमें एक देष रूप से आकुलता के अभाव लक्षण वाला सुख घटित होता है, किन्तु सर्वथा अनाकुलता लक्षण वाला अतीन्द्रिय सुख तो केवली भगवान को ही है।”
उपरोक्त प्रकार गुणस्थान परिपाटी से उक्त कर्तृत्व और भोक्तृत्व प्रकरण की पुश्टि प्रस्तुत टीका ग्रंथ में की गयी है। यह प्रयत्न इश्ट ही है क्योंकि अध्यात्म ग्रंथ के सार को ग्रहण करने हेतु यह आवष्यक है। माता जी के अनेकांतमय कर्तृत्व प्रकरण के समर्थन में यहां पं. बनारसीदास जी का छंद उद्धृत है-
जैसे सांख्यमती कहै अलख अकरता है सर्वथा प्रकार करता न होइ कबही।
तैसे जैनमती गुरूमुख एकांत पक्ष सुनि ऐसे ही मानै सो मिथ्यात्व तजै कबही।।
(समाधान) जौलों दुरमती तौलों करम को करता है सुमती सदा अकरतार कह्यो सबही।
जाके हिय ज्ञायक स्वभाव जग्यो जब ही सों सो तौ जगजाल सौं निरालो भयो तबही।।
यहां मैं अपनी बुद्धिगम्य दृश्टि से गुणस्थान शब्द के अर्थ को समास विग्रह एवं विभक्ति क्रम से स्पश्ट करना चाहूंगा यह उपयोगी होगा।
1. गुण एव स्थानं गुणस्थानं
प्रथमा विभक्ति की दृश्टि से गुण अर्थात् विषेशता ही स्थान है अर्थात् जितना गुणों में अंतर होगा उतने ही स्थान या पद घटित होंगे (दर्जे या क्लास)। इस दृश्टि से जीवों के परिणाम अनुसार गुणस्थान प्राप्त होते हैं जोकि लोकाकाष प्रदेष प्रमाण असंख्यात हैं। भले ही परिणामों की सामान्य समानता जीवों में परिलक्षित होती है किन्तु ‘णाणा जीवा णाणा कम्मं’ के अनुसार परिणाम, भाव, नाना प्रकार होने से गुणस्थान भिन्न भिन्न स्वीकार करना इश्ट है।
यहां गुणों से तात्पर्य दर्षन, ज्ञान, चारित्र, सुख, वीर्य आदि से है। मोटे तौर पर मोहनीय के आंषिक वा पूर्ण नाष से तथा योगों से आंषिक या पूर्ण समापन से जो गुण होता है वह ही गुणस्थान होता है। ‘‘गुणष्चासौ स्थानं गुणस्थानं’’ इस व्युत्पत्ति से जो स्थान गुण है वह गुणस्थान है। विषेशता रूप स्थान से यहां तात्पर्य है।
यहां विषेश यह है कि परमात्मत्व के प्रकरण में अनन्त चतुश्टय तो बारहवें गुणस्थान के बाद प्रकट होता है तथा “ चार गुण सूक्ष्मत्व, अगुरुलघुत्व, अवगाहनत्व और अव्याबाधत्व का अस्तित्व अयोगिकेवली के चरम समय के पष्चात् प्रकट होता है। चैदह गुणस्थानों का विभाजन मौटे तौर पर किया गया है। इन्हें जीवस्थान भी कहा है।
2- गुणं प्राप्नोति यद् स्थानं तद् गुणस्थानं
गुण को प्राप्त होने वाला स्थान गुणस्थान होता है। पूर्व से सभी जीव संसारी हैं, एक मिथ्यात्व में ही अवस्थित हैं। जैसे जैसे गुण को श्रेश्ठता को, विषेशता को प्राप्त होते जाते हैं वैसे वैसे स्थान अर्थात पद, श्रेणी, स्थिति परिवर्तित होती जाती है। ऊध्र्वता या उन्नति के सोपानों को यह जीव प्राप्त करता जाता है।
जिस गुण को जो जीव प्राप्त करता है उसका स्थान उसी अपेक्षा से बदलता जाता है। यद्यपि निष्चय नय से सभी जीवों के सत्ता में शक्ति अपेक्षा सभी गुण विद्यमान हैं परन्तु गुण की प्राप्ति से ही विकास होता है भले ही यह व्यवहार नय का विशय है।
3- गुणेन स्थानं गुणस्थानं
गुण के द्वारा जो स्थान होता है वह गुणस्थान है। बिना गुण के भेद के स्थान भिन्न कहना संभव नहीं है। यहां एक प्रासंगिक चर्चा करना इश्ट होगा। कतिपय जनों का यह मंतव्य है कि हमें मुनि को शुद्धोपयोग तो मानना इश्ट है साथ ही गृहस्थ के भी वैसा ही शुद्धोपयोग मुनि की अपेक्षा अल्पसमय के लिए संभव है मुनि अधिक देर तक शुद्धात्मानुभूति में ठहरते हैं, गृहस्थ थोड़ी देर के लिए। भाव दोनों का एक सा ही शुद्धोपयोग मय है।
इस भ्रम का निवारण करने हेतु सिद्धान्तमान्य गुणस्थान प्रक्रिया को स्वीकार करना होगा। सिद्धान्त में लिखा है- अर्थात् सम्यग्दृश्टि, पंचम गुणस्थानवर्ती श्रावक, महाव्रती, अनन्तानुबन्धी की विसंयोजना करने वाले, दर्षन मोह के क्षपक, चारित्र मोह का उपषम करने वाले, उपषान्त मोह वाले, क्षपक श्रेणी के आरोहक, क्षीण मोह और जिनेन्द्र भगवान (इन सबके परिणामों की विषुद्धि अधिक अधिक होने से) प्रति समय असंख्यात गुणी असंख्यात गुणी कर्म तिर्जरा करने वाले होते हैं।
यहां पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि जब निर्जरा अर्थात गुण के फलों में अंतर है तो भाव विषुद्धि रूप कारण में गुण का अंतर अवष्य है। फिर यह कहना कि चतुर्थ गुणस्थानवर्ती अव्रत सम्यग्दृश्टि और सातवें गुणस्थानवर्ती मुनि दोनों के ही समान शुद्धोपयोग है, अत्यंत भ्रामक है यह तो पहले ही कह आये हैं कि गृहस्थ के तो शुद्धोपयोग संभव ही नहीं है। प्रत्यक्ष, आगम, अनुमान तीनों प्रमाणों से ही यह सिद्ध है। मुनि के भी छठवें गुणस्थान में संभव नहीं है तथा सातवें में भी श्रेणी आरोहण के सम्मुख सातिषय अवस्था में ही है।
4- गुणाय स्थानं गुणस्थानं
चतुर्थी विभक्ति अथवा सम्प्रदान कारक के पक्ष में जो गुण के लिए, गुण हेतु स्थान है वह गुणस्थान है। ठीक ही है। आत्म विकास के पथ का पथिक मोहनीय कर्म पर विजय प्राप्त करता हुआ एवं अयोग की ओर बढ़ता हुआ लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है। इस विकास के क्रम में जिन श्रेणियों के लिए, पदों के लिए अग्रसर होता है वे ही गुणस्थान हैं।
यहां यह ज्ञातव्य है जो गुणस्थान पहले साध्य रूप में होता है, प्राप्ति के पष्चात वह साधन रूप में हो जाता है। दूसरा व तीसरा गुणस्थान इसका अपवाद है, ये दो गुणस्थान गिरने की अपेक्षा हैं एवं दषम गुणस्थान से क्षपक को बारहवां गुणस्थान प्राप्त होता है। उपषम श्रेणी के प्रकरण में यह ज्ञातव्य है कि ग्यारहवें गुणस्थान में सत्ता में विद्यमान एवं उपषमित मोहनीय कर्म के उदय में आ जाने से महामुनि भी अपेक्षित निम्न स्थानों में आ जाता है।
अतः ये दूसरे, तीसरे व ग्यारहवें गुणस्थान श्रेश्ठ गुण के लिए कारण न होकर निम्न गुण के हेतु होते हैं। यहां एक प्रष्न संभावित है कि क्या प्रथम गुणस्थान मिथ्यात्व, चतुर्थ गुणस्थान अविरत सम्यग्दृश्टि के लिए होता है अथवा कारण होता है इसका समाधान यह है कि कारण मानने में कोई दोश नही है जब मिथ्यात्व गुणस्थान में मिथ्यात्व की प्रकृतियां निर्बल हो जाती हैं तथा कशाय अनन्तानुबन्धी से विसंयोजित होता है तब करण आदिलब्धियों की स्थिति से चतुर्थ गुणस्थान प्राप्त हो जाता है अतः मन्द रूप में मिथ्यात्व गुणस्थान कारण होता है।
5- गुणात् स्थानं गुणस्थानं
== गुण से अन्य गुण को प्राप्त होने से गुणस्थान कहलाते हैं। एक स्थान छूटता है और अन्य स्थान पर पहुंचता है। जैनी नीति भी ग्रहण और त्याग की है अर्थात् एक स्थिति जब प्राप्त होती है तो अन्य छूटती है। गुणस्थान परिवर्तन भी अवष्यम्भावी है। हां प्रथम गुणस्थान में जो जीव का अनादि अनन्त निवास अभव्य या दूरान्दूर भव्य की अपेक्षा है वह इसका अपवाद है। वैसे प्रथम गुणस्थान में भी जघन्य, मध्यम और उत्कृश्ट अंषों के भेद हैं उनमें भी परिवर्तन होता है। गुणस्थानों के चैदह भेद सामान्य से है विषेश की अपेक्षा तो अनन्त भेद हैं।
6- गुणस्य स्थानं गुणस्थानं
गुण का जो स्थान है वह गुणस्थान है। सम्यक्त्व और चारित्र गुण की परिणतियां ही गुणस्थान हैं। मोह और योग की अपेक्षा सहित जो भाव हैं वे गुणस्थान हैं। मोह और योग के अन्तर की अपेक्षा इनमें अन्तर है।
7- गुणेशु स्थानं गुणस्थानं
जब गुणों को अधिकरण रूप में स्वीकार करते हैं तो यह व्युत्पत्ति घटित होती है। जिस मंजिल पर, सोपान पर, श्रेणी पर जीव स्थित होता है वह गुणस्थान है। भूमि या भूमिका शब्द भी इस हेतु उपयोगी होता है। हमने अन्य प्रकरण में पूर्व में समयसार कलष का एक छंद उद्धृत किया था जिसमें ‘श्रयति भूमिमिमां स एकः’ शब्द श्रयति के प्रयोग से ‘गुणस्थान’ पद हेतु ‘भूमि’ पद प्राप्त होता है। गुणस्थान जीव से कथचित् भिन्न है कथंचित् अभिन्न है।
यह शुद्ध द्रव्यार्थिक या शुद्ध निष्चय नय एवं पर्यायार्थिक आदि नयों से योजनीय है। हां गुण के बिना किसी स्थान का अस्तित्व नहीं है तथा स्थान के बिना भी गुण आकाष कुसुम ही सिद्ध होगा। यह कथन संसारी जीवों की अपेक्षा है। सिद्ध भगवान गुणस्थानातीत है। नियमसार अध्यात्म ग्रंथ है इसमें अध्यात्म का षिखर वर्णन है जो सापेक्ष नयों से समझने योग्य है।
इसे सही रूप से हृदयंगम करने हेतु गुणस्थान मार्गणास्थान स्वरूप को ‘शट्खण्डागम, धवला और गोम्मटसार आदि ग्रंथों से समझना आवष्यक है। स्याद्वाद चन्द्रिका में इसी हेतु अपेक्षित उन ग्रंथों के सारांष को लिए गुणस्थान निरूपण किया गया है। यह वर्णन वास्तव में नियमसार रूप करण्ड को खोलने हेतु कुंजी ही है। पू० माता जी ने हमें प्रदान कर पात्रता प्रदान की है।
प्रौढ़ आगम अभ्यासियों के लिए अथवा संक्षेप रूचि प्रज्ञावान पाठकों के लिए तो आचार्य पद्मप्रभ मलधारि देव की तात्पर्यवृत्ति ही पर्याप्त हो सकती थी किंतु जिनको न तो नय, भाशा, व्याकरण, सिद्धान्त का ज्ञान है न जिनके पास शक्ति और समय है जो पूर्वोक्त सिद्धान्त ग्रंथें का पठन कर समझ सकें, उनके लिए चन्द्रिका में सरलता से, सुगमता से सिद्धान्त का रहस्योद्घाटन कर आर्यिका ज्ञानमती जी ने श्रेश्ठ ज्ञानोपकरण प्रदान किया है “लाघ्य कार्य किया है।
अध्यात्म शस्त्रों में सर्वोत्कृश्ट उपादेय तत्व मोक्ष की,, भाव मोक्ष एवं द्रव्य मोक्ष के रूप में चर्चा की गयी है। द्रव्य से भाव और भाव से द्रव्य इस प्रकार कार्य कारण भाव उभय रूपों में जिनागम में पाया जाता है। किन्हीं परिस्थितियों में भाव का कारण द्रव्य है और किन्हीं में द्रव्य का कारण भाव है जैसे द्रव्य कर्म से भाव कर्म होता है तथा भाव कर्म से द्रव्य कर्म की उत्पत्ति होती है।
कर्म परम्परा बीज से वृक्ष तथा वृक्ष से बीज की भांति है। अन्यंत्र द्रव्यलिंग से भाव लिंग की उत्पत्ति का प्रसंग है भावलिंग से द्रव्यलिंग की प्रसूति नहीं। एवं मोक्ष प्रकरण में भाव मोक्ष के अनन्तर द्रव्य मोक्ष होता है अतः भाव मोक्ष कारण है, द्रव्य मोक्ष कार्य है। द्रव्य मोक्ष, भाव मोक्ष का कारण सिद्ध नहीं होता।
स्याद्वाद चन्द्रिका में टीकाकत्र्री ने भाव मोक्ष की उत्पत्ति, परम्परा तथा उसके कार्यरूप द्रव्य मोक्ष का गुणस्थान परिपाटी से बड़ा समीचीन एवं प्रासंगिक रूप में वर्णन किया है प्रस्तुत निम्न टीकांष पर दृश्टिपात करणीय है- अयं सम्यग्दृश्टिर्संयतो देषसंयतो वा यथोक्तं ‘ाड्दव्यं पञचास्तिकायं च अवितथं ज्ञात्वा श्रदधत्ते
, पुनः सकलचारित्रबलेन निजान्तःषक्तिं विकासयन् निर्विकल्पसमाधिमारुह्य सर्वथा मोहनीयं निर्मूल्य अन्तबर्हिग्र्रन्थाभ्यां मुक्तो निर्ग्रन्थो भूत्वा क्षीणकशायन्त्यसमये घातिकर्माणि हत्वा भावरूपेण पुद्गलकर्मभ्य पृथग्भूत्वा भावमोक्षं लभते, तदनन्तरं अयोगिकेवलिचरमसमये पौद्गलिक“ारीरादिसंयोगं सर्वतः व्यक्त्वा द्रव्यमोक्षं लभते।
तदानीमपि धर्मादीनि चतुर्द्रव्याणिगतिस्थित्यादि रूपेण उपकुर्वन्ति किन्तु जीवस्य काचिद् हानिर्न जायते।’’
अर्थ – यह असंयत सम्यग्दृश्टि अथवा देषव्रती इन आगम कथित छहों द्रव्यों और पञचास्तिकाय को वास्तविक रूप से जानकर श्रद्धान करता है। पुनः सकल चारित्र के बल से अपनी अन्तरंग शक्ति को प्रकट करता हुआ निर्विकल्प समाधि में पहुंचकर मोहनीय का निर्मूलन करके अन्तरंग बहिरंग ग्रंथियों से रहित निग्र्रन्थ होकर क्षीणकशाय गुणस्थान के अंतिम समय में घातिया कर्म का नाष करके भाव रूप से पुद्गल कर्मों से पृथक होकर भाव मोक्ष को प्राप्त कर लेता है।
अनन्तर अयोगिकेवली के चरम समय में पौद्गलिक शारीर आदि के संयोग को सब प्रकार से छोड़कर द्रव्य मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। तब उस समय उन्हें भी ये धर्मादि चार द्रव्य गमन करने, ठहरने, अवकाष प्राप्त करने और वत्र्तना करने आदि रूप से उपकार करते हैं किन्तु जीव की कुछ हानि नहीं होती है। उपरोक्त सारभूत वर्णन व गुणस्थान प्रकरण से पुश्टि का फलितार्थ निम्न है।
1- सात तत्व, नौ पदार्थ, ‘शट् द्रव्य, पंचास्तिकाय को वास्तविक रूप से जानकर श्रद्धान करने से सम्यग्दर्शन होता है केवल शाब्द से जानकर नहीं। कुछ लोग केवल इन तत्वार्थों के नाम जान लेने भर से अपने को भ्रम से सम्यग्दृश्टि मानकर संतुश्ट हो जाते हैं यह मान्यता ठीक नहीं है।
2- आगम में कथित स्वरूप से तत्वार्थों का श्रद्धान करना उचित है यद्वा तद्वा नहीं जैसे धर्म द्रव्य की परिभाशा करते हुए कहा जाता है कि जब जीव अपनी योग्यता से गमन करता है तब धर्म द्रव्य निमित्त होता है, मात्र उपस्थित रहता है सहायता नहीं करता आदि आदि। किन्तु इसके विपरीत आगम में सर्वत्र धर्म द्रव्य को जीव पुद्गलों के चलने में सहायक माना गया है कहीं भी निमित्त कारण की अकिंचित्करता नहीं है आगम प्रमाण दृश्टव्य है-
‘‘गइपरिणयाणधम्मो पुग्गलजीवाण गमण सहयारी।
तोयं जह मच्छाणं अच्छंता णेव सो णेई।।
गति परिणत जीव पुद्गलों को गमन में धर्म द्रव्य सहकारी है जैसे मछली के चलने में जल सहकारी है बिना जल के मछली चल नहीं सकती। हां बिना गति परिणत द्रव्य को धर्म गमन नहीं कराता। वह उदासीन निमित्त कारण है। जिस परम ब्रह्म (षब्द ब्रह्म) के अर्थ कर्ता आप्त हैं, शब्दात्मक या ग्रंथात्मक गूंथने वाले गणधरदेव हैं एवं आचार्यों, मुनियों ने परम्परा से जिसका उपदेष दिया है वह आगम कहलाता है, वही प्रमाण है। उसी अनुसार अपनी श्रद्धा बनाना चाहिए।
अन्यथा मिथ्यात्व की सत्ता नहीं छूटेगी।
3- जब तक जीव सकल चारित्र धारण कर ‘ गुणस्थान प्राप्त नहीं करता एवं वाह्य परित्याग (परिग्रह त्याग) नहीं करता, संसार, “ारीर, भोगांे से विरक्त होकर मुनिदषा अंगीकार नहीं करता तब तक रागद्वेश परिहरण हेतु उसकी अन्तरंग प्रकट नहीं होती। अर्थात् निर्बलता के कारण अंतरंग परिग्रहों का त्याग संभव नहीं होता। इस विशय में आ० अमृतचंद्र सूरि जी ने सुंदर शब्दों में प्रभावक वर्णन किया है जिससे माताजी के पूर्वोक्त वर्णित विशय का समर्थन होता है-
इत्थं परिग्रहमपास्यसमस्तमेवसामान्यतः स्वपरयोरविवेक हेतुं।
अज्ञानमुज्झितमना अधुना विषेशात्भूयस्तमेव परिहर्तुमयं प्रवृत्तः।।
इस प्रकार सामान्य रूप से ही निज पर के अज्ञान के कारणभूत वाह्य समस्त परिग्रह का त्याग कर मुनि अज्ञान के नाष करने के लिए पुनः परिग्रह के दूसरे रूप अन्तरंग परिग्रह का त्याग करने को उद्यत हुआ है प्रवृत्त हुआ है।
4- बारहवें क्षीणकशाय गुणस्थान में निग्र्रन्थ संज्ञा प्राप्त होती है।
5- भाव मोक्ष का तात्पर्य घातिया कर्मों का नाष होने पर राग रहित परिणाम एवं साक्षात् सर्वज्ञ रूप स्थिति, केवली अवस्था, तेरहवां गुणस्थान से लेना चाहिए। न कि भ्रम से मोक्ष प्राप्ति का भाव (इरादा) करने को ही भाव मोक्ष मान लिया जाय। यह बहुत हानिकारक विष्वास है, निगोदादि दुर्गति का कारण है। वर्तमान में ही अपने को समयसार मान लेना घोर अज्ञान है। सर्वत्र निष्चय, वह भी शुद्ध निष्चय नय नहीं लगाया जाता। पर्याय को पर्यायार्थिक नय से देखा जाता है। सम्यग्दर्शन होने मात्र से भाव मोक्ष की कल्पना भव-भव में भटकाने वाली है।
6- भाव मोक्ष की अवस्था में पुद्गल कर्मों का प्रभाव आत्मा के शुद्ध चेतना परिणाम को विकृत नहीं कर पाता। इसी हेतु अरिहन्त को भी परमात्मा संज्ञा प्राप्त है, अघातिया कर्मों का उदय तो प्रतिजीवी गुणों को घातता है जिससे अनुजीवी गुण प्रभावित नहीं होते। वे शुद्ध परिणाम रूप ही हैं। हां इतना अवष्य है कि अघातिया कर्मों का उदय अति न्यून रूप से मात्र चारित्र गुण में कुछ दूशण उत्पन्न करता है वह यहां नगण्य ही है।
7- स्याद्वाद चन्द्रिकाकत्र्री माता जी ने आगमानुकूल ही निर्दिश्ट किया है कि जीव के पुद्गलमय कर्म का संयोग वास्तविक है मात्र कथन रूप नहीं है तथा अयोग केवली गुणस्थान के अन्त्य समय में पौद्गलिक कर्मों से पृथक होना ही द्रव्य मोक्ष है तत्वार्थ सूत्र में कहा भी है-
‘‘बन्धहेत्वभावनिर्जराभ्यां कृत्स्न कर्म विप्रमोक्षो मोक्षः।’’
बन्ध के कारणों का अभाव और निर्जरा द्वारा संपूर्ण कर्मों से पृथक होना ही मोक्ष है।’’ यह द्रव्य मोक्ष की ही परिभाशा है।
8- मुक्त होने पर भी, गुणस्थानातीत अवस्था होने पर भी धर्म, अधर्म, आकाष, काल द्रव्य जीवों का उपकार करते हैं किन्तु इन पर द्रव्यों के उपकार से जीव को हानि नहीं है। परद्रव्यों के उपकारों की स्थिति में भी (निमित्त के कार्यकारी होकर प्रभाव डालने पर भी) जीव की परतंत्रता नहीं है।
9- गुणस्थान क्रम से ही अन्त्य विकास, चरम विकास होता है। अध्यात्म “ाास्त्रों को भी गुणस्थान के स्वरूप को परिपाटी से ही हृदयंगम करना चाहिए। इसी दृश्टि से माता जी ने अपेक्षित स्थलों पर करणानुयोग के अंगभूत गुणस्थानों की विवक्षा हमारे सम्मुख प्रस्तुत की है।
यही कारण है कि पं. बनारसीदास जी ने समयसार के अध्यात्म रस के हार्द खोलने हेतु समयसार नाटक में पृथक से गुणस्थान अधिकार समाविश्ट किया है ताकि श्रोता अध्यात्म के गूढ़ रहस्यों को आगमानुकूल समझ सकें। स्वयं भी पूर्व अवस्था में बनारसीदास जी समयसार के गूढ़ अध्यात्म को पढ़कर करणानुयोग से अनभिज्ञता के कारण एकान्तनिष्चयाभास से भ्रमित हो गये थे1।
पष्चात अच्छी होनहार के कारण पांडे रूपचंद्र के द्वारा गोम्मटसार व्याख्यान को स्वीकार करने से वे यथार्थ मर्म समझ सके थे। स्याद्वाद चन्द्रिका में तो तत् तत् स्थलों पर ही गुणस्थान व्यवस्था को उन प्रकरणों को स्पश्ट करने हेतु उल्लिखित किया है, भूरि-भूरि नमन माता जी की दूरदृश्टि को।
नियमसार के परमार्थ प्रतिक्रमण अधिकार की गाथा क्रमांक 77 की व्याख्या के अंतर्गत स्याद्वाद चन्द्रिका में यह निरूपित किया गया है कि मुमुक्षु को यह भावना करना चाहिए कि कथंचित् व्यवहार नय की अपेक्षा से मैं नरक, तिर्य×च, मनुश्य, देव गति पर्याय से परिणत हँू और कथंचित् निष्चय नय की विवक्षा से मैं चतुर्गति रूप भाव से रहित शुद्ध चैतन्य स्वरूप हूं। इस प्रकार की भेद भावना उपयोगी है किन्तु इस भेद विज्ञान की सीमा है। परिस्थिति को गुणस्थान क्रम से स्पश्ट करते हुए पू० माता जी ने निम्न शब्दावली प्रयुक्त की है –
‘‘तात्पर्यमेतत्, ईदृक् भेदभावना विकल्परूपेण चतुर्थगुणस्थानात् ‘श्ठगुणस्थानं यावत् जायते। पुनः निर्विकल्पध्याने स्थित्वा मुनिरेभ्यः पृथगेव स्वात्मानं ध्यायति क्षीणकशायान्तं।
शुक्लध्यानबलेन केवलिनो भावरूपेण आभ्यो कतिभ्यः पृथक् भूत्वा गुणस्थानातीतावस्थायां द्रव्यरूपेणापि पृथग्भवन्ति।’’
तात्पर्य यह है कि कथंचित् मैं मनुश्यादि गति भाव में परिणत हूं क्योंकि व्यवहार नय की अपेक्षा है। कथंचित् मैं गति भाव से रहित शुद्ध चिन्मय स्वरूप हूँ क्योंकि इसमें निष्चय नय की विवक्षा है। पुनः निर्विकल्प ध्यान में स्थित होकर मुनिराज इनसे पृथक ही अपनी आत्मा का ध्यान करते हैं।
क्षीण कशाय गुणस्थान तक यह ध्यान होता है उसके आगे केवली भगवान भाव रूप से इन चारों गतियों से पृथक होकर गुणस्थानातीत सिद्ध अवस्था में द्रव्य रूप से भी इनसे पृथक हो जाते हैं।“ माता जी ने यहां स्पश्ट किया है कि जैन धर्म में विकास का क्रम भेद से अभेद की ओर है, सविकल्प से निर्विकल्प की ओर है।
व्यवहार से निष्चय की ओर है। गुणस्थान परम्परा में क्रमषः साधक इसी प्रकार आरोहण करता है। जितना अभेद की ओर बढ़ता है उतना ही गुणस्थान बढ़ता जाता है गुणस्थान तो उस भेदाभेदत्व का मापक है। अभेद का वास्तविक पात्र तो मुनि ही है। निष्चयाभासी जिस भेद विज्ञान चर्चा, अर्थात आत्मा शरीर से भिन्न है, को ही निष्चय मान लेता है जबकि यह तो प्रत्यक्ष ही भेद रूप एवं सविकल्प दषा ही है।
इस तथ्य को स्वीकार कर निर्विकल्प समाधि की सिद्धि हेतु मुनिदषा अंगीकार कर भेदाभ्यास करना योग्य है। यह व्यवहार का आश्रय कल्याण का हेतु है हानिकर नहीं, क्योंकि यह निष्चय का साधक है। सिद्धान्त ग्रंथों में काय-वचन-मन गुप्तियों को संवर का कारण कहा गया है। आचार्य जयसेन स्वामी ने भी प्रवचनसार टीका में व्यवहार और निष्चय गुप्तियों का कथन किया है। यथा मन, वचन, काय की बुरी परिणति से हटकर, समीचीन भली प्रवृत्ति को व्यवहार गुप्ति कहा है। यहां विशय कशाय से आत्मा को गुप्त रखना, बचाना अभीश्ट है। इसी से गुप्तियों के तीन भेद संभव है।
निष्चय गुप्ति संपूर्ण प्रकार से तीनों योगों की प्रवृत्ति रोकने से ध्यान रूप होती है। इस विशय को स्याद्वाद चन्द्रिका में सुश्ठु विवेचित किया गया है। स्पश्ट अर्थ अवधारण करने हेतु गुणस्थान की विवक्षा भी संयोजित की है। ग्रंथ के पृश्ठ संख्या 258 पर गाथा संख्या 88 की टीका का हिन्दी अनुवाद अवलोकनीय है- ‘‘यहां पर निष्चय नय प्रधान गुप्तियां ग्रहण की गई हैं, जोकि निर्विकल्प समाधि लक्षण निष्चय रत्नत्रय की एकाग्र परिणति में ही सिद्ध होती है।
उस समय इन तीन गुप्तियों से सहित साधु अंतर्मुहूर्त मात्र से ही घाति कर्म का नाष कर देते हैं अथवा कदाचित् वे महामुनि छठवें गुणस्थान में आकर बिहार करते हैं तो अवधिज्ञानी अथवा मनःपर्यय ज्ञानी होकर रहते हैं जैसे कि रानी चेलनी के द्वारा संकेत किए अवधिज्ञानी महामुनि का उदाहरण प्रसिद्ध है।……………….इसलिए व्यवहार गुप्तियों से स्वषुद्धात्मा की भावना भाते हुए महर्शियों को अप्रमत्त गुणस्थान से प्रारंभ करके क्षीणकशाय गुणस्थान तक ये गुप्तियां होती हैं।
निष्चय प्रतिक्रमण स्वरूप निग्र्रन्थ दिगम्बर महामुनि उन्हीं गुप्तियों में रहते हुए समरसी भाव से परिणत परमाल्हादमय पीयूश का आस्वाद लेते हुए परम तृप्त होकर मोह रूपी अग्नि से संतप्त सर्वजगत के जीवों को तर्पित करते हैं, ऐसा जानकर दोनों प्रकार की ही गुप्तियों को प्राप्त करने की इच्छा रखते हुए तेरह प्रकार के चारित्रधारी मुनियों की सतत् भक्ति करना उचित है।’’
यहां यह ज्ञातव्य है कि गुप्ति का अधिकारी मुनि है उसको सविकल्प अवस्था में व्यवहार गुप्ति एवं निर्विकल्प अवस्था में निष्चय गुप्ति कहा है, जो कि निष्चय प्रतिक्रमण रूप होती है। व्यवहार गुप्ति साधन है और निष्चय गुप्ति साध्य है यह निर्धारण करना चाहिए। इसी हेतु गुणस्थान निरूपण भी किया जाता है जोकि पूर्वापर रूप में साधन साध्य हाता है।
जय धवला टीका के प्रारंभ में आ० वीरसेन स्वामी ने निरूपित किया है कि प्ररूपणायें बीस हैं, उनसे जीव के स्वरूप को भली भांति समझना चाहिए। इस संबंध की गाथा हम इस अध्याय के प्रारंभ में ‘गुणजीवा पज्जत्ती’ आदि प्रस्तुत कर चुके हैं। आषय यह है कि गुणस्थान, जीवस्थान, पर्याप्ति प्राण, संज्ञा, 14 मार्गणा और उपयोग ये बीस प्ररूपणायें हैं।
इससे स्पश्ट सिद्ध होता है कि गुणस्थान निरूपण संदेह निर्वारणार्थ एवं स्पश्ट अर्थ-अवधारणार्थ अनिवार्य है इसी लक्ष्य से स्याद्वाद चन्द्रिका में भी लेखिका महोदया ने अपेक्षित विशय को स्पश्ट करने हेतु गुणस्थान क्रम को यथास्थान उल्लिखित किया है। ध्यान प्ररूपक शस्त्रों में कहा गया है, ‘‘मनः एवं मनुप्याणां कारणं बन्ध- मोक्षयोः।’’ – मन ही मनुश्यों के लिए बन्ध और मोक्ष का कारण है।
जब मनुश्य के मन की परिणति अषुभ होती है तो आत्र्त और रौद्र ध्यान होता है। ये दोनों ध्यान अषुभ हैं और संसार के कारण हैं। जब मन की परिणति एकाग्र रूप में “शुभ और श्रेयस्कर होती है तो धम्र्य या “शुक्लध्यान होता है ये दोनों ध्यान मोक्ष के कारण हैं1। यह सब मन के द्वारा ही तो होता है।
ध्यानों की पात्रता विशयक भ्रामक चर्चायें प्रायः सुनने में आती हैं। “शस्त्रों से अनभिज्ञ कतिपय जन भ्रम से अपने को “शुक्लध्यानी और शुद्धपयोगी मान बैठते हैं। इन परिस्थितियों पर विचार कर पू० माता जी ने नियमसार की गाथा क्रमांक 89 की टीका करते हुए स्याद्वाद चन्द्रिका में पृश्ठ सं० 290 पर राजवात्र्तिक/अ० 9@37 एवं धवला पुस्तक 13@पृ० 74 के प्रामाणिक आधार पर गुणस्थान परिपाटी से प्रस्तुत प्रकरण को स्पश्ट किया है। वे पंक्तियां निम्न प्रकार हैं-
‘‘इतो विस्तरः – निदानं विहाय इश्टवियोगजानिश्टसंयोगजवेदनाजन्यं त्रिविधमपि आर्तध्यानं ‘श्ठगुणस्थान पर्यन्त संभवति।
हिंसानन्द्मिृशानन्दिचैर्यानन्दि- विशयसंरक्षणानन्दिरौद्रध्यानं, चतुर्विधमपि प×चमगुणस्थानपर्यन्तमेव न चागे्र।
धम्र्यध्यानं चतुर्थगुणस्थानादारभ्य सप्तमपर्यन्तम्।
सूक्ष्मसाम्परायनामदषमगुणस्थानपर्यन्तं वा परमागमे श्रूयते।
शुक्लध्यानं अश्टमगुणस्थानादेकाषमगुणस्थानाद्वा आरभ्य अयोगकेवलीनाम् भगवतां चरमसमयं यावत् जायते।
सम्प्रति दुश्शम काले शुक्लध्यानाभावात् धम्र्यध्याने एवं स्थातुं शक्यते।’’
आषय है कि निदान को छोड़कर इश्टवियोगज अनिश्ट संयोगज और वेदना जन्य ये तीनों ही आर्तध्यान छठे गुणस्थान पर्यन्त संभव है। हिंसानन्दि, मृशानन्दि, चैर्यानन्दि और विशय संरक्षणानन्दि (परिग्रहानन्दि) ये चारों प्रकार के रौद्रध्यान पंचम गुणस्थान तक हो सकते हैं आगे नहीं।
धम्र्य ध्यान चैथे गुणस्थान से प्रारंभ होकर सातवें गुणस्थान पर्यन्त होता है अथवा सूक्ष्म साम्पराय नामक दषवें गुणस्थान तक ही होता है ऐसा पट्खण्डागम सूत्र में कथन आया है। शुक्लध्यान आठवें गुणस्थान से अथवा ग्यारहवें गुणस्थान से लेकर अयोगकेवली भगवान के चरम समय पर्यन्त होता है। ‘‘वर्तमान दुश्शमकाल में शुक्लध्यान के नहीं होने से धम्र्यध्यान में ही स्थित होना संभव है। आ० कुन्दकुन्द ने कहा भी है-
भरहे दुक्खमकाले धम्मज्झाणं हवेइ साहुस्स।
तं अप्पसहावट्ठिदं ण हु मण्णइ सो वि अण्णाणी।।
भरतक्षेत्र में दुखमा (पंचम) काल में साधु के धर्मध्यान होता है वह आत्मस्वभाव में स्थित है उसे जो नहीं मानता है (ऐसा जो नहीं मानता है) वह अज्ञानी है।“ जब साधु के ही धर्मध्यान ही संभव है तो गृहस्थ के शुध्यान या शुद्धपयोग कहना हास्यास्पद है। आंख बन्द कर भ्रम से कुछ सफेद सफेद (षुक्ल) दिखाई पड़ने वाली वस्तु की कल्पना क्या शुक्लध्यान हो सकती है शुक्ल आदि वर्ण की वस्तु तो पुद्गल ही होती है, दिखाई तो पुद्गल दे उसे आत्मा का साक्षात्कार मान लेना घोर मिथ्यात्व है।
(ष्वेत आदि वर्ण तो पुद्गल के गुण हैं आत्मा के नहीं)। इस प्रकार ज्ञात होता है कि स्याद्वाद चन्द्रिका में गुणस्थान निरूपण से नियमसार प्राभृत का ही नहीं अपितु नियम अर्थात् रत्नत्रय का ही हार्द खोल दिया गया है। आ० कुन्दकुन्द देव कृत नियमसार में आषय ही रत्नत्रय प्रकाषन एवं प्रभावना ही है।
आगम में ध्यान के स्वरूप के साथ ही भावना (अनुपे्रक्षा) का स्वरूप वर्णित किया गया है। उत्तम संहनन आदि साधनों के अभाव में एकाग्र चिन्तानिरोध संभव न होने से भावना ही एक मात्र सहारा है। अभीश्ट अर्थ का पुनः पुनः दोलायमान चंचल मन के द्वारा चिंतन करना ही भावना कहलाती है। आचार्य शुभचन्द्र स्वामी ने ध्यान और भावना का अंतर स्पश्ट करते हुए ज्ञानार्णव में लिखा है,
एकाग्रचिन्तारोधो यस्तद्ध्यानं भावना परा।
अनुपे्रक्षार्थचिन्ता वा तज्ज्ञैरभ्युपगम्यते।। ज्ञानार्णव।।
जो एकाग्र चिन्तानिरोध रूप होता है वह ध्यान है इससे अन्य अनुप्रेक्षा अथवा अर्थचिन्ता को ध्यान के ज्ञानियों ने भावना कहा है। इस प्रकरण के यथार्थ अर्थ की पुश्टि करने हेतु गाथा सं. 96 की टीका में स्याद्वाद चन्द्रिका के अंतर्गत माता जी द्वारा गुणस्थानपरक विवेचन अति महत्वपूर्ण है। ध्यान दें,
‘‘इति ज्ञानी यथाजातरूपधारी मुनिः चिन्तयेत् ‘ाश्ठगुणस्थाने भावनां कुर्यात् सप्तमादिगुणस्थानेशु ध्यानपरिणतो एकाग्रचिन्तानिरोधलक्षणैकतानपरिणतिः च विद- ध्यात्।’’
इस प्रकार यथाजात रूपधारी ज्ञानी मुनि चिन्तवन करें, छठे गुणस्थान में भावना करे और सातवें आदि गुणस्थानों में ध्यान की परिणति में एक विशय में मन को रोकने रूप, एकाग्रता रूप ध्यान करें। यहां स्पश्ट है कि मोक्षोपयोगी ध्यान सातवें गुणस्थान से ही संभव है पहले नहीं। नियमसार की कारिका क्रमांक 130 के अंतर्गत मूल ग्रंथकार ने कहा है-
जो दु पुण्णं च पावं च भावं वज्जेदि णिच्चसा।
तस्स सामाइगं ठाई इदि केवलि सासणे।।
जो पुण्य और पाप रूप भाव को नित्य ही छोड़ देते हैं उन्हीं के स्थायी सामायिक होती है।’’ यह कथन निष्चय नय की अपेक्षा एवं साक्षात् मोक्ष मार्ग, निर्विकल्प ध्यान, वीतराग चारित्र अथवा वीतराग सामायिक का स्वरूप है। इसका स्याद्वाद चन्द्रिका का स्पश्टीकरण विषेश दृश्टव्य है।
यहां टीका का स्वोपज्ञ हिन्दी अनुवाद प्रस्तुत है- ‘छठे गुणस्थानवर्ती मुनियों के भी असाता, अरति, “ आदि अषुभ प्रकृ- तियों का बन्ध होता है। इसके ऊपर आठवें गुणस्थान के छठे भागपर्यन्त भी आहारक शरीर, आहारक अंगोपांग और तीर्थंकर रूप पुण्य प्रकृतियों का बन्ध सुना जाता है। चतुर्थ गुणस्थान से लेकर इस आठवें गुणस्थान तक शुभ प्रकृतियां बंधती रहती हैं।
कोई महामुनि उपषम श्रेणी में चढ़कर निर्विकल्प शुक्लध्यान को ध्याते हुए भी वहां पर आठवें गुणस्थान में तीर्थंकर प्रकृति का बन्ध करके आगे ग्यारहवें गुणस्थान तक जाकर पुनः चारित्र मोह के सूक्ष्म लोभ का उदय आ जाने पर वहां से उतरकर छठे गुणस्थान पर्यन्त वापस आ जाते हैं। वे मुनि उसी भव में या आगे के भव में तीर्थंकर प्रकृति का अनुभव करके धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करके सिद्धि कान्ता के पति हो जाते हैं।
भावार्थ :- कदचित् उसी जीवन में उनके तीर्थंकर प्रकृति का उदय आ सकता है ऐसे दो या तीन कल्याणक वाले तीर्थंकर विदेह क्षेत्र में ही होते हैं। यहां भरत और ऐरावत क्षेत्र में नहीं। यहां तो पांच कल्याणकों वाले तीर्थंकर ही होते हैं। (पृ०- 374) इस निरूपण से सिद्ध है कि पुण्य पाप का परित्याग गुणस्थान क्रम से ही होता है। पहले पापास्रव से भयभीत होकर पुण्य रूप आवष्यक क्रियायें करनी पड़ती हैं पष्चात् स्थायी सामायिक में स्थित होने पर पुण्य तो अनायास ही छूट जाता है।
पुण्य और पाप एक साथ नहीं छोड़े जा सकते। आ० कुन्दकुन्द स्वामी ने नियमसार में परम भक्ति अधिकार समाविश्ट कर यह प्रकट किया है कि बिना भक्ति के नियमसार अर्थात रत्नत्रय का श्रेश्ठ रूप प्राप्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने गाथा क्रमांक 135 में भेद कल्पनासापेक्ष व्यवहार भक्ति करने का श्रमणों को उपदेष दिया है। यह भक्ति मोक्षगत – मुक्तिप्राप्त पुरूशों की जाती है।
अग्रिम गाथाओं में निर्वाण भक्ति एवं योग भक्ति के निष्चय रूपों को भी व्यक्त किया है। प्रायः सामान्य जन निष्चय भक्ति एवं व्यवहार भक्ति के स्वरूप को न समझकर भ्रम से यद्वा तद्वा श्रद्वान कर मिथ्यात्व को ही ग्रहण किये रहते हैं। कतिपय जन एकान्त निष्चयाभास से विमोहित होकर व्यवहार भक्ति को सर्वथा हेय जानकर अनादर करके तथा अपने को निष्चय भक्ति का पात्र मानकर जो कुछ संकल्प विकल्प करते हैं उसको ही निष्चय भक्ति मान लेते हैं।
इससे वे दोनों प्रकार की भक्ति से रहित होकर पापास्रव ही करते हैं, कुगति के भाजन बनते हैं। इस प्रकार की स्थिति को लक्ष्य कर पू० ज्ञानमती माता जी ने अत्यंत करुणा के साथ गुणस्थान निरूपण के द्वारा जीवों को एतत्सम्बन्धी यथार्थ वस्तुस्वरूप का अवलोकन कराया है। उदाहरणार्थ स्याद्वाद चन्द्रिका की गाथा सं. 136 की टीका के अंतर्गत पृश्ठ 396 पर ध्यान देना योग्य है-
‘‘व्यवहारनयाश्रिता निर्वाणभक्तिः प्रमत्तसंयतमुनिपर्यंतास्ति, निष्चयनयाश्रिता सा भक्तिः श्रद्धाभावेन प्रमत्तविरतं यावत्।
पुनः अप्रमत्तगुणस्थाने जघन्या अपूर्वकरणगुणस्थानादारभ्योपषान्तकशायगुणस्थानपर्यन्तं मध्यमा, क्षीणकशायगुणस्थाने उत्तमा एवं ततोऽगे्र सयोगायोगकेवलिनां भक्तेः फलं भवति इति ज्ञात्वा स्वस्वगुणस्थानयोग्यतानुसारेण निर्वाणभक्तिस्तत्पदप्राप्तजिनदेवस्य भक्तिष्च निरन्तरं कर्तव्यास्ति सर्वप्रयत्नेन परमादरेण।’’
व्यवहार के आश्रित निर्वाण भक्ति प्रमत्त संयत मुनि तक होती है। निष्चय नयाश्रित वही भक्ति श्रद्धाभाव से प्रमत्त संयत मुनि पर्यन्त है। पुनः अप्रमत गुणस्थान में जघन्य रूप है। अपूर्वकरण से उपषान्त कशाय गुणस्थान पर्यन्त वह निष्चय भक्ति मध्यम रूप है और क्षीणकशाय गुणस्थान में वह उत्तम उत्कृश्ट रूप है।
इसके आगे सयोग केवली और अयोग केवली में भक्ति का फल ही है। ऐसा जानकर अपने अपने गुणस्थान की योग्यता के अनुसार निर्वाण भक्ति और इस निर्वाण पद को प्राप्त हुए जिनेन्द्र देव की भक्ति सर्वप्रयत्न पूर्वक परम आदर से निरन्तर करते रहना चाहिए।’’
आगम में भक्ति का लक्षण करते हुए कहा गया है ‘‘ गुणेशु अनुरागः भक्तिः’’ अर्थात अर्हन्त, सिद्ध देव, शस्त्र एवं गुरू आदि के गुणों में विषेश राग, प्रीति करना भक्ति है। अज्ञानी एकान्तनयावलम्बी जन अषुभ राग के समान इस शुभ राग को भी हेय जानकर भक्ति, पूजा, वन्दना आदि से विरत हो जाते हैं। वे समयसार की निम्न गाथा का आश्रय लेकर उक्त मान्यता ग्रहण कर लेते हैं-
कम्ममसुहं कुसीलं सुहकम्मं चावि जाणह सुसीलं।
तह किध होदि सुसीलं जं संसारं पवेसेदि।। 145।।
हे मुनि, तुम अषुभ कर्म को कुषील एवं शुभ कर्म को सुषील समझते हो वह शुभ कर्म भी सुषील कैसे हो सकता है जो संसार में प्रवेष कराता है। छहढाला की निम्न पंक्तियों का भी दुरुपयोग कर वे विचार भ्रश्ट होते हैं।
‘‘यह राग आग दहै सदा तातैं समामृत सेइये।’’
‘‘षुभ-अषुभ बन्ध के फल मंझार, रति अरति करै निज पद बिसार।’’ आदि से उनका आषय हो जाता है कि ज्ञानी जीव, शुभ-अषुभ को बराबर रूप से हेय जानते हुए, पराश्रित मानकर भक्ति करना नहीं चाहता, उसे तो करनी पड़ती है। पू० माता जी का स्पश्ट निर्देष है कि यदि करनी पड़ती है तो वह भाव शुन्य होने से फलदायी नहीं होगी।
न उससे सम्यक्त्व उत्पन्न हो सकता है, पुनः वह ज्ञानी कैसे होगा जो निरर्थक ही बन्ध कारक क्रियाओं को करता है। गुणस्थान परिपाटी का उल्लेख जो टीकाकत्र्री माता ने किया है अत्यंत उपयोगी है, क्योंकि अव्रत सम्यग्दृश्टि और व्रती गृहस्थ सम्यग्दृश्टि चतुर्थ और पंचम गुणस्थान तक ही होते हैं। वहां तक तो व्यवहार भक्तिरूप नियम से प्रवृत्ति है, हां निष्चय भक्ति की भी श्रद्धा अवष्य होती है।
जब मुनि को भी छठे गुणस्थान में व्यवहार भक्ति का पात्र कहा है तो गृहस्थ निष्चय भक्ति रूप प्रवृत्ति कैसे कर सकता है, कदापि नहीं। अतः अषुभ राग की अपेक्षा “शुभ राग रूप भक्ति को उपादेय मानकर करना उचित हे। वीतराग स्वसंवेदन रूप निष्चय भक्ति की अपेक्षा ही व्यवहार भक्ति, जो कि प्रवृत्ति रूप होती है, को हेय माना जाता है।
उसको छोड़ानहीं जाता अपितु व्यवहार भक्ति के साधन से ही निष्चय भक्ति प्राप्त होती है, उसकी प्राप्ति होने पर व्यवहार भक्ति अपने आप छूट जाती है उसे अवकाष ही नहीं मिलता। उक्त विशय को और गति देते हुए व्यवहार भक्ति पूर्वक “शुभ योग और निष्चय भक्तिपूर्वकशुद्ध योग के साधन की चर्चा स्याद्वाद चन्द्रिका में गाथा क्रमांक 140 के अंतर्गत माता जी ने की है वह भी उपयोगी ज्ञात होने से इस प्रकरण में यहां उद्धृत की जाती है, देखें पृश्ठ सं. 409-
‘‘ये केचिद् भव्योत्तमाः प्रथमतः काललब्ध्यादि-बलेन अषुभमनोवाक्काययोगानां निग्रहं कृत्वा व्यवहारयोगभक्त्या चतुर्थगुणस्थानात् “शुभयोगमारम्य प्रमत्ताप्रमत्तगुणस्थानादुपरि निष्चयपरमयोगभक्त्या शुद्धयोगेन शुद्धन्तः केवलिनो भूत्वोत्कृश्टेन किंचिदधिकाश्टवर्शन्यूनपूर्वकोटिवर्शायुःपर्यन्तं विहृत्यासंख्यजीवान् संबोध्य पष्चात् कायवाड्मनोयोगं निरुध्य विगतयोगाः सिद्धाः भवन्ति त एव अनन्तकालं नित्यनिर×जनपरमानन्दस्वरूपानन्दज्ञानदर्षनसुखवीर्याद्यनवधिगुणपु×जीभूताः कृतकृत्या भवन्ति।…………………….. तथा च व्यवहार योगभक्त्या (निष्चय) भक्तिः साध्या भवतीति।’’
अर्थ – जो कोई भी भव्योत्तम प्रथम ही काल लब्धि आदि के बल से अषुभ मन, वचन, काय, योगों का निग्रह करके व्यवहार योग भक्ति से चतुर्थ गुणस्थान से शुभ योग को प्रारम्भ करके, प्रमत्त, अप्रमत्त गुणस्थानों से ऊपर निष्चय परमयोग भक्ति से “शुद्धग के द्वारा “शुद्धते हुए केवली होकर उत्कृश्ट से कुछ अधिक आठ वर्श कम पूर्व कोटि वर्श की आयु पर्यन्त विहार कर असंख्य जीवों को संबोधित करके पष्चात् काय, वचन, मन के योग का निरोध करके योग रहित सिद्ध होते हैं।
वे ही अनन्तानन्त काल तक नित्य निरंजन परमानन्द स्वरूप अनन्त ज्ञान, दर्षन, सुख, वीर्य आदि अनन्त गुणों के पुंज रूप होकर कृतकृत्य हो जाते हैं……………………. व्यवहार योगभक्ति से ही (निष्चय) योगभक्ति साध्य होती है।’’ यहां आगमानुसार ही माता जी ने चतुर्थ से सप्तम गुणस्थान तक व्यवहार भक्ति का सद्भाव कहा है। इसी से साध्य निष्चय भक्ति अश्टम गुणस्थान सनिरूपित की है। गुणस्थान भौतिक तुला के समान है।
तराजू पर रखकर जो तौल की जाती है उसे तो समक्ष विद्यमान व्यक्ति को स्वीकार करना पड़ता है, इसी प्रकार आगमोक्त गुणस्थान व्यवस्था को कौन अस्वीकार कर सकता है। अन्यच्च गुणस्थान, जीव स्थान (जीव समास) आदि जीव के परिणाम अर्थात् करण हैं इनका वर्णन करणानुयोग का विशय है। करणानुयोग को दर्पणवत् कहा गया है-
‘‘आदर्षमिव तथा मतिरवैति करणानुयोगं च।’’
केवली गुणस्थान भक्ति का फल है वह जैसे फल भी वृक्ष का अंष है उसी प्रकार भक्ति का फल भी, भक्ति रूप वृक्ष से सर्वथा पृथक नहीं है। ब्रह्मदेव सूरि ने बृहद् द्रव्यसंग्रह की टीका में प्ररूपित किया है कि व्यवहार व्रत (भक्ति आदि) तो छूटते हैं किन्तु साधन रूप निष्चय व्रत जो कि अषुद्ध नय का विशय हैं उनके फलस्वरूप जो साध्य निष्चय व्रत हैं कभी नहीं छूटते। यहां यह भी ध्यान देने योग्य है निष्चय मोक्षमार्ग भी तो छूटता है तभी तो मोक्ष प्राप्त होता है। व्यवहार और निष्चय व्रतों के विशय में त्याग-ग्रहण संबंधी बृहद् द्रव्य संग्रह की टीका के अंतर्गत निम्न पंक्तियां अवलोकनीय हैं-
‘‘अयं तु विषेशः – व्यवहाररूपाणि यानि प्रसिद्धान्येकदेषव्रतानि तानि व्यक्तानि। यानि पुनः सर्वषुभाषुभनिवृत्तिरूपाणि निष्चयव्रतानि तानि त्रिगुप्तिलक्षण स्वषुद्धात्मसंवित्तिरूपनिर्विकल्पध्याने स्वीकृतान्येव न च व्यक्तव्यानि।’’
विषेश यह है – जो व्यवहार नय से प्रसिद्ध एकदेष व्रत है, ध्यान में उनका त्याग किया है, किन्तु समस्त त्रिगुप्ति रूप स्वषुद्धात्मानुभवरूप निर्विकल्प ध्यान में समस्त शुभ अषुभ की निवृत्ति रूप निष्चय व्रत ग्रहण किये है उनका त्याग नहीं किया है।’’ अर्थात् निष्चय व्रत ग्रहण करने के पष्चात् कार्य सिद्धि होने पर छूटते नहीं हैं। पुनः ये व्रत रत्नत्रय स्वरूप ही हैं स्वभाव हैं।
उपरोक्त वर्णन से यह स्पश्ट होता है कि भक्ति, भले ही वह निष्चय रूप हो कभी छूटती नहीं। भक्ति को सम्यक् दर्षन भी कहा है। यह भी आत्म स्वभाव रूप, ही है। हां भक्ति के साथ पूर्व अवस्था का राग छूटता जाता है और वीतराग अवस्था रूप वीतराग सम्यग्दर्शन आदि स्वभाव प्रकट होते हैं।
नियमसार मूल में जो सर्व विकल्पों के अभाव रूप, राग रहित परम सामायिक रूप परम भक्ति कही गई है वह साध्य रूप अवस्था से एकदेष भिन्न ही कही जा सकती है क्योंकि उपादान कारण के सदृष ही कार्य होता है। कारण कार्य की कथंचित् एकता है कथंचित् अनेकता है। इस समस्त विशय पर माँ ज्ञानमती जी ने पर्याप्त प्रकाष डाला है।
इसी प्रसंग में “शुभ भाव परिणति में ही संभव भक्ति की उपादेयता, जोकि आ० कुन्दकुन्द के नियमसार मूल ग्रंथ में भी निरूपित है, पर स्याद्वाद चन्द्रिका में कुछ और भी निरूपण किया गया है। गुणस्थानों की भूमिकानुसार ही तर्कपूर्ण शैली में सोदाहरण माता जी लिखती हैं- हिन्दी अनुवाद :- ‘‘सप्त ऋद्धियों से समन्वित मनःपर्यय ज्ञान से सहित श्री गौतम स्वामी सर्वश्रेश्ठ मुनिराज थे सर्व आचार्य और उपाध्याय एवं साधुओं में सबसे बड़े थे इन श्री गौतम गणधार देव ने स्वयं छठे गुणस्थान में “शुभ भाव से परिणत होते हुए ‘जयति भगवान हेमाम्भोज’ इत्यादि चैत्य भक्ति बोलते हुए देव वन्दना की थी।
इन्हीं गणधार देव ने प्रतिक्रमण सूत्र भी रचे हैं। …………………….., उसी प्रकार इस नियमसार ग्रन्थ के कर्ता श्री कुन्दकुन्दाचार्य भी “शुभ भाव से चर्या कर रहे थे।
ये सभी तपोधन जब सातवें गुणस्थान में स्थित होकर ध्यान करते थे तभी “शुद्धयोगी होते थे। आहारक “शरीर और आहारक अंगोपांग इन दोनों प्रकृतियों का बन्ध यद्यपि सातवें गुणस्थान और आठवें गुणस्थान के छठे भाग तक होता है किन्तु इनका उदय छठे गुणस्थान में ही सुना जाता है।
यदि ऋद्धिधारी महामुनि अकृत्रिम चैत्यालयों की वन्दना, गुरुओं के निशद्यास्थान – समाधिस्थानों की वन्दना, प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान, स्वाध्याय आदि क्रियायें करते थे तो फिर आजकल के सामान्य अनगारों, मुनियों को तो अवष्य ही ये आवष्यक क्रियायें करते रहना चाहिए।’’ इस प्रकरण से स्पश्ट है कि चतुर्थ अथवा पंचम गुणस्थानवर्ती गृहस्थो के लिए तो व्यवहार भक्ति ही “शरण है।
पंडित जयचंद्र छाबड़ा ने समयसार टीका की उत्थानिका में कहा भी है कि ‘‘व्यवहारी जीवों को व्यवहार ही “शरण है।’’ समयसार के अभ्यासियों को यह तथ्य भी हृदयंगम करना चाहिए। पुनष्च समयसार की गाथा क्रमांक 1 12 की तात्पर्यवृत्ति टीका के अंतर्गत आ० जयसेन स्वामी ने कहा है कि जो परमभाव में अथवा अश्टम गुणस्थान से ऊपर स्थित है उनको तो (निष्चय) “शुद्धनय जानने योग्य है, उपयोगी है तथा जो अपरम भाव अर्थात् श्रावक की अपेक्षा चतुर्थ एवं पंचम गुणस्थान और मुनि की अपेक्षा छठे प्रमत्तसंयत तथा सातवें अप्रमत्तसंयत गुणस्थान में स्थित है उसको व्यवहार नय का उपदेष प्रयोजनीय है। उपरोक्त आगमोक्त विशय का स्पश्टीकरण माता जी ने सटीक रूप से गुणस्थान निरूपण शैली से किया है। मोक्षपाहुड में आ० कुन्दकुन्द देव ने आत्मा के तीन भेद निरूपित किये हैं।
1- बहिरात्मा, 2- अन्तरात्मा, 3- परमात्मा।
नियमसार गाथा क्रमांक 145 की टीका के अंतर्गत प्रकरणवष स्याद्वाद चन्द्रिका में एतद् विशयक वर्णन एवं पुश्टि हेतु गुणस्थान परिपाटी को संयोजित किया गया है। त्रिविध आत्माओं के लक्षण भी प्रस्तुत कर उनके गुणस्थान सम्यक् निरूपित किये गये हैं। पृश्ठ सं. 425 के हिन्दी अनुवाद से प्रकट है- ‘‘प्रथम गुणस्थान में जीव मिथ्यात्व, असंयम, विशय, कशाय और दुव्र्यसनों में प्रवृत्ति करते हुए बहिरात्मा है वे सर्वथा अन्यवष ही है।
चैथे गुणस्थान में स्थित सराग सम्यग्दृश्टि जीव चारित्रमोहोदय से असंयम आदि में वत्र्तन करते हैं फिर भी अपने आत्मतत्व के श्रद्धान से ये जघन्य अन्तरात्मा हैं, ये कथंचित् स्ववष कहलाते हैं किन्तु सिद्धान्त की भाशा में ये अन्यवष ही हैं। उसी प्रकार से देषव्रती और प्रमत्तसंयत मुनि मध्यम अन्तरात्मा होने से कथंचित् स्ववष होते हुए भी इस गाथा के अभिप्राय से अन्यवष ही हैं। इसके ऊपर अप्रमत्त गुणस्थान से सूक्ष्मसांपराय पर्यन्त ध्यान में लीन हुए साधु मध्यम अन्तरात्मा हैं।
इनके बुद्धिपूर्वक रागद्वेश का अभाव होने से आत्मवष भी हैं किन्तु संज्वलन कशाय के आधीन होने से कथंचित् अन्यवष हैं। क्षीणमोह गुणस्थान वर्ती निग्र्रन्थ मुनि उत्तम अन्तरात्मा हैं इसलिए ये कथंचित् भी अन्यवष नहीं हैं, आत्मवष ही हैं ऐसा जानकर निर्विकल्प अवस्था को ध्येय बनाकर अन्तरंग और बहिरंग दोनों प्रकार की परवषता छोड़ देना चाहिए।’’
यहां यह विषेश ज्ञातव्य है कि ग्यारहवें गुणस्थान वर्ती महामुनि संज्वलन कशाय के उदयाभाव के कारण उसके अधीन न होने से वीतराग रूप परिणति के कारण की अपेक्षा से स्ववष है किन्तु सत्ता में विद्यमान चारित्रमोह की प्रकृतियों के उदय आ जाने से अन्यवषता को नियम से प्राप्त होते हैं, अतः कथंचित् अन्यवष हैं। इस विशय को संभवतः सुगम जानकर टीकाकत्र्री माता जी ने नहीं लिया है उपयोगी जानकर हमने यहां लिखा है। जैन “शासन के अनुसार मोक्ष की प्राप्ति ज्ञान और क्रिया की समश्टि से होती है यथा ‘‘ज्ञानक्रियाभ्यां मोक्षः’’। अन्यत्र भी कहा है-
हतं ज्ञानं क्रियाहीनं हता चाज्ञानिनां क्रिया।
धावन् किलान्धको दग्धः पष्यन्नपि च पंगुलः।।
क्रियाहीन ज्ञान नश्ट हो जाता है तथा ज्ञान के अभाव में क्रिया भी नश्ट हो जाती है। उदाहरणार्थ- (वन में अग्नि लग जाने पर) अंधा मनुश्य दृश्टि के अभाव में मार्ग न सूझने के कारण दौड़ते हुए भी जल जाता है एवं लंगड़ा व्यक्ति न दौड़ पाने के कारण मार्ग देखते हुए भी (क्रिया के अभाव के कारण) जल जाता है मरण को प्राप्त हो जाता है।
ज्ञान और क्रिया की परस्पर तीव्र मित्रता, अनुसारता, समश्टि से ही मुमुक्षु मोक्षमार्ग में गतिमान होकरशुद्ध ध्यान का पात्र होता है। आवष्यक महाव्रतादि क्रियाओं को करना आवष्यक एवं उपादेय है। प्रस्तुत विशय की महत्वपूर्ण चर्चा स्याद्वाद चन्द्रिका में गाथा क्रमांक 147 की टीका के अंतर्गत गुणस्थान संयोजना से प्रस्तुत की गई है।
आवष्यक क्रियायें अपरम भाव में तो स्थूल रूप में आवष्यक होती ही हैं किन्तु वे ही आत्मस्थिति रूप शुक्ल ध्यान के होने पर भी अन्तरंग परिणति क्रिया रूप में अनिवार्य है। प्रस्तुत है उस स्थल की निम्न पंक्तियां-
‘‘तात्पर्यमेतत् – आसामावष्यकक्रियाणां परिपूर्णता पूर्णवीतरागतायामेवोप- षान्तक्षीणमोहगुणस्थानयोर्जायते तथाप्यप्रमत्तगुणस्थानादारभ्य सूक्ष्मसाम्परायगुण- स्थानपर्यन्तमपि तरतमभावेन शुद्धपयोगापेक्षया घटन्ते, अतोऽप्रमत्तावस्थायाः प्राप्त्यर्थं महाव्रतमुपादेयमिति मत्वा भवद्भिरपि परमादरेण वत्र्तमानमुनीनां चर्याश्रयणीया।’’
तात्पर्य यह हुआ कि इन आवष्यक क्रियाओं की परिपूर्णता पूर्ण वीतरागता के होने पर ही उपषान्तमोह और क्षीणमोह इन दो गुणस्थानों में ही होती है, फिर भी अप्रमत्त गुणस्थान से लेकर सूक्ष्मसाम्पराय गुणस्थान पर्यन्त भी तरतमभाव से “शुद्धपयोग की अपेक्षा से घटित हो जाती है। इसलिए अप्रमत्त अवस्था को प्राप्त करने के लिए महाव्रत उपादेय है ऐसा मानकर आपको भी परमादर पूर्वक वर्तमान मुनियों की चर्चा का आश्रय लेना चाहिए। माता जी के उक्त आषय को आगम से पुश्ट करने हेतु आचार्य अमृतचन्द्र जी का निम्न कलष ध्यान देने योग्य है-
स्याद्वादकौषलसुनिष्चलसंयमाभ्यांयो भावयत्यहरहः स्वमिहोपयुक्तः।
ज्ञानक्रियानयपरस्परतीव्रमैत्री-पात्रीकृतः श्रयति भूमिमिमां स एकः।।
स्याद्वाद की कुषलता और सुनिष्चल संयम (निरतिचार महाव्रतादि) के द्वारा जो निरन्तर स्वात्मा में लीन होकर अपने को भाता है तथा ज्ञान और क्रिया नय की परस्पर तीव्र मित्रता ने जिसे पात्र बना दिया है ऐसा कोई महामुनि कारण समयसार रूप तीसरी भूमिका पर आरोहण करता है।
निर्विकल्प समाधि निष्चय रत्नत्रय “शुक्लध्यान,शुद्धपयोग, “शुद्धत्मानुभूति की अवस्था को “शास्त्रों में निश्क्रिय विषेशण से विषेशित किया जाता है वहां तात्पर्य यह है कि वाह्य क्रियाओं का इस भूमिका में अभाव होता है किन्तु अभ्यन्तर में ज्ञानादि गुणों की परिणति रूप क्रिया नवीन नवीन रूप में होती है उस निष्चय क्रिया या अभ्यन्तर ध्यान रूप क्रिया का तो सद्भाव वीतराग अवस्था तक होता है।
उसके बल से ही केवलज्ञान की प्राप्ति होती है। कारण समयसार अथवा नियमसार के बल से ही कार्य समयसार उत्पन्न होता है। ऊपर लिखित पंक्तियों में माता जी ने महाव्रतों को वाह्य क्रिया रूप में भी उपादेय बतलाया है उसी से अप्रमत्त अवस्था प्राप्त होती है। बिना क्रिया के मोक्षमार्ग नहीं बनता। पंडित प्रवर बनारसीदास, जो पूर्व अवस्था में अपनी आत्मकथा ‘अद्र्धकथानक’ के अनुसार भ्रम से निष्चय नय के एकान्त से ग्रसित हो गये थे, ने स्वयं लिखा है-
‘‘करनी को रस मिटिगयो मिल्यो न आतम स्वाद।
भई बनारसि की दसा जथा ऊंट को पाद।।’’ अद्र्धकथानक।।
‘‘जो बिन ज्ञान क्रिया अवगाहै, जो बिन क्रिया मोक्ष पद चाहै।
जो बिन मोक्ष कहै मैं सुखिया सो अजान मूढनि में मुखिया।।
प्रस्तुत पंक्तियों का मूल श्रोत आचार्य अमृतचंद्र जी का निम्न कलष है,
मग्ना कर्मनयावलम्बनपरा ज्ञानं न जानन्ति ये।
मग्नाः ज्ञाननयैशिणोऽपि यदति-स्वच्छन्दमन्दोद्यमाः।
विष्वस्योपरि ते तरन्ति सततं ज्ञानं भवन्तः स्वयं।
ये कुर्वन्ति न कर्म जातु न वषं यान्ति प्रभादस्य च।।
स्याद्वाद चन्द्रिका में इसी आषय को गुणस्थानों में निरूपित कर माता जी ने अपनी दूरदृश्टि एवं लोकहित-भ्रम निवारण लक्ष्य से ही प्रयास किया है जो प्रषंसनीय है। ऊपर पाठकों को यह हमने दर्षित कराया ही है। जिनवाणी चतुरनुयोग रूप है। प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग एवं द्रव्यानुयोग। द्रव्यानुयोग का प्रमुख विशय अध्यात्म है।
उसके रहस्य को हृदयंगम करने हेतु करणानुयोग की अनिवार्यता है, क्योंकि इसके अभाव में प्रायः स्खलन की संभावना रहती है। इसी आषय को दृश्टिगत कर नियमसार के अध्यात्म वैभव को उसके मूल अर्थ रूप से सुरक्षित रखने हेतु माता जी ने यथास्थान गुणस्थानों के माध्यम से उसका अर्थ स्पश्ट किया है। इस सम्बन्ध मेंशुद्धपयोगाधिकार की उत्थानिका दृश्टव्य है। उनका कथन है कि प्रस्तुत अधिकार का नाम “शुद्धजीवाधिकार या मोक्षधिकार कहना अधिक संगत है क्योंकि इस अधिकार मेंशुद्धपयोग के फल मोक्ष का स्वरूप आचार्य कुन्दकुन्द ने वर्णित किया है।
इस आषय की सिद्धि हेतु स्याद्वाद चन्द्रिका में प्रवचनसार, परमात्मप्रकाष, बृहदद्रव्य संग्रह आदि टीकाकारों के निरूपण को उद्धृत किया गया है। यहां हिन्दी अनुवाद, जो माता जी का स्वोपज्ञ है, का उपयोगी अंष प्रस्तुत है- ‘‘किन्तु जब अध्यात्म भाशा से उपयोग के अषुभ, “शुभ और “शुद्धकी अपेक्षा तीन भेद करते हैं तब मिथ्यात्व, सासादन और मिश्र इन गुणस्थानों में तरतमभाव से घटता हुआ अषुभोपयोग है। चैथे, पांचवें और छठवें इन तीन गुणस्थानों में तरतमभाव से बढ़ता हुआ “शुभोपयोग है।
उसके आगे अप्रमत्तविरत से लेकर क्षीण कशाय तक छह गुणस्थानों में तरतमभाव से (बढ़ता हुआ)शुद्धपयोग तथा तेरहवें और चैदहवें गुणस्थान में “शुद्धपयोग का फल है।’’ यहां गुणस्थान क्रम वर्णन में तरतम भाव का तात्पर्य यह है कि सामान्य रूप से विवक्षित उपयोग के होते हुए भी उनमें गुणीय अंषों में अन्तर है।
उदाहरणार्थशुद्धपयोग का जो गुणांष अग्रिम गुणस्थान में है वह पूर्ववर्ती में नहीं, आदि। स्याद्वाद चन्द्रिका टीका में माता ज्ञानमती जी ने पृश्ठ 548 पर गुणस्थान निरूपण की उपादेयता का उल्लेख स्वयं किया है। उनके ही वचनों पर ध्यान दना निम्नांकित रूप में समीचीन होगा-
‘‘प्रत्येक गाथाटीकासु नयविभागेन विशय स्पश्टीकृत आसीत्।
यद्यप्यस्मिन् ग्रन्थे निष्चयनयप्रधानत्वं तथापि गुणस्थानेशु तत्तद् विशयं घटयित्वा व्यवहारनय- प्रधानत्वेन तात्पर्यार्थः प्रदर्षितः।
किं चाद्यत्वे संयताः संयतिकाष्च व्यवहार करणचरणयोः निश्पन्नाः भवेयुस्तत्र “ौथिल्यं मा गच्छेयुरेश एव ममाभिप्रायः।
यतो निष्चयनयाश्रित- मात्मानमलभमानानां व्यवहारक्रियासु प्रमादः स्वार्थहानये भवति।
‘अर्थ – यद्यपि इस ग्रन्थ में निष्चय नय प्रधान है फिर भी गुणस्थानों में उस विशय को घटाकर व्यवहार नय की प्रधानता से तात्पर्यार्थ दिखलाया गया है उसमें आजकल के मुनि और आर्यिकायें व्यवहार क्रिया और चारित्र में निश्पन्न हो जावें, उसमें षिथिलता न लावें यही मेरा अभिप्राय है क्योंकि निष्चय नय के आश्रित आत्मा को प्राप्त न करते हुए व्यवहार क्रियाओं में प्रभादी हो जाना अपने प्रयोजन की हानि के लिए ही होता है।
’’ पूर्व में हमने आचार्य कुन्दकुन्द देव की मोक्षप्राभृत की गाथा उद्धृत की है जिसके अनुसार बहिरात्मा, अन्तरात्मा और परमात्मा इन तीनों भेदों का उल्लेख है। इस भेद कल्पना के अंतर्गत अन्तरात्मा के भी जघन्य, मध्यम और उत्कृश्ट ये तीन रूप विविध ग्रन्थों में पाये जाते हैं। जघन्य अंतरआत्मा माता जी के अनुसार गृहस्थ हैं।
आगे मध्यम और उत्तम अंतरात्मा का वर्णन स्याद्वाद चन्द्रिका में स्पश्ट रूप से किया गया है। विवक्षित टीकांष का हिन्दी अनुवाद पृश्ठ 438 से यहां उद्धृत किया जाता है। ‘‘छठे सातवें गुणस्थानवर्ती मुनि जब धर्मध्यान में स्थित होकर पिण्डस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और रूपातीत के भेद में से किसी का भी ध्यान करते हैं वे मध्यम अंतरात्मा हैं।
पुनः यदि श्रेणी में चढ़कर “शुक्लध्यान को करते हैं, तो भी उपषान्त- कशाय नामक ग्यारहवें गुणस्थान तक मध्यम अंतरात्मा ही है। इसके आगे बारहवें गुणस्थान में पहुंचकर ही उत्तम अंतरात्मा कहलाते हैं अथा धवला टीकाकार श्री वीरसेनाचार्य के अभिप्राय से दसवें गुणस्थन तक भी धर्मध्यान को करने वाले हैं। इसके आगे “शुक्लध्यान के ध्याता हैं। यही धर्मध्यान ‘निष्चय’ इस नाम को प्राप्त करता है। कहा भी है-
‘‘असंजदसम्मदिद्वि संजदासंजद पमत्तसंजद अप्पमत्तसंजद अपुव्वसंजद अणियह्सिंजद सुहुमसांपराइय खवगोपसामएसु धम्मुझाणस्स पवित्ती होदित्ति जिणोवएसादो।’’
असंयत सम्यग्दश्टि – संयतासंयत – प्रमत्तसंयत – अप्रमत्त संयत- अपूर्वकरणसंयत अनिवृत्तिसंयत – सूक्ष्मसाम्यराय – क्षपक और उमषापकों में जिनेन्द्र देव के उपदेषानुसार धर्मध्यान की प्रवृत्ति होती है।’’ यहां माता जी ने धर्मध्यान और “शुक्लध्यानों के गुणस्थानों में अस्तित्व सम्बन्धी दोनों मतों का उल्लेख किया है। यह अति उपयोगी है।
प्रायः1 करके श्रेणी आरोहण के काल में अर्थात् आठवें से लेकर “शुक्लध्यान माना जाता है। धवला का मत इसका अपवाद स्वरूप प्रतिभासित होता है जिसको माता जी ने यहां उद्धृत कर अपेक्षित मार्गदर्षन दिया है। टीका में आगे ध्यान का अभ्यास न करने वाले साधु वर्ग को माता जी ने बहिरात्मा रूप में स्वीकार करते हुए प्रतिदिन ध्यान का अभ्यास करने की पे्ररणा दी है ताकि वे अंतरात्मा हों। साधु को न तो प्रमाद करना अभीश्ट है और न वर्तमान परिस्थिति में ही संतुश्ट करना। उन्हें तो आगे बढ़ने की पे्ररणा दी है। जिनागम में मोक्षमार्ग दो प्रकार निरूपित किया गया है। व्यवहार और निष्चय।
व्यवहार मोक्षमार्ग साधन है और निष्चय मोक्षमार्ग साध्य। गुणस्थान परक प्रक्रिया में सातवें गुणस्थान से (सातिषय अप्रमत्त) निष्चय मोक्षमार्ग का प्रारंभ मानाजाता है जिसे “शुद्धपयोग भी कहा है। सातवें गुणस्थान के स्वस्थान अप्रमत्त और सातिषय अप्रमत्त, ये दो भेद हैं।
इन दोनों भेदों के गुण में क्या अंतर है, यह गवेशणीय समझकर माता जी ने प्रस्तुत टीका में स्पश्टीकरण किया है। साथ ही अप्रमत्त के किस भेद में कौन सा मोक्षमार्ग का विकल्प है यह निरूपित किया है। वर्तमान में इस विशय में चर्चायें विद्यमान हैं। कुछ जिज्ञासु जन अप्रमत्त के स्वस्थान रूप में हीशुद्धपयोग का सद्भाव मानते हैं, उनके लिए माता जी का टीकागत गाथा क्रमांक 152 का निम्न मार्गदर्षन उपयोगी हो सकता है। विशय विस्तार के भय से यहां मात्र उनका स्वोपज्ञ हिन्दी अनुवाद प्रस्तुत करना सार्थक होगा।
‘‘भावार्थः – सातवें गुणस्थान के प्रथम स्वस्थान अप्रमत्त में सविकल्प ध्यान होने से सविकल्प अवस्था में रत्नत्रय की एकाग्रता व्यवहार रूप में रहती है और दूसरे सातिषय अप्रमत्त में निर्विकल्प ध्यान रूप निर्विकल्प अवस्था में रत्नत्रय की एकाग्रता निष्चय रूप में मानी जाती है।’’ यहां स्पश्ट है कि सातिषय अप्रमत्त अवस्था में विकल्प का अभाव होता है। विकल्प का अर्थ राग भी है अतएव निर्विकल्प का अर्थ वीतराग सिद्ध होता है। यहाँ ही बुद्धिपूर्वक राग का अभाव हो पाता है।
उदय में जो कि×िचत् संज्वलन कशाय का अंष होता है वह बुद्धि को, उपयोग को ध्यान से विचलित करने में असमर्थ है। इसी अपेक्षा से सातिषय अप्रमत्त को ही “शुद्धपयोग या निष्चय मोक्षमार्ग मानना चाहिए। शुद्धपयोग का तात्पर्य ही रागद्वेश-कशाय रूप मलीनता से रहित ज्ञान दर्षन की एकाग्र परिणति से है। दूसरे सातिषय से ही श्रेणी आरोहण की भूमिका बनती है।
श्रेणी के तीन करण हैं,
1- अधःप्रवृत्तकरण, 2- अपूर्वकरण, 3- अनिवृत्ति करण।
इनमें अधः प्रवृत्तकरण सातवें गुणस्थान के सातिषय अप्रमत्त भेद में स्वीकार किया गया है। आठवें गुणस्थान का नाम ही अपूर्वकरण एवं नवें का नाम अनिवृत्तिकरण है। प्रथम करण अधः प्रवृत्त स्वस्थान अप्रमत्त में स्वीकृत नहीं है। स्याद्वाद चन्द्रिका कत्र्री का उक्त विवेचन इसी हेतु प्रकरण पुश्टि करता है।
सातवें में व्यवहार रत्नत्रय या “शुभोपयोग (स्वस्थान अप्रमत्त में) स्वीकार करने योग्य है। वर्तमान में साधुजनों को श्रेणी आरोहण नहीं है यही आ० कुन्दकुन्द के “शब्दों में एव आ० जयसेन स्वामी की समयसार की तात्पर्यवृत्ति टीका में मान्य अपरम भाव है। परम भावदर्षीपने हेतु साधु का सहंनन ही नहीं है। स्वस्थान अप्रमत्त में आर्यिका ज्ञानमती जी ने व्यवहार रूप रत्नत्रय की एकाग्रता का ऊपर उल्लेख किया है उसे उदाहरण के रूप में समझना चाहिए।
जैसे सोंठ, मिर्च, पीपल में तीन पदार्थ जब साबित (खंड रहित) अवस्था में मिलाये जायें तो मिले हुए भी एकाग्र या समरस नहीं हैं। जब मोटे मोटे कूट कर मिलाये जायें तो मिले होने पर भी एकरसता, समरसता गुण को प्रकट नहीं कर सकते। उसी प्रकार सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्र जब मोटे तौर पर मिले हों तो पृथक करण “वक्य होने यह मिलावट व्यवहार रूप ही है। ध्यानाग्नि प्रज्वलित करने में असमर्थ है।
किन्तु जब सोंठ, मिर्च, पीपल अत्यंत बारीक पीसकर मिला लिये जाते हैं एकरस, समरस या एकाग्र हो जाते हैं। पृथक करना, पृथक स्वाद लेना संभव नहीं रहता। उसी प्रकार मोक्षमार्ग के तीनों अवयव जब पूर्ण अंतस्तत्त्व रूप होकर, पैने होकर सूक्ष्म रूप होते हुए मिल जाते हैं एकाग्र, समरस हो जाते हैं तथा उनमें से एक का पृथक अनुभव नहीं होता तब निष्चय या अभेद रत्नत्रय रूप मोक्षमार्ग कहलाते हैं। वे अखंड हैं, अभेद हैं, निर्विकल्प हैं। जिनागम में आप्त, आगम और तत्व के श्रद्धान को सम्यग्दर्शन अथवा सम्यक्त्व कहा गया है।
मिथ्यात्व गुणस्थान में क्षयोपषम, विषुद्धि, देषना के बल से प्रायोग्य एवं करण लब्धियां उत्पन्न होती हैं। इनमें सर्वाधिक महत्व भावविषुद्धि, परिणामों की “शुभता, संक्लेष की कमी का जानना चाहिए। इसके बल से ही मिथ्यात्व प्रकृति के तीन खंड मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व, सम्यक्त्व प्रकृति होते हैं और मिथ्यात्व कर्म का उपषम होता है।
कतिपय जनों की मान्यता है, कि ज्ञान करने से, तत्वों का स्वरूप बोध करते-करते ही सम्यक्त्व उत्पन्न होता है यह ठीक नहीं है क्योंकि अनपढ़ मनुश्य, तिर्य×चों के भी प्रथमोपषम सम्यक्त्व उत्पन्न हो जाता है। वास्तविकता यह है कि सम्यक्त्व की प्राप्ति के आयतनों में लब्धियों के बल से, भावविषुद्धि (षुभ परिणाम) से श्रद्धा होने पर मिथ्यात्व कर्म का उपषम हो जाता है इसे ही सम्यक्त्व कहते हैं।
कशाय की तीव्रता हो, भक्तिभाव का अभाव हो तो मात्र जान लेने से सम्यक्त्व उत्पन्न होना असिद्ध है। सम्यक्त्व होने पर ज्ञान सम्यक् होता है यह आगम वचन है सम्यक्त्व एवं ज्ञान, स्वरूपबोधता की पूर्वापरता के विशय में स्याद्वाद चन्द्रिका में आगमानुसार स्पश्टीकरण गाथा सं. 51 की टीका के अंतर्गत किया गया है ध्यान देने योग्य है।
प्रस्तुत है वह स्थल- ‘‘गाथा 5वीं में आप्त, आगम एवं तत्वों के श्रद्धान को सम्यक्त्व कहा है और यहां गाथा 51वीं में मिथ्या अभिप्राय से रहित श्रद्धान को सम्यक्त्व कहा है सो वहां पर विधिमुख से कथन है और यहां पर निशेधमुख से कथन है। उभयकोटिस्पर्षी ज्ञान को संषय कहते हैं जैसे यह ठूंठ है या पुरुश ?
परस्पर सापेक्ष दोनों नयों से वस्तु का ज्ञान न होना विमोह है जैसे गमन करते हुए पुरूश के पैर में तृण लग जाने पर कुछ लग गया है ऐसा विकल्प होना अथवा दिषा भ्रम हो जाना। अनेकान्तात्मक वस्तु को यह नित्य ही है अथवा क्षणिक ही है ऐसा एकान्त रूप से ग्रहण करना विभ्रम है, जैसे सीप में चांदी का ज्ञान कर लेना।
इन तीनों दोशों से रहित जो ज्ञान होता है वह सम्यग्ज्ञान होता है। यद्यपि सम्यक्त्व की उत्पत्ति के अनन्तर ही सम्यग्ज्ञान प्रकट हो जाता है फिर भी दोनों के लक्षण पृथक पृथक ही हैं। यह सम्यक्त्व और ज्ञान दोनों चैथे गुणस्थान से प्रकट हो जाते हैं। ये ही मोक्ष महल की पहली सीढ़ी है।
ऐसा निष्चय करके सम्यक्त्व को प्राप्त कर प्रमाद को छोड़कर सतत् ही इस रत्न की रक्षा करनी चाहिए। आचार्य कुन्दकुन्द देव ने व्यवहार चारित्राधिकार में कथन किया है कि पंचाचार से युक्तः प×चेन्द्रिय रूपी हस्ती के दर्प को दलन करने मंे समर्थ, धीर गुण गंभीर आचार्य परमेश्ठी होते हैं, रत्नत्रय से संयुक्त, निश्कांक्षा भाव से युक्त तथा जिनोपदिश्ट तत्वार्थों के उपदेषक उपाध्याय होते हैं तथा समस्त आरम्भ परिग्रह रूप व्यापार से रहित, दर्षन, ज्ञान चारित्र एवं तप आराधना में सदा ही लीन एवं निर्मोह साधु परमेश्ठी होते हैं। इस वर्णन के पष्चात् उन्होंने निम्न गाथा की रचना की-
एरिसभावणाए ववहारणयस्स होदि चारित्तं।
णिच्छयणयस्स चरणं एत्तो उढ्ढं पवक्खामि।। 76।।
इस प्रकार की भावना में (ऊपर वर्णित त्रयोदष प्रकार चारित्र एवं पंच परमेश्ठी भक्ति भावना) व्यवहार नय का चारित्र होता है। इसके आगे मैं निष्चय नय का चारित्र कहूंगा। इस गाथा की टीका में माता जी ने वैराग्य मार्ग में भक्ति रूप अनुराग मार्ग को युक्त्यागम प्रमाण से समाविश्ट कर सिद्ध किया है, प्रकरण विषेश पठनीय है। साथ ही इस प्रकरण की पुश्टि हेतु उन्होंने गुणस्थान निरुपण भी किया है उसको यहां उद्धृत करते हैं।
‘‘पश्ठगुणस्थाने व्यवहारनयस्य चारित्रं भवति, सप्तमगुणस्थानस्यापि प्रथमस्वस्थानाप्रमत्तभागे भेदरत्नत्रयमेव तावत्पर्यन्तमिदमेव चारित्रं जायते। तत्पष्चात् सप्तमगुणस्थानस्य सातिषयाप्रमत्तनामद्वितीयभागाद् आरभ्य आक्षीणकशाय गुणस्थानात् निष्चयनयाश्रितस्य चारित्रं विद्यते।
अस्मात् कारणात् एतस्मात् ऊध्र्वं व्यवहाररत्नत्रयकथनस्यानन्तरं तदेव अहं कुन्दकुन्दाचार्यः प्रकर्शेण वक्ष्ये।’’
छठे गुणस्थान में व्यवहार नय का चारित्र होता है। सातवें गुणस्थान के पहले स्वस्थान अप्रमत्त भाग में भेद रत्नत्रय ही है। अतः वहां तक यही व्यवहार चारित्र होता है। इसके बाद सातवें गुणस्थान के सातिषय अप्रमत्त नामक दूसरे भाग से आरम्भ करके क्षीणकशाय गुणस्थान पर्यन्त निष्चय नय के आश्रित चारित्र होता है।
इसी हेतु से मैं कुन्दकुन्दाचार्य व्यवहार रत्नत्रय के कथन के अनन्तर उसी निष्चय चारित्र को कहूँगा।’’ इसके पष्चात माता जी ने तीन प्रकार के मुनियों का निरूपण किया है।
1- प्रारम्भक, 2- घटमान, 3- निश्पन्न।
प्रारम्भक और घटमान व्यवहार रत्नत्रय ही के पालक हैं। मात्र घोर तपष्चरण युक्त उपसर्ग, परीशहों के विषेश सहन करने वाले एवं ध्यान रूपी अमृत के आस्वादी निश्पन्न मुनि ही निष्चय रत्नत्रय के धारक होते हैं। सारांष यह है कि जो लोग व्यवहार रत्नत्रय के बिना निष्चय रत्नत्रय को प्राप्त करना चाहते हैं वे जिनषासन से बहिर्मुख अपनी वंचना करने वाले ही हैं। उपरोक्त वर्णन से स्पश्ट है कि स्याद्वाद चन्द्रिका में गुणस्थान निरूपण शैली से टीकाकत्र्री माँ ने नियमसार के अन्तस्तत्व का सम्यक् प्रकारेण स्पश्टीकरण किया है, वह प्रषंसनीय है।