सरल संस्कृत शिक्षा
(संज्ञा प्रकरण एवं स्वरसंधि समन्वित)
कातंत्र व्याकरण के आधार से
सरस्वति! नमस्तुभ्यं, वरदे! कामरूपिणि!
विद्यारंभं करिष्यामि, सिद्धिर्भवतु मे सदा।।१।।
प्रथमः पाठः
विभक्तियों के नाम व अर्थ

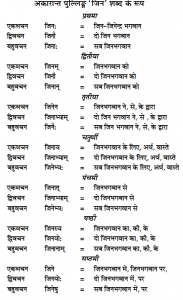
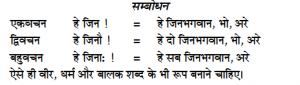
धर्म शब्द की समस्त विभक्तियों का एक पद्य में प्रदर्शन
धर्मः सर्वसुखाकरो हितकरो, धर्मं बुधाश्चिन्वते।
धर्मेणैव समाप्यते शिवसुखं, धर्माय तस्मै नमः।।
धर्मान्नास्त्यपरः सुहृद्भवभृतां, धर्मस्य मूलं दया।
धर्मे चित्तमहं दधे प्रतिदिनं, हे धर्म! मां पालय।।
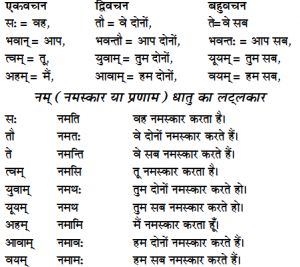
जिनः शतेन्द्र वंद्योऽस्ति, जिनं भत्त्âया श्रयाम्यहम्।
जिनेन दीयते सौख्यं, जिनाय कोटिशो नमः।।१।।
जिनाद् धर्मोऽभवज्जैनो, जिनस्य नाम क्षेमकृत्।
जिने भक्तिः स्थिरा मे स्यात्, जिन! त्वं रक्ष रक्ष माम्।।२।।
अथ संज्ञा प्रकरण
सिद्धो वर्णसमाम्नायः।।१।।
अर्थ-वर्णों का समुदाय अनादिकाल से सिद्ध है।।१।।
इन वर्णों के समूह को आज तक न किसी ने बनाया है और न कोई नष्ट ही कर सकते हैं, ये वर्ण अनादि निधन हैं। उनको जानना चाहिए। वे कौन हैं ? अ आ इ ई उ ऊ ऋ ý ऌ ल¸ ए ऐ ओ औ। क ख ग घ ङ। च छ ज झ ञ। ट ठ ड ढ ण। त थ द ध न। प फ ब भ म। य र ल व। श ष स ह। ये सैंतालीस वर्ण कहलाते हैं।
तत्र चतुर्दशादौ १स्वराः।।२।।
अर्थ–इनमें आदि के चौदह अक्षर स्वर कहलाते हैं।।२।।
इन वर्णों के समुदायों में आदि के जो चौदह अक्षर हैं, वे स्वर संज्ञक हैं। वे कौन-कौन हैं ? अ आ इ ई उ ऊ ऋ ý ऌ ल¸ ए ऐ ओ औ। ये चौदह स्वर हैं।
दश समानाः।।३।।
अर्थ-दश समान संज्ञक हैं।।३।।
इन स्वरों में आदि के जो दश वर्ण हैं उनकी ‘‘समान’’ यह संज्ञा है। वे कौन हैं? अ आ इ ई उ ऊ ऋ ý ऌ ल¸।
तेषां द्वौ द्वावन्योऽन्यस्य सवर्णौ।।४।।
अर्थ-इनमें दो-दो वर्ण आपस में सवर्णी हैं।।४।।
इस समान संज्ञक स्वरों में दो-दो वर्ण आपस में सवर्ण संज्ञक हैं। अ आ, इ ई, उ ऊ, ऋ ý, ऌ ल¸।
सूत्र में ‘‘तेषां’’ शब्द का ग्रहण क्यों किया है ? दो ह्रस्व वर्ण एवं दो दीर्घ वर्ण भी आपस में सवर्ण संज्ञक हैं इस बात को स्पष्ट करने के लिए सूत्र में ‘‘तेषां’’ पद सार्थक है। अर्थात् चार प्रकार से सवर्णता मानी गई है।
क्रमेण वैपरीत्येन, लघूनां लघुभिः सह।
गुरूणां गुरुभिः सार्धं, चतुर्धेति सवर्णता।।१।।
श्लोकार्थ-क्रम से अर्थात् ह्रस्व ह्रस्व का, दीर्घ दीर्घ का, दीर्घ ह्रस्व का और ह्रस्व दीर्घ का यह चार भेद हैं।
ऋकारऌकारौ च ।।५।।
अर्थ-ऋकार और ऌकार भी परस्पर सवर्ण हैं।।५।।
ऋकार और ऌकार भी परस्पर में सवर्ण संज्ञक हैं, जैसे-ऋ ऌ।
पूर्वो ह्रस्वः१।।६।।
अर्थ-पूर्व के वर्ण ह्रस्व हैं।।६।।
इन सवर्ण संज्ञक स्वरों में पूर्व-पूर्व पाँच स्वर ह्रस्व संज्ञक हैं। अ इ उ ऋ ऌ।
परो दीर्घः२।।७।।
अर्थ-अंत के स्वर दीर्घ संज्ञक हैं।।७।।
इन सवर्ण संज्ञक दश स्वरों में अंत-अंत के पाँच स्वर दीर्घ संज्ञक हैं। आ ई ऊ ý ल¸।
स्वरोऽवर्णवर्जो नामि।।८।।
अर्थ-अवर्ण को छोड़कर शेष स्वर नामि संज्ञक हैं।।८।।
अवर्ण को छोड़कर शेष बारह स्वरों की ‘नामि’ यह संज्ञा है। इ ई उ ऊ ऋ ý ऌ ल¸ ए ऐ ओ औ। वर्ण के ग्रहण करने से सवर्ण का अर्थात् दोनों स्वरों का ग्रहण हो जाता है और ‘कार’ शब्द के ग्रहण करने से केवल एक स्वर का ही ग्रहण होता है। जैसे अवर्ण कहने से अ आ दोनों ही आ गये एवं अकार कहने से मात्र ‘अ’ शब्द ही आता है। यह नियम सर्वत्र व्याकरण में समझना चाहिए।
एकारादीनि सन्ध्यक्षराणि।।९।।
अर्थ-एकार आदि स्वर संध्यक्षर कहलाते हैं।।९।।
एकार आदि स्वर, संध्यक्षर संज्ञक होते हैं। वे कौन हैं? ए ऐ ओ औ।
नित्यं सन्ध्यक्षराणि दीर्घाणि।।१०।।
अर्थ-ये संध्यक्षर हमेशा ही दीर्घ रहते हैं।।१०।।
संध्यक्षर नित्य ही दीर्घ होते हैं।
कादीनि व्यञ्जनानि३।।११।।
अर्थ-‘क’ आदि वर्ण व्यंजन कहलाते हैं।।११।।
ककार से लेकर हकार पर्यंत अक्षर व्यंजन संज्ञक हैं। ये ३३ हैं।
क ख ग घ ङ। च छ ज झ ञ। ट ठ ड ढ ण। त थ द ध न । प फ ब भ म। य र ल व। श ष स ह।
ते वर्गाः पञ्च पञ्च पञ्च।।१२।।
अर्थ-उनमें पाँच-पाँच के पाँच वर्ग होते हैं।।१२।।
ये ककारादि से ‘म’ पर्यंत पाँच-पाँच वर्ण मिलकर पाँच ही वर्ग होते हैं। क ख ग घ ङ ये कवर्ग संज्ञक हैं। कवर्ग कहने से ये पाँचों ही अक्षर आ जाते हैं। उसी प्रकार से चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग होते हैं।
वर्गाणां प्रथमद्वितीयाः शषसाश्चाघोषाः१।।१३।।
अर्थ-इन वर्गों में प्रथम द्वितीय अक्षर और श ष स अक्षर अघोष कहलाते हैं।।१३।।
जैसे-कख, चछ, टठ, तथ, पफ, श ष स। ये तेरह अक्षर।
घोषवन्तोऽन्ये।।१४।।
अर्थ-बचे हुए अक्षर घोषवान हैं।।१४।।
अघोष अक्षर से बचे हुए शेष तृतीय, चतुर्थ, पंचम अक्षर और य र ल व ह ये घोषवान संज्ञक हैं। जैसे-ग घ ङ, ज झ ञ, ड ढ ण, द ध न, ब भ म, य र ल व, ह। ये २० अक्षर घोष हैं।
अनुनासिका ङञणनमाः।।१५।।
अर्थ-ङ, ञ, ण, न, म ये अनुनासिक संज्ञक हैं।।१५।।
अनु-पश्चात् नासिका स्थान से जिनका उच्चारण होता है वे अनुनासिक कहलाते हैं। अर्थात् इन ङ, ञ, ण, न और म के उच्चारण में कुछ-कुछ ध्वनि नाक से भी निकलती है इसलिए ये अनुनासिक कहलाते हैं।
अन्तःस्था यरलवाः।।१६।।
अर्थ-य र ल व अक्षर अंतस्थ संज्ञक हैं।।१६।।
जो ओष्ठ आदि स्थानों के अंत में रहते हैं उन्हें अंतस्थ कहते हैं
ऊष्माणः शषसहाः।।१७।।
अर्थ-श, ष, स, ह अक्षर ऊष्म संज्ञक हैं।।१७।।
उष्ण धर्म को उत्पन्न करने वालों को ‘ऊष्म’ कहते हैं अर्थात् इनके उच्चारण काल में मुख से कुछ उष्ण वायु निकलती है।
अः इति विसर्जनीयः।।१८।।
अर्थ-‘‘अः’’ यह विसर्ग कहलाता है।।१८।।
जिसके बिना उच्चारण न किया जा सके वह उच्चारण के लिए होता है। यहाँ विसर्ग को बतलाने के लिए ‘अकार’ शब्द उच्चारण के लिए है। जैसे कः आदि में ‘क’ शब्द उच्चारण के लिए रहता है। यह विसर्ग सभी स्वर और व्यंजन में लगाया जाता है।
क इति जिह्वामूलीयः१।।१९।।
अर्थ-‘क’ यह वर्ण जिह्वामूलीय कहलाता है।।१९।।
यहां ककार उच्चारण के लिए है मतलब वङ्का्राकृति वर्ण जिह्वामूलीय संज्ञक होता है। ‘क²’२
पि इत्युपध्मानीयः३।।२०।।
अर्थ-‘प’ यह उपध्मानीय संज्ञक है।।२०।।
यहाँ ‘प’ शब्द उच्चारण के लिए है मतलब गजकुंभाकृति४ वर्ण को उपध्मानीय संज्ञा है
अं इत्यनुस्वार:।।२१।।
अर्थ-‘अं’ यह वर्ण अनुस्वार संज्ञक है।।२१।।
यहाँ भी अकार मात्र उच्चारण के लिए है। मतलब बिंदु मात्र वर्ण अनुस्वार संज्ञक है ऐसा समझना चाहिए।
लोकोपचाराद्ग्रहणसिद्धिः।।२२।।
अर्थ-लोकोपचार से शब्द ग्रहण की सिद्धि होती है।।२२।।
लोक के उपचार को व्यवहार कहते हैं। इसलिए यहाँ नहीं कहे गये भी ग्रहण-शब्दों की सिद्धि-प्रवृत्ति समझ लेना चाहिए।
प्रश्न-वह वैâसे ?
उत्तर-जैसे तुम्हारे द्वारा गाँव को जाया जाता है ऐसा वाक्य बनाने पर ‘तुम गाँव को जाते हो’ ऐसा अर्थ समझना चाहिए।
भावार्थ-जिसका दूसरा नाम है वाक्य या वृद्ध ज्ञानी जन का व्यवहार उससे तथा प्रसिद्ध पद के संयोग से निश्चय होता है। ‘सहकारे पिको विरौति’, यहाँ पिक-कोयल के संयोग से सहकार आम्र का निश्चय होता है।
।।संज्ञा प्रकरण समाप्त हुआ।।
अथ स्वर संधि
संधि किसे कहते हैं ?
पूर्व और उत्तर वर्णों का-दो पदों या अनेक पदों का व्यवधान-अंतराल के बिना परस्पर में संश्लेष हो जाना संधि कहलाती है। जैसे-
तव±अभ्युदयः, कान्ता±आगता, दधि±इदम्, नदी±ईहते आदि दो-दो पद हैं।१
अनतिक्रमयन्विश्लेषयेत् ।।२३।।
अर्थ-क्रम का उल्लंघन न करते हुए विश्लेषण करे।।२३।।
मिले हुए वर्णों में से क्रम का उल्लंघन न करते हुए पृथक्-पृथक् विश्लेषण करना चाहिए।२ जैसे-
तव् ± अ ± अभ्युदयः। कान्त् ± आ ± आगता। दध् ± इ ± इदम्। नद् ± ई ± ईहते। वस् उ ± उभयोः वध् ऊ ± उâढा, पित् ऋ ± ऋषभः, मात् ऋ ± ऋकारेण, व्â ऋ¸ ± ýकारः, व्â ऋ¸ ± ýकारेण इत्यादि।
अब सूत्र लगता है-
समानः सवर्णे दीर्घीभवति परश्च लोपम् ।।२४।।
अर्थ–सवर्ण के आने पर समान सवर्ण दीर्घ हो जाता है और पर का लोप हो जाता है।।२४।।
समान संज्ञा वाले वर्ण, आगे सवर्ण-उसी समान वर्ण के आने पर दीर्घ हो जाते हैं और आगे वाले स्वर का लोप हो जाता है। सभी जगह ह्रस्व तो दीर्घ हो जाता है और स्वभाव से ह्रस्व का अभाव होने पर (अर्थात् दीर्घ होने पर) आगे के स्वर का लोप हो जाता है।
व्यञ्जनमस्वरं परवर्णं नयेत् ।।२५।।
अर्थ-स्वर रहित व्यंजन अगले स्वर को प्राप्त कर लेते हैं।।२५।।
तो-तवाभ्युदयः, कांतागता, दधीदम्, नदीहते, वसूभयोः, वधूढा, पित¸षभः, मात¸कारेण, व¸âकारः, व¸âकारेण। इस प्रकार संधि हो जाने से ये पद सिद्ध हो गये।
आगे ‘होतृ ± ऋकारः’ यह विग्रह है-
इसमें ‘समानः सवर्णे दीर्घी भवति परश्च लोपम्’ इस सूत्र से एक बार दीर्घ होकर ‘‘होत¸कारः’’ बन गया है। पुनः-
ऋति ऋतोर्लोपो वा।।२६।।
अर्थ-ऋकार के आने पर ऋकार का लोप विकल्प से होता है।।२६।।
ऋकार के आने पर पूर्व के ऋकार को दीर्घ विकल्प से होता है और अगले ऋकार का लोप होता ही होता है। जैसे-
होतृ ± ऋकारः· होतृकारः भी बना है। देव ± इन्द्रः, कान्ता ± इयम् ये शब्द स्थित हैं-
अवर्ण इवर्णे ए।।२७।।
अर्थ-इवर्ण के आने पर अवर्ण को ‘ए’ होकर अगले स्वर का लोप हो जाता है।।२७।।
यहाँ सूत्र में वर्ण के ग्रहण करने से सवर्ण का ग्रहण हुआ समझना चाहिए। अतः-
देव् अ ± इन्द्रः · देव् ए ± न्द्रः· देवेन्द्रः।
कान्त् आ ± इयं · कान्त् ए ± यं · कान्तेयम्। हल ± ईषा, लांगल ± ईषा।
हललाङ्गलयोरीषायामस्य लोपः।।२८।।
अर्थ-ईषा के आने पर हल और लाङ्गल के ‘अकार’ का लोप हो जाता है।।२८।।
हल् ± ईषा· हलीषा, लाङ्गल ± ईषा· लाङ्गलीषा। मनस् ± ईषा।
मनसः सस्य च ।।२९।।
अर्थ-ईषा के आने पर ‘मनस्’ के ‘अस्’ का लोप हो जाता है।।२९।।
मन् ईषा· मनीषा। गंध ± उदकम्, माला ± ऊढा।
उवर्णे ओ।।३०।।
अर्थ-उवर्ण के आने पर अवर्ण को ‘ओ’ हो जाता है।।३०।।
अर्थात् आगे उवर्ण के आने पर पूर्व के अवर्ण को ‘ओ’ होकर अगले उवर्ण का लोप हो जाता है। जैसे-गंध् ओ दकम् · गंधोदकम्, माल् ओ ढा · मालोढा।
तव ± ऋकारः, सा ± ऋकारेण।
ऋवर्णे अर्।।३१।।
अर्थ-ऋवर्ण के परे अवर्ण को अर् हो जाता है।।३१।।
अवर्ण से परे ऋवर्ण के आने पर ‘अवर्ण’ को ‘अर्’ हो जाता है और ऋवर्ण का लोप हो जाता है तब-
तव् अर् कारः · ‘तवर्कारः’ बन जाता है पुनः यह अर्थ रकार यदि व्यञ्जन से पूर्व में रहता है तो ऊपर चला जाता है और यदि व्यञ्जन से आगे रहता है तो नीचे लग जाता है।
रेफाक्रान्तस्य द्वित्वमशिटो वा।।३२।।
अर्थ-शिट् के न होने पर रेफ से सहित अक्षर को विकल्प से द्वित्व हो जाता है।।३२।।
शिट् किसे कहते हैं ?
शिडिति शादयः।।३३।।
अर्थ-श, ष, स, ह इन चार वर्णों की ‘शिट्’ संज्ञा है।।३३।।
तवर्क्कारः, स् अर् क्कारेण· सर्क्कारेण बन गया।
ऋण ± ऋणम् , प ± ऋणम् इत्यादि
सूत्र लगा ‘ऋवर्णे अर्’ इस सूत्र से ऋण् अर् ± णम् आदि बन गये। पुनः ३४वां सूत्र लगा।]
ऋणप्रवसनवत्सतरकम्बलदशानामृणेऽरो दीर्घः।।३४।।
अर्थ-ऋण से परे ऋण और प्र, वसन, वत्सतर, कम्बल और दश इनके अर् को दीर्घ हो जाता है।।३४।।
तब-ऋण् आर् णम् · ऋणार्णम्, प्र् आर् ± णम् · प्रार्णम्, वसन् आर् ± णम् · वसनार्णम् , वत्सतरार्णम् , कम्बलार्णम् , दशार्णम् । शीत ± ऋतः, दुःख ± ऋतः।
इसमें समास का प्रकरण है तो इनका विग्रह- शीतेन ऋतः। शीत टा स्थित है समास के प्रकरण में ‘‘तत्स्थालोप्या विभक्तयः’’ सूत्र से ‘टा’ विभक्ति का लोप होकर ‘शीत± ऋतः’ स्थित है। ‘‘ऋवर्णे अर्’’ इस सूत्र से शीत् अर् ± तः बन गया। पुनः सूत्र लगा-
ऋते च तृतीयासमासे।।३५।।
अर्थ-तृतीया समास के प्रकरण में ऋवर्ण के आने पर अर् को दीर्घ हो जाता है।।३५।।
तब शीतार्तः, दुःखार्तः बना।
यहाँ ‘तृतीया समास में’ ऐसा क्यों कहा ?
कर्मधारय समास में अर् को दीर्घ नहीं होता है जैसे-परमश्चासौ ऋतश्च।
परम ± ऋतः · परमर्तः बन गया। तव ± ऌकारः, सा ± ल¸कारेण।
ऌवर्णे अल् ।।३६।।
अर्थ-ऌवर्ण के आने पर अवर्ण को अल् हो जाता है।।३६।।
और अगले ऌवर्ण का लोप हो जाता है।
तव् अल् ± कारः · तवल्कारः, स् अल् ± कारेण· सल्कारेण बन गया।
तव ± एषा, सा±ऐन्द्री।
एकारे ऐ ऐकारे च।।३७।।
अर्थ-आगे ए, ऐ के आने पर अवर्ण को ‘ऐ’ हो जाता है।।३७।।
और अगले स्वर का लोप हो जाता है।
तव् ऐ ± षा· तवैषा, स् ऐ ± न्द्री · सैन्द्री। स्व ± ईरम्, स्व±ईरिणी, स्व±ईरी।
इसमें ‘अवर्ण इवर्णे ए’ सूत्र लग रहा था किन्तु इसको बाधित करके आगे सूत्र लगता है-
स्वस्येरेरिणीरिषु।।३८।।
अर्थ-ईर, ईरिणी और ईरी के आने पर ‘स्व’ के ‘अकार’ को ‘ऐ’ हो जाता है।।३८।।
अगले ईवर्ण का लोप हो जाता है।
स्व् ऐ± रम् · स्वैरम् , स्व् ऐ ± रिणी · स्वैिरणी, स्व् ऐ ± री· स्वैरी।
अद्य ± एव, इह ± एव।
इसमें भी ‘एकारे ऐ ऐकारे च’ सूत्र से ‘अद्यैव’ ‘इहैव’ बनने वाला था किन्तु अगले सूत्र से विकल्प हो गया।
एवे चानियोगे नित्यम् ।।३९।।
अर्थ-अनियोग अर्थ में आगे ‘एव’ शब्द के आने पर नियम से अवर्ण का लोप हो जाता है।।३९।।
तब-अद्य् ± एव · अद्येव, इह ± एव · इहेव बन गया। इसका अर्थ आज्ञा एवं प्रेरणा नहीं है जैसे कि कोई किसी को कह रहा है कि ‘अद्येव गच्छ’ आज ही जाना चाहिए। जावो या न जावो जबर्दस्ती नहीं है किन्तु पूर्ववत् सन्धि में नियोग अर्थ-आज्ञा या प्रेरणा अर्थ विशेष होता है जैसे ‘‘अद्यैव गच्छ’’ आज ही जावो इत्यादि।
तव ± ओदनम्, सा ± औपगवी।
ओकारे औ औकारे च।।४०।।
अर्थ-ओ औ के आने पर अवर्ण को ‘औ’ हो जाता है।।४०।।
और पीछे ओ औ वर्ण का लोप हो जाता है।
तव् औ ± दनम् · तवौदनम्। स् औ ± पगवी · सौपगवी बन गया। ‘ओकारे औ औकारे च’ इस सूत्र में ‘च’ शब्द है इसका यह अर्थ होता है कि उपसर्ग से परे ए और ओ है आदि में जिसके ऐसी धातुओं के आने पर उपसर्ग के ‘अ’ का लोप हो जाता है।
प्र् अ ± एलयति · प्रेलयति, पर् आ ± ओखति· परोखति।
इण् और एध् धातु से एति और एधते क्रियायें बनती हैं यद्यपि इन दोनों क्रियाओं में आदि में ‘एकार’ है फिर भी ‘इणेधत्योर्न’ इस नियम के अनुसार इन धातुओं के आने पर पूर्व के उपसर्ग के अकार का लोप नहीं होता है। तो पूर्व के ‘एकारे ऐ ऐकारे च’ सूत्र से अवर्ण को ‘ऐ’ होकर अगले स्वर का लोप हो जाता है।
उप ± एति, उप् ए ± ति · उपैति, उप ± एधते उप् ऐ ± धते · उपैधते।
जो नामवाची शब्द से धातु बनकर क्रिया बने हैं उनमें विकल्प है अर्थात् ‘अ’ का लोप भी होता है और पूर्ववत् संधि हो जाती है जैसे-
उप ± एलकीयति, उप् ± एलकीयति·उपेलकीयति अथवा उप् ऐ ± लकीयति· उपैलकीयति। प्र ± ओषधीयति प्र् ± ओषधीयति· प्रोषधीयति, प्र् औ ± षधीयति· प्रौषधीयति बन जाता है। अद्य ± ओम् , सा ± ओम्।
ओमि च ।।४१।।
अर्थ-ओम् शब्द के आने पर नित्य ही अवर्ण का लोप हो जाता है।।४१।।
अद्य् अ ओम्, अद्य् ± ओम् · अद्योम्, स् आ ± ओम्, स् ± ओम् · सोम् बन गया।
बिम्ब ± ओष्ठः, स्थूूल ± ओतुः
ओष्ठौत्वोः समासे वा।।४२।।
अर्थ-समास के विषय में ओष्ठ और ओतु शब्द के आने पर विकल्प से अवर्ण का लोप होता है।।४२।।
बिम्ब के समान है ओष्ठ जिसका ऐसा-
बिम्ब् अ ± ओष्ठः ‘अ’ का लोप होने पर बिम्बोष्ठः और संधि होने पर बिम्बौष्ठः। स्थूल् अ ± ओतुः · स्थूलोतुः, स्थूलौतुः। जब समास का प्रकरण नहीं है तब अवर्ण का लोप नहीं होगा। जैसे-हे पुत्र ! ओष्ठं पश्य, पुत्र ± ओष्ठं · पुत्रौष्ठं बन गया। अक्ष ± ऊहिनी।
अक्षस्य ऊहिन्याम् ।।४३।।
अर्थ-ऊहिनी-सेना शब्द के आने पर अक्ष के ‘अ’ को औ होकर पर का लोप हो जाता है।।४३।।
अर्थात् ‘उवर्णे ओ’ से ‘ओ’ होना चाहिए था किन्तु इस स्वतंत्र सूत्र से औ हो गया तो-
अक्ष् औ ± हिनी · अक्षौहिनी बना पुनः ‘रषृवर्णेभ्यो’ इत्यादि सूत्र से ‘न’ को ‘ण’ होकर अक्षौहिणी हो गया।
प्र से परे ऊढः और ऊढ़िः शब्द के आने पर ‘अ’ को ‘औ’ होकर ‘ऊ’ का लोप हो जाता है।
प्र् औ ± ढः · प्रौढः, प्र् औ ± ढिः· प्रौढिः।
प्र से परे एषः और एष्यः के आने पर ‘अ’ को ‘ऐ’ होकर पर का लोप हो गया।
प्र् अ ± एषः, प्र् ऐ ± षः · प्रैषः, प्र् ऐ ±ष्यः· प्रैष्यः बना। दधि ± अत्र, नदी ± एषा।
इवर्णो यमसवर्णे न च परो लोप्यः।।४४।।
अर्थ-इवर्ण से परे-आगे असवर्ण वर्ण के आने पर इवर्ण को ‘य्’ होता है और पर का लोप नहीं होता है।।४४।।
दध् इ ± अत्र, दध् य् ± अत्र ‘व्यञ्जनमस्वरं परवर्णं नयेत्’ इस सूत्र से स्वर रहित व्यंजन अगले स्वर में मिल जाते हैं तो दध्यत्र बन जाता है। नद् य् ± एषा·नद्येषा।
मधु ± अत्र, वधू ± आसनम् ।
वमुवर्णः।।४५।।
अर्थ-उवर्ण को ‘व्’ हो जाता है।।४५।।
यदि आगे उवर्ण न होकर असवर्ण स्वर हो तो उवर्ण को ‘व्’ होकर अगले स्वर का लोप नहीं होता है जैसे-
मध् उ ± अत्र, मध् व् ± अत्र· मध्वत्र, वध् ऊ ± आसनम् · वध्वासनम् ।
पितृ ± अर्थः, मातृ ± अर्थः।
रमृवर्णः।।४६।।
अर्थ-ऋवर्ण को ‘र्’ हो जाता है।।४६।।
असवर्ण स्वर के आने पर -पित् ऋ ± अर्थः, पित् र् ± अर्थः · पित्रर्थः,
मात् र् ± अर्थः· मात्रर्थः। ऌ ± अनुबंधः, ऌ ± आकृतिः।
लम्ऌवर्णः।।४७।।
अर्थ-असवर्ण स्वर के आने पर ऌवर्ण को ‘ल्’ हो जाता है।।४७।।
एवं पर का लोप नहीं होता है।
ल् ± अनुबंधः · लनुबंधः, ल् ± आकृतिः· लाकृतिः। ने ± अनम्, चे ± अनम्।
ए अय् ।।४८।।
अर्थ-आगे स्वर के आने पर एकार को अय् हो जाता है।।४८।।
एवं पर का लोप नहीं होता है।
न् ए ± अनम्, न् अ य् ± अनम् · नयनम्, च् अ य् ± अनम् · चयनम् ।
नै ± अकः, चै ± अकः।
ऐ आय् ।।४९।।
अर्थ-ऐ को ‘आय्’ हो जाता है।।४९।।
और पर का लोप नहीं होता है।
न् ऐ ± अकः, न् आय् ± अकः · नायकः, च् आय् ± अकः · चायकः।
लो ± अनम्, पो ± अनम् ।
ओ अव् ।।५०।।
अर्थ-ओ को अव् हो जाता है।।५०।।
और आगे का लोप नहीं होता है।
ल् ओ ± अनम् , ल् अव् ± अनम् ·लवनम्, प् ओ ± अनम्, प् अव् ± अनम् · पवनम् ।
लौ ± अकः, पौ ± अकः।
औ आव् ।।५१।।
अर्थ-स्वर के आने पर औ को आव् हो जाता है।।५१।।
एवं पर का लोप नहीं होता है।
ल् औ ± अकः ल् आव् ± अकः · लावकः, प् आव् ± अकः · पावकः।
गो ± अजिनम् ।
गोर इति वा प्रकृतिः।।५२।।
अर्थ-अकार के आने पर ‘गो’ शब्द की विव्ाâल्प से संधि नहीं भी होती है।।५२।।
गो अजिनम् वा। आगे के ५७वें ‘एदोत्परः पदांते लोपमकारः’ सूत्र से ‘अकार’ का लोप हो जाता तो गोऽजिनम् बना। और अगले ५३वें सूत्र से गो के ओ को अव आदेश होकर ‘समानः सवर्णे दीर्घी’ इत्यादि से दीर्घ होकर ग् अव ± अजिनम् · गवाजिनम् हो गया।
गो ± अश्वौ, गो ± ईहा, गो ± उष्ट्रौ, गो ± एलकौ।
अवः स्वरे।।५३।।
अर्थ-गो शब्द को ‘अव’ आदेश हो जाता है।।५३।।
स्वर के आने पर विकल्प से। जैसे-एक बार ५२वें सूत्र से प्रकृति ही रहता है तो ‘गो अश्वौ’ ‘एदोत्परः’ इत्यादि सूत्र से ‘‘अ’’ का लोप होकर गोश्वौ, और ओ को ‘अव’ होने से ‘गवाश्वौ’ बन गया।
वैसे ग् अव ± ईहा· ‘अवर्ण इवर्णे ए’ से गवेहा। ‘ओ अव्’ सूत्र से ग् अव् ± ईहा· गवीहा। ग् अव ± उष्ट्रौ ‘उवर्णे ओ’ से गवोष्ट्रौ एवं ‘ओ अव्’ से गव् ± उष्ट्रौ · गवुष्ट्रौ बना। ग् अव ± एलकौ · गवैलकौ, ग् अव् ± एलकौ · गवेलकौ बना। गो ± अक्ष, गो ± इन्द्रः।
अक्षेन्द्रियोर्नित्यम् ।।५४।।
अर्थ-अक्ष और इन्द्र के आने पर नियम से गो के ओ को ‘अव’ आदेश हो जाता है।।५४।।
ग् अव ± अक्षः ‘समानः सवर्णे’ इत्यादि सूत्र से दीर्घ होकर गवाक्षः, ग् अव ± इन्द्रः ‘अवर्ण इवर्णे ए’ से संधि होकर गव् ए ± इन्द्रः · गवेन्द्रः।
ते ± आहुः, तस्मै ± आसनम्, पटो ± इह, असौ ± इन्दुः।
पहले इनमें ‘‘ए अय्, ऐ आय्, ओ अव्, औ आव्,’’ सूत्रों से संधि कर लीजिए।
तय् ± आहुः, तस्माय् ± आसनम्, पटव् ± इह, असाव् ± इंदुः।
अयादीनां यवलोपः पदान्ते न वा लोपे तु प्रकृतिः।।५५।।
अर्थ-पद के अंत में विद्यमान अय् अव् आदि के ‘य् व्’ का विकल्प से लोप हो जाता है और लोप होने पर संधि नहीं होती है।।५५।।
तय् ± आहुः य् का लोप होने पर त आहुः, लोप नहीं होने पर तयाहुः, लोप होने पर तस्मा आसनम्, नहीं होने पर तस्मायासनम्, पट इह, पटविह, असा इन्दुः, असाविंदुः।
नै ± ऋ ± अदः, रै ± उ ± अणः, मै ± ऋ ± उतः, ओ ± उ ± इंदुः, रिपु ± इ ± उदयः।
पहले ‘ऐ आय्’ सूत्र से नाय् ± ऋ ± अदः, राय् ± उ ± अणः, माय् ± ऋ ± उतः, ‘ओ अव्’ से अव् ± उ ± इंदुः ‘वमुवर्णः’ से रिप् व् ± इ ± उदयः है। पुनः ‘रमृवर्णः’ और ‘वमुवर्णः’ से ऋ को र, उ को व् ‘‘इवर्णोः यमसवर्णे’’ इत्यादि से इ को य् हुआ तो नाय् ± र् ± अदः, राय् ± व् ± अणः, माय् ± र् ± उतः, अव् ± व् ± इंदुः, रिप् व् ± य् ± उदयः। पुनः सूत्र लगा।
स्वरजौ यवकारावनादिस्थौ लोप्यौ व्यञ्जने।।५६।।
अर्थ-जो स्वर से उत्पन्न हुए ‘य् व्’ हैं और आदि में स्थित नहीं हैं, आगे व्यंजन के आने पर उन य् व् का लोप हो जाता है।।५६।।
यहाँ विकल्प नहीं है अतः
नाय् ± र् ± अदः · य् का लोप होकर · नारदः, राय् ± व् ± अणः य् का लोप होकर · रावणः, माय् ± र् ± उतः· य् का लोप · मारुतः। अव् ± व् ± इंदुः · व् का लोप· अविन्दुः, रिप् व् ± य् ± उदयः · व् का लोप · रिप्युदयः । ये शब्द सिद्ध हो गये।
ते ± अत्र, पटो ± अत्र।
एदोत्परः पदान्ते लोपमकारः।।५७।।
अर्थ-पद के अंत में ए ओ के होने पर उससे परे ‘अ’ का लोप हो जाता है।।५७।।
यहाँ एत् ओत् में जो तकार है उससे ऐसा समझना कि मात्र ‘ए ओ’ का ही नियम है ‘ऐ औ’ नहीं लिये जा सकेंगे। कार और त् के लगा देने से मात्र उसी अक्षर का बोध होता है जैसे अकार या अत् शब्द से मात्र ‘अ’ ही ग्रहण किया जाता है। अतः ‘अ’ का लोप होकर तेत्र, पटो ± त्र· पटोत्र बना। इस संधि में अ को समझने के लिए खंडाकार चिन्ह भी दिया जाता है। जैसे तेऽत्र, पटोऽत्र।
देवी ± गृहम्, पटु ± हस्तः, मातृ± मुखम्, जले ± पद्मम्, रै ± धृतिः, गो ± गतिः, नौ ± यानम् ।
न व्यञ्जने स्वराः सन्धेयाः।।५८।।
अर्थ-आगे व्यंजन के आने पर पूर्व के स्वरों की संधि नहीं होती है।।५८।।
अतः उपर्युक्त पद ज्यों के त्यों रह गये तो देवीगृहम्, पटुहस्तः आदि ही रहे।
पितृ ± यम्, भ्रातृ ± यम्, मातृ±यम्।
र ऋतस्तद्धिते ये।।५९।।
अर्थ-आगे तद्धित के यकार के आने पर ‘ऋ’ को र् हो जाता है।।५९।।
यहाँ व्यंञ्जन के आने पर भी तद्धित के प्रत्यय यकार के लिए एवं ‘ऋ’ को र् के लिए ही यह संधि हुई है। तो-
पित् र् ± यम् · पित्र्यम्, भ्रात् र् ± यम् · भ्रात्र्यम्, मात् र् ± यम् · मात्र्यम्।
गो ± यूतिः।
गव्यूतिरध्वमाने।।६०।।
अर्थ-मार्ग के माप अर्थ में गव्यूति शब्द निपात से सिद्ध हो जाता है।।६०।।
गवां ± यूतिः,-ग् अव् ± यूतिः ·गव्यूतिः बन गया।
जिसमें सूत्र का नियम लगकर संधि आदि कार्य न होवें उसे ‘निपात’ कहते हैं।
।। इस प्रकार से स्वर संधि समाप्त हुई ।।
