पद्मनंदीपञ्चविंशतिका पद्यानुवाद
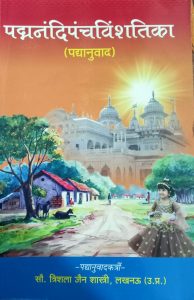
मंगलाचरण
।।‘‘श्री ऋषभदेवाय नम:” ।।
।।”ॐ श्री महावीराय नम:’’।।
।।‘‘श्री ज्ञानमती मात्रे नम:’’।।
।।‘‘श्री रत्नमती मात्रे नम:’’।।
मंगलाचरण
श्री नाभिराज सुत ऋषभ को कोटि कोटि प्रणाम।
पुन: ज्ञानमती मात का श्रद्धा से कर ध्यान।।
जिनने पढ़ इस ग्रंथ को किया आत्मकल्याण।
ऐसी माता मोहिनी को मेरा बारम्बार प्रणाम।।
(१) श्री आदिनाथ तीर्थंकर बन कर्मों को नष्ट किया ऐसे।
इक पल में पवन झकोरे से सब काष्ठ समूह जले जैसे।।
उनकी ध्यानाग्नि सूर्य से भी थी अधिक तेज वाली देखो।
जयवंत रहे श्री ऋषभेश्वर विस्तीर्ण कायधारी थे वो।।
(२) करने लायक कुछ कार्य नहीं इसलिए भुजाएं लटका दीं।
जाने को बची न कोई जगह इसलिए खड़े थे निश्चल ही।।
नहिं रहा देखने को कुछ भी इसलिए दृष्टि नासा पर की।
अत्यन्त निराकुल हुए प्रभो इसलिए उन्हें पूजें नित ही।।
(३) जो रागद्वेष अरु अस्त्र शस्त्र विरहित अर्हंत जिनेश्वर हैं।
जो इन सबसे हो सहित देव रहता भयभीत निरन्तर है।।
वह क्या रक्षा कर सकता है हम सबकी जो खुद डरा हुआ।
इसलिए वीतरागी प्रभु के चरणों की मैंने शरण लिया।।
(४) भगवन के चरण कमल जैसे धूली से रहित प्रभा वाले।
इंद्रों के मणिमय मुकुटों की आभा से लगते अति प्यारे।
ऐसे चरणों के वंदन से सब पाप नष्ट हो जाते हैं।
हैं कमल अचेतन फिर भी प्रभु पदकमल तो पाप नशाते हैं।।
(५) तीनों लोकों के जो स्वामी श्री शांतिनाथ भगवान हुए।
उनके पद में मैं नमन करूँ मन का संताप दूर करिए।।
देवों के नीलमणि से युत मुकुटों की जो कांती रहती।
लगता प्रभु के पदकमलों पर भ्रमरों की ही पंक्ति चलती।।
(६) सब ज्ञाता दृष्टा त्रिभुवन के और क्रोध लोभ से रहित प्रभो।
सत् वचन बोलने वाले वे जिनदेव सदा जयवंत रहो।।
वे मोक्षगमन करने वाले प्राणी के लिए खिवैया हैं।
उत्कृष्ट धर्म को बतलाया जिससे तिरती हर नैया है।।
धर्मोपदेशामृत
(प्रथम अधिकार)
(७) अब आवो बताएँ तुम्हें जिनधर्म की व्याख्या।
सब जीवों पे दया करो उसके हैं भेद क्या।।
दो रूप धर्म मुनि और गृहस्थ के कहे।
फिर रत्नत्रय स्वरूप से त्रयभेद भी कहे।।
इस एकदेश धर्म को गृहस्थ पालते।
उत्कृष्ट रत्नत्रय जो धर्म साधु धारते।।
यहाँ और भी क्षमादि गुण से दश धरम कहे।
उसमें जो आत्मा की परिणति से सुख लहे।।
(८) सब ही व्रतों में मुख्य यह दया ही श्रेष्ठ है।
जैसे बिना जड़ के ठहर सकता न पेड़ है।।
जिसमें नहीं दया वो शून्य के समान है।
निर्दय हृदय को कुछ भी रहता न भान है।।
(९) चिरकाल भवभ्रमण में हम क्या क्या नहीं बने।
माता पिता भाई बहन हम सबके बन चुके।
पिछले भवों के रागद्वेष वश हो मारते।
जन्मान्तरों के बैर को गुरुजन धिक्कारते।।
(१०) यदि किसी दरिद्री से कहिए वह अपने प्राणदान दे दे।
बदले में जितनी चाहे वो मुझसे मेरी संपति ले ले।।
लेकिन जब इसको ठुकरा दे तो समझो तुम हे पुरुषोत्तम।
आहार अभय औषधि व शास्त्र ये चार दान सबसे उत्तम।।
(११) व्रत रहित अव्रती भी यदि हो इस दया भाव से भरा हुआ।
वह स्वर्ग मोक्ष का अधिकारी बन जाता है यह कहा गया।।
लेकिन जो दया रहित प्राणी कितना भी भीषण तप कर ले।
वह पापी ही समझा जाता सब दान पुण्य भी व्यर्थ रहें।।
(१२) जो रत्नत्रयधारी मुनि को भक्ती से उत्तम दान करे।
ऐसे गृहस्थ अरु मुनियों को खुद सुरगण सदा प्रणाम करें।।
क्योंकि मानुष तन द्वारा ही परमेष्ठि साधु बन सकते हैं।
इस तन से ही बस मोक्ष मिले वहाँ इंद्र नहीं जा सकते हैं।।
(१३) जिस घर में पूजा होती है अर्हंत सिद्ध आचार्यों की।
भक्ति से दान दिया जाता निग्र्र्रंथ तपस्वी गुरुओं को।।
करूणा से दान दिया जाता जो दुखी दरिद्र मनुष्य दिखें।
ऐसे गृहस्थ सम्यग्दृष्टि विद्वानों से भी पूज्य हुए।।
ग्यारह प्रतिमाओं के नाम
(१४) आचार्य पद्मनंदि जी ने ग्यारह प्रतिमा बतलाई हैं।
जो दर्शन, व्रत, सामायिक और चौथी प्रोषध कहलाई हैं।।
सचित्तत्याग, रात्रिभोजन सातवीं ब्रह्मचर्य प्रतिमा।
आरम्भ, परिग्रह व अनुमति त्याग, भिक्षापूर्वक भोजन लेना।।
(१५) श्री समन्तभद्र आदिक आचार्य ने और भी विस्तृत व्याख्या की।
अतएव उपासकाध्ययन ग्रंथ से पढ़ने की भी आज्ञा दी।।
गुरुओं ने सप्त व्यसन त्यागे बिन प्रतिमा लेना व्यर्थ कही।
जो व्यसन रहित सज्जन प्राणी उनको ही पूज्यता प्राप्त हुई।।
सप्तव्यसन के नाम
(१६) -दोहा- जुआँ खेलना, मांस, मद्य, वेश्यागमन, शिकार।
चोरी, पररमणी रमण ये सातों व्यसन निवार।।
इन सातों व्यसनों का क्रमश: आचार्य प्ररूपण करते हैं।
इनसे क्या हानि होती है उसका कुछ वर्णन करते हैं।।
गर उसको समझे प्राणी तो मानव जीवन सार्थक होगा।
आत्मा उत्थान करेगी और परभव में उत्तम फल होना।।
जुआँ का स्वरूप
(१७) इस जुआँ खेलने से जग में अपर्कीित फैलती है सच में।
क्योंकि चोरी वेश्यावृत्ति इन सबका मेल हुआ इसमें।।
जिस तरह राज्य में राजा के आधीन मंत्रिगण होते हैं।।
बस इसी तरह यह जुआँ व्यसन आपत्तीकारक होते हैं।।
(१८) आचार्यों ने सारे व्यसनों में जुआँ को सबसे मुख्य कहा।
क्योंकि इससे बनकर दरिद्र बनकर आगे प्राणी विपदा में घिरा।।
जब विपदा आती तब मानव क्रोधित हो लोभ में फसता है।
इसलिए त्याग कर दो भविजन इससे बस दुख ही मिलता है।
मांस भक्षण का विरोध
(१९) जो सज्जन पुरुषों के द्वारा आँखों से देखा जा न सके।
जो दीन प्राणियों का वध कर खाते उनको हम छू न सके।।
ऐसे सर्वथा अपावन मांसाहार का जो भक्षण करते।
ना जाने कितने पापों का संचय कर नरकगती लहते।।
(२०) यदि कोई अपना पिता पुत्र बाहर से लौट के ना आये।
तो नर हो या फिर नारी हो वह बिलख बिलख कर चिल्लाये।
फिर कैसे मूक प्राणियों का वह माँस बनाकर खाता है।
आती है दया और लज्जा कैसे कट कर चिल्लाता है।।
मदिरा का निषेध
(२१) यह मदिरा पीने वाला भी धन धर्म सभी को नष्ट करे।
नरकों में जाने का भी डर इनको न कभी भी त्रस्त करे।।
यदि समझाने से भी मानव मदिरा सेवन नहिं त्याग करे।
तो समझो वह व्यसनी कोई उत्कृष्ट न कोई कार्य करे।।
(२२) मदिरा पीने वाला मानव माता को भी स्त्री माने।
खोटी चेष्टाएँ कर करके कोई भी बात नहीं माने।।
उससे भी अधिक जब नशा चढ़े तब कुत्ते भी यदि मूत्र करें।
उसको भी मिष्ट मिष्ट कहकर वह पापी उसको गटक रहे।।
वेश्यागमन
(२३) जो मद्य माँस सेवन करती जिनका स्नेह दिखावा है।
विषयी पुरुषों को बहलाकर धन लेकर करे छलावा है।।
ऐसी वेश्याओं का सेवन करने से नरकद्वार खुलता।
धन और प्रतिष्ठा भी खोकर आगे कुछ हाथ नहीं लगता।।
(२४) जैसे धोबी सबके कपड़े इक शिला पे जाकर धोता है।
वैसे ही वेश्या के समीप सब तरह का प्राणी रमता है।।
जिस तरह माँस के एक पिण्ड पर कुत्ते लड़ते रहते हैं।
ऐसे वेश्यागामी पुरुषों को तत्सम उपमा देते हैं।।
शिकार का निषेध
(२५) जो सदा वनों में भ्रमण करें जिनका निज देह सिवा न कोई।
जो तृण खाकर जीवित रहते रक्षक भी जिनका नहिं कोई।।
ऐसे में जो मांसाहारी लोभी शिकार करते मृग का।
इहलोक व्याधियों से पीड़ित परलोक नरक में घर उनका।।
(२६) आचार्य पुन: समझाते हैं इक चींटी जब पीड़ा देती।
तो भी क्यों मानव दयाहीन पशु पक्षी पर कुदृष्टि रहती।।
जो भलीभाँति यह समझ रहे हैं इनको भी पीड़ा होती।
फिर भी ऐसे दुष्कर्म करें फिर इनकी कौन गती होगी।।
(२७) जिनको तुम आज मारते हो भव भव में आगे मारेगा।
जिसको तुम सब ठग रहे आज वह कल तुमसे बदला लेगा।
शास्त्रों का और विज्ञजन का यह ही तो कहना रहा सदा।
पर फिर भी इनमें लगे रहे कुछ भी ना ज्ञान हमें रहता।।
चोरी करने का दोष
(२८) छल कपट दगाबाजी से जो परद्रव्य हड़प कर लेते हैं।
वे प्राणहरण से भी ज्यादा उस प्राणी को दुख देते हैं।।
क्योंकि धन प्राणों से प्यारा होता है सूक्ति कही जाती।
इसलिए कहा है गुरुओं ने, परद्रव्य में प्रीति न की जाती।।
परस्त्री सेवन की हानि
(२९) परस्त्री का सेवन जो करे भय िंचता आकुलता रहती।
संतप्त सदा रहता प्राणी निंह बुद्धि ठिकाने पर रहती।।
क्षुध तृषा रोग से पीड़ित वह जब नरकगती में जाता है।
लोहे की बनी पुतली से आिंलगन करवाया जाता है।।
(३०) इतना ही नहीं स्वप्न में भी जो परस्त्री का ध्यान करे।
आचार्य उसे समझाते हैं ऐसा पौरुष भी व्यर्थ अरे।।
पर धन वनिता दिलवाने में जो बनते बड़े सहायक हैं।
ऐसे मित्रों से दूर रहें दुर्बुद्धी देते घातक है।।
सप्तव्यसन में जिनको हानि हुई
(३१) जो जुएं में सब कुछ हार गये वे हुए युधिष्ठिर राजा हैं।
अरु मांस का भक्षण करने में सब छूटा वे बक राजा हैं।।
मदिरा पीने से यदुवंशी राजा के पुत्र विनष्ट हुए।
वेश्यासेवन में चारुदत्त होकर दरिद्र अतिकष्ट सहें।।
ब्रह्मदत्त नाम के राजा भी करके शिकार पदभ्रष्ट हुए।
चोरी करने में सत्यघोष को गोबर भक्षण दण्ड मिले।।
परस्त्री सेवन से रावण ने दुख सहे अरु नरक गए।
इसलिए त्याग दो सप्त व्यसन आचार्य हमारे यही कहें।।
(३२) आचार्य और भी कहते हैं केवल ये व्यसन न दुखदायी।
इनसे अतिरिक्त अल्पबुद्धी मिथ्यादृष्टी जो हैं भाई।।
वे कई तरह के गलत मार्ग से जन धन की हानी करते।
इसलिए कुमार्ग छोड़ करके सत्पथ पर चलने को कहते।।
(३३) जिनकी बुद्धी अति निर्मल है जो आत्मा का हित चाह रहे।
वे कभी न झुकते व्यसनों में जो स्वर्ग मोक्ष सुख चाह रहे।।
सब व्रत के नाशक परमशत्रु ये व्यसन प्रथम तो मधुर लगें।
पर अंत में कटु फल मिलता है इसलिए स्वप्न में भी न गहें।।
(३४) हे भव्य जीव यदि सुख चाहो तो दुर्जन की संगति न करो।
क्योंकी जैसी संगति होती वैसी ही बुद्धि की प्राप्ति हो।।
यदि उत्तम पथ पर चलना है तो सत्पुरुषों के संग रहो।
इससे निंह बुद्धि भ्रमित होगी निंह दुर्गतियों में भ्रमण करो।।
(३५) जब दुष्ट पुरुष को काम पड़े तो मीठे वचन प्रयोग करें।
लेकिन गुरुवर समझाते हैं उससे न कभी संबंध रखें।।
जैसे सरसों जब खली रूप पर्याय में परिणत होती है।
तब उसका तेल अगर आँखों में लगे तो आँखें रोती हैं।।
(३६) जिस तरह ग्रीष्म ऋतु में मछली जल के अभाव में मर जाती।
कुछ एक अगर जीवित बचतीं तो बगुले से खाई जाती।।
बस इसी तरह इस कलियुग में सज्जन प्राणी कम ही होते।
यदि हो भी जाएं इक आधे तो दुष्ट नहीं जीने देते।।
(३७) आचार्य अंत में कहते हैं यदि रहे दरिद्री तो अच्छा।
नाना पीड़ाएं सह करके मर जाना भी तो है अच्छा।।
पर नहीं दुर्जनों के संग में व्यापार आदि संबंध करें।
क्योंकी वैसी ही बुद्धी से प्राणी कर्मों का बंध करे।।
मुनिधर्म का कथन
(३८) आचार पांच दशधर्म और बारह संयम तप भी बारह।
अरु अष्टमूलगुण उत्तरगुण चौरासी लख धारें मुनिवर।।
मिथ्यात्व मोह मद त्याग और शम दम से ध्यान प्रमाद रहित।।
वैराग्य और रत्नत्रय गुण धरते, मुनि अंत समाधि सहित।।
(३९) मुनि अपने चित्चैतन्यरूप से रंचमात्र भी डिगें नहीं।
यदि पर पदार्थ में बुद्धि लगे तो कर्मबंध हो निश्चय ही।।
शारीरिक सभी पदार्थों को तजना ही मुनि की क्रिया कही।
जब तक है आयू कर्म शेष तब तक मुनिव्रत ही धरो सही।।
(४०) जो यति पूजा की इच्छा से नहिं मूलगुणों को पाल रहे।
उनको आचार्य मूल छेदक प्रायश्चित दण्ड बताते हैं।।
जैसे अंगुलि का अग्रभाग शिरछेदक बाण न रोक सके।
वैसे ही मुनि के उत्तरगुण नहिं मूलगुणों के दोष ढके।।
(४१) यदि वस्त्र संयमी रखता है तो धोने की चिंता रहती।
जब फट जाए तब वस्त्र मांगने की है आकुलता रहती।।
यदि एक लंगोटी भी रख ले तो खो जाने से दुख होगा।
इसलिए मुनीव्रत ही धारो तब दिशारूप अंबर होगा।।
(४२) नहिं धन सम्पत्ती ये रखते जिससे बालों को कटा सकें।
कैंची आदिक नहिं अस्त्र रखें नहिं केशों की वे जटा रखें।।
जूँ आदिक जीवों की हिंसा से विरत अयाचक वृत्ति रखें।
वैराग्यवृद्धि के लिए मुनी हाथों से केश का लोंच करें।।
(४३) मुनिगण ममत्व से रहित सदा इसलिए प्रतिज्ञा करते हैं।
जब तक पैरों में शक्ति रहे तब तक ही भोजन लेते हैं।।
क्योंकी हाथों की अंजलि में आहार खड़े होकर लेते।
वरना समाधि को धारण कर वे धर्ममार्ग को हैं चुनते।।
(४४) केवल शरीर में यह मेरा ऐसी ममत्व बुद्धी से है।
संसार में परिभ्रमण होता फिर बाह्य वस्तु में क्या रमते।।
फिर कोइ कुल्हाड़ी से मारे अथवा चंदन का लेप करे।
दोनों में साम्यभाव रखते अपने से खुद को भिन्न रखें।।
(४५) तृण, रत्न, शत्रु हों मित्र बन्धु सबमें वे समता रखते हैं।
सुख-दुख स्तुति अरु निंदा में निंह किंचित् क्लेश वे धरते हैं।।
शमशान भूमि और राज्यों में जीवित अरु मरणावस्था में।
समभाव रखें जो इन सबमें वे भावमुनी ही होते हैं।।
वीतरागी इस प्रकार विचार करते हैं
(४६) जिस तरह हिरण अपने समूह से जुदा हुआ विचरण करता।
हर पल सचेष्ट रहकर पर से एकला ही आनन्दित होता।।
अपने कुटुम्बियों से हम भी कब होकर जुदा मोह त्यागें।
एकान्तवास में रह करके आत्मा का सुख हम भी भोगें।।
(४७) ना जाने कितनी बार बने सम्राट चक्रवर्ती राजा।
ना जाने कितनी बार बने, चींटी हाथी पशु योनी पा।।
संसार में सब कुछ चंचल है सुख दुख में हर्ष विषाद न कर।
जिससे भवभ्रमण छूट जावे संसार से तर जाता है नर।।
(४८) उपरोक्त भावना करने से होता है परमशुद्ध संवर।
जो भी प्राचीन कर्म आत्मा के गल जाते होता निर्जर।।
तब परमशांत मुद्राधारी मुनि के न नवीन कर्म बंधते।
इससे वे मुक्तिवल्लभा के अति निकट पहुँच कर दुख हरते।।
((४९) जिन मुनि के पास छिद्रविरहित है सम्यग्ज्ञानमयी नौका।
तपरूपी पवन पास जिनके आशीर्वाद हो गुरुओं का।
उन उद्यमि मुनि के लिए नहीं है दूर मोक्ष का मार्ग सुनो।
कर लेगा झट से पार उसे कितना ही बड़ा समन्दर हो।।
(५०) हे मुनिगण ! इस आनंदमयी शुद्धात्मा का अनुभवन करो।
मत लोक रिझाने में पड़ना कृष मोह करो, तन का न करो।।
जब तक तुम इन दो बातों का नहिं दोगे ध्यान व्यर्थ सारा।
जप तप उपवास नियम आदिक से नहीं किसी ने भव तारा।।
(५१) जो मुनिवर दुष्ट कषायों को नहिं छोड़े मन को शुद्ध करे।
वे क्या संसार त्याग सकते सब परिषह सहना व्यर्थ रहे।।
आचार्य प्ररूपण करते हैं उनके सब कार्य कपट वाले।
ऐसे ढोंगी मुनि होते हैं संसार भ्रमण करने वाले।।
(५२) धन को जिसने संचयन किया वह सभी पाप में रत रहता।
क्योंकी धन से आरंभ और उससे ही लोभ प्राप्त होता।।
प्राणी हिंसा से पाप कहा वह पाप आरम्भ का कारण है।
इसलिए द्रव्य जो ग्रहण करे सन्मार्ग नाश का कारण है।।
(५३) निग्र्रंथ मुनि शय्या के कारण घास आदि यदि स्वीकारें।
दुध्र्यान कहा आचार्यों ने लज्जाकर भी इसको मानें।।
फिर यदि निर्गं्रथ यती सोना आदिक वस्तू लेकर रखे।
तो इस कलियुग का दोष कहा वरना वे अविंâचन सदा रहें।।
(५४) क्रोधादि कषायों के द्वारा, प्राणी के कर्मबंध होते।
पर प्रतिक्षण बंध नहीं होता ये कभी कभी ही हैं होते।।
लेकिन परिग्रहधारी जीवों की किसी काल में सिद्धि न हो।
इसलिए भव्य जीवों सुन लो धन धान्य से प्रीति नहीं रखो।।
(५५) अभिलाषा अगर मोक्ष की भी की जाए दोषस्वरूप कहा।
फिर स्त्री पुत्र जनों की क्या जब तक शरीर से मोह रहा।।
इसलिए कहा है मुनियों को अपनी आत्मा में लीन रहो।
तब मोक्ष स्वयं पा जावोगे नहिं पर पदार्थ में प्रीति रखो।।
(५६) यदि परिग्रहधारी जीवों का भी मोक्षगमन माना जाए।
तो अग्नी को शीतल मानो इंद्रियसुख सुख माना जाए।।
विष भी अमृत कहलायेगा और तन को भी स्थिर मानो।
यदि इंद्रजाल रमणीय कहो नभ की बिजली स्थिर मानो।।
(५७) ऐसे यतिवर जयवंत रहें जो कामदेव के योद्धा को।
निज ध्यानाग्नि से भस्म करें भय से ही भाग रहा है जो।।
फिर लौट के ना वापस आए सारा प्रभाव ही खत्म हुआ।
ऐसे ध्यानी को नमन करूँ जिन मुनि आगे वह हार गया।।
(५८) जो रत्नत्रय रूपी संपति के धारी हैं मगर दिगम्बर हैं।
हैं परमशांत मुद्राधारी फिर भी वे युद्ध में तत्पर हैं।।
क्योंकी वे कामदेव रूपी बैरी को मार गिराते हैं।
उसकी स्त्री को विधवा कर त्रैलोक्यपूज्य बन जाते हैं।।
आचार्य परमेष्ठी की स्तुति
(५९) जो स्वयं पंच आचार पालते सौख्य वृक्ष का बीज कहा।
ऐसे आचार्य शिष्य को भी पालन करवाते सौख्यप्रदा।।
नहिं लेशमात्र भी परिग्रह है जो ऐसी मुक्ति स्वयं पाते।
रत्नत्रयधारी ऐसे गुरु पर को भी मुक्ती दिलवाते।।
(६०) इस जग में भ्रम के कारक जो ऐसे अनेक ही मार्ग कहे।
उनसे छुड़वाकर जो गुरुवर सच्चा सुखकारी मार्ग कहें।।
सत्पथ बतलाते ऐसे गुरु को शीश झुकाकर नमन करूँ।
मिथ्यामारग में नहिं जाऊँ ऐसा मैं सत् आचरण करूँ।।
उपाध्याय परमेष्ठी की स्तुति
(६१) यह मोहकर्म का परदा जो है लगा अनादी कालों से।
शिष्यों को संबोधन देते वे उपाध्याय निज वचनों से।।
स्याद्वाद से अविरोधी उनके उपदेश दृष्टि निर्मल करते।
ऐसे उवझाय१ मेरी रक्षा करिए बिन हेतु व्याधि हरते।।
साधु परमेष्ठी की स्तुति
(६२) जो साधु पांचवे परमेष्ठी गृहबंधन को ठुकराय दिया।
अपने शरीर से मोह छोड़ मोहान्धकार को नष्ट किया।।
निज सम्यग्ज्ञानमयी ज्योती की सूर्य प्रभा सम वृद्धि करें।
ऐसे वे साधू परमेष्ठी हम सबमें भी समृद्धि भरें।।
वीतरागता की महिमा
(६३) जैसे बिजली के गिरने से सब लोग भयातुर हो जाते।
लेकिन शांतात्मा मुनि देखो नहिं ध्यान से हैं डिगने पाते।।
जिसने सज्ज्ञानरूप दीपक से मोह महातम नाश किया।
वे सम्यग्दर्शन के धारी परिषह सह सब कुछ जीत लिया।।
ग्रीष्म ऋतु में पर्वत शिखर पर ध्यानी मुनीश्वरों की स्तुति
(६४) जिस ग्रीष्म ऋतू की तीक्ष्ण धूप और लू के प्रबल थपेड़ों में।
अत्यन्त ताप देने वाली भूमि रेता को जो ओढ़ें।।
जिस समय सूख जातीं नदियाँ ऐसे ऋतु में पर्वत तट पर।।
जो ध्यान अग्नि से भस्म करें ऐसे मुनि होवें क्षेमंकर।।
वर्षा ऋतु में वृक्षों के नीचे ध्यानी मुनियों का तप
(६५)वर्षा ऋतु में तरु के नीचे जो ध्यान मुनीश्वर करते हैं।
वे मुनिगण रक्षा करें मेरी हम नमन चरण में करते हैं।।
जब महाभयंकर शब्द करें पृथ्वी भी नीचे धंस जाती।
बरसे ओले शोले पत्थर फिर भी कुछ विकृति नहिं आती।।
शीतकाल में मुनियों का तप
(६६) जिस शीतकाल में सर्दी से हैं कमलपत्र कुम्हला जाते।
अत्यन्त कष्ट देने वाली दीनों के रोम है हिल जाते।।
बंदर का मद भी गल जाता वृक्षों के पत्ते जल जाते।
ऐसे क्षण महा तपस्वी के तप से सब कर्म विनश जाते।।
और भी मुनिधर्म का स्वरूप
(६७) जो आत्मज्ञान से रहित मुनी इन तीनों ऋतु के दुख सहें।
आचार्य प्ररूपण करते हैं उनका सारा तप व्यर्थ रहे।।
जैसे कि धान कट जाने पर खेतों में बाड़ लगाये क्यों।
वैसे ही निज में ध्यान करे यह कहा गया है मुनियों को।।
(६८) यद्यपि कलियुग में तीन लोक से पूज्य केवली प्रभू नहीं।
फिर भी जग में प्रकाश करने वाली वाणी मौजूद सही।।
उस वाणी को गुरु बतलाते इसलिए सरस्वतिसुत मानो।
उनकी पूजन वंदन कर लो ये जिनवर की पूजन जानो।।
(६९) यह यतिवर ध्यानलीन होकर जहाँ चरण कमल रख देते हैं।
वह भूमी तीरथ बन जाती उसे इंद्र देवगण नमते हैं।।
उनके स्मरण मात्र से ही सब पाप शमन हो जाते हैं।
ऐसे यतियों को सदा ध्यान में रखकर शीश झुकाते हैं।।
(७०) रत्नत्रयधारी ये मुनिवर दुष्टों से अपमानित होकर।
समता को धारण करते हैं आत्मा की शुद्धी में रमकर।।
जो निंदा करने वाले हैं वे निज आत्मा का घात करें।
अरु कर्मों का बंधन करके जाकर नरको में वास करें।।
(७१) इस मानुष भव को पा करके भोगों को रोगतुल्य समझें।
ऐसे परिग्रह से रहित मुनी वन में जाकर तपरत रहते।।
उनके गुण को गाने वाला निंह वन में कोई होता है।
यदि कोई स्तुति कर सकता वो महापुरुष ही होता है।।
।।इति मुनिधर्म कथन।।
दशलक्षण धर्म का कथन
उत्तम क्षमा धर्म का स्वरूप
(८२) जो मूर्खजनों से किए हुए बंधन अरु हास्य क्रोध में भी।
निंह मन में जरा विकार करे समताधारी वह साधू ही।।
यह उत्तम क्षमा धार सकते जो मोक्षमार्ग में ले जाती।
बाकी हम सब गृहस्थजन से निंह एकदेश पाली जाती।।८२।।
(८३) यतिरूपी वृक्ष की शाखा है गुणरूपी पुष्प फलों शोभित।
उसमें यदि क्रोध मान आदिक अग्नी से मुनि हो जाए सहित।।
जैसे िंचगारी क्षण भर में उत्तम फलयुत तरु जला सके।
वैसे ही मुक्ति न मिल सकती इसलिए क्रोध ना कभी करें।।८३।।
(८४) रागद्वेषादि रहित होकर स्वेच्छा से निज में मगन रहे।
यह लोक भला या बुरा कहे उसकी न कोई परवाह करे।।
क्योंकि जो हमारे साथ द्वेष या प्रीतिपूर्ण व्यवहार करे।
उसका फल उसको ही मिलता यह पद्मनंदि आचार्य कहें।।८४।।
(८५) मेरे दोषों को सबसे कह करके यदि मूर्ख सुखी होता।
अथवा धन संपति लेकर के मेरा जीवन भी ले लेता।।
खुश रहे सभी कुछ लेकर भी अथवा मध्यस्थ रहे कोई।
मुझसे न किसी को दुख पहुँचे ऐसी बुद्धि होवे मेरी।।८५।।
(८६) मिथ्यादृष्टी दुर्जन जन से दी गयी वेदना से हे मन।
तुम दुख का अनुभव नहीं करो होता है कर्मों का बंधन।।
जिनधर्म का आश्रय तुझे मिला ये धर्म तुझे बतलाना है।
यह सारा लोक अज्ञानी जड़ तू इससे क्यों घबराता है।।८६।।
मार्दव धर्म का स्वरूप
(८७) जो श्रेष्ठ पुरुष कुल ज्ञान जाति बल आदि गर्व को त्याग करे।
वह सब धर्मों का अंगभूत मार्दव इस धर्म को पाल रहे।।
जो सम्यग्ज्ञानमयी दृष्टी से जग को इंद्रजाल समझे।
वे निश्चय ही मार्दव गुण को अपने अंदर धारण करते।।८७।।
(८८) अति सुंदर घर भी यदि अग्नी से चारों तरफ घिर गया हो।
तब उसके बचने की आशा वैâसे कर सके ज्ञानिजन जो।।
बस इसी तरह इस काया को वृद्धावस्था ने घेर लिया।
नहिं सदाकाल रहता कोई यह गर्व छोड़कर मान हिया।।८८।।
आर्जव धर्म का वर्णन
(८९) जो मन में वही वचन बोले इसको ही आर्जव धर्म कहा।
पर मीठी चिकनी बातों से ठगना ये बड़ा अधर्म कहा।।
ये आर्जव धर्म स्वर्गदाता अरु कपट नरक ले जाता है।
इसलिए सदा जो इसे तजे वह सरल भाव अपनाता है।।८९।।
(९०) मायाचारी से मुनियों के सद्गुण फीके पड़ जाते हैं।
और माया से उत्पन्न पाप दुर्गति में भ्रमण कराते हैं।।
क्रोधादि शत्रु जो छिप करके माया के ग्रह में बैठे हैं।
उनको निकाल करके मुनिवर निंह पास फटकने देते हैं।।९०।।
सत्य धर्म का वर्णन
(९१) उत्कृष्ट ज्ञान के धारी मुनि को सदा मौन रखना चहिए।
यदि बोले भी तो हित मित प्रिय और सत्य वचन होना चहिए।।
जो कड़वे वचन दूसरों को पीड़ा पहुँचाने वाले हों।
आचार्य प्ररूपण करते हैं निंह सच्चे साधु बोलते वो।।९१।।
(९२) जो सत्य धर्म का पालक है सब व्रत उसमें गर्भित होते।
तीनो लोकों में पूज्यनीय माँ सरस्वती सिद्धी करते।।
इस व्रत का है महात्म्य इतना वसु का िंसहासन पृथ्वी में।
था समा गया मरकर राजा, अरु स्वर्ग गया नारद सच में।।९२।।
(९३) आचार्य और भी कहते हैं सतवादी परभव में जाकर।
इंद्रादि, चक्रवर्ती राजा का वैभव पाते हैं आकर।।
इस जीवन में ही कीर्ति बढ़े आदर सम्मान बहुत होता।।
उत्तम फल मिले कई उनको अरु मोक्ष प्राप्त भी कर लेता।।९३।।
शौच धर्म का वर्णन
(९४) परधन परस्त्री में जो जन निस्पृह वृत्ती से रहता है।
अरु किसी जीव का बध करने की नहीं भावना करता है।।
अत्यंत कठिन क्रोधादि लोभ मल का जो हरने वाला है।
वह प्राणी ही तब शौच धर्म को धारण करने वाला है।।९४।।
(९५) अति घृणित मद्य से भरा हुआ घट धोने से नहिं स्वच्छ हुआ।
नहिं तीर्थस्थानों के स्नान से कोई कभी पवित्र हुआ।।
जब अंतकरण मलीमस है तो बाह्य शुद्धि से क्या होगा।
इसलिए पवित्र करो मन को तब ही निज का दर्शन होगा।।९५।।
संयम धर्म का वर्णन
(९६)जो हृदय दया से ओत प्रोत पाँचों समिति पालन करते।
ऐसे साधू षट्काय जीव की भी हरदम रक्षा करते।।
पंचेन्द्रिय के जो विषय भोग उनसे भी सर्वथा विरत रहे।
ऐसे मुनिश्रेष्ठ धर्म संयम को पाले गणधर देव कहें।।९६।।
(९७) यह मनुष धर्म अति दुर्लभ है उसमें भी अच्छी जाति मिले।
यदि दैवयोग से मिल जावे उसमें अर्हंत वचन न मिले।।
सद्वचन श्रवण को मिल जावे तो जीवन अधिक नहीं मिलता।
सब कुछ मिलने के बाद रत्नत्रय धारण कर संयम धरता।।९७।।
तप धर्म का वर्णन
(९८) ज्ञानावरणादिक आठ कर्म क्षय करने को जो ज्ञान कहा।
उस सम्यग्ज्ञानमयी दृष्टी से तप करते दो रूप कहा।।
बाह्याभ्यंतर से दोनों के हैं बारह भेद कहे जाते।
संसार जलधि से तिरने में ये नौका सम माने जाते।।९८।।
(९९) यद्यपि कषाय रूपी चोरों को जीता जाना मुश्किल है।
लेकिन तपरूपी योद्धा के सम्मुख टिकना नहिं मुमकिन है।।
इसलिए योगिजन मोक्षनगर में बाधा रहित चले जाते।
आचार्य प्ररूपण करते हैं योगी से न कोई जीत पाते।।९९।।
(१००) मिथ्यात्व उदय से घोर दुख सहने पड़ते हैं नरकों में।
फिर हे प्राणी ! क्यों घबराता है तप के थोड़े कष्टों से।।
जैसे अथाह सागर आगे जल का कण छोटा होता है।
वैसे ही तप में दुख बहुत अल्प करके तो देखो होता है।।१००।।
त्याग धर्म का वर्णन
(१०१) जो मुनियों के श्रुतपाठन के हेतू पुस्तक का दान करे।
अरु संयम के साधन हेतू पिच्छी व कमण्डलु दान करे।।
उनके रहने के लिए श्रेष्ठ स्थान आदि भी दान करे।
तन से भी ममता तजकर ऐसे यति आकिंचन धर्म धरें।।१०१।।
आकिञ्चन्य धर्म का वर्णन
(१०२) अपने हित में जो लगे हुए गृहत्याग पुत्र स्त्री तजकर।
वे मोक्ष हेतु तप करते हैं सबसे सर्वथा मोह तजकर।।
ऐसे मुनि विरले होते हैं मिलते हैं बड़ी कठिनता से।
पर को शास्त्रादि दान करके तप में भी बनें सहायक वे।।१०२।।
(१०३) यदि कहो वीतरागी मुनि को सब त्याग दिया क्यों पुस्तक दें।
तन से क्यों मोह नहीं त्यागा आचार्यदेव तब कहते ये।।
जब तक है आयूकर्म शेष इस तन को नष्ट न कर सकते।
अपघातक दोष लगेगा तब, निंह तन से वे ममता रखते।।१०३।।
ब्रह्मचर्य धर्म का वर्णन
(१०४) जैसे कुम्हार का चाक तीक्ष्ण धारण से घट निर्माण करे।
वैसे ही भव के भ्रमने में स्त्री दुख का आधार रहे।।
इसलिए मुमुक्षूजन स्त्री में माता बहिन सुता देखें।
जो ब्रह्मचर्य के धारी हैं वह स्त्री सुख में नहीं रमे।।१०४।।
(१०५) जो रागी पुरुष स्त्रियों में प्रीति उपजाने वाले हैं।
उनको भी अच्छा कहा मगर जो नर विरक्त मन वाले हैं।।
ऐसे वैरागी साधक के चरणों में चक्रवर्ति नमते।
जो जगतपूज्य बनना चाहें वे नहीं स्त्रियों में रमते।।१०५।।
(१०६) वैराग्य त्याग रूपी अतिसुंदर काष्ठ लगे हों इधर उधर।
दशधर्म रूपी दण्डे लगकर वह सीढ़ी बनी बड़ी सुंदर।।
उस पर चढ़ने के योग्य मनुज दशधर्म पालने वाला हो।
तीनों लोकों में पूज्यनीय और वंदनीय बन जाता वो।।१०६।।
।।इति दशधर्म निरूपण।।
शुद्धात्मा की परिणति रूप धर्म का कथन
(१०७) जो निर्मल शील व गुणस्वरूप समता से युक्त अवस्था है।
अरु अनंत चतुष्टयमय अमृत सरिता के भीतर रहता है।।
उसको दुष्कर संसार दु:खरूपी अग्नी नहिं जला सके।
ऐसी शुद्धात्मा की परिणति रूपी आत्मा को नमन करें।।१०७।।
(१०८) कर्मादि वैरियों के नाशक तन का भी आश्रय नहीं रहा।
ऐसी शुद्धात्मा सूर्य चंद्र अग्नी से जिसका तेज बड़ा।।
उसके आगे सब पर पदार्थ क्षण भर में ऐसे अस्त हुए।
चैतन्य स्वरूपी तेज पुंज को नमस्कार कर धन्य हुए।।१०८।।
(१०९) नहिं जन्म मरण अरु जरा रोग कर्मों का भी संबंध नहीं।
है सदा प्रकाशित प्रभु आत्मा स्वात्मैक ज्ञान का धारी ही।।
जिनकी न किसी से उपमा हो सकती ऐसे उन सिद्धों की।
मैं शरण गहूँ रक्षा करिए जो अविनाशी पद धरते भी।।१०९।।
(११०) इस चिच्चैतन्य आत्मा का िंकचित वर्णन जो किया मैंने।
उसमें न कोई छल किया अत: अल्पज्ञानी मुझको समझे।।
क्योंकी सब कर्मों के राजा हैं मोहनीय अंतराय शत्रू।
दर्शन ज्ञानावरणी चारों ये मेरे संग में लगे प्रभू।।११०।।
(१११) विद्वान मानते अपने को शृंगारादिक के व्याख्याता।
प्रिय वचनों के आडम्बर से सन्मार्ग भुला दे जो वक्ता।।
इस दुनिया में हैं बहुत लोग ऐसे भाषण देने वाले।
पर सम्यग्ज्ञानप्रणेता जो वे दुर्लभ हैं देखे जाते।।१११।।
(११२) यह रागद्वेष माया आदिक सबके स्वभाव से होते हैं।
इसलिए काव्य यदि ऐसा हो जो मन के मल को धोते हैं।।
उस वीतरागता के वर्णन का काव्य सदा फल देता है।
शृंगार आदि रस काव्य सदा प्राणी को दुख ही देता है।।११२।।
(११३) मोहान्धकार से व्याप्त जगत में मोही अज्ञानी घूमें।
उनको न दिखाई कुछ पड़ता उस पर यदि दुर्जन कथा सुनें।।
आचार्य हमें समझाते हैं सत्पुरुषों की संगती करें।
आँखों में धूलि डालने वालों से सदैव ही दूर रहें।।११३।।
(११४) यह तन विष्टा मूत्रादिक नाना कीड़ों से युत भरा हुआ।
अरु प्रबल घृणाकारी अस्थी मज्जा रजवीर्य से पुष्ट हुआ।।
ऐसे ही मल से बना हुआ जो कवी कुमाता से जन्मा।
वह नारी को जब चंद्रमुखी कहते हैं तो आश्चर्य घना।।११४।।
(११५) स्त्री के केश जुओं के घर मुख हाड़ समूह चाम्र वेष्टित।
और मांसिंपड सम स्तन है, अरु उदर आदि विष्ठा पूरित।।
खम्भे की तरह पैर दोनों जिन स्थानों पर टिके हुए।
अत्यन्त घृणित इस काया में निंह विद्वतजन हैं राग करें।।११५।।
(११६) यह कामदेव रूपी धीवर उत्कृष्ट धर्म नदि से बाहर।
हैं जीवरूप मछली उसको पकड़े काटें में लटकाकर।।
भू पर भूंजे बस उसी तरह, नारी के जाल में फंस करके।
संभोगरूप भू पर भूंजें, ज्ञानीजन इससे दूर रहें।।११६।।
(११७) जितने दुनिया में दोष कहे वे सभी अहित ही करते हैं।
पर सबसे बड़ा अहितकारक नारी के रूप को कहते हैं।।
इनसे अति मोह उत्पन्न होकर नाना प्रकार दुख सहते हैं।
क्रोधादि कषाय बने दुर्जय भवदधि को निंह तर सकते हैं।।११७।।
(११८) जिस तरह कबूतर आदिक खग दाना देकर पकड़े जाते।
उस तरह विषय के जाल में भोले प्राणी हैं फांसे जाते।।
इसलिए इन्हें दुख का कारण लख विद्वतजन नहिं फंसते हैं।
कांक्षा न करें वे विषयों की अतएव सुखी वे रहते हैं।।११८।।
(११९) जैसे कोई बैरी जिस पर मंत्रादिक का उपयोग करे।
विपरीत बुद्धि हो जाती है नाना आपत्ति आदि भोगे।।
वैसे ही मोहरूप बैरी उसके प्रयोग से विषयों में।
होकर प्रवृत्त दुख सहें सभी सुख मानें चंचल भोगों में।।११९।।
(१२०) भवरूपी घने जंगलों में यह मोहरूप ठग बैठे हैं।
जो स्त्री क्रोध मान माया से सबको ठगते रहते हैं।।
इसलिए ज्ञानरूपी आत्मा का ही आश्रय लेना चहिए।
आचार्य प्ररूपण करते हैं बस निज में ही रमना चहिए।।१२०।।
(१२१) मैं ज्ञानी अरु मैं धनी बहुत इस तरह मूर्ख समझा करते।
और चंचल बिजली के समान पुत्रादिक को अपना कहते।।
जबकी कुछ भी निंह स्थिर है यह सभी लोग हैं देख रहे।
इसलिए मोह को वश में कर आचार्य हमें सम्बोध रहे।।१२१।।
(१२२) क्या करें कहाँ जाएं वैâसे लक्ष्मी को प्राप्त करें वैâसे।
इस उलझन में हरदम प्राणी किस नृप की सेवा टहल करे।।
सब जान बूझकर भी ये मन ना किसी तरह भी समझ सके।
इसलिए ग्रंथकर्ता कहते यह मोह बहुत ही भ्रमित करे।।१२२।।
(१२३) हे बुद्धिमान ! तुम मोह तजो धन सदन पुत्र मित्रादिक से।
जिससे निंह जन्म दुबारा हो मिट जाये भ्रमण चौरासी से।।
क्योंकि उत्तम कुल जैनधर्म की शरण बहुत ही दुर्लभ है।
फिर मिले ना मिले पता नहीं जो मिला आज मानुष तन है।।१२३।।
(१२४) यह वीतराग अर्हंत देव की वाणी ही सद्वाणी है।
जो रागद्वेष से रहित और सब ज्ञाता दृष्टा ज्ञानी है।।
इसलिए भव्यजन मुक्ती की प्राप्ति के हेतु इसे मानो।
क्यों इधर उधर तुम फिरते हो अज्ञानी वचन असत् मानो।।१२४।।
(१२५) जो मूर्ख लोग जिन वचनों में संदेह हमेशा करते हैं।
अपनी जड़बुद्धि से हरदम वे बस असत् कल्पना करते हैं।।
जैसे जन्मांध पुरुष पक्षी की गणना में यदि बहस करे।
तब नेत्र सहित मानव वैâसे उसकी बातों से सहज रहे।।१२५।।
(१२६) श्रुत के दो भेद कहे प्रभु ने जो अंग बाह्यश्रुत रूपी हैं।
उसमें बारह भेदों से युत अंगश्रुत पढ़ते वे ज्ञानी हैं।।
और बाह्यश्रुत के हैं अनंत भेद उसमें जो ज्ञानमयी आत्मा।
उसको ही ग्रहण योग्य कहते तद्भिन्न त्याज्य है परमात्मा।।१२६।।
(१२७) इस पंचमकाल में ज्ञान आयु आदिक सब क्षीण हुए जानो।
इसलिए नहीं सब पढ़ सकते जो रत अभ्यासमयी मानो ।।
अभ्यास सदा जो किया करे वह मोक्षमार्ग का अभिलाषी।
यह श्रुताभ्यास ही मुक्तीपथ देता जो होता हितकारी।।१२७।।
(१२८) जो सूक्ष्म अगोचर है पदार्थ उनमें भी संशय नहीं करे।
जो दिव्यध्वनि जिनवचनों की उसको अवश्य स्वीकार करें।।
इस युग में जितने प्राणी हैं उनको निंह ज्यादा ज्ञान मिला।
इसलिए हमें परमागम से जो मिला समझिए बहुत मिला।।१२८।।
(१२९) चैतन्य बिना सब ज्ञानवान है शून्य कहा है भव वन में।
आत्मा के होने से पदार्थ में ज्ञान भान होता सच में।।
इसलिए भव्यजीवों को ऐसी सारभूत इस आत्मा में।
रमना चहिए बस इसमें ही और ध्यान करें शुद्धात्मा में।।१२९।।
(१३०) अज्ञानी प्राणी कोटि वर्ष में जितना तप कर कर्म नशे।
इक क्षण में नष्ट करे ज्ञानी स्थिर होकर जब ध्यान करे।।
यह आत्मा है चैतन्यरूप जितना बन सके करो तप को।
जिससे भव में नहिं आना हो, आत्मा सिद्धालय स्थित हो।।१३०।।
(१३१) यदि कर्म उदयरूपी समुद्र में कोई व्यक्ति जब गिर जावे।
जब तक नहिं मिले ज्ञानरूपी नौका निंह पार उतर पावे।।
नाना प्रकार आपत्ति रूप बैठे हैं मगरमच्छ इसमें।
तब ज्ञानरूप नौका बनती जीवों को सहायक तिरने में।।१३१।।
(१३२) मोहरूपी सघन अंधेरे में है व्याप्त त्रिलोकमयी मकान।
उसमें प्रवेश करने वाला जिनवच रूपी दीपक महान।।
तब ही पदार्थ का ज्ञान प्राप्त होगा क्या छोड़े ग्रहण करें।
वरना अज्ञान अंधेरे में यह प्राणी कुछ ना ढूंढ सके।।१३२।।
(१३३) जब कर्मों का उपशम होने से क्षेत्र काल शुभ योग बने।
तब आत्मा में हो लीन मनुज अपने निज का िंचतवन करे।।
संसार दुखों से छुड़वाए उसको ही धर्म कहा मुनि ने।
इसके अतिरिक्त न कोई धर्म इससे तल्लीन रहे निज में।।१३३।।
आत्मा के वास्तविक स्वरूप का वर्णन
(१३४) निंह शून्य न जड़ निंह पंचभूत से आत्मा की उत्पत्ती है।
निंह कर्ता, एक न क्षणिक लोकव्यापी नहिं नित्य से बनती है।।
अपने शरीर परिमाण तथा रत्नत्रण गुण से शोभित है।
अपने ही कर्मों का कर्त्ता भोक्ता उत्पाद ध्रौव्य व्यय है।।१३४।।
(१३५) जो आत्मा को नहिं पहचाने वह वैâसी और कहाँ रहती।
यह प्रश्न पूछने वाली ही आत्मा में है जाग्रत बुद्धी।।
क्योंकी जड़ वस्तू में कोई भी प्रश्न विकल्प नहीं होते।
आत्मा का असली रूप समझ निज से कर्मों को क्षय करते।।१३५।।
(१३६) यद्यपि आत्मा नहिं मूर्तिक है यह तन के अंदर रहता है।
प्रत्यक्ष नहीं दिखता फिर भी यह कर्ता और ये ज्ञाता है।।
इत्यादि विकल्पों से आत्मा का है अस्तित्व जगत भर में।
इसलिए इसे अनुभवन करो और मोह हटावो तुम मन से।।१३६।।
(१३७) यह व्यापक नहीं इसी हेतू तन के प्रमाण में रहता है।
इसका स्वभाव है ज्ञानरूप नहिं पंचतत्व से बनता है।।
सर्वथा नित्य अरु क्षणिक नहीं क्योंकि ना जन्म न मरण इसे।
यह एकरूप भी नहीं कही क्रोधादिक कई भाव इसमें।।१३७।।
(१३८) यह आत्मा शुभ और अशुभ कर्म से सुख दुख भोगा करता है।
ना कोई दूसरा है सुख दुख जो दे आगम यह कहता है।।
चिद्रूप आत्मा संसारी जीवन में कर्म सहित होता।
पर मोक्ष अवस्था में कर्मों से रहित त्रिलोकपती होता।।१३८।।
(१३९) आचार्य हमें समझाते हैं हे भव्य ! अगर तिरना चाहो।
तो एकचित्त होकर प्रमाण नय आदिक से इसको जानो।।
यह मोहरूप जो मगरमच्छ से सहित भवोदधि विकट बड़ा।
आत्मा के सिवा कोई वस्तु नहिं ग्राह्य यही मुनियों ने कहा।।१३९।।
(१४०) हे आत्मा ! जब तक मेरे संग कर्मों का बंधन लगा हुआ।
तब तक संसार रूप वैरी दुख देंगे यह ही कहा गया।।
यह रागद्वेष ही वैरी है यदि इनको तू तज सकता है।
तो मेरी आत्मा कर्मों के दुख से जल्दी छुट सकता है।।१४०।।
(१४१) इस लोक का ना तू लोक तेरा फिर क्यों प्रीति को धरता है।
यह सुख दुख अरु संतोष क्रोध तू व्यर्थ ही सबसे करता है।।
यह काया नश्वर इसीलिए अपने स्वरूप में रमण करो।
विषयों की आशा में रमकर मत दीन हीन सम भ्रमण करो।।१४१।।
(१४२) जहाँ प्रतिक्षण दुख ही दुख रहता ऐसी तिर्यंच नरकगति में।
निंह जाना पड़े मगर सुरगति में लक्ष्मी रहती चरणों में।।
उस देवगति से भी जब आयू पूर्ण होए तब दुख होता।
इसलिए हमेशा अविनाशी पद प्राप्ती में ही सुख मिलता।।१४२।।
(१४३) हे मन् ! तूने दुख बहुत सहे स्त्री आदिक से न ममता कर।
इन बाह्य पदार्थों में चेतन तू िंकचित भी अनुराग न कर।।
श्री परमगुरू से दुखों के नाशक ऐसा उपदेश सुनो।
जिससे मुक्ति की प्राप्ति हो और अंतरंग में प्रवेश करो।।१४३।।
(१४४) आचार्य और भी कहते हैं यदि आत्म रमण की इच्छा है।
तो हे भव्यों ! इंद्रिय सुख को कर त्याग धार लो दीक्षा है।।
कोलाहल में क्या रखा है सारे परिग्रह का त्याग करो।
और चंचल मन को स्थिर कर एकांतवास का स्वाद चखो।।१४४।।
(१३४)जीव और मन का परस्पर संवाद
(१४५) रे मन तू वैâसे रहता है वह बोला िंचतित रहता हूँ।
ये िंचता रागद्वेष वश से बस इसमें ही रत रहता हूँ।।
जो इष्ट अनिष्ट समागम से होता है वैâसे इन्हें तजूं।
तब जीव कहे रे मन सब तज नरकों के दुख मैं क्यों भोगूं।।१४५।।
(१४६) जिसके स्मरण मात्र से ही मोहांधकार भग जाता है।
अरु सम्यग्ज्ञान उदित होता आनंद हृदय में छाता है।।
कृतकृत्यपने की प्राप्ती से आत्मा की शक्ती पहचानो।
निज में ही आत्मा रहती है तुम व्यर्थ न भटको यह जानो।।१४६।।
(१४७) इस जग में जीव अजीव रूप नाना प्रकार के बंधन में।
हो वशीभूत इस मोहकर्म के राग द्वेष रखता मन में।।
इससे ही हम चिरकालों तक दुख भोग रहे हैं इस जग में।
सब जान बूझकर पर पदार्थ में बुद्धी रहती है सच में।।१४७।।
(१४८) मलमूत्रादिक के घर स्वरूप इस तन से सदा भिन्न हूँ मैं।
मन के विकल्प अरु शब्द आदि रस से भी सदा पृथक््â हूँ मैं।।
मैं शांत और आनंदरूप चैतन्यात्मा में स्थित हूँ।
आरंभ परिग्रह छोड़ के मैं संसार से भी भयभीत न हूँ।।१४८।।
इस विचार से संसार से भय का निवारण
(१४९)निंह तुम्हें प्रयोजन लोक और उसके आश्रय से जो पदार्थ।
निंह तुझे प्रयोजन द्रव्य और इंद्रिय संबंधी अशुभ भाव।।
सब पुद्गल की पर्याय कही तू तो चैतन्य स्वरूपी है।
फिर क्यों दृढ़ बंधन बांध रहा तू दर्शन ज्ञान स्वरूपी है।।१४९।।
(१५०) जिसके मन में ऐसे विचार उत्पन्न हो गये ज्ञानी है।
जो भोगों के सुख अशुभ मान आत्मा के सुख सुख माने हैं।।
लेकिन इसकी विपरीत अवस्था अज्ञानी की होती है।
जो भोगे गये भोग उनकी ही हरदम स्मृति रहती है।।१५०।।
(१५१) जिस तरह खाज के रोगी को अग्नि से सेक कर सुख मिलता।
लेकिन वह दुख ही देता है निंह रोग नष्ट उससे होता।।
बस उसी तरह से क्षुधा तृषा से पीड़ित प्राणी होता है।
खाने पीने में सुख माने पर क्षणभंगुर सुख होता है।।१५१।।
(१५२) जब यह आत्मा अपने स्वरूप को देख वही चेष्टा करता।
उसमें ही होकर लीन उसी में खुद को आनंदित करता।।
अपने ही हित में सुख माने अपना ही संबंधी होता।
ऐसी प्रवृत्ति ही आत्मा की इसके अतिरिक्त न कुछ होता।।१५२।।
(१५३) जिस तरह भ्रमर सब पुष्पों में इक कमलपुष्प को चुनता है।
वैसे ही योगीजन विकल्प तजकर निज में ही रमता है।।
क्योंकि मनरूपी भ्रमर एक क्षण में ना जाने कहाँ कहाँ।
उड़कर चल देता है उसको ज्ञानीजन वश में करें अहा।।१५३।।
(१५४) जो शुद्धात्मा में रम जाते उनको सारे रस विरस लगें।
स्त्री पुत्रादिक कथा दूर तन से भी प्रीति नहीं रहे।।
हो जाते वचन मौन उनके मन से रागादिक नष्ट हुए।
ऐसे भव्यों के लिए कहा शुद्धात्मा में ही मगन रहें।।१५४।।
(१५५) जो दर्शन ज्ञानमयी आत्मा निंह उससे भिन्न मेरा कुछ भी।
ऐसी हो गयी बुद्धि निर्मल पर से छूटी परिणति मन की।।
फिर ग्राम नगर वन एक सदृश सबमें सुख दुख का नहिं आना।
आत्मा में हो तल्लीन यही उत्कृष्ट कही है आराधना।।१५५।।
(१५६) आचार्य और भी कहते हैं यदि इंद्रिय का शुद्धात्मा से।
संबंध रहा तो व्यर्थ कहा तप करना बाह्य वस्तुओं से।।
हो गये जुदा या बंधे हुए शुद्धात्मा से या नहीं रहे।
तब भी तप करना व्यर्थ कहा जब तक अंतर में ममत्व रहे।।१५६।।
(१५७) यद्यपि नय शुद्ध है ग्रहण योग्य व्यवहार बिना कुछ ना होता।
इसलिए शुद्धनय की व्याख्या व्यवहार से ही करना होता।।
व्यवहार बिना निश्चयनय का निंह कोई प्रयोजन रह जाता।
इन दोनों को संग लेकर ही साधक मुक्ती का पथ पाता।।१५७।।
(१५८) व्यवहारनयापेक्षा आत्मा दर्शन अरु ज्ञान से भिन्न कहा।
अरु शुद्ध नयापेक्षा आत्मा निंह भिन्न सभी कुछ देख रहा।।
जो दर्शज्ञानमय आत्मा को गुण पर्यायों युत जान लिया।
उसने सब कुछ ही देख लिया अरु जान लिया अरु प्राप्त किया।।१५८।।
(१५९) ज्ञानीजन यह विचार करते रस गंधादिक पुद्गल विकार।
इससे मैं भिन्न न भीतर हूँ नहिं बाहर, हल्का वजनदार।।
निंह मोटा पतला और नहीं स्त्री नर और नपुंसक हूँ।
नहि शब्द वर्ण नहिं गणना हूँ मैं दर्शन ज्ञान स्वरूपी हूँ।।१५९।।
(१६०) मोहांधकार को तप द्वारा जब नाश करे केवलज्ञानी।
तब चिच्चैतन्य तेज को वे क्षण में जानें आनंदकारी।।।
वह तेज सूर्य और चंदा की आभा से अधिक प्रभाशाली।
ऐसा वह तेज त्रिलोकी में जयवंत रहे महिमाशाली।।१६०।।
(१६१) जिस तरह कर्म के वशीभूत नहिं साता और असाता है।
उनसे उत्पन्न विकल्प जाल नहिं होते वही विधाता हैं।।
वो मोक्षधाम में रहते हैं इंद्रादिक भी स्तुति करते।
उस पद को पाने हेतू हम भी उनकी शरण ग्रहण करते।।१६१।।
(१६२) जिनमें अज्ञानी सुख माने संताप मिटाती चंद्रकिरन।
कर्पूर मिला चंदन रस हो या स्त्री के हो कमल नयन।।
ज्ञानीजन ऐसे चंचल सुख को सदा सदा धिक्कार रहे।
बस गुरुओं के अमृतसम वचनों से ही शांती प्राप्त करें।।१६२।।
(१६३) जो योगीश्वर इस मोहरूप ठग से निज की रक्षा करते।
संसार रूप बड़वानल में जो इधर उधर घूमा करते।।
जैसे धनयुक्त पथिक कोई चोरों से निजधन रक्षा कर।
घर जाकर सुख अनुभवन करे वैसे ही करते योगी तब।।१६३।।
धर्म की महिमा तथा धर्म के उपदेश
(१६४) जो अब तक धर्म स्वरूप कहा वह धर्म बड़ा सुख देता है।
वह इंद्र तथा अहमिन्द्र और षट्खंड राज्य भी देता है।।
दुख का नाशक निर्वाणरूप प्रासाद की सीढ़ी है ये धरम।
इसका वर्णन केवली और गणधर ही कर सकते अपरम।।१६४।।
(१६५) हे भव्यजीव ! यदि जन्म जरा आदिक दुख से बचना चाहो।
संसार रूप जो महारोग उसको भी शमन करना चाहो।।
तो धर्म रसायन का आश्रय लेकर कषाय का त्याग करो।
मिथ्यात्व बड़ा दुखदायी है इसको न झांककर भी देखो।।१६५।।
(१६६) जैसे समुद्र में गिरा रत्न मिलना अत्यन्त कठिन होता।
दो काष्ठखंड जो अलग दिशा में बहकर गया नहीं मिलता।।
अंधे को निधि मिलना दुर्लभ वैसा ही दुर्लभ मनुष जनम।
यह दुर्लभ मनुष जनम पाकर भव्यों ! जिनधर्म करो धारण।।१६६।।
(१६७) अंधे के हाथ बटेर लगे वैसे ही मनुष जन्म मिलता।
पर इसको पाकर जो प्राणी खोटे गुरु देवों में रमता।।
उनके खोटे उपदेशों से जो विषय व्यसन में फंसा रहा।
उसका निगोद राशी से मानव तन पाना भी व्यर्थ रहा।।१६७।।
(१६८) हे भव्यजीव ! बहु पुण्य उदय से मनुज जन्म ये तुझे मिला।
इसको पाकर अतिशीघ्र कोई हितकारी कारज करो भला।।
क्योंकि तिर्यंचगती में कोई ज्ञान नहीं दिलवा सकता।
इसलिए न खोटी गती मिले कर ले जो धर्म तू कर सकता।।१६८।।
(१६९) आचार्य और भी कहते हैं जो उत्तमकुल है तुझे मिला।
नरतन पाकर बहुपुण्य उदय से जैनधर्म भी तुझे मिला।।
इतना सब कुछ पाकर भी यदि निंह धर्ममार्ग अपनाओगे।
तो आया हुआ रत्न हाथों में खोकर व्यर्थ गवांओगे।।१६९।।
(१७०) शुभ धर्म कार्य करने हेतू है उम्र बहुत ही पड़ी हुई।
शारीरिक शक्ती धन आदिक है भोग भोगने हेतु मिली।।
आगे भविष्य में वृद्धावस्था में आराधन कर लेंगे।
यह ही विचार करते मूरख इक दिन मृत्यू को वर लेंगे।।१७०।।
(१७१) जो ज्ञानी हैं वे श्वेत केश लखकर विरक्त हो जाते हैं।
अज्ञानीजन जब उम्र बढ़े तो तृष्णा और बढ़ाते हैं।।
उनको वैराग्यजनित गुरु के उपदेश तनिक नहिं भाते हैं।
इस तरह मूर्ख अज्ञानीजन अपना संसार बढ़ाते हैं।।१७१।।
(१७२) हे तृष्णे तू है प्रिया मेरी आजन्म साथ रहने वाली।
तू प्रौढ़ा है मेरी स्त्री फिर तू वैâसे सहने वाली।।
यह दुष्ट जरा ने केश मेरे पकड़े हैं फिर भी तू चुप है।
इससे मेरा संबंध छुड़ा क्योंकी ये तेरी सौतन है।।१७२।।
(१७३) इस जग में रंक धनी होता और धनी रंक हो जाता है।
क्षण भर का पता नहीं कुछ भी बलवान मृत्यु पा जाता है।।
इसलिए नहीं विद्वान पुरुष धन जीवन का मद करता है।
ज्यों कमलपत्र पर ओसिंबदु अस्थिर सब वस्तु समझता है।।१७३।।
(१७४) प्राणी के प्राण मित्र सुत सब पत्ते पर पड़े ओस सम हैं।
चंचल हैं तथा इंद्रियों के सुख भी होते विष सदृश हैं।।
अक्षय सुख एक धर्म ही है पर मोही समझ न पाते हैं।
वह मोहजनित दुख की दाता वस्तू में सुक्ख मनाते हैं।।१७४।।
(१७५) जब तक राजा जीवित रहता तब तक सेना में जोश रहे।
तब तक तलवार शत्रुओं से लड़ने में खूब स्वरोष रहे।।
जब तक बलवान भुजाएँ हों तब तक प्राणी में कोप रहे।
पर कालबली जब डस जाए तब नहीं किसी को होश रहे।।१७५।।
(१७६) जैसे मल्लाह के जाल में फंसकर भी मछली क्रीड़ा करती।
नहिं आगत दुख का भान उसे प्राणी की स्थिति भी वैसी।।
इस मृत्युरूप नाविक का जो भी बिछा हुआ है जाल प्रबल।
विषयों में फिर भी प्रीति करे नहिं नरकादिक गतियों का डर।।१७६।।
(१७७) यह मनुष क्षुधा को भोजन से और प्यास शीत जल पीकर के।
मंत्रों से भूत को शांत करे वैरीजन को दण्डादिक से।।
औषधि रोगादिक शांत करे पर मृत्यु का कोई उपाय नहीं।
उस पर यदि विजय प्राप्त करना, तो धर्म ही एक उपाय सही।।१७७।।
(१७८) जिस तरह हंस नामक पक्षी निर्मल जल में क्रीड़ा करते।
पंखों के बल पर इक सरवर से दूजे में रमते रहते।।
वैसे ही भव्य जीव रूपी ये हंस धर्म के पंखों से।
दुर्गति रूपी तालाबों को तज शोभित हों उत्तम पद में।।१७८।।
(१७९) यह मनुष धर्म के बल पर ही तीर्थंकर चक्रवर्ति बनते।
बलभद्र और इंद्रादिक बन उत्तम-उत्तम कीर्ती लभते।।
जो धर्मरहित वे निश्चय से नरकादिक दु:ख भोगते हैं।
यह सब कुछ जान समझकर भी क्यों धर्म न धारण करते हैं।।१७९।।
(१८०) जो सुन्दरता की खान कहा ऐसे स्वर्गों में भ्रमण करें।
जहाँ सुन्दर सुन्दर नंदनवन में देवांगना सह रमण करें।।
जिन इंद्रों की विमान पंक्ती में दिव्य पताकाएं शोभित।
ऐसे पद को पाने वाले होते हैं धर्मों से भूषित।।१८०।।
(१८१) षट्खंड और नवनिधियाँ भी मिलती हैं इसी धर्म से ही।
चौदह रत्नों के स्वामी बन मिले चौरासी लख हाथी भी।।
अठरह करोड़ घोड़े होते रथ बड़े मिले चौरासी लख।
छ्यानवे हजार स्त्रियों संग जीवन जीते हैं सुखपूर्वक।।१८१।।
(१८२) जो करे धर्म की रक्षा उन प्राणी की रक्षा धर्म करे।
इसके विनाश हो जाने पर धरती पर कुछ नहिं शेष रहे।।
योगीजन जिसका ध्यान करे मुक्ति पद को देने वाला।
यह धर्म सदा सच्चा साथी अनुपम सुख को देने वाला।।१८२।।
(१८३) नरकादि योनिरूपी जल में नाना दुख रूप तरंगे हैं।
उसमें शुभ अशुभ कर्मरूपी है मगर जिन्हें वह खाते हैं।।
जिसका निंह आदि अंत कोई ऐसे समुद्र में प्राणी को।
बस धर्मरूप नैया करती है पार अत: ध्यायें उनको।।१८३।।
(१८४) उत्तम कुल में हो जन्म तथा लावण्य, निरोग शरीर मिले।
आयू आदिक समस्त बातें इस धर्मकृपा से हमें मिलें।।
उत्तमलक्ष्मी और उत्तमसुख निर्मलगुण की प्राप्ती होती।
इसलिए धर्म का आराधन करते रहिए कह गए यती।।१८४।।
(१८५) भौंरा पुष्पित पुष्पों का आश्रय स्वयं प्राप्त कर लेता है।
वन में मृग को इच्छित जगहें नदि को समुद्रतल मिलता है।।
और हंस पक्षि को मानसरोवर स्वयं प्राप्त हो जाता है।
बस वैसे ही धर्मात्मा को यश संपति सब मिल जाता है।।१८५।।
(१८६) सौभाग्य कामिनी सुत सुख की यदि तुम अभिलाषा करते हो।
अथवा सुंदर घर लक्ष्मी को पाने की इच्छा रखते हो।।
सुन्दरता पाकर सब जग में प्रिय बनने की यदि इच्छा है।
तो सदा धर्म में स्थित हो तुम धारो गुरु की शिक्षा है।।१८६।।
(१८७) इसके प्रभाव से निर्जल जगहों में भी बने सरोवर हैं।
निर्जन जंगल में क्षण भर में बन जाते विशाल घर हैं।।
अब कहे कहाँ तक पुण्य उदय से सब वांछित मिल जाते हैं।
सुन्दरियों के संग बिन मांगे रत्नादिक भी मिल जाते हैं।।१८७।।
(१८८) इस पुण्य उदय से दूर गयी वस्तू भी प्राप्त हुआ करती।
जब अशुभ कर्म का उदय हुआ तो आकर के वापस जाती।।
मन में विचार तब आते हैं उसने मेरे संग बुरा किया।
पर वह निमित्त केवल बनता अपने कर्मों से दुखी हुआ।।१८८।।
(१८९) इस पुण्य उदय से अंधा अरु रोगी भी रूपवान होता।
निर्बल भी पुण्य उदय से ही शेरों सा पराक्रमी होता।।
बदसूरत कामदेव सा बन घर बैठे ही लक्ष्मी मिलती।
सब पुण्य उदय से दुर्लभ भी वस्तुएँ सुलभता से मिलतीं।।१८९।।
(१९०) यद्यपि हाथी बलवान तथा बाँधते महावत ही उनको।
बोझा लादें अंकुश मारें और वही चलाते हैं उनको।।
बस इसी तरह उत्तम पुरुषों पर नीच कुचेष्टा करते हैं।
इसे दुष्टकर्म की चाल समझ ज्ञानीजन इससे बचते हैं।।१९०।।
(१९१) इस धर्म की इतनी महिमा है जो सर्प हार बन जाते हैं।
पैनी तलवार पुष्पमाला विष भी अमृत बन जाते हैं।।
बैरी भी प्रीति दिखाता है सुरगण अधीन हो जाते हैं।
यह है कितना महिमाशाली आकाश रतन बरसाते हैं।।१९१।।
(१९२) जो ग्रीष्मकाल में सूरज की ज्वालाओं से तप्तायमान।
कोमल शरीर के धारी को जब मिला हुआ पथ मरुस्थान।।
उसको यदि दैवयोग से मिल जाए हिमगिरि की फव्वारें।
बस उसी तरह का सुख समझो जब मिले धर्म की बौछारें।।१९२।।
(१९३) जैसे समुद्र में प्रलयकाल में उठता हुआ बवंडर हो।
उसमें भ्रमते जो मगरमच्छ आदिक जलजीव भयंकर हों।।
ऐसे समुद्र में गिरे हुए प्राणी को धर्म सहायक है।
नभ में विमान की रचनाकर अवलंब बने सुखदायक है।।१९३।।
(१९४) धर्मात्मा जन को इंद्र आदि अपने शिर पर धारण करते।
सुरनर किन्नरियाँ उनके गुण को भक्ति से गाया करते।।
धर्मात्मा पुरुषों की कीर्ती खुशबू की तरह पैâलती है।
इसलिए धर्म धारण करिए इससे लक्ष्मी भी मिलती है।।१९४।।
(१९५) लक्ष्मी को वश करने वाला अरु इच्छित फल देने वाला।
यह धर्म कल्पतरु सम यह सब िंचताओं को हरने वाला।।
यह पर्वत से उत्पन्न हुई नदियों की निर्मल धारा है।
इससे सब कार्य सिद्ध होते सुख मिलता अपरम्पारा है।१९५।।
(१९६) जो धर्म मार्ग पर गमन करे उसके सुख का तो कहना क्या।
जो केवल उसको सुन लेवे स्वामी त्रैलोक्य संपदा का।।
जैसे शीतल जल पीने से अथवा स्नान से सुख मिलता।
पर थके हुए प्राणी को शीतल सरवर का तट सुख देता।।१९६।।
(१९७) जिनके पद पंकज की रज से भव्यों को ज्ञान प्राप्त होता।
ऐसे श्री ‘‘वीरनंदि गुरु’’ को मैं श्रद्धा से वंदन करता।।
है यही याचना हे प्रभुवर ! मुझको भी मुक्ति प्रदान करो।
मेरे सब पाप शमन करके निज चरणों का आश्रय दे दो।।१९७।।
(१९८) परमानंद को देने वाला यह धर्म परम अमृत सम है।
संसार मार्ग से थके हुए प्राणी के लिए सुखासन है।।
यह पुण्यहीन को दुर्लभ है ऐसा ऋषियों ने कहा सदा।
‘‘श्री पद्मनंदि मुनि’’ के मुख से इतना धर्मामृत सार कहा।।१९८।।
