मूलाचार सार
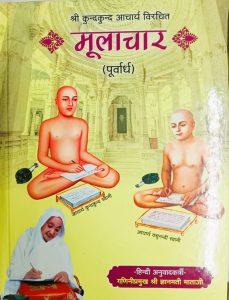
(१) छह आवश्यक अधिकार पंच नमस्कार-
काऊण णमोक्कारं अरहंताणं तहेव सिद्धाणं।
आइरियउवज्झाए लोगम्मि य सव्वसाहूणं।।५०२।।
अरिहंति णमोक्कारं अरिहा पूजा सुरुत्तमा लोए।
रजहंता अरिहंति य अरहंता तेण उच्चंदे।।५०५।।
दीहकालमयं जंतू उसिदो अट्ठकम्महिं।
सिद्धे धत्ते णिधत्ते य सिद्धत्तमुवगच्छइ।।५०७।।
सदा आयारबिद्दण्हू सदा आयरियं चरो।
आयारमायारवंतो आयरिओ तेण उच्चदे।।५०९।।
बारसंगे जिणक्खादं सज्झायं कथितं बुधे।
उवदेसइ सज्झायं तेणुवज्झाउ उच्चदि।।५११।।
णिव्वाणसाधए जोगे सदा जुंजंति साधवो।
समा सव्वेसु भूदेसु तह्मा ते सव्वसाधवो।।५१२।।
एवं गुणजुत्ताणं पंचगुरूणां विसुद्धकरणेहिं।
जो कुणदि णमोक्कारं सो पावदि णिव्वुदिं सिग्घं।।५१३।।
अर्हंतों को, सिद्धों को, आचार्यों को, उपाध्यायों को और लोक में सर्व साधुओं को नमस्कार करके मैं आवश्यक अधिकार कहूँगा। जो नमस्कार के योग्य हैं, लोक में उत्तम देवों द्वारा पूजा के योग्य हैं, आवरण कर्म और मोहनीय शत्रु का हनन करने वाले हैं इसलिए वे अरहंत कहे जाते हैं। यह जीव अनादिकाल से आठ कर्मों से सहित है, कर्मों के नष्ट हो जाने पर सिद्ध पद को प्राप्त हो जाता है। जो सदा आचार के ज्ञाता हैं, सदा पाँच आचार का आचरण करते हैं और शिष्यों को आचारों का आचरण कराते हैं, इसलिए वे आचार्य कहलाते हैं। जिनेन्द्रदेव द्वारा व्याख्यात द्वादशांग को बुद्धिमानों ने स्वाध्याय कहा है, जो उस स्वाध्याय का उपदेश देते हैं वे इसी कारण उपाध्याय कहलाते हैं। जो निर्वाण के साधक योगों में सदा अपने को लगाते हैं, सभी जीवों में समताभावी हैं वे इसीलिए साधु कहलाते हैं। इन गुणों से युक्त पाँचों परम गुरुओं को जो विशुद्ध मन-वचन-काय से नमस्कार करते हैं, वे शीघ्र ही निर्वाण को प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार पंच नमस्कार का निरुक्तिपूर्वक व्याख्यान करके अब छह आवश्यकों को कहेंगे-
आवश्यक का निर्युक्ति अर्थ-
ण वसो अवसो अवसस्सकम्ममावस्सयंति बोधव्वा।
जुत्तित्ति उवायत्ति य णिरवयवा होदि णिज्जुत्ती।।५१५।।
जो वश में नहीं है वह अवश है। उस अवश मुनि की क्रिया को आवश्यक कहते हैं। युक्ति और उपाय एक हैं, इस प्रकार सम्पूर्ण उपाय निर्युक्ति कहलाता है। तात्पर्य यह है कि- जो मुनि हिंसा आदि पाँच पाप, पाँच इन्द्रियाँ और क्रोध आदि कषायों के वश में नहीं हैं, वे ‘अवश’ हैं, उन साधुओं का अहोरात्र का आचरण वही आवश्यक कहलाता है अथवा अवश्य करने योग्य क्रियाओं को आवश्यक कहते हैं। आवश्यक छह प्रकार के माने गये हैं। यथा-सामायिक, चतुर्विंशतिस्तव, वंदना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और कायोत्सर्ग। प्रश्न-पंडित बुधजन जी ने तो प्रत्याख्यान की जगह स्वाध्याय को लिया है। जैसा कि पाठ है-
समता धर वंदन करें नाना थुती बनाय।
प्रतिक्रमण स्वाध्यायजुत कायोत्सर्ग लगाय।।
इसी तरह छहढाला में भी पंडित दौलतराम ने स्वाध्याय ही लिया है। सो कैसे ? इस मूलाचार में तो प्रत्याख्यान नाम से ही पाँचवाँ आवश्यक है, स्वाध्याय नाम से नहीं। जैसा कि-
सामायिय चउवीसत्थव वंदणयं पडिक्कमणं।
पच्चक्खाणं च तहा काओसग्गो हवदि छट्ठो।।५१६।।
ऐसे ही आचारसार अनगारधर्मामृत आदि ग्रंथों में भी मुनियों के आवश्यक में प्रत्याख्यान को ही लिया है। पंडित बुधजन कवि ने कहाँ से ऐसा पाठ लिया है, सो विद्वानों को विचार करना चाहिए। प्रश्न-पुन: यह स्वाध्याय क्रिया मुनियों के लिए आवश्यक नहीं रही ? उत्तर-ऐसी बात भी नहीं है, इसी मूलाचार में साधुओं द्वारा अवश्य करने वाले अट्ठाईस कृतिकर्म (विधिवत् कायोत्सर्ग) गिनाये हैं। उसमें चार बार स्वाध्याय के बारह कायोत्सर्ग लिखे गये हैं इसलिए यह चार बार का स्वाध्याय इन्हीं आवश्यकों में गर्भित हो जाता है, ऐसा समझ में आता है।
यथा-
चत्तारि पडिक्कमणे किदियम्मा तिण्णि होंति सज्झाए।
पुव्वण्हे अवरण्हे किदियम्मा चोद्दसा होंति।।६०२।।
इसकी टीका में अट्ठाईस कृतिकर्म का स्पष्टीकरण है और उसी में चार बार के स्वाध्याय का खुलासा है।
सामायिक आवश्यक
प्रश्न-सामायिक का अर्थ क्या है ? उत्तर-सुख-दु:ख, जीवन-मरण, लाभ-अलाभ, शत्रु-मित्र आदि में समताभाव-राग-द्वेष रहित परिणाम ही सामायिक है तथा त्रिकाल में देववंदना अर्थात् विधिवत् ‘जयतु भगवान्’ इत्यादि रूप चैत्यभक्ति और पंचगुरुभक्ति का पाठ करना सो सामायिक है। यह मूलाचार के आधार से ही है।
यथा-
‘‘जीवितमरणलाभालाभसंयोगविप्रयोगबन्ध्वरिसुखदु:
खादिषु यदेतत्समत्वं समानपरिणाम:
त्रिकालदेववंदनाकरणं च तत्सामायिवं व्रतं भवतीत्यर्थ:।’’
प्रश्न-सामायिक संयम भी तो है जो कि पाँच भेदरूप संयम का प्रथम भेद है, उसमें और इसमें क्या अंतर है ?
उत्तर-‘सर्वसावद्ययोगाद्विरतोऽस्मि’ मैं सर्व पाप सहित मन, वचन, काय की प्रवृत्ति से विरक्त होता हूँ। इस प्रकार से एक अभेदरूप संयम को सामायिक संयम कहते हैं तथा मैं हिंसा को छोड़ता हूँ, असत्य को छोड़ता हूँ, चोरी को छोड़ता हूँ, मैथुन को छोड़ता हूँ और सर्व परिग्रह को छोड़ता हूँ। इस प्रकार भेद करके सर्व सावद्य-पापों का त्याग करना छेदोपस्थापना संयम है। तीर्थंकर आदि महापुरुष एक सामायिक संयम को ही ग्रहण करते हैं। शेष साधारण पुरुष दोनों संयम को धारण करते हैं तथा बाईस तीर्थंकरों के तीर्थ में भी जन्मे पुरुष अभेदरूप संयम ही धारण करते हैं।
मूलाचार में श्री कुन्दकुन्ददेव ने कहा है-
बावीसं तित्थयरा सामायियसंजमं उवदिसंति।
छेदुवठावणियं पुण भयवं उसहो य वीरो य।।५३५।।
अजितनाथ से लेकर पाश्र्वनाथ पर्यंत बाईस तीर्थंकरों ने एक सामायिक संयम का ही उपदेश दिया है, भगवान आदिनाथ तथा भगवान महावीर ने सामायिक और छेदोपस्थापना इन दोनों संयम का उपदेश दिया है।
प्रश्न-ऐसा क्यों ?
उत्तर-अन्य शिष्यों को प्रतिपादन करने के लिए, अपनी इच्छानुसार उनका अनुष्ठान करने के लिए, विभाग करके समझने के लिए भी सामायिक संयम सरल हो जाता है इसलिए महाव्रत पाँच कहे गये हैं। इस भेद का नाम ही छेदोपस्थापना संयम है।
प्रश्न-आदि तीर्थ में और अंत तीर्थ में छेदोपस्थापना की आवश्यकता क्यों हुई ?
उत्तर-आदिनाथ के तीर्थ में शिष्य दु:ख से-कठिनता से शुद्ध किये जाते थे क्योंकि वे अत्यर्थ सरल स्वभावी थे। अंतिम तीर्थंकर के तीर्थ में भी शिष्यों का कठिनता से प्रतिपालन किया जाता है क्योंकि वे अत्यर्थ वक्र स्वभावी होते हैंं। ये पूर्वकाल के शिष्य और पश्चिम काल के शिष्य योग्य-उचित और अयोग्य-अनुचित को ठीक से नहीं समझते हैं इसीलिए आदि और अंत के दोनों तीर्थंकरों ने छेदोपस्थापना संयम का उपदेश दिया है। आदिनाथ के तीर्थ के समय भोगभूमि समाप्त होकर ही कर्मभूमि प्रारंभ हुई थी अत: उस समय के शिष्य बहुत ही सरल किन्तु जड़ (अज्ञान) स्वभाव वाले थे तथा अंतिम तीर्थंकर के समय पंचमकाल का प्रारंभ होने वाला था अत: उस समय के शिष्य बहुत ही कुटिल परिणामी और जड़ स्वभावी थे इसीलिए इन दोनों तीर्थंकरों ने छेद अर्थात् भेद के उपस्थापन अर्थात् कथन रूप पाँच महाव्रतों का उपदेश दिया है। शेष बाईस तीर्थंकरों के शिष्य विशेष बुद्धिमान थे इसीलिए उन तीर्थंकरों ने मात्र ‘सर्वसावद्ययोग’ के त्यागरूप एक सामायिक संयम का ही उपदेश दिया है क्योंकि उनके लिए उतना ही पर्याप्त था। आज भगवान महावीर का ही शासन चल रहा है अत: आजकल के सभी साधुओं को मुख्यरूप से भेदरूप चारित्र के पालन का ही उपदेश है। इस सामायिक के नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की अपेक्षा छह भेद हो जाते हैं। शुभ-अशुभ नाम सुनकर राग-द्वेष नहीं करना नाम सामायिक है। सुस्थित, सुप्रमाण, सर्व अवयवों से संपूर्ण, तदाकार मूर्तियों में और अशुभ चेष्टायुक्त, अप्रमाण, हीनावयव आदि मूर्तियों में राग-द्वेष का अभाव स्थापना सामायिक है। सुवर्ण, चांदी, हीरा आदि और तृण, मिट्टी आदि में समभाव रखना द्रव्य सामायिक है। रमणीय नगर, उद्यान आदि अच्छे क्षेत्र में और रुक्षस्थान, जंगल आदि में समताभाव रखना क्षेत्र सामायिक है। वर्षा, शिशिर आदि ऋतुओं में राग द्वेष का त्याग करना काल सामायिक है अथवा जिस काल में सामायिक करते हैं वह पूर्वाण्ह, मध्यान्ह, अपराण्ह काल से भेदरूप काल सामायिक है। सभी जीवों से मैत्री भाव रखना और अशुभ परिणामों का त्याग करना भाव सामायिक है।
सम्मत्तणाणसंजमतवेहिं जं तं पसत्थसमगमणं।
समयंतु तं तु भणिदं तमेव सामाइयं जाण।।५१९।।
सम्यग्दर्शन, ज्ञान, संयम और तप के साथ जो प्रशस्त समागम है वह समय कहा गया है, तुम उसे ही सामायिक जानो। आगे भी ऐसे ही अनेक गाथाएँ हैं कि जिनमें राग, द्वेष का अभाव, सावद्य योग से विरति, कषायों के निग्रह आदि से परिणत हुई आत्मा के ही सामायिक कहा है।
यथा-
जस्स सण्णिहिदो अप्पा संजमे णियमे तवे।
तस्स सामायियं ठादि इदि केवलिसासणे।।५२५।।
जिसकी आत्मा संयम, नियम और तप में स्थित है उसके ही सामायिक होता है, ऐसा श्रीकेवली भगवान के शासन में कहा है। तात्पर्य यह है कि सामायिक के नियतकालिक और अनियतकालिक ऐसे दो भेद हैं। उनमें से त्रिकालसामायिक नियतकालिक है और सदा समताभाव सामायिक अनियतकालिक है। नियतकालिक सामायिक करने का क्रम कहते हैं-
पडिलिहियअंजलिकरो उवजुत्तो उट्ठिऊण एयमणो।
अव्वाखित्तो वुत्तो करेदि सामाइयं भिक्खू।।५३८।।
पिच्छी को हाथ में लेकर अंजलि जोड़कर उपयोगपूर्वक उठकर, एकाग्रमना होकर मन को विक्षेपरहित करके मुनि सामायिक करते हैं। इस सामायिक में कृतिकर्म विधिपूर्वक चैत्यभक्ति और पंचगुरुभक्ति का पाठ होता है। वह विधि क्रियाकलाप, यतिक्रियामंजरी, सामायिक१ आदि पुस्तकों में प्रकाशित हुई है। यह संक्षेप में सामायिक आवश्यक कहा है।
चतुर्विंशति स्तव आवश्यक
वृषभ आदि चौबीस तीर्थंकरों की स्तुति करना चतुर्विंशति स्तव नाम का दूसरा आवश्यक है। इस स्तव में नामस्तव, स्थापनास्तव, द्रव्यस्तव, क्षेत्रस्तव, कालस्तव और भावस्तव, यह छह प्रकार का निक्षेप घटित करना चाहिए। नाम स्तव-चौबीस तीर्थंकरों के वास्तविक अर्थ का अनुसरण करने वाले एक हजार आठ नामों से स्तवन करना नामस्तव है। स्थापना स्तव-चौबीस तीर्थंकरों की कृत्रिम-अकृत्रिम प्रतिमाएं स्थापना प्रतिमाएं हैं। इनमें राजा, महाराजा, चक्रवर्ती, सामान्य श्रावक आदि द्वारा निर्मापित प्रतिमाएं-कृत्रिम प्रतिमाएं अगणित हैं और सुमेरु पर्वत आदि के जिनमंदिरों में विराजमान अकृत्रिम प्रतिमाएं असंख्यात हैं। उनका स्तवन करना स्थापनास्तव है। द्रव्य स्तव-तीर्थंकरों के शरीर, जो कि परमौदारिक हैं, उनके वर्ण भेदों का वर्णन करते हुए स्तवन करना द्रव्यस्तव है। जैसे कि पद्मप्रभ और वासुपूज्य भगवान लाल कमल के वर्ण के थे। चन्द्रप्रभ और पुष्पदंत भगवान श्वेत कमल के सदृश शरीर वाले थे। ‘‘द्वौ कुंदेदु तुषारहारधवलौ’’ आदि। क्षेत्र स्तव-वैâलाशगिरि, सम्मेदगिरि, ऊर्जयन्तगिरि, पावापुरी, चंपापुरी आदि निर्वाणक्षेत्रों का और समवसरण क्षेत्रों का स्तवन करना क्षेत्रस्तव है। काल स्तव-तीर्थंकरों के स्वर्गावतरण, जन्म, दीक्षा, केवलज्ञान और निर्वाणकल्याणक के काल का स्तवन करना कालस्तव है। भाव स्तव-तीर्थंकरों के केवलज्ञान, केवलदर्शन, अनंतवीर्य, अनंतसुख आदि गुणों का स्तवन करना भावस्तव है। भरत और ऐरावत क्षेत्रों की अपेक्षा यह चतुर्विंशतिस्तव कहा गया है किन्तु पूर्वविदेह और अपरविदेह की अपेक्षा से सामान्य ‘तीर्थंकरस्तव’ नाम का ही आवश्यक समझना चाहिए। इस प्रकार से इसमें कोई दोष नहीं है अर्थात् पाँच भरत और पाँच ऐरावत क्षेत्रों में ही काल परिवर्तन है। इनमें चतुर्थकाल में ही चौबीस-चौबीस तीर्थंकर होते हैं किन्तु एक सौ साठ विदेह क्षेत्रों में हमेशा ही तीर्थंकर होते रहते हैं अत: उनकी संख्या का कोई नियम नहीं है। उन विदेह क्षेत्रों की अपेक्षा इस आवश्यक को ‘तीर्थंकरस्तव’ ही कहना चाहिए। अब श्री कुन्दकुन्ददेव स्वयं तीर्थंकरस्तव करते हुए एक गाथा कहते हैं-
लोगुज्जोए धम्मतित्थयरे जिणवरे य अरहंते।
कित्तण केवलिमेव य उत्तमबोहिं मम दिसंतु।।५४१।।
लोक में उद्योत करने वाले, धर्मतीर्थ के कर्ता, अर्हंत, केवली, जिनेश्वर प्रशंसा के योग्य हैं। वे मुझे उत्तम बोधि प्रदान करें। तात्पर्य यह है कि लोक को प्रकाशित करने वाले, धर्म तीर्थकर, जिनवर, केवली, अर्हंत भगवान उत्तम हैं। इस प्रकार से उनका कीर्तन करना, उनकी प्रशंसा करना तथा ‘वे मुझे बोधि प्रदान करें ऐसा कहना ही तीर्थंकरों का स्तव है। अब इन पदों में दश भेद करके उनका खुलासा करते हैं। उनमें से सर्वप्रथम ‘लोकोद्योतकर’ विशेषण को कहते हैं-लोक-लोकन करना-अवलोकन करना, जिनेन्द्रदेव द्वारा यह सर्व जगत् लोकित-अवलोकित कर लिया जाता है, इसीलिए इसकी ‘लोक’ यह संज्ञा सार्थक है अथवा जहाँ तक जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और काल ये पाँचों द्रव्य देखे जाते हैं वह ‘लोक’ है, उससे परे अलोक है। मूलाचार में इस लोक के नाम, स्थापना आदि के भेद से नव भेद किये हैं। विशेष जिज्ञासु को वहीं से देख लेना चाहिए। उद्योत-प्रकाश, इसके दो भेद हैं-द्रव्य उद्योत और भाव उद्योत। अग्नि, चन्द्र, सूर्य और मणि आदि द्रव्य उद्योत हैं चूँकि इनसे बाह्य वस्तुएँ देखी जाती हैं। ज्ञान को भाव उद्योत कहा है क्योंकि वह ज्ञान ही स्व-पर प्रकाशक है। इसके मति, श्रुत, अवधि, मन:पर्यय और केवलज्ञान ये पाँच भेद हैं। द्रव्योद्योत अन्य प्रकाश से बाधित होता है तथा परिमित क्षेत्र में रहता है किन्तु भावोद्योत लोक-अलोक को प्रकाशित करने में समर्थ है। चौबीसों तीर्थंकर भाव उद्योत से सर्वलोक को प्रकाशित करने वाले हैं, इसलिए ‘लोकोद्योतकर’ कहलाते हैं।
अब ‘धर्मतीर्थकर’ पद का व्याख्यान करते हैं- धर्म-जो उत्तम सुख में धरे-पहुँचावे, वह धर्म है। इसके तीन भेद हैं-श्रुतधर्म, अस्तिकायधर्म और चारित्रधर्म। यहाँ पर श्रुतधर्म की प्रमुखता है क्योंकि इससे ही संसार समुद्र को पार किया जाता है। तीर्थ के दो भेद हैं-द्रव्यतीर्थ और भावतीर्थ। दाह को उपशम करना, तृष्णा का नाश करना और मल-कीचड़ को धो डालना, इन तीन कारणों से युक्त तीर्थ गंगा, पुष्कर आदि द्रव्य तीर्थ हैं। दर्शन, ज्ञान और चारित्र इन तीन कारणों से युक्त तीर्थ भावतीर्थ हैं। चौबीसों तीर्थंकर भावतीर्थ के कर्ता हैं इसलिए वे ‘धर्मतीर्थंकर’ कहलाते हैं। अब ‘जिनवर’ पद को स्पष्ट करते हैं- जिन-जो क्रोध, मान, माया और लोभ को जीत चुके हैं, वे ‘जिन’ कहलाते हैं। उनमें वर-प्रधान को ‘जिनवर’ कहते हैं। ‘अर्हंत’ पद को कहते हैं- अरि-कर्म शत्रुओं का और जन्म का हनन करने वाले होने से ये तीर्थंकर ‘अर्हंत’ कहलाते हैं अथवा जो वंदना और नमस्कार के योग्य हैं, पूजा सत्कार के योग्य हैं और सिद्धि गमन के योग्य हैं, वे ‘अर्हंत’ कहलाते हैं। अरिहंत और अर्हंत, ऐसे दो पद माने गये हैं। व्युत्पत्ति के अनुसार अरि अर्थात् मोह का हनन करने वाले ‘अरिहंत’ हैं और अर्ह-योग्य-समर्थ अर्थ में जो इंद्रों द्वारा पूजा आदि के योग्य हैं, वे ‘अर्हंत’ कहलाते हैं। महामंत्र में ‘अरिहंताणं’ और ‘अरहंताणं’ ऐसे दोनों पाठ बोले जाते हैं। ये दोनों ही शुद्ध हैं। इस प्रकार ये तीर्थंकर लोकोद्योतकर हैं, धर्मतीर्थ के कर्ता हैं, जिनवर हैं और अर्हंत हैं। किसलिए इनका कीर्तन करना ? ऐसा प्रश्न होने पर कहते हैं-कीर्तनीय-ये चौबीसों तीर्थंकर, सुर-असुर आदि सभी के द्वारा कीर्तन, वर्णन और प्रशंसन करने योग्य इसीलिए हैं कि इन्होंने दर्शन आदि के विनय का उपदेश दिया है। ये तीर्थंकर केवली हैं- केवली-ये अर्हंत भगवान केवलज्ञान के विषयभूत संपूर्ण लोक-अलोक को जानते हैं तथा देखते हैं और इनका चारित्र केवलज्ञान ही है अर्थात् इनके अशेष व्यापार छूट चुके हैं, इसीलिए ये ‘केवली’ कहलाते हैं। ये तीर्थंकर ‘उत्तम’ हैं- उत्तम-ये तीर्थंकर मिथ्यात्व, ज्ञानावरण और चारित्रमोह इन तीन तम-गाढ़ अंधकार से उन्मुक्त हो चुके हैं इसलिए ये ‘उत्तम’ कहलाते हैं। अब प्रश्न यह होता है कि इन विशेषणों से सहित तीर्थंकर हमें क्या देवें ? सो ही कहते हैं- आरोग्य-बोहिलाहं दिंतु समाहिं च मे जिणविंरदा। किं ण हु णिदाणमेयं णवरि विभासेत्थ कायव्वा।।५६८।। वे जिनेन्द्रदेव मुझे आरोग्य, बोधि का लाभ और समाधि प्रदान करें।
प्रश्न- क्या यह निदान नहीं है ?
उत्तर- नहीं है, यहाँ केवल विकल्प समझना चाहिए। अर्थात् यह भक्ति का एक प्रकार है। आगे उसी को कहते हैं-
भासा असच्चमोसा णवरि हु भत्तीय भासिदा एसा।
ण हु खीणरागदोसा दिंति समाहिं च बोहिं च।।५६९।।
जं तेहिं दु दादव्वं तं दिण्णं जिणवरेहिं सव्वेहिं।
दंसणणाणचरित्तस्स एस तिविहस्स उवदेसो।।५७०।।
यह असत्यमृषा भाषा है, वास्तव में यह केवल भक्ति से कही गई है क्योंकि राग द्वेष से रहित भगवान् समाधि और बोधि को नहीं देते हैं। उनके द्वारा जो देने योग्य था, वह सभी जिनवरों ने दे ही दिया है। सो वह दर्शन, ज्ञान और चारित्र इन तीनों का उपदेश है अर्थात् जिनेन्द्रदेव ने रत्नत्रय का उपदेश दिया है, वही बोधि है। इस प्रकार तीर्थंकरों की भक्ति से क्या-क्या फल मिलते हैं ? सो ही बताते हैं-
भत्तीए जिणवराणं खीयदि जं पुव्वसंचियं कम्मं।
आयरियपसाएण य विज्जा मंता य सिज्झंति।।५७१।।
अरहंतेसु य राओ ववगदरागेसु दोसरहिएसु।
धम्मम्हि य जो राओ सुदे य जो बारसविधम्हि।।५७२।।
आयरियेसु य राओ समणेसु य बहुसुदे चरित्तड्ढे।
एसो पसत्थराओ हवदि सरागेसु सव्वेसु।।५७३।।
तेसिं अहिमुहदाए अत्था सिज्झंति तह य भत्तीए।
तो भत्ति ‘रागपुव्वं’ वुच्चइ एदं ण हु णिदाणं।।५७४।।
जिनेन्द्रदेव की भक्ति से पूर्वसंचित कर्म नष्ट हो जाते हैं और आचार्यों की भक्ति के प्रसाद से विद्या और मंत्रों की सिद्धि होती है। राग, द्वेष रहित अर्हंतों में, धर्म में, द्वादशांग श्रुत में, अचार्यों में, मुनियों में, और चारित्र युक्त बहुश्रुत विद्वानों में जो राग होता है, वह प्रशस्त-शुभ राग है वह सभी सरागी मुनियों में पाया जाता है अर्थात् सरागसंयमी मुनि इन सभी में अनुरागरूप भक्ति करते ही हैं। उनके अभिमुख होने से तथा उनकी भक्ति से मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं इसलिए यह भक्ति रागपूर्वक ही कही गई है। यह निदान नहीं कहलाती है, ‘क्योंकि इससे संसार के कारणों का अभाव होता है१।’ मुनिराज चार अंगुल के अंतराल से पैर रखकर खड़े होकर पिच्छिका लेकर हाथ जोड़कर एकाग्रमना होकर चौबीस तीर्थंकरों की स्तुति करते हैं। यहाँ यह स्तव आवश्यक पढ़कर यह समझना कि आज पंचमकाल में आहार-विहार आदि क्रियाओं को करने वाले मुनि सराग संयमी ही हैं उन्हें यह क्रिया करनी ही होती है। वे भी अपने योग्य आरोग्य, बोधिलाभ, समाधिलाभ आदि की याचना करते हैं। न यह याचना निदान है और न ईश्वर को कर्ता मानने का दोष ही आता है। ऐसे ही श्रावकगण यदि ऐसा बोलते हैं कि- ‘‘दरिद्रीन को द्रव्य के दान दीने, अपुत्रीन को तू भले पुत्र कीने।’’ इत्यादि स्तोत्र पाठ बोलने से भगवान को कर्तापने का आरोप नहीं होता है किन्तु भक्त की भक्ति विशेष उसके मनोरथों को निश्चित ही सफल कर देती है। वास्तव में कोई भी गृहस्थ क्यों न हो वह दरिद्री, नि:संतान या रोगी नहीं रहना चाहता है तो यदि वह कुदेवों को छोड़कर जिनेन्द्रदेव की भक्ति करते हुए कुछ याचना कर भी लेता है तो भी उसका सम्यक्त्व नष्ट नहीं होता है। प्रथमानुयोग में ऐसे अनेक-अनेक उदाहरण भरे पड़े हैं। यहाँ जब मुनियों के लिए भक्तिमार्ग की इतनी विशेषता, महानता व प्रधानता कही है तब गृहस्थ श्रावकों के लिए तो जिनेन्द्रदेव की भक्ति अधिक रूप में करते रहना चाहिए। संकट के समय शांति विधान, सिद्धचक्र विधान, इन्द्रध्वज विधान आदि अनुष्ठान करना चाहिए। विधिवत् किये गये ये विधान आज भी भक्तों के अभीष्ट को सिद्ध करते हैं, यह प्रत्यक्ष देखा जा रहा है। अत: प्रत्येक श्रावक का कर्तव्य है कि वह प्रतिदिन देवपूजा अवश्य करे, यदि न कर सके तो देवदर्शन तो अवश्य ही करे और अपने बालकों में भी दर्शन करने के संस्कार डाले।
वंदना आवश्यक
सामान्यरूप से ‘जयति भगवान् हेमांभोजप्रचारविजृंभिता-’ इत्यादि चैत्यभक्ति से लेकर पंचगुरुभक्ति पर्यंत विधिवत् जो स्तुति की जाती है, उसे वंदना कहते हैं अथवा शुद्ध भाव से पंचपरमेष्ठीविषयक नमस्कार करना वंदना है। इसके भी छह भेद हैं-नामवंदना, स्थापनावंदना, द्रव्यवंदना, क्षेत्रवंदना, कालवंदना और भाववंदना। एक तीर्थंकर का नाम उच्चारण करना तथा सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधुओं का नाम उच्चारण करना नामवंदना है। एक तीर्थंकर के प्रतिबिम्ब का तथा सिद्ध, आचार्यादि के प्रतिबिम्बों का स्तवन करना स्थापनावंदना है। एक तीर्थंकर के शरीर का तथा सिद्ध और आचार्य आदि के शरीर का स्तवन करना द्रव्यवंदना है। इन एक तीर्थंकर, सिद्ध और आचार्य आदि से अधिष्ठित जो क्षेत्र हैं, उनकी स्तुति करना क्षेत्रवंदना है। इन एक तीर्थंकर तथा सिद्ध, आचार्य आदि से युक्त जो काल है, उसके आश्रित स्तुति करना कालवंदना है। एक तीर्थंकर और सिद्ध तथा आचार्यों के गुणों का शुद्ध परिणाम से स्तवन करना भाववंदना है। नामवंदना का विस्तार से वर्णन-कृतिकर्म, चितिकर्म, पूजाकर्म और विनयकर्म, ये वंदना के पर्यायवाची नाम हैं। फिर भी इन चारों का अर्थ कहते हैं- कृतिकर्म-जिस अक्षर समूह से या जिस परिणाम से अथवा जिस क्रिया से आठ प्रकार के कर्मों को काटा जाता है-छेदा जाता है, वह कृतिकर्म है अर्थात् पापों के विनाशन का उपाय कृतिकर्म है। चितिकर्म-जिन अक्षरों से या जिन परिणामों से अथवा जिस क्रिया से तीर्थंकर प्रकृति आदि पुण्य कर्म का चयन-संचय हो जाता है-सम्यक्प्रकार से अपने साथ एकीभावरूप हो जाता है। ऐसा यह पुण्यकर्म के संचय का कारण चितिकर्म कहलाता है। पूजाकर्म-जिन अक्षरों के द्वारा या जिन परिणामों अथवा क्रियाओं से अरहंत देव आदि पूजे जाते हैं। उन्हें आह्वानन आदि कर जो पुष्प माला१, चंदन आदि चढ़ाया जाता है, वह पूजाकर्म-पूजा क्रिया है। विनयकर्म-जिसके द्वारा कर्मों का निराकरण किया जाता है, उन्हें संक्रमण, उदय या उदीरणा आदि भाव से परिणत करा दिया जाता है, वह विनयक्रिया है, जो कि गुरुजनों की शुश्रूषारूप है।
यह वंदना क्रिया नामक आवश्यक कर्म किसे करना चाहिए ?
किसकी करना चाहिए ? किस विधान से करना चाहिए ?
किस अवस्था विशेष में करना चाहिए ?
और कितनी बार करना चाहिए ?
इसमें कितनी अवनति (प्रणाम) होती हैं ?
कितनी शिरोनति होती हैं ?
कितने आवर्त होते हैं ?
और कितने दोषों से रहित यह ‘वंदना’ नामक कृतिकर्म होता है ?
इस प्रकार यहाँ नव प्रश्न हुए हैं,
इन प्रत्येक का उत्तर देते हैं-
(१) यह कृतिकर्म, विनयक्रिया अथवा ‘वंदना’ कौन करते हैं ? ऐसा प्रश्न होनेपर श्री कुन्दकुन्ददेव कहते हैं-जो पाँच महाव्रतों से युक्त हैं, धर्म और धर्म के फल में हर्ष से रोमांचित हो जाते हैं, आलस्य रहित हैं, मान कषाय से रहित हैं और कर्मों की निर्जरा करने के इच्छुक हैं, ऐसे मुनिराज ही अरहंत, सिद्ध, आचार्यादि की और अपने से दीक्षा में बड़े मुनियों की वंदना करते हैं।
(२) वह वंदना कृतिकर्म किसका करना चाहिए ? आचार्य, उपाध्याय, प्रवर्तक, स्थविर और गणधर इन पाँचों की कृतिकर्म विधिपूर्वक वंदना करनी चाहिए।
(३) गुरुजन किस तरह विराजमान हों, जब वंदना करे ? आसन पर बैठे हुए हों, शांतचित्त हों एवं सन्मुख मुख किये हुए हों, उनकी अनुज्ञा लेकर विद्वान् मुनि ‘वंदना’ विधि का प्रयोग करें।
(४) वंदना कब करना ? दोषों की आलोचना के समय, छह आवश्यक क्रियाओं के समय, प्रश्न करने के समय, पूजा के समय, स्वाध्याय के समय, अपने से कुछ अपराध हो जाने पर, गुरू-आचार्य, उपाध्याय आदि की वंदना करे।
(५) कितनी बार वंदना करना चाहिए ? त्रिकाल-तीन बार देववंदना के छह कृतिकर्म होते हैं, दो बार के प्रतिक्रमण के आठ, चार बार के स्वाध्याय के बारह और प्रात:-सायं दो बार योगभक्ति के दो ऐसे ६±८±१२±२·२८ बार कृतिकर्म विधिपूर्वक वंदना होती है। इसका स्पष्टीकरण ऐसा है कि मुनियों के अहोरात्र संबंधी अट्ठाईस कायोत्सर्ग कहे गये हैं। इन कायोत्सर्गों में कृतिकर्म की विधि से वंदना की जाती है। इनमें देववंदना, श्रुतवंदना ही प्रधान है, गुरुओं की वंदना भी है किन्तु इन २८ कृतिकर्म में गौण है। एक देववंदना में चैत्य और पंचगुरुभक्ति संबंधी दो कृतिकर्म होते हैं इसलिए त्रिकाल देववंदना के ६ कृतिकर्म हुए। प्रतिक्रमण में सिद्धभक्ति, प्रतिक्रमण भक्ति, वीरभक्ति और चौबीस तीर्थंकर भक्ति इन चार संबंधी चार कृतिकर्म होते हैं इसलिए दैवसिक प्रतिक्रमण के ४ और रात्रिक के ४ ऐसे ८ कृतिकर्म हो गये। पूर्वाण्ह स्वाध्याय में प्रारंभ में श्रुत व आचार्य भक्ति तथा समापन में श्रुतभक्ति इन तीन भक्ति संबंधी ३ ऐसे अपराण्ह, पूर्वरात्रिक और अपररात्रिक इन चार बार के स्वाध्याय के १२ कृतिकर्म हुए। रात्रियोग ग्रहण और विसर्जन इन दो समयों में दो बार योगभक्ति संबंधी २ कृतिकर्म ये सब मिलकर २८ कृतिकर्म होते हैं। गुरुओं की वंदना त्रिकाल सिद्धभक्ति, श्रुतभक्ति और आचार्यभक्तिपूर्वक होती है। विशेष प्रसंगों में भी भक्तिपाठपूर्वक होती है तथा सामान्यतया ‘नमोऽस्तु’ कहकर नमस्कार कर लेने रूप भी होती है।
कितनी अवनति ? कितनी शिरोनति ? और कितने आवर्त होते हैं ? इन तीनों प्रश्नों का उत्तर देते हुए श्री कुन्दकुन्ददेव कहते हैं–
दोणदं तु जहाजादं बारसावत्तमेव च।
चदुस्सिरं तिसुद्धं च किदियम्मं पउंजदे।।६०३।।
यथाजात मुद्राधारी मुनि दो नमस्कार, बारह आवर्त और चार शिरोनति करते हुए मन-वचन-काय की शुद्धिपूर्वक कृतिकर्म को करे। महामंत्र पढ़ने की आदि में एक बार भूमिस्पर्शनात्मक नमस्कार तथा चतुर्विंशति स्तव के दूसरी बार अवनति-भूमि स्पर्शनात्मक नमस्कार, ये दो अवनति एक कृतिकर्म में की जाती हैं। महामंत्र के आदि और अंत में दो हाथ मुकुलित जोड़कर माथे से लगाना तथा चतुर्विंशति स्तव के आदि और अंत में हाथ मुकुलित जोड़कर माथे से लगाना, ऐसी ये चार शिरोनति होती हैं। महामंत्र उच्चारण के आदि में जुड़ी हुई अंजलि को दाहिनी तरफ से तीन बार घुमाना सो तीन आवर्त हुए। सामायिक दंडक की समाप्ति में ऐसे ही तीन आवर्त करना। चतुर्विंशति स्तव के आदि में और अंत में तीन-तीन बार अंजलि को घुमाना ऐसे ये बारह आवर्त होते हैं। इस विधि का स्पष्टीकरण यह है- एक बार के कायोत्सर्ग में यह उपर्युक्त विधि की जाती है। उसी का नाम कृतिकर्म है। यह विधि देववंदना, प्रतिक्रमण आदि सर्व क्रियाओं में भक्तिपाठ के प्रारंभ में की जाती है। जैसे देववंदना में चैत्यभक्ति के प्रारंभ में-
‘अथ पौर्वाण्हिक-देववंदनायां पूर्वाचार्यानुक्रमेण सकलकर्मक्षयार्थं
भावपूजावंदनास्तवसमेतं श्रीचैत्यभक्तिकायोत्सर्गं करोम्यहं।’’
यह प्रतिज्ञा हुई, इसको बोल कर भूमिस्पर्शनात्मक पंचांग नमस्कार करें, यह एक अवनति हुई। अनंतर तीन आवर्त और एक शिरोनति करके ‘‘णमो अरिहंताणं,……चत्तारि मंगलं…..अड्ढाइज्जदीव…..इत्यादि पाठ बोलते हुए…….दुच्चरियं वोस्सरामि’’ तक पाठ बोले यह ‘सामायिक स्तव’ कहलाता है। पुन: तीन आवर्त और एक शिरोनति करें। इस तरह सामायिक दण्डक के आदि और अन्त में तीन-तीन आवर्त और एक-एक शिरोनति होने से छह आवर्त और दो शिरोनति हुर्इं। पुन: नौ बार णमोकार मंत्र को सत्ताईस स्वासोच्छ्वास में जपकर भूमिस्पर्शनात्मक नमस्कार करें। इस तरह प्रतिज्ञा के अनंतर और कायोत्सर्ग के अनन्तर ऐसे दो बार अवनति हो गर्इं। बाद में तीन आवर्त और एक शिरोनति करके ‘‘थोस्सामि स्तव’’ पढ़कर अन्त में पुन: तीन आवर्त, एक शिरोनति करें। इस तरह चतुर्विंशति स्तव के आदि और अन्त में तीन-तीन आवर्त और एक-एक शिरोनति करने से छह आवर्त और दो शिरोनति हो गर्इं। ये सामायिक स्तव संबंधी छह आवर्त, दो शिरोनति तथा चतुर्विंशति स्तव संबंधी छह आवर्त और चार शिरोनति होती हैं। जुड़ी हुई अंजुलि को दाहिनी तरफ से घुमाना सो आवर्त का लक्षण है। यहाँ पर टीकाकार ने मन वचन काय की शुभ प्रवृत्ति का करना आवर्त कहा है जो कि उस क्रिया के करने में होना ही चाहिए। इतनी क्रियारूप कृतिकर्म को करके ‘‘जयतु भगवान्’’ इत्यादि चैत्यभक्ति का पाठ पढ़ना चाहिए। ऐसे ही जो भी भक्ति जिस क्रिया में करनी होती है तो यही विधि की जाती है।
(९) कितने दोषों से रहित कृतिकर्म करना चाहिए ?
कृतिकर्म-विधि वंदना-देववंदना बत्तीस दोषों से रहित करना चाहिए। उन दोषों के नाम निम्न प्रकार हैं-अनादृत, स्तब्ध, प्रविष्ट, परिपीडित, दोलायित, अंकुशित, कच्छपरिंगित, मत्स्योद्वर्त, मनोदुष्ट, वेदिकाबद्ध, भय, विभ्यत्व, ऋद्धिगौरव, गौरव, स्तेनित, प्रतिनीत, प्रदुष्ट, तर्जित, शब्द, हीलित, त्रिबलित, वुंâचित, दृष्ट, अदृष्ट, संघकरमोचन, आलब्ध, अनालब्ध, हीन, उत्तरचूलिका, मूक, दर्दुर और चुलुलित इस प्रकार साधु इन बत्तीस दोषों से रहित-विशुद्ध कृतिकर्म का प्रयोग करते हैं। इन बत्तीस दोषों का अर्थ मुनिगण, आर्यिकाओं या श्रावक-श्राविकाओं को भी मूलाचार, अनगार- धर्मामृत आदि से देख लेना चाहिए। यदि साधु इन बत्तीस दोषों से रहित पूर्वोक्त विधि से देववंदना करता है तो वह विपुल कर्मों की निर्जरा करता है क्योंकि इन बत्तीस दोषों के परिहार से बत्तीस ही गुण होते हैं। इसी प्रकार हास्य, भय, आसादन, राग, द्वेष, गौरव, आलस्य, मद, लोभ, चौर्यभाव, प्रतिवूâलता, बालभाव, उपरोध हीन या अधिक पाठ बोलना, शरीर का स्पर्श करना, वचन बोलना, भृकुटी चढ़ाना, खात्कार-खखारना-खांसना इत्यादि दोषों को छोड़कर वंदना करे। जिनकी वंदना कर रहे हैं ऐसे भगवान् या गुरु आदि में अपने मन को लगाकर उनके गुणों का चिंतवन करते हुए अन्य कार्यों से उपयोग हटाकर विशुद्ध मन-वचन-काय से मौनपूर्वक वंदना करें तथा भक्तिपाठ आदि का उच्चारण ऐसा करें, जो स्वयं को प्रिय लगे व सुनने वालों को भी अच्छा लगे। जिनकी वंदना करनी है और जो वंदना करते हैं उन दोनों में एक हाथ का अंतर रहना चाहिए अर्थात् गुरु या जिनप्रतिमा की वंदना करते समय उनसे एक हाथ के अंतर से स्थित होकर उनको बाधा न करते हुए वंदना करें। अपने शरीर का स्पर्श और प्रमार्जन करके शरीर की शुद्धि करके पहले देव या गुरु के समक्ष वंदना की याचना करें। अर्थात् हे भगवन्! मैं आपकी वंदना करूँगा। ऐसी प्रार्थना करके गुरु का उपयोग अपनी तरफ करके उनकी वंदना और प्रणाम करें। संयत महाव्रती मुनि व आर्यिकाएं अपने असंयत माता-पिता की, असंयत विद्यागुरु की, चारित्र में भ्रष्ट दीक्षागुरु या विद्या गुरु की वंदना न करें। राजा, पाखंडी, तापसी, शास्त्रादि के ज्ञानी भी देशव्रती श्रावकों की या नाग, यक्ष, चंद्र, सूर्य इन्द्रादि देवों की भी वंदना करें तथा पाश्र्वस्थ, कुशील, संसक्त, अपसंज्ञक और मृगचरित्र शिथिलचारित्री दिगम्बर साधु हैं, इनकी भी वंदना न करें।
यहाँ तक तो वंदना करने वालों की बात हुई, अब जिनकी वंदना करते हैं, वे क्या करें ? सो बताते हैं- ‘देववंदना’ में वर्तमान में श्रीजिनेन्द्रदेव की प्रतिमाओं के समक्ष वंदना की जाती है अथवा वैसी सुविधा न होने से परोक्ष में भी की जाती है। साधुओं की यह त्रिकाल सामायिक क्रिया है। भगवान् की वंदना से तो विपुल कर्मों की निर्जरा और महान् पुण्यबंध होता है। आचार्य, उपाध्याय आदि की वंदना करने से वे ‘प्रतिवंदना’ करते हुए अपने शिष्यों की वंदना स्वीकार करते हैं अर्थात् जब शिष्य मुनि गुरुओं की वंदना करते हैं तब ‘नमोऽस्तु’ शब्द का उच्चारण करके हाथ में पिच्छिका लेकर अंजलि जोड़कर वंदना करते हैं। उसके बाद आचार्य आदि भी हाथ में मुकुलित मुद्रा से पिच्छिका लेकर ‘नमोऽस्तु’ बोलकर प्रतिवंदना करते हैं यही वंदना की स्वीकृति होती है। नमस्कार व आशीर्वाद की पद्धति-जब आर्यिकाएँ आपस में ‘गणिनी’ आदि बड़ी आर्यिकाओं को ‘वंदामि’ कहकर वंदना करती हैं तब वे बड़ी आर्यिकाएँ भी ‘वंदामि’ कहकर ही प्रतिवंदना करती हैं। आर्यिकाएँ तथा क्षुल्लक, क्षुल्लिकाएँ जब आचार्य आदि मुनियों को ‘नमोस्तु’ कहकर वंदना करती हैं तब मुनिगण दाहिना हाथ उठाकर ‘समाधिरस्तु’ ऐसा आशीर्वाद देते हैं। यही आशीर्वाद व्रतिकों को आर्यिकाएँ भी देती हैं। क्षुल्लक-क्षुल्लिकाएं आपस में ‘इच्छामि’ करते हैं। क्षुल्लक-क्षुल्लिकाएं भी व्रतिकों को समाधिरस्तु आशीर्वाद देते हैं। मुनि, आर्यिकाएँ, क्षुल्लक-क्षुल्लिकाएं ये सभी सामान्य जैन को सद्धर्मवृद्धिरस्तु आशीर्वाद देते हैं। विधर्मियों को ‘धर्मलाभोऽस्तु’ आशीर्वाद देते हैं और पामर, चांडाल, हिंस्र आदिवासी आदि को नमस्कार करने पर ‘पापं क्षयोऽस्तु’ आशीर्वाद देते हैं। ब्रह्मचारी-ब्रह्मचारिणी को श्रावक ‘वंदना’ कहकर हाथ जोड़कर नमस्कार करते हैं। बदले में वे ‘दर्शन- विशुद्धि’ कहकर आशीर्वाद देते हैं।
यही शास्त्रों की और संघों की परम्परा है।
देववंदना-मुनि-आर्यिकाएँ आदि त्रिकाल सामायिक में ही उपर्युक्त विधि से चैत्यभक्ति और पंचगुरुभक्ति पढ़कर देववंदना करें। यह देववंदना ही सामायिक है और सामायिक ही देववंदना है। आचारासार, चारित्रसार और अनगारधर्मामृत में इसका अच्छा खुलासा है। जयधवला टीका में भी यही विधि वर्णित है। जिज्ञासुओं को वहाँ से ही देख लेना चाहिए। ऐसे ही प्रात:काल और मध्यान्ह में सामायिक के बाद तथा सायंकाल में प्रतिक्रमण के बाद विधिवत् कृतिकर्मपूर्वक आचार्यदेव की गुरुवंदना करे तथा अन्य समय में भी आचार्य की वंदना करें। उपाध्याय, साधु आदि की तथा अपने से दीक्षा में बड़े मुनियों की भी वंदना करें।
प्रतिक्रमण आवश्यक
कृत, कारित, अनुमोदना से अपने व्रतों में लगे हुए अतिचारों को दूर करना प्रतिक्रमण है। इसके भी नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव ऐसे छह भेद हैं। नाम प्रतिक्रमण-पाप हेतुक नामों से हुए अतिचारों को दूर करना या प्रतिक्रमण के दण्डक सूत्रों का उच्चारण करना नाम प्रतिक्रमण है। स्थापना-सराग प्रतिमाओं से परिणाम का हटाना स्थापना प्रतिक्रमण है। द्रव्य-पापकारक द्रव्यों के सेवन से परिणाम का हटाना द्रव्य प्रतिक्रमण है। क्षेत्र-क्षेत्र के आश्रित हुए अतिचारों से दूर होना क्षेत्र प्रतिक्रमण है। काल-काल के निमित्त से हुए अतिचारोें से दूर होना काल प्रतिक्रमण है। भाव-राग, द्वेष आदि भावों के निमित्त से हुए अतिचारों को दूर करना भाव प्रतिक्रमण है। प्रतिक्रमण के भेद-दैवसिक, रात्रिक, ऐर्यापथिक, पाक्षिक, चातुर्मासिक, सांवत्सरिक और उत्तमार्थ प्रतिक्रमण के ये सात भेद हैं।
(१) दिवस भर के किये हुए दोषों को दूर करने हेतु सूर्यास्त के पूर्व जो प्रतिक्रमण होता है वह दैवसिक है।
(२) रात्रि में हुए अतिचारों को दूर करने के लिए जो सूर्यादय से पूर्व-रात्रि के अंत में प्रतिक्रमण किया जाता है वह रात्रिक है।
(३) चार हाथ आगे देखकर चलते हुए भी जो जीव विराधना आदि दोषों को दूर करने के लिए किया जाता है वह ईर्यापथ प्रतिक्रमण है।
(४) पंद्रह अहोरात्र में जो दोष हुए हैं, उनका शोधन करने के लिए जो प्रत्येक चतुर्दशी या अमावस और पूर्णिमा को जो प्रतिक्रमण किया जाता है वह पाक्षिक है।
(५) चार महीने हो जाने पर जो कार्तिकी शुक्ला चतुर्दशी या पूर्णिमा को तथा फाल्गुन के अंत में जो बड़ा प्रतिक्रमण होता है वह चातुर्मासिक है।
(६) आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी या पूर्णमासी को वर्ष भर में हुए अतिचारों के शोधन हेतु सांवत्सरिक प्रतिक्रमण किया जाता है।
(७) उत्तम अर्थ-सल्लेखना से संबंधित प्रतिक्रमण उत्तमार्थ प्रतिक्रमण है।
इसमें यावज्जीवन चार प्रकार के आहार का त्याग किया जाता है अर्थात् मरण के काल में जो चतुर्विध आहार त्याग कर दीक्षित जीवन भर के दोषों का शोधन किया जाता है वह उत्तमार्थ प्रतिक्रमण है। अनगारधर्मामृत में सात बृहत्प्रतिक्रमण और सात लघु प्रतिक्रमण, ऐसे चौदह प्रतिक्रमण माने हैं।
बृहत्प्रतिक्रमण के नाम-व्रतारोपिणी, पाक्षिक, कार्तिकान्तचातुर्मासिक, फाल्गुनान्न्तचातुर्मासी, आषाढ़ान्तसांवत्सरी, सार्वातिचार और उत्तमार्थ ये सात बृहत्प्रतिक्रमण हैं।
लघु प्रतिक्रमण के नाम-लोच प्रतिक्रमण, रात्रिक, दैवसिक, गोचारप्रतिक्रमण, निषेधिकागमन प्रतिक्रमण, ईर्यापथप्रतिक्रमण और अतिचार प्रतिक्रमण ये सात लघु प्रतिक्रमण हैं।
तथा पाँच वर्ष में करने योग्य जो प्रतिक्रमण है वह ‘युगप्रतिक्रमण१’ है। ये सर्व प्रतिक्रमण के भेद उपर्युक्त सात में ही गर्भित हो जाते हैं। इस प्रतिक्रमण के विषय में प्रतिक्रामक, प्रतिक्रमण और प्रतिक्रमितव्य-प्रतिक्रमण करने योग्य वस्तु इन तीनों को जानना आवश्यक है। जो साधु अपने किये हुए दोषों को अपने से हटाते हैं, वे प्रतिक्रामक हैं। महाव्रत आदि में लगे हुए अतिचारों से विरति अथवा व्रत शुद्धि निमित्त अक्षरों का समूह प्रतिक्रमण है। मिथ्यात्व, असंयम और कषाय आदि अतिचाररूप द्रव्य त्याग करने योग्य हैं, इन्हें ही प्रतिक्रमितव्य कहते हैं। जिन द्रव्यों से, जिन क्षेत्रों से, जिन कालों में और जिन भावों से अपने व्रतों में दोष लगता है, वे छोड़ने योग्य हैं।
प्रतिक्रमण के दो भेद भी माने हैं-द्रव्य प्रतिक्रमण और भाव प्रतिक्रमण। मिथ्यात्व, असंयम, कषाय और अप्रशस्त योग का प्रतिक्रमण भाव प्रतिक्रमण है और प्रतिक्रमण पाठ के दण्डक सूत्रों का उच्चारण द्रव्य प्रतिक्रमण है। यह प्रतिक्रमण आलोचनापूर्वक ही होता है अत: यहाँ पर आलोचना भी सात प्रकार की होती है-दैवसिक, रात्रिक, ऐर्यापथिक, पाक्षिक, चातुर्मासिक, सांवत्सरिक और उत्तमार्थ। गुरु के पास अपने अपराध का निवेदन करना अथवा गुरु के अभाव में अर्हंत भगवान की प्रतिमा के समक्ष अपने दोषों को प्रगट करना यह आलोचना है। गुरु के सामने चारित्राचारपूर्वक दोषों की आलोचना कर देने पर सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्र की शुद्धिरूप आराधना सिद्ध होती है तथा दोषों की आलोचना न करने से आराधना की सिद्धि होनी कठिन है।
किनके लिए प्रतिक्रमण करना आवश्यक ही है ?
प्रथम तीर्थंकर वृषभदेव और अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी इन दोनों का धर्म प्रतिक्रमण सहित है। अपराध हों अथवा न हों किन्तु इनके तीर्थ में रहने वाले साधुओं को प्रतिक्रमण करना ही चाहिए किन्तु अजितनाथ से लेकर पाश्र्वनाथ पर्यंत मध्य के बाईस तीर्थंकरों का धर्म अपराध के होने पर ही प्रतिक्रमण करने रूप है क्योंकि उनके शिष्यों में अपराध की बहुलता नहीं होती है। तात्पर्य यही है कि भगवान आदिनाथ और भगवान महावीर स्वामी के तीर्थ में रहने वाले मुनि-आर्यिकाएं चाहें उनसे अपराध हो या न हो फिर भी वे यथासमय दैवसिक आदि प्रतिक्रमण के काल में पूरा प्रतिक्रमण पाठ पढ़ते हुए सर्व दण्डकसूत्रों का उच्चारण करें ही करें तथा शेष बाईस तीर्थंकरों के शासन में रहने वाले साधुओं से जो अपराध होवे, उसका ही प्रतिक्रमण करें, इन सातों प्रतिक्रमणों को समय-समय पर करना जरूरी नहीं है। ऐसा क्यों ? प्रश्न होने पर उत्तर देते हैं-
मज्झिमया दिढबुद्धी एयग्गमणा अमोहलक्खा य।
तम्हा हु जमाचरंति तं गरहंता वि सुज्झंति।।६३१।।
पुरिमचरिमादु जम्हा चलचित्ता चेव मोहलक्खा य।
तो सव्वपडिक्कमणं अंधलयघोडय दिट्ठंतो।।६३२।।
मध्य तीर्थंकरों के शिष्य दृढ़बुद्धि वाले, एकाग्रमन सहित और मूढ़ मन रहित होते हैं इसलिए जिस दोष को लगाते हैं उसकी गर्हा-प्रतिक्रमण करके ही शुद्ध हो जाते हैं, किन्तु प्रथम और चरम तीर्थंकर के शिष्य चंचलचित्त होते हैं तथा मूढ़चित्त वाले होते हैं-उनको बहुत बार शास्त्रों का प्रतिपादन करने पर भी नहीं समझते हैं अर्थात् प्रथम तीर्थंकर के शासन के शिष्यों में अति सरलता और अति जड़ता रहती थी और आज अंतिम तीर्थंकर के शासन में शिष्यो में कुटिलता और जड़ता रहती है इसीलिए इन साधुओं के लिए सर्व प्रतिक्रमण के काल में विधिवत् सर्व दण्डकों के पढ़ने का विधान है। इसके लिए अंधे घोड़े का दृष्टांत दिया गया है- किसी राजा का घोड़ा अंधा हो गया, उसने उस घोड़े के लिए वैद्य के पुत्र से औषधि पूछी। वह वैद्यक शास्त्र जानता नहीं था और उसका पिता वैद्य अन्य ग्राम को चला गया था। तब उस वैद्यपुत्र ने घोड़े की आँख के निमित्त सभी औषधियों का प्रयोग कर दिया अर्थात् सभी औषधि उस घोड़े की आँख में लगा दिया। उन औषधियों के प्रयोग से वह घोड़ा स्वस्थ हो गया अर्थात् जो आँख खुलने की औषधि थी उसी में वह भी आ गई। उसके लगते ही घोड़े की आँख खुल गई। वैसे ही साधु भी यदि एक प्रतिक्रमण दण्डक में स्थिरचित्त नहीं होता तो अन्य दण्डक में हो जावेगा अथवा यदि अन्य दण्डक में भी स्थिरमना नहीं होगा तो अन्य किसी दण्डक में स्थिरचित्त हो जावेगा इसलिए सर्व दण्डकों का उच्चारण करना न्याय ही है और इसमें विरोध भी नहीं है क्योंकि प्रतिक्रमण के सभी दण्डक सूत्र कर्मक्षय करने में समर्थ हैं। इस प्रकार यह प्रतिक्रमण नाम की आवश्यक क्रिया मुनियों के लिए कही गई है। व्रतिक श्रावक भी अपने पद के अनुरूप व्रतों में लगे हुए अतिचारों के शोधन के लिए प्रतिक्रमण करते हैं।
प्रत्याख्यान आवश्यक
अतिचार के लिए कारणभूत ऐसे सचित्त, अचित्त एवं मिश्र द्रव्यों का त्याग करना तथा तप के लिए प्रासुक-भक्ष्य द्रव्यों का भी त्याग करना ‘प्रत्याख्यान’ है। इसके भी नाम स्थापना आदि से छह भेद हैं- नाम प्रत्याख्यान-अयोग्य नाम पाप के हेतु हैं और विरोध के कारण हैं। ऐसे नामों का न रखना, न रखवाना, न रखते हुए की अनुमोदना करना। यह नाम प्रत्याख्यान है। स्थापना-अयोग्य स्थापनारूप मूर्तियाँ पाप बंध के लिए कारण हैं, मिथ्यात्व आदि की प्रवर्तक हैं तथा जो काल्पनिक रूप देवता आदि के प्रतिबिम्ब हैं वे भी पाप के कारण हैं ऐसी अयोग्य स्थापना रूप- प्रतिबिम्बों को न करना, न कराना न अनुमति देना स्थापना प्रत्याख्यान है। द्रव्य-पापबंध के कारणभूत सदोष द्रव्य कन्दमूल आदि हैं तथा तप के निमित्त से त्यागे गये जो निर्दोष द्रव्य-नमक, घी आदि हैं इनको ग्रहण न करना, न त्यागी वस्तु को ग्रहण कराना, न अनुमति देना यह द्रव्य प्रत्याख्यान है। क्षेत्र-असंयम आदि के कारणभूत ऐसे क्षेत्र को छोड़ देना, क्षेत्र प्रत्याख्यान है। काल-जिस काल में असंयम आदि होते हैं, उसको छोड़ देना काल प्रत्याख्यान है। भाव-मिथ्यात्व, असंयम, कषाय आदि भावों का त्याग करना भाव प्रत्याख्यान है। प्रश्न-प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान में क्या अंतर है ? उत्तर-अतीत काल में लगे हुए दोषों का शोधन करना प्रतिक्रमण है और अतीत, अनागत तथा वर्तमान इन तीनों काल के अतिचारों का त्याग करना प्रत्याख्यान है अथवा व्रत आदि के अतिचारों का शोधन करना प्रतिक्रमण है और सचित्त आदि वस्तु का तथा तप के लिए योग्य भी वस्तु का त्याग करना प्रत्याख्यान है। जब मुनि-आर्यिका आदि संयमी साधु-साध्वी आहार के लिए जाते हैं वहाँ नवधाभक्ति के बाद पूर्व में जो चतुर्विध आहार का त्याग था, उसका निष्ठापन करके आहार ग्रहण कर लेते हैं। पुन: मुखशुद्धि के बाद वहीं पर तत्क्षण ही आगे आहार न लेने तक सिद्धभक्तिपूर्वक विधिवत् चतुर्विध आहार का त्याग कर देते हैं। अनंतर गुरु के पास आकर अथवा गुरु के अभाव में भगवान् के पास आकर लघु सिद्ध भक्ति, लघु योग भक्ति पढ़कर अगले दिन आहार ग्रहण के पूर्व तक चतुर्विध आहार का त्याग ले लेते हैं। फिर गुरुभक्तिपूर्वक गुरुवंदना करते हैं। यह प्रतिदिन के प्रत्याख्यान आवश्यक की विधि है। इसके प्रत्याख्यायक, प्रत्याख्यान और प्रत्याख्यातव्य ये तीनों ही जानने योग्य हैं। संयम से सहित मुनि प्रत्याख्यान करने वाले होने से प्रत्याख्यायक हैं।
त्यागरूप परिणाम प्रत्याख्यान है।
सदोष हों या निर्दोष, सचित्त, अचित्त और मिश्र ये तीन प्रकार के द्रव्य प्रत्याख्यान करने-त्यागने योग्य पदार्थ हैं इन्हें ही प्रत्याख्यातव्य कहते हैं। जैन साधु के मूलगुण २८ होते हैं और उत्तरगुण ३४। बाईस परीषहजय और बारह प्रकार के तप ही उत्तरगुण कहलाते हैं। इन उत्तर गुणों में अनेक प्रकार के सिंहनिष्क्रीडित, आचाम्ल, कवलचांद्रायण आदि व्रत, उपवास जो भी हैं वे सब प्रत्याख्यान कहलाते हैं। सो यह भी उपवास आदि रूप प्रत्याख्यान यहाँ मूलाचार में दश भेद रूप माना गया है-अनागत, अतिक्रांत, कोटिसहित, निखंडित, साकार, अनाकार, परिणामगत, अपरिशेष, अध्वानगत और सहेतुक।
(१) भविष्यतकाल के किए जाने वाले उपवास आदि पहले कर लेना, जैसे चतुर्दशी आदि में जो उपवास करना था उसको त्रयोदशी आदि में कर लेना अनागत प्रत्याख्यान है।
(२) अतीतकाल के किए जाने वाले उपवास आदि को आगे करना अतिक्रान्त प्रत्याख्यान है। जैसे-चतुर्दशी आदि में जो उपवास आदि करना है, उसे प्रतिपदा आदि में करना।
(३) शक्ति आदि की उपेक्षा से संकल्प सहित उपवास करना कोटिसहित प्रत्याख्यान है। जैसे-कल प्रात: स्वाध्याय बेला के अनन्तर यदि शक्ति रहेगी तो उपवास आदि करूँगा, यदि शक्ति नहीं रही तो नहीं करूँगा। इस प्रकार से जो संकल्प करके प्रत्याख्यान होता है, वह कोटिसहित है।
(४) पाक्षिक आदि में अवश्य किये जाने वाले उपवास का करना निखण्डित प्रत्याख्यान है।
(५) भेद सहित उपवास करने वाले को साकार प्रत्याख्यान कहते हैं। जैसे-सर्वतोभद्र, कनकावली आदि व्रतों की विधि से उपवास करना, रोहिणी आदि नक्षत्रों के भेद से उपवास करना।
(६) स्वेच्छा से उपवास करना, जैसे-नक्षत्र या तिथि आदि की अपेक्षा के बिना ही स्वरुचि से कभी भी उपवास कर लेना अनाकार प्रत्याख्यान है।
(७) प्रमाण सहित उपवास को परिणामगत कहते हैं। जैसे-बेला-तेला, चार उपवास, पाँच उपवास, सात दिन, पन्द्रह दिन, एक मास आदि काल के प्रमाण से उपवास आदि करना परिमाणगत प्रत्याख्यान है।
(८) जीवन पर्यंत के लिए चार प्रकार के आहार आदि का त्याग करना अपरिशेष प्रत्याख्यान है।
(९) मार्गविषयक प्रत्याख्यान अध्वानगत है। जैसे-जंगल, नदी आदि से निकलने के प्रसंग में उपवास आदि करना अर्थात् इस वन से बाहर पहुँचने तक मेरे चतुर्विध आहार का त्याग है या इस नदी से पार होने तक चतुर्विध आहार का त्याग है। ऐसा उपवास करना सो अध्वानगत प्रत्याख्यान है।
(१०) हेतु सहित उपवास सहेतुक है।
यथा- उपसर्ग आदि के निमित्त से उपवास आदि करना सहेतुक नाम का प्रत्याख्यान है।
जिस प्रत्याख्यान में विनय के साथ, अनुभाषा के साथ, प्रतिपालन के साथ और परिणाम शुद्धि के साथ आहार आदि का त्याग होता है वह प्रत्याख्यान इन चार भेद से भी कहा गया है-
(१) कृतिकर्म, औपचारिक विनय तथा दर्शन, ज्ञान और चारित्र में विनय, जो इन पाँच विध विनय से युक्त है, वह विनय शुद्ध प्रत्याख्यान है।
(२) गुरु के वचन के अनुरूप वचन बोलना, अक्षर पद, व्यंजन क्रम से विशुद्ध उच्चारण करना तथा घोष-ह्रस्व, दीर्घ आदि वर्णों का यथायोग्य उच्चारण करना, इस प्रकार जो प्रत्याख्यान है वह अनुभाषण शुद्ध प्रत्याख्यान है।
(३) आकस्मिक व्याधि, उपसर्ग, श्रम, आहार का अलाभ-अंतराय आदि और गहन वन प्रवेश आदि के समय जो चतुर्विध आहार का त्याग किया हो, उसको भंग न करना अनुपालना शुद्ध है अर्थात् सहसा कोई व्याधि, वेदना उठ गई या तिर्यंच आदि द्वारा उपसर्ग हो गया या अधिक श्रमादि से मरणासन्न स्थिति आ गई या निर्जनवन में मार्ग भूल गये, इत्यादि प्रसंगों पर ऐसा प्रत्याख्यान करना चाहिए कि इस कष्ट से छूटने तक मेरे चतुर्विध आहार का त्याग है, इसको पूरा निभाना अनुपालना शुद्ध प्रत्याख्यान है।
(४) राग-द्वेष आदि परिणामों से जो दूषित नहीं हो अर्थात् सम्यग्दर्शन आदि युक्त, कांक्षा रहित, वीतराग, समभावयुक्त और अहिंसादि व्रतों से सहित शुद्ध भाव वाले मुनियों का प्रत्याख्यान परिणाम शुद्ध प्रत्याख्यान है।
आहार के चार भेद कौन से हैं ?
क्षुधा-भूख को शांत करने वाला भोजन-रोटी, पूड़ी, भात, दाल आदि अशन पदार्थ ‘अशन’ हैं। प्राणों पर अनुग्रह करने वाले पदार्थ-ठंडाई, दूध, रस, जल आदि ‘पान’ है। जो खाया जाये वह ‘खाद्य’-लड्डू आदि वस्तुएँ एवं जिसका स्वाद लिया जाये, वे ‘स्वाद्य’-इलायची आदि पदार्थ स्वाद्य हैं। गृहस्थाश्रम में रहते हुए श्रावक-श्राविकाएँ भी प्रत्याख्यान करते हैं। रात्रि में चतुर्विध आहार का त्याग करना बहुत बड़ा प्रत्याख्यान है। इसमें एक वर्ष मेें छह महीने के उपवास का फल मिल जाता है। यदि चारों विध का त्याग न कर सके तो कम से औषधि, दुग्ध आदि के सिवाय अन्न आदि पदार्थ रात्रि में छोड़ देना चाहिए। प्याज, लहसुन आदि अभक्ष्य वस्तुएँ, चलितरस-जिन पर फफूदी आदि लग गई हैं ऐसे पदार्थ भी छोड़ देने चाहिए। घर में शुद्ध, सात्विक भोजन बनाकर खाना चाहिए। व्रतोें में सोलहकारण, दशलक्षण, आष्टान्हिक आदि पर्वों में व अष्टमी, चतुर्दशी आदि पर्वों में उपवास अथवा एक बार भोजन आदि से व्रत किये जाते हैं। शास्त्रों में रोहिणी, जिनगुणसंपत्ति, रविवार आदि बहुत से व्रत प्रचलित हैं, ये सब तप हैं, इनसे इस लोक में सुख, संपत्ति, संतति आदि प्राप्त होती हैं और परलोक में स्वर्ग के सुख प्राप्त कर परम्परा से मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाती है। यदि गृहस्थ सोते समय इतना भी नियम कर लेता है कि ‘निद्रा में रहने तक मेरे चतुर्विध आहार का त्याग है तो भी उसका यह त्याग प्रत्याख्यान कहलाता है। कदाचित् वह निद्रा में ही सर्प के काटने से या किसी छत आदि के गिर जाने से मर गया तो उत्तम-देवगति प्राप्त कर सकता है इसलिए प्रतिदिन और प्रतिक्षण कुछ न कुछ त्याग अवश्य करते रहना चाहिए। यह परलोक सिद्धि के लिए बहुत ही लाभप्रद है।
कायोत्सर्ग आवश्यक
काय-शरीर का त्याग करना अर्थात् शरीर से ममत्व छोड़ कर महामंत्र का चिंतवन करना ‘कायोत्सर्ग’ है।
इसके भी नाम आदि की अपेक्षा छह भेद हैं-
(१) तीक्ष्ण, कठोर आदि पापयुक्त नाम के द्वारा उत्पन्न हुए अतिचारों का शोधन करने के लिए जो कायोत्सर्ग किया जाता है, वह नाम कायोत्सर्ग है।
(२) अशुभ या सरागमूर्ति की स्थापना द्वारा हुए अतिचारों के शोधन हेतु कायोत्सर्ग करना स्थापना कायोत्सर्ग है।
(३) सदोष द्रव्य के सेवन से उत्पन्न हुए अतिचारों को दूर करने के लिए जो कायोत्सर्ग होता है, वह द्रव्य कायोत्सर्ग है।
(४) सदोष क्षेत्र से होने वाले अतिचारों को नष्ट करने के लिए जो कायोत्सर्ग हो, वह क्षेत्र कायोत्सर्ग है।
(५) सदोष काल के आश्रय से हुए दोषों का परिहार करने के लिए जो कायोत्सर्ग किया जाए, वह काल कायोत्सर्ग है।
(६) मिथ्यात्व आदि अतिचारों के शोधन के लिए किया गया कायोत्सर्ग भाव कायोत्सर्ग है।
कायोत्सर्ग, कायोत्सर्गी और कायोत्सर्ग के कारण इन तीनों को जानना जरूरी है।
(१) चार अंगुल के अंतर से समपाद रूप, दोनों भुजाओं को लटका कर, सर्वांग के हलन-चलन से रहित जिनमुद्रा से धर्मध्यान या शुक्लध्यान में लीन हो जाना या बैठकर पद्मासन मुद्रा से-योगमुद्रा से ध्यान करना यह कायोत्सर्ग है।
(२) मोक्ष का इच्छुक, भव्य, निद्राविजयी, जिनागम के ज्ञान में निपुण, चारित्रधारी मुनि, देशव्रती श्रावक या असंयत सम्यग्दृष्टी श्रावक, विशुद्ध परिणामी ही कायोत्सर्ग करते हैं अत: ये ही कायोत्सर्गी कहलाते हैं।
(३) राग, द्वेष कषाय आदि से हुए अतिचारों को दूर करने के लिए कायोत्सर्ग किया जाता है अथवा देव, मनुष्य या तिर्यंच आदि के द्वारा उपसर्ग के आ जाने पर भी कायोत्सर्ग किया जाता है या कायोत्सर्ग में स्थित हों और उपसर्ग आदि आ जावे तो उन्हें सहन करना चाहिए।
कायोत्सर्ग का फल-कायोत्सर्ग का उत्कृष्ट काल एक वर्ष पर्यंत है, अंतर्मुहूर्त का काल जघन्य है और अंतर्मुहूर्त से एक समय अधिक लेकर एक वर्ष में एक समय कम शेष जितना भी काल है, वह सब मध्यम है, इसके अनेक भेद हो जाते हैं। कायोत्सर्ग में उच्छ्वासों की गणना-अप्रमत्त साधु और वीरभक्ति में दैवसिक के १०८, रात्रिक के ५४, पाक्षिक के ३००, चातुर्मासिक प्रतिक्रमण में ४०० और वार्षिक प्रतिक्रमण में ५०० उच्छ्वासों में कायोत्सर्ग करें।
तात्पर्य यह है कि दैवसिक प्रतिक्रमण पाठ में चार भक्तियाँ होती हैं-सिद्धभक्ति, प्रतिक्रमणभक्ति, वीरभक्ति और चौबीस तीर्थंकर भक्ति। इनमें से तीन भक्ति के कायोत्सर्ग २७ उच्छ्वासों में होते हैं तथा वीर भक्ति का कायोत्सर्ग १०८ उच्छ्वासों में होता है। इसमें ३६ बार महामंत्र का उच्चारण किया जाता है। उच्छ्वास की गणना कैसे लेना ? एक बार णमोकार मंत्र के जप में तीन उच्छ्वास होते हैं, यथा ‘णमो अरिहंताणं’ श्वांस ऊपर खींचना और ‘णमो सिद्धाणं’ बोलकर श्वांस नीचे छोड़ना, यह एक श्वासोच्छ्वास हुआ। ऐसे ही ‘णमो आइरियाणं’ ‘णमो उवज्झायाणं’ इन दो पदों में एक श्वासोच्छ्वास तथा ‘णमो लोए’ पद व ‘सव्व साहूणं’ पद इनके उच्चारण में एक श्वासोच्छ्वास ये तीन श्वासोच्छ्वास हुए। इस तरह नौ बार णमोकार मंत्र के जपने से २७ श्वासोच्छ्वास, अठारह बार णमोकार मंत्र के जपने से ५४ एवं ३६ बार जाप से १०८ श्वासोच्छ्वास हो जाते हैं। अन्य क्रियाओं में उच्छ्वासों की गणना-गोचार प्रतिक्रमण में, एक गाँव से दूसरे गाँव जाने पर, जिनेन्द्र देव की निर्वाणभूमि आदि कल्याणक स्थानों की वंदना के समय, मुनियों के निषद्या स्थान की वंदना में, मल-मूत्र विसर्जन के बाद २५ उच्छ्वास में कायोत्सर्ग करना चाहिए। गं्रथ के प्रारंभ में, समाप्ति में, स्वाध्याय में, देववंदना-गुरु वंदना में और अशुभ परिणाम से हुए दोषों के शोधन में २७ उच्छ्वासों में कायोत्सर्ग करना चाहिए। कायोेत्सर्ग काल में चिंतन-कायोत्सर्ग करते समय साधु यदि ईर्यापथ दोष विशोधन हेतु कायोत्सर्ग कर रहे हैं तो चलने की क्रिया से हुए दोषों के विनाश का चिंतवन करके पुन: महामंत्र के अर्थ का स्मरण करते हुए धर्मध्यान और शुक्लध्यान का चिंतवन करें। कायोत्सर्ग का प्रत्यक्ष फल-कायोत्सर्ग में हलन-चलन रहित शरीर की मुद्रा स्थिर होने से जैसे शरीर के अवयव भिद जाते हैं वैसे ही कायोत्सर्ग के द्वारा कर्मधूलि भी आत्मा से पृथक् हो जाती है। कायोत्सर्ग के दोष-इस कायोत्सर्ग के भी घोटक, लता, स्तंभ, कुड्य आदि ३२ दोष माने हैं। उन दोषों से रहित स्थिर योगमुद्रा या जिनमुद्रा से स्थित होकर कायोत्सर्ग करना चाहिए। इन दोषों के लक्षण मूलाचार, अनगार धर्मामृत आदि से देख लेना चाहिए।
कायोत्सर्ग के चार भेद- उत्थितोत्थित, उत्थितनिविष्ट, उपविष्टोत्थित और उपविष्टनिविष्ट, ये चार भेद कायोत्सर्ग के होते हैं।
(१) उत्थितोत्थित- दोनों प्रकार से खड़े होकर जो कायोत्सर्ग होता है अथवा जिसमें शरीर से भी अचल खड़े हैं और परिणाम से भी खड़े हैं, धर्मध्यान या शुक्लध्यान कर रहे हैं, वह कायोत्सर्ग प्रथम भेदरूप है। यह महान से भी महान सर्वश्रेष्ठ है।
(२) उत्थितनिविष्ट- जो शरीर से तो खड़े हैं फिर भी भावों से निविष्ट-बैठे हैं अर्थात् आर्तध्यान या रौद्रध्यान में उपयोग जा रहा है उस समय वह कायोत्सर्ग उत्थितनिविष्ट कहलाता है।
(३) उपविष्टोत्थित- जो शरीर से तो बैठे हुए हैं किन्तु भावों से खड़े हैं अर्थात् बैठकर भी धर्मध्यान या शुक्लध्यान का चिंतन कर रहे हैं, उनका यह कायोत्सर्ग उपविष्टोत्थित होता है।
(४) जो शरीर से भी बैठे हुए हैं और भावों से भी, उनका वह कायोत्सर्ग उपविष्टनिविष्ट कहलाता है। इन चारों प्रकार के कायोत्सर्गों में पहला और तीसरा भेद ही ग्राह्य है-उत्तम है, कर्मनिर्जरा का कारण है और दूसरा तथा चौथा भेदरूप कायोत्सर्ग अग्राह्य-त्यागने योग्य एवं कर्मबंध का कारण है।
शुभ मन:संकल्प-दर्शन, ज्ञान और चारित्र में जो मन का लगाना है, वह शुभ मन:संकल्प है। ऐसे ही संयम, प्रत्याख्यान आदि क्रियाएँ, धर्मध्यान आदि परिणाम, समिति, विद्या, व्रताचरण, समाधि, ब्रह्मचर्य, क्षमा, आर्जव आदि भाव, विनय, श्रद्धान आदि में मन का उपयोग जाना सो यह सब प्रशस्त और विश्वस्त संकल्प है, यह सब जिनशासन में सम्मत है। अशुभ मन:संकल्प-परिवार, ऋद्धि, सत्कार, पूजा, भोजन-पान, शयन, आसन आदि के लिए मन का उपयोग चला जाना यह सब अप्रशस्त मन का संकल्प कायोत्सर्ग के समय छोड़ने योग्य है। इस प्रकार यहाँ संयम, तप और ऋद्धि के इच्छुक निग्र्रंथ महार्षियों के लिए यह कायोत्सर्ग आवश्यक कहा गया है। पूर्व काल में श्रावक भी अष्टमी-चतुर्दशी आदि पर्वों में श्मशाम भूमि या निर्जन वन में जाकर दिगम्बर होकर रात्रि में प्रतिमायोग में खड़े होकर कायोत्सर्ग किया करते थे। इसके लिए सेठ सुदर्शन, श्रेणिकपुत्र वारिषेण आदि श्रावकों के उदाहरण प्रसिद्ध हैं। आज भी श्रावक-श्राविकाएं मंदिर में, घर में या तीर्थों पर जो निश्चल आसन से बैठकर महामंत्र का जाप्य करते हैं, वह इस कायोत्सर्ग में सम्मिलित है।
णमोकार मंत्र के जप करने के तीन प्रकार माने गये हैं-मानसिक, उपांशु और वाचनिक। वाचनिक जाप्य में शब्दों का उच्चारण स्पष्ट होता है। उपांशु जाप्य में शब्द भीतर ही भीतर वंâठस्थान में गूंजते रहते हैं तथ मानसिक जाप्य में बाहर और भीतर दोनों तरह से शब्दोच्चारण का प्रयास रुक जाता है। हृदय में ही मंत्राक्षरों का चिंतवन चलता रहता है। यही क्रिया ध्यान का रूप धारण कर लेती है। पुण्यफल-वाचनिक जाप्य से सौगुणा अधिक पुण्य उपांशु जाप से होता है और उससे हजार गुणा अधिक पुण्य मानस जाप से होता है। इस प्रकार यह कायोत्सर्ग आवश्यक पूर्णरूप से मुनियों में ही होता है फिर भी श्रावकों को भी इसका अभ्यास करते रहना चाहिए। जो मुनि इन आवश्यकों को यथासमय करते हैं, उनमें हानि नहीं करते हैं, उनके ‘आवश्यक अपरिहाणि’ नाम की भावना भी हो जाती है।
सव्वावासणिजुत्तो णियमा सिद्धोत्ति होइ णायव्वो।
यह णिस्सेसं कुणदि ण णियमा आवासया होंति।।६८६।।
सर्व आवश्यकों से परिपूर्ण हुए मुनि नियम से सिद्ध हो जाते हैं और जो इन्हें परिपूर्ण नहीं कर पाते हैं वे नियम से स्वर्गादि में निवास करते हैं।
आसिका और निषीधिका का लक्षण-
जो होदि णिसीदप्पा णिसीहिया तस्स भावदो होदि।
अणिसिद्धस्स णिसीहियसद्दो हवदि केवलं तस्स।।६८९।।
जो नियमित आत्मा हैं उनके भाव से निषिधिका होती है और जो अनियंत्रित हैं उनके निषीधिका शब्द मात्र है।
आसाए विप्पमुकस्स आसिया होदि भावदो।
आसाए अविप्पमुक्कस्स सद्दो हवदि केवलं।।६९०।।
जो आशा से रहित हैं उनके भाव से आसिका होती है और जो आशा से सहित हैं उनके शब्द मात्र होती है। इसी मूलाचार में चतुर्थ अध्याय में कहा है-
‘‘णिग्गमणे आसिया भणिया। पविसंते य णिसीही।
णिग्गमणे-निर्गमनकाले।
आसिया-आसिका देवगृहस्थादीन् परिपृच्छय
यानं पापक्रियादिभ्यो मनो निर्वर्तनं वा।
भणिया-भणिता: कथिता:।
पविसंते य-प्रविशति च प्रवेशकाले,
णिसिही-निषेधिका तत्रस्थानभ्युपगम्य
स्थानकरणं सम्यग्दर्शनादिषु स्थिरभावो वा।’’
वसति से निकलकर गमन करते समय देव, गृहस्थ आदि को पूछकर निकलना अथवा पाप क्रिया आदि से मन को दूर करना यह ‘आसिका’ क्रिया है। प्रवेश के समय वहाँ के देवता, गृहस्थ आदि को पूछकर नि:सही शब्द का प्रयोग कर उनकी स्वीकृति लेकर वहाँ रहना यह ‘निषेधिका’ क्रिया है। इस आवश्यक अधिकार में सर्वप्रथम पाँच परमेष्ठी का स्वरूप बताया है और उन्हें नमस्कार किया है पश्चात् छह आवश्यक क्रियाओं को कहकर आसिका, निषीधिका का वर्णन किया है। ये तेरह प्रकार की क्रियाएँ या करण कहलाती हैं अर्थात् पाँच परमेष्ठी को नमस्काररूप से पाँच, छह आवश्यक क्रियारूप से छह और असही, निसही ये तेरह क्रियाएँ साधुओं को अहर्निश करनी होती हैं।
(२)द्वादश अनुप्रेक्षा अधिकार
अद्धुवमसरणमेगत्तमण्णसंसारलोगमसुचित्तं।
आसवसंवरणिज्जरधम्मं बोधिं च चिंतेज्जो।।६९४।।
अध्रुव, अशरण, एकत्व, अन्यत्व, संसार, लोक, अशुचित्व या अशुभत्व, आस्रव, संवर, निर्जरा, धर्म और बोधिदुर्लभ ये द्वादश अनुप्रेक्षा हैं। इनका चिंतवन करना चाहिए।
अध्रुव अनुप्रेक्षा- सामग्गिंदियरूवं मदिजोवणजीविय बलं तेजं।
गिहसयणासणभंडादिया अणिच्चेति चिंतेज्जो।।६९६।।
सामग्री-राज्य आदि, इन्द्रियाँ, रूप, मति, यौवन, जीवन, बल, तेज, गृह, शयन, आसन और भांड-वस्त्र, कार्पास आदि सर्व पदार्थ अनित्य हैं, ऐसा चिंतवन करना चाहिए।
अशरण अनुप्रेक्षा- मरणभयह्मि उवगदे देवा वि सइंदया ण तारंति।
धम्मो त्ताणं सरणं गदित्ति चिंतेहि सरणत्तं।।६९९।।
मरण का भय प्राप्त होने पर इंद्र सहित सुर और असुर भी रक्षा नहीं कर सकते हैं। जिनेन्द्र द्वारा कथित एक धर्म ही रक्षक है, शरण है और गति है-उसी का आश्रय लेने से उत्तम गति है। इस प्रकार अशरण अनुप्रेक्षा का चिंतवन करना चाहिए।
एकत्व अनुप्रेक्षा- एक्को करेइ कम्मं एक्को हिंडदि य दीहसंसारे।
एक्को जायदि मरदि य एवं चिंतेहि एयत्तं।।७०१।।
यह जीव अकेला ही शुभ-अशुभ कर्म करता है, अकेला ही इस दीर्घ संसार में भ्रमण करता है, अकेला ही जन्म धारण करता है और अकेला ही मरण करता है, ऐसी एकत्व भावना का चिंतवन करो।
अन्यत्व अनुप्रेक्षा- अण्णं इमं सरीरादिगं पि जं होज्ज बाहिरं दव्वं।
णाणं दंसणमादात्ति एवं चिंत्तेहि अण्णत्तं।।७०४।।
यह शरीर, इंद्रियां और मन आदि भी जब मेरे से अन्य-भिन्न हैं, तो पुन: जो बाह्य द्रव्य-घर, पुत्र, धन आदि हैं, वे तो अन्य हैं ही किन्तु ज्ञान-दर्शन ही अपने आत्मा के हैं, वे भिन्न नहीं हैं, ऐसा अन्यत्व भाव का चिंतवन करो।
संसार अनुप्रेक्षा-
मिच्छत्तेणाछण्णो मग्गं जिणदेसिदं अपेक्खंतो।
भमिहदि भीमकुडिल्ले जीवो संसारवंâतारे।।७०५।।
मिथ्यात्वरूप अंधकार से व्याप्त हुआ यह जीव जिनेन्द्रदेव द्वारा उपदिष्ट मार्ग को नहीं देख पाता है अत: अत्यन्त भयंकर इस संसाररूपी वन में भ्रमण कर रहा है।
एवं बहुप्पयारं संसारं विविहदुक्खथिरसारं।
णाऊण विचिंतिज्जो तहेव लहुमेव णिस्सारं।।७१२।।
इस प्रकार यह संसार नाना प्रकार का है और अनेक प्रकार के दु:ख ही इसमे स्थिर हैं, ऐसा यह संसार है उसको जानकर इस संसार के नि:सार स्वरूप का शीघ्र ही विचार करना चाहिए।
लोक अनुप्रेक्षा- लोओ अकिट्टिमो खलु अणाइणिहणो सहावणिप्पण्णो।
जीवाजीवेहिं भुडो णिच्चो तालरुक्खसंठाणो।।७१४।।
यह लोक अकृत्रिम है, अनादि अनिधन है, स्वभाव से बना हुआ है, जीव-अजीव द्रव्यों से परिपूर्ण-भरा हुआ है, नित्य है और तालवृक्ष के समान आकार वाला है अर्थात् पुरुषाकार है।
णाऊण लोगसारं णिस्सारं दीहगमणसंसारं।
लोगग्गसिहरवासं झाहि पयत्तेण सुहवासं।।७२१।।
लोक का सार नि:सार है, यह संसार दीर्घ गमनरूप अनंत अपार है, इसमें लोक के अग्रभाग पर निवास करना ही सुखवास है, ऐसा चिंतवन करो।
अशुभ अनुप्रेक्षा-
मोत्तूण जिणक्खादं धम्मं सुहमिह दु णत्थि लोगम्मि।
ससुरासुरेसु तिरिएसु णिरयमणुएसु चिंतेज्जो।।७२८।।
सुर-असुरों में, तिर्यंचों में, नारकी और मनुष्यों में, सर्वत्र इस संसार में जिनेन्द्रदेव द्वारा कथित धर्म को छोड़कर और कुछ भी शुभ नहंीं है। मात्र एक धर्म ही शुभ है ऐसा चिंतवन करना अशुभ अनुप्रेक्षा है अथवा शरीर के अशुचिपने का विचार करना अशुचित्व अनुप्रेक्षा है।
आस्रवानुप्रेक्षा- दु:खभयमीणपउरे संसारमहण्णवे परमघोरे।
जंतू जं तु णिमज्जदि कम्मासवहेदुयं सव्वं।।७२९।।
जिसमें दु:ख और भय को करने वाले बहुत से मत्स्य-मीन भरे हुए हैं, जो बहुत ही भयंकर-घोर है, ऐसे संसाररूपी महासमुद्र में यह जीव डूब रहा है, उसमें कर्मों का आस्रव ही कारण है।
संवर अनुप्रेक्षा- तम्हा कम्मासवकारणाणि सव्वाणि ताणि रुधेज्जो।
इंदियकसायसण्णागारवरागादिआदीणि ।।७४०।।
इसलिए इंद्रिय, कषाय, संज्ञा, गारव और राग आदि, इन सर्व कर्मों के आस्रव के कारणों को रोकना चाहिए, यही संवर है।
संवरफलं तु णिव्वाणमेत्ति संवरसमाधिसंजुत्तो।
णिच्चुज्जुत्तो भावय संवर इणमो विसुद्धप्पा।।७४५।।
संवर का फल निर्वाण है, ऐसा जानकर नित्य ही उद्यमशील, विशुद्ध आत्मा संवर और समाधि से संयुक्त होता है। इस प्रकार संवर भावना को भाओ।
निर्जरा अनुप्रेक्षा- रुद्धासवस्स एवं तवसा जुत्तस्स णिज्जरा होदि।
दुविहा य सा वि भणिया देसादो सव्वदो चेव।।७४६।।
जिन्होंने आस्रव के कारणों को रोककर संवर किया है, तपश्चरण से युक्त ऐसे मुनि के कर्मों की निर्जरा होती है। उसके दो भेद हैं-कर्मैकदेश निर्जरा और सर्वकर्म निर्जरा। एकदेश निर्जरा होते-होते जब सर्वकर्म निर्जरा हो जाती है व मोक्ष हो जाता है, ऐसा चिंतवन करना निर्जरा अनुप्रेक्षा है।
धर्म अनुप्रेक्षा- सव्वजगस्स हिदकरो धम्मो तित्थंकरेहिं अक्खादो।
धण्णा तं पडिवण्णा विसुद्धमणसा जगे मणुया।।७५२।।
उत्तम क्षमादि दशलक्षण धर्म सर्व जगत् का हित करने वाला है, यह धर्म तीर्थंकरों के द्वारा कथित है। इस धर्म को जिन्होंने विशुद्ध चित्त से ग्रहण किया है, वे धन्य हैं, ऐसा चिंतवन करना धर्म अनुप्रेक्षा है।
बोधिदुर्लभ अनुप्रेक्षा-
सेयं भवभयमहणी बोधी गुणवित्थडा मए लद्धा।
जदि पडिदा ण हु सुलहा तम्हा ण खमो पमादो मे।।७६०।।
यह बोधि (रत्नत्रय) भव-संसार के भय को नष्ट करने वाली है, गुणों से विस्तृत है-सर्व गुणों का आधार है, ऐसी बोधि-रत्नत्रय या सम्यग्दर्शन मुझको प्राप्त हो गया है। यदि पुन: यह बोधि मुझसे गिर जायेगी-नष्ट हो जाएगी, तो पुन: इस संसार में सुलभ नहीं है-बहुत ही दुर्लभ है इसलिए मुझे प्रमाद नहीं करना चाहिए। ऐसा चिंतवन करना बोधिदुर्लभ भावना है। यह बारह अनुप्रेक्षाएं वैराग्य की जननी-माता हैं-
दस दो य भावणाओ एवं संखेवदो समुद्दिट्ठा।
जिणवयणे दिट्ठाओ बुहजणवेरग्गजणणीओ।।७६५।।
ये बारह भावनाएँ इस प्रकार यहाँ संक्षेप से कही गई हैं। ये जिनेन्द्रदेव के आगम में विद्वानों के लिए वैराग्य को उत्पन्न करने में माता के समान देखी-मानी गई हैं।
अणुवेक्खाहिं एवं जो अत्ताणं सदा विभावेदि।
सो विगदसव्वकम्मो विमलो विमलालयं लहदि।।७६६।।
इन द्वादश अनुप्रेक्षाओं के द्वारा जो अपनी आत्मा को सदा भावित करता रहता है-आत्मा की भावना करता है, वह विमल आत्मा सर्व कर्मों से छूटकर विमलस्थान-मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। यह बारह भावनाएँ वैराग्य को जन्म देने के लिए माता हैं। तीर्थंकरों ने भी विरक्त होते ही इन बारह भावनाओं का चिंतवन किया है। यहाँ मूलाचार में वैराग्य को प्राप्त दीक्षित हुए मुनियों के लिए मध्य में इनका उपदेश है अत: ये वैराग्य को दृढ़ करने, बढ़ाने व परीषह-उपसर्ग को सहन कराने में समर्थ हैं। संवर के कारणों में श्री उमास्वामी आचार्य ने इन्हें लिया है। यथा-‘‘स गुप्तिसमितिधर्मानुप्रेक्षापरीषहजयचारित्रै:।’’ इस अनुप्रेक्षा अधिकार के बाद अनगार भावना अधिकार और समयसार अधिकार है जिनमें श्री वट्टकेर स्वामी ने जिनकल्पी महामुनियों की चर्या का प्रधानरूप से कथन किया है। स्थविरकल्पी-संघ में रहने वाले मुनि भी उन भावनाओं को भाते हुए यथाशक्ति उनका पालन करते हैं।
(३) अनगार भावना अधिकार
लिंगं वदं च सुद्धी वसदिविहारं च भिक्ख णाणं चं।
उज्झणसुद्धी य पुणो वक्वं च तवं तधा झाणं।।७७१।।
एदमणयारसुत्तं दसविधपद विणयअत्थसंजुत्तं।
जो पढइ भत्तिजुत्तो तस्स पणस्संति पावाइं।।७७२।।
लिंगशुद्धि, व्रतशुद्धि, वसतिशुद्धि, विहारशुद्धि, भिक्षाशुद्धि, ज्ञानशुद्धि, उज्झनशुद्धि, वाक्यशुद्धि, तप:शुद्धि और ध्यानशुद्धि, ये दश प्रकार के अनगार सूत्र हैं, जो कि विनय और अर्थ संयुक्त हैं जो इनको पढ़ते हैं, उनके पाप नष्ट हो जाते हैं।
(१) लिंगशुद्धि-जो मनुष्य इस शरीर को नश्वर जानकर गृह भोगों से विरक्त हो जिनवर मत में प्रीति से युक्त हो निग्र्रन्थ जिनमुद्रा धारण कर लेते हैं, उनके लिंग शुद्धि होती है। इस लिंगशुद्धि में ही सम्यग्दर्शन शुद्धि, ज्ञानशुद्धि, तप शुद्धि और चारित्रशुद्धि भी आ जाती है।
(२) व्रतशुद्धि-जीवहिंसा, असत्य, चौर्य, मैथुन और परिग्रह इन पापों का मन, वचन, काय से त्यागकर पाँच महाव्रतों में दृढ़ बुद्धि रखना व्रत शुद्धि है। ये मुनि सर्व आरंभ से निवृत्त होकर जिनवर कथित धर्म में उद्युक्त रहते हैं। ये महासाधु मुनिपद के अयोग्य ऐसे बालमात्र परिग्रह में भी ममत्व नहीं करते हैं। और तो क्या अपने शरीर से भी ममत्व नहीं करते हैं, उन्हीं के यह शुद्धि होती है।
(३)
वसतिशुद्धि-गामेयरादिवासी णयरे पंचाहवासिणो धीरा।
सवणा फासुविहारी विवित्त एगंतवासी ये।।७८९।।
जो मुनि गाँव में एक रात्रि और नगर में पाँच दिवस रहते हैं पुन: प्रासुक प्रदेश देखकर विहार कर जाते हैं, वे प्राय: एकांत प्रदेश में रहते हैं। उन्हीं के यह वसतिशुद्धि होती है।
एगंतं मग्गंता सुसमणा वरगंधहत्थिणो धीरा।
सुक्कज्झाणरदीया मुत्तिसुहं उत्तमं पत्ता।।७८८।।
एकांत स्थान की खोज करने वाले ये मुनि उत्तम गंधहस्ती के समान धीर, वीर होते हैं और शुक्लध्यान में लीन होकर उत्तम मुक्ति सुख को प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ शुक्लध्यान करने में सक्षम ऐसे जिनकल्पी मुनि की ही यह चर्या है, सामान्य स्थविरकल्पी मुनि के लिए यह अनिवार्य नहीं है, चूँकि वे एक स्थान पर एक माह भी रह सकते हैं। चूँकि इनके लिए और भी कहा है-
एयाइणो अविहला वसंति गिरिकंदरेसु सप्पुरिसा।
धीरा अदीणमणसा रममाणा वीरवयणम्मि।।७८९।।
ये मुनि एकाकी रहते हैं, विह्वलता से रहित, धैर्य आदि गुणों से सहित होकर पर्वत व वंâदराओं में निवास करते हैं तथा दीनता रहित होकर वीरप्रभु के वचन में ही अनुराग रखते हैं। कई गाथाओं में इनके निर्जन, घनघोर, भयंकर वनों में निवास का वर्णन है। ऐसे महाधीर, उत्तम संहनन वाले मुनि के लिए यह वसति शुद्धि पूर्णरूप से होती है।
(४) विहारशुद्धि-जो मुनि सर्वसंग रहित होकर वायु के समान नगर, उद्यान आदि से सहित वसुधा में सर्वत्र स्वच्छंद-इच्छानुसार विचरण करते हैं उन्हीं के यह शुद्धि होती है। ये नाना देशों में विहार करते हुए भी ज्ञान के उपयोग से व समितिपूर्वक विहार करने से जीवों में बहुल प्रदेश में भी पाप से लिप्त नहीं होते हैं। ये साधु सदा गर्भवास आदि दु:खों से भयभीत रहते हैं-
घोरे णिरयसरिच्छे कुंभीपाए सुपच्चमाणाणं।
रुहिरचलाविलपउरे वसिदव्वं गब्भवसदीसु।।८०८।।
घोर, नरक के समान, कुंभीपाक में पकते हुए नारकियों को जैसा दु:ख होता है, वैसा ही रुधिर से बीभत्स गर्भवास में निवास करने से दु:ख होता है, ऐसा विचार करते हुए ये मुनि वैराग्य भावना का चिंतवन करते रहते हैं।
(५) भिक्षाशुद्धि-दो, तीन, चार, पाँच आदि उपवासों को करके वे तपस्वी मुनि श्रावक के घर में आहार लेते हैं। चारित्रसाधना के लिए और क्षुधा बाधा को दूर करने के लिए वे आहार ग्रहण करते हैं, सरस भोजन आदि की लंपटता के लिए नहीं लेते हैं, उन्हीं मुनि के यह भिक्षा शुद्धि होती है।
(६) ज्ञानशुद्धि-जिनको ज्ञान चक्षु प्राप्त हो चुका है और उस ज्ञान प्रकाश से जिन्होंने परमार्थ को देख लिया है, वे नि:शंकित और निर्विचिकित्सा गुणों से सहित होते हुए अपनी शक्ति के अनुसार उत्साह धारण करते हैं। ये तपश्चरण के बल से क्षीणशरीरी होकर भी अंग-पूर्व ग्रंथों का अथवा अपने समय के अनुसार श्रुत का सतत अध्ययन मनन करते रहते हैं। उन्हीं मुनि के यह ज्ञानशुद्धि होती है।
(७) उज्झनशुद्धि-जो मुनि अपने शरीर में भी स्नेह रहित होकर बंधु आदि में स्नेह का त्याग कर देते हैं तथा संस्कार आदि नहीं करते हैं उन्हीं के यह शुद्धि होती है। ये मुनि व्याधि से वेदना के होने पर भी उसका प्रतिकार नहीं चाहते हैं। ये क्या औषधि लेते हैं ?
जिणवयणमोसहमिणं विसयसुहविरेयणं अमिदभूदं।
जरमरणबाहिवेयण खयकरणं सव्वदुक्खाणं।।८४३।।
जिनेन्द्र भगवान के वचन ही महाऔषधि हैं, ये विषय सुख का विरेचन कराने वाले हैं, अमृतरूप हैं, जरा मरणरूपी व्याधि की वेदना और सर्व दु:खों का क्षय करने वाले हैं। शरीर तो रोगों का घर है उसके प्रति ऐसा विचार करने वाले मुनि के यह शुद्धि होती है।
(८) वाक्यशुद्धि-जो मुनि कानड़ी, मराठी, गुजराती, हिन्दी, संस्कृत आदि भाषा को विनयपूर्वक बोलते हैं। धर्म विरोधी वचन नहीं बोलते हैं। आगम के अनुवूâल स्व-पर हितकर वचन ही बोलते हैं अथवा मौन रखते हैं उन्हीं के वाक्यशुद्धि होती है। ये मुनि स्त्रीकथा आदि विकथा नहीं करते हैं।
(९) तप:शुद्धि-जो मुनि हेमंत ऋतु में धैर्य से युक्त हो खुले मैदान में रात्रि में बर्पâ, तुषार को झेलते हैं। ग्रीष्म ऋतु में सूर्य की तरफ मुख करके खड़े हो जाते हैं और वर्षाऋतु में वृक्ष के नीचे बूंदों को सहन करते रहते हैं, इत्यादि नाना प्रकार के तपश्चरण में लगे हुए मुनि के यह तप:शुद्धि होती है।
(१०) ध्यानशुद्धि-पांच इन्द्रियों का दमन करने वाले और मन को जीतने वाले मुनि धर्म, शुक्ल- ध्यान की शुद्धि को करते हैं।
ये मुनि-
णिट्ठिविदकरणचरणा कम्मं णिद्धुद्धदं धुणित्ताय।
जरमरणविप्पमुक्का उवेंति सिद्धिं धुदकिलेसा।।८८७।।
पूर्णरूप से त्रयोदशविध और क्रिया और त्रयोदशविध चारित्र के पालन में निष्णात ये मुनि गाढ़ कर्मबंधन को नष्टकर जन्म, मरण से मुक्त होकर और सर्व अघातिया कर्मों से भी छूटकर सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं। ये दश प्रकार की शुद्धि पालने वाले मुनि किन-किन नामों से कहे जाते हैं ?
समणोत्ति संजदोत्ति य रिसि मुणि साधुत्ति वीदरागोत्ति।
णामाणि सुविहिदाणं अणगार भदंत दंतोत्ति।।८८८।।
श्रमण, संयत, ऋषि, मुनि, साधु, वीतराग, अनगार, भदंत और दांत ये सब इन साधुओं के सुविहित-अन्वर्थ नाम कहे जाते हैं। इस प्रकार से इस अनगार भावना अधिकार में विस्तार से उत्कृष्ट मुनियों की चर्या कही गई है।
(४) समयसार अधिकार
इस अधिकार में सर्व आगम का सार अथवा स्व समय और पर समय का सार है। टीकाकार कहते हैं- ‘‘समयसारं द्वादशांगचतुर्दशपूर्वाणां सारं परमतत्त्वं मूलोत्तरगुणानां च दर्शनज्ञानचारित्राणां शुद्धिविधानस्य च भिक्षाशुद्धेश्च सारभूतं स्तोवं वक्ष्ये।’’ यह समयसार द्वादशांग और चौदह पूर्वों का सार-परम तत्त्व है। मूलगुण, उत्तरगुण, दर्शन, ज्ञान, चारित्र की शुद्धि और भिक्षाशुद्धि का सारभूत है, ऐसे इस समयसार को संक्षेप से मैं कहूँगा। चूँकि इस आचारांग के अंतर्गत मूलाचार में मुनियों का आचार ही प्रधान है। उसी से स्वात्मतत्त्व की सिद्धि निश्चित है। क्योंकि-
भिक्खं चर वस रण्णे थोवं जेमेहि मा बहू जंप।
दुक्खं सह जिण णिद्दा मेत्तिं भावेहि सुट्ठु वेरग्गं।।८९९।।
हे मुने! तुम भिक्षावृत्ति से आहार लो, वन में रहो, थोड़ा सा भोजन करो, बहुत मत बोलो, दु:ख-परीषह सहन करो, निद्रा को जीतो, मैत्री भाव को भावो और अच्छी तरह वैराग्य का चिंतवन करो। और भी कहते हैं-
थोवम्हि सिक्खिदे जिणइ बहुसुदं जो चरित्तसंपुण्णो।
जो पुण चरित्तहीणो विं तस्स सुदेण बहुएण।।८९९।।
थोड़ा पढ़े हुए भी मुनि चारित्र को परिपूर्ण कर बहुत ज्ञानी को जीत लेते हैं क्योंकि जो चारित्र से हीन हैं उनके बहुत श्रुतज्ञान से क्या लाभ ?
णाणं पयासओ तओ सोधओ संजमो य गुत्तियरो।
तिण्हं पिय संपजोगे होदि हु जिणसासणे मोक्खो।।९०१।।
ज्ञान प्रकाशक है, तप शोधक है, संयम गुप्ति को करने वाला है। इन तीनों के मिलने से जिनशासन में मोक्ष माना गया है। चार प्रकार के लिंग कल्प माने हैं-
अच्चेलक्वं लोचो वोसट्टसरीरदा य पडिलिहणं।
एसो हु लिंगकप्पो चदुव्विधो होदि णायव्वो।।९१०।।
आचेक्य-वस्त्र का त्याग-नग्नमुद्रा, लोच, व्युत्सृष्टशरीरता-शरीर के स्नान आदि संस्कार का त्याग और प्रतिलेखन-पिच्छिका ग्रहण ये चार लिंग दिगम्बर मुनि के चिन्ह हैं। अचेलकत्व आदि दश स्थितिकल्प-
अच्चेलक्कुद्देसियसेज्जाहररायपिंड किदियम्मं।
वद जेट्ठ पडिक्कमणं मासं पज्जो समणकप्पो।।९११।।
अचेलकत्व, औद्देशिक, शय्यागृह, राजपिंड, कृतिकर्म, व्रत, ज्येष्ठ, प्रतिक्रमण, मास और पर्या ये दश मुनियों के स्थितिकल्प होते हैं। अचेलकत्व-वस्त्र आदि परिग्रह का त्याग। औद्देशिक-अपने उद्देश्य से बनाया हुआ आहार औद्देशिक है, उसका त्याग अनौद्देशिक है। शय्यागृह त्याग-जो मेरी वसतिका में ठहरेगा, उसे ही मैं आहार दूँगा, ऐसे संकल्प करने वाले वसतिका के स्वामी के यहाँ आहार नहीं लेना। राजपिंडत्याग-गरिष्ठ भोजन का त्याग या दानशाला के भोजन का त्याग। कृतिकर्म-विधिवत् कृतिकर्मपूर्वक वंदना आदि करना। व्रत-पाँच महाव्रत आदि का पालन। ज्येष्ठ-श्रावक आदि में श्रेष्ठ होने से ज्येष्ठता-पूजनीयता। यह मुनि पद इन्द्र, चक्रवर्ती से भी श्रेष्ठ होने से ज्येष्ठ है। प्रतिक्रमण-सात प्रकार के प्रतिक्रमणों से आत्मा की भावना। मासस्थितिकल्प-वर्षायोग से पूर्व एक माह और पश्चात् भी एक माह उस ग्राम में रहना। अथवा प्रत्येक ऋतु में एक माह एक ग्राम में रहना, एक माह विहार करना। पर्या-निषद्यका और तीर्थंकरों के पंचकल्याण स्थानों की वंदना पर्या स्थितिकल्प है। ये दश श्रमणकल्प कहलाते हैं। मयूर पंख की पिच्छिका में पाँच गुण होते हैं-
रजसेदाणमगहणं मद्दव सुकुमालदा लहुत्तं च।
जत्थेदे पंचगुणा तं पडिलिहणं पसंसंति।।९१२।।
यह पिच्छिका धूलि और पसीने से खराब नहीं होती, मृदु है, सुकुमार है और लघु है। ये पाँच गुण मयूर पंख से बनी पिच्छी में ही होते हैं अन्य में नहीं। मुनि अपने मूलगुणों की रक्षा करते हुए योग आदि उत्तर गुणों का पालन करें-
मूलं छित्ता समणो जो गिण्हादी य बाहिरं जोगं।
बाहिरजोगा सव्वे मूलविहूणस्स किं करिस्संति।।९२०।।
जो मुनि मूलगुणों की विराधना कर बाह्य-आतापन आदि योग धारण करता है उसके वे योग मूलरहित होने से निष्फल हैं।
जो जत्थ जहा लद्धं गेण्हदि आहारमुवधिमादीयं।
समणगुणमुक्कजोगी संसारपवड्ढओ होइ।।९३२।।
जो साधु जिस किसी शुद्ध या अशुद्ध देश में जो कुछ भी प्राप्त हुआ शुद्ध या अशुद्ध आहार, उपकरण आदि ले लेता है, वह मुनि के गुण से रहित संसार को बढ़ाने वाला ही है अर्थात् आगम के अनुकूल ही आहार आदि लेना चाहिए।
फासुगदाणं फासुगउवधिं तह दो वि अत्तसोधीए।
जो देदि जो य गिण्हदि दोण्हं पि महप्फलं होई।।९३८।।
प्रासुक आहार और प्रासुक उपकरण-वसतिका आदि ये दोनों आत्मशुद्धि के लिए होते हैं। जो गृहस्थ प्रासुक आहार आदि देते हैं वे तथा जो ऐसा प्रासुक ही लेते हैं वे मुनि, इन दोनों को महाफल होता है क्योंकि आचार्य वैद्य हैं, विरक्त मुनि रोगी हैं, निर्दोष आहार चर्या ही औषधि है। आचार्यदेव क्षेत्र, बल, काल और पुरुष को जानकर शिष्य को स्वस्थ कर देते हैं। आगे कहते हैं-
आयरियकुलं मुच्चा विहरदि समणो य जो दु एगागी।
ण य गेण्हदि उवदेसं पावस्समणोत्ति वुच्चदि दु।।९६१।।
जो श्रमण आचार्यकुल-गुरुसंघ को छोड़कर एकाकी विहार करता है और गुरु का उपदेश नहीं ग्रहण करता है वह पापश्रमण-पापयुक्त साधु है क्योंकि स्वैर विहार में अनेक दोष आ जाते हैं-
चदुरंगुला य जिव्भा असुहा चदुरंगुलो उवत्थो वि।
अट्ठंगुलदोसेण दु जीवो दुक्खं खु पप्पोदि।।९९१।।
चार अंगुल प्रमाण जिह्वा अशुभ है और चार अंगुल प्रमाण ही उपस्थ-पुरुष का लिंग है। इन आठ अंगुल के दोष से यह जीव अनंत संसार में दु:ख भोग रहा है। अत: हे मुने! तुम रसना इन्द्रिय और स्पर्शनेन्द्रिय के कामजन्य विषय को जीतो क्योंकि जितेन्द्रिय मुनि चलते-फिरते भगवान हैं-
भिक्खं वक्वं हिययं सोधिय जो चरदि णिच्च सो साहू।
एसो सुट्ठिद साहू भणिओ जिणसासणे भयवं।।१००६।।
जो मुनि भिक्षा, वचन और हृदय को शुद्ध करके अर्थात् आहार शुद्धि, वचनशुद्धि और मन:शुद्धि को करके नित्य ही विचरण करते हैं, ऐसे साधु सुस्थित-सच्चे साधु हैं उन्हें जिनशासन में ‘भगवान्’ कहा है। श्री गणधर देव ने तीर्थंकर परमदेव से पूछा-
कधं चरे कधं चिट्ठे कधमासे कधं सये।
कथं भुंजेज्ज भासेज्ज कधं पावं ण वज्झदि।।१०१४।।
हे भगवन्! मैं कैसे आचरण करूँ ? कैसे ठहरूं ? कैसे बैठूं ? कैसे सोऊं ? कैसे भोजन करूँ ? और कैसे बोलूं ? कि जिससे पाप का बंध न होवे। तब भगवान् उत्तर देते हैं-
जदं चरे जदं चिट्ठे जदमासे जदं सये।
जदं भुंजेज्ज भासेज्ज एवं पावं ण बज्झइ।।१०१५।।
हे मुनियों! तुम यत्नपूर्वक आचरण करो, यत्नपूर्वक ठहरो, यत्नपूर्वक बैठो, यत्नपूर्वक भोजन करो और यत्नपूर्वक बोलो, इससे पाप का बंध नहीं होता है। क्योंकि-
जदं तु चरमाणस्स दयापेहुस्स भिक्खुणो।
णवं ण बज्झदे कम्मं पोराणं च विधूयदि।।१०१६।।
यत्नपूर्वक-सावधानीपूर्वक आचरण करते हुए, दयालु मुनि के नवीन कर्म नहीं बंधते हैं और पुराने कर्म झड़ जाते हैं। यहाँ पर समयसार अधिकार में मुनियों की उत्कृष्ट चर्या को दिखाया है।
(५) शीलगुणाधिकार
इस शील-गुण अधिकार में शील के अठारह हजार भेदों को और गुणों के चौरासी लाख भेदों को गिनाया है तथा उनको संख्या, प्रस्तार, नष्ट, उद्दिष्ट, परिवर्तन इन पाँच गणित भेदों से बताया है। उनमें से सर्वप्रथम शील के मूलभेदों को कहते हैं-
जोए करणे सण्णा इंदिय भोम्मादि समणधम्मे य।
अण्णोण्णेहिं अभत्था अट्ठारहसीलसहस्साइं।।१०१९।।
योग, करण, संज्ञा, इंद्रिय, पृथिवी आदि दश और दश श्रमण धर्म, इनको परस्पर गुणित करने से शील के १८००० भेद हो जाते हैं। मन-वचन-काय का शुभ क्रियाओं से संयोग होना योग है यह तीन प्रकार का है। क्रिया या परिणामों को करण कहते हैं, मन-वचन-काय का अशुभ क्रिया से संयोग होना करण है, यह भी मन, वचन, काय की अपेक्षा तीन प्रकार का है। संज्ञाएं चार हैं-आहार, भय, मैथुन और परिग्रह। इंद्रियाँ पाँच हैं-स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और श्रोत्र। पृथिवी, जल, अग्नि, वायु, प्रत्येक वनस्पति, साधारण वनस्पति, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पंचेन्द्रिय ये पृथिवी आदि दश प्रकार के जीव भेद हैं। उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, आविंâचन्य और ब्रह्मचर्य से दश श्रमण धर्म हैं। इस प्रकार-३²३·९, ९²४·३६, ३६²५·१८०,१८०²१०·१८००, १८००²१०·१८००० शील के भेद हो जाते हैं। शीलों के आलाप की उत्पत्ति में निमित्त अक्षसंचार के विशेष हेतु को संख्या कहते हैं। इनके स्थापन का नाम प्रस्तार है। अक्ष संचार का नाम परिवर्तन है। संख्या रख कर अक्ष निकालना नष्ट है और अक्ष रखकर संख्या निकालना उद्दिष्ट है। इस तरह संख्या, प्रस्तार, परिवर्तन, नष्ट और उद्दिष्ट, इन पाँच प्रकारों से शील और गुणों को जानना चाहिए१।’’ इन भेदों में प्रथम शील के भेद का उच्चारण इस प्रकार होता है-मनोगुप्ति से गुप्त, मन:करण से रहित, आहार संज्ञा रहित, स्पर्शन इन्द्रियविजयी, पृथिवीकायिक संयम से युक्त और क्षमागुण संयुक्त मुनि के अट्ठारह हजार शील के भेदों में यह पहला भेद कहा है। ऐसे ही सर्व भेद कोष्ठक से निकाल लेना चाहिए। ये सर्व भेद केवली भगवान के ही पूर्ण होते हैं। गुणों के भेद-
इगवीस चदुर सदिया दस दस दसगा य आणुपुव्वीय।
हिंसादिक्कमकाया विराहणा लोयणा सोही।।१०२५।।
इक्कीस, चार, सौ, दस, दस, दस, ऐसे अनुक्रम से हिंसादि त्याग को परस्पर गुणा करने से ८४ लाख उत्तर गुण हो जाते हैं। हिंसादि २१-प्राणिवध, मृषावाद, अदत्त, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, भय, अरति, रति, जुगुप्सा, मनोमंगुल, वचनमंगुल, कायमंगुल, मिथ्यादर्शन, प्रमाद, पैशून्य, अज्ञान और अनिग्रह, ये इक्कीस हिंसादि दोष हैं। अतिक्रमादि ४-अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार और अनाचार ये चार दोष हैं। पृथिवी आदि १००-पृथिवी, जल, अग्नि, वायु, प्रत्येक वनस्पति, अनंतकाय वनस्पति, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पंचेन्द्रिय। इनको आपस में गुणने से १०० भेद हो जाते हैं। अब्रह्म १०-स्त्रीसंसर्ग, प्रण्ीातरसभोजन, गंधमाल्यसंस्पर्श, शयनासन, भूषण, गीतवादित्र, अर्थसंप्रयोग, कुशीलसंसर्ग, राजसेवा और रात्रिसंचरण ये दश अब्रह्म हैं। आलोचना के दोष १०-आवंपित, अनुमानित, यद्दृष्ट, बादर, सूक्ष्म, छन्न, शब्दाकुलित, बहुजन, अव्यक्त और तत्सेवी ये दश दोष आलोचना के हैं। प्रायश्चित्त के दोष १०-आलोचना, प्रतिक्रमण, उभय, विवेक, व्युत्सर्ग, तप, छेद, मूल, परिहार और श्रद्धान ये दश दोष प्रायश्चित्त के हैं। इन सब दोषों से रहित उतने ही गुण हो जाते हैं। इनको परस्पर में गुणित करने से २१²४·८४, ८४²१००·८४००, ८४००²१०·८४०००, ८४०००²१०·८४००००, ८४००००²१०·८४००००० उत्तर गुण होते हैं।
इसका पहला भेद इस प्रकार है- प्राणातिपातविरत, अतिक्रमणदोष रहित, पृृथिवीकाय आरंभ से शून्य, स्त्रीसंसर्गवियुत, आवंâपितदोषरहित और आलोचना शुद्धियुत वीर मुनि के यह चौरासी लाख गुणों में प्रथम गुण का उच्चारण होता है। ये सर्व भेद सिद्धों में ही पूर्ण होते हैं। पूर्व कथित शील और गुणों को जानकर जो उनका पालन करते हैं वे इन शील गुणों को पूर्ण कर सर्वकल्याण को प्राप्त कर लेते हैं।
(६) पर्याप्ति अधिकार
इस अधिकार में पर्याप्तियों का कथन करेंगे। यहाँ पर ‘पर्याप्ति’ यह उपलक्षण मात्र है। इससे १. पर्याप्ति, २. देह, ३. काय संस्थान, ४. इन्द्रिय संस्थान, ५. योनि, ६. आयु, ७. प्रमाण, ८. योग, ९. वेद, १०. लेश्या, ११. प्रवीचार, १२. उपपाद, १३. उद्वर्तन, १४. स्थान, १५. कुल, १६. अल्पबहुत्व, स्थिति अनुभाग, १७. प्रकृतिबंध, १८. स्थिति बंध, १९. अनुभाग बंध और २०. प्रदेश बंध इसमें इन बीस सूत्र पदों का निरूपण किया गया है। पर्याप्ति के छह अधिकार हैं- संज्ञा, लक्षण, स्वामित्व, संख्यापरिमाण, निर्वृति और स्थितिकाल ये छह अधिकार पर्याप्तियों के होते हैं।
१. पर्याप्ति- आहार, शरीर, इन्द्रिय, आनप्राण-श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन ये छह भेद पर्याप्ति के हैं। एकेन्द्रिय जीवों के प्रारंभ की चार पर्याप्तियाँ होती हैं। द्वीन्द्रिय से असंज्ञी पंचेन्द्रिय तक पाँच एवं पंचेन्द्रिय संज्ञी जीवों को छहों पर्याप्तियाँ होती हैं। तिर्यंच और मनुष्यों में पर्याप्तियों की पूर्णता भिन्न मुहूर्त में (एक समय कम दो घड़ी में) होती है और देव, नारकियों के पर्याप्ति की पूर्णता प्रतिसमय होती है अर्थात् देव, नारकियों के सर्व अवयवों की रचना अंतर्मुहूर्त काल में ही हो जाती है। तिर्यंच और मनुष्यों के शरीर की रचना में बहुत काल लगता है किन्तु पर्याप्तियाँ अंतर्मुहूर्त में ही पूर्ण हो जाती हैं। चारों प्रकार के देवों के यहाँ उपपाद गृह में उपपाद शिला है। उसका आकार शुक्तिपुट के समान है। उसके ऊपर मणिखचित पलंग हैं। उसमें दिव्य शय्या पर दिव्य रूप से देव सम्पूर्ण यौवन सहित, सर्व आभरणों से भूषित उत्पन्न होते हैं।
२. देह- देवों का शरीर अंतर्मुहूर्त में ही पूर्ण बन जाता है। इसमें सात धातु, रक्त, शुक्र, वीर्य, मल-मूत्रादि नहीं होते हैं। उनका शरीर दिव्य वैक्रियिक रहता है। नारकियों का शरीर भी अंतर्मुहूर्त में बन जाता है। वैक्रियिक है फिर भी अत्यंत घिनावना, दुर्गंधियुक्त, भयंकर होता है। तिर्यंचों के एकेन्द्रिय से लेकर पंचेन्द्रिय पर्यंत अनेक भेद हैं, मनुष्य पंचेन्द्रिय ही होते हैं। नारकी नीचे की सात पृथिवियों में रहते हैं। देव अधोभाग में, मध्यलोक में व ऊध्र्वलोक में रहते हैं। मनुष्य ढाई द्वीप तक रहते हैं और तिर्यंच सारे मध्यलोक में रहते हैं। प्रकरण प्राप्त मध्यलोक के द्वीप, समुद्र का किंचित् वर्णन करते हैंं- जम्बूद्वीप, धातकीखण्ड, पुष्करवरद्वीप, वारुणीवरद्वीप, क्षीरवरद्वीप, घृतवरद्वीप, क्षौद्रवरद्वीप, नंदीश्वरद्वीप, अरुणद्वीप, अरुणभासद्वीप, कुण्डलवरद्वीप, शंखवरद्वीप, रुचकवरद्वीप, भुजगवरद्वीप, कुशवरद्वीप और क्रौंचवरद्वीप। जंबूद्वीप को घेर कर लवण समुद्र है, धातकीखण्ड के बाद कालोदधि समुद्र है। शेष समुद्र अपने-अपने द्वीप के नाम वाले ही हैं। एक द्वीप के बाद समुद्र और समुद्र को घेरकर द्वीप ऐसे द्वीप-समुद्र असंख्यात हैं। प्रारंभ में द्वीप है और अंत में स्वयंभूरमण समुद्र है। लवणसमुद्र का जल नमक जैसा है, वारुणीवर समुद्र का जल मद्य जैसा है, क्षीरवर समुद्र का जल दूध रूप है और घृतवरसमुद्र का जल घीरूप है। कालोदसमुद्र, पुष्करवरसमुद्र और स्वयंभूरमण समुद्र का जल जल के स्वाद जैसा है। शेष सर्व असंख्यातों समुद्रों का जल मधुर रस वाला है। जम्बूद्वीप, धातकीखण्डद्वीप और मानुषोत्तर से पूर्व आधा पुष्करद्वीप इन ढाई द्वीपों तक ही मनुष्य होते हैं। इनसे आगे सर्वत्र द्वीपों में पंचेन्द्रिय भोगभूमिज तिर्यंच हैं। आगे अंतिम स्वयंभूरमण के उस तरफ आधे में कर्मभूमिज तिर्यंच हैं। लवणसमुद्र, कालोदसमुद्र और स्वयंभूरमण समुद्र में जलचर जीव, मत्स्य, मगर आदि पाए जाते हैं। शेष समुद्रों में जलचर जीव नहीं हैं। यहाँ लवण समुद्र के नदीमुख के स्थान में नौ योजन प्रमाण देहधारी मत्स्य हैं, आगे स्वयंभूरमण समुद्र में एक हजार योजन प्रमाण शरीरधारी महामत्स्य होते हैं।
३. कायसंस्थान- तिर्यंचों और मनुष्यों में छहों संस्थान होते हैं। नारकी के हुंडक संस्थान ही है और देवों में एक समचतुरस्र संस्थान ही है।
४. इन्द्रिय संस्थान- श्रोत्रेन्द्रिय का आकार जव की नली के समान है, चक्षु इन्द्रिय का मसूर के समान है, घ्राणेन्द्रिय का तिल के पुष्प समान है, जिह्वा का आकार अर्धचन्द्राकार है और स्पर्शन इन्द्रिय के अनेक आकार होते हैं।
५. योनि- सचित्त, शीत, संवृत, अचित्त, उष्ण, विवृत, सचित्ताचित्त, शीतोष्ण और संवृतविवृत ये नव प्रकार की योनियाँ हैं। शंखावर्त, कूर्मोन्नत और वंशपत्र ये तीन भेद भी योनि के होते हैं। वूâर्मोन्नत योनि से तीर्थंकर, चक्रवर्ती आदि महापुरुष जन्म लेते हैं। वंशपत्र योनि से अन्य सभी भोगभूमिज, कर्मभूमिज मनुष्य जन्मते हैं और शंखावर्त योनि में गर्भ नहीं रहता है। योनि के ८४ लाख भेद भी होते हैं।
६. आयु- शुद्ध पृथिवीकायिक की उत्कृष्ट आयु १२ हजार वर्ष है। खर पृथिवीकायिक की २२ हजार वर्ष है। जलकायिक की ७ हजार वर्ष, अग्निकायिक की ७ दिन, वायुकायिक की ३ हजार वर्ष और वनस्पति कायिक की १० हजार वर्ष की उत्कृष्ट आयु है। द्वीन्द्रिय की १२ वर्ष, तीन इन्द्रिय की ४९ दिन, चतुरिन्द्रिय की ६ महीने उत्कृष्ट आयु है। पंचेन्द्रिय मत्स्य की उत्कृष्ट आयु एक कोटि पूर्व वर्षों की है। मनुष्यों में भोगभूमिजों की उत्कृष्ट आयु तीन पल्य है और कर्मभूमिजों की एक कोटि वर्ष पूर्व की है। नारकी और देवों की उत्कृष्ट आयु तेतीस सागर प्रमाण है। तिर्यंच व मनुष्यों की जघन्य आयु अंतर्मुहूर्त है और देव, नारकियों की जघन्य आयु दश हजार वर्ष है।
७. प्रमाण- प्रथम नरक में नारकियों के शरीर का प्रमाण-ऊँचाई जघन्य रूप से तीन हाथ प्रमाण है। सातवें नरक में उत्कृष्ट प्रमाण पाँच सौ धनुष है। देवों में सर्वार्थसिद्धि के देवों का शरीर प्रमाण एक हाथ प्रमाण है। भवनवासी देवों में उत्कृष्ट ऊँचाई पच्चीस धनुष है। तिर्यंचों में उत्कृष्ट ऊँचाई एक हजार योजन है। जघन्य घनांगुल के असंख्यातवें भाग मात्र है। मनुष्यों की जघन्य ऊँचाई छठे काल में एक हाथ है और उत्कृष्ट ऊँचाई सवा पाँच सौ धनुष प्रमाण है।
८. योग- मन-वचन-काय के निमित्त से जो आत्मप्रदेशों में चंचलता होती है, वह योग है। यह मन-वचन-काय से तीन भेदरूप है। एकेन्द्रिय जीवों के एक काययोग है, द्वीन्द्रिय से लेकर असंज्ञी पंचेन्द्रिय तक काययोग और वचनयोग हैं और संज्ञी पंचेन्द्रिय में तीनों योग रहते हैं।
९. वेद- एकेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय, नारकी और संमूच्र्छन जीव इनके एक नपुंसक वेद ही है। देव और भोगभूमिजों में स्त्रीवेद और पुरुषवेद ये दो वेद होते हैं। पंचेन्द्रिय तिर्यंच तथा मनुष्यों में तीनों वेद होते हैं।
१०. लेश्या- कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म और शुक्ल ये छह लेश्या हैं। नारकियों में प्रारंभ की तीन अशुभ लेश्या ही हैं। देवों में तीन शुभ लेश्या हैं। तिर्यंच और मनुष्यों में छहों लेश्याएँ होती हैं।
११. प्रवीचार- तिर्यंच और मनुष्यों में काय-शरीर से प्रवीचार-काम सुख होता है। भवनवासी व्यंतर, ज्योतिष्क और सौधर्म, ईशान स्वर्ग तक देवों में काय से प्रवीचार सुख है। इससे ऊपर सानत्कुमार-माहेन्द्र स्वर्ग में स्पर्शजन्य प्रवीचार है। ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लांतव और कापिष्ठ स्वर्गों में रूप देखने का प्रवीचार है। शुक्र, महाशुक्र, शतार, सहस्रार स्वर्गों में शब्द का प्रवीचार है अर्थात् ये देव देवांगनाओं का रूप देखकर या शब्द सुनकर काम सुख की तृप्ति कर लेते हैं। आगे आनत, प्राणत, आरण और अच्युत स्वर्गों में देव-देवांगना अपने-अपने पति-पत्नियों का मन में विचार कर ही कामसुख से सुखी हो जाते हैं। आगे नव ग्रैवेयक, नव अनुदिश और पाँच अनुत्तरों में देवांगनाएं ही नहीं हैं।
१२. उपपाद- असंज्ञी पंचेन्द्रिय तिर्यंच पहले नरक पृथिवी तक जाते हैं। सरीसृप आदि दूसरी पृथिवी तक, पक्षी तीसरी तक, उर: सर्प आदि चौथी तक, सिंह आदि पाँचवीं तक, स्त्रियाँ छठे तक और मनुष्य तथा महामत्स्य आदि तिर्यंच सातवीं पृथिवी तक जाते हैं। सर्व अपर्याप्तकों में, सर्वसूक्ष्म जीवों में, सर्व अग्निकायिक, वायुकायिक और सर्व असंज्ञी जीवों में तिर्यंच और मनुष्य उत्पन्न होते हैं। जिन्होंने दान दिया है या दान की अनुमोदना की है, ऐसे मनुष्य और तिर्यंच भोगभूमि में उत्पन्न होते हैं। पंचेन्द्रिय तिर्यंच और मनुष्य सम्यक्त्व के बिना ही भवनत्रिक देवों में जन्म लेते हैं। सम्यक्त्व और व्रत सहित तिर्यंच सोलहवें स्वर्ग तक जा सकते हैं। मनुष्य सम्यक्त्व सहित या रहित भी नवग्रैवेयक तक भी जाते हैं किन्तु इससे आगे सम्यक्त्व-व्रत से सहित ही जन्मते हैं।
१३. उद्वर्तन- सातवें नरक से निकले नारकी तिर्यंच ही होते हैं। छठे नरक के मनुष्य भव पा सकते हैं, उन्हें सम्यक्त्व हो भी सकता है। पाँचवें नरक से निकलकर संयम लाभ कर सकते हैं। चौथे से निकलकर मनुष्य होकर मोक्ष भी प्राप्त कर सकते हैं। तीसरे, दूसरे व पहले नरक से निकलकर नारकी तीर्थंकर भी हो सकते हैं किन्तु नरक से निकले जीव चक्रवर्ती, बलभद्र, नारायण, प्रतिनारायण नहीं होते हैं। पृथिवी, जल, अग्नि और वनस्पतिकायिक अपर्याप्त जीव वहाँ से निकलकर तिर्यंच या मनुष्य भी हो सकते हैं तथा विकलेन्द्रिय और पंचेन्द्रिय लब्धि अपर्याप्तक जीव तिर्यंच या मनुष्य हो सकते हैंं। देव, नारकी और भोगभूमियाँ जीव मरकर लब्धि अपर्याप्तक नहीं होते हैं। भवनत्रिक देव व ईशान स्वर्ग तक के देव वहाँ से च्युत होकर कदाचित् एकेन्द्रिय भी हो जाते हैं। उसमें पर्याप्तक ही होते हैं। आगे तीसरे स्वर्ग से बारहवें स्वर्ग तक के देव कदाचित् पंचेन्द्रिय तिर्यंच हो जाते हैं। इससे ऊपर के देव मरकर मनुष्य ही होते हैं। मनुष्य मरकर सर्व एकेन्द्रिय आदि तिर्यंचों में, नरकों में व देवों में जन्म ले सकता है और यदि पुरुषार्थ करे तो कर्मों का नाश कर मोक्ष प्राप्त कर लेता है।
सव्वट्ठादो य चुदा भज्जा तित्थयर चक्कवट्टित्ते।
रामत्तणेण भज्जा णियमा पुण णिव्वुदिं जंति।।११८६।।
सक्को सहग्गमहिसी सलोगपाला य दक्खिणिंदा य।
लोगंतिगा य णियमा चुदा दु खलु णिव्वुदिं जंति।।११८७।।
सर्वार्थसिद्धि से च्युत हुए जीव तीर्थंकर पद, चक्रवर्ती पद और बलभद्र पद के धारक होते हैं अथवा नहीं भी होते हैं, परन्तु वे नियम से मोक्ष प्राप्त करते हैं। सौधर्म इन्द्र शची देवी, लोकपाल, दक्षिण इन्द्र और लौकांतिक देव ये वहाँ से च्युत होकर मनुष्य होकर नियम से मोक्ष प्राप्त करते हैं।
१४. स्थान- इसमें जीवसमास, गुणस्थान और मार्गणा आदि का विस्तार से वर्णन है। जैसे एकेन्द्रिय के सूक्ष्म-बादर दो भेद हैं, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, असंज्ञी पंचेन्द्रिय और संज्ञी पंचेन्द्रिय ये सात हुए, इनके पर्याप्तक और अपर्याप्तक से दो-दो भेद करने से चौदह जीवसमास होते हैं। मिथ्यात्व, सासादन, मिश्र, असंयत, देशविरत, प्रमत्तविरत, अप्रमत्तविरत, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, सूक्ष्मसांपराय, उपशांतमोह, क्षीणमोह, सयोगकेवली और अयोगकेवली ये चौदह गुणस्थान हैं। गति, इन्द्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, लेश्या, भव्यत्व, सम्यक्त्व, संज्ञित्व और आहारक ये चौदह मार्गणा हैं। इन मार्गणाओं के अवांतर भेद करके उनमें गुणस्थान और जीवसमास को घटाया है।
१५. कुल- संपूर्ण जीवों के कुलों की संख्या एक कोड़ाकोड़ी, सत्तानवे लाख, पचास हजार कोटि है।
१६. अल्पबहुत्व- मनुष्यगति में सबसे थोड़े मनुष्य हैं, फिर भी श्रेणी के असंख्यात भाग मात्र हैं। मनुष्यों से असंख्यात गुणश्रेणी नारकी हैं। नारकियों से देवगति में देव असंख्यात गुणे अधिक हैं। देवों से अनंतगुणे अधिक जीव सिद्धगति में हैं और सिद्धों से भी अनंतगुणे तिर्यंचगति के जीव हैं।
१७. प्रकृतिबंध- यह जीव मिथ्यादर्शन, अविरति, कषाय और योग के निमित्त से कर्मों को ग्रहण करता है। उन कर्म पुद्गलों का जीव के आत्मप्रदेशों में मिल जाना-एकमेक हो जाना बंध है। इसके प्रकृतिबंध, स्थितिबंध, अनुभाग बंध और प्रदेशबंध ये चार भेद हैं। उसमें से प्रथम प्रकृति बंध के आठ भेद हैं-ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय। इनके उत्तर भेद एक सौ अड़तालीस हैं।
१८. स्थितिबंध- ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय और अंतराय इन कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति तीस कोड़ाकोड़ी सागर है। मोहनीय की सत्तर कोड़ाकोड़ी सागर है। नाम और गोत्र की बीस कोड़ाकोड़ी सागर और आयु की उत्कृष्ट स्थिति तेतीस सागर प्रमाण है। वेदनीय की जघन्य स्थिति बारह मुहूर्त है, नाम और गोत्र की आठ मुहूर्त है, शेष पाँच कर्मोें की अंतर्मुहूर्त है।
१९. अनुभाग बंध- ज्ञानावरणादि कर्मों का जो परिणामों के द्वारा शुभ-अशुभ रस-अनुभव उत्पन्न होता है जो कि जीव को सुख और दु:ख देता है, वह अनुभाग बंध है। ज्ञानावरण आदि चार घातिया कर्म पापरूप हैं और चार अघातिया कर्मों में पाप तथा पुण्य ये दोनों रूप हैं। नीम, कांजीर, विष और कालट, अशुभ प्रकृतियों के ये चार स्थान हैं। गुड़, खांड, शर्वरा और अमृत, शुभ प्रकृतियों के ये चार स्थान हैं। मोहनीय और अंतराय को छोड़कर शेष छह कर्मों का उत्कृष्ट अनुभाग चार स्थानों का है और जघन्य अनुभाग दो स्थानों का है। बाकी का अनुभाग बंध-अनुत्कृष्ट और अजघन्य दो, तीन और चारस्थान युक्त है। मोहनीय का उत्कृष्ट अनुभाग चतु:स्थानिक है, जघन्य अनुभाग एकस्थानिक है। अवशेष-अजघन्य, अनुत्कृष्ट अनुभाग एक, दो, तीन व चतु:स्थानिक है। अंतराय का उत्कृष्ट अनुभाग चतु:स्थानिक है। जघन्य अनुभाग एकस्थानरूप है और शेष में सर्व हैं। प्रदेशबंध-आत्मा के प्रत्येक प्रदेश में अनंत कर्म आकर स्थित हो जाते हैं, ये सूक्ष्म हैं, मन, वचन, काय के विशिष्ट व्यापार से आते हैं, आत्मा के साथ एक क्षेत्रावगाही होकर और ज्ञानावरणादि रूप से परिणत होकर तिल में तेल के समान रहते हैं। इसे ही प्रदेशबंध कहते हैं। आत्मा के साथ एक समय में बंधे हुए कर्म समयप्रबद्ध नाम से कहे जाते हैं। इस एक समयप्रबद्ध में आयु का एक भाग है। नाम और गोत्र को आयु से अधिक भाग मिलता है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय को इन नाम-गोत्र से अधिक भाग मिलता है। इनसे अधिक मोहनीय का भाग है और इस मोहनीय से अधिक वेदनीय का हिस्सा है। प्रकृति बंध, स्थितिबंध, अनुभागबंध और प्रदेशबंध ये चार भेद जिनके हैं वे कर्म मूल में आठ भेदरूप हैं और इनके उत्तर भेद एक सौ अड़तालीस हैं अथवा ये भेद असंख्यात लोक प्रमाण हैं। इन कर्मों का नाश हो जाने पर आत्मा ज्ञानादि अनंतगुण स्वरूप, परमज्योतिर्मय हो जाता है।
इस आचार ग्रंथ के आधार से निर्दोष चर्या को पालन करने वाले मुनि इन कर्मों का नाश करते हैं। यहाँ गुणस्थान के क्रम से कर्मों के नाश-क्षपणविधि को कहते हैं- कर्मक्षपण विधि-
मोहस्सावरणाणं खयेण अह अंतरायस्स य एव।
उववज्जइ केवलयं पयासयं सव्व भावाणं।।१२५०।।
मोहनीय ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय के क्षय से सर्व पदार्थों का-लोक, अलोक का प्रकाशक केवलज्ञान उत्पन्न हो जाता है। उन कर्मों के नाश का क्रम यहाँ कहते हैं- अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, मिथ्यात्व, सम्यङ्मिथ्यात्व और सम्यक्त्व इन सात प्रकृतियों का असंयत सम्यग्दृष्टि, संयतासंयत, प्रमत्तसंयत और अप्रमत्तसंयत ऐसे चार गुणस्थानों में से किसी भी गुणस्थान में नाश करके क्षायिक सम्यग्दृष्टि हो जाते हैं। जो मुनि क्षपकश्रेणी में आरोहण करके कर्मों का क्षय करने वाले हैं उनके नरक, तिर्यंच और देव इन तीनों आयु की सत्ता ही नहीं है। पुन: सातवें से आठवें गुणस्थान में जाकर नवमें में पहुँचते हैं, वहाँ उस गुणस्थान के नव भागों में से प्रथम भाग में नरकगति, नरकगत्यानुपूर्वी, तिर्यंचगति, तिर्यंचगत्यानुपूर्वी, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रियजाति, निद्रानिद्रा, प्रचलाप्रचला, स्त्यानगृद्धि, उद्योत, आतप, एकेन्द्रिय, साधारण, सूक्ष्म और स्थावर इन सोलह प्रकृतियों का नाश करते हैं। दूसरे भाग में अप्रत्याख्यानावरण की चार और प्रत्याख्यानावरण की चार ऐसी आठ प्रकृतियों का नाश होता है। तीसरे भाग में नपुंसक वेद, चौथे भाग में स्त्रीवेद, पाँचवें भाग में हास्य, रति, अरति, शोक, भय और जुगुप्सा इन छह प्रकृतियों का नाश होता है। छठे भाग में पुरुषवेद, सातवें में संज्वलन क्रोध, आठवें भाग में संज्वलन मान और नवमें भाग में संज्वलन माया का नाश होता है। ये छत्तीस प्रकृतियाँ नवमें गुणस्थान में नष्ट हो जाती हैं। दशवें गुणस्थान में संज्वलन लोभ का नाश होता है। इसके बाद बारहवें क्षीणकषाय नाम के गुणस्थान में ज्ञानावरण की पाँच, दर्शनावरण की चार, अंतराय की पाँच, निद्रा और प्रचला इन सोलह प्रकृतियों का नाश होता है। इसके बाद तेरहवें गुणस्थान में पहुँचकर अर्हंत केवली हो जाते हैं। ऊपर में कही ये प्रकृतियाँ त्रेसठ हैं। यथा ७±३±३६±१±१६·६३, इन त्रेसठ प्रकृतियों के सर्वथा विनाश हो जाने से केवलज्ञान प्रगट हो जाता है। यद्यपि चार घातिया-मोहनीय, दर्शनावरण, ज्ञानावरण और अंतराय इनका नाश कहा है फिर भी नामकर्म की तेरह और आयु की तीन ऐसे सोलह प्रकृतियाँ भी इनमें शामिल हैं। ये सयोगकेवली भट्टारक कुछ भी कर्मक्षपण नहीं करते हैं। पुन: क्रम से विहार करते हुए अंत में योग निरोध कर अयोगकेवली हो जाते हैं।
तत्तोरालियदेहो णामा गोदं च केवली जुगवं।
आऊण वेदणीयं चदुहिं खिवइत्तु णीरओ होई।।१२५१।।
तदनंतर वे अयोगकेवली औदारिक शरीर, नामकर्म, गोत्रकर्म, आयुकर्म और वेदनीय कर्म ऐसे चार कर्मों का युगपत् क्षय करके नीरज-सर्व कर्मरज से रहित सिद्ध परमात्मा हो जाते हैं। अयोगकेवली भगवान के अपने काल के द्विचरम समय में पाँच शरीर, पाँच संघात, पाँच बंधन, छह संस्थान, तीन अंगोपांग, छह संहनन, पाँच वर्ण, पाँच रस, दो गंध, आठ स्पर्श, देवगति, देवगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघु, उपघात, परघात, उच्छ्वास, साता-असाता में से कोई एक वेदनीय, दो विहायोगति, अपर्याप्त, स्थिर-अस्थिर, शुभ-अशुभ, सुस्वर-दु:स्वर, सुभग, दुर्भग, अनादेय, अयश:कीर्ति, निर्माण और नीचगोत्र, ऐसी बहत्तर प्रकृतियों का नाश होता है। अनंतर उनके चरम समय में शेष रही एक वेदनीय, मनुष्यगति, मनुष्यगति प्रायोग्यानुपूर्वी, मनुष्यायु, पंचेन्द्रिय जाति, त्रस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक, आदेय, यश:कीर्ति, उच्चगोत्र और तीर्थंकर प्रकृति इन तेरह प्रकृतियों का नाश कर एक समय में ही सिद्ध होकर यहाँ से ऊध्र्वगमन कर लोक के अग्रभाग में जाकर विराजमान हो जाते हैं। ये सिद्ध भगवान औदारिक शरीर से रहित-अशरीरी, कर्मरज रहित, निर्मल, निर्लेप, अनंत ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य सहित, अक्षय, अविनाशी, अनंतगुणों के आधार हो जाते हैं।
एसो मे उवदेसो संखेवेण कहिदो जिणक्खादो।
सम्मं भावेदव्वो दायव्वो सव्वजीवाणं।।
जिनेन्द्रदेव द्वारा कथित यह मुनियों के चारित्र का उपदेश मैंने संक्षेप से कहा है। हे साधुओं! तुम्हें सतत सम्यक् प्रकार से इसकी भावना करनी चाहिए-इसे ग्रहण करना चाहिए और सर्व भव्य जीवों के लिए यह उपदेश देना चाहिए, उन्हें ग्रहण करना चाहिए।
दइदूण सव्वजीवे दमिऊण य इंदियाणि तह पंच।
अट्ठविहकम्मरहिआ णिव्वाणमणुत्तरं जाथ।।
हे साधुगण! तुम सर्व जीवों पर दया करो तथा पाँचों इन्द्रियोें का दमन करो, आठ प्रकार के कर्मों से रहित होकर सबसे उत्कृष्ट निर्वाण पद को प्राप्त करो।
