समयसार के अनुसार गृहस्थ भी परस्पर में आचार्यत्व करते हैं
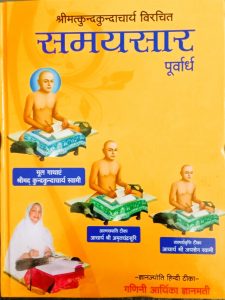
आत्मा और पुद्गल इन दो के आधार पर संसार टिका हुआ है। संसारी प्राणी भेदज्ञान के बिना आत्मा से विमुख होकर अज्ञानी संज्ञा को प्राप्त है इसीलिए वह विषय भोगों के प्रति आकर्षित होकर अपने आत्मज्ञान से शून्य हो रहा है। वह एकत्वस्वरूप आत्मा सबको सुलभ नहीं है, इस बात को सूचित करते हुए आचार्यश्री कुन्दकुन्द स्वामी कहते हैं—
सुदपरिचिदाणुभूदा सव्वस्सवि कामभोगबन्धकहा।
एयत्तस्सुवलंभो णवरि ण सुलहो विहत्तस्स।।४।।
अर्थ
काम-भोग सम्बन्धी कथायें सभी जीवों को सुनने में, परिचय में और अनुभव में आई हुई हैं। केवल पर से भिन्न एक रूप आत्मा की उपलब्धि सुलभ नहीं है। इस संसार में ये सभी संसारी जीव संसारचक्र के मध्य में स्थित हैं, अनन्तों बार द्रव्य-क्षेत्र-काल-भव और भाव रूप पंच परावर्तनों के द्वारा सतत ही परिभ्रमण कर रहे हैं।
उपर्युक्त गाथा की टीका में श्री अमृतचन्द्रसूरि कहते हैं कि ‘‘जिसने सर्व जगत् को अपने एकछत्र शासन से वश में किया हुआ है ऐसे महान् मोहरूपी पिशाच के द्वारा बैल के सदृश जोते जा रहे हैं। अतिशय रूप से वृद्धिंगत हुई जो तृष्णा, उसके संताप से जिनका अन्तरंग संतप्त हो रहा है, उस त्रास से संतप्त होकर मृगतृष्णा के समान आचरण करते हुए इन्द्रियों के विषयों की ओर दौड़ लगा रहे हैं।
और तो क्या ? परस्पर में एक दूसरे के प्रति आचार्यत्व को कर रहे हैं अर्थात् सभी एक दूसरे को भी इन्द्रिय विषयों में फसने का ही उपदेश देते रहते हैं।’’ आगे आचार्यश्री पुनः कहते हैं कि
‘‘परेषामात्मज्ञानमनुपासनाच्च न कदाचिदपिश्रुतपूर्व—अर्थात् स्वयं आत्मतत्व से अनभिज्ञ होने से और आत्मज्ञानी परम गुरुजनों की उपासना न करने से संसारी जीवों ने पूर्व के कदाचित् भी इस आत्मतत्वस्वरूप एकत्व को न तो सुना ही है, न पूर्व में कदाचित् इसका परिचय ही किया है और न ही कभी पूर्व में इसका अनुभव ही किया है अतः एक एकत्वरूप आत्मतत्व सुलभ नहीं है।’’
समयसार की इस चतुर्थ गाथा की हिन्दी ‘‘ज्ञानज्योति टीका’’ में पूज्य गणिनीप्रमुख आर्यिका श्री ज्ञानमती माताजी एक विशेषार्थ में लिखती हैं— जिस प्रकार अरहट के घटी यंत्र में जोते गये बैल उसी में घूमा करते हैं, उन्हें किसान जोते रहता है उन्हें श्रम से प्यास की बाधा भी होती है और उसकी शांति के लिए पानी की तरफ दौड़ने की कोशिश भी करते हैं उसी प्रकार से ये सभी संसारी प्राणी संसार रूपी चक्र में द्रव्य-क्षेत्र-काल-भव और भाव रूप पंच परावर्तनों को अनादिकाल से लेकर अब तक अनंतों बार कर चुके हैं।
मोहरूपी पिशाच के द्वारा प्रेरित हुए या बांधे गये होने से पराधीन हैं, विषयों की चाह रूपी दाह उत्पन्न होती रहती है उसको बुझाने के लिए विषयों की ओर ही दौड़ लगाते रहते हैं फिर भी इनकी प्यास बुझती नहीं है। इतना होेने पर भी ये जीव परस्पर में एक-दूसरे को इन विषयों का ही उपदेश देते रहते हैं।
यही कारण है कि इन सभी संसारी जीवों के लिए ये काम, भोग से सम्बन्धित कथायें नवीन नहीं हैं। इन जीवों ने हमेशा ही इनको सुना है, इनका परिचय किया है और अच्छी तरह से इनका अनुभव भी किया है फिर भी आज तक कभी भी इनसे किसी जीव को तृप्ति नहीं मिली है किन्तु एकत्वस्वरूप जो शुद्ध आत्मतत्व है वह यद्यपि प्रकाशमान ज्योतिस्वरूप है फिर भी कषायों के निमित्त से वह अत्यन्त तिरोभूत हो रहा है।
यही कारण है कि उसका ज्ञान नहीं हो पा रहा है। जिन्होंने उस आत्मतत्व को जाना है ऐसे अरहंत-सिद्ध-आचार्य—उपाध्याय और साधुगण उनकी उपासना न करने से इन जीवों ने उस आत्मतत्व के स्वरूप को न कभी सुना है, न परिचय किया है और न अनुभव ही किया है इसीलिए वह सुलभ नहीं है किन्तु अतीव दुर्लभ है। इसमें परमेष्ठी की उपासना से ही आत्मतत्व का बोध होना प्रबल निमित्त की महत्ता को सूचित करता है।
यहाँ कोई कहे कि कामभोग से सम्बन्धित कथा से पाँचों इन्द्रियों के विषय लिये जाते हैं। उसमें जिनप्रतिमा का दर्शन, उपदेश श्रवण आदि भी तो चक्षु इन्द्रिय व कर्णेन्द्रिय के विषय हैं। ये भी श्रुत, परिचित, अनुभूत हैं किन्तु ऐसा नहीं है क्योंकि मूल में ‘‘सव्वस्स वि’’ पाठ है, ये सभी के लिए सुलभ नहीं हैं, हजारों लाखों में किन्हीं को ही प्राप्त होते हैं।
दूसरी बात यह है कि मूलाचार में आचार्यदेव ने पंचेन्द्रियनिरोध नाम के पाँच मूलगुणों के बाद ही छह आवश्यक मूलगुणों में देवदर्शन, उपदेशश्रवण आदि को लिया है अतः ये इन्द्रियों के विषय नहीं हैं। ये कामभोग कथा में कथमपि गर्भित नहीं किये जा सकते।
षट्खंडागम, गोम्मटसार कर्मकांड आदि ग्रन्थ बन्ध कथा में शामिल नहीं किये जा सकते हैं क्योंकि जीव के कर्मबन्ध को निरूपित करने वाले ग्रन्थ और उनके फल का वर्णन करने वाले ग्रन्थ ये सभी द्वादशांग के अन्तर्गत हैं।
कर्मप्रवाद पूर्व में कर्मों का विस्तृत विवेचन है और आत्मप्रवाद न पूर्व परिचय में आये हैं और न अनुभव में ही आये हैं इसीलिए उनका ज्ञान भी दुर्लभ ही है सुलभ नहीं है तथा अपायविचय धर्मध्यान में अशुद्ध आत्माओं के लिए ही संसार से निकालने का उपाय चितवन किया जाता है और विपाकविचय धर्मध्यान में भी कर्मों के उदय-सत्व-बन्ध आदि की दशाओं का चितवन किया जाता है।
ये धर्मध्यान भी चौथे गुणस्थान से लेकर सातवें तक पाये जाते हैं अतः यहाँ पर इन ग्रन्थों के स्वाध्याय को सुलभ व हेय नहीं समझना चाहिये किन्तु कर्मबन्ध को कराने वाली और उनके फलस्वरूप नर—नारकादि पर्यायों में ले जाने वाली जो कथाएँ हैं उनको सुलभ समझकर उनका निषेध समझना चाहिये।
यहाँ पर श्री जयसेनाचार्य ने निर्विकल्प अवस्था रूप परम समाधि में ही निश्चय रत्नत्रय से परिणत आत्मतत्व को ‘‘एकत्व’’ कहा है और उसकी दुर्लभता बताई है जो कि शुक्लध्यान रूप है अतः उस ध्यान में यह उपर्युक्त बन्ध कथा भी छूट जाती है और उस अपूर्व अवस्था के आने पर अपूर्व आदि गुणस्थानों में जाकर यह जीव उस शुद्ध आत्मा को प्राप्त कर लेता है कि जिसको पहले कभी भी नहीं पाया था।
सार यह निकलता है कि यह एकत्वस्वरूप आत्मतत्व अतीव दुर्लभ है इसका अनुभव निवकल्प ध्यान में अप्रमत्त मुनि ही करते हैं। चतुर्थ, पंचम और छठे गुणस्थानवर्ती सराग सम्यग्दृष्टि उसकी श्रद्धा करते हुए उसके अनुभव करने का और प्राप्त करने का पुरुषार्थ ही करते रहते हैं अतः हम सबको भी उस आत्मतत्व का श्रद्धान करते हुए यथाशक्ति संयम पालन का पुरुषार्थ करना चाहिये ताकि शीघ्रातिशीघ्र उस एकत्व विभक्त आत्मा का आनन्द प्राप्त कर सके।
