समयसार में अज्ञानी को सम्बोधन
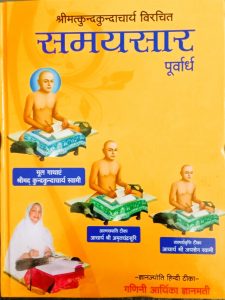
छहढाला में पं. श्री दौलतरात जी ने कहा है कि—
‘‘मोहमहामद पियो अनादि, भूल आपको भरमत वादि।’’
अर्थात् अनादिकाल से यह जीव मोहरूपी मदिरा को पी करके अपने आत्मस्वरूप को भूला हुआ है इसीलिए दुःखी होकर चतुर्गति में परिभ्रमण कर रहा है। आचार्य श्री कुन्दकुन्ददेव भी समयसार में कहते हैं—
अण्णाणमोहिदमदी, मज्झमिणं भणदि पुग्गलं दव्वं।
बद्धमबद्धं च तहा, जीवो बहुभावसंजुत्तो।।२३।।
सव्वण्हुणाणदिट्ठो, जीवो उवओगलक्खणो णिच्चं।
कह सो पुग्गलदव्वी-भूदो जं भणसि मज्झमिणं।।२४।।
जदि सो पुग्गलदव्वी-भूदो जीवत्तमागदं इदरं।
तो सत्तो वुत्तुंं जे, मज्झमिणं पुग्गलं दव्वं।।२५।।
अर्थात् अज्ञान से मोहित बुद्धि वाला जीव इन सम्बद्ध और असम्बद्ध पुद्गल द्रव्यों को मेरा कहता है उसी प्रकार यह बहुत भावों से सहित हो रहा है किन्तु सर्वज्ञ के ज्ञान में देखा गया यह जीव सदा ही उपयोग लक्षण वाला है वह पुद्गलद्रव्य कैसे हो सकता है ? जो कहता है कि यह मेरा है, यदि वह पुद्गलद्रव्य रूप हो जावे तो अन्य पुद्गल जीवरूप हो जायेगा तब तो यह कहना शक्य होगा कि यह पुद्गल द्रव्य मेरा है। इन गाथाओं की आत्मख्याति टीका में श्री अमृतचन्द्रसूरि ने कहा है—
‘‘युगपदनेकविधस्य बंधनोपाधेः सन्निधानेन—स्वीकुर्वाणः
पुद्गल द्रव्यं ममेदमित्यनुभवति किलाप्रतिबुद्धो जीवः।
अथायमेव प्रतिबोध्यते रे द्वरात्मन्! आत्मसंपन्
जहीहि जहीहि परमाविवेकस्मरसतृणाभ्यवहारित्वं।’’
उसकी हिन्दी टीका करती हुई पूज्य गणिनीप्रमुख श्री ज्ञानमती माताजी लिखती हैं—
‘‘पुद्गलद्रव्य—अचेतन परद्रव्यों को’’ ‘‘यह मेरा है’’ अज्ञानी जीव ऐसा अनुभव करता है। अत्यन्त आच्छादित हुए अपने स्वभाव से इसकी समस्त भेदज्ञानरूप ज्योति अस्त हो गई है, महा अज्ञान से इसका हृदय अपने आप ही विमोहित हो रहा है। ऐसे ही अज्ञानी जीव को समझाते हुए आचार्य कहते हैं—
‘‘रे दुरात्मन् ! अरे आत्मघाती ! आत्मवंचक ! तू छोड़, छोड़!
परम अविवेक से अतिगृद्धि को करके तृृणसहित भोजन को छोड़ अर्थात् जैसे तृणसहित सुन्दर भोजन को हस्ती आदि पशु खाते हैं, ऐसे खाने का स्वभाव छोड़ दे। सर्वज्ञ के ज्ञान से प्रकट हुआ यह जीव द्रव्य नित्य ही उपयोग स्वभावरूप है तब भला वह पुद्गलद्रव्यरूप कैसे हो सकता है ? कि जिससे तू ‘‘यह पुद्गल द्रव्य मेरा है’’ ऐसा अनुभव करता है।
यह सम्पूर्ण प्रकरण समयसार ग्रन्थ में पढ़ने योग्य है कि आचार्यश्री किस प्रकार से मुनियों को सम्बोधन करते हुए उन्हें आत्मा में स्थिर करने हेतु उनकी भत्र्सना भी करते हैं जो कि उनका वात्सल्यमय अधिकार भी है। एक कलश काव्य में भी उन्होंने कहा है—
मालिनी छन्द
अयि कथमपि मृत्वा तत्त्वकौतुहाली सन्,
अनुभव भव मूर्तेः पार्श्ववर्ती मुहूर्तं।
पृथगथ विलसन्तं स्वं समालोक्य येन,
त्यजसि झगिति मूत्र्या साकमेकत्वमोहं।।२३।।
अर्थात् हे वत्स! तू किसी तरह मर-पचकर भी तत्त्वों का कौतूहली होता हुआ इस शरीर के पड़ोसी—आत्मा का एक मुहूर्त तक भी अनुभव कर, जिससे कि अपनी आत्मा को प्रकाशरूप परद्रव्यों से पृथक देखकर इस शरीर या पुद्गल द्रव्य के साथ एकत्व के मोह को—विपरीत भाव को शीघ्र ही छोड़ सके।
वास्तव में द्रव्यदृष्टि से यह जीव शुद्ध, बुद्ध, चिच्चमत्कार रूप एक ज्ञानदर्शनस्वभावी ही है, पर्यायदृष्टि से पुद्गलमय शरीर के साथ सम्बन्ध रखते हुए भी स्वयं कभी जड़—अचेतन नहीं हुआ है इसीलिए कलश काव्य में मर पचकर भी तत्त्वचर्चा में रस लेने की प्रेरणा दी गई कि हे आत्मन्।
अपनी आत्मा को तू शरीर का पड़ोसी समझ ले और मुहूर्त मात्र—४८ मिनट भी स्थिर होकर आत्मा का अनुभव कर। यह निश्चयनय की अवस्था मुनियों की अत्यन्त उच्चश्रेणी है जिसे अध्यात्म ग्रन्थों के माध्यम से जाना जाता है। इससे पूर्व भी हमें करणानुयोग के शास्त्रों से आत्मा और पुद्गल के सम्बन्ध को जानना होगा, जैसा कि गोम्मटसार कर्मकांड में आचार्य श्री नेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्ती ने कहा भी है—
पयडी सील सहाओ, जीवंगाणं अणाइसम्बन्धो।
कणयोवले मलं वा, ताणत्थित्तं सयं सिद्धं।।
अर्थात् स्वर्णपाषाण जिस प्रकार खान से निकलने पर अशुद्ध—मलयुक्त रहता है उसे पुरुषार्थपूर्वक ही शुद्ध करके स्वर्णत्व प्राप्त किया जाता है उसी प्रकार जीव और पुद्गल का अनादिकाल से सम्बन्ध चला आ रहा है पुरुषार्थपूर्वक संयम और तप के द्वारा शुद्ध परमात्मा बनाया जा सकता है।
