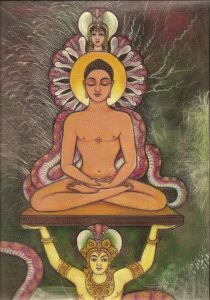व्याकरण का अध्ययन
चातुर्मास शुरू होते ही मैं संस्कृत व्याकरण और सिद्धान्त ग्रंथ आदि खूब पढ़ना चाहती थी किन्तु अभी तक मेरी इच्छा पूर्ण नहीं हो रही थी। इससे मेरे परिणामों में कभी-कभी बहुत ही अशांति हो जाती थी, यहाँ तक कि कभी-कभी मेरी आँखों में अश्रु आ जाते।’’ ‘‘भगवान् ! मुझे पढ़ने का साधन मिलेगा? मेरी ज्ञान की बुभुक्षा कैसे शान्त होगी?’’
मेरी यह स्थिति देखकर विशालमती माताजी आचार्यश्री के पास पहुँचकर सजल नेत्र करके मेरी वेदना सुनातीं और निवेदन करतीं- ‘‘महाराज जी! इसकी पढ़ाई का कुछ प्रबंध कीजिये।’’ महाराज जी कहते-‘‘अम्मा! इतनी छोटी उम्र है। आजकल का जमाना बहुत ही खराब है। पण्डितोें से पढ़ाने में कभी भी कोई उंगली उठा सकता है अतः इसे खूब स्वाध्याय करके स्वयं ही श्लोक रट-रट कर अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहिए, चिन्ता नहीं करनी चाहिए।’’
एक बार मैंने कहा-‘‘महाराज जी! मैं सर्वार्थसिद्धि ग्रंथ का स्वाध्याय करने बैठी, मूल संस्कृत पंक्तियों से अर्थ समझना चाहती थी किन्तु कुछ समझ में नहीं आया, मैं चाहती हूँ कि मुझे आप एक बार इस ग्रन्थ को पढ़ा दीजिये।’’ महाराज जी ने कहा-‘‘आज तुम्हें मैं एक ग्रन्थ तो पढ़ा दूँ फिर भी संस्कृत के ग्रन्थों को पढ़कर स्वयं अर्थ करने की क्षमता प्राप्त करने के लिए संस्कृत व्याकरण का पढ़ना बहुत ही जरूरी है।’’ मैं तो स्वयं व्याकरण पूर्ण करना चाहती ही थी।
इस उत्तर से कुछ शांति मिली पुनः विशालमती माताजी के अत्यधिक अनुनय-विनय से महाराज जी ने स्थानीय पंडितप्रवर इन्द्रलाल जी शास़्त्री से कहा- ‘‘पंडित जी! मेरी शिष्या वीरमती को आप संस्कृत व्याकरण पढ़ा दें।’’ पंडित जी ने महाराज जी की आज्ञा को शिरोधार्य कर मेरा अध्यापन शुरू किया। पूज्या क्षुल्लिका विशालमती माताजी मेरे साथ व्याकरण पढ़ने बैठ गर्इं।
पंडित जी ने दो- तीन सूत्र कराये और खूब समझाया। उतनी ही देर में मुझे वे सूत्र, उनकी वृत्ति और अर्थ याद हो गये पुनः पंडित जी ने कहा- ‘माताजी! इन सूत्रों को मैं कल कंठाग्र सुनूँगा।’’ तब मैंने कहा-पंडित जी! आप अभी ही सुन लो और मुझे आगे के आठ-दस सूत्र और बता दो।’’ पंडित जी ने कहा-‘‘यह लोहे के चने हैं हलुआ नहीं है। बस एक-दो सूत्र ही पढ़ो ज्यादा हविश (लालच) मत करो।’’ दो-तीन दिन पंडित जी ने पढ़ाया किन्तु मुझे इस गति से संतोष नहीं हुआ।
तब विशालमती जी के आग्रह से आचार्यश्री ने दूसरे पंडितों को बुलाया। वे भी ऐसे ही असफल रहे, तब पंडित इंद्रलाल जी आदि कई महानुभावों ने विचार किया कि- ‘‘इन्हें तो व्याकरण पढ़ने की भस्मक व्याधि है सो कोई ब्राह्मण विद्वान् जो कि अतिप्रौढ़ हो, जिसे व्याकरण कंठाग्र हो और जो ५० सूत्र पढ़ाकर भी न थके ऐसा विद्वान् ढूँढकर लाना चाहिए।’’
उस समय जैन कालेज में कातन्त्र रूपमाला व्याकरण को पढ़ाने वाले एक दामोदर शास्त्री थे, उन्हें बुलाया गया और आचार्यश्री के सामने उनका परिचय दिया गया। पंडित इंद्रलाल जी बोले- ‘‘महाराज जी! ये पंडितजी ही इन्हें व्याकरण पढ़ा सकते हैं क्योंकि इन्हें व्याकरण के सारे सूत्र वंâठाग्र हैं। रात-दिन यही व्याकरण पढ़ाते हैं।’’
तभी आचार्यश्री ने मुझे बुलाया और विनोदपूर्ण शब्दों में बोले- ‘‘वीरमती! देखो, ये विद्वान् दामोदर शास़्त्री जी तुम्हें व्याकरण पढ़ायेेंंगे, यह कातन्त्र रूपमाला नाम की व्याकरण का यहाँ जैन कालेज में दो वर्ष का कोर्स है लेकिन हाँ, तुम्हें दो महीने में पूरी कर लेनी है।’’ मैंने प्रसन्नता से कहा-‘‘हाँ, महाराज जी! जैसी आपकी आज्ञा है, वैसा ही करूँगी, मैं तो दो महीने से एक दिन कम में ही पूरी कर लूूँगी।’’
इसी बीच पंडित दामोदर जी बोले-‘‘पूज्य महाराज जी! मैं प्रतिदिन एक घण्टे समय दे सकता हूँ इससे अधिक नहीं, चूँकि मेरे पास अधिक समय ही नही हैं।’’ विशालमती माताजी ने कहा- ‘‘ठीक है पंडित जी! आप कल से ही इनकी व्याकरण शुरू कर दीजिए। मुझे भी व्याकरण की रुचि है। साथ ही मैं भी अध्ययन करूँगी।’’
दूसरे दिन से कातन्त्र रूपमाला का अध्ययन शुरू हो गया। पंडित दामोदर जी सूत्र बोलते, उसका अर्थ कर देते पुनः संधि तथा रूपसिद्धि आदि करना बता देते। मैं सुनती रहती सब समझ लेती, किसी दिन शायद ही दूसरी बार व्याकरण हाथ में उठाई हो, उसी समय जो मनन हो जाता था सो ठीक, दूसरे दिन यदि पंडित जी कोई संधि या रूप पूछ लेते तो मैं विधिवत् सूत्रोच्चारण करके बता देती। विशालमती माताजी भी आश्चर्य से कहा करतीं-‘‘अम्मा! तुमने पूर्वजन्म में व्याकरण पढ़ी है ऐसा प्रतीत होता है।
यही कारण है कि एक पाठी के समान तुम्हें व्याकरण याद हो जाती है, पुनः पुनः दिन भर रटना नहीं पड़ता है।’’ मुझे भी स्वयं ऐसा लगता था कि वास्तव में जैसे मैंने इस पुस्तक को भी पढ़ा ही होगा, यही कारण है कि मुझे न तो वह व्याकरण कठिन महसूस होती, न लोहे के चने लगती। मैं सोचा करती-भला विद्वान् लोग व्याकरण को लोहे का चना क्यों कहते हैं? उस समय कातन्त्र व्याकरण की मूल प्रति बड़ी मुश्किल से १-२ मिली थीं एवं मुझे भी उस व्याकरण की सरलता तथा जैनाचार्यों की कृति होने से बहुत ही प्रेम हो गया था,
अतः मेरी इच्छा व क्षुल्लिका विशालमती माताजी की प्रेरणा और गुरुदेव आचार्यश्री देशभूषणजी महाराज की आज्ञा से खण्डाका सरदारमलजी ने वीर प्रेस में उसी समय यह व्याकरण प्रति छपवाई थी। पंडित भंवरलालजी न्यायतीर्थ सामने वीर प्रेस में हमेशा रहते थे अतः सामने के कमरे में सतत मेरी चर्या का अवलोकन कर एवं अध्ययनरत देखकर प्रसन्नता व्यक्त किया करते थे।
कभी-कभी निकट आकर क्षुल्लिका विशालमती माताजी से कुछ धर्मचर्चायें भी किया करते थे। मुझे उन दिनों आहार में अन्तराय अधिक होती रहती थी जिससे शरीर, मस्तिष्क और आँखें कमजोर रहती थीं परन्तु फिर भी अपनी आवश्यक क्रियाओं को करके मैं स्वाध्याय भी अधिक करती थी अतः व्याकरण का रटना नहीं होता था।
फिर भी रात्रि में स्वप्न में अनेक रूप सिद्ध कर लिया करती थी। जो-जो सूत्र एक रूप के सिद्ध करने में काम आते थे, प्रायः सुबह उठकर व्याकरण देखने से वे सूत्र सही मिलते थे। कुल मिलाकर मैं दिन में व्याकरण नहीं रटती थी तो भी रात्रि स्वप्न में रटना हो जाया करता था। इसे कहते हैं संस्कार। प्रायः सभी लोग अनुभव करते हैं कि जो कार्य दिन में किया जाता है या जिस कार्य में अधिक रुचि होती है स्वप्न में प्रायः वे ही कार्य दिखते रहते हैं। जैसे कि कपड़े के व्यापारी स्वप्न में भी कपड़ा फाड़ते रहते हैं।
विशालमती माताजी कभी-कभी आचार्यश्री के समीप आकर कहा करतीं- ‘‘महाराज जी! वीरमती अम्मा दिन में एक बार व्याकरण पढ़ने के बाद उठाकर देखती भी नहीं हैं और रात्रि स्वप्न में सारे सूत्र याद कर लिया करती हैं।’’ तब निकट में बैठे पंडित कन्हैयालालजी आदि यही कहते कि इन्होंने पूर्वजन्म में सब कुछ पढ़ा हुआ है इसलिए बिना याद किये सूत्र वंâठाग्र हो जाते हैं।
पंडित इंद्रलाल जी प्रतिदिन दर्शन करने आते थे, तब वे व्याकरण में मेरी इतनी योग्यता देखकर कहा करते थे-‘‘ये माताजी ‘व्युत्पन्नमती’ हैं।’’ क्षुल्लिका विशालमती जी से भी कहते कि-तुम इन्हें व्युत्पन्नमती कहा करो। इनका व्युत्पन्नमती नाम सार्थक है। तब विशालमती माताजी भी अतीव वात्सल्यपूर्वक व्युत्पन्नमती कहने लगती थीं।
अनन्तर दो महीने में एक दिन शेष रहने पर ही मैंने व्याकरण पूर्ण पढ़ लिया, तब विशालमती माताजी मुझे साथ में लेकर आचार्यश्री से आशीर्वाद दिलाने लार्इं। आचार्य देव ने कहा- ‘‘बस, इतने मात्र व्याकरण से तुम सभी शास्त्रों का अर्थ समझ लोगी, अब तुम्हें किसी से कोई भी ग्रन्थ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है।’’
इसके बाद दामोदर शास्त्री को यथोचित पुरस्कार दिलाकर आचार्यश्री ने कहा-‘‘पंडित जी! बस आपका कार्य हो चुका है।’’ उस समय पंडित जी बहुत ही दुःखी हुए। वे बोले-‘‘गुरुदेव! मैं इन माताजी को और भी कुछ अध्यापन कराकर इनकी सेवा करना चाहता हूँ।’’ आचार्य श्री ने कहा-‘‘पुनः सोचा जायेगा।’’
फिर भी मेरी इच्छा सब कुछ पूर्ण हो चुकी थी और गुरु आज्ञा को ही मैं सब कुछ मानती थी। इसी बीच ‘‘चारित्र चक्रवर्ती आचार्यश्री शान्तिसागर जी महाराज सल्लेखना लेने वाले हैं’’ इतना सुनकर मुझे उनके दर्शनों की तीव्र अभिलाषा हो उठी। मैंने चातुर्मास के बाद दक्षिण जाने का विचार बना लिया।
आचार्य श्री देशभूषण जी महाराज के मुख से चारित्रचक्रवर्ती आचार्यदेव श्री शान्तिसागर जी महाराज की प्रशंसा सुना करती थी। क्षुाल्लका विशालमती जी ने भी उनके उत्कृष्ट चारित्र और कठोर तपश्चरण की बहुत ही प्रशंसा की थी। मेरे मन में भी तीव्र भावना जागृत हुई कि चारित्र चक्रवर्ती महाराज के दर्शन अवश्य करना। मैंने उन गुरुदेव के दर्शन न होने तक नमक का त्याग कर दिया। उस समय मैं आचार्यश्री देशभूषण जी के सामने बहुत ही कम बोलती थी अतः मैं गुरू से कुछ भी नहीं कह सकी।
मैंने क्षुल्लिका विशालमती जी से बार-बार दर्शन कराने के लिए आग्रह करना शुरू कर दिया। तब उन्होंने एक दिन आचार्यश्री के पास निवेदन किया- ‘‘महाराज जी! इन्होंने नमक त्याग कर दिया है। कहती हैं कि जब आचार्य शांतिसागर जी महाराज के दर्शन करूँगी तभी नमक लूँगी। आचार्यश्री तो सल्लेखना ले चुके हैं अतः इन्हें दर्शन नहीं मिले तो इनका यह त्याग जीवन भर के लिए हो जायेगा।’’ आचार्य महाराज ने कहा-‘‘अच्छा, चातुर्मास के बाद मैं तुम्हारे साथ इन्हें भेज दूँगा।
तुम इन्हें आचार्यदेव के दर्शन कराकर वापस मेरे पास छोड़ जाना।’’ विशालमती जी ने यह बात स्वीकार कर ली, तब मुझे बहुत ही शांति मिली। सानन्द चातुर्मास सम्पन्न होने के बाद हम दोनों आचार्यश्री से आज्ञा लेकर दक्षिण की ओर जाने लगीं। उस चातुर्मास में यहाँ पर सरदारमल जी खडाका की माँ ने आचार्यश्री से क्षुल्लिका दीक्षा ली थी।
इनका नाम ‘क्षुल्लिका वृषभसेना’ रखा गया था तथा लखनऊ की महिला, जो मेरे पास ब्रह्मचारिणी थीं, उन्होंने भी क्षुल्लिका दीक्षा ले ली थी। ये दोनों हमारे पास ही रहती थीं तथा बाराबंकी की ब्रह्मचारिणी चन्द्रावती भी हमारे पास ही थीं। यद्यपि ये भी दक्षिण की ओर चलने के लिए उत्सुक थीं, परन्तु विशालमती जी ने इन्हें यहीं संघ में ही रहने को कहा और अपने साथ मुझे लेकर जयपुर से बम्बई आ गर्इं। यहाँ परम तपस्वी श्री नेमिसागर जी महामुनि के दर्शन किये। मन बहुत ही प्रसन्न हुआ।
बम्बई में उस समय रथ यात्रा का महोत्सव रुका हुआ था, बात यह थी, यहाँ ऐसा वातावरण बन चुका था कि ‘नग्नमुनि शहर में रथयात्रा के साथ नहीं चल सकते हैं।’ इसी बात को लेकर श्री नेमिसागर जी महाराज ने सत्याग्रह कर दिया था और रथयात्रा रोक दी गई थी। शहर के प्रमुख श्रीमान् और धीमान् इस सरकारी आर्डर को हटवाने के लिए प्रयत्नशील थे। क्षुल्लिका विशालमती जी भी इन धर्म प्रभावना के कार्यों में बहुत ही रुचि रखती थीं।
अतएव रथयात्रा निकलने तक हम दोनों ने बम्बई शहर में ही रुकना निश्चित कर लिया। मैंने आचार्य श्री देशभूषण जी महाराज के मुख से अनेक बार सुना था कि सन् १९३१ में जब चारित्र चक्रवर्ती आचार्यश्री शान्तिसागर जी महाराज के संघ का दिल्ली में चातुर्मास था उस समय नग्न मुनियों को सर्वत्र विचरण करने में बाधायें थीं।
अमुक मार्ग से नग्न मुनि नहीं निकल सकते हैं, इतना सुनते ही आचार्यदेव ने अपने संघ के मुनि श्रीr वीरसागर जी, नेमिसागर जी, चन्द्रसागर जी आदि को उन्हीं-उन्हीं रोक के स्थानों में जाने का आदेश दे दिया था और आप स्वयं तो उधर सिंहवृत्ति से विहार किया ही करते थे बल्कि चाँदनी चौक आदि कई स्थानों पर खड़े होकर आचार्य जी ने अपने फोटो भी खिंचवाये थे।
वह इसलिए कि अमुक सन्-संवत् में नग्न दिगम्बर मुनियों का यहाँ पर निराबाध विहार होता रहा है। इस इतिहास को स्थायी रखने के लिए कि जिससे भविष्य में नग्न दिगम्बर मुनियों को कहीं पर भी रोक-टोक न हो सके। निजाम स्टेट-हैदराबाद में आचार्य देशभूषण जी महाराज ने भी नग्न मुनि को विहार से रोकने पर वहीं ध्यान में बैठकर मार्ग प्रशस्त किया था।
यह सभी बातें हमें याद आ गई। क्षुल्लिका विशालमती जी ने भी मुझे अनेक बातें बतार्इं और आगम का भी चिंतन अच्छा हुआ। वास्तव में ये नग्न मुनि नंगे नहीं हैं। (दिक्-दिशा और अम्बर-वस्त्र) अथवा ये हमेशा शीलरूपी वस्त्राभरण से विभूषित हैं, क्योंकि कायर लोग कभी भी यह मुद्रा धारण नहीं कर सकते हैं। महान् वीरों की ही यह मुद्रा है। कवि भूधरदास जी ने बहुत ही अच्छे शब्दों में कहा है-
अंतर विषयवासना बरते बाहर लोकलाज भय भारी।
यातें परमदिगम्बर मुद्रा धरि नहिं सके दीन संसारी।।
ऐसी दुर्धर नगन परीषह जीतें साधु शीलव्रत धारी।
निर्विकार बालक वत् निर्भय तिनके पायन धोक हमारी।।
क्षुल्लिका विशालमती माताजी कहा करती थीं कि- ‘‘यह नग्नमुद्रा ब्रह्मचर्यव्रत की कसौटी है और अपरिग्रह की चरम सीमा है।’’ ‘दूसरी बात यह है कि ‘‘यह नग्नरूप तो सचमुच में प्रकृति प्रदत्त प्राकृतिक रूप है। ठंंडी, गर्मी, डाँस-मच्छर आदि से शरीर की रक्षा के लिए अथवा विकार को छिपाने के लिए अथवा लज्जा के लिए वस्त्र धारण किये जाते हैंं यदि इनमें से सभी पर विजय प्राप्त कर ली गई हो तो पुनः वस्त्रों की क्या आवश्यकता है?
कहने का तात्पर्य यही है कि जब तक शरीर से निर्मम नहीं हुआ जायेगा और जब तक निरतिचार पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत नहीं होगा तथा जब तक निर्विकल्प धर्म-शुक्ल ध्यान नहीं होगा तब तक मुक्ति की प्राप्ति भी नहीं होगी। इसलिए मोक्ष प्राप्त करने के लिए यह नग्नवेश ही-यह दिगम्बर मुनि मुद्रा ही एक साधन है।
यद्यपि इस दुःषमकाल में मोक्ष की प्राप्ति नहीं है, फिर भी पंचम काल के अन्त तक मोक्ष मार्ग चालू रहेगा। तब तक मुनि, आर्यिका और श्रावक, श्राविका आदि चतुर्विध संघ रहेगा। जिस दिन यह संघ समाधि ग्रहण कर लेगा, उसी दिन धर्म का नाश हो जायेगा, राजा का नाश हो जायेगा और अग्नि का भी नाश हो जायेगा अतः जब तक धर्म, राजा और अग्नि हैं तब तक ये यथाजातरूप धारी मुनि इस पृथ्वीतल पर विचरण करते ही रहेंगे। बम्बई शहर में नग्न मुनियों को कहीं भी विहार करने से रोका नहीं जा सकता है, यही भावना जिनके अंतस्थल में थी, ऐसे श्री नेमिसागर जी महाराज ने रथयात्रा रोक दी थी।
उन्हें रथयात्रा के जुलूस में जाने का हठवाद नहीं था, प्रत्युत् नग्न दिगम्बर मुनि रथयात्रा में जुलूस में या अकेले,कैसे भी कहीं भी विहार कर सकते हैं। उन्हें ‘रोकना-बन्धन लगाना’ यह ठीक नहीं है। इसी बन्धन को हटाने के लिए वे कटिबद्ध थे। इतिहास साक्षी है कि जब- ‘‘सुकौशल राजा के पिता राजा सिद्धार्थ महामुनि हो गये थे, रानी ने आदेश निकलवा दिया कि मेरी राजधानी में नग्न मुनि विहार न करें, तब महामुनि सिद्धार्थ ही उस बन्धन को तोड़ने के लिए उस शहर में आ गये थे।’’१
इत्यादि चर्चाओं से क्षुल्लिका विशालमती जी ने उस समय वहाँ के श्रावकों को कर्तव्य पालन में और भी अधिक दृढ़ करने का प्रयास किया था। उस समय मैंने देखा, मुनिश्री नेमिसागर जी महाराज बहुत सरल प्रकृति के साधु थे। उनकी तपश्चर्या महान् थी, शरीर अत्यंत कृश था फिर भी मनोबल विशेष था। मैंने उनकी चर्या में एक और विशेषता देखी थी, जो कि आज तक भी मेरे स्मरण पथ में बनी हुई है। वह यह थी- महाराज जी दिन भर अपने हाथ में माला रखते थे और जाप्य करते रहते थे।
जब कोई चर्चा आ जाती थी तब वे बीच में ही माला छोड़कर उसी बीच की मणि पर उँगली रोककर बात कर लेते थे, पुनः जपने लगते थे। मुझे ऐसा करना बहुत ही आश्चर्य सा लगा। मैं सोचने लगी- ‘‘अहो! ये इतने महान् साधु हैं, ज्ञानी हैं, चारित्र में भी उत्कृष्ट हैं और इन्होंने अपने पूरे जीवन भर आचार्यश्री शांतिसागर जी महाराज का चरण सानिध्य प्राप्त किया है।
वास्तव में सभी शिष्यों की अपेक्षा सबसे अधिक काल तक ये ही अपने गुरु के पास रहे हुए हैं पुनः ये इस प्रकार से जाप्य क्यों कर रहे हैं? बीच-बीच में क्यों बोल देते हैं?’’ मैंने यह अपने मन की आशंका क्षुल्लिका विशालमती जी से कह दी। वे भी प्रायः ऐसे ही दिन भर माला हाथ में रखती थीं और जपा करती थीं। उन्होंने कई तरह से समाधान किया किन्तु संतोष नहीं हुआ। तब उन्होंने कहा- ‘‘अच्छा, चलो, आज मुनिश्री से इस शंका का समाधान करना है।’
महाराज जी के पास पहुँचकर उन्होंने यह मेरा प्रश्न रख दिया, तब महाराज जी ने बहुत ही सरलता से उत्तर दिया- ‘‘अम्मा! मैं कोई गिनती का जाप्य नहीं कर रहा हूँ। दिन भर भगवान का नाम जपना, महामंत्र का स्मरण करते रहना यही मेरा लक्ष्य है। उसके सहयोग के लिए यह माला हाथ में ले लेता हूूँ।
मैं इस पर ‘‘णमो सिद्धाणं’’, मात्र इतने ही मंत्र को जपते रहता हूँ। वह मंत्र हर बार १०८-१०८ हो ही, यह कोई नियम नहीं है। इसलिए बीच-बीच में बोल देता हूँ। जब नियम से करता हूँ तब मौन पूर्वक मन, वचन, काय को संभाल करके ही करता हॅूं। ऐसे ही जब मैं रात्रि में ‘‘जाप’’ करता हूँ तब भी उपयोग को एकाग्र करके ही जाप करता हूँ।’’
उनका यह समाधानजनक उत्तर मुझे अच्छा लगा और मन में स्मरण आया कि ऐसे ही जब कभी आचार्य श्री देशभूषण जी महाराज आसन पर बैठे हुए होते हैं, स्वाध्याय, लेखन अथवा बातचीत नहीं करते हैं उस समय उनके हाथ की भी उँगलियाँ चलती रहती हैं। एक बार किसी के प्रश्न करने पर उन्होंने भी यह बताया था कि- ‘‘मैं महामंत्र का जाप करता रहता हॅूं।’’
इससे यह बात समझ में आ जाती है कि साधुओं को प्रति क्षण उठते, बैठते, चलते-फिरते, बातचीत करते हुए भी मन-मन में महामंत्र का अथवा किसी भी छोटे से मंत्राक्षर का स्मरण करते ही रहना चाहिए। कालांतर में सन् १९५७ में जब महावीरकीर्ति जी आचार्य का चातुर्मास खानिया में आचार्य श्री वीरसागर जी महाराज के सानिध्य में हुआ था, उन दिनों मेरे आहार में अंतराय बहुत आती थी।
तब गुरुदेव कहा करते थे कि- ‘‘ज्ञानमती! तुम आहार को जाते हुए तथा श्रावकों द्वारा नवधा भक्ति के समय, यहाँ तक कि आहार करते समय भी मन-मन में णमोकार मंत्र जपती रहा करो।’’ मैं कहती-‘‘महाराज जी! आहार के लिए जाते हुए तथा वहाँ चौके में बैठे हुए तक तो मंत्र जपा जा सकता है किन्तु आहार करते समयकैसे जपना?’’
उनकी अधिक प्रेरणा से धीरे-धीरे मैंने अनुभव किया कि आहार करते समय भी मन-मन में जपा जा सकता है। यह केवल अभ्यास की बात है। श्री महावीर कीर्ति जी महाराज तो हमेशा कहा करते थे- ‘‘उठते-बैठते, चलते-फिरते, खाते-पीते, सोते-जागते, यहाँ तक कि प्रत्येक कार्य करते समय महामंत्र का जप करते रहना चाहिए।’’
इन सभी प्रसंगों में मुझे वह मुनिश्री नेमिसागर जी का समाधान और उनके हाथ की माला का स्मरण हो ही जाया करता था। आज भी उनकी वह मुद्रा और सरलता मेरे नेत्रों के सामने स्पष्ट झलक आया करती है। मैं समझती हूँ कि उनके उस ‘जप’ का प्रभाव था कि जो जल्दी ही सरकारी विरोध दूर हुआ और ‘नग्न’ मुनि भी रथयात्रा के साथ बम्बई शहर में घूम सकते हैं।’’
दो दिन बाद ही यह स्वीकृति मिली, तब श्रावकों ने बड़े ही उत्साह के साथ महामहोत्सवपूर्वक बम्बई शहर में रथयात्रा का जुलूस निकाला। उस समय जैनधर्म की महती प्रभावना हुई और रानी उर्विला के जैनरथ महोत्सव को जैसे मुनिश्री वङ्काकुमारजी ने निकलवा कर धर्म प्रभावना की थी, वह इतिहास स्मरण हो आया।
मैंने भी वहाँ का सन् १९५४ का वह रथयात्रा महोत्सव देखा, हृदय पुलकित हो उठा, अंतरंग में महामुनि की दृढ़ता के प्रति श्रद्धा बहुत ही वृद्धिंगत हुई। गुरुदेव श्री नेमिसागर जी महाराज के मुख से आचार्यश्री शान्तिसागर जी के विषय में अनेक प्रत्यक्ष अनुभव सुने पुनः वहाँ से निकलकर हम दोनों ‘पूना’ शहर के पास एक ‘बाल्हा’ गाँव में आ गयीं।
यह आर्यिका चन्द्रमती माताजी का शायद जन्म स्थान था। मुनिश्री नेमिसागर जी महाराज जब आचार्यश्री के पास से अलग हुए थे, तब उन्हें गुरु वियोग का अधिक दुःख हो रहा था। उस समय वे इस ‘बाल्हा’ गाँव में ही आकर रहे थे और एक चातुर्मास यहीं पर सम्पन्न किया था। वहाँ के भक्त श्रावक और श्राविकायें महाराजश्री के बारे में अनेक प्रत्यक्ष के अनुभव सुनाने लगे।
अधिकतर बातें इस संदर्भ में ही थीं कि महाराजश्री को इस समय गुरुवियोग बहुत ही दुःखद रहा है। किन्हीं ने कहा कि- ‘‘आचार्यश्री ने अब सल्लेखना के अवसर पर अपने प्रिय शिष्य को भी अलग करना ही उचित समझा, अतः इनकी इच्छा न होते हुए भी इन्हें विहार करने का आदेश दे दिया है।’’ जो भी हो, पूज्य नेमिसागर जी महाराज स्वयं भी बिना इच्छा के ही गुरु के आदेश से अलग हुए थे, यह निश्चित था।
एक वृद्धा महिला ने एक दिन बताया कि- ‘‘मुनिश्री यहाँ मंदिर जी में ध्यान-अध्ययन एवं सामायिक आदि क्रिया करते थे। यहीं मुहल्ले के बच्चे उनके पास आकर बहुत बार इकट्ठे हो जाया करते थे। मुनिश्री की सरल प्रकृति होने से यह नन्हें-नन्हें बालक उनके पास बैठकर निर्भीकता से उनसे वार्तालाप किया करते थे। एक बार की घटना है कि यहाँ का उपाध्याय पंडित मेरे पास में शिकायत लेकर आया कि आप लोग अपने बच्चों को यहाँ आने से रोके।
उसने यह भी बताया कि मध्याह्न में महाराजश्री सामायिक में स्थित थे कदाचित् उनके नेत्रों से अश्रुजल आ गया। एक तीन-चार वर्ष के बालक ने देख लिया और वह मुनिश्री के अश्रु पोंछते हुए बोलने लगा- ‘‘स्वामी जी! आपण कशाला रडता! सांगा आपल्याला काय पाहिजे, माझी आई आपलेला बाटल ते देणार।-हे स्वामी जी! आप क्यों रो रहे हैं?
कहिये! आपको क्या चाहिए? मेरी माँ आपको क्या चाहिए, सो देगी। ऐसे शब्द बोलते हुए बालक को पंडित-पुजारी ने देख लिया, उसने उसी क्षण महाराज जी के पास से बालकों को भगा दिया और मेरे पास आकर सारी स्थिति बता दी। मैंने उसी समय महाराजश्री के पास आकर पूछा-महाराज जी! आज आपके नेत्रों से आँसू कैसे आ गये? क्या कारण है सो आप बताइये।
महाराज जी ने कहा-बाई! आज प्रातःकाल से ही मुझे आचार्यश्री की बहुत ही याद आ रही थी, मैंने बहुत कुछ अपने को समझाया, सान्त्वना दी, किन्तु अकस्मात् सामायिक में बैठे-बैठे ही आँसू आ गये। इतना सुनकर मैंने यही कहा कि महाराज जी! यह मोह ही तो संसार का कारण है।
आप बारह भावना का चिंतवन कीजिये, शांति मिलेगी। महाराज जी तो सरलता की प्रतिमूर्ति ही थे। उन्होंने कहा-हाँ, आपका कहना सच है, फिर भी मोक्षमार्ग में लगाने वाले सच्चे गुरु की यादकैसे भुलाई जा सकती है? इस घटना को सुनकर उस समय क्षुल्लिका विशालमती जी की आँखों में भी आँसू आ गये, वे कहने लगीं-‘‘देखो, वीरमती अम्मा! हम लोग अनादिकाल से माता-पिता, स्त्री, पुत्र, मित्र, धन आदि के लिए रोते हैं किन्तु ऐसे धर्मगुरू के लिए नहीं रोना आया होगा तभी तो स्त्री पर्याय मिली है और पंचम काल जैसे इस निकृष्ट काल में जन्म लेना पड़ा है।
मैंने उस समय विचार किया कि-‘‘बात किसी अंश में सच है। धर्म-प्रेम बगैर गुरु के वियोग में भी भला अश्रुकैसे आ सकते हैं?’’ वास्तव में जो निकट संसारी है वही गुरु का सानिध्य सतत चाहेगा, अन्यथा स्वच्छन्द बनने में आनन्द मानेगा। यह गुरु-प्रेम का उदाहरण आज के एकल विहारी साधुओं के लिए ग्राह्य है।
जिस समय आचार्यश्री वीरसागर जी महाराज की सल्लेखना हुई थी, कितना ही मन मजबूत करने पर भी मेरी आँखों में अकस्मात् आँसू आ गये थे और ऐसा झटका सा लगा था कि- ‘‘अहो! अब इन वीतरागी गुरु की देशना का लाभ, उनके आदेश का लाभ हमें जीवन में कभी नहीं मिलेगा।’’
ऐसे ही जब मैंने श्रवणबेलगोला से विहार किया था, इसके पूर्व वहाँ मैं एक वर्ष तक रह चुकी थी अतः विहार करने के बाद रह रहकर भगवान बाहुबली की प्रतिमा दृष्टि के सन्मुख दिखती रहती थी और बरबस ही नेत्रों से अश्रु गिरने लगते थे। ऐसा लगता था कि अब मुझे इस जीवन में ऐसी महिमामयी विशालकाय मूर्ति के दर्शन नहीं हो सकेगे। ये नेमिसागर जी महाराज महान् तपस्वी थे। सदा ही एक उपवास और एक पारणा करते थे।
आहार में प्रायः सब रस का त्याग रहता था। बहुत ही शांत प्रकृति के थे। उन्होंने बम्बई शहर में आचार्यश्री के स्मरण को चिरस्थायी करने के लिए ‘तीनमूर्ति पोदनपुर’ नाम से एक पावन तीर्थ ही बनवा दिया है। इस महान् कार्य में उन्हें यहाँ पर लगभग २० वर्ष तक रहना पड़ा है। उनकी सहनशीलता और गुरुभक्ति बहुत ही विशेष थी।
सन् १९७१ में उन्होंने सल्लेखना विधि से इस नश्वर शरीर को छोड़कर स्वर्ग में गुरु का सानिध्य अवश्य ही पा लिया होगा, ऐसा कहने में मुझे किंचित् संकोच या संदेह नहीं है। यहाँ से निकलते ही मैंने अम्मा से कहा-‘‘अब मुझे आप शीघ्र ही चारित्र चक्रवर्ती आचार्यश्री के दर्शन करा दो, बाद में अन्यत्र कहीं चलना है।’’ अतः उन्होंने आचार्यश्री कहाँ हैं? यह पता लगाकर नीरा गाँव की ओर प्रस्थान कर दिया।