१४ वर्षों का लम्बा अंतराल, आचार्य परम्परा का विवाद
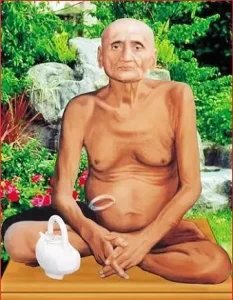
(ज्ञानमती माताजी की आत्मकथा)
१४ वर्षों का लम्बा अंतराल-अप्रैल सन् १९८० तक मैंने अपनी स्मृतियों के आधार पर जो खट्टे-मीठे अनुभव इस पुस्तक में प्रस्तुत किये, उन्हें पढ़कर सैकड़ों पाठकों ने अपने दैनिक जीवन में लाभ उठाया, सामाजिक कार्यकलापों के लिए लोगों ने प्रेरणा प्राप्त की, धर्मप्रभावना के क्षेत्र में अनेक युवक-युवतियों ने प्रगति की तथा कई मुनि-आर्यिकाओं ने भी इस कृति को अपने जीवन का आधार बनाया, यह उनके पत्रों एवं वार्ताओं से जानकर मुझे अत्यधिक प्रसन्नता हुई और मैंने अनिच्छापूर्वक भी किये गये अपने लेखन परिश्रम को सार्थक माना।
पहले भी संघस्थ शिष्य-शिष्याओं एवं कतिपय विद्वानों के आग्रह पर ही मैंने किसी तरह अपने ३५-४० वर्ष के अनुभवों को लेखनीबद्ध किया था और अब भी जब वीर ज्ञानोदय ग्रन्थमाला इसका दूसरा संस्करण प्रकाशित कर रहा है, मेरे पास पुनः पुनः आर्यिका चंदनामती ने निवेदन शुरू कर दिया कि माताजी! आप चाहे संक्षेप में लिखें किन्तु ‘मेरी स्मृतियाँ’ के इस द्वितीय संस्करण में आगे का प्रकरण अवश्य पूरा कर दें। इससे पूर्व भी कई बार डा. शेखरचंद्र जैन-अहमदाबाद एवं कुछ विद्वानों ने, श्रावकों ने इसी प्रकार का निवेदन किया था किन्तु मेरा मूड नहीं बन पाता था।
मैं सबसे यही कह देती थी कि षट्खण्डागम सूत्रों की संस्कृत टीका लिखने में मुझे बहुत आनंद आता है, उससे आत्मिक तृप्ति मिलती है अतः अब मुझसे मेरी स्मृतियाँ (आत्मकथा) लिखने की बात मत कहा करो पुनः एक दिन (१८ मई २००४ को) कुण्डलपुर में मेरे दर्शनार्थ पधारे प्राचार्य श्री नरेन्द्र प्रकाश जैन-फिरोजाबाद ने मुझसे पूछा कि माताजी! आप अपनी आगे की आत्मकथा कब प्रकाशित करवा रही हैं?
उनसे जब मैंने यह कहा कि उसे तो मैंने अभी लिखा ही नहीं है तब उन्होंने भी आग्रहपूर्वक आगे का लेखन कार्य करने हेतु निवेदन किया। इन्हीं प्रेरणाओं ने ही शायद मेरी लेखनी को दुबारा चलने को मजबूर कर दिया है किन्तु मैं स्वयं नहीं समझ पा रही हूँ कि कितने दिन यह लेखनी चल पाएगी, क्योंकि अब ७० वर्ष की आयु में जहाँ शारीरिक शक्ति अत्यन्त क्षीण हुई है, वहीं षट्खण्डागम की सोलहों पुस्तकों के सूत्रों की टीका लिखने की तीव्र अभिलाषा है इसीलिए मेरी दृष्टि में इस लेखन की अपेक्षा षट्खण्डागम लेखन का महत्व अधिक रहता है।
मेरी स्मृतियाँ का लेखन छूटने का दूसरा कारण यह भी रहा कि अपने बारे में कुछ भी लिखते हुए मुझे कभी-कभी आत्मप्रशंसा जैसा लगने लगता है अतः मैं अपनी दृढ़ता और सफलता अथवा दूसरों के द्वारा किये जाने वाले भक्तिपरक मूल्यांकन को भी अति अल्प शब्दों में प्रगट कर पाती हूँ।
इसी प्रकार अच्छे कार्यों में भी ईर्ष्यावश दूसरों के द्वारा किये गये अपकार या प्रस्तुत किये गये विघ्नों का प्रस्तुतीकरण भी अति कठिन तो होता ही है, उसे याद करके मन में अंशमात्र भी क्षोभ, द्वेष न आ जावे, इस बात की चिंता बनी रहती है तथा ज्यों का त्यों लिखने में परनिन्दा जैसा अर्थ न प्रगट हो, यह ध्यान रखना भी आवश्यक होता है।
आचार्य परम्परा का विवाद
जैसा कि मैंने पूर्व के अपने लेखन में चारित्रचक्रवर्ती आचार्य श्री शांतिसागर जी महाराज की वंशावली में निर्दोष आचार्य परम्परा का किंचित् वर्णन किया है कि चतुर्थ पट्टाचार्य श्री अजितसागर जी महाराज की भीषण अस्वस्थता के कारण संघ परम्परा में वयोवृद्ध मुनि आचार्यकल्प श्री श्रेयांससागर महाराज को सभी लोग पंचम पट्टाचार्य के पद पर अभिषिक्त करना चाहते हैं।
आखिर दुर्योग से ९ मई १९९० वैशाख शु. पूर्णिमा को साबला (राजस्थान) में आचार्य श्री अजितसागर जी महाराज की समाधि हो गई, उसके बाद आचार्यपट्ट के विषय में सम्पूर्ण चतुर्विध संघ के अन्दर भारी विवाद रहा। संघ के ८० प्रतिशत साधु-साध्वियों ने मिलकर लोहारिया (राज.) में वरिष्ठता, ज्ञान एवं दीर्घकालीन तपस्या के आधार पर १० जून १९९० को आचार्यकल्प श्रेयांससागर महाराज को पंचम पट्टाचार्य पद प्रदान किया
इसके अतिरिक्त २४ जून १९९० को महासभा नामक संस्था के अध्यक्ष निर्मल कुमार जैन सेठी द्वारा प्रस्तुत किये गये एक गोपनीय पत्र के आधार पर कतिपय श्रेष्ठियों और साधुओं ने संघस्थ मुनि श्री वर्धमानसागर जी को भी पंचम पट्टाचार्य पद प्रदान कर दिया। इस प्रकार सन् १९२४ से चल रही चारित्रचक्रवर्ती की अखण्ड आचार्य परम्परा सन् १९९० में खण्डित होकर दो पंचम पट्टाचार्यों में विभक्त हो गई। इस आचार्य परम्परा का सही विवरण समय-समय पर ‘‘सम्यग्ज्ञान’’ मासिक पत्रिका में प्रकाशित होता रहा है।
मैं यहाँ उसका विश्लेषण न करके मात्र इतना ही कहूँगी कि चारित्रचक्रवर्ती की इस निर्दोष परम्परा में जब तक किसी हठाग्रही श्रावक ने अधिकार नहीं जमाया था, तब तक वह परम्परा पूर्ण शालीन और गौरवपूर्ण ढंग से चलती रही पुनः अब संस्थाओं एवं श्रेष्ठियों के प्रवेश से संघ का विभाजन देखकर मुझे एवं अनेक वरिष्ठ साधु-साध्वियों के हृदय को अत्यन्त आघात पहुँचा है अतः श्रावकों के लिए मेरी यही प्रेरणा है
कि साधु संघों में जाकर उनकी भक्ति, वैयावृत्ति आदि खूब करें किन्तु उन्हें पद या धन की लिप्सा में फंसाकर संघ को तोड़ने-फोड़ने का पुरुषार्थ कभी न करें जिससे कि सदैव संतों की कृपा दृष्टि से जीवन सुखी बना रहे। वर्तमान में पंचम पट्टाचार्य (प्रथम) के स्वर्गारोहण के पश्चात् सन् १९९२ से षष्ठम पट्टाचार्य के रूप में पूज्य आचार्य श्री अभिनंदनसागर जी महाराज चतुर्विध संघ के साथ उस पट्ट परम्परा का संरक्षण कर रहे हैं तथा पूज्य आचार्यश्री वर्धमानसागर महाराज (पंचम पट्टाचार्य द्वितीय) भी उस परम्परा का संचालन कर रहे हैं।
विवाद सुलझा
१४ मार्च १९९७ में आखिर वह पुण्य दिवस भी आया जब उदयपुर (राज.) से आचार्य श्री अभिनंदनसागर महाराज एवं भिण्डर (राज.) से आचार्य श्री वर्धमानसागर महाराज अपने-अपने संघ के साथ अतिशयक्षेत्र ‘‘अडिन्दा पार्श्वनाथ’’ तीर्थ पर पहुँचे। उस समय मैं अपने संघ के साथ मांगीतुंगी से दिल्ली की ओर विहार कर रही थी।
रास्ते में ब्र. रवीन्द्र जी ने आकर कहा कि संघ से मुझे बुलाने हेतु फोन आया है और ब्र. सूरजमल बाबाजी ने भी मुझे आग्रहपूर्वक कहा है कि मैं अस्वस्थतावश नहीं जा पाऊँगा सो तुम अवश्य जाकर आपसी विवाद को सुलझा कर आओ, तुम जैसा भी निर्णय करके आओगे, मुझे मान्य होगा। मुझे तो इस दिन का इंतजार था ही अतः मैंने रवीन्द्र कुमार को कहा कि तुम शीघ्र जाओ और कुछ न कुछ अन्तिम निर्णय करवा कर ही आना।
रवीन्द्र कुमार तुरंत मेरी आज्ञा लेकर अडिन्दा चले गये पुनः १५ मार्च १९९७ को जयपुर शहर में मेरा प्रवेश हो रहा था, तब रवीन्द्र जी ने अडिन्दा से वापस आकर मुझे बताया कि दोनों आचार्यों ने आपस में वार्ता करके हम लोगों के समक्ष निर्णय किया है कि अब दोनों ही आचार्यों के नाम के आगे पंचम या षष्ठम पद का प्रयोग नहीं किया जायेगा। सारी रिपोर्ट सुनकर मैंने यही कहा कि चलो! ठीक है, किसी तरह से पारस्परिक विद्वेष समाप्त होना ही चाहिए था।
मुझे तो यूँ भी न वर्धमानसागर महाराज से कभी द्वेष रहा है और न ही अभिनंदन सागर जी से राग, दोनों आचार्य प्रारंभ से ही मुझे माँ के रूप में मानते रहे हैं और मेरे से अनेकों ग्रंथों का अध्ययन किया है अत: मेरी यही भावना है कि चारित्र चक्रवर्ती परम्परा की निर्दोष संयमधारा को प्रवाहित करने में अपना योगदान देते रहें तथा पारस्परिक संघ वात्सल्य अवश्य बनाये रखें तभी समाज को आपस में जोड़ने की शिक्षा दी जा सकती है।
मुनिचर्या ग्रंथ के लेखन की आवश्यकता क्यों पड़ी?
सन् १९९१ में मैंने सरधना (मेरठ-उ.प्र.) ससंघ चातुर्मास किया। वहाँ मुनि-आर्यिकाओं की चर्या से संबंधित प्रतिक्रमण सूत्रों का मैं हिन्दी पद्यानुवाद कर रही थी, तब मैंने अनुभव किया कि अन्य भक्तिपाठ की नूतन पुस्तकों में किये गये अनेक संशोधन आर्षमार्ग के संरक्षण में अत्यन्त घातक हैं।
यदि संशोधन की यही परम्परा चलती रही तो हमारे पूर्वाचार्यों की वास्तविक वाणी ही समाप्त हो जायेगी और उसके अध्ययन से प्राप्त होने वाला पुण्य भी कैसे प्राप्त होगा? मैं यहाँ प्रसंगानुसार कतिपय विषयों को पाठकों की जानकारी हेतु प्रस्तुत करती हूँ जिससे वस्तुस्थिति स्पष्ट हो सकेगी।
सामायिक दण्डक और थोस्सामिस्तव
कृतिकर्म की विधि मूलाचार ग्रंथ के आधार से मुनिचर्या में दी गई है उसमें सामायिक दंडक और थोस्सामिस्तव को ही पढ़ना होता है। मुनिचर्या ग्रंथ में पृ. ७, १००, २९६ पर ऐसे तीन बार सामायिक दंडक पाठ आया है और पृ. १०, १०२, ३०० पेज पर तीन बार थोस्सामिस्तव पाठ आया है। सामायिक दंडक में पाठ भेद को ध्यान में रखना चाहिए।
मुनिचर्या पृ. क्रियाकलाप पृ. पच्चक्खामि णिंदामि गरहामि अप्पाणं ९ पच्चक्खामि णिंदामि गरहामि अप्पाणं १५ पच्चक्खामि णिंदामि गरहामि अप्पाणं २९६ पच्चक्खामि णिंदामि गरहामि अप्पाणं ९० पडिक्कमामि णिंदामि गरहामि अप्पाणं १०२ पडिक्कमामि णिंदामि गरहामि अप्पाणं १४६ पडिक्कमामि णिंदामि गरहामि अप्पाणं १२६क्रियाकलाप में तृतीय पाठ की टीका भी है अतः ये सभी पाठ प्रामाणिक हैं
इन्हें गलत नहीं समझना चाहिए। ‘‘जीवियमरणे लाहालाहे.’’ यह टीकाकार का श्लोक है अतः इसे सामायिक दंडक के मूलपाठ में नहीं जोड़ना चाहिए। थोस्सामिस्तव में ‘‘वंदामि रिट्ठणेमिं’’ पाठ गलत नहीं है। रिट्ठणेमिं का अरिष्टनेमि अर्थ ही निकलेगा।
लघु कृतिकर्म विधि
प्रत्येक भक्तिपाठ की प्रतिज्ञा में सामायिक दंडक व थोस्सामि पढ़ना आवश्यक है। लघुभक्तिपाठ में या कभी समयाभाव में इनको पढ़ने में प्रमाद आ सकता है अतः विधि की पूर्ति के लिए मुनिचर्या पुस्तक में लघु सामायिक दंडक और लघु थोस्सामि पाठ भी पृ. १२-१३ पर दिया है। यह लघु पाठ मैंने प्रतिष्ठातिलक ग्रंथ१ से लिया है अतः प्रामाणिक है।
करोम्यहं- आजकल कुछ साधु-साध्वियाँ ‘‘कुर्वेऽहं’’ क्रिया को पढ़ने लगे हैं किन्तु मुझे यह संशोधन नहीं जंचा है अतः मैंने यहाँ ‘करोम्यहं’’ ऐसा आचार्य प्रणीत प्राचीनपाठ ही सर्वत्र रखा है। सिद्धांतचक्रवर्ती श्रीवीरनंदि आचार्य ने आचारसार ग्रंथ में ‘‘करोम्यहं’’ पाठ ही लिया है। यथा-
‘‘क्रियायामस्यां व्युत्सर्गं भत्तेरस्याः करोम्यहं२।’’
अनगार धर्मामृत में पाक्षिक प्रतिक्रमण के लक्षण की स्वोपज्ञटीका में ‘‘करोम्यहं’’ क्रिया का प्रयोग पन्द्रह बार आया है। उदाहरण के लिए देखिए-
‘‘सर्वातिचारविशुद्ध्यर्थं पाक्षिकप्रतिक्रमणक्रियायां सिद्धभक्तिकायोत्सर्गं करोम्यहं।’’
इत्यादि। क्रियाकलाप में देववंदना, दैवसिक प्रतिक्रमण, पाक्षिकप्रतिक्रमण एवं अन्य क्रियाओं की प्रयोगविधि में ‘‘करोम्यहं’’ पाठ ही उपलब्ध है।
चारित्रसार ग्रंथ में भी-‘‘चैत्यभक्तिकायोत्सर्गं करोमीति विज्ञाप्य इत्यादि पाठों में ‘‘करोमि’’ क्रिया ही है। ऐसे ही सामायिक भाष्य ग्रंथ एवं प्रतिष्ठातिलक ग्रंथ में भी ‘‘करोमि, करोम्यहं’’ पाठ ही उपलब्ध हो रहे हैं। कुल मिलाकर सभी ग्रंथों में इस परस्मैपदी ‘‘करोमि’’ क्रिया की ही उपलब्धि हो रही है पुनः इसे बदलकर ‘‘कुर्वेऽहं’’ पाठ क्यों रखा गया ? यह विचारणीय है।
भक्तियों एवं प्रतिक्रमण सूत्रों के कत्र्ता
चैत्यभक्ति, वीरभक्ति तथा दैवसिक-रात्रिक प्रतिक्रमण एवं पाक्षिकादिप्रतिक्रमण इन दोनों प्रतिक्रमणों में प्रतिक्रमणभक्ति और प्रतिक्रमण दंडक सूत्र इनके रचयिता श्री गौतमगणधर देव हैं ऐसा इनके टीकाकार श्री प्रभाचन्द्राचार्य ने माना है।
यथा-श्री गौतमस्वामी मुनीनांदुष्षमकाले दुष्परिणामादिभिः प्रतिदिनमुपार्जितस्य कर्मणो विशुद्ध्यर्थं प्रतिक्रमणलक्षणमुपायं विदधानस्तदादौ मंगलार्थमिष्टदेवताविशेषं नमस्करोति श्रीमते वर्धमानाय नमो नमितविद्विषे।’’ इत्यादि।
सहस्रनाम के टीकाकार श्री अमर मुनिराज ने वीरभक्ति को भी श्री गौतमस्वामी कृत कहा है। सिद्धभक्ति आदि सभी संस्कृत और प्राकृत भक्तियों के टीकाकार श्री प्रभाचन्द्राचार्य ने लिखा है कि-
‘‘संस्कृताः सर्वा भक्तयः पादपूज्यस्वामीकृताः प्राकृतास्तु कुन्दकुन्दचार्यकृताः।’’ संस्कृत की-
| १. सिद्धभक्ति | २. श्रुतभक्ति |
| ३. चारित्रभक्ति | ४. योगिभक्ति |
| ५. आचार्यभक्ति | ६. निर्वाणभक्ति |
| ७. नंदीश्वरभक्ति |
८. शांतिभक्ति
|
ये आठ भक्तियाँ आचार्य श्री पादपूज्य-पूज्यपाद स्वामी द्वारा रचित हैं। शांतिभक्ति के आठ श्लोक के बाद ‘‘शांतिजिनं शशिनिर्मलवक्त्रं’’ इत्यादि श्लोक श्रीपूज्यपाद स्वामी के नहीं हैं ऐसा पं. पन्नालाल जी सोनी ने लिखा है।
संस्कृत की चतुर्विंशतितीर्थंकरभक्ति एवं समाधिभक्ति को भी श्रीपूज्यपादस्वामी कृत एवं ‘‘निःसंगोऽहं जिनानां. इत्यादि ईर्यापथशुद्धि (भक्ति) को भी कुछ विद्वान् श्री पूज्यपाद स्वामी कृत ही मानते हैं।
| १. प्राकृतसिद्धभक्ति | २. श्रुतभक्ति |
| ३. चारित्रभक्ति | ४. योगिभक्ति |
| ५. आचार्यभक्ति |
ये पाँच प्राकृत भक्तियाँ ही श्रीकुन्दकुन्ददेव रचित हैं ऐसा पं. पन्नालाल सोनी ने लिखा है। वे प्राकृत निर्वाणभक्ति के बारे में संदिग्ध थे किन्तु कुन्दकुन्दभारती ग्रंथ में पं. पन्नालाल साहित्याचार्य ने पांचों भक्तियों के साथ,
| ६. प्राकृत निर्वाणभक्ति | ७. प्राकृत पंचमहागुरुभक्ति |
| ८. प्राकृत चतुर्विंशतितीर्थंकरभक्ति (थोस्सामि हं जिणवरे में अंचलिका जोड़कर) | ९. नंदीश्वर भक्ति (अंचलिका मात्र) |
| १०. शांतिभक्ति |
(अंचलिका मात्र) को लेकर ऐसी दश भक्तियों को श्रीकुन्दकुन्ददेव कृत माना है। इन भक्तियों का पद्यानुवाद-भावानुवाद मेरे द्वारा किया हुआ है।
लघु भक्तियाँ
बृहद् भक्तियों के किन्हीं खास श्लोकों को लेकर अंचलिका दे देने से भी लधु भक्तियाँ बन जाती हैं। जैसे चारित्रभक्ति में- व्रतसमुदयमूलः संयमस्वंधबंधो३।
इत्यदि अथवा तिस्रः सत्तमगुप्तयस्तनुमनो इत्यादि एक श्लोक पढ़कर अंचलिका बोलना, लघु चारित्र भक्ति बन गई है। श्रुतभक्ति में भी- ‘‘श्रुतमपि जिनवरविहितं ।’’ मात्र एक श्लोक बृहद्भक्ति से लेकर अंचलिका जोड़कर लघु श्रुतभक्ति हो गई है। अन्य सभी लघु भक्तियाँ प्रायः क्षेपक श्लोकों को पढ़कर अंचलिका पढ़ लेने से हो जाती हैं।
जैसे-‘‘प्रावृट्काले ’’ इत्यादि से लघु योगिभक्ति बन गई है। मुनिचर्या ग्रंथ में क्रियाकलाप और प्रतिष्ठातिलक के आधार से लघु भक्तियों को दिया गया है। निर्वाणभक्ति, नंदीश्वरभक्ति, चैत्यभक्ति, आचार्यभक्ति, शांतिभक्ति और समाधिभक्ति के क्षेपक श्लोक ‘‘भक्त्यादिक्रियासंग्रह’’ पुस्तक से लिए गये हैं। श्रुतभक्ति के क्षेपक श्लोक मेरे द्वारा संकलित हैं।
’ वर्षायोगप्रतिष्ठापनक्रिया में ‘‘स्वयंभुवा भूतहितेन’’ इत्यादि रूप से श्रीऋषभदेव से लेकर श्रीचंद्रप्रभ भगवान तक जो आठ स्तुतियाँ हैं, वे श्रीसमंतभद्रस्वामी विरचित हैं। आहार प्रत्याख्यान कब करना? मुनि-आर्यिकाएं आहार के लिए निकलते समय आचार्य के पास लघु सिद्धभक्ति और लघु योगिभक्ति पढ़कर प्रत्याख्यान निष्ठापन कर आहार को जावें ऐसा कथन न तो क्रियाकलाप, मूलाचार, अनगारधर्मामृत आदि में ही है और न चारित्रचक्रवर्ती आचार्यश्री शांतिसागर जी की परम्परा में ही रहा है। मैंने सन् १९५६-५७ में आचार्यश्री वीरसागरजी का चरणसानिध्य पाया है।
सन् १९५७ से १९६२ तक पुनः १९६८ से १९६९ में समाधि होने तक पूज्य शिवसागरजी के संघ में रही हूँ। अनन्तर आचार्य श्रीधर्मसागर जी के आचार्यत्व काल में सन् १९७५ तक उनके संघ का लाभ प्राप्त किया है। न तो इन आचार्यों ने कभी ऐसा आदेश ही दिया था और न कभी ऐसी क्रिया उनके सानिध्य में हुई थी फिर भी यह परम्परा कैसे चल पड़ी और ‘श्रमणचर्या’ में कैसे लिखी गई, कौन जाने? ‘मुनिचर्या’ में पृ. १४७ से पृ. १५४ तक आगम आधार से यह प्रत्याख्यान विधि स्पष्ट की गई है।
दैवसिक प्रतिक्रमण
दैवसिक-रात्रिक प्रतिक्रमण क्रियाकलाप से लिया है। संस्कृत छाया भी क्रियाकलाप से ही ली है। भावरूप पद्यानुवाद मेरे द्वारा रचित है। इस प्रतिक्रमण में जो कुछ संशोधन पाठ हैं उन्हें प्रायः कोष्ठक में रखा है या टिप्पण में दे दिया है, मूल में कहीं एक-दो जगह परिवर्तन है सो यह परिवर्तन प्रतिक्रमण ग्रंथत्रयी के आधार से ही है।
मन से मैंने कहीं भी परिवर्तन या संशोधन नहीं किया है। ‘‘इच्छामि भंते! चरित्तायारो पाँचों दंडकों में से चार दंडकों में ‘‘तेसिं उद्दावणं’’ पाठ हैं, पाँचवें में ‘‘एदेसिं उद्दावणं’’ पाठ है। तेसिं का अर्थ तेषां और एदेसिं का अर्थ एतेषां है। दोनों में अर्थ भेद नहीं है फिर भी प्रतिक्रमणग्रंथत्रयी में इन दोनों पाठों का ही अर्थ किया है१। अतः मैंने कई एक साधुओं के कहने पर भी एकरूपता रखने के लिए पाठ नहीं बदला है यथास्थान दोनों पाठ हैं।
आजकल ‘‘श्रमणचर्या’’ आदि आधुनिक कई एक पुस्तकों में बहुत से पाठ बदले गये हैं। जैसे कि वीरभक्ति के अंतिम श्लोक का तृतीय चरण बदल दिया गया है। जो कि ऐसा है- क्रियाकलाप पृ. श्रमणचर्या पृ. देवा वि तस्स पणमंति ६६ देवा वि तं णमंसंति ४० प्रतिक्रमणग्रंथत्रयी में टीकाकार ने यही क्रियाकलाप वाला पाठ रखकर इसी की टीका की है।
जैसे- ‘‘देवा वि तस्स पणमंति-देवा अपि तस्य प्रणमंति।’’
ऐसे ही अनेक संशोधन वर्तमान में किये जा रहे हैं किन्तु विचार करने की बात है कि इन टीकाकार प्रभाचंद्राचार्य तक तो यह प्राचीन पाठ ही प्रमाणभूत माना गया है और श्रीटीकाकार भी प्राकृत-संस्कृत व्याकरण व छंद शास्त्रादि के ज्ञाता अवश्य थे फिर भी उन्होंने यह पाठ नहीं बदला है। आजकल ऐसे ही अनेक संशोधन हुए हैं जो कि हमें इष्ट नहीं हैं।
पूर्वाचार्यों ने भी जहाँ कहीं पाठभेद देखे या जहाँ कहीं किसी विषय में मतभेद देखा, तो उसमें से एक को हटाकर दूसरे को प्रामाणिक कहने का साहस नहीं किया, बल्कि दोनों को ही मानने का उपदेश दिया है। षट्खंडागम की धवला टीका में श्री वीरसेनाचार्य ने तो एक जगह यहाँ तक कह दिया
कि ‘‘श्री एलाचार्य के वत्स-शिष्य को इस विषय में-यह प्रामाणिक है और यह अप्रामाणिक, ऐसी जबान नहीं चलाना चाहिए।’ इत्यादि। आज भी विद्वान या ‘साधु-साध्वियों’ को पाठ परिवर्तन आदि कार्य नहीं करना चाहिए। प्रत्युत् पापभीरुता रखते हुए प्राचीन पाठ को ही प्रमाण मानना चाहिए।
क्रियाकलाप
मुनिचर्या ग्रंथ का संपादन और प्रकाशन पं. पन्नालाल सोनी ने चारित्रचक्रवर्ती आचार्य श्री शांतिसागर जी की एवं संघस्थ मुनियों की प्रेरणा से वीर नि. सं. २४६२ में किया था। उन्होंने प्राप्त हस्तलिखित गुटका के आधार से और अनगारधर्मामृत के आधार से ही इसे संकलित किया था, ऐसा वे स्वयं कहा करते थे
अतः यह क्रियाकलाप एक प्रामाणिक ग्रंथ है। आज यह उपलब्ध नहीं है फिर भी साधुओं को इसे प्राप्त कर अवश्य देखना चाहिए व पुनः प्रकाशित कराना चाहिए।
प्रतिक्रमण ग्रन्थत्रयी
इसे श्रीजिनसेनभट्टारक ने वीर नि. सं. २४७३ में चारित्रचक्रवर्ती आचार्य शांतिसागर दिगम्बर जैन जिनवाणी जीर्णोद्धारक संस्था से प्रकाशित किया है। पं. मोतीचंद गौतमचंद कोठारी, एम.ए. फलटण इसके संपादक थे। इसमें दैवसिक-रात्रिक, पाक्षिक और अष्टमी इन तीन प्रतिक्रमण सूत्रों पर श्रीप्रभाचन्द्राचार्य विरचित टीका है।
श्रीप्रभाचन्द्राचार्य ने इन प्रतिक्रमण दंडक सूत्रों को श्रीगौतमस्वामी विरचित कहा है। इसमें तीन प्रतिक्रमण होने से ही इसका ‘प्रतिक्रमण ग्रंथत्रयी’ यह सार्थक नाम है। विद्वान् साधुओं को इसका स्वाध्याय अवश्य करना चाहिए, इसका पुनर्मुद्रण भी अति आवश्यक प्रतीत होता है।
अष्टमी का प्रतिक्रमण
यह पाठ पाक्षिक प्रतिक्रमण से लिया गया है। अनगारधर्मामृत में सालोचना चारित्रभक्ति-चारित्रालोचना सहित चारित्रभक्ति पढ़ने का विधान है। प्रतिक्रमण ग्रंथत्रयी में भी अष्टमी के प्रतिक्रमण को पृथक् लिया है। इस ही आधारों से अष्टमी की क्रिया में यह प्रतिक्रमण जोड़ा गया है। इसकी छाया ‘‘भक्त्यादि क्रियासंग्रह’’ पुस्तक में ली है और पद्यानुवाद मेरे द्वारा रचित है। अष्टमी और पाक्षिक प्रतिक्रमण में चारित्रभक्ति के पश्चात् चारित्रालोचना के अंत में दंडक सूत्र हैं-
णवसु बंभचरगुत्तीसु, चउसु सण्णासु, चउसु पच्चएसु, दोसु अट्टरुद्दसंकिलेसपरिणामेसु, तीसु अप्पसत्थसंकिलेसपरिणामेसु, मिच्छाणाणमिच्छादंसणमिच्छाचरित्तेसु, चउसु उवसग्गेसु, पंचसुचरित्तेसु, छसु जीवणिकाएसु, छसु आवासएसु, सत्तसु भएसु, अट्ठसु सुद्धीसु (णवसु बंभचेरगुत्तीसु) दससु समणधम्मेसु, दससु धम्मज्झाणेसु, दससु मुंडेसु, बारसेसु संजमेसु, बावीसाए परीसहेसु,पणवीसाए भावणासु, पणवीसाए किरियासु, अट्ठारससीलसहस्सेसु, चउरासीदिगुणसयसहस्सेसु, मूलगुणेसु, उत्तरगुणेसु, अट्ठमयम्मि पक्खियम्मि (चउमासियम्मि संवच्छरियम्मि) अइक्कमो वदिक्कमो अइचारो अणाचारो आभोगो अणाभोगो जो तं पडिक्कमामि मए पडिक्कंतं, तस्स मे सम्मत्तमरणं समाहिमरणं पंडियमरणं वीरियमरणं दुक्खक्खओ कम्मक्खओ बोहिलाओ सुगइगमणं समाहिमरणं जिणगुणसंपत्ती होउ मज्झं।।१४।।
‘‘श्रमणचर्या’ आदि नई पुस्तकों में इसमें भी परिवर्तन कर दिया है।
यथा- दोसु अट्ट-रूद्द-संकिलेस-परिणामेसु, तीसु अप्पसत्थ-संकिलेसपरिणामेसु, मिच्छाणाण-मिच्छादंसण-मिच्छाचरित्तेसु, चउसु उवसग्गेसु, चउसु सण्णासु, चउसु पच्चएसु, पंचसु चरित्तेसु, छसु जीव-णिकाएसु, छसु आवासएसु, सत्तसु भयेसु, अट्ठसु सुद्धीसु, णवसु बंभचेर-गुत्तीसु, दससु समण-धम्मेसु, दससु धम्मज्झाणेसु, दससु मुंडेसु, बारसेसु संजमेसु, बावीसाए परीसहेसु, पणवीसाए भावणासु, पणवीसाए किरियासु अट्ठारससील-सहस्सेसु, चउरासी-गुण-सय-सहस्सेसु मूलगुणेसु, उत्तरगुणेसु (अट्ठमियम्मि) (पक्खियम्मि), (चउमासियम्मि), (संवच्छरियम्मि)-अदिक्कमो, वदिक्कमो, अइचारो, अणाचारो, आभोगो, अणाभोगो जो तं पडिक्कमामि।
मए पडिक्वंतं तस्स मे सम्मत्त-मरणं, पंडियमरणं, वीरिय-मरणं, दुक्खक्खओ, कम्मक्खओ, बोहिलाहो, सुगइ-गमणं, समाहिमरणं, जिणगुणसम्पत्ति होउ मज्झं।।
क्रियाकलाप आदि सभी पुस्तकों में ‘णवसु’ से ही पाठ प्रारंभ है। प्रतिक्रमणग्रंथत्रयी टीका ग्रंथ में भी पृ. १८६ से १९४ तक ‘णवसु’ से ही प्रारंभ हुआ है। अतः प्राचीन पाठ ही प्रामाणिक है।
पाक्षिक प्रतिक्रमण
पाक्षिक प्रतिक्रमण में भी पच्चीसों स्थान पर पाठ परिवर्तित हैं। वे प्रतिक्रमणग्रंथत्रयी टीका ग्रंथ से भी असंगत हैं। कुछ प्रकरण टीका ग्रंथ में नहीं हैं उन्हें क्रियाकलाप के आधार से ज्यों की त्यों पढ़ना ही मुझे उचित प्रतीत होता है। पाठ बदलने से उसका मूलरूप ही समाप्त हो जायेगा। उदाहरण के लिए देखिये-
विचारणीय-पाठ परिवर्तन
इसी प्रतिक्रमण में वीरभक्ति के पहले श्रावकों के व्रतों का वर्णन करके उनके फल को कहते हुए दंडक सूत्र है- ‘जो एदाइं वदाइं धरेइ सावया सावियाओ वा खुड्ढया खुड्ढियाओ वा अट्ठदहभवणवासियवाणविंतर जोइसियसोहम्मीसाणदेवीओ वदिक्कमित्तउवरिमअण्णदरमहड्ढियासु देवेसु उववज्जंति।
जो श्रावक या श्राविका अथवा क्षुल्लक या क्षुल्लिका इन उपर्युक्त बारह व्रतों को या ग्यारह प्रतिमाओं को धारण करते हैं वे अठारह (स्थान) को भवनवासी, वान व्यंतर, ज्योतिषी और सौधर्म-ईशान स्वर्ग की देवियों को छोेड़कर ऊपर के स्वर्गों में से किसी भी स्वर्ग में महद्र्धिक देवों में उत्पन्न होते हैं।
सन् १९५८ में ब्यावर में एक बार ब्र. श्रीलालजी ने कहा कि ‘अट्ठदह’ पाठ का अर्थ समझ में नहीं आता है अतः इसके स्थान में ‘णट्ठदेहा’ पाठ हो सकता है।’ कुछ पुस्तकों में उन्होंने ऐसा संशोधन करा दिया किन्तु मैंने कहा-पंडित जी! श्रावक-श्राविका और क्षुल्लक-क्षुल्लिका ‘नष्टदेहाः’-देहरहित तो होते नहीं हैं अतः यह संशोधन मुझे संगत नहीं लगता है।
चर्चा के प्रसंग में ऐसी बात आई- ‘अठारह स्थान ऐसे ढूंढने चाहिए जहाँ व्रती नहीं जाता हो तथा उन अठारह स्थानों में ये भवनत्रिक और सौधर्म-ईशान की देवियाँ नहीं आनी चाहिए चूँकि इन्हें पृथक् से लिया है। तभी उमास्वामी श्रावकाचार के दो श्लोक स्मृतिपथ में आ गये, वे ये हैं-
सम्यक्त्वसंयुतः प्राणी, मिथ्यावासेन जायते।
द्वादशेषु च तिर्यक्षु, नारकेषु नपुँसके।।८८।।
स्त्रीत्वे च दुष्कृताल्पायु-र्दारिद्यादिकवर्जितः।
भवनत्रिषु षट्भूषु, तद्देवीषु न जायते।।८९।।
सम्यक्त्व से सहित जीव मिथ्यात्व के निम्नस्थानों में नहीं जाता है-
| १. पृथ्वीकायिक | २. जलकायिक |
| ३. अग्निकायिक | ४. वायुकायिक |
| ५. वनस्पतिकायिक | ६. दो इंद्रिय |
| ७. तीन इंद्रिय | ८. चार इंद्रिय |
| ९. निगोद | १०. असंज्ञीपंचेन्द्रिय |
| ११. कुभोगभूमि | १२. म्लेच्छखंड, मिथ्यात्व के इन बारह स्थानों में उत्पन्न नहीं होता है |
| १३. तिर्यंचों में | १४. नरकों में |
| १५. नपुंसक में | १६. स्त्रीवेद |
में उत्पन्न नहीं होता है। पुनः पापी, अल्पायु, दरिद्रादि से वर्जित रहता है। यह सम्यग्दृष्टी भवनत्रिकों में, प्रथम नरक से अतिरिक्त छह नरकभूमियों में व स्वर्ग की देवियों में भी नहीं जाता है। चर्चा में यह बात और आई कि यहाँ प्रतिक्रमण में तो व्रतिक श्रावकों के लिए कथन है अतः व्रतीजन तो सुभोगभूमि और मनुष्य पर्याय में भी नहीं जाते हैं क्योंकि गाथा है कि-
अणुवदमहव्वदाइं ण लहइ देवाउगं मोत्तुं।
(गोम्मटसार कर्मकांड) अणुव्रती और महाव्रती तो देवायु के सिवाय अन्य किसी आयु का बंध ही नहीं कर सकता है इसलिए उपर्युक्त १६.स्थानों में १७. सुभोगभूमि और १८. मनुष्य इन दो स्थानों को मिला देने से अठारह स्थान हो जाते हैं।
व्रतिक व क्षुल्लक-क्षुल्लिका इनमें नहीं जाते हैं। ये अठारह स्थान आचार्य श्रीशिवसागरजी महाराज को भी बहुत ही संगत प्रतीत हुए थे। तब ब्र. श्रीलालजी द्वारा संशोधित पाठ ‘‘णट्ठदेहा’’ हटा दिया गया था। उसके बाद वह चर्चा वहीं समाप्त हो गई थी। कुछ दिन पूर्व श्रमणचर्या में ‘अट्ठदह’ पाठ को उलट कर ‘दहअट्ठ’ पाठ लिया गया जिसका अर्थ यह निकाला गया-‘दश प्रकार के भवनवासी और आठ प्रकार के वानव्यंतर पुनः ‘श्रमणचर्या’ में छपा है-‘दह-अट्ठ-पंच’ जिसे भवनवासी, वानव्यंतर और ज्योतिषी देवों के भेदरूप से माना गया। जो भी हो, मेरी विचारधारा तो यही है
कि यदि कुछ पाठ संशोधित भी करना है तो पुराने विद्वानों के समान उस मूलपाठ को न हटाकर कोष्ठक में उसे रख देना चाहिए। जैसा कि- अट्ठदह (दह अट्ठ पंच) इससे मूल पाठ सुरक्षित रहेगा और अन्य ग्रंथों के आधार से भी साधुओं को व विद्वानों को सोचने का अवसर मिलेगा।
ऐसे ही एक पाठ परिवर्तन और है जो कि अतीव विचारणीय है-मूलपाठ है-
‘‘से अभिमदजीवाजीव-उवलद्धपुण्णपावआसवसंवरणिज्जर बंधमोक्खमहिकुसले।’
अब इसे बदल कर ऐसा पाठ रखा गया है-
‘से अभिमदजीवाजीव उवलद्धपुण्णपाव-आसवबंधसंवरणिज्जरमोक्खमहिकुसले।’
मूलपाठ में नवतत्त्वोें का क्रम यह था-जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आस्रव, संवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष। परिवर्तित पाठ का क्रम ऐसा हो गया है-जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आस्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। विचार करने से यह समझ में आता है कि-इस मूलपाठ के क्रम के अनुसार ही श्रीकुन्दकुन्दददेव ने समयसार में गाथा रखी है-
भूयत्थेणाभिगदा जीवाजीवा य पुण्णपावं च।
आसवसंवरणिज्जरबंधो मोक्खो य सम्मत्तं।।१३।।
और इसी गाथा के क्रम के अनुसार ही श्रीकुन्दकुन्दददेव ने समयसार में अधिकार विभक्त किये हैं। जीवाजीवाधिकार के बाद पुण्य-पापाधिकार है पुनः आस्रव अधिकार, संवर अधिकार, निर्जरा अधिकार लेकर तब बंध अधिकार है, इसके बाद मोक्ष अधिकार है। क्या इस गाथा को और समयसार के इन अधिकारों के क्रम को भी बदला जा सकता है? नहीं, पुनः यहाँ भी श्रीगौतमस्वामी के मुखकमल से निकले हुए दण्डकसूत्रों को बदलना उचित नहीं लगता है।
अभी तक हम लोग श्रीकुन्दकुन्दददेव की गाथाओं में कहे गये क्रम को श्री गौतमस्वामी द्वारा कथित प्रतिक्रमण सूत्रों के क्रम से तुलना किया करते थे। ऐसे और भी पाठ हैं। जैसे- ‘‘तवायारो वारसविहो’’-में बहिरंग तप में
‘‘सरीरपरिच्चाओ विवित्तसयणासणं चेदि।’’
अभ्यंतर तप में भी ‘झाणं विउसग्गो चेदि’ पाठ है। मूलाचार में भी-
‘‘कायस्स विपरितावो विवित्तसयणासणं छट्ठं१।।।३४६।।
और आगे इसी क्रम से इनके स्वरूप का वर्णन किया है। ऐसे ही अभ्यंतर तप में-
‘‘झाणं च विउसग्गो अब्भंतरओ तवो एसो।।३६०।।
आगे इसी क्रम से पांचवे तप में ध्यान का विस्तृत वर्णन करके छठे तप में व्युत्सर्ग का वर्णन किया है३। ‘‘श्रमणचर्या’’ में पाठ बदलकर ‘‘विउसग्गो झाणं चेदि।’’ ऐसा पाठ रखा है, सो कहाँ तक उचित है? ऐसे ही-इस पाक्षिक प्रतिक्रमण में श्रावकों के बारह व्रतों में शिक्षाव्रतों के नाम इस प्रकार हैं
‘‘तत्थ पढमे सामाइयं, विदिये पोसहोवासयं, तदिए अतिथिसंविभागो,
चउत्थे सिक्खावदे पच्छिमसल्लेहणामरणं।
’’ चारित्तपाहुड ग्रंथ मेंकुन्दकुन्दकुंददेव ने भी इसी क्रम से शिक्षाव्रत लिये हैं।
‘‘पाँच अणुव्रत, तीन गुणव्रत-
दिशिविदिशिपरिमाण, अनर्थदंडत्याग, भोगोपभोगपरिमाण, चार शिक्षाव्रत-सामायिक, प्रोषधोपवास, अतिथिपूजा और सल्लेखनामरण, ये बारह व्रत हैं। पांच अणुव्रत तो सर्वत्र सभी ग्रंथों में एक सदृश हैं, गुणव्रत और शिक्षाव्रतों में ही अन्तर है। इस प्रतिक्रमण में और चारित्रपाहुड़ ग्रंथ में सल्लेखना मरण को अंतिम शिक्षाव्रत में ही ले लिया है। यथा-
दिसविदिसपमाणं पढमं अणत्थदंडस्स वज्जणं विदियं।
भोगोपभोगपरिमाणं, इयमेवगुणव्वया तिण्णि।।२५।।
सामाइयं च पढमं विदियं च तहेव पोसहं भणियं।
तइयं अतिहि पुज्जं चउत्थ सल्लेहणा अंते।।२६।।
पद्यानुवाद
संस्कृत भक्तियों का एवं प्राकृत भक्तियों का पद्यानुवाद मैंने संघस्थ आर्यिका श्री रत्नमती माताजी की विशेष प्रेरणा से किया था। वे कहा करती थीं-‘‘माताजी! आप जैसे संस्कत के विद्वान साधु-साध्वियाँ नित्य-नैमित्तिक क्रियाओं की भक्तियों को पढ़ते समय अर्थ समझ लेते हैं किन्तु हम जैसे संस्कृत-प्राकृत व्याकरण के ज्ञान से शून्य साधु-साध्वियाँ अर्थ नहीं समझ पाते हैं अतः आप इन भक्तियों का और प्रतिक्रमण का हिन्दी पद्यानुवाद अवश्य कर दीजिए।
उनके आग्रह से मैंने सन् १९७२ में ही संस्कृत भक्तियों का पद्यानुवाद किया था बाद में सन् १९७९ में प्राकृत भक्तियों का भी अनुवाद कर दिया था कुन्दकुन्दकुंद का भक्तिराग’’ नाम से पुस्तक में ये सभी भक्तियाँ पद्यानुवाद सहित छपी हैं किन्तु यह पुस्तक आर्यिका रत्नमतीजी के सामने छपकर नहीं आ पाई थी। यद्यपि उन्होंने प्रतिक्रमण के पद्यानुवाद के लिए भी बहुत ही प्रेरणा दी थी। इच्छा तो मेरी भी थी किन्तु योग नहीं आया था।
इस वर्ष क्षुल्लक चितसागर जी (हिम्मतनगर-गुजरात) के भी कई पत्र प्रतिक्रमण के पद्यानुवाद के लिए आये। मुनिचर्या पुस्तक छप रही थी बल्कि दैवसिक प्रतिक्रमण छप रहा था। तभी ६कार्तिक कृ. ११ को प्रातः सामायिक के बाद लेखनी उठाई और अनुवाद प्रारंभ कर दिया। यद्यपि गद्य सूत्रों को पद्य में संक्षिप्त करना कठिन था फिर भी मेरी समझ में अर्थ के जिज्ञासुओं को यह अनुवाद रुचिकर ही होगा।
गणधरवलय मंत्र- क्रियाकलाप पृ. ९१ पर गणधरवलय स्तोत्र छपा है-
‘‘जिनान् जितारातिगणान् गरिष्ठान्। श्रीसिद्धिदाः सदृषीन्द्रान्।।१०।।
इसी पृष्ठ पर टिप्पण दिया है, यथा- मैंने प्रतिक्रमणग्रंथत्रयी पुस्तक भी पढ़ी थी। उसमें पाक्षिक प्रतिक्रमण के दंडक सूत्रों की संस्कृत टीका में इसी प्रतिक्रमण में कहे गये ‘‘णमो जिणाणं’’ आदि ४८ गणधरवलय मंत्रों की टीका है। इन मंत्रों की टीका के बाद पृ. ९६ पर-इति गणधरवलयाख्य प्रतिक्रमणामंगलदंडकः।।
ऐसा पाठ आया है। ब्यावर के सन् १९५८ के चातुर्मास में मैंने ‘क्रियाकलाप’ ग्रंथ के सम्पादक पं. पन्नालाल सोनी को यह पंक्ति दिखाई। तब उन्होंने कहा-‘‘पहले मैंने ‘‘णमो जिणाणं’’ आदि ४८ मंत्रों को ‘‘गणधरवलय’’ पाठ नहीं समझा था अतः मैंने श्रीसकलकीर्ति विरचित ‘‘गणधरवलयपूजा विधान’’ पुस्तक से गणधरवलय स्तोत्र को निकालकर यहाँ जोड़ा था। यह मेरे से गलती हुई है यह स्तोत्र अनावश्यक-अधिक यहाँ जुड़ गया है। अगले संस्करण में इस स्तोत्र को मैं निकाल दूँगा।
उन्होंने यह भी कहा- ‘‘माताजी! अपनी तरफ से दूसरे ग्रंथ से निकालकर यहाँ पाठ बढ़ाने से ‘‘कहीं मेरे से गलत कार्य तो नहीं हो रहा है?’’ इसी डर से ही मैंने टिप्पण दे दिया था। आपने प्रतिक्रमणग्रंथत्रयी दिखा दी सो बहुत ही अच्छा हुआ इत्यादि। अस्तु! वास्तव में इस टिप्पण से पं. पन्नालाल सोनी ब्यावर (राज.) आदि पुराने विद्वानों की पापभीरुता व सत्यता स्पष्ट दिखती है। आज के विद्वानों को यह गुण नहीं छोड़ना चाहिए।
सन् १९६२ में ब्र. श्रीलालजी काव्यतीर्थ ने ‘‘शांतिसागर जैन सिद्धांत प्रकाशिनी संस्था’’ से मेरे द्वारा लिखित ‘‘यतिक्रियामंजरी’’ पुस्तक छपाई थी। उसमें पाक्षिकप्रतिक्रमण में मैंने पं. पन्नालाल सोनी से परामर्श लेकर ही यह ‘‘जिनान् जितारातिगणान्’’ इत्यादि स्तोत्र निकाल दिया था। अभी भी मैंने ‘‘मुनिचर्या’’ में पाक्षिक प्रतिक्रमण में यह स्तोत्र पाठ मूल में नहीं रखा है किन्तु इस प्रतिक्रमण की संस्कृत छाया में इन ४८ गणधरवलय मंत्रों की छाया के सदृश ही इस स्तोत्र को पृ. ३०२ पर दे दिया है।
पाठांतर व पाठ अधिक
‘क्रियाकलाप’ और ‘प्रतिक्रमणग्रंथत्रयी’ में हमें पाठांतर-पाठभेद मिले हैं। उनमें से कतिपय पाठांतरों को मैंने ‘मुनिचर्या’ में लिया है। कहीं-कहीं पाठांतर को टिप्पण में दिया है तो कहीं मूल में कोष्ठक में दे दिया है। जैसे मुनिचर्या में पृ. ४८ पर मूल में ‘वीरं’ पाठ है, प्रतिक्रमणग्रंथत्रयी के आधार से ‘घोरं’ यह पाठांतर टिप्पण में दे दिया है। ऐसे ही अष्टमी के प्रतिक्रमण में इसमें पृ. २०८ पर ‘आहावरे’ और ‘दुव्वे’ पाठ हैं।
प्रतिक्रमणग्रंथत्रयी के आधार से वहीं कोष्ठक में (अहावरे) पाठ दिया है और ‘दुव्वे’ का पाठभेद ‘दोच्चे’ टिप्पण में दे दिया है, इत्यादि। इसी तरह इसी पृ. २०८ पर ‘भसेण वा’ पाठ के आगे ‘पदोसेण वा’ यह पाठ प्रतिक्रमणग्रंथत्रयी में अधिक मिला है यहाँ इसे कोष्ठक में रख दिया है मुनिचर्या पुस्तक में सर्वत्र यही प्रक्रिया अपनाई गई है अतः यह ग्रंथ ‘प्रामाणिक’ है।
यतिक्रियामंजरी
सन् १९५८ का चातुर्मास ब्यावर (राज.) में हुुआ था। आचार्यश्री शिवसागर जी के विशाल संघ में मैं भी थी। मैं कई एक आर्यिकाओें के साथ ऐलक पन्नालाल सरस्वती भवन में ऊपर कमरे में ठहरी थी। उन दिनों मैं संघस्थ साधु-साध्वी, ब्रह्मचारी-ब्रह्मचारिणी, श्राविकाओं आदि को अध्यापन कराती थी और रात्रि में सामायिक के बाद सरस्वती भवन के अनेक हस्तलिखित ग्रंथों का अवलोकन करती रहती थी और ‘यतिक्रियामंजरी’ नाम से मुनि-आर्यिकाओं की नित्य-नैमित्तिक क्रियाओं का लेखन व संकलन भी कर रही थी।
मुनियों की त्रिकाल सामायिक व त्रिकाल देववंदना क्रिया एक ही है। उसकी विधि क्रियाकलाप, अनगार धर्मामृत, चारित्रसार, आचारसार, भावसंग्रह आदि ग्रंथों में वर्णित है,कहीं संक्षिप्त संकेत है तो कहीं विस्तृत वर्णन है। हस्तलिखित संहिताग्रंथ-एक संधिसंहिता, इन्द्रनंदिसंहिता आदि और अकलंक प्रतिष्ठा पाठ आदि अनेक ग्रंथों का अवलोकन कर उनसे देववंदना सामायिक संबंधी प्रकरण के उद्धरण निकालती रहती थी।
इसी प्रकार मुनियों-आर्यिकाओं को रात्रिक प्रतिक्रमण पूर्वाण्ह सामायिक के पहले करना चाहिए, इस संबंधी प्रमाण भी निकाले थे। इस कार्य में पं. पन्नालाल जी सोनी भी रुचि रजते थे और कभी-कभी अनेक उद्धृत प्रमाणों को देखकर प्रसन्नता व्यक्त किया करते थे। कुल मिलाकर मैंने संपूर्ण नित्य-नैमित्तिक क्रियाओं के बहुत से प्रमाण अनेक ग्रंथों के आधार से संकलित किये थे तथा प्रत्येक क्रियाओं के प्रमाण के साथ विधिवत् उन-उन भक्तियों का पाठ भी यथास्थान ही दे दिया था।
इसी का नाम ‘यतिक्रियामंजरी’ रखा था। यह पुस्तक ब्र. श्रीलालजी को छापने के लिए दी गई, तब उन्होंने क्रियाओं के प्रमाणसंबंधी उद्धृत श्लोक आदि नाममात्र के रहने दिये, बाकी सभी प्रमाण के पाठ उसमें से निकाल कर मुझे वापस दे दिये और बोले- ‘‘माताजी! इस क्रिया की पुस्तक में ज्यादा विषय मत बढ़ाओ। इन प्रमाणों की पुस्तक अलग से छप जायेगी।’’ तभी ‘‘यतिक्रियामंजरी’’ में प्रारंभ में स्तोत्र पाठ आदि जोड़कर यह पुस्तक छपने दे दी गई।
इसमें मैंने अनेक साधु व विद्वानों के आग्रह पर भी अपना नाम नहीं दिया था। उसके संपादक के रूप में ब्र. सूरजमल जी का नाम दिया है। यह पुस्तक सन् १९६२ में छप चुकी है। उस समय के जो प्रमाणों का मेरा संकलन था, उसमें मैंने बहुत ही परिश्रम किया था। सन् १९६२ की दिसम्बर में सम्मेदशिखर यात्रा के लिए विहार करते समय मैंने वह बस्ता कुचामन के एक श्रावक…..को सुरक्षित रखने के लिए दे दिया था। खेद है कि उनसे मुझे आज तक वह बस्ता उपलब्ध नहीं हो पाया।
अस्तु! ऐसे ही उन्हीं दिनों सन् १९५९ में ‘‘श्रावकक्रियामंजरी’’ का भी मैंने अनेक प्रमाणों सहित अच्छा संकलन किया था। श्रावकों की देवपूजा क्रिया आदि विधिवत् होती है तो वही उनकी सामायिक है, इस विषय के भी प्रमाण संकलित किये थे। यह संकलित पुस्तक का बस्ता मैंने सन् १९६६ में अकलूज के एक सुप्रसिद्ध श्रावक को दिया था चूँकि वे छपाना चाहते थे, आज तक वह बस्ता भी उनसे उपलब्ध नहीं हो सका है।
ऐसे कई एक कटु अनुभव जब मुझे आये, तब संघस्थ ब्र. मोतीचंद आदि ने मेरे लिखित ग्रंथों को टाइप कराकर ही प्रेस आदि में देने का निर्णय किया। आजकल तो हस्तलिखित ग्रंथों की फोटो कापी कराना बहुत सरल हो गया है। इस ‘‘यतिक्रियामंजरी’’ में संकलनकत्र्री में अपना नाम न देने में मेरी निःस्पृहता ही मूल कारण थी। यद्यपि सन् १९५५ में सर्वप्रथम रचना में ‘‘सहस्रनाम के मंत्र’’ की पुस्तक ‘‘श्रीजिनसहस्रनाम व्रतविधि व पूजा’’ को क्षुल्लिका श्रीविशालमती जी ने छपाया था। उसमें क्षुल्लिकावस्था में मेरा नाम (क्षुल्लिका वीरमती माताजी) डाला था।
फिर भी सन् १९६०-६१ में मैंने पुस्तक संकलन में अपना नाम देने के लिए सर्वथा मना कर दिया था। इसके बाद सन् १९६६ में सोलापुर चातुर्मास में मेरे द्वारा लिखित ‘‘श्रीबाहुबली चरित, ‘‘भक्तिसुमनावली’’, ‘‘व्रतविधिसुमनावली’’ आदि पुस्तके छपीं तब ब्र. सुमतीबाई आदि अनेक विदुषी व विद्वानों ने मेरे से निवेदन किया-‘‘माताजी! अपनी किसी भी कृति में अपना नाम न डालने से पहली बात तो उनकी प्रमाणिकता नहीं रहती है और दूसरी बात यह है कि कोई मायाचारी विद्वान उस कृति में अपना नाम डालकर अपनी कृति घोषित कर देते हैं। उन्होंने ‘‘पंचाध्यायी’’ अमरकोष’’ आदि अनेक पुरातन ग्रंथों के व आज के भी कई पुस्तक आदि के नाम बताये। तब मैंने पुस्तकों में अपना नाम देना स्वीकृत किया था।
