प्रकृति प्रकरण
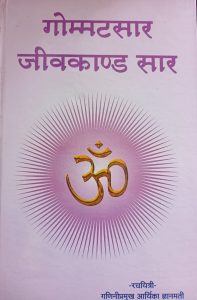
“मंगलाचरण”
पणमिय सिरसा णेमिं गुणरयणविभूसणं महावीरं।
सम्मत्तरयणणिलयं पयडिसमुक्कित्तणं वोच्छं।।१।।
प्रणम्य शिरसा नेमिं गुणरत्नविभूषणं महावीरम्।
सम्यक् त्वरत्ननिलयं प्रकृतिसमुत्कीर्तंनं वक्ष्यामि।।१।।
अर्थ—मैं नेमिचंद्र आचार्य, ज्ञानादिगुणरूपी रत्नों के आभूषणों को धारण करने वाले, मोक्षरूपी महालक्ष्मी को देने वाले, सम्यक्त्वरूपी रत्न के स्थान ऐसे श्रीनेमिनाथ तीर्थंकर को मस्तक नवा-प्रणाम कर, ज्ञानावरणादि कर्मों की मूल व उत्तर दोनों प्रकृतियों के व्याख्यान करने वाला प्रकृतिसमुत्कीर्तननामाधिकार कहता हूूँ।
प्रकृति शब्द का अर्थ क्या है?
पयडी सील सहावो जीवंगाणं अणाइसंबंधो।
कणयोवले मलं वा ताणत्थित्तं सयं सिद्धं।।२।।
प्रकृति: शीलं स्वभाव: जीवांगयोरनादिसम्बन्ध:।
कनकोपले मलं वा तयोरस्तित्वं स्वयं सिद्धम्।।२।।
अर्थ—कारण के बिना वस्तु का जो सहज स्वभाव होता है उसको प्रकृति, शील अथवा स्वभाव करते हैं। जैसे कि आग का स्वभाव ऊपर को जाना, पवन का तिरछा बहना और जल का स्वभाव नीचे को गमन करना है, इत्यादि। प्रकृति में यह स्वभाव जीव तथा अंग (कर्म) का ही लेना चाहिए। इन दोनों में से जीव का स्वभाव रागादिरूप परिणमने (हो जोन) का है, और कर्म का स्वभाव रागादिरूप परिणमावने का है। तथा यह दोनों का संबंध, सवर्ण पाषाण में मिले हुए मल (मैल) की तरह अनादिकाल से है। और इसलिये जीव तथा कर्म का अस्तित्व भी स्वयं-ईश्वरादि कर्ता के बिना ही अपने आप सिद्ध है।
भावार्थ—जिस तरह भंग अथवा शराब का स्वभाव बावला कर देने का और इसके पीने वाले जीव का स्वभाव बावला हो जाने का है, उसी तरह जीव का स्वभाव रागद्वेषादि कषायरूप हो जाने का तथा कर्म का स्वभाव रागादिकषायस्वरूप परिणमा देने का है। सो जब तक दोनों का संबंध रहता है तभी तक विकाररूप परिणाम होता है। अंतर इतना ही है कि जीव और कर्म का यह संबंध अभी का नहीं, अनादिकाल का है। जैसे कि खानि से निकला हुआ सोना अनादिकाल से ही कीट कालिमा रूप मैल से मिला हुआ रहता है, वैसे ही जीव और कर्मों का अनादिकाल से स्वत: संबंध हो रहा है, किसी ने इनका संबंध किया नहीं है। जीव का अस्तित्व तो ‘‘अहम्’’ (मैं) ऐसी प्रतीत होेने से सिद्ध होता है, तथा कर्म का अस्तित्व, जगत् में कोई दरिद्री (भिखारी) है तो कोई धनवान्, इत्यादि विचित्रपना प्रत्यक्ष देखने से, सिद्ध होता है। इस कारण जीव और कर्म दोनों ही पदार्थ अनुभवसिद्ध हैं।
संसारी जीव द्वारा कर्म और नोकर्म का ग्रहण कैसे होता है?
देहोदयेण सहिओ जीवों आहरदि कम्म णोकम्मं।
पडिसयमं सव्वंगं तत्तायसपिंडओव्व जलं।।३।।
देहोदयेन सहितो जीव आहारति कर्म नोकर्म।
प्रतिसमयं सर्वांगं तप्ताय: पिंउमिव जलम्।।३।।
अर्थ—यह जीव औदारिक आदि शरीननामा कर्म के उदय से योग सहित होकर ज्ञानावरणादि आठ कर्मरूप होने वाली कर्मवर्गणाओं को, तथा औदारिक आदि चार शरीर (१.औदारिक, २. वैक्रियक, ३. आहारक, ४. तैजस) रूप होने वाली नोकर्मवर्गणाओं को हरसमय चारों तरफ से ग्रहण (अपने साथ संबंध) करता है। जैसे कि आग से तपा हुआ लोहे का गोला पानी को सब ओर से आपनी तरफ खींचता है। भावार्थ—जब यह शरीर सहित आत्मा मन, वचन, काय की प्रवृत्ति करता है तभी इसके कर्मों का बंध होता है। किन्तु मन, वचन, काय की क्रिया रोकने से कर्म बंध नहीं होता।
प्रतिसमय आने वाले कर्मपरमाणुओं की संख्या क्या है?
सिद्धाणंतिमभागं अभव्वसिद्धादणंतगुणमेव।
समयपबद्धं बंधदि जोगवसादो दु विसरित्थं।।४।।
सिद्धानन्तिमभागं अभव्यसिद्धादनन्तगुणमेव।
समयप्रबद्धं बध्नाति योगवशात्तु विसदृशम्।।४।।
अर्थ—यह आत्मा, सिद्धजीवराशि के जो कि अनंतानंतप्रणाम कही है अनंतवें भाग और अभव्यराशि जो जलघन्युक्तानंत प्रमाण है उससे अनंतगुणे समय-प्रबद्धको अर्थात् एक समय में बंधने वाले परमाणु समूह को बाँधता है,-अपने साथ संबद्ध करना है। परन्तु मन, वचन, काय की प्रवृत्तिरूप योगों की विशेषता से (कमती बढ़ती होने से) कभी थोड़े और कभी बहुत परमाणुओं का भी बंध करता है। सारांश—परिणामों में काषाय की अधिकता तथा मंदनात होने पर आत्मा के प्रदेश जब अधिक वा कम सकंप (चलायमान) होते हैं तब कर्मपरमाणु भी ज्यादा अथवा कम बंधते हैं। जैसे अधिक चिकनी दीवाल पर धूलि अधिक लगती है और कम चिकनी पर कम।
प्रतिसमय झड़ने वाले कर्मों की संख्या क्या है?
जीरदि समयपबद्धं पओगदो णेगसमयबद्धं वा।
गुणहाणीण दिवड्ढं समयपबद्धं हवे सत्तं।।५।।
जीर्यते समयप्रबद्धं प्रयोगत: अनेकसमयबद्धं वा।
गुणहीनीनां द्वयद्र्धं समयप्रबद्धं भवेत् सत्वम्।।५।।
अर्थ—एक-एक समय में कर्मपरमाणुओं का एक-एक समयप्रबद्ध फल देकर खिर जाया करता है। परन्तु कदाचित् तपश्चरणरूप विशिष्ट अतिशयवाली क्रिया से होने पर बंधे हुए अनेक समयप्रबद्ध भी झड़ जाया करते हैं। फिर भी कुछ कम डेढ़ गुणहानि आयाम से गुणित समय प्रमाण समय प्रबद्ध सत्ता (वर्तमान) अवस्था में रहा करते हैं। इसका विशेष कथन आगे चलकर कर्म की अवस्था के अधिकार मे कहेंगे। वहीं पर
कर्म के सामान्य भेद दो हैं
कम्मत्तणेण एकं दव्वं भावोत्ति होदि दुविहंतु।
पोग्गलपिंडो दव्वं तस्सत्ती भावकम्मं तु।।६।।
कर्मत्वेन एकं द्रव्यं भाव इति भवति द्विविधं तु।
पुद्गलपिण्डो द्रव्यं तच्छक्ति: भावकर्म तु।।६।।
अर्थ—सामान्यपने से कर्म एक ही है, उसमें भेद नहीं हैं। लेकिन द्रव्य तथा भाव के भेद से उसके दो प्रकार हैं। उसमें ज्ञानावरणादि रूप पुद्गलद्रव्य का पिंड द्रव्य कर्म है, और उस द्रव्यपिंड के फल देने की जो शक्ति है वह भावकर्म है अथवा कार्य के कारण का व्यवहार होने से उस शक्ति से उत्पन्न हुए जो अज्ञानादि वा क्रोधादि रूप परिणाम हैं वे भी भाव कर्म ही हैं।कर्म के भेद-प्रभेद कितने हैं?
तं पुण अट्ठविहं वा अडदालसयं असंखलोगं वा।
ताणं पुण घादित्ति अ-घादित्ति य होंति सण्णाओ।।७।।
तत् पुनरष्टविधं वा अष्टचत्वारिंशच्छतमसंख्यलोकं वा।
तेषां पुन: घातीति अघातीति च भवत: संज्ञे।।७।।
अर्थ—वह कर्म सामान्य से आठ प्रकार का है। अथवा एक सौ अड़तालीस आ असंख्यात लोकप्रमाण भी उसके भेद होते हैं। उन आठ कर्मों में भी घातिया तथा अघातिया ये दो भेद हैं।
आठ कर्मों के नाम
णाणस्स दंसणस्स य आवरणं वेयणीयमोहणियं।
आउगणामं गोदंतरायमिदि अट्ठ पयडीओ।।८।।
ज्ञानस्य दर्शनस्य च आवरणं वेदनीयमोहनीयम्।
आयुष्कनाम गोत्रान्तरायमिति अष्टप्रकृतय:।।८।।
अर्थ —१.ज्ञानावरण, २. दर्शनावरण, ३. वेदनीय, ४. मोहनीय, ५ आयु, ६. नाम, ७. गोत्र और ८. अंतराय, ये आठ कर्मों की मूल प्रकृतियाँ (स्वभाव) हैं। कर्मों के घाती-अघाती भेद
आवरणमोहविग्घं घादी जीवगुणघादणत्तादो।
आउगणामं गोदं वेयणियं तह अघादित्ति।।९।।
आवरणमोहविघ्नं घाति जीवगुणघातनत्वात्।
आयुष्क नाम गोत्रं वेदनीयं तथा अघातीति।।९।।
अर्थ— १.ज्ञानावरण, २ . दर्शनावरण, ३. मोहनीय, ४. अंतराय, ये चार घातिया कर्म हैं। क्योंकि जीव के अनुजीवी गुणों को घातते (नष्ट करते हैं) १. आयु, २. नाम, ३. गोत्र और ४. वेदनीय, ये चार अघाती कर्म हैं। क्योंकि जली हुई रस्सी की तरह इनके रहने से भी अनुजीवों गुणों का नाश नहीं होता।
कर्मों के उत्तर भेद
पंच णव दोण्णि अट्ठावीसं चउरो कमेण तेणउदी।
तेउत्तरं सयं वा दुगपणगं उत्तरा होंति।।१०।।
पंच नव द्वौ अष्टाविंशति: चत्वार: क्रमेण त्रिनवति:।
च्युत्तरं शतं वा द्विकपंचकमुत्तरा भवन्ति।।१०।।
अर्थ—ज्ञानावरण आदि आठ कर्मों में से प्रत्येक के भेद क्रम से पाँच, नौ, दो, अट्ठाईस, चार, तिरानवै अथवा एक सौ तीन, दो और पाँच होते हैं।
एक सौ अड़तालीस प्रकृतियों के नाम व लक्षण
ज्ञानावरण के ५ भेद—ज्ञानावरण के ५ भेद हैं— (१) मतिज्ञानावरण, (२) श्रुतज्ञानावरण, (३) अवधिज्ञानावरण, (४) मन:पर्ययज्ञानावरण, (५) केवलज्ञानावरण।
१.मतिज्ञानावरण—जो मतिज्ञान को नहीं होने देता उसे मतिज्ञानावरण कहते हैं।
२.श्रुतज्ञानावरण—जो शास्त्रज्ञान को नहीं होने देता उसे श्रुतज्ञानावरण कहते हैं।
३.अवधिज्ञानावरण—जो अवधिज्ञान को नहीं होने देता उसे अवधिज्ञानावरण कहते हैं।
४.मन:पर्ययज्ञानावरण—जो मन:पर्ययज्ञान को नहीं होने देता उसे मन:पर्ययज्ञानावरण कहते हैं।
५.केवलज्ञानावरण—जो केवलज्ञान को नहीं होने देता उसे केवलज्ञानावरण कहते हैं।
दर्शनावरण के ९ भेद हैं— (१) चक्षुदर्शनावरण, (२) अचक्षुदर्शनावरण, (३) अवधिदर्शनावरण, (४) केवलदर्शनावरण, (५) निद्रा, (६) निद्रानिद्रा, (७) प्रचला, (८) प्रचलाप्रचला, (९) स्त्यानगृद्धि।
१. चक्षुदर्शनावरण—जो कर्म चक्षुइन्द्रिय से होने वाले सामान्य अवलोकन को नहीं होन देता, उसे चक्षुदर्शनावरण कहते हैं।
२. अचक्षुदर्शनावरण—जो चक्षु इन्द्रिय के बिना शेष चार इंद्रिय और मन से होने वाले सामान्य अवलोकन को नहीं होने देता, उसे अचक्षुदर्शनावरण कहते हैं।
३.अवधिदर्शनावरण—जिसके उदय से अवधिदर्शन का घात होता है, उसे अवधिदर्शनावरण कहते हैं।
४. केवलदर्शनावरण—जिसके उदय से केवलदर्शन प्रगट नहीं होता है, उसे केवलदर्शनावरण कहते हैं।
५. निद्रा—जिस कर्म के उदय से निद्रा आती है, उसे निद्रादर्शनावरण कहते हैं।
६. निद्रानिद्रा—जिसके उदय से नींद पर नींद आती है, उसे निंद्रानिंद्रा कहते हैं।
७. प्रचला—जिसके उदय से प्राणी कुछ जागता है कुछ सोता है, उसे प्रचला कहते हैं।
८. प्रचलाप्रचला—जिसके उदय से सोते समय मुख से लार बहती है और कुछ आँगोपाँग भी चलते हैं, उसे प्रचलाप्रचला कहते हैं।
९. स्त्यानगृद्धि—जिसके उदय से प्राणी सोते समय नाना प्रकार के भयंकर काम कर डालता है और जागने पर कुछ मालूम नहीं रहता कि मैंने क्या किया है, उसे स्त्यागृद्धि कहते हैं।
वेदनीय के भेद
वेदनीय के दो भेद हैं—सातावेदनीय और असातावेदनीय।
१.सातावेदनीय—जिस कर्म के उदय से शारीरिक और मानसिक अनेक प्रकार की सुख सामग्री मिले या सुख मिले उसे सातावेदनीय कहते हैं।
२. असातावेदनीय—जिसके उदय से दु:खदायक सामग्री या दु:ख प्राप्त हो वह असातावेदनीय है।
मोहनीय के भेद
मोहनीय कर्म के दो भेद हैं—दर्शनमोहनीय और चारित्रमोहनीय। इसमें दर्शनमोहनीय के ३ भेद हैं तथा चारित्रमोहनीय के पहले दो भेद हैं कषायवेदनीय और अकषायवेदनीय। कषायवेदनीय के १६ भेद हैं और अकषायवेदनयी के ९ भेद हैं। ऐसे दर्शनमोहनीय के ३ और चारित्रमोहनीय के २५ मिलकर २८ भेद हुए।
दर्शनमोहनीय के भेद
जो आत्मा के सम्यक्त्व गुण का घात करता है, उसे दर्शनमोहनीय कहते हैं। उसके तीन भेद हैं—मिथ्यात्व, सम्यङ्मिथ्यात्व और सम्यक्त्व।
१.मिथ्यात्व—जिस कर्म के उदय से तत्त्वों का यथार्थ श्रद्धान नहीं होता, उसे मिथ्यात्व कहते हैं।
२.सम्यङ्मिथ्यात्व—जिस कर्म के उदय से दही और गुड़ से मिश्रित स्वाद के समान तत्त्वों का श्रद्धान और अश्रद्धान दोनों रूप से मिश्रित भाव होता है वह सम्यङ्मिथ्यात्व कहलाता है।
३.सम्यक्त्व—जिस कर्म के उदय से सम्यग्दर्शन में दोष उत्पन्न होता है, वह सम्यक्त्व प्रकृति है।
चारित्रमोहनीय के भेद
जिस कर्म के उदय से आत्मा के चारित्र गुण का घात होता है उसे चारित्रमोहनीय कहते हैं। इसके दो भेद हैं—कषायवेदनीय और अकषायवेदनीय। जो आत्मा के गुण-शुभ या शुद्धभाव को कषता है, नष्ट करता है, उसे कषायवेदनीय कहते हैं।
इसके सोलह भेद हैं—अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ, अप्रत्याख्यानावरण, क्रोध, मान, माया, लोभ, प्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, लोभ और संज्वलन क्रोध, मान, माया, लोभ।
४. अनंतानुबंधी— जो अनंत अर्थात् मिथ्यात्व के साथ-साथ बंधती है, उसे अनंतानुबंधी कहते हैं अथवा जिसके उदय से सम्यक्त्व का घात हो वह अनंतानुबंधी है। उसके क्रोध, मान, माया, लोभ ये चार भेद हैंं। अप्रत्याख्यानावरण—जिसके उदय से जीव मुनियों के चारित्र को धारण नहीं कर सके, वह प्रत्याख्यानावरण है।
संज्वलन— जिसके उदय से यथाख्यात चारित्र न हो सके, उसे संज्वलन कहते हैं। जो क्रोधादि की तरह आत्मा के गुणों का घात नहीं करे किन्तु किंचित् घात करे अथवा कषाय के साथ-साथ अपना फल देवे, वह अकषाय वेदनीय है। उसके ९ भेद हैं—हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुंवेद और नपुंसकवेद।
१. हास्य—जिसके उदय से हँसी आवे।
२. रति—जिसके उदय से इंद्रिय के विषयों में राग हो।
३. अरति—जिसके उदय से इंद्रिय के विषयों में द्वेष हो।
४. शोक—जिसके उदय से शोक या चिंता हो।
५. भय—जिसके उदय से डर या उद्वेग हो।
६. जुगुप्सा—जिसके उदय से दूसरे से ग्लानि हो।
७. स्त्रीवेद—जिसके उदय से पुरुष में रमने की इच्छा हो।
८. पुंवेद—जिसके उदय से स्त्री में रमने की इच्छा हो।
९. नपुंसकवेद—जिसके उदय से स्त्री-पुरुष दोनों में रमने की इच्छा हो।
आयु के भेद
आयुकर्म के चार भेद हैं—नरकायु, तिर्यंचायु, मनुष्यायु और देवायु। नरकायु—जिस कर्म के उदय से प्राणी नारकी के शरीर में रूका रहता है, उसे नरकायु कहते हैं। इसी तरह शेष आयु के भी लक्षण समझना चाहिए।
नाम कर्म के भेद
नामकर्म के ९३ भेद हैं—गति ४, जाति ५, शरीर ५, अंगोपंग ३, निर्माण १, बंधन ५, संघात ५, संस्थान ६, संहनन ६, स्पर्श ८, रस ५, गंध २, वर्ण ५, आनुपूर्वी ४, अगुरूलघु, उपघात, परघात, आतप, उद्योत, उच्छावास, प्रशस्तविहायोगति, अप्रशस्तविहायोगति, प्रत्येक, साधारण, त्रस, स्थावर, सुभग, दुर्भग, सुस्वर, दु:स्वर, शुभ, अशुभ, सूक्ष्म, बादर, पर्याप्त, अपर्याप्त, स्थिर, अस्थिर, आदेय, अनादेय, यशकीर्ति, अपयशकीर्ति और तीर्थंकर ये ९३ प्रकृतियाँ हैं।
गति—जिस कर्म के उदय से प्राणी दूसरे भव या पर्याय में जाता है, वह गति है।
उसके ४ भेद हैं—नरकगति, तिर्यंग्गति, मनुष्यगति और देवगति। जाति—जिस कर्म के उदय से अनेक प्राणियों के अविरोधी समान अवस्था प्राप्त होती है, उसे जाति कहते हैं।
इसके पाँच भेद हैं—एकेन्द्रिय जाति, द्वीन्द्रिय जाति, त्रीन्द्रिय जाति, चतुरिन्द्रिय जाति और पंचेन्द्रिय जाति। जिस कर्म के उदय से जीव एकेन्द्रिय जाति में पैदा हो वह एकेन्द्रिय जाति है, इत्यादि। शरीर—जिस कर्म के उदय से प्राणी शरीर की रचना होती है, वह शरीर है।
इसके ५ भेद हैं—औदारिक, वैक्रियिक, आहारक, तैजस और कार्मण।
१. औदारिक—जिस कर्म के उदय से औदारिक शरीर की रचना होती है, मनुष्य और तिर्यंच के स्थूल शरीर को ओदारिक शरीर कहते हैं।
२. वैक्रियिक शरीर—जिस कर्म के उदय से शरीर में स्थूल, सूक्ष्म, हल्का, भारी आदि अनके प्रकार से होने की योग्यता होती है।
३. आहारक शरीर—आहारक ऋद्धि वाले छठे गुणस्थानवर्ती मुनि के मस्तक से जो एक हाथ का पुतला निकलता है। उसे आहारक शरीर कहते हैं।
४. तैजस शरीर—जिस कर्म के उदय से शरीर में तेह होता है।
५. कार्मण शरीर—ज्ञानावरणादि आठ कर्मों के समूह को कार्मण शरीर कहते हैं।
बंधन—शरीर नाम कर्म के उदय से ग्रहण किये गये पुद्गल स्कंधों का परस्पर मिलने जिस कर्म के उदय से होता है, उसे बंधन नाम कर्म कहते हैं। इसके पाँच भेद हैं—औदारिक बंधन, वैक्रियिकबंधन, आहारक बंधन, तैजस बंधन, कार्मण बंधन।
संघात—जिस कर्म के उदय से औदारिक आदि शरीर के प्रदेशों का परस्पर छिद्र रहित एकमेकपना होता है, वह संघात है।
उसके पाँच भेद हैं—औदारिकसंघात, वैक्रियिकसंघात, आहारकसंघात, तैजससंघात और कार्मणसंघात। संस्थान—जिस कर्म के उदय से शरीर का आकार बनता है, वह संस्थान है।
इसके छ: भेद हैं—समचतुरस्रसंस्थान, न्यग्रोधपरिमंडलसंस्थान, स्वातिसंस्थान, कुब्जकसंस्थान, वामनसंस्थान और हुैडकसंस्थान।
१. समचतुरस्र—जिस कर्म के उदय से शरीर की लम्बाई, चौड़ाई, सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार ठीक-ठीक बनी हो, उसे समचतुरस्रसंस्थान कहते हैं।
२. न्यग्रोधपरिमंडल—जिस कर्म के उदय से शरीर का आकार वटवृक्ष की तरह नाभि के नीचे पतला और ऊपर मोटा हो।
३. स्वाति—जिस कर्म के उदय से शरीर का आकार सर्प की बामी की तरह ऊपर पतला और नीचे मोटा हो।
४. कुब्जक—जिस कर्म के उदय से शरीर कुबड़ा हो।
५. वामन—जिस कर्म के उदय से शरीर बौना हो।
६. हुंडकसंस्थान—जिस कर्म के उदय से शरीर के आकार किसी विशेष रूप के न हों, प्रत्युत बेडौल हों।
अंगोपांग—जिस कर्म के उदय से अंग और उपांगों की रचना होती है, उसे अंगोपांग कहते हैं।
इसके तीन भेद हैं—औदारिक शरीर, अंगोपांग, वैक्रियिक अंगोपांग और आहारक अंगोपांग। दो हाथ, दो पैर, नितंब, पीठ, वक्षस्थल और मस्तक ये आठ अंग हैं तथा अंगुलि, आँख, कान आदि उपांग हैं।
संहनन—जिस कर्म के उदय से हड्डियों में विशेषता हो, वह संहनन है।
इसके छ: भेद हैं—बङ्कावृषभनाराच, वङ्कानाराच, नाराच, अर्धनाराच, कीलित और असंप्राप्तसृपाटिकासंहनन।
१. बङ्कावृषभनाराच—जिस कर्म के उदय से वृषभ (नसों की हड्डियों का बंधन) नाराच (कील), संहनन (हड्डियाँ) वङ्का के समान अभेद्य हों।
२. बङ्कानाराच—जिस कर्म के उदय से वङ्का हड्डियाँ और वङ्का की कीलों हों परन्तु नसों में जाल वङ्का के समान नहीं हो।
३. नाराच—जिस कर्म के उदय से हड्डियों तथा संधियों में कीलें तो हों परन्तु वङ्का के समान कठोर न हों और नसा जला भी बङ्कावत् कठोर न हो।
४. अर्धनाराच—जिस कर्म के उदय से हड्डियों की कीलियों अर्धकीतिल हों। एक तरफ कीलें हों दूसरी तरफ से न हों।
५. कीलित—जिस कर्म के उदय से हड्डियाँ परस्पर कीलित हों।
६. असंप्राप्तसृपाटिका—जिस कर्म के उदय से हड्डियों की संधियाँ नसों से बंधी होती हैं परन्तु परस्पर में कीलित नहीं होती हैं।
स्पर्श—जिस कर्म के उदय से स्पर्श हो।
इसके ८ भेद हैं—कोमल, कठोर, गुरू, लघु, शीत, उष्ण, स्निग्ध और रूक्ष।
रस—जिस कर्म के उदय से शरीर में रस हो।
इसके ५ भेद हैं—तिक्त (चरपरा), कटुक, (कडुवा, कषाय (कषायला), आम्ल (खट्टा) और मधुर (मीठा)।
गंध—जिस कर्म के उदय से शरीर में गंध।
उसके दो भेद हैं—सुगंध और दुर्गन्ध।
वर्ण—जिस कर्म के उदय से शरीर में रूप हो।
उसके ५ भेद हैं— नील, शुक्ल, कृष्ण, रक्त और पीत।
आनुपूर्वी—जिस कर्म के उदय से अन्य गति को जाते हुए प्राणी का आकार विग्रहगति में पूर्व शरीर के आकार का रहता है।
इसके ४ भेद हैं— नरकगत्यानुपूर्वी, तिर्यग्गत्यानुपूर्वी, मनुष्यगत्यानुपूर्वी और देवगत्यानुपूर्वी।
नरकगत्यानुपूर्वी—जिस समय कोई मनुष्य मरकर नरक गति की ओर जाता है वहाँ पहुँचने तक बीच में (विग्रह गति से) उसके आत्मा के प्रदेशों का पूर्ण शरीर का आकार बना रहता है, उसे नरकगत्यानुपूर्वी कहते हैं। ऐसे ही शेष सभी में समझना।
अगुरुलघु—जिस कर्म के उदय से जीव का शरीर लोके के गोले की तरह भारी और आक की रूई की तरह हल्का नहीं होवे, वह अगुरुलघु है।
उपघात—जिस कर्म के उदय से अपने ही घातक अंगोपांग होते हैं।
परघात—जिस कर्म के उदय से पर के घातक अंगोपांग होते हैं।
उच्छ्वास—जिस कर्म के उदय से श्वासोच्छ्वास हों, उसे उच्छ्वास कर्म कहते हैं। आतप—जिस कर्म के उदय से आतपकारी शरीर होता है। इसका उदय सूर्य के विमान में स्थित बादर पृथ्वीकायिक जीवों के होता है।
उद्योत—जिस कर्म के उदय से उद्योत रूप शरीर हो। इसका उदय चंद्रमा के विमान में स्थित पृथ्वीकायिक जीवों के तथा जुगुनू आदि जीवों के होता है। विहायोगति—जिस कर्म के उदय से आकाश में गमन होता है।
इसके २ भेद हैं—प्रशस्तविहायोगति और अप्रशस्तविहायोगति।
त्रस—जिस कर्म के उदय से द्वीन्द्रिय आदि जीवों में जन्म होता है।
बादर—जिस कर्म के उदय से दूसरे को रोकने वाला और दूसरों से रुकने वाला शरीर प्राप्त हो।
पर्याप्ति—जिस कर्म के उदय से अपने योग्य पर्याप्तियाँ पूर्ण हो जावें। ये पर्याप्तियाँ ६ हैं-आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन।
प्रत्येक शरीर—जिस कर्म के उदय से एक शरीर का स्वामी एक ही जीव हो।
स्थिर—जिस कर्म के उदय से शरीर के रस आदि धातु तथा वात पित्तादि उपधातु अपने-अपने स्थान में स्थिर रहें। अनेक व्रत उपवास आदि से भी शिथिलता न आवे।
शुभ—जिस कर्म के उदय से मस्तक आदि अवयव सुंदर मालूम हों।
सुभग—जिस कर्म के उदय से दूसरों को अपने से प्रीति हो।
सुस्वर—जिस कर्म के उदय से अच्छा स्वर हो।
आदेय—जिस कर्म के उदय से शरीर में प्रभा हो।
यशस्कीर्ति—जिस कर्म के उदय से जीव का पुण्य गुण जगत् में प्रसिद्ध हो अथवा बिना गुण के भी प्रशंसा हो।
निर्माण—जिस कर्म के उदय से शरीर के अंगोपांगों की यथास्थान और यथाप्रमाण रचना हो।
तीर्थंकर—जिस कर्म के उदय से तीर्थंकर पद की प्राप्ति हो।
स्थावर—जिस कर्म के उदय से एकेन्द्रियों में जन्म हो।
सूक्ष्म—जिस कर्म के उदय से दूसरों को नहीं रोकने वाला और दूसरों से नहीं रुकने वाला शरीर हो।
अपर्याप्ति—जिस कर्म के उदय से पर्याप्तियों की पूर्णता न हो बीच में ही मरण हो जावे।
साधारण—जिस कर्म के उदय से एक शरीर के स्वामी अनेक जीव हों।
अस्थिर—जिस कर्म के उदय से शरीर में धातु-उपधातु अपने स्थान में स्थिर न रहें। किंचित् उपवास आदि से शरीर अस्वस्थ हो जावे।
अशुभ—जिस कर्म के उदय से शरीर के अवयव सुंदर न हों।
दुर्भग—जिस कर्म के उदय से रूपादि गुणों से युक्त होने पर भी दूसरे जीवों को अप्रीति होती है।
दु:स्वर—जिस कर्म के उदय से खराब स्वर हो।
अनादेय—जिस कर्म के उदय से शरीर में कांति नहीं हो।
अयशकीर्ति—जिस कर्म के उदय से लोक में निंदा हो। कदाचित् गुणों में भी दोषों का आरोप हो जावे।
गोत्र कर्म के भेद
गोत्र कर्म के २ भेद हैं—उच्च गोत्र और नीच गोत्र।
उच्चगोेत्र—जिसके उदय से जीव लोकमान्य उच्चकुल में जन्म लेवे, वह उच्च गोत्र है।
नीचगोत्र—जिसके उदय से जीव लोकनिंदा नीचकुल में जन्म लेवे, वह नीच गोत्र है।
अंतराय कर्म के भेद
अंतराय कर्म के ५ भेद हैं। दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय और वीर्यान्तराय।
१. दानांतराय—जिस कर्म के उदय से दान की इच्छा करता हुआ भी दान नहीं दे सके।
२. लाभांतराय—जिस कर्म के उदय से लाभ की इच्छा होते हुए भी लाभ की प्राप्ति न हो सके।
३. भोगांतराय—जिस कर्म के उदय से अन्नादि भोगरूप वस्तु को भोगना चाहता हुआ भी भोग न सके।
४. उपभोगांतराय—जिसके उदय से वस्त्रादि उपभोग्य वस्तु को उपभोग करने का इच्छुक भी उपभोग न कर सके।
५. वीर्यांतराय—जिस कर्म के उदय से अपनी शक्ति प्रगट करना चाहता हुए भी प्रगट न कर सके, सामथ्र्यहीन, कायर, अनुत्साहित ही रहे। इस प्रकार १४८ प्रकृतियों का वर्णन हुआ। इन कर्मों के पिंड प्रकृति और अपिंड प्रकृति रूप से भी दो भेद हो जाते हैं—
पिंड प्रकृतियाँ १४ हैं—१. गति, २. जाति, ३. शरीर, ४. बंधन, ५. संघात, ६. संस्थान, ७. अंगोपांग, ८. संहनन, ९. वर्ण, १०. गंध ११. रस, १२. स्पर्श, १३. आनुपूर्वी, १४. विहायोगति।
इनके भेद ४+५+५+५+५+६+३+६+ ५+२+५+८+४+२·६५ होते हैं।
अपिंड प्रकृतियाँ २८ हैं— १. अगुरुलघु, २. उपघात, ३. परघात, ४. उच्छ्वास, ५. आतप, ६. उद्यात, ७. त्रस, ८. बादर, ९. पर्याप्त, १०. प्रत्येक शरीर, ११. स्थिर, १२. शुभ, १३. सुभग, १४. सुस्वर, १५. आदेय, १६. यशस्कीर्ति, १७. निर्माण, १८. तीर्थंकर, १९. स्थावर, २०. सूक्ष्म, २१. अपर्याप्त, २२. साधारण २३. अस्थिर, २४. अशुभ, २५. दुर्भग, २६. दुस्वर, २७. अनादेय और २८. अयशस्कीर्ति। उपर्युक्त पिंड प्रकृति १४ और पिंड प्रकृति २८ मिलाकर नाम कर्म की प्रकृतियाँ ४२ होती हैं। इन्हीं में पिंड प्रकृतियाँ के भेद करके गिनने से ६५+२८·९३ तिरानवे प्रकृतियाँ नाम कर्म की होती हैं।
आगे इन्हीं प्रकृतियों में समूह के वाचक शब्दों से किन-किन को लेना, सो खुलासा करते हैं— त्रसबारस कहने से त्रस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक शरीर, स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, यशस्कीर्ति, निर्माण और तीर्थंकर ये १२ प्रकृतियाँ लेना। त्रसदस कहने से निर्माण और तीर्थंकर छोड़ देना। त्रसचतुष्क कहने से त्रस, बादर, पर्याप्त और प्रत्येक शरीर लेना। स्थावरदसक कहने से स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याप्त, साधारण, अस्थिर, अशुभ, दुर्भग, दुस्वर, अनादेय और अयशकीर्ति लेना। स्थावरचतुष्क कहने से स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारण ये चार लेना। अगुरुलघुषट्क कहने से अगुरुलघु, उपघात, परघात, उच्छ्वास, आतप और उद्योत लेना। अगुरुलघुचतुष्क कहने से अगुरुलघु, उपघात, परघात और उच्छ्वास लेना। जातिचतुष्क कहने से एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय और चतुरिन्द्रिय ये चार जाति लेना। वैक्रियकअष्टक कहने से वैक्रियिकशरीर, वैक्रियिक अंगोपांग, देवगति, देवगत्यानुपूर्वी, देवायु, नरकगति, नरकगत्यानुपूर्वी और नरकायु ऐसी आठ प्रकृतियाँ लेना। वैक्रियकषष्क से दोनों आयु छोड़कर छह प्रकृतियाँ लेना। नरकचतुष्क से नरकगति, नरकगत्यानुपूर्वी, वैक्रियकशरीर और वैक्रियक अंगोपांग लेना। देवचतुष्क से देवगति, देवगत्यानुपूर्वी, वैक्रियकशरीर और वैक्रियक अंगोपांग लेना। वर्णचतुष्क से वर्ण, रस, गंध और स्पर्श ये चार लेना। निद्रापंचक से स्त्यानगृद्धि, निद्रानिद्रा, प्रचलाप्रचला, निद्रा और प्रचला ये पाँच लेना। स्त्यानत्रिक से प्रारंभ की तीन निद्रायें लेना। तिर्यकचतुष्क से तिर्यंचगति, तिर्यंचगत्यानुपूर्वी, औदारिकशरीर और औदारिकअंगोपांग लेना। नरचतुष्क से मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, औदारिक शरीर और औदारिक अंगोपांग लेना। त्रसत्रिक से त्रस, बादर पर्याप्त और त्रसत्रिक युगल से त्रस, बादर, पर्याप्त, स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याप्त ऐसी छह प्रकृतियाँ लेना। सुभगचतुष्क से सुभग, सुस्वर, आदेश और यशस्कीर्ति लेना और सुभगचुतुष्क युगल से इनके युगल से सुभग, दुर्भग, सुस्वर, दु:स्वर, आदेय, अनादेय, यशकीर्ति और अयशकीर्ति ये आठ प्रकृतियाँ लेना। इसी प्रकार से और भी ‘समूहवाची’ नाम समझ लेना चाहिए।
दर्शन मोहनीय के तीन भेद कैसे हुये?
जंतेण कोद्दवं वा पढमुवसमसम्मभावजंतेण।
मिच्छं दव्वं तु तिधा असंख्यगुणहीणदव्वकमा।।११।।
यन्त्रेण कोद्रवं वा प्रथमोपशमसमक्त्वभावयन्त्रेणे।
मिथ्यात्वं द्रव्यं तु विधा असंख्यगुणहीनद्रव्यक्रमात्।।११।।
अर्थ—यन्त्र अर्थात् घरटी-चक्की से दले हुये कोदों की तरह प्रथमो-पशमसम्क्त्वपरिणामरूप यंत्र से मिथ्यात्वरूपी कर्मद्रव्य द्रव्यप्रमाण में क्रम से असंख्यातगुणा असंख्यातगुणा कम होकर तीन प्रकार का हो जाता है।
भावार्थ—जैसे कोदों-धान्यविशेष दलने पर तंदुल कण और भूसी, ऐसे तीन रूप हो जाते हैं, उसी तरह मिथ्यात्वरूप कर्मद्रव्य भी उपशम-सम्यवत्वरूपी यंत्र के द्वारा मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व और सम्यक्त्व इन तीन स्वरूप परिणमन करता है। इस प्रकार एक मिथ्यात्वरूप दर्शनमोहनीय कर्म के ही तीन भेद कहे हैं।
शरीर में अंगोपांग कौन-कौन हैं?
णलया बाहू य तहा णियंबपुट्ठी उरी य सीसो य।
अट्ठेव दु अंगाइं देहे सेसा उवंगाइं।।२।।
नलकी बाहू च तथा नितम्बपृष्ठे उरश्च शीर्षं च।
अष्टैव तु अंगानि देहे शेषाणि उपांगानि।।१२।।
अर्थ—दो पैर, दो हाथ, नितम्ब-कमर के पीछे का भाग, पीठ, हृदय और मस्तक ये आठ शरीर में अंग हैं और दूसरे सब नेत्र कान वगैर: उपांग कहे जाते हैं।
आतप और उद्योत का लक्षण
मूलण्हपहा अग्गी आदावो होदि उण्हसहियपहा।
आइच्चे तेरिच्छे उण्हूणपहा हु उज्जोओ।।१३।।
मूलोष्णप्रभा: अग्नि: आतापो भवति उष्णसहितप्रभ:।
आदित्ये तिरश्चि उष्णोनप्रभा हि उद्योत:।।१३।।
अर्थ—आग के मूल और प्रभा दोनों ही उष्ण रहते हैं। इस कारण उसके स्पर्शनामकर्म के भेद उष्णस्पर्शनामकर्म का उदय जानना और जिसकी केवल प्रभा (किरणों का फैलाव) ही उष्ण हो उसको आताप कहते हैं। इस आतपनामकर्म का उदय सूर्य के बिम्ब (विमान) में उत्पन्न हुये बादरपर्याप्त पृथ्वीकरण के तिर्यंच जीवों के समझना तथ जिसकी प्रभा भी उष्णता रहित हो उसको नियम से उद्योत जानना।
बंध प्रकृतियाँ कितनी हैं?
पंच णव दोण्णि छव्वीसमवि य चउरी कमेण सत्तट्ठी।
दोण्णि य पंच य भणिया एदाओ बंधपयडीओ।।१४।।
पंच नव द्वौ षड्विंशतिरपि च चतस्र: क्रमेण सप्तषष्टि:।
द्वौ च पंच च भणिता एता बंधप्रकृतय:।।१४।।
अर्थ—ज्ञानावरण की ५, दर्शनावरण की ९, वेदनीय की २, मोहनीय की २६, आयुकर्म की ४, नामकर्म की ६७, गोत्रकर्म की २, अंतरायकर्म की ५ ये सब बंध होेने योग्य प्रकृतियाँ हैं। क्योंकि मोहनीय में सम्यग्मिथ्यात्व और सम्यक्त्व प्रकृति बंध में नहीं हैं और नाम कर्म में पहले गाथा में १०+१६·२६ प्रकृतियाँ अभेद विवक्षा से बंध अवस्था में नहीं हैं। सो ९३ में से २६ कम करने पर (९३-२६·६७) ६७ बाकी रह जाती हैं। इस प्रकार बंध योग्य प्रकृतियौं १२० हैं।
उदययोग्य प्रकृतियाँ
पंच णव दोण्णि अट्ठावीसं चउरो कमेण सत्तट्ठी।
दोण्णि य पंच य भणिया एदाओ उदयपयडीओ।।१५।।
पंच नव द्वौ अष्टाविंशति: चतस्र: क्रमेण सप्तषष्टि:।
द्वौ च पंच च भणिता एता उदयप्रकृतय:।।१५।।
अर्थ—पाँच, नौ, दो, अट्ठाईस, चार, सड़सठ, दो और पाँच ये सब उदय प्रकृतियाँ हैं। मोहनीय की पहली छब्बीस प्रकृतियों में सम्यग्मिथ्यात्व और सम्यक्त्व प्रकृति ये दो भी उदय अवस्था में शामिल करने से अट्ठाईस प्रकृतियाँ हो जाती हैं। इस प्रकार कुल १२२ उदय प्रकृतियाँ है।
सत्तायोग्य प्रकृतियाँ
पंच णव दोण्णि अट्ठावीसं चउरो कमेण सत्तट्ठी।
दोण्णि य पंच य भणिया एदाओ सत्तपयडीओ।।१६।।
पंच नव द्वौ अष्टाविंशति: चतस्र: क्रमेण त्रिनवति:। द्वौ च पंच च भणिता एता: सत्त्वप्रकृतय:।।१६।।
अर्थ—पाँच, नौ, दो, अट्ठाईस, चार, तिरानवै, दो और पाँच इस तरह सब १४८ सत्तारूप (मौजूद रहने योग्य) प्रकृतियाँ कहीं हैं।
सर्वघाती प्रकृतियाँ
केवलणाणावरणं दंसणछक्कं कसायबारसयं।
मिच्छं च सव्वघादी सम्मामिच्छं अबंधह्मि।।१७।।
केवलज्ञानावरण दर्शनषट्कं कषायद्वादशकम्।
मिथ्यात्वं च सर्वघातीनि सम्यग्मिथ्यात्वमबन्धे।।१७।।
अर्थ—केवलज्ञानावरण १, केवलदर्शनावरण और पाँच निंद्रा इस प्रकार दर्शनावरण के छ: भेद तथा अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, क्रोध मान माया लोभ ये बारह कषाय और मिथ्यात्व मोहनीय, सब मिलकर २० प्रकृतियाँ सर्वघाती हैं तथा सम्यग्मिथ्यात्व प्रकृति भी बंधरहित अवस्था में अर्थात् उदय और सत्ता अवस्था में सर्वघाती हैं। परन्तु यह सर्वघाती जुदी ही जाति को है।=
देशघाती प्रकृतियाँ
णाणावरणचउक्कं तिदंसणं सम्मगं च संजलणं।
णव णोकसाय विग्घं छव्वीसा देसघादीओ।।१८।।
ज्ञानावरणचतुष्कं त्रिदर्शनं सम्यक्त्वं च संज्वलनम्।
नव नोकषाया विघ्नं षड्विंशति: देशघातीनि।।१८।।
अर्थ—ज्ञानावरण के चार भेद (केवलज्ञानावरण को छोड़कर), दर्शनावरण के तीन भेद (उक्त छ: भेदों के सिवाय), सम्यक्त्वप्रकृति, संज्वलन-क्रोधदि चार, हास्यादि नोकषाय नव और अंतराय के पाँच भेद, इस तरह छब्बीस देशघाती कर्म हैं। क्योंकि इनके उदय होने पर भी जीव का गुण प्रगट रहता है।
प्रशस्त प्रकृतियाँ’
सादं तिण्णेवाऊ उच्चं णरसुरदुगं च पंचिंदी।
देहा बंधणसंघादंगोवंगाइं वण्णचओ।।१९।।
सातं त्रीण्येवायूं षि उच्चं नरसुरद्विकं च पंचेन्द्रियम्।
देहा बंधनसंघातांगोपांगानि वर्णचतुष्कम्।।१९।।
समचउरवज्जरिसहं उवघादूणगुरुछक्क सग्गमणं।
तसबारसट्ठी बादालमभेददो सत्था।।२०।।
समचतुरस्रवर्जर्षभमुपघा तोनागुरुषट्कं सद्गमनम्।
त्रसद्वादशाष्टपष्टिष: द्वाचत्वारिंशदभेदत: शम्ता:।।२०।।युग्मम्
अर्थ—सातावेदनीय १, तिर्यंच मनुष्य देवायु ३, उच्चगोत्र १, मनुष्यगति१, मनुष्यगत्यानुपूर्वी १ देवगति १, देगत्यानुपूर्वी १, पंचेन्द्रिय जाति १, शरीर ५, बंधन ५, संघात ५, अंगोपांग ३, शुभ वर्ण, गंध, रस, स्पर्श इन ४ के २० भेद, समचतुरस्रसंस्थान १, वङ्कार्षभनाराच संहनन १ और उपघात के बिना अगुरुलघु आदि तथा प्रशस्तविहायोगति १ और त्रस आदिक १२, इस प्रकार ६८ प्रकृतियाँ भेदविवक्षा से प्रशस्त (पुण्यरूप) कही हैं और अभेद विवक्षा से ४२ ही पुण्य प्रकृतियाँ हैं। क्योंकि पहिली रीति के अनुसार २६ कम हो जाती हैं।
अप्रशस्त प्रकृतियाँ’
घादी णीचमसादं णिरयाऊ णिरयतिरियदुग जादी।
संठाणसंहदीणं चदुपणपणगं च वण्णचओ।।२१।।
घातीनि नीचमसातं निरयायु: निरयतिर्यग्द्विकं जाति।
संस्थानसंहतीनां चतु: पंचपंचकं च वर्णचतुष्कम्।।२१।।
उवघादमसग्गमणं थावरदसयं च अप्पसत्था हु।
बंधुदयं पडि भेदे अडणउदि सयं दुचदुरसीदिदरे।।२२।।
उपघातमसद्गमनं स्थावरदशकं च अप्रशस्ता हि।
बन्धोदयं प्रति भेदे अष्टनवति: शतं द्वि-चतुरशीतिरितरे।।२२।। युग्मम्।।
अर्थ—चारों घातिया कर्मों की प्रकृतियाँ, नीचगोत्र, असाता वेदनीय नरकायु, नरकगति, नरकगत्यानुपूर्वी, तिर्यंचगति, तिर्यंचगत्यानुपूर्वी, एकेन्द्रियादि जाति ४, समचतुरस्र को छोड़कर पाँच संस्थान, पहले संहनन के सिवाय पाँच संहनन, अशुभ वर्ण, रस, गंध, स्पर्श ये चार अथवा इनके बीस भेद, उपघात, अप्रशस्त विहायोगति और स्थावर आदिक दस, ये अप्रशस्त (पाप) प्रकृतियाँ हैं। ये भेद विवक्षा से बंध रूप ९८ हैं और उदयरूप १०० हैं तथा अभेद विवक्षा से बंधयोग्य ८२ और उदयरूप ८४ प्रकृतियाँ हैं। क्योंकि वर्णदिक चार के सोलह भेद कम हो जाते हैं।
भावार्थ—घातिया कर्मों में सर्वघाती और देशघाती ये दो भेद हैं। अघातिया कर्मों में प्रशस्त और अप्रशस्त ये दो भेद हैं। इन्हें पुण्य और पाप प्रकृतियाँ भी कहते हैं।
अनंतानुबंधी आदि कषायों का कार्य
पढमादिया कसाया सम्मत्तं देससयलचारित्तं।
जहखादं घादंति य गुणणामा होंति सेसावि।।२३।।
प्रथमादिका: कषाया: सम्यक्त्वं देशसकलचारित्रम्।
यथाख्यातं घातयन्ति च गुणनामानो भवन्ति शेषा अपि।।२३।।
अर्थ—पहल अनंतानुबंधी आदिक अर्थात् अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संज्वलन ये चार कषाय, क्रम से सम्यक्त्व को, देशचारित्र को, सकलचारित्र को और यथाख्यातचारित्र को घातती हैं अर्थात् सम्यक्त्व वगैरह को प्रकट नहीं होने देतीं। इसी कारण इनके नाम भी वैसे ही हैं जैसे कि इनमें गुण हैं। इनके सिवाय दूसरी जो प्रकृतियाँ हैं वे भी सार्थक (नाम के अनुसार अर्थवाली) ही हैं।
इन कषायों का संस्कार काल
अंतोमुहुत्त पक्खं छम्मासं संखऽसंखणंतभवं।
संजलणमदियाणं वासणकालो दु णियमेण।।२४।।
अनंतर्मुहूर्त: पक्ष: षष्मासा: संख्यासंख्यानन्तभवा:।
संज्वलनाद्यानां वासनाकाल: तु नियमेन।।२४।।
अर्थ—संज्वलन वगैरह अर्थात् संज्वलन, प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान और अनंतानुबंधी इन चार कषायों की वासना का काल क्रम से अनंतर्मुहर्त, पक्ष (पंद्रह दिन) छ: महीना और संख्यात, असंख्यात तथा अनंत भव हैं, ऐसा निश्चय कर समझना। अभिप्राय यह है कि, किसी ने क्रोध किया, पीछे वह दूसरे काम में लग गया। वहाँ पर क्रोध का उदय तो नहीं है, परन्तु जिस पुरुष पर क्रोध किया था उस पर क्षमा भी नहीं हैं। इस प्रकार जो क्रोध का संस्कार चित्त में बैठा हुआ है उसी की वासना का काल यहाँ पर कहा गया है।
पुद्गलविपाकी प्रकृतियाँ
देहादी फासंता पण्णासा णिमिणतावजुगलं च।
थिरसुहपत्तेयदुगं अगुरुतियं पोग्गलविवाई।।२५।।
देहादय: स्पर्शान्ता: पंचाशत् निर्माणातापयुगलं च।
स्थिरशुभप्रत्येकद्विकमगुरुत्रयं पुद्गलविपाकिन्य:।।२५।।
अर्थ—पाँच शरीरों से लेकर स्पर्शनाम तक ५०, तथा निर्माण, आताप, उद्योत, तथा स्थिर शुभ और प्रत्येक का जोड़ा अर्थात् स्थिर, अस्थिर वगैरह छ: तथा अगुरुलघु आदिक तीन, ये सब ६२ प्रकृतियाँ पुद्गगलविपाकी हैं। अर्थात् इनके उदय का फल पुद्गल में ही होता है।
भवविपाकी, क्षेत्रविपाकी और जीवविपाकी प्रकृतियाँ
आऊणि भवविवाई खेत्तविवाई य आणुपुव्वीओ।
अट्ठत्तरि अवसेसा जीवविवाई मुणेयव्वा।।२६।।
आयूंषि भवविपाकीनि क्षेत्रविपाकीनि च आनुपूव्र्याणि।
अष्टसप्ततिरवशिष्ट जीवविपाकिन्य: मन्तव्या:।।२६।।
अर्थ—नरकादिक चार आयु भवविपाकी हैं। क्योंकि नरकादि पर्यायों के होने में ही इन प्रकृतियों का फल होता है। चार आनुपूर्वी प्रकृतियाँ क्षेत्रविपाकी हैं, क्योंकि परलोक को गमन करते हुए जीव के मार्ग में ही इनका उदय होता है। और बाकी जो अठत्तर प्रकृतियाँ हैं वे सब जीवविपाकी जानना। क्योंकि नारक आदि जीव की पर्यायों में ही इनका फल होता है। भावार्र्थ—ये सब प्रकृतियाँ पुद्गलविपाकी, भवविपाकी, क्षेत्रविपाकी और जीवविपाकी ऐसे चार भेदरूप हैं। जिनका फल शरीरादि पुद्गल में हो वे पुद्गगलविपाकी हैं। जिनका फल जीव को पर्यायों में हो वे जीवविपाकी हैं।
जीवविपाकी प्रकृतियाँ के नाम वेदणियगोदघादीणेकावण्णं तु णामपयडीणं।
सत्तावीसं चेदे अट्ठत्तरि जीवविवाई।।२७।।
वेदनीयगोत्रघातिनामेकपंचाशत्तु नामप्रकृतीनाम्।
सप्तविंशतिश्चता अष्टसप्तति: जीवविपाकिन्य:।।२७।।
अर्थ—वेदनीय की २, गोत्र की २, घातिया कर्मों की ४७, इस प्रकार ५१ और २७ नाम कर्म की इस तरह ५१+२७·७८ प्रकृतियाँ जीवविपाकी हैं।
सत्ताईस प्रकृतियों के नाम
तित्थयरं उस्सायं बादरपज्जत्तसुस्सरादेज्जं।
जसतसविहायसुभगदु चउगइ पणजाइ सगवीसं।।२८।।
तीर्थंकरमुच्छ्वासं बादरपर्याप्तसुस्वरादेयम्।
यशस्रसविहाय: सुभगद्वयं चतुर्गतय: पंचजातय: सप्तविंशति:।।२८।।
अर्थ—तीर्थंकर प्रकृति और उच्छवास प्रकृति, तथा बादर-पर्याप्त-सुस्वर-आदेय-यशकीर्ति-त्रस विहायोगति और सुभग इनका जोड़ा, अर्थात् बादर सूक्ष्म आदिक १६ और नरकादि चार गति, तथा एकेन्द्रियादि पाँच जात, इस प्रकार सत्ताईस नाम कर्म की प्रकृतियाँ जीवविपाकी जानना।
सत्ताईस प्रकृतियों के नाम गदि जादी उस्सासं विहायगदि तसतियाण जुगलं च।
सुभगादिचउज्जुगलं तित्थयरं चेदि सगवीसं।।२९।।
गति: जाति: उच्छ्वास विहायोगति: त्रसत्रयाणां युगलं च।
सुभगादिचतुर्युगलं तीर्थंकर चेति सप्तविंशति:।।२९।।
अर्थ—चार गति, पाँच जाति, उच्छ्वास, विहायोगति, त्रस-बादर-पर्याप्त इन तीन का जोड़ा (त्रस, स्थावर, वगैरह) एवं सुभग-सुस्वर-आदेय-यशकीर्ति इन चार का जोड़ा (सुभग, दुर्भग आदि) और एक तीर्थंकर प्रकृति, इस प्रकार क्रम से सत्ताईस की गिनती कही है।
कदलीघात मरण का लक्षण विसवेयणरत्तक्खयभयसत्थग्गहणसंकिलेसेहिं।
उस्सासाहारणं णिरोहदो छिज्जदे आऊ।।३०।।
विषवेदनारक्तक्षयभयशस्त्रघातसंक्लेशै:।
उच्छ्वासाहारयो: निरोधत: छिद्यते आयु:।।३०।।
अर्थ—विष भक्षण से अथवा विष वाले जीवों के काटने से, रक्तक्षय अर्थात् लोहू जिसमें सूखता जाता है ऐेसे रोग से अथवा धातुक्षय से, (उपचार से-लोहू के संबंध से यहाँ धातुक्षय भी समझना चाहिए) भयंकर वस्तु के दर्शन से या उसके बिना भी उत्पन्न हुए भय से, शस्त्रों (तलवार आदि हथियारों) के घात से, संक्लेश अर्थात् शरीर, वचन तथा मन द्वारा आत्मा को अधिक पीड़ा पहुँचाने वाली क्रिया होने से श्वासोच्छ्वास के रूक जाने से और आहार (खाना पीना) नहीं करने से इस जीव की आयु कम हो जाती है। इन कारणों से जो मरण हो अर्थात् शरीर छूटे उसे कदलीघात मरण या अकाल मृत्यु कहते हैं।
कर्म प्रकृतियों में चार निक्षेप
नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव के भेद से कर्म चार तरह का है। इनमें पहला भेद संज्ञारूप है। प्रकृति, पाप, कर्म और मल ये कर्म की संज्ञायें हैं। इन संज्ञाओं को ही नाम निक्षेप से कर्म कहते हैं। अब प्रकरणवश इन चार निक्षेपों का स्वरूप कहते हैं। क्योंकि इनका स्वरूप जाने बिना वस्तु का किस तरह व्यवहार होता है सो मालूम नहीं होता। जो युक्ति से सुयुक्तमार्ग होते हुए कार्य के वश से नाम, स्थापना, द्रव्य और भावरूप से पदार्थ का व्यवहार करना उसे निक्षेप कहते हैं वह नामादि भेद से चार प्रकार का है। जिस वस्तु में जो गुण नहीं है उनको उस नाम से कहना उसे नाम निक्षेप कहते हैं। जैसे किसी ने अपने लड़के की संज्ञा ऋषभदेव रक्खी। उसमें यद्यपि ऋषभदेव तीर्थंकर के गुण नहीं हैं, फिर भी केवल व्यवहार के लिए वह संज्ञा रक्खी है। अतएव उसको ऋषभदेव का नामनिक्षेप कहेंगे। स्थापना निक्षेप वह है जो कि साकार तथा निराकार (मनुष्यादि शरीर का आकार न हो और किसी आकार का पिंड हो) काठ, पत्थर चित्राम (मूर्ति) वगैरह में ‘‘ये वे ही ऋषभदेव तीर्थंकर हैं’’ इस प्रकार का अपने परिणामों से निवेश करना। इन दोनों में इतना ही भेद है कि, नाम के मूल पदार्थ की तरह सत्कार आदिक की प्रवृत्ति नहीं होती और स्थापना में मूल पदार्थ सरीखा ही आदर सत्कार किया जाता है। जो पदार्थ आगामी (होने वाली) पर्याय की योग्यता रखता हो उसको द्रव्य निक्षेप कहते हैं। जैसे-राजा के पुत्र को राजा कहना अथवा केवलज्ञान अवस्था को जो प्राप्त होने वाले हैं उन ऋषभदेव को गृहस्थादि अवस्था में तीर्थंकर कहना। वर्तमान पर्याय सहित वस्तु को भावनिक्षेप कहते हैं। जैसे-राज्य कार्य करते हुए को राजा कहना अथवा केवलज्ञान प्राप्त हो जाने पर ऋषभदेव को तीर्थंकर कहना। इस तरह चार निक्षेपों का स्वरूप कहा।
आगे स्थापनारूप कर्म को कहते हैं : सदृश अर्थात् कर्मसरीखा और असदृश अर्थात् जो कर्म के समान न हो ऐसे किसी भी द्रव्य में अपनी बुाqद्ध से ऐसी स्थापना करना कि जो जीव में कर्म मिले हुए हैं वे ही ये हैं इस अवधानपूर्वक किये गये निवेश को ही स्थापना कर्म कहते हैं।
आगे द्रव्य निक्षेपरूप कर्म का स्वरूप दिखाते हैं :—
द्रव्य निक्षेपरूप कर्म दो प्रकार का है—एक आगमद्रव्य कर्म, दूसरा नोआगमद्रव्य कर्म। इन दोनों में जो कर्म का स्वरूप कहने वाले शस्त्र का जानने वाला परन्तु वर्तमान काल में उस शास्त्र में उपयोग (ध्यान) नहीं रखने वाला जीव है वह पहला आगमद्रव्य कर्म हैं :—
अब दूसरा नोआगम द्रव्य कर्म कहते हैं :— दूसरा जो नोआगमद्रव्य कर्म है वह जायकशरीर १ भावि २ तद्व्यतिरिक्त के भेद से तीन प्रकार का है। उनमें से ज्ञायक शरीर कर्म (कर्मस्वरूप के जानने वाले जीव का शरीर) भूत-वर्तमान भावी, इस तरह तीन कालों की अपेक्षा तीन प्रकार का है। उन तीनों में से वर्तमान तथा भावी शरीर इन दोनों का अर्थ समझने में सुगम है, कठिन नहीं है। क्योंकि वर्तमान शरीर वह है जिसको कर रहा है और भावि शरीर वह है कि जिसको आगामी काल में धारण करेगा।
आगे भूत शरीर (जिसको छोड़कर आया है वह शरीर) के भेद दिखलाते हैं— भूत ज्ञायकशरीर, च्तुत १ च्यावित २ त्यक्त के भेद से तीन तरह का है। उनमें जो दूसरे किसी कारण के बिना केवल आयु के पूर्ण होने पर नष्ट हो जाए वह च्युत शरीर है। यह च्तुत शरीर कदलीघात (अकाल मृत्यु) और संन्यास इन दोनों अवस्थाओं से रहित होता है।
अब कदलीघात मरण का लक्षण कहते हैं :—विष भक्षण से अथवा विष वाले जीवों के काटने से, रक्तक्षय अर्थात् लोहू के संबंध से यहाँ धातुक्षय भी समझना चाहिए) भयंकर वस्तु के दर्शन से या उसके बिना भी उत्पन्न हुए भय से, शास्त्रों (तलवार आदि हथियारोें) के घात से, संक्लेश अर्थात् शरीर वचन तथा मन द्वारा आत्मा को अधिक पीड़ा पहुँचाने वाली क्रिया होेने से, श्वासोच्छ्वास के रूक जाने से और आहार (खाना-पीना) नहीं करने से इस जीव की आयु कम हो जाती है। इन कारणों से जो मरण हो अर्थात् शरीर छूटे उसे कदलीघात मरण अथवा अकाल मृत्यु कहते हैं।
आगे च्यावित और त्यक्त भूतज्ञायशरीर का लक्षण कहते हैं :— जो ज्ञायक का भूत शरीर कदलीघात सहित नष्ट हो गया हो परन्तु संन्यास विधि से रहित हो उसे च्यावित शरीर कहते हैं और जिसने कदलीघात सहित अथवा कदलीघात के बिना संन्यास रूप परिणामों से शरीर छोड़ दिया हो उसे त्यक्त कहते हैं।
अब त्यक्त शरीर (संन्यास सहित शरीर) के भेद दिखाते हैं :—त्यक्त शरीर—भक्तप्रतिज्ञा, इंगिनी और प्रायोग्य की विधि से तीन प्रकार का है। उनमें भक्तप्रतिज्ञा, जघन्य, मध्यम तथा उत्कृष्ट के भेद से तीन तरह का है।
आगे इन जघन्य आदि भेदों का काल कहते हैं :— भक्तप्रतिज्ञा अर्थात् भोजन की प्रतिज्ञा कर जो संन्यास मरण हो उसके काल का प्रमाण् जघन्य (कम से कम अंतर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट (ज्यादा से ज्यादा) बारह वर्ष प्रमाण है तथा मध्य के भेदों का काल एक-एक समय बढ़ता हुआ है। उसके अंतर्मुहूर्त से ऊपर और बारह वर्ष के भीतर जितने भेद हैं उतना प्रमाण समझना। इब इंगिनीमरण और प्रायोपगमन (प्रायोग्य विधि) मरण का लक्षण कहते हैं— अपने शरीर की टहल आप ही अपने अंगों से करे, किसी दूसरे से रोगादि का उपचार न करावे, ऐसे विधान से जो संन्यास धारण कर मरे उस मरण को इंगिनीमरण संन्यास कहते हैं और जिसमें अपना तथा दूसरे का भी उपचार (सेवा) न हो अर्थात् अपनी टहन न तो आप करे न दूसरे से ही करावे ऐसे संन्यास मरण को प्रायोपगमन कहते हैं।
आगे नोआगमद्रव्य कर्म का दूसरा भेद जो भावी है उसे कहते हैं :— जो कर्म के स्वरूप को कहने वाले शास्त्र का जानने वाला आगे होगा वह ज्ञायकशरीर भावी जीव है, ऐसा जिनेन्द्रदेव ने कहा है।
अब तीसरा भेद जो तद्व्यतिरिक्त है उसे कहते हैं:— तद्व्यतिरिक्त जो नोआगमद्रव्य कर्म का भेर है वह कर्म और नोकर्म के भेद से प्रकार है। ज्ञानावरणादि मूलप्रकृतिरूप अथवा उनके भेद मतिज्ञानावरणादि उत्तरप्रकृतिस्वरूप परिणमता हुआ जो कार्मणवर्गणा रूप पुद्गल द्रव्य वह कर्मतद्व्यतिरिक्त नोआगमद्रव्य कर्म है ऐसा नियम से जानना।
आगे नोकर्मतद्व्यतिरिक्त का स्वरूप और भावनिक्षेपरूप कर्म के भेद दिखाते हैं :— कर्मस्वरूप द्रव्य से भिन्न जो द्रव्य है वह नोकर्मतद्व्यतिरिक्त नोआगमद्रव्य कर्म है और भावनिक्षेपस्वरूप कर्म आगम तथा नोआगम के भेद से दो प्रकार का कहा है।
अब आगमभावनिक्षेपकर्म को स्वरूप कहते हैं :— जो जीव कर्मस्वरूप के कहने वाले आगम (शास्त्र) का जानने वाला और वर्तमान समय में उसी का चिन्तवन (विचार) रूप उपयोग सहित हो उसी जीव का नाम भाव आगम कर्म अथवा आगम भाव कर्म निश्चय से कहा जाता है।
आगे नोआगम भावनिक्षेपकर्म को कहते हैं :— कर्म के फल को भोगने वाला जो जीव वह नोआगम भाव कर्म है। इस तरह निक्षेपों की अपेक्षा सामान्य कर्म चार प्रकार का नियम से जानना। आगे कर्म के विशेष भेद जो मूलप्रकृति तथा उत्तर प्रकृतियाँ हैं उनमें नामादि चार निक्षेप के भेदों की विशेषता दिखाते हैं –कर्म की मूल प्रकृति ८ तथा उत्तर प्रकृति १४८ हैं। इन दोनों के जो नामादि चार निक्षेप हैं उनका स्वरूप सामान्यकर्म की तरह समझना, परन्तु इनती विशेषता है कि, जिस प्रकृति का जो नाम हो उसी के अनुसार १ नाम, २ स्थपना, ३ द्रव्य तथा ४ भाव निक्षेप होते हैं। =
अब कुछ और भी विशेषता दिखाते हैं :— मूल प्रकृति तथा उत्तर प्रकृतियों के नामादिक चार भेदों का स्वरूप समझना सरल है, परन्तु उनमें द्रव्य तथा भावनिक्षेप के भेदों में से नोकर्म तथा नोआगम भावकर्म का स्वरूप समझना कठिन है। अतएव उन दोनों को अर्थात् नोकर्म और नोआगम भावकर्म को मूल तथा उत्तर दोनों प्रकृतियों में घटित करते हैं और उसमें भी क्रमानुसार पहले नोकर्म को मूलप्रकृतियों में जोड़ते हैं — द्रव्यनिक्षेप कर्म का जो एक भेद ‘नोकर्मतद्व्यतिरिक्त’ है उसी को यहाँ नोकर्म शब्द से समझना और जिस प्रकृति के फल देने में जो निमित्तकारण हो (सहायता करता हो) वही उस प्रकृति का नोकर्म जानना। इस अभिप्राय को धारण करके ही यहाँ पर नोकर्मों को बताते हैं।
ज्ञानावरणादि ८ मूलप्रकृतियों के नोकर्म द्रव्यकर्म क्रम से, वस्तु के चारों तरफ लगा हुआ, १. कनात का कपड़ा, २. द्वारपाल, ३. शहद लपेटी तलवार की धार, ४. शराब, ५. अन्नादि आहार, ६. शरीर, ७. प्रशस्त-अप्रशस्त शरीर और ८. भंडारी, ये आठ जानना।
आगे उत्तरप्रकृतियों के नोकर्म कहते हैं :— वस्तु स्वरूप के ढकने वाले वस्त आदि पदार्थ मतिज्ञानावरण के नोकर्म द्रव्यकर्म हैं और इंद्रियों के रूपादिक विषय श्रुताज्ञान (शास्त्र ज्ञान व एक पदार्थ के ज्ञान) को नहीं होने देते इस कारण श्रुतज्ञानावरण कर्म के नोकर्म हैं अर्थात् जो विषयों में मग्न रहता है उसे शास्त्र के विचार करने में रूचि नहीं होती। इसलिए (शास्त्रज्ञान अथवा अपने आत्मा के स्वरूप का विचार करने में बाधा करने वाले होने से) इंद्रियों के विषयों को श्रुतज्ञानावरण का नोकर्म कहा है।
अब अवधिज्ञानावरण और मन:पर्ययज्ञानावरण के नोकर्म दिखाते हैं :— अवधिज्ञान और मन:पर्ययज्ञान इन दोनों के घात करने का निमित्त कारण जो संक्लेशरूप (खेदरूप) परिणाम है उसको करने वाली जो बाह्य वस्तु वह अवधिज्ञानावरण तथा मन:पर्ययज्ञानावरण का नोकर्म है और केवलज्ञानावरण का नोकर्म द्रव्यकर्म कोई वस्तु नहीं है। क्योंकि केवलज्ञान क्षायिक (कर्मों के क्षय से प्रगट) है। वहां संक्लेश परिणाम नहीं हो सकते। और इसीलिए उस केवलज्ञान का घात करने वाले संक्लेषरूप परिणामों को कोई भी वस्तु उत्पन्न नहीं कर सकती।
अब दर्शनावरण के भेदोें के नोकर्म कहते हैं :— पाँच निद्राओं को नोकर्म, भैंस का दही, लहसर, खलि इत्यादिक हैं। क्योंकि ये निद्रा की अधिकता करने वाली वस्तुयें हैं और चक्षु तथा अचक्षुदर्शन के रोकने वाले वस्त्र वगैरह द्रव्य चक्षुदर्शनावरण और अचक्षुदर्शनावरण कर्म के नोकर्म द्रव्य कर्म हैं। अवधिदर्शनावरण और केवलदर्शनावरण का नोकर्म अवधिज्ञानावरण तथा केवलज्ञानावरण के नोकर्म की तरह ही जानना और सातावेदनीय तथा असातावेदनीय का नोकर्म क्रम से अपने को रुचने वाली तथा अपने को नहीं रुचे ऐसी खाने-पीने वगैरह की वस्तु जानना।
अब मोहनीय कर्म के भेदों के नोकर्म दिखाते हैं :— १. जिन, २. जिनमंदिर, ३. जिनागम, ४. जिनागम के धारण करने वाले, ५. तप और ६. तप के धारक ये छह आयतन सम्यक्त्व प्रकृति के नोकर्म हैं और १. कुदेव, २. कुदेव का मंदिर, ३. कुशास्त्र, ४. कुशास्त्र के धारक, ५. खोटी तपस्या और ६. खोटी तपस्या के करने वाले ये ६ अनायतन मिथ्यात्व प्रकृति के नोकर्म हैं तथा आयनत और अनायतन दोनों मिल हुये सम्यग्मिथ्यात्व दर्शन मोहनीय के नोकर्म हैं, ऐसा निश्चय कर समझना। अनंतानुबंधीकषाय के नोकर्म मिथ्या आयतन अर्थात् कुदेव वगैरह दह अनायतन हैं और वाकी बची हुई बारह कषायों के नोकर्म देशचारित्र, सकलचारित्र तथा यथाख्यातचारित्र के घात में सहायता करने वाले काव्य, नाटक, कोक शास्त्र इत्यादि और पापी जार (कुशीली) पुरुषों की संगति करना इत्यादिक हैं, ऐसा नियम से जानना। स्त्रीवेद को नोकर्म स्त्री पर शरीर, पुरुषवेद का नोकर्म पुरुष का शरीर है और नपुंकसवेद का नोकर्म द्रव्यकर्म उक्त दानों का कुछ-कुछ मिश्रित चिन्ह रूप नपुंसक का शरीर है। हास्यकर्म के नोकर्म विदूषक व बहुरूपिया वगैरह हैं जो कि हँसी ठ्ठठा करने के पात्र हैं। रति कर्म का नोकर्म अच्छा गुणवान् पुत्र है, क्योेंकि गुणवान् पुत्र पर अधिक प्रीति होती है। अरति कर्म का नोकर्म द्रव्य इष्ट का (प्रियवस्तु का) वियोग होना और अनिष्ट अर्थात् अप्रियवस्तु का संयोग (प्राप्ति) होना है। शोक का नोकर्म द्रव्य सुपुत्र स्त्री वगैरह का मरना है और सिंह आदिक भय के करने वाले पदार्थ भय कर्म के नोकर्म द्रव्य हैं तथा निंदित वस्तु जुगुप्साकर्म की नोकर्म द्रव्य हैं।
अब आयुकर्म के भेदों के तथा नामकर्म के भेदों के नोकर्म कहते हैं :—अनिष्ट आहार अर्थात् नरक की विषरूप मिट्ठी आदि नरकायु का नोकर्म द्रव्य है और बाकी तिर्यंच आदि तीन आयुकर्मों का नोकर्म इंद्रियों को प्रिय लगे ऐसा अन्न-पानी वगैरह है और गतिनामकर्म का नोकर्म द्रव्य चार गतियों का क्षेत्र (स्थान) है। नरकादि चार गतियों का नोकर्म द्रव्य नियम से नरकादि गतियों का अपना-अपना क्षेत्र है और जातिकर्म का नोकर्म द्रव्येन्द्रिय रूप पुद्गल की रचना है। एकेन्द्रिय आदिक पाँच जातियों के नोकर्म अपनी-अपनी द्रव्येन्द्रियों हैं और शरीर नामकर्म का नोकर्म द्रव्य शरीर नामकर्म के उदय से उत्पन्न हुए अपने शरीर के स्कंध रूप पुद्गल जानना। औदारिक-वैक्रियक-आहारक-तैजस शरीर नामकर्म का नोकर्म द्रव्य अपने उदय से प्राप्त हुई शरीरवर्गणा हैं। क्योंकि उन वर्गणाओ से ही शरीर बना है और कामर्ण शरीर का नोकर्म द्रव्य विस्रसोपचयरूप (स्वभाव से कर्मरूप होने योग्य कार्मण वर्गणा) परमाणु हैं। शरीर बंधन नामकर्म से लेकर जितनी पुद्गल विपाकी प्रकृतियाँ हैं उनका और पहले कही हुई प्रकृतियों के सिवाय जीवविपाकी प्रकृतियों में से जितनी बाकी बची उनका नोकर्म शरीर ही है। क्योंकि उन प्रकृतियों से उत्पन्न हुये सुखादिरूप कार्य का कारण शरीर ही है। क्षेत्र विपाकी चार आनुपूर्वी प्रकृतियों को नोकर्म द्रव्य अपना-अपना क्षेत्र ही है, इतनी विशेष बात जाननी। स्थिर कर्म का नोकर्म अपने-अपने स्थान पर स्थिर रहने वाले रस रुधिर वगैरह और अस्थिर प्रकृति के नोकर्म अपने-अपने स्थान से चलायमान हुए रस रुधिर आदिक हैं। शुभ प्रकृति के नोकर्म द्रव्य शरीर के शुभ अवयव हैं तथा अशुभ प्रकृति के नोकर्म द्रव्य शरीर के अशुभ (जो देखने में सुंदर न हों ऐसे) अवयव हैं। स्वर नामकर्म को नोकर्म सुस्वर-दु:स्वर रूप परिणमें पुद्गल परमाणु हैं।
अब गोत्र कर्म तथा अतंराय कर्म के भेदों के नोकर्म दिखाते हैं :— उच्च गोत्र का नोकर्म द्रव्य लोकपूजित कुल में उत्पन्न हुआ शरीर है और नीच गोत्र का नोकर्म लोकनिंदित कुल में प्राप्त हुआ शरीर है। दानादिक चार का अर्थात् १. दान, २. लाभ, ३. भोग और ४. उपभोगान्तराय कर्म का नोकर्म द्रव्य दानादिक में विघ्न कराने वाले पर्वत, नदी, पुरुष,स्त्री वगैरह जानने। वीर्यांतराय कर्म के नोकर्म रूखा आहार वगैरह बल के नाश करने वाले पदार्थ हैं। इस प्रकार उत्तर प्रकृतियों के नोकर्म द्रव्यकर्म का स्परूप कहा।
अब नोआगमभावकर्म को कहते हैं :— जिस-जिस कर्म का जो-जो फल को भोगते हुए जीव को ही उस-उस कर्म का नोआगमभाव कर्म जानना। पुद्गलविपाकी प्रकृतियों को नाआगमभावकर्म नहीं होता क्योंकि उनका उदय होने पर भी जीवविपाकी प्रकृतियों की सहायता के बिना साताजन्य सुखादिक की उत्पत्ति नहीं हो सकती। इस तरह सामान्य कर्म की मूल उत्तर दोनों प्रकृतियों के चार निक्षेप कहे हैं।
