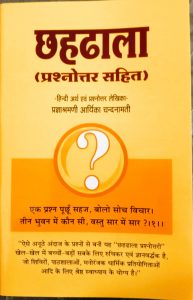प्रथम ढाल
मंगलाचरण
-सोरठा-
तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता।
शिवस्वरूप शिवकार, नमहुँ त्रियोग सम्हारिवैं।।
अर्थ – त्रिभुवन अर्थात् तीन लोकों में सर्वोत्तम वस्तु है, वीतराग विज्ञानता अर्थात् रागद्वेष रहित केवलज्ञान। यही केवलज्ञान आनन्दस्वरूप है और मोक्ष देने वाला है अत: मैं मन-वचन-काय को संभालकर केवलज्ञान को नमस्कार करता हूँ।
विशेषार्थ – अनन्तानन्त आकाश द्रव्य के बहुमध्य भाग के जितने प्रदेशों में छह द्रव्यों का आवास है, उसे लोक कहते हैं। ऊर्ध्व, मध्य और अधोलोक के भेद से यह तीन प्रकार का है और तीन वातवलयों के आधार पर अवस्थित है। रागयुक्त जीवद्रव्य की शुद्धावस्था अर्थात् अठारह दोषों से रहित अवस्था होना वीतरागता है और विशिष्टज्ञान अर्थात् केवलज्ञान का नाम विज्ञानता है। (चौपाई छन्द) ग्रन्थ रचना का उद्देश्य व जीव की चाह जे त्रिभुवन में जीव अनन्त, सुख चाहें दु:खतैं भयवन्त। तीनों लोकों में जो अनन्त जीव हैं, वे सभी सुख चाहते हैं और दु:ख से डरते हैंं इसलिए आचार्य कृपा करके उन जीवों को दु:ख हरने वाली और सुख को देने वाली शिक्षा प्रदान करते हैं।
विशेषार्थ – ज्ञान, दर्शन अर्थात् जानने-देखने की शक्ति से युक्त द्रव्य को जीव कहते हैं। जो मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान एवं मन:पर्ययज्ञान का विषय न हो, मात्र केवलज्ञान का विषय हो, उसे अनन्त कहते हैं अथवा जिसमें घंटे की ध्वनि सदृश व्यय निरन्तर होता रहे, आय कभी न हो, फिर भी राशि समाप्त न हो, उसे अनन्त कहते हैं। ‘‘संसार के सभी प्राणी सुखी रहें’’ आत्मा के इस सुकोमल भाव का नाम करुणा है। सम्यग्दृष्टि जीव का यह सुकोमल परिणाम शुभ राग है किन्तु मोह का कार्य कदापि नहीं है।
संसार भ्रमण का कारण ताहि सुनो भवि मन थिर आन, जो चाहो अपनो कल्यान।
मोह-महामद पियो अनादि, भूल आपको भरमत वादि।।२।।
अर्थ – हे भव्यजीवों! यदि तुम अपनी भलाई या सुख चाहते हो तो उस कल्याणकारी उपदेश को स्थिर मन से सुनो। यह जीव अनादिकाल से मोहरूपी मदिरा-शराब पीकर अपने स्वरूप को भूलकर व्यर्थ में चारों गतियों में भ्रमण कर रहा है।
विशेषार्थ – रत्नत्रय की प्राप्ति की योग्यता युक्त जीव को भव्य कहते हैं। परपदार्थों में अपनत्व बुद्धि होना, मोह कहलाता है। जिसकी आदि अर्थात् प्रारंभ न हो, उसे अनादि कहते हैं। कृति की प्रामाणिकता और निगोद के दु:ख तास भ्रमण की है बहु कथा, पै कछु कहूँ कही मुनि यथा।
काल अनन्त निगोद मँझार, बीत्यो एकेन्द्री-तन धार।।३।।
निगोद के दु:ख व निगोद से निकलकर प्राप्त पर्यायें
एक स्वाँस में अठ-दस बार, जन्म्यो मरयो भरयो दु:ख भार।
निकसि भूमि जल पावक भयो, पवन प्रत्येक वनस्पति थयो।।४।।
त्रस पर्याय की दुर्लभता और तिर्यंचगति के दु:ख
लट पिपील अलि आदि शरीर, धर-धर मर्यो सही बहुपीर।।५।।
तिर्यंच गति में असैनी और सैनी के दु:ख
सिंहादिक सैनी ह्वै व्रूर, निबल पशू हति खाये भूर।।६।।
पंचेन्द्रिय पशुओं के निर्बलता आदि अन्य दु:ख
छेदन भेदन भूख पियास, भार वहन हिम आतप त्रास।।७।।
तिर्यंचगति में दु:खों की अधिकता और नरकगति की प्राप्ति का कारण
अति संक्लेश-भावतैं मर्यो, घोर श्वभ्र-सागर में पर्यो।।८।।
नरक की भूमि स्पर्श और नदीजन्य दु:ख
तहाँ राध-शोणित-वाहिनी, कृमि-कुल-कलित-देह दाहिनी।।९।।
नरक में सेमर वृक्ष, सर्दी और गर्मी के दु:ख
मेरु समान लोह गलि जाय, ऐसी शीत उष्णता थाय।।१०।।
पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे तथा पाँचवें नरक के दूसरे-तीसरे भाग में गर्मी है और पाँचवें नरक के प्रथम-द्वितीय-तृतीय भाग में सर्दी है एवं छठवें तथा सातवें नरक में भयंकर सर्दी है।
नरक में अन्य नारकियों व असुरकुमारों द्वारा उदीरित और प्यास के दु:ख
सिन्धु-नीरतैं प्यास न जाय, तो पण एक न बूंद लहाय।।११।।
नरक की भूख, आयु और मनुष्यगति प्राप्ति का वर्णन
ये दु:ख बहु सागर लौं सहै, करम जोग तैं नरगति लहै।।१२।।
मनुष्यगति में गर्भवास और प्रसवजन्य दु:ख
निकसत जे दु:ख पाये घोर, तिनको कहत न आवै ओर।।१३।।
मनुष्यगति में बाल्यावस्था, जवानी व वृद्धावस्था के दु:ख
अर्धमृतक सम बूढ़ापनो, कैसे रूप लखै आपनो।।१४।।
देवगति में भवनत्रिक के दु:ख
विषय-चाह-दावानल दह्यौ, मरत विलाप करत दु:ख सह्यो।।१५।।
अर्थ – कभी इस जीव ने अकाम निर्जरा की, तो मंद कषाय के परिणाम स्वरूप मरकर भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिषी देवों में से किसी एक का शरीर धारण किया परन्तु वहाँ भी हर समय इन्द्रियों के विषयों की चाहरूपी भयानक अग्नि में जलता रहा और मरते समय रो-रोकर दारुण दु:ख सहन किया।
विशेषार्थ – अनायास (बिना इच्छा के) भूख, प्यास, वेदना, रोग एवं आपत्ति-विपत्ति आ जाने पर समता परिणामों से सहन कर लेना अर्थात् मन्दकषाय द्वारा फल देकर कर्मों का स्वयं झड़ जाना अकाम निर्जरा कहलाती है। भवनवासी, व्यन्तरवासी और ज्योतिषी देवों को भवनत्रिक कहते हैं।
देवगति में वैमानिक देवों के दु:ख
तहँ ते चय थावर-तन धरै, यों परिवर्तन पूरे करै।।१६।।