मिथ्यादृष्टि के ध्यानसिद्धि संभव नहीं है
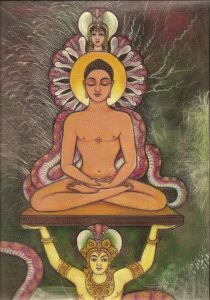
श्री शुभचन्द्राचार्य ने ‘‘ज्ञानार्णव’’ नामक ग्रंथ में ध्यान का प्रमुखता से विचेन किया है। ज्ञान + अर्णव: अर्थात् ज्ञान का समुद्र। कहने का तात्पर्य यह है कि ध्यान के द्वारा ही ज्ञानरूपी समुद्र में गोता लगाया जा सकता है। प्रस्तुत ग्रंथ में ध्यान का वर्णन करते—करते आचार्यश्री कहते हैं कि आकाश में पुष्प और गधे के सींग कदाचित् हो सकते हैं परन्तु गृहस्थों को किसी भी स्थिति में शुक्ल ध्यान की सिद्धि नहीं हो सकती है। इसी ग्रंथ में कहा गया है कि मिथ्यादृष्टियों को भी ध्यान की सिद्धि कदापि नहीं हो सकती है। यथा—
दुर्दशामपि न ध्यान—सिद्धि: स्वप्नेऽपि जायते।
गृण्हतां दृष्टिवैकल्याद् वस्तुजातं यदृच्छया।।१८।।
अर्थात् दृष्टि की विकलता से वस्तुसमूह को अपनी इच्छानुसार ग्रहण करने वाले मिथ्यादृष्टियों के ध्यान की सिद्धि स्वप्न में भी नहीं होती है। अब यहाँ यह प्रश्न उठता है कि यदि मिथ्यादृष्टि गृहस्थावस्था का त्याग करके मुनि हो जाए तो क्या उसको ध्यान की सिद्धि हो सकती है ? इसके समाधान में आचार्यश्री कहते हैं कि मिथ्यादृष्टि को गृहस्थावस्था छोड़कर मुनि होने पर भी ध्यान की सिद्धि नहीं होती क्योंकि वे पूर्वापर विरुद्ध पदार्थों के स्वरूप में समीचीनता (सत्यता) मानने वाले हैं अर्थात् अन्य मत में सत्ता—यथार्थता नहीं है।
सब ही अन्यमती पाखण्डी सर्वथा एकान्तता से दूषित हैं जबकि वस्तु का स्वरूप अनेकान्तात्मक है अत: वे उनके यथार्थ स्वरूप को जानने में असमर्थ हैं स्याद्वाद के जाने बिना विरोध आदि दूषणों का परिहार उनसे नहीं किया जा सकता है क्योंकि मिथ्यादृष्टियों में कोई—कोई तो वस्तु को नित्य ही मानते हैं और कोई—कोई अनित्य ही सिद्ध करते हैं परन्तु यह जगत् नित्य—अनित्य दोनों स्वरूप है।
भावार्थ यह है कि सांख्य, नैयायिक, वेदान्त और मीमांसक मत वाले तो आत्मा को सर्वथा नित्य तथा जगत् को अविद्यादिक के विलास से विभ्रमरूप अनित्य मानते हैं और कहते हैं कि ‘‘आत्मा को अनित्य मानने से आत्मा का नाश होकर नास्तिकता का मत आता है और नित्यानित्य दोनों स्वरूप मानने से विरोधादिक दूषण आते हैं।’’
इस प्रकार अपनी कपोल कल्पना करके आत्मा को सर्वथा नित्य ही मानते हैं और बौद्धमती वस्तु को क्षणिक तथा अनित्यस्वरूप मानते हैं, नित्य मानने को अविद्या कहते हैं और नित्यानित्य मानने में विरोधादि दूषण कहते हैं किन्तु सबको जानना चाहिए कि वास्तव में वस्तु का स्वरूप जो नित्य—अनित्य रूप है, वह स्याद्वाद से ही सिद्ध होता है उसमें विरोध आदि कोई दूषण नहीं आते।
खेद है कि ऐसा स्वरूप अन्यमती समझते नहीं हैं और अपनी बुद्धि से कल्पना करके जिस तिस प्रकार सिद्धि करके सन्तुष्ट हो जाते हैं परन्तु वास्तव में विचार किया जावे तो उनके ध्याता, ध्यान, ध्येयादि की सिद्धि नहीं होती इसलिए उनका कहना सब प्रलापमात्र जानना चाहिए। सो ही आगे कहते हैं—
वस्तुतत्त्वापरिज्ञानात्वकं ध्येयं क्व च भावना।
ध्यानाभ्यासस्ततस्तेषां प्रयासायैवकेवलम्।।२२।।
अर्थात् उक्त मिथ्यादृष्टि अन्य मतावलम्बियों के यथार्थ स्वरूप के ज्ञानरूप अभाव से ध्येय कहाँ और भावना कहाँ ? इस कारण उनका ध्यान करना केवल प्रयासमात्र ही है।
जैसा कि हम तत्त्वार्थसूत्र का प्रथम सूत्र पढ़ते हैं—‘‘सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्ग:’’ अर्थात् सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र इन तीनों की एकता ही मोक्ष का मार्ग है इसी बात की पुष्टि करते हुए श्री शुभचन्द्राचार्य आगे कहते हैं— ज्ञानवादी मात्र ज्ञान से इष्टसिद्धि मानते हैं, कई वादी मात्र दर्शन से और कोई—कोई मात्र चारित्र से ही इष्ट की सिद्धि मानते हें और कितने ही वादी अपने सिद्धान्त के गर्व से संसार की सन्तति के नाश की परिपाटी में विज्ञान, दर्शन और चारित्र इन तीनों में से दो—दो को इष्ट कहते हैं अर्थात् कोई तो दर्शन और ज्ञान को ही मानते हैं, किसी ने दर्शन और चारित्र ही माना है और कोई—कोई ज्ञान और चारित्र को ही मानते हैं इन वादियों में तीन वादियों ने तो एक–एक को नष्ट किया और तीन वादियों ने दो—दो को नष्ट किया। इनके अतिरिक्त एक को ये तीनों ही नहीं रुचते, इस प्रकार मिथ्यामतियों के सात भेद हुए।
कहने का तात्पर्य यह है कि जिसने ज्ञान और दर्शन दो को ही मोक्ष का मार्ग माना उसने तो एक चारित्र को नष्ट किया, जिसने ज्ञान और चारित्र माना उसने एक दर्शन को नष्ट किया और जिसने दर्शन और चारित्र ये दो माने उसने एक ज्ञान को नष्ट किया। इसी प्रकार जिसने एक दर्शन को ही माना उसने ज्ञान चारित्र को नष्ट किया और जिसने एक ज्ञान को ही माना उसने दर्शन और चारित्र को नष्ट किया और जिसने एक चारित्र को ही माना उसने दर्शन और ज्ञान पर पानी फैर दिया।
इस प्रकार छह पक्ष तो ये हुए और एक नास्तिक का पक्ष है जो इन तीनों में से किसी को नहीं मानता है, इस प्रकार सात पक्ष मिथ्यादृष्टियों के हैं। इसी बात को आचार्यश्री अन्य ग्रन्थ के एक उदाहरण द्वारा समझाते हैं—
‘‘ज्ञानहीने क्रियापुंसि परं नारभते फलम्।
तरोश्छायेव किं लभ्या फलश्रीर्नष्टदृष्टिभि:।।१।।
ज्ञानं पङ्गौ क्रिया चान्धे नि:श्रद्धे नार्थकृद्द्वयम्।
ततो ज्ञानं क्रिया श्रद्धा त्रयं तत्पदकारणम्।।२।।
हतं ज्ञानं क्रियाशून्यं हता चाज्ञानिन: क्रिया।
धावन्नप्यन्धको नष्ट: पश्यन्नपि च पङ्गुक:।।३।।
अर्थ—
ज्ञानहीन पुरुष की क्रिया फलदायक नहीं होती। जिसकी दृष्टि नष्ट हो गई है वह अन्धा पुरुष चलते—चलते जिस प्रकार वृक्ष की छाया को प्राप्त होता है, उसी प्रकार क्या उसके फल को भी पा सकता है ? कदापि नहीं।।१।।
पंगु में तो वृक्ष के फल का देख लेना प्रयोजन को नहीं साधता और अंधे में फल जानकर तोड़ने रूप क्रिया प्रयोजन को नहीं साधती। श्रद्धारहित के ज्ञान और क्रिया दोनों ही (दवाई के समान) प्रयोजनसाधक नहीं हैं, इस कारण ज्ञान, क्रिया और श्रद्धा तीनों एकत्र होकर ही वांछित अर्थ की साधक होती हैं।।२।।
क्रियारहित तो ज्ञान नष्ट है और अज्ञानी की क्रिया नष्ट हुई। देखो, दौड़ता-दौड़ता तो अन्धा नष्ट हो गया और देखता-देखता पंगु नष्ट हुआ। भावार्थ—एक वन में आग लगी तब एक अंधे ने इधर-उधर दौड़ने की क्रिया तो की किन्तु दृष्टि के बिना आग में गिरकर जल गया और पंगु (लंगड़ा) किधर को आग है और किधर को रास्ता है, सब देखता तो है परन्तु दौड़ा नहीं गया इस कारण अग्नि में जलकर मर गया। इस कारण ज्ञान, श्रद्धा और क्रिया इनसे ही प्रयोजन की सिद्धि होती है।।३।।
